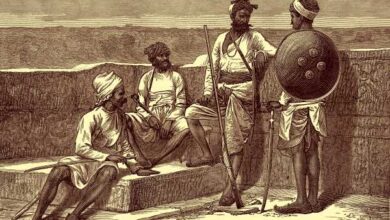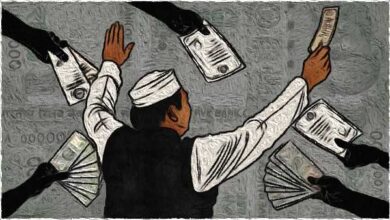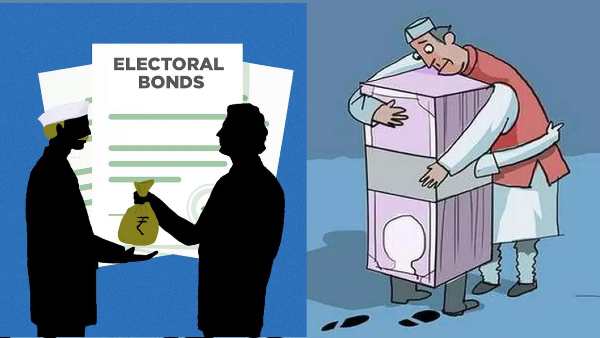यूट्यूब की शॉट फिल्मों के सन्दर्भ में
लैंडस्केप का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष, प्राकृतिक दृश्य, परिवेश विशेष को उसके विविध पहलुओं के साथ व्यापकता में चित्रित करना। स्त्री केन्द्रित यूट्यूब की इन शार्ट फिल्मों में स्त्री मन की आशाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओ उनके अतिसंवेदनशील मन के भीतर झांककर, समझने का प्रयास है। आभासी माने जाने वाली सोशल मीडिया की फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम यूट्यूब जैसे अति सक्रिय प्लेटफार्म पल-पल बदलती जिन्दगी को अपडेट करने के सशक्त पैमाने बनकर उभरे हैं। और इस आभासी दुनिया में सफलता का पैमाना लाइक्स, शेयर और कमेंट हैं। इसी सन्दर्भ में यूट्यूब की लघु शॉट फिल्मों का संसार अब मिलियन व्यूज़ को पार कर, अत्यंत व्यापकता की श्रेणी में पहुँच चुका है।
5-6 मिनट से लेकर 22-23 या अधिकतम आधे घंटे की इन स्त्री केन्द्रित लघु फिल्मों में गजब का गुरुत्वाकर्षण है। स्त्री मन का लैंडस्केप ये फ़िल्में चंद लम्हों में उनके स्वपन, संकल्पनाओं, आशाओं, निराशाओं, सुख-दुःख का अत्यंत खूबसूरती से चित्रांकन करती हैं, वास्तव में हमारी चेतना को झकझोरती हैं, संवेदनाओं को कुरेदती और आन्दोलित करती हैं और दर्शकों को अपने घरों की स्त्रियों के विषय में ही नहीं पुरुषों की मानसिकता पर पुनः सोचने को विवश करती हैं। जिसका प्रमाण है फिल्म के अन्त के कमेंट बॉक्स, जहाँ न केवल स्त्री अपितु पुरुष भी अपने अब तक के व्यवहार और मानसिकता पर ग्लानि प्रकट करते हैं। इन फिल्मों में चित्रित स्त्रियों की तुलना जब मैं नारी सशक्तिकरण आधारित विमर्शों पर करती हूँ तो लगता है कि दिन-प्रतिदिन सशक्त होती स्त्री की मुक्ति के प्रश्न अभी ज्यों के त्यों है। 

14 मिनट की फिल्म ‘जूस’ में स्त्री-पुरुष के कई पक्षों को एक साथ उजागर किया है। आरंभ ‘पार्टी’ पुरुषों की? घर की महिलाओं ने किचन का मोर्चा संभाला हुआ है और तभी एक टिपण्णी “यार एक बात बता तुझे परेशानी किससे है ई-मेल से या फीमेल से” (जोकि उसकी बॉस है) और एक ज़ोरदार ठहाका। पत्नियां रसोईघर में गर्मी से जूझते हुए काम कर रहीं है और बैठक के कूलर में पानी भी डाल रही है ताकि पति के मित्रों को शिकायत न हो जबकि पति रसोई के पंखे को ठीक करने की बात तक नहीं सुनता, एक महिला छोटी सी बच्ची को कहती है ‘भैया लोगों को खाना दो’…‘नौकरी तो छोड़नी ही पड़ेगी, कैसे कर पाओगी’…‘जरूरी नहीं कि हमने नौकरी छोड़ी तो ये भी वही करें’…‘जब अंकल लोग बातें करते हैं बीच में नहीं जाते, कभी हमें देखा है ऐसे जाते?
और इसी माहौल में ‘मंजू’ गिलास में जूस निकालती है कुर्सी उठाती है और कूलर के सामने बैठ जाती है। कुर्सी उठाना, बैठना इस बात का प्रतीक है कि पुरुष प्रधान समाज में वो अपना स्थान निर्धारित करना चाहती है जो उसे कभी दिया ही नहीं गया आज उसे स्वयं हासिल करना होगा। और जूस! जूस जीवन रस का प्रतीक है जिसका वो भी आनंद लेना चाहती है वो भी खुली हवा में चैन की स्वछंद सांस लेना चाहती है। उसका क्रोध, दुःख और लगभग धृष्ट लाल आंखे, फूलते नथुने स्पष्ट कह रहें है कि अपनी इस विजय पर वह बहुत खुश नहीं, क्योंकि यह धृष्टता न तो उसके संस्कारों में है और न ही व्यक्तित्व में लेकिन ‘इतना मत डराओ कि डर ही न लगे’ वाला भाव रोंगटे खड़े करने वाला है।
सात लाख व्यू तथा लगभग सात हजार लोगों के कमेंट वाली यह फिल्म, स्त्री की घुटन और बचैनी का दृश्य प्रस्तुत करती है और सोचने पर विवश करती है कि किस प्रकार हमारे समाज में बचपन से ही ‘भैया लोगो’ यानी पुरुषों की सेवा करने के लिए तैयार किया जाता है। सभी पुरुष ठहाके लगाते हुए, विश्व की प्रसिद्ध महिला हिलेरी क्लिंटन को भी तुच्छ प्रमाणित करने में लगे हैं। पुरुष समाज स्त्री की सफलता को कभी भी गम्भीरता से नहीं लेता मजाक बना कर रख देता है? और बैठक जहाँ सभी के पास कुर्सी (‘सत्ता’) है स्त्रियों का घर में एक ही स्थान है रसोईघर जहाँ वो खड़ी इंतजार कर रही है कि जाने कब बैठक से फरमाइश आये और वे दौड़ती हुई जाती है। पितृसत्तात्मक दुनिया की आधी आबादी के प्रति हमारा उदासीन समाज को इस लघु फिल्म के दृश्य बखूबी व्याख्यित करते है। लड़कियों को बचपन से ही तन, मन, मस्तिष्क से कमजोर मानकर पुरुष सेवा के उद्देश्य से तैयार किया जाता है इसलिए सामंजस्य, समझौता, मौन, सहनशीलता जैसे भाव महिमामंडित कर बोये जाते हैं जैसे पुरुषों की सुविधा हेतु कूलर में पानी डालना और स्वयं ख़राब पंखे से तालमेल बिठाना।
Every thing is fine नामक फ़िल्म परिवार में सामंजस्य, समझौता, मौन, सहनशीलता और तालमेल बिठाती ‘माँ’ की मार्मिक और तीक्ष्ण अभिव्यक्ति हमारे सामने रखती है कि असल में कुछ भी ठीक नही। बेटी के पूछने पर ‘किस चीज़ की कमी है? सब ठीक तो है?’ माँ आश्चर्यजनक रूप से निराश हो कहती है- ‘हाँ सब ठीक है!’ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बेटी माँ की आंखो में अधूरी आकांक्षाओं को नहीं देख पाती जो घर परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण में कहीं दबी रह गयी, जब बेटी से कहती कि मैं तो अकेले ही आने वाली थी तेरे पापा कहने लगे कि‘तुम अपना ध्यान नहीं रख पाओगी’ बेटी हँसती है कि ‘क्यों मैं नहीं रख सकती’ यही वह पल है जब संभवत: आज बेटी की स्वच्छंद जीवन शैली को देखकर प्रसन्न तो है किन्तु कहीं किसी कोने में अफ़सोस है कि‘वह तो इतना भी न पढ़ लिख पाई की चेक साइन कर पावे’ तिस पर पति का कटाक्ष कि‘पढ़ लिख कर कौन-सा तुम्हें पोथियाँ लिखनी थी’ मन मसोसकर रह जाती है।
मजाक के नाम पर पत्नियों का अपमान करना आम है, परिवार समाज में हास्य-व्यंग्य और मज़ाक का केंद्र बनाकर स्त्री को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बनी ही हुई है, चुटकुले इसका जीवन्त उदाहरण है। फ़िल्म के अन्त में वह एक संकल्पशक्ति के साथ (जीवन की एक नयी शुरुआत) सुबह-सुबह उठती है, और अकेली बाज़ार के लिए निकल जाती है जहाँ उसके जीवन में कोई दखलंदाजी न करे, अपनी पसंद से सैंडिल खरीदकर, बीड़ी (जिसे उसने पति की जेब से निकाला था ) का धुआं उड़ाती है, वह धुंआ जिसके तले उसने अपना सारा जीवन घुटन में ही बिता दिया लेकिन आज अपने जीवन की तमाम घुटन को धुएं में उड़ाकर मानो तमाम बोझ से हलकी हो गयी। लगता है उसने अपनी सभी फ़िक्र को भी उड़ा दिया। ये उसकी मुक्ति के क्षण हैं।
मजबूत इरादों को प्रबलता से सुदृढ़ बनाने वाली यह फ़िल्म आपको भी विवश करेगा कि आप भी माँ से पूछे आप कैसे हो? जो पहले कभी नहीं हुआ क्योंकि माँ ने कभी शिकायत नहीं की। ऐसा उत्तर सुनने को मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और आपके जीवन में भी हलचल मच जाती है आप बैचैन हो उठतें हैं कि माँ को शिकायत थी! तो कभी कहा क्यों नहीं?‘…मैं इस तरह नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं रह सकती’ माँ को रोते हुए देखना उफ्फ! अत्यंत दर्दनाक है! माँ अपनी महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को भूलकर एक नकली आदर्श जीवन ढो रही है, 80-90 प्रतिशत महिलाएं इसी प्रकार का दोहरा उदास जीवन जी रहीं हैं।
फिल्म के आरम्भ में जब वह बड़े चाव से बेटी को उपहार दिखा रही है पति कहता कि ‘क्या फालतू बाज़ार लेकर बैठ गयी सफर से कमर दुःख गयी जाओ चाय बनाओ’ जबकि वह भी सफर में उसके साथ ही आई है वो नहीं थकी क्या? इस तरह का व्यवहार बंद करना होगा यह फिल्म मध्यवर्ग की नब्ज़ को न केवल टटोलती है अपितु घोषणा करती है कि आत्म केंद्रित, हावी, भावहीन पुरुष समाज में स्त्रियों के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। सीमा पाहवा का शानदार अभिनय जो बिना बोले “मौन भी अभिव्यंजना है” चरितार्थ करता है। 

घर की मुर्गी’ संस्कार परम्परा और पारिवारिक खूँटें में बंधी छटपटाहट को व्यक्त कर रही है पर जब पति पत्नी के ब्यूटी पार्लर के काम की मजाक उड़ाते हुए मित्र मंडली के बीच कहता है कि ‘मैं अकेला घर चलाने वाला…अपर लिप्स और आई ब्रो बनाने से घर चलता है क्या?’ पत्नी घर की नौकरानी से अपने दर्द को बयां करती है‘हमसे अच्छा तो ये प्रेशर कूकर है गुब्बार भर जाता है तो चिल्ला तो देता है सिटी बजाकर’। आहत हो कह उठती है “मुझे ब्रेक चाहिए…नहीं मुझे अकेले जाना है…मैंने टिकट करवा लिया…मैंने आई ब्रो और अपर लिप्स बना बना कर पैसे जोड़े हैं… आपसे नहीं चाहिए”
ये सभी संवाद उसके आहत और सदा कुचले गये आत्मसम्मान को इंगित करते हैं कि भरे-पूरे परिवार में भी वो अकेली है एक मैड से ज्यादा कुछ नहीं, और वो बेड़िया तोड़ अस्तित्व की तलाश में निकल भी पड़ती है। पर हाय रे, भारतीय नारी के संस्कार! उसके जीवन के यथार्थ, जिम्मेदारियों के प्रति दायित्व भाव और वो भारतीय संस्कारों से जकड़ी हुई ख़ासकर बच्चो की चिंता और मोह से, वापस लौट आती है जो भारतीय स्त्री के उस पक्ष को उजागर करता है जहाँ वह अपना अस्तित्व परिवार से अलग समझ ही नहीं पाती। ये उसका उदार समर्पित भाव है जो इस समाज द्वारा बचपन से बुना गया है
यह भी पढ़ें – स्त्री विमर्श के देशी आधारों की खोज
न्यूलीमैरिड गर्ल होलिका दहन नामक फिल्म सिखा जाती है, अपने व्यक्तित्व पर मन पर जीवन पर किसी और को नियंत्रित न करने दें अपने अधिकारों को समझें। पुरुष कैसे अपनी धूर्तता से स्त्री के लिए कटु यथार्थ निर्मित करता है‘मेरा और मेरे बाप का पैसा है चाहे जैसे खर्च करूं …तुम पर एक पाई नही खर्च करूंगा ..तुम्हरे साथ घुटन होती है…तुम हमेशा लव लव करके मूड ऑफ कर देती हो…मेरे सामने ही मेरे दोस्तों के साथ फ्लर्ट करती हो पीछे जाने क्या करती होगी…जाओ निकलो यहाँ से …जहाँ मज़े लेने है लो इस घर में दोबारा मत आना’…मैंने तुमसे नहीं कहा था माँ बाप का घर छोड़ आओ” उसके सपनों का ताजमहल ध्वस्त हो जाता है सफ़ेद संगमरमर ताज तो पत्थर का है, जिसमें संवेदनाएं नहीं लेकिन ये पुरुष तो मानव है इसकी संवेदनाये कहाँ दफ़न हो गयी।
पति के कटु व्यवहार के कारण को न समझकर उन बातों चीजों को दिनचर्या का अभिन्न अंग मान लेती हैं खुद ही को दोषी भी मान बैठती हैं। लेकिन कब तक अपने प्रियजनों की नफरत को संजोएगी? यह जीवन बहुत बड़ा है। कमजोर व्यक्तित्व जो देवियों के महिमामंडन के व्याज से निर्मित किया है उसका (होलिका दहन) त्याग करो सपनों का आकांक्षाओं का नहीं। नकली मूर्तियों-सी सुसज्जित देवी का आवरण उतार फेंकों क्योंकि उसे जला कर समाज उत्सव ही मनायेगा। आम मनुष्य सा जीवन जीकर देखों कितना चैन और सुकून है होली के रंगों की भांति जीवन के सभी रंगों का आनंद लो। 

That Day After Everyday फ़िल्म देखते हुए आप अपराध बोध में जा सकते है और छेड़छाड़ जैसी मामूली समझे जाने वाली हरकतों पर गम्भीरता से सोचने लगते हो, आप अपनी माँ, बहन, दोस्त सभी की सुरक्षा को लेकर डर जाते हैं। स्त्री की इस कमज़ोर स्थिति का कारण महिलाओं के प्रति दमनकारी संस्कृति है तो छेड़ने के लिए लड़कों द्वारा गाये गये भद्दे गीत भी इसके लिए जिम्मेदार है। फ़िल्म के आरम्भ में लड़की चुपचाप रसोई में सभी काम जल्दी-जल्दी कर रही है उसे ऑफिस जाना है चाय, टिफ़िन, लंचबॉक्स आदि और पति जो निठल्ला है ज़ोर-ज़ोर से अखबार में मुम्बई नगरी में औरतों की सुरक्षा के बारे में खबरें पढ़ रहा है लड़कियों के रेप कारण गिना रहा है ‘औरतें जितना चुप रहें उतना ही अच्छा है…लड़कों के मुंह लगना कोई अच्छी बात है क्या? तुम कोई ऐसा काम क्यों नही करती जो घर में बैठकर हो जाये…कहीं ऐसा न हो कि तुम भी किसी नाले में कटी-फटी मिलो’ कामचोर पति वितृष्णा होती है ऐसे समाज से जहाँ इस प्रकार के वाक्य दिल-दिमाग में भरे जाते हैं।
दूसरे दृश्य में भी दिल्ली में पांच वर्ष की लड़की के रेप की खबर आ रही है ‘माँ बेटी से कहती है की घर में रहो थोड़े कम में गुज़ारा कर लेंगे। ’यानी स्त्री घर में कैद रहे क्योंकि बाहर राक्षस प्रवृति का पुरुष आपको नोंच खायेगा। तब एक सेल्फ डिफेन्स की ट्रेनिंग वाली दीदी उन्हें समझाती है कि ‘ताकत शरीर में नहीं मन में होती है जिस दिन तुमने मन पक्का कर लिया, तुम्हें कोई नहीं नहीं रोक सकता, खुद को कमज़ोर मान लोगी तो वो फायदा उठाएंगे ही’ कहानी अन्त अत्यंत मजेदार है पति किचन में खाना चाय बना रहा है, और पति की प्रशंसा कर रहा है संकेत स्पष्ट है कि डरोगे तो डरायेंगे सहोगे तो दबायेंगे इसलिए सामना करने को सदैव तैयार रहो। काम का कोई बटवारा स्त्री पुरुष के आधार पर नहीं होना चाहिए काम नहीं है तो घर का काम करना ही होगा रसोईघर केवल औरत का कर्तव्य नहीं। 

कोरोना काल में देवी नामक लघु फिल्म का प्रसारण मानो घर में डरे दुबके बैठे पुरुष समाज को सपष्ट कर देना चाहती है कि स्त्री का तो पूरा जीवन ही असुरक्षा के घेरे में कैद लॉकडाउन में बीतता है कहाँ-कहाँ, किस-किस से वह स्वयं को सुरक्षित रखें, क्या घर, क्या बाहर उसकी सुरक्षा के लिए कोई सैनेटाईज़र भी नहीं। लगभग 22 हजार कमेंट इस ओर इशारा करते हैं की भारत में स्त्री सुरक्षा को लेकर सभी को शिकायत है, पर फिर भी सुरक्षा को लेकर सभी आशंकित हैं।
10-12 महिलाओं से भरा एक कमरा जो भारत में बलात्कार की रौंगटे खड़े करने वाली अनगिनत कथाओं का लैंडस्केप ही है जिसमें भारत की हर वर्ग, भाषा, आयु की महिलाएं हैं। टीवी एंकर स्त्री सुरक्षा व्यवस्था पर चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा है और अचानक टीवी बंद। यानी जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो अब मर गयी इसलिए अब वो खबर भी नहीं रही। यहाँ कोई ‘देव’ नहीं ?…(देवियाँ ही देवियाँ है) यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही, टीवी से तो लगता है कि रोज़ नये आयेगें, कितनों को बाहर बिठाएंगे सबको बकरियों की तरह ठूंस दिया। संवाद पितृसत्तात्मक समाज में पारिवारिक संस्थाओं, राजनितिक वर्चस्व सभी कीपोल खोल रहीं हैं पृष्टभूमि में घंटी का बज रही है जो न्याय व्यवस्था कोजगाना चाहती है।
अन्त में ज्योति कहती है ‘कोई कहीं नहीं जायेगा जितनी जगह है उसी में एडजस्ट कर लेंगे’ समझौता जो स्त्री का स्वाभाव ही है समाज में उसे कोई ‘स्पेस’ नहीं मिला। और समझ अत है कि सभी मृत है (अहल्या की भांति पत्थर) तन के साथ मन भी कुचला हुआ है अपनों के द्वारा, अदालत में दबी पड़ी है लंबित फाइलों में। जब एक छोटी लड़की कमरे में प्रवेश करती है तो वह दृश्य पुरुष की हैवानियत के प्रति क्रोध, घृणा, आक्रोश पैदा करते हैं। एक लड़की जिसे जला दिया गया था वो वैक्सीन कर रही है, अपने सौन्दर्य का ईनाम उसे इस रूप में मिला। एक लड़की कहती है ‘तो क्या हुआ मुझे खून नहीं निकला, मुझे जलाया, काटा नहीं गया पर दर्द तो मुझे भी हुआ था मैं…मैं सदमे से’… मेरे भीतर कांच की बोतल डालकर हाईवे पर फेंक दिया … तेरह साल की थी तब शादी कर दी… रोज़ रोज़…चाक़ू से गला रेतकर’ बलात्कार के शारीरिक मानसिक कष्टों व सामजिक लांछनो का सामना करते हुए, दर्द की विभीषिकाओं से जूझती ये स्त्रियाँ उस दुनिया को ही छोड़ आई। ‘चुपचाप’ नामक फिल्म में भी बलात्कार के बाद पति पत्नी को समझाता है ‘नहीं पुलिस नहीं तुम्हें चुप रहना होगा’ चुप रहने को अभिशप्त स्त्री!
यह भी पढ़ें – वेब शृंखला की संस्कृति और राजनीति में स्त्री
वस्तुत: भारतीय परिवेश में परिवार संस्था में स्त्री की असहायता को अत्यंत सहज अभिनय व कैमरे की विशेष शैलियों के साथ इन फिल्मों में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें देखते हुए अनुभव होता है कि हमारी माँ, दादी-नानी, मौसी, बहन, सखी-सहेलियों ने सदियों से अधूरी आकांक्षाओं के ट्रंक का बोझ बड़े ही संभाल कर उठा रखा है और कहीं थाह नहीं है। संवाद, अभिनय, मौन, संगीत, परिवेश आदि के माध्यम से घरों को आजीवन अपनी फ्री सेवाएं देती आम भारतीय नारी मन को खोलकर हमारे सामने रख देंती हैं। भारतीय पुरुष की स्त्रियों के प्रति उपेक्षा का भाव, उन्हें दोयम दर्जे का मान लेने की अटूट धारणा के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। लॉकडाउन काल में जिस तरह से घरेलु हिंसा की ख़बरें बड़ी है तो इनकी लोकप्रियता महत्ता और जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है। साहित्यिक संवेदनशीलता और तकनीक की विशेषता के साथ बड़ी ही सादगी से वर्तमान समाज में स्त्री मन का अत्यंत सुंदर सूक्ष्म लैंडस्केप चित्रांकित करने वाली यह फ़िल्में बहुत गूढ़, गहन, गम्भीर विषयों को हमारे समक्ष रखतीं हैं।