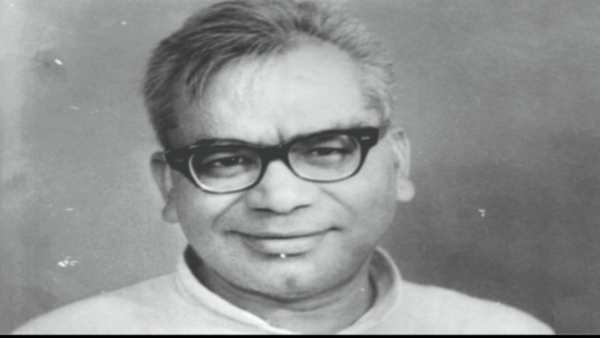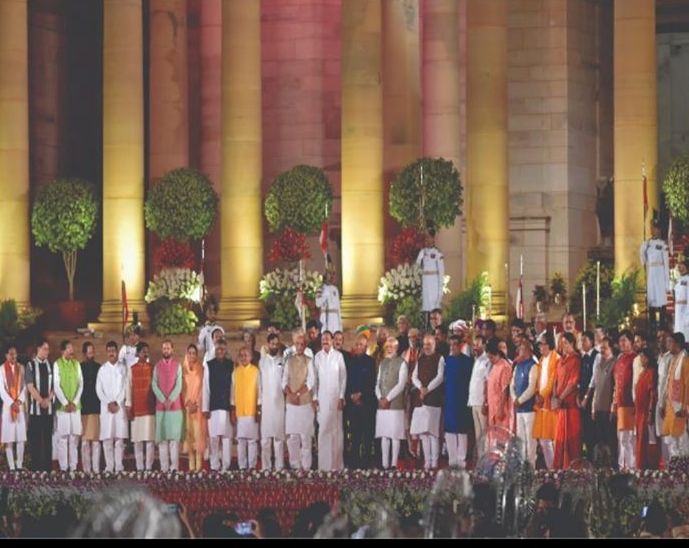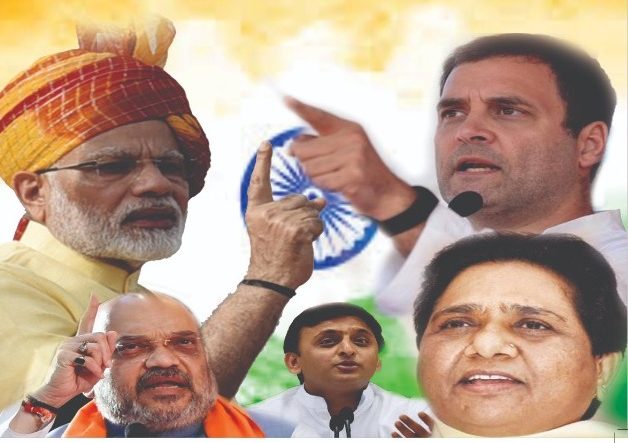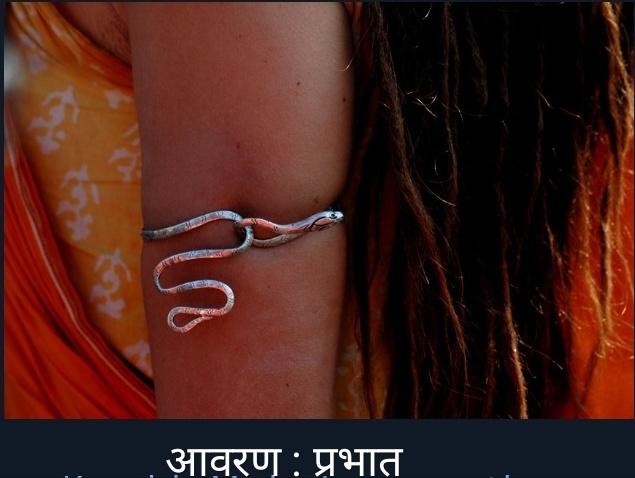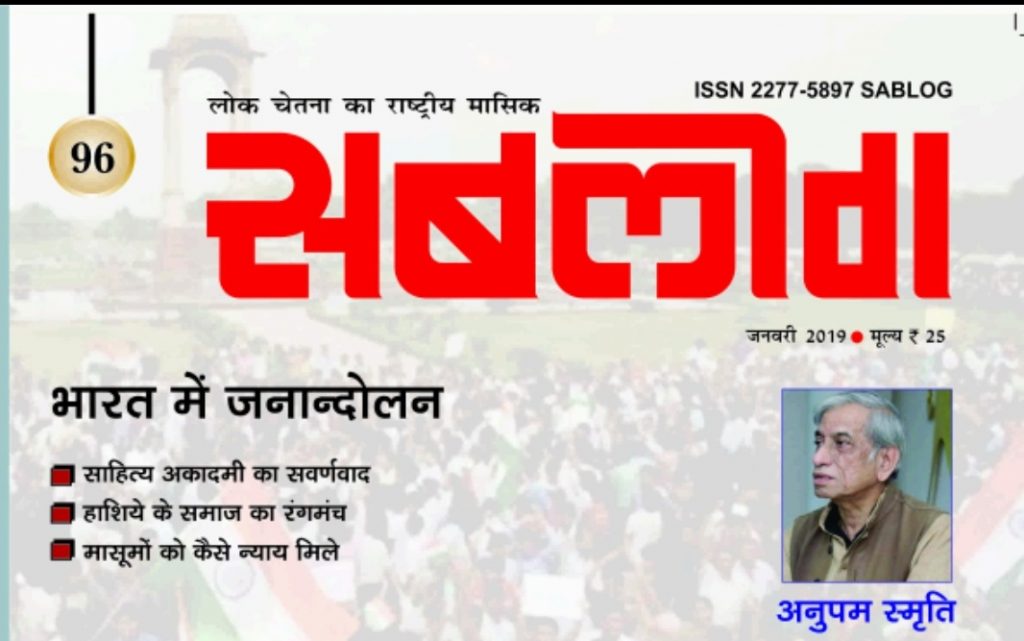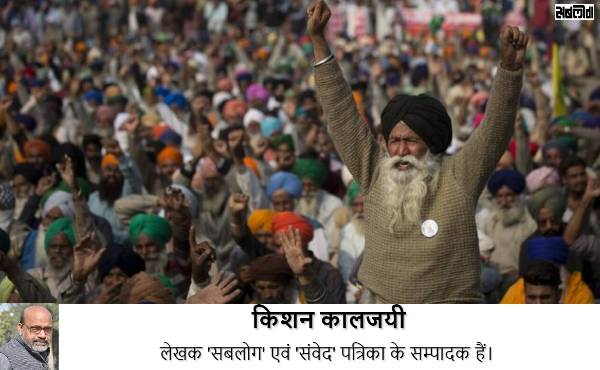
किसानों के देश में किसान की उपेक्षा त्रासद
किसानों और केन्द्र सरकार के बीच हुई नौवीं बातचीत भी बेअसर रही, अब अगली वार्त्ता 19 जनवरी को होगी। किसान नेताओं ने कहा है कि जब जब सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी, वे जाएँगे। इस बीच प्रसिद्ध न्यायाधीश मार्कण्डेय काट्जू ने पत्र लिखकर प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया है कि सरकार नया अध्यादेश जारी करके इन कृषि कानूनों को रद्द करे। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस की पैरेड में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ऐसे में टकराव और हिंसा की सम्भावना प्रबल है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गणतन्त्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से मना कर दिया है। पत्र तो अन्ना हजारे ने भी प्रधानमन्त्री को लिखा है कि अगर किसानों की माँगें नहीं मानी गयीं तो जनवरी के अन्त से वे दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर रहेंगे और यह उनके जीवन की अन्तिम भूख हड़ताल होगी।
यह एक करुण सच्चाई है कि दिल्ली में किसानों के आन्दोलन के पचासवें दिन तक 121 लोग इस आन्दोलन में शहीद हो चुके हैं। स्वतन्त्रता आन्दोलन के बाद स्वतन्त्र भारत में शायद यह पहला मौका है जब किसी शान्तिपूर्ण आन्दोलन में इतने किसानों और सन्तों की शहादत हुई है। अपनी जान की बाजी लगाकर किसान पिछले पचास दिनों से ठिठुरती रात में भी इस बात के लिए सड़कों पर आन्दोलनरत हैं कि सरकार ने कृषि सम्बन्धी जो तीन कानून बनाये हैं, उन्हें वापस ले, लेकिन सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। दूसरी तरफ सरकार शोर यह मचा रही है कि उसने किसानों के हित में तीनों कानून बनाये हैं और किसान अपने ही हित के कानून को समझ नहीं रहे हैं। क्या भारतीय किसान इतने नासमझ हैं कि अपने हितों को भी वे नहीं पहचान सकते?
हमारे यहाँ के किसान प्रायः स्वाबलम्बी रहे हैं। उनके स्वाबलम्बन को आजादी के बाद धीरे धीरे कुतरा गया और अब तो किसानी और किसान दोनों को निगलने की तैयारी हो रही है। अँग्रेजों के समय 1925 में 10 ग्राम सोने का मूल्य 18 रुपये और एक क्विण्टल गेहूँ का मूल्य 16 रुपये था। अर्थात तब का किसान 112.5 किलोग्राम गेहूँ बेचकर दस ग्राम सोना खरीद सकता था और इतने गेहूँ से आज एक जोड़ा अच्छा जूता भी नहीं ख़रीदा जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों के अनाज को छोड़कर सभी चीजें महँगी हुई हैं।
सूखा और बाढ़ के कारण जब फसल में मन्दी होती है तो राहत की राजनीति तेज हो जाती है। इसलिए भारत में यह मुहावरा ठीक लगता है कि जिस वर्ष यहाँ खेतों में अच्छी फसल लगती है राजनीति और नौकरशाही में सूखा रहता है। चौपट खेती और कम उपज के कारण (जिजीविषा, जीवट और संघर्ष के लिए ख्यात) किसान आत्महत्या कर ले यह बात तो भारी मन से समझ में आती है, लेकिन अधिक उपज भी आत्महत्या का कारण बन सकती है, यह समझ से परे है। मामला महाराष्ट्र का है। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब प्याज राजनीति को प्रभावित करता था। प्याज की कमी और बढ़ते भाव के कारण राजनीतिक भविष्य को खतरे में देखते हुए सरकार के लोगों ने प्याज के किसानों को खेती के लिए उदारता से कर्ज दिया। संयोग से प्याज की अच्छी फसल हुई, कायदे से प्याज के किसानों को अमीर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।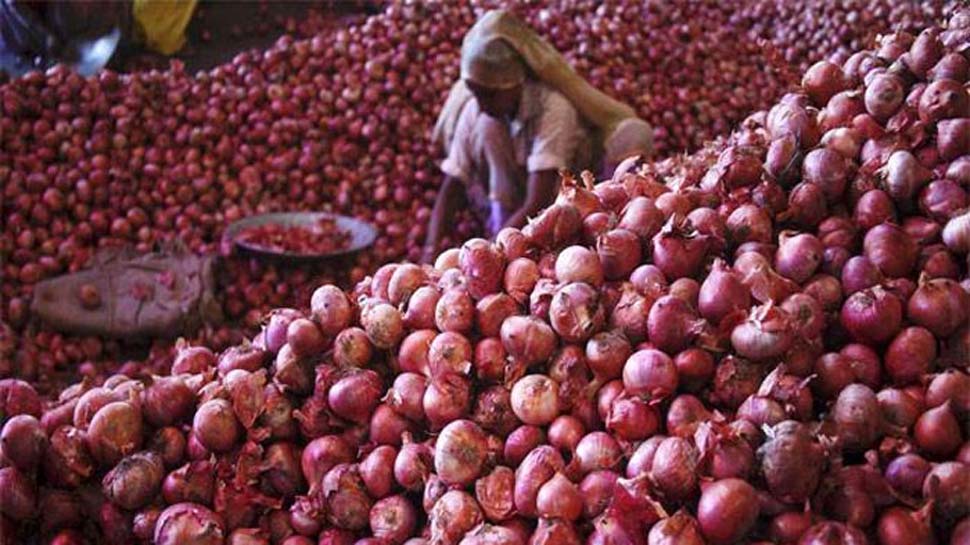
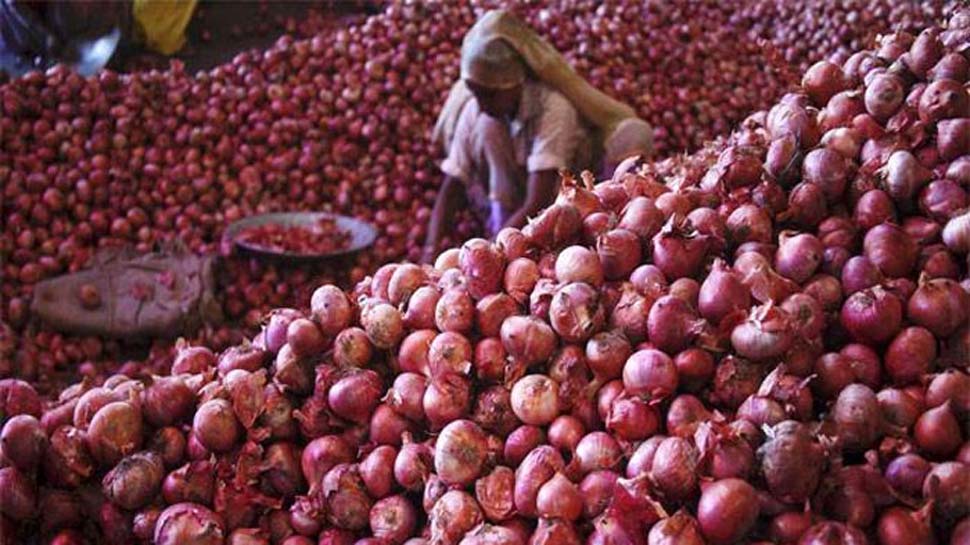
प्याज की फसल इतनी अधिक हो गयी कि रखने की जगह ही नहीं रही,प्याज सस्ते हो गये,सड़ने लगे। आखिरकार औने पौने दाम में किसानों को प्याज बेचना पड़ा। उनकी लागत भी नहीं लौटी और कर्ज के दबाव में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। प्याज की उपज के ठीक बाद यदि सरकार इन्हें खरीद लेती तो आत्महत्या की नौबत नहीं आती। न्यूनतम समर्थन मूल्य की यहीं जरुरत होती है और इसी मूल्य के लिए दिल्ली में किसान जान की बाजी लगाए हुए हैं। किसान बस इतना चाहते हैं कि उनके फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती रहे। आन्दोलनकारियों से सरकार कहती रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा। आन्दोलनकारी इसी आश्वासन को लिखित में माँगते हैं तो सरकार चुप हो जाती है। नये कृषि कानून में निजी कम्पनियों को यह आजादी रहेगी कि वह मण्डियों के बाहर भी किसानों की फसल की खरीद कर सकती है। सरकारी महकमे के काम काज करने के जो तरीके रहे हैं, उसमें यह बिल्कुल सम्भव है कि निजी कम्पनियाँ सरकारी मण्डियों को निष्क्रिय और निष्प्राण कर देंगी। किसान इसी बात से डरकर नये कानून का विरोध कर रहे हैं।
संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि, कृषि,पानी, शिक्षा आदि राज्य के अधीन हैं, फिर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और विभिन्न किसान संगठनों से विचार विमर्श किए बिना लॉकडाउन की चुप्पी और अँधेरे में अध्यादेश के रास्ते इन कानूनों को बनाने का यह उतावलापन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से अवैध और अनैतिक साँठ-गाँठ का ही संकेत देता है। दरअसल किसानों पर जबरन थोपे जा रहे इन कृषि कानूनों की जड़ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मुनाफाखोरी और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक हितों से जुड़ी हुई है। शायद इसीलिए भारत के किसान भले इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हों लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन कानूनों को अच्छा बताते हुए इनका समर्थन कर रहा है। किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच जिस दिन (15 जनवरी) वार्ता होने वाली थी,उसकी पूर्व संध्या को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रवक्ता गैरी राइस कह रहे थे कि भारत में बने ये कानून बहुत अच्छे हैं, इन्हें ढंग से लागू किया जाना चाहिए। हाँ यह बात उन्होंने जरुर जोड़ी कि इनसे किसानों को कोई नुकसान हो रहा हो तो उनका ख्याल रखा जाना चाहिए ठीक उसी तरह जैसे शराब की बोतलों और सिगरेट के पैकेटों पर यह वैधानिक चेतावनी रहती है कि स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है।
यह भी पढ़ें – कृषि कानून और किसान आन्दोलन
यह बात समझने की जरुरत है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत सरकार द्वारा बनाए गए ये कृषि कानून अच्छे क्यों लग रहे हैं? यह बात दुनिया से छिपी हुई नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था का अधिकांश विदेशी कर्ज पर निर्भर है। नरेन्द्र मोदी जब (2014) प्रधानमन्त्री बन रहे थे उस समय भारत पर 84 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज भारत पर 162 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और 2022 तक यह 197 लाख करोड़ रुपये का होने वाला है। कर्ज देने वाली वैश्विक संस्थाएँ चाहती हैं कि पूरी दुनिया की खेती पर पूँजीवादी व्यापारिक घरानों का नियन्त्रण हो जाए और ये सारे कारोबार उनके द्वारा प्रदत्त कर्ज की पूँजी से संचालित हों। भारत में बने ये कानून खेती में बड़े व्यापारिक घरानों का प्रवेश द्वार हैं।
इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ये नये कृषि कानून अच्छे लग रहे हैं। इसकी सम्भावना प्रबल है कि आने वाले समय में थोड़ा और कठिन ब्याज दर और असुविधाजनक शर्तों पर मुद्रा कोष भारत को कर्ज देगा और उस कर्ज के पैसे से भारत की सरकार किसानों को सहूलियत नहीं देकर उन व्यापारिक घरानों को कर्ज के रूप में प्रोत्साहन पूँजी देगी जो खेती को अपना व्यापार बनाएँगे। यदि खेती का व्यापार उनका नहीं चला तो यह कर्ज भी माफ कर दिया जा सकता है, भले देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता जाए। पिछले दस वर्षों में 12 हजार कार्पोरेट कम्पनियों के 500 करोड़ रुपये तक के कर्ज माफ कर दिए गये। जब कि इसी अवधि में 45 हजार रुपये तक का कर्ज बैंकों को नहीं चुका पाने की ग्लानि में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान स्वाभिमानी होते हैं, उनके पास शर्म भी होती है और कई बार वे शर्म से भी मर जाते हैं, लेकिन कुछ व्यापारी भ्रष्ट और अनैतिक ही नहीं बेशरम भी होते हैं; वे राजनीतिक सत्ता से साँठ-गाँठ कर अपना कर्ज माफ करा लेते हैं, यदि मनोनुकूल माफी नहीं मिलती तो देश ही छोड़कर भाग जाते हैं।

इन्हीं दिनों मैंने एक किसान को 15 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर बेचते देखा, उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद जब खेतों से टमाटर और निकलने लगेंगे तो यह 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो जाएगा। 30 किलोग्राम टमाटर खेत से तोड़ने और उसे बाजार में लाकर बेचने में किसान को कम से कम डेढ़ दिन लगेंगे। डेढ़ दिन की न्यूनतम मजदूरी 450 रुपये और कुल टमाटर बेचने के बाद उसे 300 रुपये मिलेंगे, किसान को हासिल क्या हुआ? एमोजोन पर मक्का के आटे का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 420 रुपये प्रति किलोग्राम है। अपनी लुभावनी नीति के तहत यह कम्पनी इसे 399 रुपये में बेचती है। जबकि एक किलोग्राम मक्के के लिए किसान को 12 रुपये से अधिक नहीं मिलता। आलू के चिप्स में भी यही गणित देखा जा सकता है। चाय, नमक, बिस्कुट के मामले में भी लगभग ऐसी ही बाते हैं। अन्य उत्पादकों के साथ सहूलियत यह है कि वे अपने उत्पाद की कीमत खुद तय करते हैं। लागत मूल्य के साथ मुनाफा, प्रचार-प्रसार और मालिक के साथ नौकर के सैर- सपाटे का भी खर्च उत्पाद के मूल्य में जुड़ा रहता है। और एक किसान है खेती से जिनकी लागत वसूल हो जाती है तो वह अपने को धन्य समझता है।
यह सच्चाई है कि बीज,खाद,मजदूरी और कृषि उपकरण की कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं और अनाजों की कीमत उस अनुपात में नहीं बढ़ी हैं। यही कारण है कि किसानों की आर्थिक हालत लगातार खराब होती गयी और कर्ज के मकड़जाल में वे फँसते चले गये। इस फाँस से मुक्ति का रास्ता उन्हें आत्महत्या में दिखता है, इक्कीसवीं सदी का इससे बड़ा अभिशाप कुछ और नहीं हो सकता। किसानों की उपज और मेहनत का अवमूल्यन आजाद भारत में जितना हुआ उतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बल्कि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि किसानों की जान का भी मोल नहीं समझा जा रहा है। यह विचारना आवश्यक है कि किसानों की यह दुर्दशा किसने की और क्यों?
यह भी पढ़ें – किसान आन्दोलन और महिलाएँ
दरअसल खेती और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपना नियन्त्रण इसलिए भी बढ़ाना चाह रही हैं कि ये व्यापार सुरक्षित और सुनिश्चित हैं। सौन्दर्य-प्रसाधन, स्कूटर-मोटर, क्रीम-पाउडर, साबुन-सेम्पू आदि के मामले में थोड़ा विकल्प बचा भी रहता है, आप चाहें तो इसकी जरूरत को थोड़े दिनों के लिए टाल भी सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए यदि आटा,चावल, दाल सब्जी पर इन कम्पनियों ने नियन्त्रण ले लिया तो ये मनमानी कीमत हमसे वसूलेंगी। फिर कोई लोकतन्त्र कोई संसद और कोई सरकार हमारी रक्षा नहीं करेगी क्योंकि यह सरकार पहले से ही अपने नागरिकों को उपभोक्ता बनाने के लिए आमादा है। संसद की हालत तो यह है कि आज जो विपक्ष में हैं उन्हीं के लोगों ने 90 के दशक में किसान दुर्दशा की यह पटकथा लिखी थी।
राहुल गाँधी का किसानों के धरने में शामिल होना यदि किसी को हास्यास्पद या राजनीतिक रस्म लगता है तो यह अनुचित इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं की काँग्रेस ने नयी आर्थिक नीति लागू करके उदारीकरण और भूमण्डलीकरण का द्वार खोला था। क्या राहुल गाँधी को यह याद दिलाने की जरूरत है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार ने ही 2004 में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था? उन्हें मालूम तो यह भी होगा कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2006 में ही इसी सरकार को सौंप दी थी। किसान-आन्दोलन के समर्थन में किसानों के साथ बैठे हुए राहुल गाँधी ने क्या यह सोचा होगा कि यदि 2006 में ही स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अमल हो गया होता तो इस आन्दोलन की शायद नौबत ही नहीं आती और हजारों किसान आत्महत्या से भी बच जाते?

1984 के दंगे में सिखों का जिस तरह से संहार हुआ था उसके लिए सोनिया गाँधी और मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी और राहुल गाँधी ने भी इस माफीनामे से अपना इत्तफाक रखा था जो उचित ही था। जाहिर है स्वर्ण मन्दिर में सैन्य कार्रवाई, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी की हत्या और सिखों का संहार; ये हादसों का दुखद सिलसिला था और बड़ी दुर्घटनाएँ थीं। लेकिन अब तक चार लाख किसानों की भी (आत्म)हत्या हो चुकी है। इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? किसी में किसानों की उपेक्षा के लिए माफी माँगने का नैतिक साहस है? स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 वर्षों तक दबाए रखने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन के नेताओं को किसानों से माफी नहीं माँगनी चाहिए? किसानों की उपेक्षा इतनी भर ही नहीं है। 2014 के लोक सभा चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि उसकी पार्टी की सरकार आएगी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। क्या भाजपा सरकार ने वादा निभाया?
भाजपा की सरकार आयी, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की जब बात हुई तो सरकार की तरफ से कहा यह जाने लगा कि इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार के पास संसाधन नहीं हैं। दुखद आश्चर्य यह है कि एक तरफ नरेन्द्र मोदी की सरकार संसाधन की कमी का रुदाली गा रही है, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने सत्ता सँभालते ही नयी योजनाओं की बौछार लगा दी। प्रधानमन्त्री आवास योजना,मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना जैसी लगभग 135 नयी योजनाएँ इस सरकार ने शुरू की हैं। बेशक इनमें से कुछ योजनाएँ काफी लोकप्रिय और हितकारी हैं। जब इसी दौर में इसी सरकार ने 78 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज लिया तो संसाधनों का रोना क्यों? केन्द्र सरकार को साहस के साथ स्पष्ट कहना चाहिए कि किसान हित उनकी प्राथमिकताओं में नहीं है।
यह भी पढ़ें – किसान आन्दोलनः सवाल तथा सन्दर्भ
किसान-आन्दोलन के विरोधियों द्वारा यह बात प्रमुखता से कही जा रही है कि यह सिर्फ पंजाब और हरियाणा के मालदार किसानों का आन्दोलन है। इस बात में सच से ज्यादा दुराग्रह है। सच यह है कि अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद का जो ढाँचा रहा है,उससे इन दोनों राज्यों को ज्यादा फायदा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की नीति ने इनके दिन बदले हैं और इनके घर सम्पन्नता आयी है। यही कारण है कि आज आय के मानक पर पंजाब और हरियाणा ऊपर हैं। यहाँ से ये किसान पीछे नहीं जाना चाहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य इन किसानों का प्राण-वायु है। ऐसी बात भी नहीं कि अन्य राज्यों को इन नीतियों का लाभ नहीं मिला है। आज से 20 वर्ष पहले गेहूँ और धान की खरीद का 80% पंजाब और हरियाणा से होता था। गेहूँ की खरीद में मध्य प्रदेश ने 2019-20 में बड़ा योगदान(40%) किया है। धान में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी खरीद में वृद्धि हुई है। इस आन्दोलन में लगभग सभी प्रान्तों के किसान प्रतिनिधि शामिल हैं, यह बात अलग है कि नजदीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा,पंजाब और हिमाचल के किसान ज्यादा संख्या में हैं।
उत्तर भारत में पंजाब इस मायने में बिल्कुल अलग प्रान्त है जहाँ के चुनाव में नरेन्द्र मोदी का जादू नहीं चलता। इस गुस्से और पंजाब के किसान की बहुतायत के कारण केन्द्र सरकार यदि आन्दोलन की उपेक्षा कर रही है तो राजनीतिक तौर पर भी एक ऐसी बड़ी गलती की तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं, जिसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि केन्द्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो सभी ने किसानों की उपेक्षा की है तो इसलिए कि किसान उनके लिए वोट बैंक नहीं हैं और दुर्भाग्य से अभी तक इस देश में वे राजनीतिक ताकत भी नहीं बने हैं। लेकिन इस किसान आन्दोलन की प्रकृति कुछ अलग है।उनकी वोट की ताकत भले एकजुट नहीं हो, लेकिन सत्ता और सियासत को यह समझने में भूल नहीं करनी चाहिए कि वे अन्नदाता हैं और वे ही देश की भूख मिटाते हैं। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे उन किसानों से टकरा रहे हैं जिनका यह देश है। किसानों का गुस्सा यदि देश का गुस्सा बन गया तो फिर क्या होगा कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता।
.