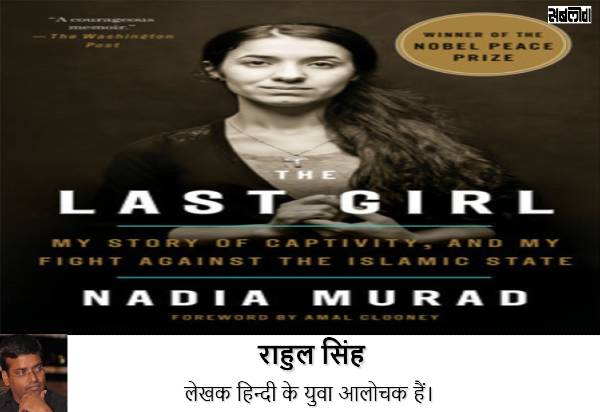पढ़ा लिखा अंगूठा छाप भारतवर्ष बनेगा विश्वगुरु
जिन्होंने जमाना देखा है, वे प्रतिप्रश्न करते हैं कि क्या कोई ऐसा भी जमाना था जब सब बराबर रहे हों, असमानता न रही हो? हाथ कंगन को आरसी क्या की ठसक से वे अपनी हथेलियों की अंगुलियाँ भी दिखाते हैं कि सब बराबर कहाँ हैं। अंगुलियाँ दिखाते समय उनका अंगूठा किसी कड़कनाथ की थप्पड़ की तरह तना होता है।
लेकिन इसके बावजूद समता की माँग उठती रही है। पहले ज्यादा उठती थी। आन्दोलन होता था। हड़कम्प मचाया जाता था। इससे असमानता के खिलाफ एक वातावरण बनता था। समता के लिए एक सपना बनता था। हाल के इतिहास में एक काल खण्ड समता की माँग से उबलता रहा है। पूरा का पूरा एक युग।
अब समता एक सपना है। जमीन पर अब इसकी कोई माँग नहीं है। कोरोना में मजदूरों के बेहाल दृश्य देखकर किसी को भी समता की जरूरत का ख्याल नहीं आया। सबने फौरी राहत की माँग की। उचित भी था। आदमी जख्मी हो, तो तत्काल मरहम अवश्य चाहिए। लेकिन अंतिम लक्ष्य तो यह होना ही चाहिए कि ऐसा घायल समय दोबारा न आए। आर्थिक इम्यूनिटी बढ़े। सरकारी महकमों में तमीज बढ़े। इतनी बढ़े कि पूरी आबादी का जीवन स्तर सम्मानजनक और पीड़ारहित हो। समता ही रास्ता है। साथी हाथ बढ़ाना।
समता का रास्ता रोक कर खड़ी होती है किस्मत। वे जो समता की माँग से सहमत नहीं होते वे किस्मत के दर्शन को अपना हथियार बना लेते हैं। बार बार वार करते रहते हैं इससे। वे बताते रहते हैं जिसकी जैसी किस्मत उसका वैसा प्रारब्ध। यह सिक्का खूब चलाया गया है। आज भी ऐसे लोग हैं जो इस सिक्के में चमक देखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इसे अचल भी बना दिया गया है।
किस्मत के तर्क वाले सिक्के में जब छेद किया जाने लगा तो वे दिमाग और प्रतिभा की आड़ लेने लगे। बताने लगे कि सब का दिमाग एक जैसा नहीं होता। इस हथियार से सबसे ज्यादा चोट स्त्रियों पर की गयी। बताया जाता रहा कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। यह भी बताया गया कि प्रतिभा अर्जित नहीं की जाती, जन्मजात होती है। यह सब विषमता या असमानता को सर्वमान्य बनाने का अकाट्य तर्क हुआ करता था। इन दलीलों की हवा निकाली जा चुकी है। जन्मजात वाले तर्क में वंशवाद और वर्चस्व वोध की गमक मिलती है।
हवा दलीलों की निकली, असमानता की नहीं। असमानता बढ़ी। दिन दूनी रात चौगुनी। इतनी कि अंदाजा लगाने से कलेजा मुँह को आ जाए।
शिक्षा और आधुनिकता बहिनी बन कर आईं भारत। इन्हें उम्मीद से देखा गया। माना गया था कि शिक्षा समता का ड्राइवर बनेगी। समता से परहेज करने वालों ने
शिक्षा को ही अपना पायलट बना लिया। समता के रास्ते का रोड़ा बना दिया शिक्षा को। बताया कि जैसी शिक्षा वैसी नौकरी, वैसी हैसियत। शिक्षा से असमानता को साधा। मानो शिक्षा वह गदहा हो जो अर्थव्यवस्था की ढुलाई ढो रहा हो।
असमानता को साधने के लिए ही शिक्षा की सवारी की गयी और उसका नकेल नियन्त्रण में रखा गया। बजट में शिक्षा के लिए प्रावधान की गयी राशि यह खुल्लमखुल्ला बोलती है। व्यवसाय के कुएँ में धकेला गया शिक्षा को। शिक्षा को केवल व्यवसाय नहीं बनाया गया, शिक्षा को व्यवसाय को समर्पित भी किया गया। शिक्षा से आदमी नहीं पैदा हुआ, मानव संसाधन पैदा हुआ। मानव संसाधन नामक उत्पाद भी कितना और कैसा? शिक्षा उद्योग के उत्पाद की मात्रा और उसकी गुणवत्ता नियोजित हैं। उत्पादन का हिसाब किताब कुछ ऐसा है। हर साल दस लाख इंजीनियर और डाक्टर अट्ठाईस हजार। ऐसी है सूझबूझ। ऐसा है करिश्मा !
विभिन्न स्तर के स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था का पोषण असमानता का लालन पालन करना है। शिक्षा के क्षेत्र में म्युनिसिपल स्कूल से लेकर रिलायंस स्कूल तक हैं। इनके दरमियान कितने स्तर हैं? यह असमानता की बुनियाद तैयार करता है जिसपर विषमता का पिरामिड बनता है।


नारा है, सब के लिए शिक्षा। सबके लिए समान शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा। समान गुणवत्ता वाली शिक्षा। समस्या क्या है, शिक्षा उद्योग में समान परिवेश और परिस्थिति बना कर समान गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में? स्कूलों के भिन्न परिवेश और परिस्थितियों की वजह से एक ही सिलेबस से अलग अलग तरह की गुणवत्ता वाले उत्पाद निकलते हैं।
इतना ही नहीं, मानव संसाधन उत्पाद की गुणवत्ता स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग, कैंपस से भी तय होती है। इनमें बड़ी पूंजी लगती है। जितना गुड़ उतनी मिठास वाली बात। सरकारी – गैरसरकारी शिक्षा संस्थानों की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कीमत आंकी जाए तो कई लाख करोड़ होगी। निवेश इतना बड़ा और उत्पाद भूसा। असल में भूसा ही चाहिए। भूसा माने रबड़ स्टांप।
वर्तमान शिक्षा सिद्धान्त असमानता को मजबूत करता है। ऐसा शिक्षा सिद्धान्त सम्पन्नता की अर्थव्यवस्था की फसल है। दरअसल ‘सम्पन्नता का अर्थशास्त्र’ से समानता की फसल नहीं लहलहा सकती। सच तो यह है कि समानता की माँग अगर कहीं अंकुर देती दिखती है तो उसकी मिट्टी खराब कर दी जाती है।
कोरोना के रथ पर सवार अब शिक्षा
कोरोना आया है। इसे एक अभूतपूर्व महामारी बताया गया है। बताया जा रहा है, इस महामारी की मार चौतरफा है। सब कुछ खत्म हो रहा है। मगर क्या खत्म हुआ और क्या खत्म हो रहा है, इसे समझने के लिए थोड़़ा पीछे चलते हैं।
जमाना इक्कीसवीं शताब्दी की शुरुआत का। डिजिटल जीवन दर्शन की शुरुआत। डिजिटल लाइफ स्टाइल माने मानवीय हस्तक्षेप एवं मानव मिलन – सम्मिलन के अवसर का खात्मा। नव उदार आर्थिक व्यवस्था की यह एक जरूरत भर नहीं, अनिवार्य जरूरत है। कोरोना काल में उत्कर्ष पर है यह। पिछले तीन महीनों में अर्बन लाइफ इस तरह से ननपार्टिशिपेटिव हुआ है कि धीरे धीरे पार्टिशिपेसन की जरूरत ही महसूस न हो। डिजिटल के पालतू को यह फालतू लगेगा। मनोरंजन डिजिटल। बौद्धिक सर्कस और सरकश दोनों डिजिटल। प्रवचन डिजिटल। विरोध और विद्रोह डिजिटल। सब का हिसाब किताब रहेगा। जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर किया जा सकेगा।

पिछले तीन दशकों में ऐसी व्यवस्था बनी कि देश की पन्द्रह – बीस प्रतिशत आबादी बिना मानव मुलाकात के सम्पन्न जीवन जी सके। डिजिटल जिन्दगी। यही डिजिटल जिन्दगी अब डर के मारे जरूरत बन गयी है। आगे यह सभ्यता बन जाएगी। सोशल डिस्टेंशिंग का फलसफा अनजाने नहीं आया।
नव उदार आर्थिक व्यवस्था ने अपने शुरुआती दौर में छोटे छोटे दुकानदारों को मारा। जिन्हें नहीं मारा जा सका था उनका हिसाब कोरोना ने बराबर कर दिया। मध्यम दर्जे के व्यापारियों की कमर तोड़ने का रास्ता भी करोना ने बना दिया है। कोरोना महामारी सम्पन्नता की महामारी पर ब्रेक नहीं लगा रही है। उसकी गति को तेज करने के लिए उसने सारे स्पीड ब्रेकर या बंपर हटा दिए हैं। नव उदार आर्थिक व्यवस्था की बुलेट ट्रेन अब अबाध गति से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेगी। भारत में निजीकरण की बुलेट ट्रेन का नजारा देखते जाइए। सम्पन्नता की ओर का हर कदम असमानता के लिए एक नयी पहल है। सम्पन्नता के टापू बनेंगे असमानता के महासागर में ही।
शिक्षा का रामराज्य
जब सब कुछ वैसा होगा जैसा ऊपर बताया गया है तो शिक्षा पुरानी राह पर नहीं बनी रहेगी। उसकी भी नयी राह बनेगी, नया मंजिल बनेगा। कोरोना ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि स्कूल कॉलेज की बिल्डिंगें बेमानी लग रही हैं। ऐसी झलक भी मिलने लगी है कि बिना कैंपस और बिल्डिंगों के भी शिक्षा दी जा सकती है। गुणवत्ता में कोई कमी लाए बगैर। निश्चित रूप से इशारा डिजिटल शिक्षा की ओर है। सरकार इस दिशा में बढ़ रही है। सक्रिय है।
कोरोना के जोखिम का ख्याल रखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को घर से बाहर न निकलना पड़े।
हिन्दुस्तान की कुल आबादी का तीस प्रतिशत अंदाजतन ऐसा है जो रोज स्कूल कालेज जाने के लिए घर से निकलता है। अगर ये बच्चे घर से निकलेंगे तो कोरोना से मुठभेड़ की संभावना बनती है। पच्चीस साल तक के युवाओं को पढ़ने के लिए घर से न निकलना पड़े, कोरोना से बच कर रह सकें, इसका पुख्ता इन्तजाम करना है। कोरोना से सम्बन्धित जो भविष्यवाणियाँ आ रही हैं, वे अभिभावकों को मानसिक रूप से तैयार कर रही हैं कि बच्चों को स्कूल कालेज के लिए बाहर न निकलना पड़े और पढा़ई भी होती रहे।
धीरे धीरे ऐसा ही होगा। इससे पहला मकसद यह पूरा होगा कि आपस में मिलने – जुलने का कोई अवसर नहीं बचेगा। फालतू की बतकही और अड्डा नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इससे चेतना बनती है। संगठन बनता है। और जब ऐसा होता है तो सरकार का सर दर्द बढ़ता है। मास्टर लोग भी एक बड़ा वायरस हैं। वे भी नजरबंद रहेंगे। स्कूल कालेज भी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनेंगे। बच्चे पढ़ने से मतलब रखेंगे और मास्टर पढ़ाने से। नव आर्थिक उदार व्यवस्था का बीज वाक्य ही है मतलबी बनो, अपने से मतलब रखो। एकांत भीषण स्वार्थ अपने में सब भर कैसे विकास करेगा, अपना विनाश करेगा ! सच तो यह है कि एकांत भीषण स्वार्थ का अर्थशास्त्र अपना विनाश नहीं करेगा।

छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त की नीति है भारत सरकार की। मगर अफसोस कि अभी भी आठ दस करोड़ बच्चों ने स्कूल का मुँह तक नहीं देखा है। चौदह वर्ष की उम्र यानी कक्षा आठ तक की पढ़ाई।
आठवीं तक की पढ़ाई के लिए टीवी को माध्यम बनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए अपने अपने बोर्ड का टीवी चैनल बनाएँ। स्कूल समय यानी दस से चार बजे तक रूटीन बना कर इसे चलाना चाहिए। क्लास की व्यवस्था भाषा के आधार पर की जानी चाहिए। भारत सरकार के त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को तीन चैनल बनाने होंगे। हिन्दी, राज्य की भाषा और अंगरेजी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। वजह साफ है। ऐसा करने से जो मानव संसाधन उत्पाद तैयार होगा, उसका सप्लाई कहाँ होगा? जब कोरोना पूर्व सामान्य स्थिति में सप्लाई की गुंजाइश नहीं थी तो अब कहाँ? कोरोना पश्चात हालात में मानव संसाधन की माँग गिरी है।
किसी भी उद्योग की बड़ी चिन्ता होती है उत्पाद की सप्लाई। शिक्षा उद्योग भी ऐसी चिन्ता से गुजरता है। मानव संसाधन नामक उत्पाद एफएमसीजी उत्पाद नहीं है। यह ऐसा उत्पाद है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट में दूरी बहुत कम होती है। जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाता है। इसलिए आउट ऑफ डेट होते ही सड़ने लगता है। सड़ने पर भी फेंका नहीं जा सकता। गंधाने लगता है। सड़ने और गंधाने के दौरान कई तरह के कैमिकल बनने लगते हैं सोच में। इससे लोचा होता है। कई बार आग पकड़ लेती है। ब्लास्ट की संभावना बनती है। सरकार को ब्लास्ट मैंनेजमेंट की प्रक्रिया आरम्भ करनी पड़ती है।
सरकार ऐसे ब्लास्ट से परेशान होती है। केवल सप्लाई न होने की वजह से ही बलास्ट नहीं होता है। ब्लास्ट उस सोच या समझ से भी होता है जो पाठ्यक्रम फेडरल और सिटिजन होने का अर्थ भी समझाती हो और समझ भी देती हो। नव आर्थिक उदार व्यवस्था में फेडरल और सिटिजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर भारत के संविधान के ये दो महत्वपूर्ण कारक और समास हैं। मगर राम राज्य को ऐसे कारक और समास से खतरा महसूस होता है। तभी यह हुआ है कि भारत की वर्तमान सरकार ने बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को कोरोना महामारी की वजह से पॉलिटिकल साइंस से फेडरल और सिटिजनशिप वाले अध्याय को हटा दिया है। क्योंकि नव आर्थिक उदार व्यवस्था को पढ़ा लिखा अंगूठा छाप वाला उत्पाद चाहिए। पढ़ा लिखा अंगूठा छाप वाला ही भारतवर्ष विश्वगुरु बनेगा। किसी ने सही फरमाया है, खुले दिमाग से खुले बाजार का विकास होगा। खुला दिमाग का मतलब ही तो दिमाग खोल कर रख देना है। आत्मनिर्भरता का विश्वमॉडल होगा ऐसा भारतवर्ष।

कोरोना का यह समय कम से कम इस बात के लिए उचित समय है कि एक पॉलिसी बना कर टीवी एवं डिजिटल शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करे। इस ड्राफ्ट का मुख्य मकसद शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता समाप्त करना होना चाहिए। ड्राफ्ट अवश्य तैयार किया जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता समाप्त करने के लिए नहीं, नव उदार आर्थिक व्यवस्था की नयी जरूरत पूरी करने के लिए। यह गौर करने वाली बात है कि शिक्षा नीति के नए ड्राफ्ट में
समता शब्द के लिए एक बार भी गुंजाइश नहीं बनी है।
लगाम कौन लगाए?
ऐसे में यह माँग करना कि ऐसी नयी शिक्षा की प्रकृति बदली जाए,ऐसी जिससे समता की बुनियाद बने, लोकतंत्र की समझ बचे, सामासिकता की आधारशिला न खिसके – आकाश में सूराख करने के लिए पत्थर उछालना है। मगर क्या पत्थर उछालने के लिए बाजुओं में बल बचा है? विकल्पहीन दुनिया मानवीय आत्मविश्वास और भरोसा दोनों का हरण करती है। विकल्पहीन दुनिया के प्रवर्तक और पैरोकार उस भैंसा पर सवार हो गए हैं जिस पर यमराज सवारी करते हैं। कोरोना ऐसा ही भैंसा है। विश्व की महाशक्तियाँ इस कोरोना भैंसे पर चढ़ कर आमने सामने हैं। नरमेध। लोकमेध। दोनों का मकसद अश्वमेध। लगाम पकड़ने वाला कौन?
लगाम लगाई जा सकती, जो होते कोई रवींद्रनाथ हमारे जाने में हमारे खजाने में। लेकिन हमारा खजाना खाली है। जो हैं वे सरकारी खजाने से चलती चक्की का मेवा खाते हैं। मेधा में मलाई जमी है। विश्व अश्वमेधी अभियान उन्हें रोमांच से भरता है केवल। समानांतर या वैकल्पिक शिक्षा का मॉडल वे दे सकें, इसके लिए उनकी खुमारी नहीं टूटती है। खुमारी की कौन कहे, मुर्दों से बाजी लगा कर सोई हुई कौम है यह। फिलवक्त।
.