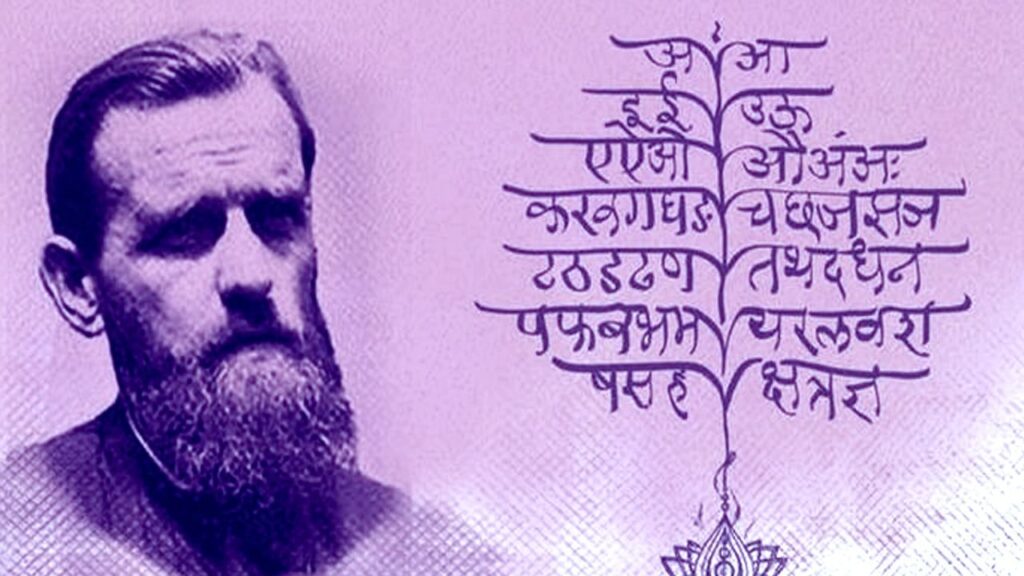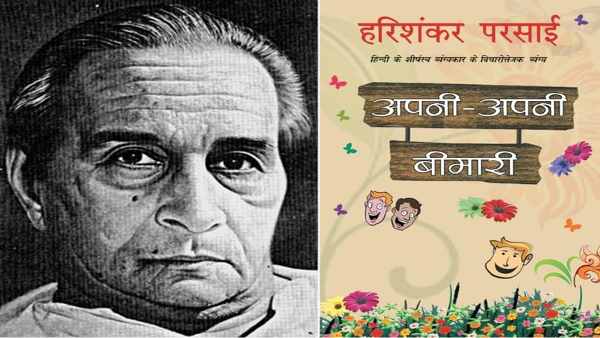सत्ता के दमनकारी उपायों और कानूनों को दृढ़ता से अस्वीकार करना तथा सम्पूर्ण अहिंसक तरीके से उनका प्रतिवाद करने की अवधारणा ‘मानेंगे नहीं – मारेंगे नहीं’ का, आधुनिक दौर में सर्वप्रथम गाँधीजी द्वारा प्रयोग किया गया था। भारतीय जनजीवन के प्राचीन एवं मध्य काल में आर्यों की आयुधों से सज्जित देव मूर्तियों-प्रतीकों, यज्ञों तथा पशुबलियों की हिंसा की वैदिक संस्कृति के विरुद्ध गौतम बुद्ध-कबीर-रैदास जैसे अहिंसक श्रमण संस्कृति के सामाजिक व्यक्तित्वों द्वारा प्रतिवाद के इस उपकरण के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। पुरा कथाओं के मिथकीय चरित्र प्रहलाद तथा एथेंस के प्रतिवादी बौद्धिक सुकरात का उल्लेख भी इस सिलसिले में जरुरी लगता है।
सत्ता के अन्याय के विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन के प्रभावी उपकरण के रूप में, गाँधीजी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी अंग्रेज सरकार के खिलाफ 1908 में किया था। निष्क्रिय प्रतिरोध के इस प्रभावी उपकरण के समर्थन में रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय ने गाँधी को लिखे एक पत्र में कहा था, ‘निष्क्रिय प्रतिरोध का सवाल न केवल भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।’ इसे गाँधीजी ने बाद में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन के रूप में प्रचारित किया। अमरीकी लेखक हेनरी डेविड थोरो (1817 – 1862) ने अपनी चर्चित किताब ‘सिविल डिसओबिडिएंस (नागरिक असहयोग) में लिखा है, ‘नागरिक अवज्ञा स्वाधीनता की सच्ची आधारशिला है। जो अंध आज्ञाकारी हैं वे गुलाम हैं।… न्याय से विमुख सरकार का प्रतिरोध जरूरी होता है।’
गौरतलब है गुलाम भारत में रौलट एक्ट, खिलाफत आन्दोलन एवं अनेक छोटे-बड़े आन्दोलनों से लेकर 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन तक गाँधीजी द्वारा सत्याग्रह के इस हथियार का कारगर उपयोग इतिहास में ज्वलंत अक्षरों में दर्ज है।
यह तथ्य है कि सत्याग्रह के दर्शन के रूप में, दुनिया को एक ऐसा शाश्वत सत्य प्राप्त हुआ है जो अव्यवस्था, अनैतिकता, अमानवीयता, अन्याय, अनाचार और अंततः हर प्रकार के अत्याचार का अहिंसक प्रतिरोध पैदा करने में, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में कारगर है। सत्याग्रह के दर्शन और प्रयोग की इस चर्चा का मूल उद्देश्य भारत में समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी व्यक्तित्व डॉ. राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक लक्ष्यों के प्रमुख आधारों की पड़ताल है। साथ ही यह भी देखा जाना है कि आज और भविष्य के भारत में पूँजीवाद तथा कट्टरपंथ की राक्षसी शक्तियों से जनता की मुक्ति के संघर्षों में इस औजार की उपयोगिता कितनी हो सकती है। इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि गाँधी जी की सत्य-अहिंसा केंद्रित राजनीति के वास्तविक उत्तराधिकारी डॉक्टर लोहिया ही थे। जवाहरलाल नेहरु से, जिन्हें गाँधी जी ने स्वतन्त्र भारत का प्रथम नेतृत्वकारी व्यक्तित्व चुना था, उनका मोहभंग भारत विभाजन की राजनीति के चलते पहले ही हो चुका था।
यह भी पढ़ें – लोहिया होते तो राजनीति इतनी क्षुद्र न होती
गाँधी के आदर्श और आचरण से धीरे-धीरे स्खलित होते जाते गाँधीवादियों को डॉ. लोहिया ने उनके चाल चरित्र चेहरे के आधार पर सरकारी, मठी और कुजात श्रेणियों में बांटा। स्वयं को उन्होंने कुजात श्रेणी में रखना पसन्द किया। उनकी श्रद्धा गाँधीजी के उसूलों में थी। पर उससे भी ज्यादा उनके आचरण में। यही वजह है कि केरल में चुनाव जीतकर आई सोशलिस्ट पार्टी की अपनी ही सरकार से इस्तीफा मांगने में उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया, जब थानम पिल्लई की सरकार ने आन्दोलनरत निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाई। गौरतलब है राजनीति में अकपट नैतिकता के पक्षधर डॉ. लोहिया उस समय सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
बर्लिन विश्वविद्यालय से ‘भारत में नमक कानून’ पर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेकर भारत लौटे डॉ. लोहिया ने 1934 में गाँधीजी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मानवीय करुणा के साथ-साथ संतुलित राजनैतिक कर्म के लिए डॉ. लोहिया ने गाँधी जी के सत्याग्रह / सविनय अवज्ञा को सिविल नाफरमानी के रूप में अपनाया। गुलाम और आजाद भारत की भिन्न-भिन्न राजनैतिक परिस्थितियों के ठोस यथार्थ पर सिविल नाफरमानी के हथियार को कसते हुए, उन्होंने जन आन्दोलनों में हिंसा और अहिंसा के सवाल की चुनौतियों से मुठभेड़ किया। नये समाजवादी समाज निर्माण के मद्देनजर डॉ.क्टर लोहिया ने सिविल नाफरमानी की समझ और प्रयोग को परिष्कृत तथा प्रखर बनाया। सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं में उनके विश्वस्त सहयोगी मधु लिमए के अनुसार, ‘डॉ. लोहिया विदेशी अंग्रेज शासन के खिलाफ हथियारों से लड़ने के सिद्धांत का विरोधी नहीं थे। न ही तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल को गलत समझते थे। पर हिंदुस्तान की विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें गाँधीजी का रास्ता ही व्यवहारिक और कारगर प्रतीत हुआ।’
1942 के राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ. लोहिया ने चाहा था कि सिविल नाफरमानी द्वारा जन प्रतिरोध इतना प्रखर हो कि अंग्रेजी शासन की जड़ें उखड़ जाएं। ‘करेंगे या मरेंगे’ की गाँधी प्रतिज्ञा के साथ आन्दोलन में ‘न हत्या – न चोट’ का संकल्प वे अपने लेखों, भाषणों और परिपत्रों में हमेशा दोहराते थे। सरकार की बर्बर हिंसा द्वारा लाठी-गोली से निहत्थे नागरिकों की हत्या के प्रतिवाद के दौरान अन्यायी सत्ता के प्रतीकों, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर उनकी स्पष्ट राय थी की ‘टाइपराइटर मशीनें टूट सकती हैं मगर टाइपिस्ट का सर तोड़ना हिंसा है, अपराध है।’
यह भी पढ़ें – डॉ. लोहिया भारत-रत्न के लिए क्यों अयोग्य हैं?
डॉ. लोहिया की धारणा थी कि स्वतन्त्र और लोकतांत्रिक देशों में बुनियादी परिवर्तन केवल वोट और परंपरागत आन्दोलनों द्वारा संभव नहीं है। वोट एक प्रासंगिक और निश्चित अंतराल पर होने वाला राजनैतिक कर्म है। अन्याय की परिस्थिति में, जिंदा कौमें पांच साल तक प्रतीक्षा नहीं करती हैं। गो सिविलनाफरमानी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में एक कारगर स्थाई चीज है। छोटे- बड़े अन्याय के खिलाफ हर व्यक्ति को इसके इस्तेमाल की स्थाई आदत डाल लेनी चाहिए। कट्टरपंथी और सैनिक तानाशाही शासन के दौरान सिविल नाफरमानी की सफलता पर लोहिया के मन में सवाल थे। मार्क्स ने हिंसा को क्रांति की दाईं (मिडवाइफ) कहा है। प्रसव के अंतिम क्षणों में मां का स्वल्प रक्त क्षरण प्राकृतिक घटना है। गाँधी जी ने भी लिखा है, ‘दुनिया केवल तर्क के सहारे नहीं चलती। जीवन में थोड़ी बहुत हिंसा तो है ही। अतः हमें न्यूनतम हिंसा के रास्ते को अपनाना है ‘(हरिजन, 28-9-1934)।
फ्रांसीसी, रूसी तथा बाद में बांग्लादेश और चेकोस्लोवाकिया की लोक क्रांतियों की प्रारंभिक अवस्था में अहिंसात्मक आन्दोलन ही हुआ। मगर सत्ताधारी वर्ग की हिंसक बर्बरता के खिलाफ, हथियार बाद में आए। बावजूद इसके, डॉक्टर लोहिया का अभिमत था कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य वाले संघर्ष का बहुलांश अहिंसक सिविल नाफरमानी के प्रयोग से ही सफल होगा। अन्याय के विरुद्ध प्रतिवाद और परिवर्तन के उपाय स्वरुप, बीसवीं सदी की दो बड़ी घटनाओं का डॉ. लोहिया हमेशा उदाहरण दिया करते थे : पहला, आणविक शक्ति के विखंडन का हिंसक रास्ता (हिरोशिमा-नागासाकी)। दूसरा, गाँधी जी द्वारा सिविल नाफरमानी का अहिंसक रास्ता, जहां एक अकेला आदमी भी अन्याय, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। इसमें संदेह नहीं, परिपूर्ण दर्शन न होते हुए भी, प्रयोग के रूप में सिविल नाफरमानी की सफलता पर समस्त मानव जाति का परिवर्तनकामी भविष्य निर्भर है।
राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के दौरान जनता ने अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के जो महान सपने गाँधी, भगत सिंह अंबेडकर एवं अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों की आंखों से देखे थे, आजादी के दो दशकों में ही वे लगातार टूटते और बिखरते गये।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश ने विकास का जो पूँजीवादी मार्ग चुना था, उसके गंभीर नतीजे भयावह महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,किसानों की आत्महत्याएं, मुस्लिमों-दलितों-औरतों के प्रति घृणा, द्वेष, हिंसा तथा धर्मांध कट्टरता आदि के रूप में सामने आते गये। यह डॉ. लोहिया जैसे ईमानदार, जुझारू, गहरी राजनीतिक सूझबूझ तथा साहसी चरित्र वाले व्यक्तित्व के लिए ही संभव था कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सपनों को साकार करने में बहुलांशत: विफल नेहरू को संसद से लेकर सड़क तक सवालों के घेरे में खड़ा किया। गौरतलब है नेहरु उस समय अपनी लोकप्रियता के सातवें आसमान पर थे। नेहरू की आलोचना का ऐसा साहस मजबूत विपक्ष साम्यवादी दल ने भी नहीं दिखाया। इतिहास बताता है कि कतिपय साम्यवादी नेताओं के नेहरू और कांग्रेस प्रेम के चलते वाम दल विखंडित होता चला गया। यह तथ्य चिंताजनक है कि वामपंथ आज पचास से ज्यादा पंजीकृत दलों में विभक्त है।
यह भी पढ़ें – आरएसएस समर्थक क्यूँ बने डॉ. लोहिया
नेहरू के दौर से लेकर अपने जीवन के अंत (1967) तक, ‘फावड़ा-जेल-वोट’ की सक्रिय राजनीति के दृढ़चेता व्यक्तित्व डॉ. लोहिया लोकतांत्रिक समाजवाद के अपने वैश्विक आदर्शों पर आधारित वैकल्पिक विश्व सभ्यता का सपना देखते रहे और उसके लिए राजनीतिक संघर्ष करते रहे। उनका कहना था, पूँजीवादी लोकतन्त्र बहुत हद तक धोखा है। उसकी राजनीति भले ही बहुमत की हो, उसका अर्थशास्त्र पूँजीपतियों के हितरक्षक अल्पमत के हाथ में होता है। उन्होंने समाजवाद को दो शब्दों से परिभाषित किया था–समता और समृद्धि। न गरीबी रहे, न विषमता। हिंदुस्तान में व्यापक क्रांति न होने का मुख्य कारण हिन्दू समाज का सदियों तक जाति और योनि के कटघरे में कैद होकर विषमता की संस्कृति को सतत खाद पानी देते रहना था। वे जाति व्यवस्था को सामाजिक कोढ़ मानते थे। उनका मत था, जाति से मुक्ति में ही भारतीय समाज की मुक्ति है। भारत की बहुसंख्यक जनता को गरीबी (वर्ग) और जाति विभाजन (वर्ण) के जुड़वा राक्षसों से एकसाथ अनिवार्यतः लड़ना होगा। भारत के मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की अवधारणा से आगे न जा सके थे। कई ‘ऐतिहासिक भूलों’ और किसान विरोधी सिंगूर-नंदीग्रामी पूँजी हितैषी हिंसक राजनीति के कारण, उनका एक बड़ा हिस्सा जनता में अपनी लोकप्रियता खोता और अविश्वसनीय होता गया। डॉ. लोहिया ने मार्क्सवाद में अहिंसा, लोकतन्त्र, विकेंद्रीकरण और मानव अधिकारों के सवालों को जोड़ने के साथ ही, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और स्त्रियों के विशेष अवसर (आरक्षण) के लिए कठोर संघर्ष किया।
लोकतन्त्र से समाजवाद का रिश्ता शरीर और आत्मा का है। परन्तु आज दुनिया भर में लोकतन्त्र एक छीजती हुई ताकत है पूँजी की शक्तियों के हित में, खरीदी हुई बौद्धिकता के सहारे लोकतन्त्र बहुमत की तानाशाही में बदल चुका है, जिसमें सबाल्टर्न आवाजों के लिए कोई सम्मान नहीं। आज नागरिकता कानून के विरोध की शाहीनबाग आवाज और विगत कई महीनों से काले कृषि कानूनों के विरुद्ध मुकम्मल गाँधीवादी साहस और समझदारी से सत्याग्रह कर रहे, किसानों के साथ देश की केंद्रीय सत्ता का क्रूर और कठोर सुलूक इसी बात की पुष्टि करता है।
हिंसा, भ्रष्टाचार, घृणा-द्वेष और जुमलेबाजी के दलदल में धंसी भारतीय राजनीति आज अपने निकृष्टतम बिंदु पर है। वह समस्याओं का समाधान करने की बजाय स्वयं एक समस्या बन चुकी है। राजनीतिक दलों को संदेह की नजर से देखा जाता है और नेताओं को घृणा की नजर से। समाज में त्याग, आत्मनिर्भरता, इमानदारी, भाईचारा, परोपकार, सादगी एवं सदाचार का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। इसकी जगह उपभोक्तावाद, परजीविता, स्वार्थपरता, कपट, असहिष्णुता, उद्दंडता तथा भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़े हैं।
यह भी पढ़ें – लोहिया आन्दोलनकारी थे या आन्दोलनजीवी?
सच, कर्म और प्रतिकार वाले चरित्र के साथ निजी और सामाजिक जीवन में डॉ. लोहिया सादगी, त्याग, ईमानदारी और सहिष्णुता के मूर्त पक्षधर थे। उन्होंने अपने समाजवादी आदर्शों को साकार करने के लिए जो पार्टी बनाई उसका अनुशासन बड़ा कड़ा था और वे उसे सख्ती से लागू करते थे। अपने साथियों से नीति, नीयत और आचरण में एका की अपेक्षा रखते थे। मगर पद और सुविधाओं की चाह के कारण उनके दल में टूट-फूट चलती रही। ‘सुधरो अथवा टूटो’ की उनकी सीख पर न चल सकने के कारण, उनके निधन के बाद उनकी पार्टी बिखरती गयी।
अपने तार्किक विचारों और दृढ़ स्पष्टवादिता के कारण वे न सिर्फ अपने ही कुछ साथियों के वरन कांग्रेस, जनसंघ (समप्रति भाजपा – संघ) और कम्युनिस्ट आदि दलों की भी आलोचना के निशाने पर हमेशा रहे। गैर-कांग्रेसवाद, कट्टर हिन्दूत्व विरोध, आदिवासी,दलित, स्त्री और मुस्लिमों के लिए आरक्षण का समर्थन तथा कम्युनिस्टों की हिंसा, सत्ता भोग और कांग्रेस-प्रेम की आलोचना सम्बन्धी उनके विचार उसी श्रेणी के थे। मगर उनकी छवि कभी म्लान नहीं हुई। राजनीतिज्ञों में ज्ञानात्मक संवेदना वाले अप्रतिम बौद्धिक के रुप में और बौद्धिकों के बीच सादगी, त्याग, ईमानदार, मित्रसुलभ चरित्र वाले जमीनी राजनेता की उनकी छवि में कोई मिलावट नहीं थी। अपने दौर के असंख्य बौद्धिकों को उन्होंने समाजवाद की राजनीति में प्रवृत किया था।
वैश्विक पूँजीवादी सत्ताओं के केंद्रीकृत शोषण के खिलाफ डॉ. लोहिया की ‘चौखंभा-राज’ की अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता और समानता के लिए वास्तविक विकेंद्रीकरण की ठोस समझ पर आधारित है। सप्तक्रांति के रुप में भारत ही नहीं, विश्व की अधिकांश समस्याओं के समाधान की संवेदना और तर्क प्रणाली उनके पास थी। उन्होंने जिन सात क्रांतियों का आह्वान किया था वे हैं –
1) नर नारी की समानता के लिए
2) चमड़ी के रंग पर रची राज्य की आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ
3) संस्कारगत, जन्मजात जातिप्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए
4) परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतन्त्रता तथा विश्व लोक-राज के लिए
5) निजी पूँजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए
6) निजी जीवन में अन्याय हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्री पद्धति के लिए तथा
7) अस्त्र-शस्त्र के खिलाफ और सिविल नाफरमानी के लिए।
डॉ. लोहिया ने सही कहा था, संपूर्ण दुनिया में समता और समृद्धि स्थापित होने तक, ये सातों क्रांतियां विश्व भर में चलनी चाहिएं। वे चलती रहेंगी। उत्तर रामायण के लेखक भवभूति की तरह डॉ. मनोहर लोहिया भी कहते थे, आज मेरी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, पर भविष्य में वे अवश्य सुनेंगे।
.