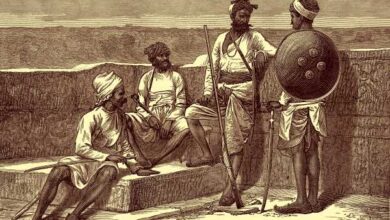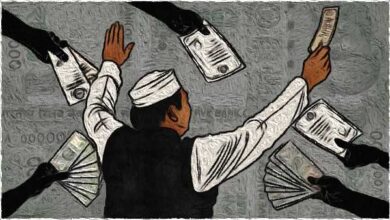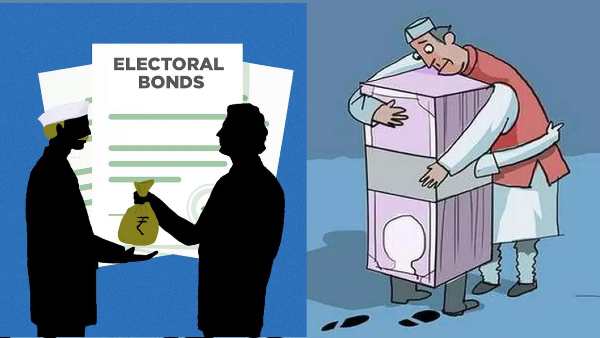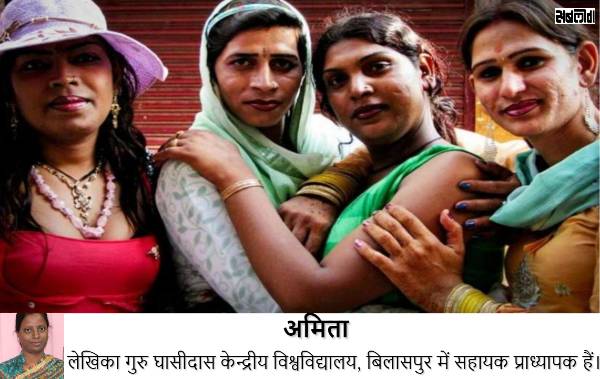
व्यवस्था के मारे किन्नर
समाज अथवा देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम-कानून या व्यवस्था आवश्यक होता है। किन्तु किसी भी समाज में व्यवस्था को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि व्यवस्था सही न हो तो आम जनता को जीवन के हर मोड़ पर कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इनके लिए जीवन गुजरना किसी तपस्या से कम नहीं होता। काफी लम्बे समय से ट्रेन तक में यात्रा करना भी आम जनता पर भारी पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोरोना महामारी के बाद समस्या का स्वरूप बदल गया है। जहाँ एक ओर रेलवे प्रशासन (सरकार) अभिजात्य वर्ग को ध्यान में रखकर रेलवे में विभिन्न सुविधाएँ मुहैया कराता है वहीं सामान्य जन को अधिकांश सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। भोजन आम जनता के लिए बहुत महंगा है, जनरल डिब्बे, आरक्षित और वातानुकूलित डिब्बों से कम होते हैं, जिसमें गरीब जनता भेड़-बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर रहते हैं।
अनारक्षित डिब्बे में बैठने की जगह तो दूर, खड़े रहने तक की भी जगह नहीं मिलती। ऐसी समस्याएँ त्योहारों और छुट्टियों के दौरान और भी बढ़ जाती है। लोग एक-दूसरे पर गिरते-पड़ते और धक्के खाते अपने गन्तव्य तक पस्त हाल में किसी तरह पहुँच जाते हैं। गरीब यात्री यह सब कुछ झेलने को मजबूर होते हैं। ऊपर से किन्नरों का आतंक। इन्हें देखते ही अधिकांश लोगों के चेहरे पर भय का भाव स्वत: प्रकट होने लगता है। कई बार तो यहाँ तक देखा जाता है कि रेलवे प्रशासन और पुलिस का भी सहयोग किन्नरों के इस कार्य में प्राप्त होता है, क्योंकि, किन्नरों द्वारा वसूल किए गये पैसे का लाभ इन्हें भी तो मिलता है। इस तरह अधिकांश किन्नर मजबूरी में ऐसी हरकतें करने को बाध्य होते हैं, जिससे वे पैसा कमा सकें। ऐसी स्थिति के बीच गरीब पीसते हैं और वे ‘बली का बकरा’ बनने को मजबूर हो जाते हैं। 

ऐसा अक्सर होता रहा है कि किन्नर, जिनके प्रति लोगों के मन में एक विशेष प्रकार की सहानुभूति होती है, वे ट्रेनों में चढ़कर जबरदस्ती लोगों से पैसा वसूलते हैं, खासकर पुरूष वर्ग से। एक बार जब मैं बिलासपुर-पुणे एक्सप्रेस के सामान्य डिब्बे में सफर कर रही थी, तब कुछ अजीब नजारा देखने को मिला। डिब्बा पूरी तरह से यात्रियों से भरा हुआ था। खड़े होने की भी जगह बहुत मुश्किल से मिल पा रही था। टी.टी. अपने दाने-पानी के चक्कर में मुर्गा तलाश रहे थे। अंतत: उन्हें मुर्गा मिल ही गया, जिसके पास एक्सप्रेस का टिकट था और वे सुपरफास्ट में बैठे थे। टी.टी. उनसे वसूली करने में सफल भी रहे। फिर अचानक सबके चेहरे पर एक डर सा दिखा। कुछ छत्तीसगढ़ी महिलाएँ बोल रही थी, ‘आवत हे-आवत हे’(आ रहे हैं-2)।
मैंने उन महिलाओं से पूछा क्या हुआ? आप लोग इतनी डरी हुई क्यों हैं? कौन आ रहे हैं? तभी उनमें से एक महिला ने कहा ‘छक्के’(किन्नर)। फिर क्या किन्नरों का हुजूम उस डिब्बे में चढ़ा और वे लगे अपना तमाशा दिखाने। महिलाएँ लगातार बोलती रही कि हम बहुत गरीब हैं। ये हमारे लड़के हैं, इन्हें छोड़ दो। हम नागपुर कमाने जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ ऑटो भाड़ा है। खाने तक को पैसे नहीं हैं तो हम आपको कहाँ से दे? फिर भी किन्नर नहीं माने। तब लड़कों ने दस-दस रुपये निकालकर उन्हें दे दिये लेकिन किन्न्रों ने कहा- दुर्गा की पूजा करनी है, बीस रूपये से कम नहीं लूंगी और बीस रूपया लेकर ही माने। खैर ट्रेन दुर्ग पहुँच गयी थी और किन्नरों का जत्था नीचे उतर गया था।
नीचे उतरने के बाद किन्नरों के कई जत्थे आपस में मिल-जुल रहे थे। लोगों ने ये सोचकर राहत की सांस ली कि चलो बला टली। लेकिन जैसे ही ट्रेन खुली किन्न्रों का दूसरा जत्था फिर से ट्रेन में चढ़ गया और वसूली शुरू कर दी। सब आपस में बोल रहे थे कि फिर से इन्हें पैसे हम कहाँ से देंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तभी दो किन्नर आयें और लड़कों को गंदी-गंदी गाली देते हुए कहने लगे- निकाल बीस-बीस रूपये। लड़कों ने कहा अभी-अभी तो दिया है, अब कहाँ से दे? फिर गाली देते हुए किन्नरों ने कहा “निकाल बीस रुपये जल्दी, वो हिजड़े थे, तो क्या हम हिजड़े नहीं हैं? निकाल पैसे।” परंतु लड़कों के पास पैसे नहीं थे, तो वे कहाँ से देते? फिर क्या था, ये किन्नर लगे अपने कपड़े उतारने। इस पर भी जब लड़कों से पैसा नहीं मिला, तब किन्नरों के जत्थे एकजुट होकर लड़कों को मारना शुरू कर दिया और जब मारते-मारते थक गये तो कहा- आइंदा बिना पैसे के ट्रेन में दिखा तो ट्रेन से बाहर फेंक दूंगी। इस तरह एक जत्थे का उतरना और दूसरे जत्थे का चढ़ना लगातार बना रहा। यात्रियों ने बताया, यह कोई नयी बात नहीं है। यह रोज का तमाशा है। 

इतना होने के बावजूद प्रशासन के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती। किन्नर जिसे एक कमजोर (दुर्बल) तबके के रूप में देखा जाता है। आज वे प्रशासन के सह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और इस गुंडागर्दी का सामना सिर्फ भोली-भाली गरीब जनता को ही रोज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग वातानुकूलित डिब्बे में घुसते नहीं, और आरक्षित कक्षों में भी बहुत कम घुसते हैं और घुसते भी हैं तो डर से इस तरह का व्यवहार नहीं करते। किन्नरों के द्वारा इस तरह के हथकंडे/व्यवहार अपनाने का क्या कारण हो सकता है? जो कल तक सहानुभूति और भीख माँग कर रहने को मजबूर थे उनका ये रूप क्यों? ऐसी हालात के लिए कौन जिम्मेदार हैं? वह जनता जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है या फिर ये किन्नर जो कुदरत की देन का दुरूपयोग कर गरीबों का शोषण कर रहे हैं, या फिर सरकार जो इनके (किन्नरों) के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है? या फिर वे नेता जो दलित, महिला और पिछड़े वर्ग के लिए तो आरक्षण की माँग कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा तबका इसमें शामिल हैं, जिनके वोट से सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन इस वंचित तबके से सत्तासीन लोगों को शायद ही कोई फायदा मिल सकता है।
लक्ष्मी त्रिपाठी जी, जो खुद भी किन्नर समुदाय से सम्बन्ध रखती हैं, उन्होंने किन्नरों की इस समस्या पर अपनी किताब ‘मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी’ में भी प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि प्राचीन काल से ही किन्नरों का एक विशेष महत्व रहा है। रामायण, महाभारत काल में भी किन्नर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। “प्राचीन काल में भी उन्हें सम्मान मिलता था, समाज में उनकी मान्यता थी। बहुत से राजाओं के दरबार में हिजड़ों ने कूटनीति की है, ऐसा उल्लेख है। मतलब राजनीति में भी हिजड़े साझीदार थे। संघराज्य के समय जागीदार हिजड़ों से सलाह लेते थे। बाद में मुसलमान राजाओं ने हिजड़ों की ‘खोजे’ के रूप में जनानखाने पर निगरानी रखने के लिए नियुक्ति की। हिजड़ों की ताकत, शौर्य का इन राजाओं को इल्म था और भरोसा भी था। राजशाही में हिजड़ों को अलग-अलग रूप में रोजगार मिलता था, इसलिए गरीब लोग अपने परिवार के लड़के का लिंगछेद करके उसे हिजड़ा बना देते थे और उसकी कमाई पर पूरे परिवार का गुजारा चलाते थे। यह भी कुछ भी कुछ जगहों पर लिखा गया है। हिजड़ों में अलग-अलग ओहदे होते थे। ‘ख्वाजासारा’ उनका प्रमुख, और उसके नीचे अन्य सब होते थे। ये ‘ख्वाजासरा’ कप्तान का काम करते थे। उसका हुक्म सब बजाते थे। लेकिन औरंगजेब के शासन काल में लिंगछेद पर रोक लगाई गयी।” इस तरह किन्नरों को बेरोजगार करने की पहल कर दी गयी। 

आगे इसी किताब में वे उल्लेख करती हैं कि “वात्सायन के ‘कामसूत्र’ में ‘तृतीय प्रकृति’ कहकर हिजड़ों का उल्लेख मिलता है। वे स्त्री अथवा पुरूष किसी के कपड़े पहन सकते थे, ऐसा उसमें कहा गया है। वात्स्यायन ने और शेष बहुत से पंडितों ने उन हिजड़ों को ‘नायिका’ कहा है। कोई राजकुमार या किसी सरदार का पुत्र काम-क्रीड़ा में कमजोर हो तो उसे सिखाने के लिए हिजड़ों की नियुक्ति की जाती थी। अठारहवीं शताब्दी में राजशाही खत्म हुई। राज, सरदार बचे नहीं। फिर हिजड़ों को कौन काम देता और क्या? उनके जीने के रास्ते खत्म हो गये। उनमें बहुत सी कलाएँ थी। उन्हें नाच-गाना आता था। सिर्फ आता था, ऐसा नहीं है, उसमें वो प्रवीण थे।
अंत में पेट भरने के लिए वे सड़कों पर आ गये और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भीख माँगना शुरू किया। कुछ हिजड़े नवजात शिशुओं को बधाई देती रहीं। नव-दंपत्ति को वो आशीर्वाद देते रहे। पर ये काम कितने लोग कर सकते थे? कुछ लोग शरीर बेचने लगी। उनके पास कोई चारा नहीं था, दूसरा रास्ता ही नहीं था। समाज ही उन्हें कुछ करने नहीं देता, और कुछ करें, तो उसे रिस्पांस नहीं देता। ऐसी ही आफत में हिजड़े फंसे थे। फिर वे और ज्यादा अलग होते गये, उसी से अधिक आक्रामक भी होते गये। लोग उनसे डरने लगे। डर के मारे भी भीख मिलती है, इसलिए हिजड़ा न होते हुए भी कई लोग साड़ी पहनकर भीख माँगने लगे। भीख न देने पर दादागिरी, मारमीट भी करने लगे। समाज में उनकी छवि और खराब होने लगी। समाज उनसे दूर रहने लगा और वो भी उनसे दूर जाने लगे। इसे रोकने के लिए किसी ने खास कोशिश की हो, ऐसा सुनने में, पढ़ने में, देखने में भी नहीं आता।” लक्ष्मी त्रिपाठी जी ने किन्नरों के दर्द को अपनी आत्मकथा के माध्यम से बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। किन्नरों की वर्तमान स्थितियों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। सरकारी अनदेखी का भी उल्लेख किया है। उनकी कोशिशों से कई अच्छी पहल भी किन्नरों के भलाई के लिए शुरू हुई।
21वीं सदी के युग में भी भारत जैसे देश में किन्नर आज भी एक हाशिए का वर्ग है, जिसकी हर तरफ उपेक्षा की जाती है। इन्हें रोजगार की सुविधा, समानता नहीं दी जाती है। आज भी यह समुदाय अपने लिए अलग प्रसाधन तक की माँग करते देखे जा सकते हैं। आज भी शैक्षणिक संस्थानों में अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इन्हें जो अधिकार दिए भी गये हैं, तो वे भी सिर्फ कागजों पर। इनके अच्छे व्यक्तित्व अथवा गुणों और कार्यों को कभी भी तवज्जों नहीं दिया जाता है। व्यावहारिक स्तर पर आज भी यह वर्ग वहीं खड़ा है, जहाँ से इन्होंने चलना प्रारम्भ किया था। अत: जब तक इनके सम्मान और अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक इन्हें तमाम तरह के असामाजिक कार्य अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा।
.