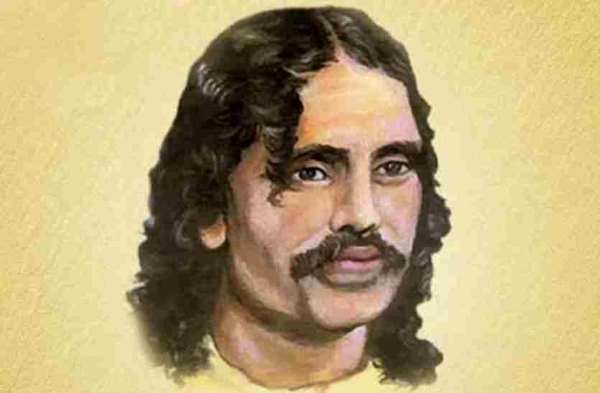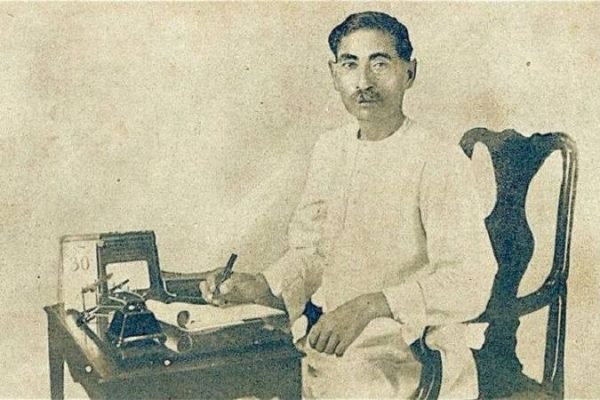‘ना उम्मीदी के बीच’ कहानी में बाल विमर्श का अस्तित्व
“वर्तमान दौर विमर्शों का हैं उसमें फिर आदिवासी विमर्श हो या किन्नर विमर्श, स्त्री विमर्श हो या दलित विमर्श सभी पर साहित्य के माध्यम से खूब चर्चा, परिचर्चा, बहस चल रही हैं फिर बाल विमर्श अछूता क्यों रहें। बाल विमर्श को कटघरे में खड़ा करना मतलब समूचे समाज को घेरना होगा। क्योंकि बच्चें स्वयं अपनी समस्या रख नहीं सकते यकीनन यहीं कारण कि इस विषय पर चर्चा आज भी और विमर्शों की तुलना में कम हैं, इस विषय पर अध्ययन करना ना केवल बड़ों के लिए अपितु बच्चों के लिए भी अनुरंजन होगा। प्रचीन समय से गांवों में पानी के लिए कुएं और तालाब ही साधन रूप में रहें हैं। तालाब के किनारे कपड़े धुलना और मछलियां पकड़ना बच्चों के लिए आम बात हैं, तालाब में कंकड़ फेक कर मछलियों को मारना और उन्हें रानी कह कर छेड़ना, फिर गुनगुनाते हुए कविता पाठ करना–
‘मछली जल की रानी है
जीवन उसका पानी है
हाथ लगाओ डर जाएगी
बाहर निकालो मर जाएगी
हा हा हा।‘
ये सब मस्ती और अठखेलियां आजाद भारत के कुछ वर्षों तक गाँव के बच्चों ने खूब किया किन्तु परिवर्तन समय का नियम हैं और इसी परिवर्तन में जो मछलियां कल तक आपने जलाशय की रानी थी आज वहीं पट्टों के रसूखदार की कैदी सी हो गयी हैं जिसे अब कोई बच्चा कंकड़ नहीं मारता, ना असमय मिलने, टहलने जाता हैं वहाँ। इसी परिवर्तन का जिक्र कथाकार डॉ सुभाष चन्द्र कुशवाहा की कहानी –‘ना उम्मीदी के बीच’ में हमें बखूबी देखने को मिलती हैं नायिका सात वर्ष की ‘मुन्नी’ और उसके दोस्तों के माध्यम से।
मुन्नी तीन भाई बहनों में सबसे छोटी, नटखट और चंचल हैं उसका मन मछलियों की तरह ही बेचैन हैं और बचपन घिरा हुआ हैं। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, कटोरा लेकर जाती हैं, मिड–डे मील की खिचड़ी खाती हैं, ‘वन्दे मातरम्! वन्दे मातरम्’ गाती हैं, जो प्रार्थना – सभा से सीखी हैं, घर से खेत, खेत से तालाब खूब सैर लगाती हैं। परन्तु एक दिन मुन्नी की चमकती आँखों में तालाब की एक मछरी ने हलचल मचा दी, भून कर उसे खाने की। किन्तु तालाब रसूखदार का था मुन्नी उसे निकाल कर बेच कर पैसे दे सकती थी रसूखदार को लेकिन बिना पैसे के खा नहीं सकती थी ..
किन्तु मुन्नी की आंखों का कौतूहल देखने लायक था, उस दिन मछली को लेकर अपने दोस्तों से मुन्नी ने जितना प्रतिवाद किया यकीनन उस उम्र के बच्चे उतनी दलील नहीं दे पाते। कहते हैं ना गरीबी समय से पहले ही अनुभवी और प्रतिवादी बना देती हैं। वास्तव में गरीबी में पला/ बढ़ा बच्चा बाहर से जितना बच्चा होता हैं भीतर से वह उतना ही बड़ा और समझदार होता हैं। इस कहानी कि मुन्नी की मासूमियत भी ऐसी ही हैं जो अपने आप को बहुत संयमित करती हैं किन्तु घड़ी–घड़ी उसका मन मछली खाने के लिए मचल उठता हैं और वह अपना धैर्य खो देती हैं ..बाल मन की जिज्ञासा को लेखक ने जिस तरह से यहाँ सजीव चित्र खींचा हैं वह बाल अस्तित्व पर कई सवाल खड़े करता हैं और अपने बड़ों से, समाज के रसूखदारों से कई तरह के जवाब मांगता हैं !
एक संवाद कहानी में आता हैं जब मुन्नी अपने मछरी खाने की इच्छा का दमन करती हैं कहती हैं–
” ‘मुन्नी’! चन्नों ने मुन्नी की पीठ पर हाथ फेरते हुए पुकारा हैं।
‘ ए ‘…! “मुन्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी हैं जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गयी हो। जल्दी–जल्दी आँसुओं को पोछने लगी हैं मुन्नी।” परतहिया की मछरी खाओगी?….छी!”
“नहीं तो। मैं … मैं काहें खाऊॅ॑ परतहिया की मछरी? तुम ही खाओ।”
“मुझे नहीं खानी गन्दी मछरी।”
इस तरह झूठ का सच और सच का झूठ ओढ़े बचपन, हम उम्रों के बीच अपनी गरिमा बचाने की कोशिश कर रहा था तीनों के चेहरों का बचपना मुरझाया हुआ था। फिर भी चन्नों ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, “चलों टीवी देखने चलें।”
इस संवाद में बच्चे अक्कड़– बक्कड़ खेलने की उम्र में अपनी स्वाभाविक इच्छाओं का दमन कर रहें हैं वह भी तालाब की मामूली सी मछरी के लिए जो कि बहुतायत मात्रा में बरसात के मौसम में गांवों के तालाबों में पाई जाती हैं फिर भी मुन्नी जैसे ना जाने कितने बच्चें आज अपने इस स्वाभाविक इच्छा का दमन कर रहे हैं उसका एक मात्र कारण हैं – वर्तमान समय में गाँव के सार्वजनिक तालाब का एकीकृत तालाब (सरकारी पट्टा) होना हैं।
जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि पर पता नहीं कितना न्याय संगत हैं किन्तु इस तरह के सरकारी हस्तक्षेप से गांवों का बचपन भी सिकुड़ने सा लगा हैं जिसमें बच्चें मिट्टी से ज्यादा ईट, पत्थरों पर खेलने लगे हैं ..उससे उनमें थोड़ी स्वच्छता तो आ गयी हैं पर आत्मबल बहुत कमजोर सा हो गया, प्रभाव हैं मनोवैज्ञानिक उसका क्योंकि डर के साथ ही पहला पांव उसने रखा ईट पर ..। ‘वन्दे मातरम् ! ‘का तीव्र स्वर भाव तो हैं पर उनमें सुभाषचन्द्र बोस और भगतसिंह जैसा प्रेम भाव नहीं हैं कारण हैं– टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने देशभक्ति की गाथा को देखा तो किन्तु ! कहानियों में सुना नहीं, कल्पना में जिया नहीं। यहीं कारण हैं कि आज के बच्चें जानते तो सब हैं किन्तु समझते कुछ खास नहीं।
यह भी पढ़ें- लोककथा और बाल साहित्य
वास्तव में देखा जाए तो यह दौर बच्चों को भरमाने की कला का हैं ! अस्तित्व की खोज कौन करें ?
अब बाल मन कल्पना नहीं करता, जो कल तक बड़ों का हुनर था खुशियों को गोपनीय रखने का, इच्छाओं को दमन करने का अब वह कला बच्चों ने सीख ली हैं बच्चें वाकई आजाद भारत में हैं।किन्तु मुन्नी के व्यवहार की गुत्थी सुलझाने में उसकी माई आज तक उलझी हुई हैं। जो बाग–बगीचे, नदी–तालाब, पशु पक्षी, पेड़– पौधें कल तक बच्चों का कुटुंब था आज उसकी जड़ें बहुत कमजोर हो गयी हैं इसे एक सूत्र में बंधा हुआ देखना ही –” ‘ना उम्मीदी के बीच’ मुन्नी के मुस्कुराने जैसा ही हैं।।