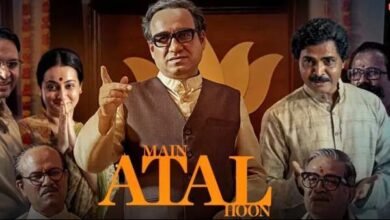समसामयिकता में ऐतिहासिक सद्भावना
(संदर्भ: अविनाश दास की फिल्म ‘इन गलियों में’)
भारत में समाजोन्मुखी सिनेमा की एक लम्बी परम्परा रही है। राज कपूर और ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्मों में समाजवाद का पाठ पढ़ कर आज़ादी के बाद की एक नस्ल तैयार हुई थी। तकनीक की क्रान्ति के साथ श्याम बेनेगल, गोविंद निलहानी आदि ने यथार्थपरक फिल्मों की जो ठोस बुनियाद रखी, उसने मसाला फिल्म के समानांतर एक मजबूत लकीर खींची थी। लोकप्रिय आख्यान के सामने रचनात्मक मानस की तेजस्विता ने वैकल्पिक सिनेमा को समुचित आदर दिया। शायद इसी लिए इस माध्यम के बड़े चेहरे धारा से अलग चलते हुए भी सम्मान पाने में किसी से पीछे नहीं रहे। ऐसे निर्देशक और कलाकार अपना अस्तित्व और अपने सम्मान की रक्षा करने में सफल रहे वरना सत्यजीत रे, मृणाल सेन, उत्पल दत्त, शयाम बेनेगल, गोविंद निहलानी, नसीरुद्दीन शाह, सईद जाफरी, शबाना आजमी, ओमपुरी आदि हमारे इतिहास के गुमनाम किरदार बन कर हमारी स्मृतियों से निकल चुके होते।

युवा निर्देशक अविनाश दास की नयी फिल्म ‘इन गलियों में’ जब रिलीज हुई तो बहुत तरह की अपेक्षाएँ भी पैदा हुईं। उन्होंने अपनी पिछली फिल्म ‘अनारकली ऑफ आरा’ से जो उम्मीदें पैदा की थीं, दर्शकों को उनसे एक नयी और बेहतर फिल्म का इंतजार भी था। उनकी छोटी बड़ी कोशिशें कुछ अन्य माध्यमों पर नजर आयीं मगर एक भरपूर काम का सबको इंतज़ार था। अति लोकप्रिय और स्टारडम से लैस फिल्मों में अविनाश दास की वैसी रूचि नहीं है जिससे ये उम्मीद की जाए कि वे बाजार के हिसाब से कोई बड़ा काम करने का इरादा रखते हैं। उन की पिछली फिल्म से यह बात भी समझ में आने लागी थी कि वे कलावादी फिल्मों का रास्ता भी नहीं चुनेंगे। निर्देशक की हैसियत से उन की असली परीक्षा यही रही कि वे मसाला फिल्मों से भी दूर रहे और दर्शकों से निरपेक्ष हो कर अपने मन की तरंग में डूबी फिल्में बनाने से भी उन्होंने खुद को दूर रखा। कहना चाहिए कि उन्होंने किसी बीच के रास्ते की कल्पना कर के अपनी रचनाशीलता को आजमाने का निशाना रखा।
फिल्म की इस नयी जमीन की तलाश में उनके लिए कुछ आसानियाँ भी थीं। छोटे बजट की फिल्म बनाने में स्टार कास्ट के लिए सीमित अवसर हो सकते हैं। आडम्बरों से भरे बड़े-बड़े लोकेशन के लिए भी छोटे बजट में कम ही गुंजाइश होती है। बड़े स्टार और अचंभित करने वाले भव्य सेट बनाने से वे स्वतः अलग होते गए। अब उन के पास बिखराव के बहुत सीमित कारण थे। उन्होंने साधन की सीमा को अवसर में बदलने का टारगेट रखा। सामान्य कहानी और आसपास की जिन्दगी के जाने-अनजाने और आम तौर से गली-मुहल्लों में बदलती हुई जिन्दगी के कुछ निशान उन्हें तलाश करने थे। अविनाश दास ने इन सब कामों को करते हुए यह कोशिश की कि उसी घर-आँगन में हमारा इतिहास, वर्तमान, भविष्य सब-कुछ झलक जाए। इसी के साथ वह देश और विश्व भी अपने बदलते हुए माहौल के साथ दिखा पाने में सक्षम रहे हैं।
अविनाश दास ने पूरी फिल्म को अपनी मुट्ठी में कैद रखा है। कहना चाहिए कि यह पूर्णरूपेण निर्देशक की फिल्म है। शायद इसी लिए न कभी कहानी में बिखराव आता है और न कभी किसी मोड़ पर कोई चरित्र फिल्म को अपनी राह पर ले जाने के लिए विवश करता है। जावेद जाफरी जैसा मँझा हुआ कलाकार भी अपनी छाया में विवान शाह, अवन्तिका दसानी जैसे नये कलाकारों को निर्मूल नहीं बना देता। सब के लिए निर्देशक ने एक तयशुदा मौका रखा है और उसी धुरी पर सब किरदार चलते-फिरते और जीते नजर आते हैं।

कहने को स्वर्गीय वसु मलवीय की कहानियों पर आधारित यह फिल्म है और अपने पोस्टर पर यह उद्घोष करती है कि यह ‘नये दौर में आपसी भाइचारे की कहानी’ है। ‘भाईचारा’ शब्द पर उर्दू के चर्चित हास्य-व्यंग्य कवि मरहूम असरार जामई की बात याद आती है कि ‘हम उन्हें भाई समझते हैं और वह चारा हमें’। 2024-25 में घोषित कर के ‘भाइचारे’ पर फिल्म बनाना अविनाश दास ने इस लिए भी तय किया होगा कि इतिहास में बदलते हुए भारतीय समाज की एक आखिरी निशानी सुरक्षित कर ली जाए जिससे आने वाली पीढ़ी को विश्वास हो सकेगा कि हमारा देश किताबों-कहानियों से अलग भी भाइचारे का जीवन जीता था। बदलते हुए भारतीय समाज की कहानियों पर आधारित इस प्रकार की फिल्मों की सदैव जरूरत से इनकार करना मुश्किल है।
फिल्म का नाम बड़ा सामान्य सा है –‘इन गलियों में’। शहर, देश और विश्व का कोई दावा नहीं। कमाल तो यह है कि इन्हीं दो गलियों से यह कहानी शुरू होती है और वहीं खत्म भी हो जाती है। ‘हनुमान गली’ और ‘रहमान गली’ के नाम भी स्पष्ट करते हैं कि किस तरह कहानी बुनी जाएगी। स्वभाव से शायर और पेशे से चाय बेचने वाले मिर्जा यानी जावेद जाफरी की दुकान पर आकर दोनों गलियाँ मिल जाती हैं। यह मुहल्ले का अड्डा भी है। पास में शब्बो और हरिया की सब्जी की दो अलग अलग दुकानें भी हैं। लोकेशन इतना सादा है कि कभी कभी महसूस होता है कि इसे हम सिनेमा के पर्दे पर शायद नहीं देख रहे हैं। उसी तरह वेशभूषा भी इतना सामान्य है कि विश्वास नहीं होता कि ऐसे में हमारी जिन्दगी से पर्दे पर यह कहानी कैसे चली आई। सब से चर्चित कलाकार जावेद जाफरी हैं मगर वह इतने सामान्य तरीके और उतने ही सामान्य अन्दाज से फिल्म को सम्भाले रखते हैं।

शब्बो और हरिया की प्रेम-कहानी आरम्भ से अंत तक फिल्म में चलती रहती है। निर्देशक ने तो जरूर तय कर रखा था कि उसे इन गलियों में जन्म लेने वाले पात्रों की प्रेम-कहानी लिखनी है, इस लिए मसाला फिल्मों का एक छौंक भी यहाँ आने नहीं देता। इस मामले में निर्देशक और सम्पादक इतने निर्मम हैं कि आरम्भ से अन्त हो जाता है मगर शब्बो को अभिनेत्री की चमक दमक में घिरने ही नहीं देते। पूरी प्रेम कहानी में तथाकथित एक भी इंटीमेट सीन नहीं है। कोई जरूरी-गैर जरूरी मांसलता भी नहीं है। प्रेम के किसी भी एक दृश्य पर सस्ती ताली बजने की कोई सम्भावना भी नहीं है। निर्देशक का कमाल यह है कि उस ने भाइचारे की एक प्रेम कहानी उत्सर्जित की है। अविनाश दास ने ठेले पर सब्जी बेचने वाले दो पड़ोसी बच्चों की पनपती हुई प्रेम कहानी में कभी कटहल काट देने, कभी सब्जी तौल देने, कभी बड़े नोटों के खुदरा करने जैसे कामों से प्रेम-सम्बन्धों को आकार देने की कोशिश की है। कभी माँ का व्यवधान, कभी समाज की नजर और इन सब से जूझते हुए इन प्रेमी जोड़ों को मिर्जा के सुझाव और सहयोग मिलते रहते हैं।
विवान शाह के चरित्र में थोड़ी सी चमक दमक जरूर शामिल की गयी है मगर इसी के सहारे उसके व्यक्तित्व में जोर और शक्ति भी पैदा हुई है वरना धर्मों की मान्यताओं से आगे जाकर इस प्रेम को वह मुखरता प्रदान न कर पाता। शान्त स्वाभाव और मरी-बंधी शब्बो के विपरीत हरिया में अगर उतावलापन न आता तो इस प्रेम कहानी की कभी शुरुआत ही नहीं हो सकती थी। लेकिन यह उतावलापन कभी निर्देशक के दायरे में आकर दूसरी फिल्मों की तरह मांसलता का प्रतिरूपण नहीं करता। फिल्म देखते हुए निर्देशक ने हमें अवसर दिया है कि एक नये पनपते हुए प्रेम को सामाजिक सहयोग, जीवन-यापन की जिम्मेदारियों और वायु-तरंगों से पहचानें। ऐसे सच्चे प्रेम हमारे जीवन से उठते चले गए। अब मासूम भावनाओं को उकेरती हुईं सामान्य कविताएँ और कहानियाँ भी कम मिलती हैं। फिल्मों के बारे में तो शायद कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता। अविनाश दास ने प्रेम की नैसर्गिकता और वास्तविकता को इस फिल्म में बड़ी मेहनत और कलात्मकता से बचाने में सफलता पाई है। प्रेम हमारे जीवन में, हमारे घरों में कहीं अंदर से फूटता है और बाहर के अँधेरों को रौशन करता है, निर्जीव को सजीव बनाता है और दुर्बल को सबलता प्रदान करता है। अविनाश दास ने इस फिल्म के मुख्य पात्रों के जीवन से यह स्पष्ट कर दिया।

फिल्म की कहानी सामान्य है और आज के दर्शक के लिए यह मुश्किल नहीं कि आरम्भ में ही वह अन्त तक की परिस्थितियों को समझ ले। सामाजिक बन्धन और उसकी चुनौतियों का ऊबड़-खाबड़ जो हमारे दिमाग में है, अविनाश दास ने वैसी ही कहानी इस फिल्म के लिए चुनी। उन के लिए यह कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा कि जानी-समझी सामाजिक कहानी को वह क्यों उसी अंदाज से कह रहे हैं? ये कहानी भारतीय समाज की वही पुरानी कहानी है जिसे नये नये संदर्भों में हम रोज देखते रहते हैं। अविनाश दास को भी किसी नयी और चौंकाने वाली कहानी सुनाने में कोई बहुत रुचि नहीं है। उनके लिए चुनौती यह है कि भाइचारे की उसी कहानी को दर्शक नये सिरे से उन के साथ-साथ देखने और सुनने के लिए मजबूर हो जाएँ।
अविनाश दास ने समाज के बीच समझदार और नासमझ, अच्छे और बुरे, स्वार्थी और निस्वार्थ भाव से जीने वाले हर तरह के चरित्रों को पहचानने की कोशिश की है। अंतर-धार्मिक प्रेम को दिन-प्रतिदिन के सामाजिक माहौल में बड़ी मेहनत से सफलता की मंजिलों तक पहुंचाया है। साम्प्रदायिक सद्भाव का ताना-बाना रह रह कर टूटता बिखरता है और फिर उसी समाज में लोगों की सूझबूझ से फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। यह राजकपूर के काल की आशावादिता नहीं है वरना मिर्जा को अपनी जान गँवाने के लिए निर्देशक अवसर नहीं देता। यह सवाल कितनों के दिमाग में आया ही होगा कि मिर्जा दोनों समुदाय का मुखर, निर्दोष और सर्वग्राह्य पात्र है। उस के बलिदान से फिल्म की कहानी में कहीं मानवता की हार न सामने आ जाए।
मिर्जा की जान साम्प्रदायिक शक्तियों ने ली। फिल्म में इस दृश्य को तेज़ हवा के झोंके की तरह दिखाया गया है ताकि दर्शक इसी संत्रास में अटके न रह जाएँ। शायद यह इतना संक्षिप्त इसलिए भी है कि निर्देशक इसकी पीड़ा में उलझने, आरोप-प्रत्यारोप में शामिल होने की परिस्थितियों से फिल्म को दूर ले जाना चाहता है। कुछ लोग उनके घर में घुसते हुए एक फ्रेम में नजर आए। वह दरवाज़े पर बेग़ैर किसी खौफ के उससे पहले के फ्रेम में नजर आए। दो चार सेकेंड का उसके बाद का दृश्य है जिसमें बंद दरवाज़े के नीचे से बहता हुआ खून यह सिद्ध करता है कि मिर्जा मार दिये गए हैं या उनपर जानलेवा हमला हुआ है। अस्पताल का एक दृश्य है जिसमें हरिया और शब्बो बेचैनी से उनकी स्थिति पता करने की कोशिश करते हैं और फिर यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि मिर्जा की जान ले ली गयी है। तीन-चार मिनट में फिल्म में यह सारी घटनाएँ इतनी तेजी से हो जाती हैं कि एक सन्नाटा पैदा हो जाता है। जीवन-पर्यन्त संघर्ष और मेलजोल के लिए अपनी समस्त शक्ति लगा देने वाले का अपने आसपास के धर्मान्धों द्वारा मार दिया जाना फिल्म में आखिर कौन सा संदेश देता है?
जिन्दा रहकर मिर्जा जितना कर सकता था, उसने कर दिया था। फिल्म को वास्तविकता के धरातल पर मजबूत करना था, इसलिए अविनाश दास ने आदर्श के मुकाबले अपनी आँखों के सामने बदलते हुए भारत को रखा जहाँ रोज़ कहीं न कहीं एक मिर्जा इन्हीं कारणों से मार दिया जाता है। मिर्जा का दोष बस यही है कि वह सामाजिक समरसता के साथ जीना चाहता है। गाँधी की जान आखिर क्यों ली गई? सफ़दर हाशमी का जीवन क्यों कर लूट लिया गया? रोज़-रोज़ अनाम चेहरे कभी अपने घर में, कभी अपने मुहल्ले में, कभी बाजार और रेल या बस में अपनी जान लुटाने के लिए बेबस हैं। इसलिए अविनाश दास ने अपनी फिल्म की समसामयिकता उभारने के लिए कहानी में कोई बनावटी मोड़ पैदा करके मिर्जा की जान नहीं बचाई।

गाँधी जी की शहादत बर्बरता की एक मिसाल थी मगर एक लम्बे समय तक समाज में साम्प्रदायिक शक्तियों का मनोबल इसी कारण टूटा रहा। आज तक इस कुकृत्य के लिए वैसे लोगों का सिर झुका रहता है। अविनाश दास जिन्दा मिर्जा पात्र से फिल्म में सामाजिक परिवर्तन या हृदय परिवर्तन की आँधी उठाने में पूरे तौर पर कामयाब हुए। दोनों गली के लोगों को इतनी आसानी से यह बात समझ में आयी कि उन्हें बहकावे में नहीं आना चाहिए था। मिर्जा की मौत के पश्चाताप से फिर से इन गलियों में प्रेम और सद्भाव लौट आता है और वह भी हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सब मिलजुल कर हरिया और शब्बो की अंतरधार्मिक शादी की मंजिल तक सहर्ष पहुँचाते हैं। अब यह कौन कहेगा कि मिर्जा के जीते जी पता नहीं ऐसी सफलता मिलती भी या नहीं। स्पष्ट है कि फिल्म के इस आखिरी स्टेज पर जिन्दा मिर्जा से बढ़ कर मिर्जा की मौत ने अपना आदमकद अस्तित्व तैयार कर दिया है।
यह फिल्म जितने गम्भीर विषय पर, स्पष्ट दृष्टिकोण और वैचारिक दृढ़ता के साथ बनाई गयी है, इसमें अगर हास्य-व्यंग्य, नाटक, नौटंकी और अनिश्चित खलंडरा खिलन्दरापन न होता तो दर्शकों की साँसें उखड़ गयी होतीं। कुछ की हृदयगति रुक जाती और कुछ चीखते-चिल्लाते फिल्म छोड़ कर चले आते। अविनाश दास ने फिल्म के हीरो नुमा मुख्य पुरुष चरित्र हरिया को कुछ इस तरह से गढ़ा है कि अगर वह फिल्म में शामिल नहीं होता तो फिल्म का सारा गठन ही टूट जाता। महान कलाकार नसीरुद्दीन शाह का पुत्र होना विवान के जीवन की एक वास्तविक घटना है। फिल्म के स्क्रीन पर वह सबसे सुंदर, चमकदार और आकर्षित नज़र आता है मगर उछल-कूद, नाच-गान या दौड़-भाग में वह और आकर्षक हो जाता है। निर्देशक ने उसके चरित्र की इस ऊर्जा को ईद और होली की पृष्ठभूमि में और भी जगमगा दिया है। हनुमान गली और रहमान गली के जवान और बूढ़े, औरत और मर्द हरिया के नेतृत्व में इन दोनों पर्वों का मजा लेते हैं। वास्तविकता यही है कि भारत में पर्व-त्योहार का यही असली रस है।
अविनाश दास हमारे घरों और मुहल्ले में इसी जीवन-रस की तलाश में निकले थे जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि अगर मिर्जा साहब तैयार करते हैं तो उसका महापार्विक उल्लास और आनन्द हरिया से पैदा होता है। सामाजिक जिन्दगी के इन दो रंगों में माँ-बाप खो चुकी, ठेले पर सब्जी बेचने वाली शब्बो की आधी-अधूरी बातें रह रह कर कहानी का केन्द्र बन जाती हैं। अपने दिल का हाल बताते हुए पहले, दूसरे, तीसरे, और चौथे दिल में कौन-कौन रहता है, इस का जो विवरण वह देती है, वहाँ वेदना और हास्य-विनोद का एक ऐसा संगम उभरता है जिसे असली जिन्दगी के अलावा और कहीं नहीं तलाश किया जा सकता है। अविनाश दास ने ऐसे खामोश पात्रों की बोलती हुई जिन्दगी को केन्द्र में लाकर फिल्म में अनोखा आकर्षण प्रदान कर दिया है।
इस फिल्म में अपनाई गयी यद्यपि नपी-तुली भाषा और चुस्त-दुरुस्त तथा अक्सर कटीले वार्तालाप दर्शकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं मगर इन सब पर सौ मन का हाथी इश्तियाक़ खाँ साबित हुए हैं जो फिल्म में भँगा के नाम से सामने आते हैं। यह पागल है या विक्षिप्त या आम समाज के लिए एक गैर-जरूरी पात्र, कहना मुश्किल है। मगर हर जगह वह मौजूद रहता है। सब की बातों से अलग वह अपना राग और अपनी बात चलाता है। एक वाक्य बोल कर आसमानों में वह कोई सवाल उछाल देता है। बार-बार “भारत एक खोज है” का टुकड़ा उसके मुँह से निकलता है और वह किसी दूसरी राह निकल लेता है। मंटो के ‘टोबा टेक सिंह’ को याद कीजिए तो यह भँगा हमारी कथा-परम्परा का उसी प्रकार का एक जाना पहचाना किरदार मालूम होता है। जब समाज में सही दिमाग के लोगों की तर्क-शक्ति काम न आए या कोई उन्हें सुनने वाला न हो तो ऐसे मौके पर इन पागलों के मुख से अरस्तू या प्लेटो जैसी बातें कहलवाना हारे हुए समाज का आखिरी संघर्ष होता है। इस फिल्म में अविनाश दास ने भँगा के चरित्र पर जितना विश्वास किया है, शायद ही कोई दूसरा निर्देशक इस तरह ऐसे किसी चरित्र को अवसर दे सकता था। इस प्रयोग से निर्देशक ने अपनी फिल्म को परत-दर-परत अर्थपूर्ण बनाने में सफलता पायी है।
मेरी स्मृतियों में अब से तीस-बत्तीस वर्ष पूर्व का वह अविनाश दास अब भी जागृत है जिसने मैथिली के कुछ गीत स्कूली जीवन में लिख लिए थे। वह उन्हें बहुत सुंदर आवाज़ में गाता भी था। हिन्दी की कविताओं में भी दखल-अंदाजी शुरू कर चुका था। दसवीं पास करने के बाद से साहित्यिक समागमों में आना-जाना और विशेष रूप से बाबा नागार्जुन का सेवक एवं सहयोगी बनकर गोष्ठियों में पहुंचना मुझे खूब-खूब याद है। दरभंगा से पटना आकर साहित्य के साथ पत्रकारिता के जंगल में बिहार और झारखण्ड के गली-कूचों में भटकना और फिर टेलीविजन में कुछ वर्षों तक दिल्ली में संघर्ष करते-करते, हर सतह के शहरों और उनके समाज का अनुभव लेते हुए मुम्बई पहुँचना एक सामान्य घटना नहीं थी। अविनाश दास ने अपने व्यक्तित्व की ठोस जमीन में जगह-जगह की ईटें और गारा मिलाकर अपना यह फिल्म निर्देशक रूप सामने लाया है। इसलिए इस फिल्म में वह गीतकार भी हैं, पत्रकार भी हैं और गायक भी। हर भंगिमा को मथ कर उन्होंने एक ऐसी फिल्म तैयार की है जिसे आसानी से कोई खारिज नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी फिल्में बनती रहती हैं मगर इतनी मासूम और सादा फिल्म बनाने का आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ अविनाश दास में नजर आता है।