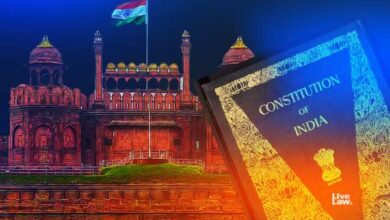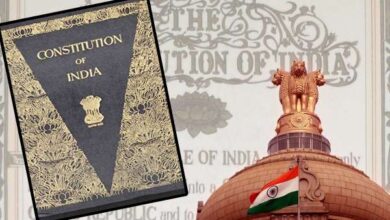परम्परा से मुठभेड़
मई 2014, हिन्दू राष्ट्र की प्रखर मुखालत करने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद ही ‘नये भारत’ की कल्पना को गढ़ता चला गया। इस ‘नये भारत’ में अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुस्लिमों को कोई जगह नहीं दी गयी। चूँकि सत्ता का अपना चरित्र होता है, इसलिए मोदी जैसे कट्टरपंथियों को भी नरम होने पर विवश होना पड़ता है। लेकिन उनके विचार को मनाने वाले राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े व्यक्ति आए दिन ‘नये भारत’ की कल्पना को साकार बनाने में जूटे हुए हैं। यही कारण है कि मोबलिंचिंग के नाम पर चुन-चुन कर व्यक्ति विशेष को मारा जा रहा है। इस ‘नये भारत’ में असहमति के लिए कोई जगह नहीं दी गयी है। भारत में लोकतंत्र तो है, जो ‘लोक’ विशेष यानी सत्ता में स्थापित विचारधारा को मनाने वालों का ‘तंत्र’ हो चुका है। इस ‘नये वाला भारत’ में बदलाव के नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
इस ‘नये भारत’ यानी बदलाव की ही एक कड़ी है- ‘इतिहास की पुनर्रचना’। इतिहास को पुनः लिखना अर्थात अपने सुविधा विशेषानुसार इतिहास बदलने की शुरुआत सत्ता में आते ही कर दी गयी। यही कारण है कि मई 2014 में सरकार बनती है और उसी वर्ष जुलाई में ‘इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च’ (आईसीएचआर) के अध्यक्ष को बदला जाता है और एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है, जो संघ से तालुक रखते हैं तथा उसके इशारे पर काम कर सकते हैं। आईसीएचआर के नए अध्यक्ष ककाटिया यूनिवर्सिटी के इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो. वाई सुदर्शन राव को बनाया जाता है। प्रो. राव आंध्रप्रदेश राज्य के आरएसएस यानी संघ का इतिहास बदलने वाला संगठन “भारतीय इतिहास संकलन योजना” के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।


2007 में प्रो. राव अपने ब्लॉग पर एक लेख में लिखते हैं-
“प्राचीन काल में जाति व्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही थी और हमें इसके खिलाफ़ किसी पक्ष से कोई शिकायत भी नहीं मिलती है। इसे कुछ ख़ास सत्ताधारी तबके ने अपनी आर्थिक और सामाजिक हैसियत बनाए रखने के लिए दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रचारित किया। इसके बारे में हमेशा गलत समझा गया कि यह शोषण पर आधारित कोई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है।” आगे धर्मशास्त्रों के हवाले से वे कहते हैं- “जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में समाहित हो गयी।”
अब सवाल उठता है कि वह कौन-सा प्राचीन काल था, जिसमें जाति व्यवस्था अच्छा काम कर रही थी, कौन-सा धर्मशास्त्र है, जिसमें यह जिक्र है कि कैसे जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में परिणित हो गई? एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो वे जवाब देने के बजाय पूछ रहे थे कि उन्हें ‘आईसीएचआर’ के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ही यह सवाल क्यों? आगे वे कहते है कि उनका यह लेख कोई एकेडमिक पेपर नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन उनके जैसे इतिहासकार भूल जाते हैं कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपके पेशे का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता।
दूसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही हैं। हालांकि यह विमर्श विवादित रहा है, लेकिन फिर भी इतिहास की लगभग सभी धाराएँ एक सामान्य निष्कर्ष को मान चुकी हैं। हिंदू दक्षिणपंथियों का मानना हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है जो ख़ुद को आर्य कहते थे। जिन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेदों की रचना की। वे आर्य को एक नस्ल के रूप में मानते हैं, जबकि इतिहासकर तथा अन्य जानकारों की मान्यता है कि आर्य वे थे जो इंडो-यूरोपियन भाषाएं बोलते थे।

हाल ही में, डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे ने राखीगढ़ी की खुदाई का नेतृत्व किया और प्रोफेसर डेविड रीच के ग्रुप को राखीगढ़ी के कंकाल सौंपे। प्रो. शिंदे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से सम्बद्ध रखते हैं और उनके विज्ञान संगठन ‘विज्ञान भारती’ से जुड़े रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में प्रो. शिंदे कहते हैं कि राखीगढ़ी के आनुवांशिक प्रमाण से पता चलता है कि आर्य कोई आक्रमणकारी नहीं थे बल्कि वे यहीं के थे और सिंधु घाटी के समय वे लोग संस्कृत बोलते थे।
अब सवाल उठता है कि क्या महज़ सिर्फ प्राचीन डीएनए के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि उस डीएनए के लोग कौन-सी भाषा बोलते थे? यह महज़ कपोल कल्पना से इत्तर कुछ भी नहीं लगता। न्यूज़क्लिक में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, मौजूदा खुदाई से राखीगढ़ी में दफन 61 कंकालों में से मात्र एक ही प्राचीन डीएनए के बारे में पर्याप्त जानकारी दे पाने में समर्थ था जिसे ठीक से अनुक्रमित किया जा सकता था। क्योंकि प्राचीनतम डीएनए ठंडे और शुष्क जलवायु में बेहतर तरीके से संरक्षित रह सकते हैं, और यह दोनों चीजें ही भारत में नहीं हैं। फिर सवाल उठता है कि प्रो. शिंदे ने महज़ सिर्फ एक कंकाल, जो प्राचीन डीएनए देने में सक्षम थे, से कैसे पता लगा लिया कि आर्य संस्कृत बोलते थे! जबकि प्रो. रिच के रिपोर्ट में इस बात की कहीं भी जिक्र नहीं है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आनुवांशिकी विज्ञानी डेविड रिच तथा उनके 92 सह-लेखकों ने मार्च 2018 में एक शोध में दावा कर चुके हैं कि पिछले 10 हज़ार साल में भारत में दो बार बड़ी मात्रा में लोग बाहर से आये। पहली बार, 7000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच दक्षिण-पश्चिम ईरान के ज़ैग्रोस प्रांत से कृषक और पशुपालक बड़े मात्रा में भारत में आये। वहीं दूसरी बार, 2000 ईसा पूर्व की शताब्दियों में यूरेज़ियन स्टेपी से, जिसे आज कज़ाख़स्तान के नाम से जाना जाता है।

‘अर्ली इंडियंस: द स्टोरी ऑफ़ आर एनसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम’ के लेखक टोनी जोज़फ़ लिखते है “यही लोग (दूसरी मौके पर आने वाले) संस्कृत का शुरुआती प्रारूप अपने साथ लाये। वे घुड़सवारी करना और बलि परंपरा जैसे नयी सांस्कृतिक तौर-तरीक़े भी अपने साथ लाए। इसी से वैदिक संस्कृति का आधार बना।” प्रमाण के रूप में वे कहते है कि एक हज़ार साल पहले यूरोप में भी स्टेपी से लोग गए थे जिन्होंने वहां के खेतिहरों की जगह ली थी या उनके साथ मिश्रित हो गये। इसी से नयी संस्कृतियाँ उभरी थीं और इंडो-यूरोपीय भाषाओं का विस्तार हुआ था।
शोध से पता चलता है कि वर्त्तमान भारतीयों और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में आनुवांशिकी संबंध हैं और यह दक्षिण भारतीयों से ज्यादा मिलते हैं। वहीं आज वगैर किसी तथ्य के यह साबित करने की कोशिश की जा रही हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्तर भारत के उच्च वर्ग के लोगों के ज्यादा करीब थे।
वहीं दूसरी ओर, प्रो. शिंदे के ही नेतृत्व में जब पिछली साल राखीगढ़ी में 4500 साल पुरानी कंकाल मिली तो उसके प्राचीन डीएनए की जाँच से यह दावा किया गया था कि हड़प्पा सभ्यता और हिन्दू संस्कृति में अंतर हैं, जिसे वे आज खुद ही नकार रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि वे अपनी ही बातों का खंडन वगैर किसी तथ्य का कर रहे हैं! जाहिर है खुले तौर पर सत्तारूढ़ दल ने इतिहास बदलने का जो अभियान शुरू किया है, प्रो. शिंदे उसी अभियान के हिस्से हैं।