
स्वतन्त्रता के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव की संकल्पना शताब्दियों के संघर्ष के बाद मिली स्वतन्त्रता के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए भारत सरकार की पहल है। इस सन्दर्भ में लैंगिक समानता की बात करें तो यह तथ्य विचारणीय है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के बावज़ूद स्त्रियाँ इस ‘अमृततत्व’ से कोसों दूर हैं, समुद्र मंथन के बाद देवियों को अमृत चखाया गया या नहीं? शायद नहीं, तभी तो स्त्री सशक्तिकरण के दौर में भी उनकी स्वतन्त्रता पितृसत्तात्मक समाज के खूँटे से बंधी है, स्त्री को पंख मिले हैं पर कटाई-छँटाई के बाद, पंख प्रसाधन तक सीमित रह गए, स्त्री आज भी साज-सज्जा सामान की तरह घर की शोभा है, अभी हाल ही में आये एक सर्वे ने सिद्ध किया शादी के लिए कामकाजी लड़कियों को पसंद नहीं किया जा रहा, यानी वे घर में ही रहें।
सिनेमा में भी स्त्री शोपीस या वस्तु की तरह प्रस्तुत की जाती है क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है पर उद्योग भी है। सिनेमा निर्माण, लेखन, संगीत, लेखन आदि में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ने लगी है पर सिनेमा का बहुधा भाग आज भी मध्यकालीन बोध में गोते लगा, नायिका भेद चित्रण करने में लिप्त है, पुरुष व पारिवारिक खाँचो के अनुकूल स्त्री चरित्र रचे जातें है जो इनके अनुकूल न हो वे खलनायिका कहलाती है, श्री 420 (1955) में नायिका का विद्या और खलनायिका का माया नाम रखने के पीछे यही मानसिकता है।
आज दर्शकों यानी समाज में बदलाव आये हैं, सिनेमा-उद्योग ने समझ लिया है कि ‘स्त्री विषयक स्क्रिप्ट’ से भी पैसे कमाए जा सकतें है। बावजूद इसके सिनेमा का यथार्थ यह है कि इस बाज़ार में स्त्री आज भी एक ‘वस्तु’ से अधिक कुछ नहीं चाहे पर्दे पर हो या पर्दे के पीछे या उसे महिमामंडित किया जाए, अन्यथा क्या कारण है कि ‘मीटू जैसा आन्दोलन’ विषय को लेकर कोई फिल्म नहीं आई जबकि इस तरह के सनसनीखेज विषय पर बनने वाली फिल्म को लोग हाथों-हाथ लेते लेकिन इससे फिल्म इंडस्ट्री का पितृसत्तात्मक चरित्र उजागर हो जाता जो पहले ही बदनाम है। सच तो यह है कि सुनहले सपने दिखाने वाला सिनेमा-उद्योग पितृसत्तात्मक सोच से संचालित है, जहाँ पुरुषों का वर्चस्व है वे अपने विशेषाधिकारों बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करतें रहें और कर रहें है, अपवाद यहाँ भी हैं।
भारतीय फ़िल्मों का इतिहास स्त्री सन्दर्भ
‘राजा हरिश्चंद्र’ (1913) की पत्नी रानी तारामती की भूमिका के लिए फाल्के जी को स्त्री कलाकार इसलिए नहीं मिला कि सिनेमा का क्षेत्र स्त्री के लिए वर्जित या अच्छा नहीं माना जाता था; यह तो अभी बना ही रहा था, बल्कि स्त्रियों का घर से बाहर काम करना वर्जित था, घर की चारदीवारी, चूल्हा चक्की उनकी दुनिया थी। लेकिन इस फिल्म में स्त्री की कोई भूमिका या योगदान नहीं था यह कहना गलत होगा, दादा साहब फाल्के के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म ‘हरिश्चन्द्राची फैक्ट्री’ (2009) में हम देखतें हैं उनकी पत्नी सरस्वती फ़िल्म निर्माण के लिए अपने गहने बेच देती है, ड्रेस बनाती है, क्रू मेम्बर्स के लिए भोजन बनाती है, आज की भाषा में कहें तो वे फ़िल्म निर्माता, फाईनेंसर, ड्रेस-डिज़ाइनर, केटरर्स हैं लेकिन अफ़सोस उनका नाम कहीं नहीं दिखता है।


दादा साहब ने जब सरस्वती को भी तारामती बनने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये बाकी काम कौन संभालेगा। ‘मोहिनी भस्मासुर’ में पहली महिला कलाकार कमलाबाई गोखले और उनकी मां दुर्गा गोखले ने जब काम किया तो इसलिए नहीं कि हमारा समाज अचानक प्रगतिशील हो गया था बल्कि रंगमच की इन कलाकारों के लिए फ़िल्में करना आर्थिक विवशता थी। फातिमा बेगम सुल्ताना पहली महिला हैं जिन्होंने ‘फतामा फिल्म्स’ के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और 1926 में ‘बुलबुले परिस्तान’ का निर्देशन भी किया। पहली महिला संगीतकार नर्गिस की माँ जद्दनबाई ने 1935 में ‘तालाश-ए-हक़’ नामक फिल्म में अभिनय भी किया और नर्गिस ने बाल कलाकार के रूप में काम किया, इसके बाद ‘अछूत कन्या’ (1936) फ़िल्म की संगीतकार सरस्वती देवी का ‘मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलू रे’ गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ जो रूढ़ियों में बंधी अछूत लड़की की मासूम इच्छा भी दर्शाता है, 1955 ‘मिस्टर एंड मिसेज़ 55’ में ‘पीतम आन मिलो’ गीत लिखकर सरोज मोहिनी नायर पहली गीतकार बनी।
प्रश्न उठता है कि जब आरंभिक काल में स्त्रियाँ फिल्मों में सक्रिय योगदान दे रहीं थी तो स्वतन्त्रता के बाद स्त्रियाँ धीरे-धीरे हाशिये पर कैसे सरकती चली गईं? फ़िल्म उद्योग में पुरुषों की प्रधानता के कारण! जब कोई निर्माता-निर्देशक किसी खास सिचुएशन के लिए तड़कते-भड़कते दृश्य या गीत-संगीत की माँग करता है तो स्त्री गीतकार, संगीतकार या निर्देशक निश्चय ही असहज हो जाती होंगीं इसलिए इस क्षेत्र में वे कम ही आना पसंद करती, फिर उन्हें वह स्पेस नहीं दिया गया जिसकी वे हकदार थी बल्कि ‘नैनों में दर्पण है’ जैसे खूबसूरत गीत लिखने वाली माया गोविन्द ने भी उनके हिसाब से गीत लिखे, और अश्लीलता का आरोप भी लगे। रानी मालिक ने 90के दशक में कई सुपर हिट गीत दिए लेकिन आज भी महिला गीतकार या संगीतकारों की कमी है। पुन्सवादी सोच फ़िल्मी गीतों पर बुरी तरह हावी है। स्त्री स्वयं को सहर्ष दोयम दर्जे का मान, नायक के प्रेम करने पर अपना जीवन धन्य समझती है अन्यथा खलनायिका न हो जायेगी ! पुरुष को ‘गगन के चंद्रमा बताती है और खुद को धरा की धूल’ जो स्त्री के उद्गार नहीं पुरुष की सोच है ‘अगर तुम हो सागर में प्यासी नदी हूं‘ नदी सबकी प्यास बुझाती है, पर समुद्र में विलीन होना उसकी नियति है, पर उसकी प्यास और आकांक्षा को देह-प्यास तक सीमित मान लिया जाता है।
आज स्त्री इस सोच परंपरागत ढांचे को तोड़कर बाहर निकल रही है वह जान चुकी है कि गगन के चंद्रमा में कितने दाग हैं उसका वास्तविक चेहरा कितना बदसूरत है और अपनी धूल-धूसरित सृजनशक्ति को भी पहचान लिया है। 80-90 के दशक में नारी ने अपनी हस्ती को पहचानते हुए तमाम नियम-कायदों (खूबसूरत) को तोड़ा और ‘खून भरी माँग’ लिए वह ‘जख्मी औरत’ अपना बदला खुद लेने के लिए उतर आई। स्त्री केन्द्रित फिल्मों का चलन चल पड़ा दामिनी, बैंडिट क्वीन, फायर, बवंडर, वाटर, सरदारी बेगम, गॉडमदर, चांदनी बार, चमेली लज्जा, जुबैदा इसी श्रृंखला की फ़िल्में हैं जिसमें कोई नायक उद्धारक नहीं।
स्वतन्त्रता के बाद भी स्टीरियोटाइप में बंधी स्त्री


स्वतन्त्रता पूर्व 40 के दशक में लगभग 50 फिल्मों में काम करने वाली ‘फीयरलेस नाडिया’ का बोलबाला था यह नायिका ‘हंटरवाली’ के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी फिल्मों का मूल स्वर था ‘अब तुम औरत पर राज नहीं कर सकते, इस राष्ट्र को स्वतन्त्रता चाहिए तो सबसे पहले यहाँ की औरतों को आज़ादी देनी होगी’ लेकिन क्या कारण रहा कि अत्याचारों का डटकर मुकाबला करने वाला ऐसा निडर चरित्र घर-परिवार, रसोई, नायक की शोभा बढ़ाने लगा? संभवत: स्वतन्त्रता संग्राम में साम्प्रदायिक दंगो ने स्त्रियों की अस्मिता, आत्मस्वाभिमान को कुचल डाला शायद इसलिए आज़ादी के बाद स्त्रियों को घरों में ही रखना सुरक्षित मान लिया गया। सुरक्षा के नाम पर और पुरुष की अपनी सत्ता और वर्चस्व को बनाये रखने की महत्वाकांक्षा ने स्त्री को स्वतन्त्रता के सुख से वंचित कर दिया, सपनीले सपने दिखाने वाले सिनेमा ने भी बदलाव के लिए पहल न की बल्कि इसमें दो राय नहीं कि फिल्मों ने इस स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ‘तुम्हारें चरणों में आ गई हूँ यहीं जियूँगी यहीं मरूँगी ’ पंक्तियाँ स्त्री की पुरुष पर निर्भरता तथा अन्य कोई विकल्प न होने की गवाही दे रहे है, ऐसे अनगिनत गीत बिखरे पड़े हैं।
फिल्मों का आदर्शीकृत समाज
आजादी के बाद भारतीय समाज का आदर्शीकरण होना आरंभ हुआ लेकिन इन आदर्शों का भार सबसे ज्यादा स्त्री पर ही पड़ा, त्याग समर्पण, बलिदान आदि के झंडे उसने ही उठाये। और आज भी संस्कारों से भरी नैतिकता की पोटली उसके ही सिर है। हाँ, शिक्षा का दायरा बढ़ा पर इतना ही कि पढ़ने पर लड़का अच्छा मिलेगा, स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता था। ‘आवारा’ (1951) की वकील नायिका भी है अदालत में कहती है “मेरा दिल कहता है कि राजू बेगुनाह है” पर अदालत दिल की नहीं दिमाग और तर्क को मानती है यानी स्त्री वकालत नहीं कर सकती। ‘ऐतराज’(2004) की वकील नायिका शादी के बाद वकालत छोड़ देती है, पर पति का केस लड़ने के लिए पुन: वकालत शुरू करती है और केस जीत भी जाती है यानी पति जेल न जाता तो वह घर ही संभालती, 1951-2004 सिनेमा की सोच न बदली। 1962 तक ‘मैं चुप रहूँगी’ कहने वाली नायिका ने 1988 में घोषणा करती है ‘कब तक चुप रहूंगी’। फिर भी वकालत स्त्रियों के लिए अच्छा पेशा नहीं माना जाता कि ये तो शादी के बाद जिरह-बहस करेगी, क्योंकि समाज को बोलती औरत नहीं पसंद।
शिक्षा तो फिल्मों का मुद्दा कभी रहा ही नहीं, शिक्षित लोग तर्कहीन फूहड़ फ़िल्में देखने सिनेमा नहीं जायेंगे, सिनेमा की सुंदर चुलबुली नायिका कॉलेज में स्टेज नृत्य करेगी ही, उसका प्रेम और गाने नायक के चरित्र को उभारने काम करतें हैं क्योंकि नायक उसका उद्धार जो करने वाला है। ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’(2012) में चीयर गर्ल तक बनेगी लेकिन किताबें? वो तो नायक से टकराते ही गिर जाती है (मेरे महबूब) फिल्मों में नायक ही विदेश से पढ़कर आता है। ‘कुछ कुछ होता है’ (1998) में नायिका विदेश से पढ़कर आती है पर एक चुलबुली लड़की से अधिक कुछ नहीं। स्त्री शिक्षा का महत्व एकमात्र ‘अनपढ़’ (1962) में दीखता है जहाँ अनपढ़ नायिका कहने को विवश है ‘आपकी नजरो ने समझा प्यार के काबिल मुझे’ वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के वकील बनाती है।1990 के आरक्षण-परिदृश्य के साथ रिलीज़ ‘हुडदंग’ (2022) की नायिका मस्त और बिंदास है, स्वतन्त्रता के नाम पर अपने हीरो के साथ सिगरेट शराब पीती है, लाइब्ररी या क्लासरूम से ज्यादा उसके कमरे में दिखती है, पढ़ाई से ज्यादा उसे शादी की चिंता है उसका चरित्र ‘लड़की बचाओ:लड़की पढ़ाओ’ के नारे की धज्जियाँ उड़ाता नज़र आता है। हाँ, हाल ही में हिंदी डब मराठी फ़िल्म ‘जयंती’ (2020) की पढ़ी-लिखी नायिका शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित कर रही है। उच्चशिक्षा में तो स्त्री-शिक्षा दर कमतर होती जाती है, SMET यानी साइंस मैथ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में तो स्त्रियों को आज भी महत्व नहीं दिया जाता ‘मिशन मंगल’(2019) फ़िल्म के शीर्षक पर अक्षय कुमार कहतें है, मंगलयान मिशन में महिला वैज्ञानिकों के योगदान के कारण फ़िल्म का नाम ‘महिला मंडल’ रखा गया लेकिन बाद में लगा पुरुषों के योगदान को नज़रंदाज़ नहीं करना चाहिए इसलिए इसका नाम ‘मिशन मंगल’ रख दिया, पर क्या घर-परिवार में स्त्री योगदान पर कभी फिल्म बनी? इसी तरह जब विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ ‘शकुंतला देवी’ पर फ़िल्म बनती है तो उनका चरित्र पति को छोड़ने वाली महत्वाकांक्षी स्वार्थी स्त्री के रूप में मोल्ड कर दिया।
विवाह संस्था में परिवार, सिनेमाई माँ/बहू
70-80 के दशक में जहां ‘एंग्री यंग मैन’ जब व्यवस्था के प्रति अपना असंतोष और विद्रोह जाहिर कर रहा था वहाँ नायिका ‘आजा पिया तोहे प्यार दूँ’ के लिए थी और माँ गाजर के ‘हलवे और खीर’ के लिए। बेटी के लिए यह संवाद कभी किसी माँ ने नहीं बोला ‘बेटी आज मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है’ बेटियों की पसंद ! दूसरे ‘अब बूढ़ी होने लगी हूँ काम नहीं होता, बहु ला दे, यानी माँ के रिटायर्मेंट के बाद नई बहु का अपॉइंटमेंट होगा, पितृसत्ता से संचालित विवाह-संस्था पुरुष सुविधा के लिए ही बनी है न! ‘कालिया’(1981) में पढ़ी लिखी स्वतन्त्र विचारों वाली लड़की को उसे माथे पर अंडा तोड़ते हुए दिखाया गया है क्योंकि उसने कभी रसोई नहीं झाँकी इसलिए नायक उसे अच्छी बहू की विशेषताएं सिखा रहा है ‘चांद में जैसे बदरी में छुप जाता है ऐसे ही आपका चेहरा घुंघट में छुप जाना चाहिए चेहरा दिखाना पश्चिम की नुमाइश है जबकि छिपाना भारतीय संस्कार’ परिवार संभालते संभालते तन भले ही टूट जाए, मन बीमार पड़ जाए लेकिन देह की ‘पवित्रता’ बनी रहे बीमारियां उसे पुरुष संसर्ग से भी मिलती है जो वह बाहर से लेकर आता है। समझ नहीं आता 1980 की ‘खूबसूरत’ रेखा जो सारे नियम तोड़, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाती है, खिलखिला कर हँसती है, यहाँ तक कि सास के भी विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर चुकी थी, मात्र छह वर्ष बाद 1986 ‘सदा सुहागन’ की कर्तव्य परायण, त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति गृहलक्ष्मी का महिमामंडन करने लगी है, जो सुबह उठकर पति के पैर छूती है, शेविंग किट से लेकर टूथ ब्रश जूते पॉलिश सभी करती है, बच्चों को तैयार करके प्रसन्नचित्त गीत गाती है ‘मेरा घर स्वर्ग जैसा है और मेरे पति मेरे स्वामी हैं’ ये पत्नियां पितृसत्तात्मक समाज की सेवा के लिए रोबोट की तरह तत्पर रहती हैं। सूरज बड़जात्या की पारिवारिक फ़िल्में इसलिए ही पसंद की जाती है उनकी नायिकाएं (मैंने प्यार किया 1989) मटर छीलने के लिए तैयार हैं “और नहीं छिलेगी तो हम छिलवाएंगे ” जैसे संवाद पितृसत्ता में स्त्री के स्थान को निर्धारित करता है ‘हम आपके हैं कौन’(2015) विवाह पूर्व नायिका अपने प्रेमी के लिए खाना बनाकर इंतजार करती है यानी एक सुघड़ बहू बनने की तैयारी अभी से कर रही है जहाँ वह जीवन भर सबकी सेवा करेगी और सेवा अवैतनिक हुआ करती है ‘गृह+लक्ष्मी हैं जो मुफ्त में काम करके लक्ष्मी बचाती हैं’। घर संसार, विवाह, बाबुल, घर की इज्जत, दिलवाले दुल्हनियाँ ले जायेंगे, घर परिवार, परिणीता, सुहागन, जैसी फ़िल्में समाज में परिवार के महत्व को दर्शाती हैं।चाहे मुखिया ‘गृहस्थी’ (1963) दूसरी ‘गृहस्थी’ बसा के बैठा है वह उसकी ‘एक ही भूल’ तो है जिसे सभी दर्शक यानी पूरा समाज माफ़ कर देते हैं लेकिन पत्नी ऐसा करने का आज भी नहीं सोच सकती अगर सोच रही है तो पूरी ईमानदारी से बता कर वह सम्बन्ध तोड़ती है, तब उसे शकुन्तला देवी की तरह खलनायिका का-सा शेड दे दिया जाता है।‘मदर इंडिया’ ने माँ से बहुत उम्मीदें जगाई इसलिए जरूरी है माँ का महिमामंडन बंद किया जाए। हाईवे (2014) परिवार के भीतर स्त्री की सुरक्षा पर ही प्रश्नचिन्ह लगाती है, पहली दफा यह यथार्थ दिखाया गया कि बच्चियों का यौन शोषण करने वाले रिश्तेदार ही होते हैं, माएँ उन्हें चुप करा देतीं हैं। बेटियाँ भी डर और घर की मान मर्यादा के लिए चुप रहती है।
विवाह संस्था में दहेज़ प्रथा बेटी की ख़ुशी से ज्यादा सुरक्षा का प्रश्न होता है दहेज़ (1952) में प्रताड़ित बेटी के लिए पिता दहेज़ लाने पर बेटी कहती है ‘पिताजी आप एक चीज लाना भूल गए कफन’ लोभी ससुराल वालों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली फिर भी फिल्मों में वैवाहिक दृश्यों का भव्य चित्रांकन होता है, अमेरिका में विवाहित बिजनौर की मनदीप कौर ने ससुराल वालों से तंग आकर आत्महत्या कर लेती है जबकि 1955 में जब हिन्दू विवाह बिल में विशेष परिस्थितियों के वैवाहिक संबंध विघटित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो ‘सब ठीक हो जायेगा’ की शिक्षा दी जाती है। 1955 में ‘मिस्टर एंड मिसेज़ 55’ आती है जिसमें नारीवादी बुआ विवाह संस्था को लड़कियों के लिए खराब मानती है लेकिन कहानी का अंत सन्देश देता है कि विवाह की खूबसूरत स्थिति से निकलकर तलाक लेना मूर्खता है आज भी तलाक के लिए हमेशा स्त्री को दोषी करार किया जाता है।
प्रेम विवाह, लिव इन
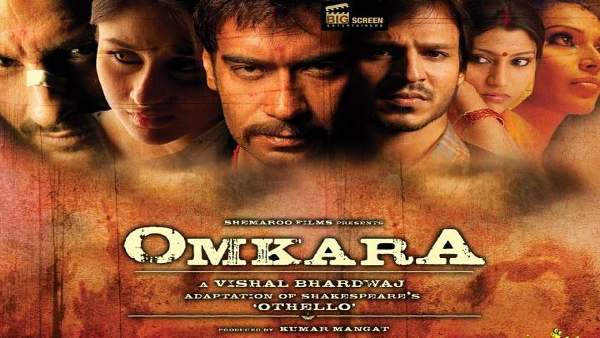
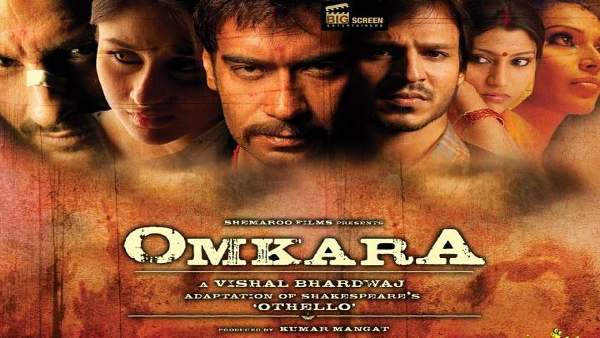
ओमकारा (2006) का संवाद है ‘जो बेटी अपने बाप की न हुई वो किसी और की क्या होगी’ यह एक सामाजिक मुहावरा है जो लड़की को अपने पिता के हर निर्णय को मानने के लिए बाध्य करता है, वह प्रेम नहीं कर सकती अगर करेगी तो ‘पारो’ की तरह बदनाम होगी या अनारकली की तरह उसकी ओनर किलिंग होगी। ‘NH10’ (2015) फिल्म का संवाद गाँव की पंचायतों में पितृसत्ता की पैठ का भयानक रूप सामने रखता है ‘गुडगाँव के मॉल ख़त्म होते ही सारे नियम क़ानून भी ख़त्म हो जाते हैं’ इसलिए भी आज युवा विवाह-संस्था से परे लिवइन रिलेशनशिप की ओर जा रहा है इस संदर्भ में ‘इजाजत’ (1987) महत्वपूर्ण फिल्म है, बाइक चलते हुए अपने ही मफलर के द्वारा गला घुट कर अनुराधा पटेल का एक्सीडेंट हो जाता है, निर्देशक बताना चाहता है कि लिवइन अपना ही गला घोंटने जैसा है। गहराइयाँ (2022) में लिवइन में रहने वाली नायिका घर संभालती दिखाई गई है, लड़का बस लैपटॉप पर काम करते दिखाया है जो बताता है स्त्री लिवइन में भी स्वतन्त्र नहीं इसलिए वह अकेले सिंगल रहना पसंद कर रही है जहाँ कोई बंधन नहीं, देह के भी नहीं पर देह मुक्ति के प्रश्न फ़िल्मों में देह प्रदर्शन (/स्त्री/पुरुष दोनों) की हदें तोड़ने लगतें हैं जो पुरुषों के लिए मसाला भर हैं। जैसे डर्टी पिक्चर, पार्च्ड, लक्ष्मी बम, टोटा पटाखा आईटम मॉल, सेमी पोर्न की तरह सुर्ख़ियों में आती हैं, यहाँ ‘बैंडिट क्वीन’ भी करुणा के स्थान पर कामुकता का आनंद दे सकती है, हाँ, डेढ़ इश्किया(2014) में स्त्री अपनी यौनिकता का इस्तेमाल कर चाचा भतीजे को सबक सिखाती हैं तो वह अश्लील नहीं लगता, इसी तरह ‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ स्त्री की यौन इच्छाओं को खुलकर सामने लाने का साहासिक प्रयास है।
घर परिवार से बाहर के क्षेत्रों में खेल का क्षेत्र पुरुषों के लिए रिज़र्व है, अगर वो बेडमिंटन खेलती भी है तो ‘ढल गया दिन हो गई रात’ जैसे रोमांटिक गीत गाते हुए। चूल्हे चौके ने स्त्री प्रतिभा का सदैव हनन किया है। ‘सुल्तान’ की नायिका अनुष्का अपने खेल का त्याग करती है, ‘मेरी कॉम’ का संघर्ष किसी से छिपा नहीं। ‘चक दे इंडिया’ लड़कियों की हॉकी टीम से भी ज्यादा कोच की फिल्म है, ‘दंगल’ के बापू यदि बेटे के बाप बन गए होते तो तीनों बेटियाँ अपनी माँ की तरह चूल्हा चक्की में गुमनाम जीवन व्यतीत कर रही होती, ‘साला खडूस’ नाम से ही पुरुष प्रधान लग रही है भले ही लड़कियों के मुक्केबाजी पर हो, साहेब, हिप हिप हुर्रे, धन धना धन गोल, द गोल पुरुष प्रधान फ़ुटबाल खिलाड़ियों में गुरिंदर चड्ढा ‘बेंड इट लाइक बेकहम’(2002) एक लड़की के फ़ुटबाल खिलाड़ी बनने के सच होते सपने को लेकर आती है जो एक महिला निर्देशक ही कर सकती थी हम देखतें हैं लडकियाँ अपने सपनों को यथार्थ में बदल रहीं है मुक्केबाज, मेरी कॉम, सांड की आँख, पंगा, सायना, शाबास मिट्ठू जैसी फ़िल्में लड़कियों को खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।
कॉर्पोरेट, जलसा, दिल धड़कने दो, सत्ता, आँधी, इंदिरा, महारानी डर्टी पॉलिटिक्स जैसी फ़िल्में स्त्री के पारिवारिक दायित्वों से अलग राजनीति और कॉर्पोरेट जगत में स्त्रियों की स्थिति को बताती है इन क्षेत्रों में शादी बिजनेस डील बन कर रह जाती है, राजनीति हो या बिजनेस उसका उत्तराधिकारी बेटा ही होगा ‘दिल धड़कने दो’ में बेटा कहता है मैं आपका बिसनेस नहीं संभल सकता पर बेटी वो भी शादीशुदा कैसे? माँ ही पहला विरोध करती है लेकिन यह फ़िल्म एक बदलाव को स्वीकार करती दिखती है और बेटी को बिजनेस सौंप देतें हैं। जयललिता पर बनी थालाईवी (2021) एम.जी.रामचंद्रन की अधिक लगती है। फ़ौज में स्त्रियों की बात की जाये तो ‘राजी’(2018) महिला प्रधान फ़िल्म लगेगी पर देशभक्ति की अधिक है, राज़ी अपने पिता से कहती है ‘अगर मैं आपका बेटा होता तब भी तो आप मुझे फ़ौज में भेजतें न?’ यानी यहाँ समस्या स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं बल्कि देशभक्ति है पर महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि देशभक्ति सिर्फ पुरुषों में नहीं स्त्रियों में होती है। अगर देह व्यापार या देहकर्मी की बात करें तो फ़िल्में उन्हें भले ‘पाक़ीज़ा’ कह दें पर ‘उमराव जान’ की तरह वे अपने घर लौट नहीं सकती गंगूबाई कहती है ‘यही समझा रही हूँ एक तवायफ घर कैसे बसा सकती है’ हालाँकि ‘गंगूबाई’ भी ‘ट्रेजेडी क्वीन गाथा’ ज्यादा प्रतीत होती है।
‘भूमिका’ (1988) फिल्म एक फिल्म अभिनेत्री की कथा कहती है जो अपने शोषणों के बाद भी पर्दे पर खुश दिख रही है, अभिनेत्री के जीवन पर आई वेब सीरीज आई ‘फेम गेम” में अंतिम एपिसोड के आते-आते एक समर्पित स्त्री की संकल्पना करने वाला बॉलीवुड नायिका की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को प्रेम-स्वार्थ से जोड़ कर खलनायिका के रूप में परिवर्तित कर देता है। “वो मैजिकल नहीं बल्कि ब्रिलियंट है” संवाद उसके चरित्र कटाक्ष है। इसे कामकाजी महिला के शोषण से भी जोड़ कर देखना चाहिए जबकि स्त्री सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतन्त्रता को सर्वोपरि माना जाता है, वही फिल्म उसके दोहरे शोषण का चक्रव्यूह भी स्पष्ट करती है, जिसमें उसके सभी अपनों ने, उसे शिकंजे में कसा हुआ है। लेकिन पुरुष प्रधान फ़िल्म उद्योग में जब स्त्री फिल्म बनाती है वह स्त्री अधिकारों, उसके शोषण उस की दयनीय स्थिति के साथ-साथ उसकी शक्ति को बहुत ही सहजता और तर्कों के साथ संप्रेषित करने का प्रयास करती हैं। साईं परांजपे, अपर्णा सेन, दीपा मेहता, कल्पना लाजमी, मीरा नायर, जोया अख्तर, मेघना गुलजार, तनूजा चंद्रा आदि का नाम उल्लेखनीय है।
जिन अगली पंक्ति के दर्शकों के लिए मूलत: फिल्म बनाई जाती है उनसे निर्माता-निर्देशक को सिर्फ हिट की उम्मीद होती है यहाँ सिनेमा की नियत संदेहास्पद हो जाती है। फिर ये ये दर्शक/समाज सिनेमा के सन्देश को कितना ग्रहण कर पाता है? हाल ही में ‘जयेश भाई जोरदार’(2022) भ्रूण-हत्या और स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी सोच के गंभीर मुद्दे को हलके फुल्के मजाकिया ढंग से लेकर आती है फ़िल्म आशानुकूल ‘जोरदार’ नहीं बन पाई।कम बजट की ‘छोरी’ ज्यादा बेहतरीन फिल्म है। घरेलू हिंसा पर डार्क कॉमेडी ‘डार्लिंग्स’(2022) भी विषय से भटकती, बदले की भावना की फ़िल्म बन जाती है स्त्री सशक्त हो रही है लेकिन घरों में होने वाली हिंसा को फ़िल्म बेहतर तरीके से चित्रित करती है जो बताती है कि सिनेमा के सुनहरे पर्दे की ‘हैप्पी एंडिंग’ अभी यथार्थ से दूर हैं।











