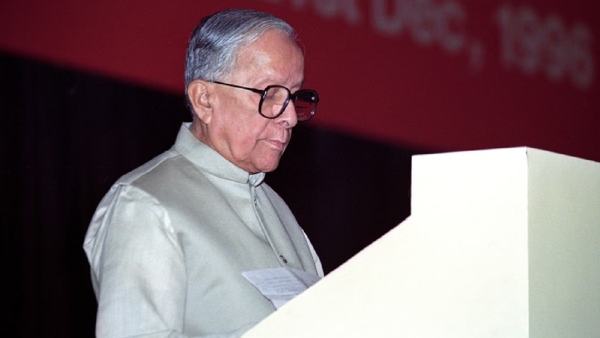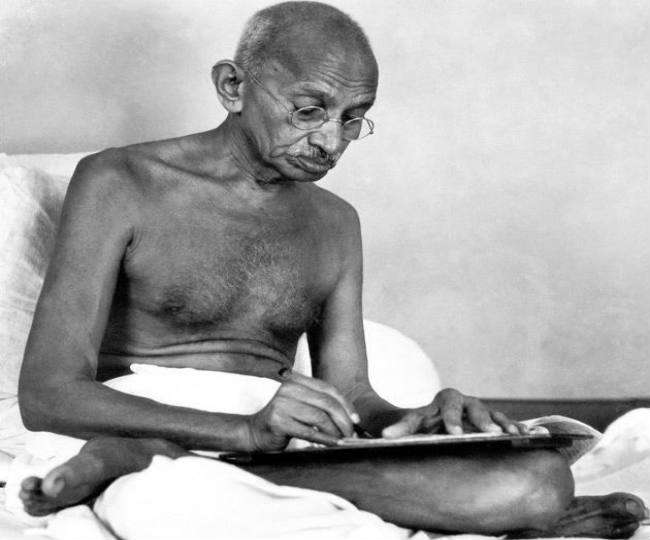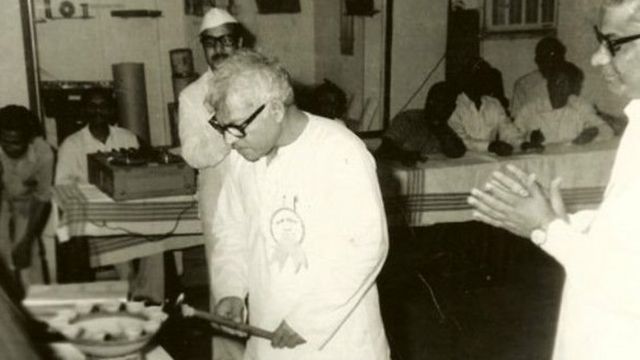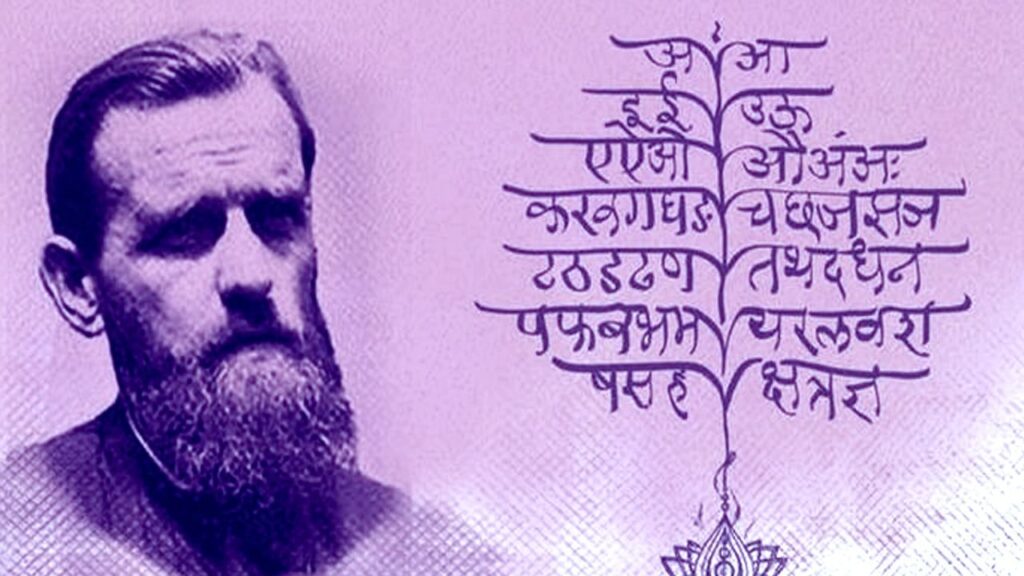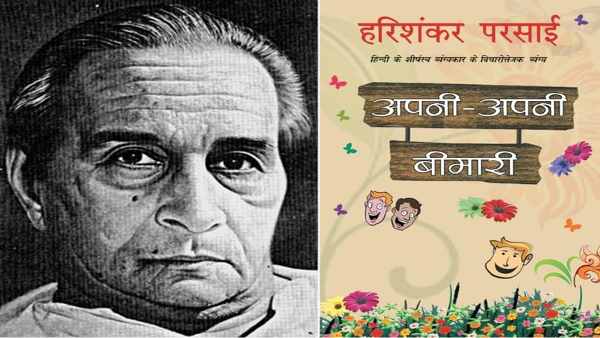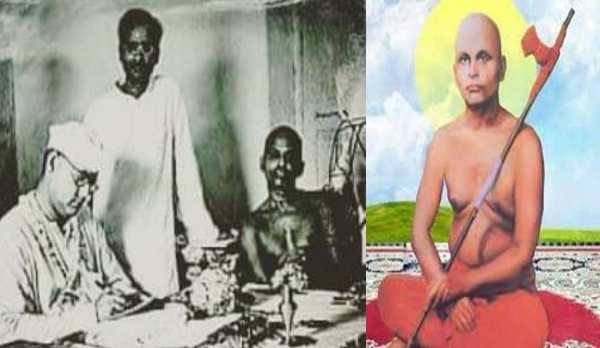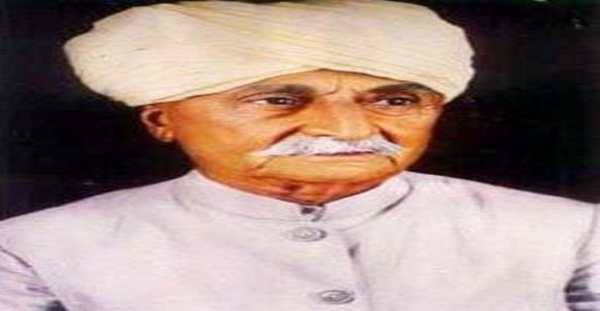‘ज़ौक़’, उनकी शायरी और उनकी दुनिया
शेख मोहम्मद इब्राहिम ‘ज़ौक़’ (1788-1854)
ज़ौक़, यानी शेख़ मुहम्मद इब्राहिम ‘ज़ौक़’, का नाम आते ही क्या विचार आता है? अन्तिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फर के उस्ताद। ज़्यादातर उनके बारे इससे ज्यादा कोई याद नहीं रखता। इससे आगे कहने को हुआ तो कोई ज़ौक़ और ग़ालिब की अदावत के बारे में बता देगा। कोई दिल्ली के शायरों की समझ रखने वाला, इस अदावत को बयाँ करने के लिए ग़ालिब का कोई शेर जैसे -‘हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता’- पढ़ देगा। और कोई दिल्ली का इतिहास जाने वाला, उस समय जफ़र के प्रिय बेटे जवां बख्त की शादी के अवसर पर ग़ालिब और ज़ौक़ के लिखे सेहरे (निकाह के बाद पढ़ी जाने वाली नज़्म) के मुक़ाबले का ज़िक्र कर देगा।
ज़्यादातर उनका ज़िक्र-ए–बयाँ यहीं खत्म हो जाता है। ज़ौक़ के जीवन, उनकी शायरी और उनकी दुनिया के बारे में लोग बहुत कम जानते है। इसके कई कारण है। कुछ तो लोग उस समय को भूल गए। साथ ही, उनके समकालीन शायरों-जैसे ग़ालिब, के बारे में कुछ ज़्यादा ही लिखा-पढ़ा गया है। इस कारण ज़ौक़ पृष्ठभूमि में चले गए। और बाकी का खेल किस्मत ने कर दिया है- जो ज़ौक़ की विरासत से समकालीन लोग महरूम हैं। तो आइये उनके जन्मदिन, 22 अगस्त, के अवसर पर इस अज़ीम शायर के बारे मे कुछ और जाने।
इब्राहीम से ज़ौक़ का सफ़र
ज़ौक़ के बारे मे ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। और जो कुछ भी लिखा गया है वह ज्यादातर मौलाना मोहम्मद हुसैन ‘आजाद’ की उर्दू शायरी की समीक्षा, आब-ए-हयात, से ही लिया गया है। ज़ौक़ के पिता का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे से ताल्लुक रखते थे। यहीं से आज के मशहूर सिने-कलाकार नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी आते हैं। जिन्होंने अपना शुरुआती दौर पास के महानगर, दिल्ली मे बिताया। और जैसे आज भी इस इलाके के ज़्यादातर नौजवान अपने रोटी-रोजी का जुगाड़ करने के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। वैसे ही रमज़ान साहब भी नौकरी के फिराक मे दिल्ली आ गए। यह शहर उन्हें ऐसा पसंद आया कि वह सदा के लिए यहीं के हो के रह गए।
बहरहाल, दिल्ली आकर बहुत से नौकरियों में हाथ-पैर मारे। चूंकि वह युद्धों का दौर था तो सैनिकों की बहुत जरुरत हुआ करती थी। तो उन्होने इसमे भी हाथ आज़माया। वो सैनिक तो खास न थे। हाँ, पर किस्सेबाज़ और अफ़सानानिगार अव्वल दर्जे के थे। साथ ही उनके भरोसेमंद, नेक नियत और सज्जन होने के चलते, स्थानीय अमीर, नवाब लुत्फ अली खान, ने रमज़ान साहब को अपने हरम का कार्यवाहक मुकर्रर कर दिया। यहीं उनके इकलौते पुत्र इब्राहीम का जन्म हुआ।
दिल्ली में इब्राहीम का घर काबुली दरवाजा नामक इलाके के एक साधारण मकान में था। इलाके मे उस वक्त शहर के सबसे कुलीन वर्ग के लोग निवास करते थे। यहीं पर उनसे पहले के शायर सौदा (1713-1781) रहा करते थे। इस इलाके की बहुत-सी बड़ी-बड़ी आलिशान हवेलीयों के बीच इब्राहीम का मकान शायद सबसे छोटा था। आज उस बस्ती का नामोनिशान भी नहीं है। ज़ौक़ के जीवनीकार, तनवीर अहमद, अल्वी कहते हैं कि इस इलाके के सभी घर 1857 के ग़दर के बाद ढहा दिए गए थे। और बाद में, 1864 में, दिल्ली में ट्रेन की शुरुआत के बाद पहला स्टेशन बनाया गया। इसे आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है।
मिया इब्राहीम की शुरुआती तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल के मदरसे में हुई जो ख़ुद ‘शौक़’ के तख़ल्लुस से शायरी करते थे।. संभवतः इब्राहीम ने उनसे मुतासिर होकर अपना तख़ल्लुस ‘ज़ौक़’ रख लिया हो। ‘ज़ौक़’ का मतलब है ‘ज़ायका’, और जो उस वक्त बहुत ही कुलीन चीजों के रसज्ञान और समझ के लिए प्रयुक्त होता था।.यहीं पर उनकी मित्रता नवाब लुत्फ अली खान के भतीजे मीर काज़िम हुसैन ‘बेक़रार’ से हो गयी।
मीर काज़िम, उस्ताद शाह नसीरुद्दीन नसीर के शागिर्द थे। उस समय नसीर दिल्ली के बहुत ही पहुँचे हुए उस्ताद माने जाते थे और उन्हें प्यार से लोग काले साहेब कहा करते थे। उनकी पहुँच किल्ला-ए-मुल्ला यानि लाल किले तक थी, जहाँ पर उन्होंने मुगलिया खानदान के कई लोगों को शिक्षित किया था। वह ग़ालिब और जफ़र के करीबी और शायर मोमिन (1800-1851) के उस्ताद भी थे। इब्राहीम भी उनकी सरपरस्ती में चले गये। काले साहेब को इब्राहीम के पैर पालने में ही दिख गए थे। पर वे अपनी औलाद को आगे बढ़ाने की जुगत में लगे रहे। इब्राहीम को जल्द ही ये बात समझ में आ गयी और उन्होंने उस्ताद के बिना अकेले ही महफ़िलों में शेर पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर काले साहब के दक्कन चले जाने के बाद जल्द ही इब्राहीम को उनकी जगह शोहरत भी हासिल होने लगी।
अब उनकी मंज़िल थी कि उनकी शोहरत शाही क़िले तक पंहुचे। तो कुछ ताल्लुकात, कुछ मशक़्क़त और बाकी क़िस्मत की बदौलत यह भी हो गया। हुआ यह कि उन दिनों अकबर शाह द्वितीय गद्दीनशीं था। उसे तो शायरी का शौक़ न था। हां, उसका बेटा अबू ज़फर ज़रूर शायरी मे गहरी दिलचस्पी रखता था। जफ़र की शेरों को पहले काले साहेब सुधारा करते थे। उनके दक्कन जाने के बाद यह काम मीर काज़िम हुसैन के सुपुर्द हो आया। चूँकि कुछ समय बाद मीर काज़िम अँग्रेज अफसर जॉन एल्फिन्स्टन के सेक्रेटेरियट में एक ऊँचा ओहदा पा कर दक्षिण भारत का रुख कर गए। तो आख़िरकार यह काम इब्राहीम के पास आया।
अबू ज़फ़र ने इब्राहीम को अपना उस्ताद क़ुबूल किया। इसी दौरान अकबर शाह पर लिखे अपने कसीदे (उर्दू शायरी की एक विधा जोकि शायर अपने आश्रयदाता की शान में लिखता था) पर इब्राहीम को ‘ख़ाकानी-ए-हिंद (ख़ाकानी बारहवी सदी में फारस के महानतम कसीदेकार थे) के ख़िताब से नवाज़ा गया। तो उस वक्त चेले और उस्ताद की क़िस्मत बुलंदी पर थी। और जल्द ही, अबू ज़फर, बहादुर शाह ज़फ़र बन गया और शेख़ इब्राहीम उस्ताद ‘ज़ौक़’ कहलाने लगे।


ज़ौक़ अपने समकालीन ग़ालिब से कम फक्कड़ नहीं थे। पर उन्होंने इसका हउआ नहीं बनाया। यूं तो ज़ौक बादशाह के उस्ताद थे, पर क़िले के अंदर की चालबाज़ियों के चलते उनकी रहमत से अधिकतर महरूम ही रहे। उनकी तनख्वाह महज़ चार रुपये महीना थी और मुफ़लिसी उन पर भी कहर बरपाती रही। पर उन्होंने ग़ालिब की तरह न तो कभी अपनी ग़ुर्बत का ढोल पीटा और न वजीफ़े के लिए हाथ-पैर मारे। मुद्दतों बाद उनकी तनख्वाह 500 रूपये की गयी। ज़ौक़’ में ग़ालिब की तरह न तो कोई ऐब था और न ही वे दिलफेंक ही थे। वे सादगी पसंद थे। उम्र भर वह एक छोटे से मकान में रहते रहे। उनके कई शेरों से पता चलता था कि वह किस्मत को मानने वाले थे और मनुष्य के कर्म के दायरे मे ही रखते थे।
लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले
अपनी ख़ुशी न आए, न अपनी ख़ुशी चले
दुनिया ने किस का राह-ए-फ़ना में दिया है साथ
तुम भी चले चलो यूँही जब तक चली चले
बादशाह की उस्तादी मिलना तो शान की बात थी पर मुश्किलें भी कमतर न थीं। यदि ज़फर को कोई मिसरा (शेर की प्रत्येक पंक्ति को मिसरा कहते हैं, इस प्रकार एक शेर में दो पंक्तियाँ अर्थात दो मिसरे होते हैं) पसंद आ जाता, तो ज़ौक़ को उसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी दे दी जाती। या फिर बादशाह को कभी राह चलते कोई जुमला पसंद आ गया, तो उस पर शायरी करने का दारोबदार ज़ौक़ के जिम्मे होती। हज़ारों टप्पे, ठुमरियां, गीत, ग़ज़लें ऐसे ही बनीं और बादशाह की भेंट चढ़ गईं। उनका यह शेर उनकी मुश्किलों को बख़ूबी बयान करता है।
‘ज़ौक़’ मुरत्तिब क्योंकि हो दीवां शिकवाए-फुरसत किससे करें,
बांधे हमने अपने गले में आप ‘ज़फ़र’ के झगड़े हैं’।
शायद यही वजह भी रही कि जीते-जी वो कभी अपना दीवान (शेरों का संकलन ) नहीं छपवा पाए। और, कई बार ऐसा हुआ कि कभी ज़फ़र ने ज़ौक़ का कोई मिसरा सुन लिया तो उसी ज़मीन पर एक ग़ज़ल बना ली और भेज दी उनके पास सुधार के लिए। और ज़ौक़ की हालत ‘मरता क्या न करता’ वाली हो जाती। तो उनको अपनी शायरी जफ़र के नाम करनी पड़ती । इस वजह से ज़ौक़ ज़फर से अपनी शायरी छुपाया करते थे। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि ज़फर के जो चार दीवान छपे हैं, उनमें ज़ौक़ की शायरी की भरमार है। शायद इसी वजह से फैज़ अहमद फैज़ सरीखे शायर तो ज़फर को शायर ही नहीं मानते थे।
ज़ौक़ की शायरी और शख़्सियत के अलग रंग
शायरी मे फ़ारसी शब्दों के इस्तेमाल के सिलसिले में ग़ालिब और मोमिन का नाम अक्सर आता है। ज़ौक़ ने ज़्यादातर उर्दू में लिखा। उनकी उर्दू की शायरी ग़ालिब या मोमिन से किसी दर्ज़े कमतर नहीं है।. ज़ौक पर एक किताब ‘जौक और उनकी शायरी’ लिखने वाले प्रकाश पंडित कहते हैं कि वे आकारवाद के शायर थे। लफ़्ज़ों के सही इस्तेमाल और नज़्म की रवानगी में उनका कोई सानी नहीं था। उस्ताद ज़ौक़ इश्क़, हुस्न, और आशिक़ी के शायर थे।और उनका कमाल ख़ूबसूरती की बयानबाज़ी में नज़र आता है। इनके कलामों में सादा ज़ुबानी, हुस्नपरस्ती और मुहब्बत की कशिश मौजूद होती है।. विशुद्ध रूमानी ग़जलों की शायरी के वे उस्ताद थे। सटीक और नियमनिष्ठ अंदाज़गी के लिए उनकी शायरी अपने आप मे एक अलग स्थान रखती है। वह शायरी के स्थापित दस्तूर और शैली के दायरे में ही रहना पसंद करते थे। उससे कभी विचलित नहीं हुये। वह प्रयोगवाद में बिलकुल यकीन नहीं करते थे। उनके बाद उन की विरासत को उनके शागिर्द दाग़ देहलवी ही आगे ले गए। ज़ौक़ के शेर खुद उनके मुख्तलिफ अंदाज को बयां करते हैं।
वक्त-ए-पीरी में शबाब की बातें,
ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें,
फिर मुझे ले चला उधर देखो,
दिल-ए-खाना-खराब की बातें।
ज़ौक़ साधारणजन के शायर थे। उनकी शायरी में भी आम बोल-चाल की भाषा की प्रचुरता थी। उनकी शायरी का संकलन, कुल्लीयत-ए-ज़ौक़, हिंदुस्तानी मुहावरे और वाक्यशैली के सुगंध से भरपूर है। दिल्ली में प्रचलित आम जन की भाषा के शब्द जैसे – तूती बोलना, लहू लगा के शहीदों मे मिलना (शहीदी का ढोंग करना), घर का काटने को दौड़ना, और कुएं का प्यासे के पास जाना का प्रयोग उन्होंने अपने शेरों में बखूबी किया है।
है कफ़स से शोर एक गुलशन तलक फर्याद का,
खूब तूती बोलता है इन दिनो सय्याद का।
गुल उस निगाह के ज़ख़म-रसीदों में मिल गया,
ये भी लहू लगा के शहीदों में मिल गया ।
दिन काटा जाये अब रात किधर काटने को,
जब से वो पास नहीं, दौड़े है घर काटने को।
कहने लगा की जाता है प्यासा कुएं के पास,
या जाता है कुआं कहीं तिशना-दहन के पास।
कफ़स- पिंजड़ा या क़ैदख़ाना
तिशना-दहन- बहुत ही प्यासा
हालाँकि ज़ौक़ ने कभी शराब को मुंह नहीं लगाया था। फिर भी इसकी रूमानियत की बातें वे किसी ठेठ शराबी की तरह ही करते हैं। और अपनी रूमानी गज़ल के मकते (शायरी का अन्तिम शेर) में पढ़े-लिखों मुल्लावों को शराबखाने आने की नसीहत देते हैं।
ज़ौक़ जो मदरसे के बिगड़े हुये हैं मुल्ला,
उनको मैखाने में ले आओ सँवर जाएंगे।
इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद वो कभी अपने को अर्श पर नहीं देखते थे। और अपने से पहले के शायरों की कद्र मे कसीदे कहते थे। जैसे की शायर मीर को खुद से बेहतर बताते हुये कहते हैं कि
न हुआ पर न हुआ ‘मीर’ का अंदाज़ नसीब,
ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर ग़ज़ल मे मारा।
उर्दू आलोचना के उस्ताद शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी का मानना है कि ग़ालिब और मीर एक ही तरह के शायर थे। प्रकाश पंडित कहते हैं कि ज़ौक़ पर सौदा की शायरी का असर है। यहां बताना लाज़मी है कि सौदा और मीर समकालीन थे और दोनों की तनातनी ज़ौक़ और ग़ालिब के जैसी ही थी।
ज़ौक़ बड़े अच्छे गणितज्ञ और भविष्य वाचने वाले भी थे। उन्हें कुण्डलियां बनाना आता था। मौसिकी के ख़ासे जानकार और सूफ़ीवाद की समझ में उनकी गहरी पैठ थी। याददाश्त इतनी तेज़ कि एक बार जो पढ़ लिया वह ज़हन पर चस्पां हो गया। बताते हैं उन्होंने उस्तादों के लगभग 350 दीवान पढ़े थे।
ज़ौक़ को दिल्ली से दिली मुहब्बत थी। विकट परिस्थितियों मे भी वह ‘दाग़’ देहलवी या मीर के जैसे दिल्ली को छोड़ कर न जा सके। क़िस्सा है कि दक्कन के नवाब ने अपने दीवान चन्दूलाल के हाथों उन्हें चंद ग़ज़लें सुधार के लिए भेजीं और साथ में 500 रुपये और ख़िलअत (बहुमूल्य वस्त्र जिसे जिसे शाही व्यक्ति किसी प्रसन्न हो कर प्रदान करता था) देकर वहां आने का न्यौता दे डाला। ज़ौक़ ने ग़ज़लें तो दुरस्त कर दीं पर ख़ुद न गए। जो ग़ज़ल सुधार करके भेजी थी उसका मक़ता (गज़ल के अन्तिम दो मिसरे) था।
आजकल गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्र-ए-सुखन,
कौन जाये ‘ज़ौक़’ पर दिल्ली की गलियाँ छोड़कर।
दिल्ली की गलियाँ तो न छोड़ीं, पर हाँ, वे 16 नवंबर, 1854 को दुनिया से कूच कर गए। इंतकाल से तीन घंटे पहले उन्होंने यह शेर कहा था.
कहते हैं ‘ज़ौक़’ आज जहां से गुज़र गया
क्या ख़ूब आदमी था, ख़ुदा मग़फ़रत करे
मग़फ़रत- मोक्ष, मुक्ति
जीते जी एक भी दीवान नहीं छपा। जो कुछ भी लिखा उसमें से बहुत कुछ ज़फ़र को दे दिया। बाक़ी जो बचा, सत्तावन की ग़दर की भेंट चढ़ गया। जो रह गया, उसका हिसाब यह है-167 ग़ज़लें, 194 अकेले शेर, 24 क़सीदे, 1 मसनवी, 20 रुबाइयां, 5-6 क़ते, 1 सेहरा और कुछ अधूरे क़सीदे। जिसे देखकर उनके प्रतिद्वंदी ग़ालिब का शेर बहुत ही मौजूं जान पड़ता है।
चंद तस्वीरें बुतां, चंद हसीनों के ख़तूत,
बाद मरने के मेरे घर से ये सामां निकला।
कहते है कि कसिदागोई में ज़ौक़ का कोई सानी नहीं हुआ। उनकी लगभग 60 फीसदी रचनाएँ इसी विधा में लिखी गयीं है, जोकि अकबर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र के तारीफ में कही गयी थी। जिस कसीदे पर खक्कानी-ए-हिन्द की उपाधि मिली थे उस में 18 शेर 18 मुख्तलिफ़ भाषा और बोलियों में थे. उनकी शायरी में उनकी जबान पे पकड़ खुद-ब –खुद बयान हो जाता है. जैसे
हड्डियाँ हैं इस तन-ए-लाघर में खस की तीलियाँ,
तीलियाँ भी वो जो होवें, सौ बरस की तीलियाँ,
जोश-ए-गिर्या में हुआ ये उस्तख्वान-ए-तन का हाल,
जिस तरह गल जाती हैं पानी में खस की तीलियाँ।
तन-ए-लाघर- शरीररूपी घर
जोश-ए-गिर्या- आँसुओं की बाढ़
उस्तख्वान-ए-तन- शरीर की हड्डियाँ
और उनकी हड्डियाँ उनकी उसी प्यारी दिल्ली दफ़न की गयी जिससे वह जुदा नहीं होना चाहते थे। लेकिन यह दुःख की बात है जहाँ बल्लीमारन के गली कासिम जान मे गालिब की हवेली एक सांस्कृतिक धरोहर का रुतबा पाती है। और हर आते-जाते को गालिब का पुतला उसकी एतिहासिकता को ब्यान करता है। उसी दिल्ली में ज़ौक़ के मकान का कोई सुराग नहीं मिलता। और तो और 1961 में, शहर के कोर्पोरेशन ने उनकी कब्र को, जोकि पहाड़ गंज के मुल्तानी धांडा इलाके के गली नंबर 13 में ‘कूड़ाखत्ता‘ के नाम से थी, एक जन-सुविधा बनवा दिया। यह शौचालय यहाँ बीस साल तक रहा। फिर 1990 के दशक के अंत में, न्यायिक हस्तक्षेप के उपरांत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह जमीन अधिगृहित कर और शौचालय को तोड़ कर वहाँ एक एक छोटा सा स्मारक ‘यादगार-ए-ज़ौक़’ बनवा दिया। तिस पर भी इतने महान शायर के बारे में उस स्मारक पर कुछ भी नहीं लिखा है। उस इलाके में किसी ने में ज़ौक़ या उसके स्मारक का नाम तक नहीं सुना है। यह दुखद बात है की ज़ौक़ दिल्ली के लाल किले से कुछ ही दूरी पर एक परित्यक्त कूड़ा घर के पास ही दफ़न है। जिस दिल्ली की साहित्यिक दुनिया के वह एक समय बादशाह थे।