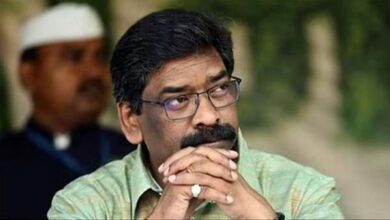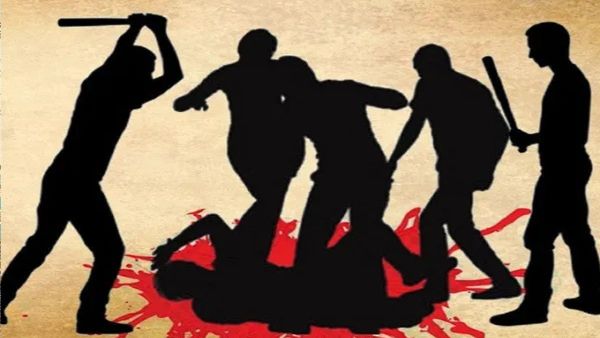हूल का साहित्यिक परिदृश्य
30 जून 1855 ई. का वह दिन, जिसके बाद न संताल परगना का, न झारखण्ड और न देश का इतिहास वैसा रहा जैसा उससे पहले था। महाजनों और अंग्रेजों के शोषण से उपजी इतिहास के गर्भ की छटपटाहट हूल का रूप लेकर जंगल की आग की तरह फ़ैल गयी थी। जिसने अंग्रेजों को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। भारतीयों को कमजोर और डरपोक मानने की उनकी सोच को संताल हूल से बड़ा झटका लगा था। चार भाई और दो बहनों के नेतृत्व में संतालों के साहस और जज्बे ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला डाली थी। इसी हूल ने बाद में उलगुलान का रूप लिया और फिर आज़ादी की लड़ाई की मजबूत सड़क की बुनियाद रची।
संताली हूल के इतिहासकार कल्याण हाड़ाम ने पश्चिम बंगाल संताली अकादेमी से प्रकाशित अपनी किताब ‘होड़कोरेन मारी हापड़ामको रेयाक् कथा’ में संताल हूल को याद करते हुए लिखा है कि सिदो-कान्हू का यह नारा कि ‘राजा-महाराजा को ख़त्म करो’, ‘दिकुओं को गंगा पार भेजो’ और हमारा राज्य हमारा शासन’ (आबुआ राज आबुआ दिसोम) का नारा संताल परगना के जंगल-पहाड़ में चारों तरफ गूँज रहा था। संताल, पहाड़िया और गैर आदिवासी जातियाँ जो यहाँ पहले से रह रही थीं वह सिदो-कान्हू के नेतृत्व में बाहर से आये महाजनों और अंग्रेजों के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई के लिए तैयार हो रहीथीं।
साहित्य के परिप्रेक्ष्य से संताली लोकगीतों-लोककथाओं में सिदो,कान्हू, चाँद,भैरव, फूलो और झानो के साथ-साथ हूल विद्रोह के कई अन्य लड़ाकों से सम्बंधित साहित्य दिखाई पड़ता है। आधुनिक संताली साहित्य में भी हूल और उनके शहीदों को लेकर रचनाएँ दिखाई पड़ती हैं। हिन्दी कविता या हिन्दी साहित्य पर अगर विचार किया जाए तो इस दृष्टि से थोड़ी निराशा हाथ लगती है। एक तरफ बिरसा और उनके आन्दोलन उलगुलान पर आधारित प्रचुर लेखन दिखाई पड़ता है।
न सिर्फ हिन्दी में बल्कि मराठी,बांग्ला सहित अन्य भारतीय भाषाओँ में भी बिरसा की उपस्थिति गौरतलब है। भुजंग मेश्राम ने मराठी में बिरसा पर कविता लिखी तो महाश्वेता देवी ने बिरसा के आन्दोलन पर ‘अरण्येर अधिकार’ जैसा प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। अंग्रेजी में भी बिरसा पर आधारित लेखन दिखाई पड़ जाता है। दूसरी तरफ हिन्दी साहित्य में सिदो-कान्हू और उनके हूल पर आधारित लेखन बहुत कम दिखाई पड़ता है। जबकि यह सच है कि सिदो-कान्हू के हूल की विरासत के बिना बिरसा का उलगुलान संभव न था। हूल का ही अगला कदम उलगुलान था और उसका परिणाम तात्कालिक तौर पर संताल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के रूप में दिखाई पड़ता है।


ऐसा नहीं है कि हूल पर आधारित या हूल से प्रेरित साहित्य बिलकुल नहीं है। हिन्दी कविता में झारखण्ड के अब जो कुछ नये नाम अपनी जगह बना रहे हैं वे अपनी कविताओं में हूल की क्रांतिधर्मिता को जगह दे रहे हैं। जसिंता केरकेट्टा और अनुज लुगुन कुछ ऐसे ही नाम हैं। बिनोद सोरेन संताली के एक समकालीन कवि हैं जिनकी कविताएँ संताली के साथ हिन्दी में भी प्रकाशित होती हैं। उनकी एक कविता ‘कुल्ही के धुल में हूल’ में वह बच्चों के खेल के माध्यम से यह बताते हैं कि संताल परगना की मिट्टी और धुल तक में हूल की आग बरकरार है और लगातार जल रही रही है। वे लिखते हैं कि खेलने के लिए बच्चे तय करते हैं कि-‘तय हुआ खेलेंगे ‘हुल’… /खड़े हो गये वे दो कतारों में/ एक तरफ गोरों की पलटन/ दूसरे सिदो-कान्हु के हूलगरिया’।
उनके अनुसार ये बच्चे भी सिदो-कान्हू की विद्रोही सेना के हुलगरिया यानि हूल में शामिल होने वाले दस्ते के ही सदस्य हैं। आदिवासी अपने इतिहास और उसके सबक को हमेशा नये-नये तरीके से संजो कर रखते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते जाते हैं। इस नजरिए से इनका इतिहासबोध आपको चौंका सकता है। हूल की आग जो निरंतर बोरसी के आग की तरह लगातार जलती रही इसे चंद्रमोहन किस्कू अपनी कविता में इस तरह दर्ज करते है –‘जब छीन-उजाड़ रहे थे / लोगों का घर-आंगन / कपड़े-लत्ते / हरियाली जंगल / खेत-खलिहान / और मिट्टी के अंदर का पानी/ तब हूल की आग जली।’
हूल को अक्सर सामाजिक और राजनीतिक असंतोष से जोड़कर देखा जाता है, जो इसका सबसे बड़ा पहलू भी है। परन्तु हूल को प्रकृति के साथ होने वाले विनाश की पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए। 1819ई की अपनी रिपोर्ट में सदरलैंड ने 1855 के हूल को देशी महाजनों और जमीदारों के अत्याचार का परिणाम बताया है। उसका मानना था कि अंग्रेजी सरकार आदिवासियों तक नहीं पहुँच पा रही थी इसलिए संतालों के साथ छल कपट और अन्याय हो रहा था। इसी कारण दामिन-ए-कोह यानि संताल परगना में विद्रोह फूट पड़ा। बड़ी चालाकी से सदरलैंड ने अपनी रिपोर्ट में हूल को भारतीयों द्वारा भारतीयों के खिलाफ किया गया षड्यंत्र बता दिया।
8 जून 1819 को सौंपे अपनी रिपोर्ट में लिखा-अंग्रेज आधिकारियों की अनुपस्थिति में बंगाली तथा अन्य दिकुओं का शोषण चक्र तेज हो गया था। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट जिसे दामिन-ए- कोह की जिम्मेदारी दी गयी थी वह सिर्फ देवघर में बैठता था और संताल इतनी दूर अपनी शिकायत उस तक पहुंचा नहीं पाते थे। इसलिए हूल जैसा विद्रोह हुआ। दूसरी तरफ इन्हीं अंग्रेजों ने सिदो-कान्हू को उपद्रवी के रूप में प्रचारित किया। अन्य आदिवासी शहीदों के प्रति भी इनका यही रवैया था।पर संताली भाषा के साहित्यकारों ने इस राजनीति का पर्दाफाश अपने रचनाओं में बखूबी किया है। जदुनाथ टुडू का ‘लो बीर’, रबीलाल टुडू का ‘बीर बिरसा’, कालीराम सोरेन का ‘सिदो-कान्हू हूल’ ऐसी ही कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं।


सामाजिक एवं आर्थिक शोषण के साथ प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ और इससे आदिवासियों के जीवन का प्रभावित होना भी हूल का एक प्रमुख कारण था। इस दृष्टि से हूल की प्रासंगिकता पर विचार किया जाना अभी शेष है। परन्तु ये कई इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि राजमहल की पहाड़ियों में रेल की पटरी निर्माण और और उससे होने वाले प्रकृति के विनाश का सम्बन्ध भी हूल से था। हूल सिर्फ बरहेट के भोगनाडी या सिदो-कान्हू और उनके भाई बहनों तक सीमित कोई आंदोलन नहीं था। इसमें पूरा संताल परगना और इसके लोग शामिल थे।
इसलिए हूल की आग 1855 तक भी महदूद नहीं है बल्कि विकास के लिए होने वाले विनाश का प्रतिकार के रूप में आज भी जीवित है। चंद्रमोहन किस्कू अपनी इसी कविता में लिखते हैं कि हूल की आग तब भी जलती है या जलनी चाहिए ‘जब छीन रहे थे/विकास के नाम पर/लोगों का हक़ और अधिकार/ जब कुचल रहे थे/निर्धन-गरीब लोगों को/ चौड़ी सड़क पर’। प्रकृति के साथ आदिवासियों का अटूट सम्बन्ध होता है। उसे भी हूल के आलोक में समझे और विश्लेषित करने की जरुरत है।
आज संताल परगना के साथ तमाम झारखण्ड और यहाँ के आदिवासियों की स्थिति बदहाल है। विकास की रफ़्तार जितनी भी तेज़ हो इन आदिवासियों तक नहीं पहुंची और पहुंची भी तो धक्का देने का ही काम ज्यादा किया। आज हूल की क्रांतिधर्मिता की लगतार हत्या यहाँ दिखाई पड़ रही है। जसिंता केरकेट्टा अपनी कविता ‘हूल की हत्या’ में लिखती हैं, “हाँ मैं वही गाछ हूँ / पंचकठिया-बरहेट के क्रांति स्थल का / वक़्त की अदालत में खड़ा / एक जीवित गवाह / जो पहचानता है / हूल के हत्यारों के चेहरे’। वह बरगद का पेड़ आज भी वहीँ खड़ा है जिस पर वीर सिदो को अंग्रेजों ने बेरहमी से फांसी पर चढ़ा दिया था। जसिंता के अनुसार बरगद का पेड़ हूल की उस सच्चाई का जिंदा सबूत है जो इतिहास को नींद में भी जगाये रखता है।
यह भी पढ़ें – स्वाधीनता आन्दोलन की पूर्वपीठिका ‘संथाल हूल विद्रोह’ (1855-1856)
अदालत द्वारा हत्यारों के चेहरों के बारे में पूछे जाने पर पेड़ बताता है कि उनका चेहरा हर काल में एक सा ही होता है और यह सुनकर अदालत की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती है। आज भी अपने राज्य में आदिवासियों को कितना न्याय मिल रहा है इस पर भी विचारे जाने और इसके वजहों को कायदे से खंगाले जाने की जरुरत है। हूल की आग हल्की जरूर पड़ी है पर मिटाई नहीं जा सकी है। हूल की हत्या संभव भी नहीं है। जब तक राजमहल की पहाड़ियों में आखिरी पेड़ और आखिरी आदिवासी बचा हुआ है तब तक यह लौ जलती रहेगी। इसलिए कवयित्री भी गहरे भरोसे के साथ यह लिखती हैं, ‘उसकी (सिदो) देह से अंतिम बार निकली पसीने की गंध / कुचले हूल की सिर उठाती गंध बन / बह रही जंगल की शिराओं में /पारे की तरह आज भी’।
इस एक पहलू पर भी विचार करना जरुरी है कि क्या कारण है कि संताल हूल या सिदो-कान्हू से प्रेरित या उन पर आधारित रचनाओं का हिन्दी में अभाव दिखाई पड़ता है। छोटानागपुर अंचल की तुलना में संताल परगना से बहुत कम ही साहित्यकार हिन्दी की पटल पर अपनी पहचान बना पाए हैं। पर ऐसा नहीं है कि संताल परगना से हिन्दी में लिखने वाले हुए ही नहीं। संताल परगना के पत्थरगामा के कवि ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादेमी जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। संताल परगना के कई नाम आज हिन्दी में सक्रिय हैं,पर उनकी रचनाओं में हूल की प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। आश्चर्य तो निर्मला पुतुल जैसी संताली कवियत्री के रचना संसार को देख कर होता है। उनके तीन कविता संग्रह के सौ से भी ज्यादा कविताओं में मात्र एक कविता सिदो -कान्हू की मूर्ति से हुई छेड़-छाड़ की एक घटना पर आधारित है। हूल की विरासत और प्रेरणा का इनके यहाँ भी अभाव ही दिखाई पड़ता है।
हिन्दी साहित्य का यह परिदृश्य थोड़ा निराशाजनक है पर उम्मीद की जानी चाहिए की निकट भविष्य में इससे प्रभावित साहित्य हिन्दी में भी दिखाई पड़ेगा। हाल के वर्षों में झारखण्ड के साथ देश भर में संताल हूल को लेकर नये तौर पर विचार-विमर्शों का दौर शुरू हुआ है। हूल के राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्त्व को स्वीकार किया जा रहा है और इतिहास के पन्नों को शिद्दत से टटोला जा रहा है। इससे इस उम्मीद को बल मिलता है कि हूल की आग, फूल बनकर जो जून 1855 में खिला था वह आगे और भी लहलहाएगा। समकालीन कवि अनुज लुगुन के शब्दों में इस उम्मीद को बेहतर ढंग से प्रकट किया जा सकता है, जिसमें अनुज हूल को फूल की संज्ञा देते हुए लिखते हैं – ‘तू फूल सिदो, कान्हू, तिलका, बिरसा, गोविन्द, तांत्या बाबा का / तुझे खोंसता हूँ तो उलगुलान नाचता है / तुझे पूजता हूँ तो जंगल लहलहाता है / खिला रहे यह फूल जंगल जंगल/ हूल हूल हूल हूल’।