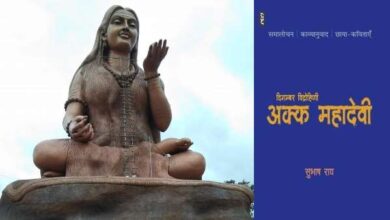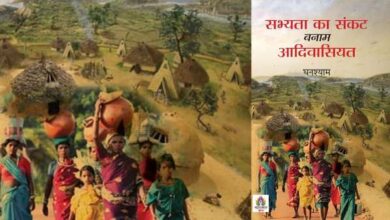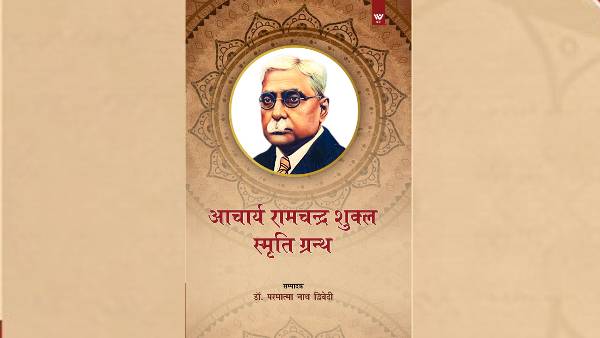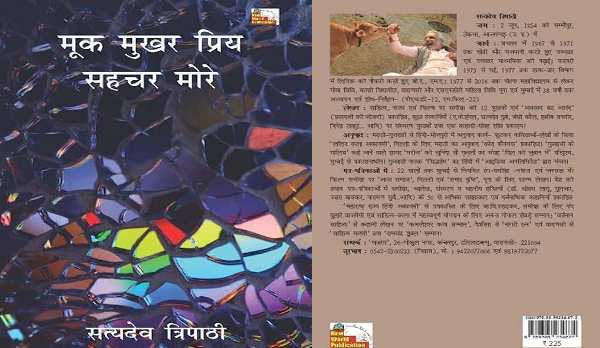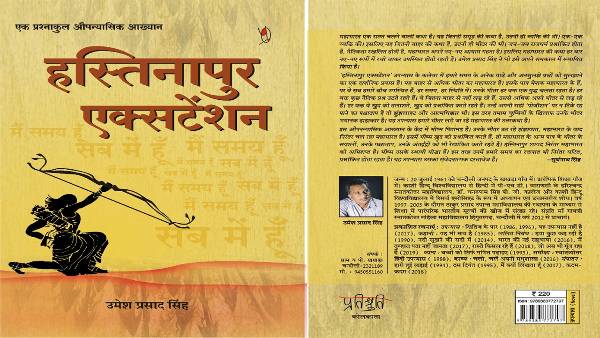पुरस्कारों के लिये सर्वथा निरापद एक सरियलिस्ट उपन्यास : ‘रेत समाधि’
आज कथा सम्राट प्रेमचंद की 143वीं जयंती का दिन है। सम्राट, अर्थात् हेगेलियन अवधारणा के अनुसार कथा जगत का ईश्वर। मनोविश्लेषण की भाषा में इस जगत की प्राणीसत्ता जिसके आत्म-विस्तार का ही प्रकृत रूप है आज का हिन्दी का कथा जगत।
फेसबुक पर अभी प्रेमचंद की परंपरा को लेकर एक फिजूल सी चर्चा के सिलसिले में एक मित्र ने प्रेमचंद को कहानी का मानक बताये जाने पर प्रश्न करते हुए यह मासूम सा सवाल उठाया था कि ‘मानक’ क्या चीज होती है ? उस पर हमने लिखा : ‘मानक वह बिंदु होता है जिससे धरती पर हम अपनी जगह को मापते हैं। अगर वह न हो तो हर कोई स्वयं-केंद्रित, खुद से उत्पन्न और खुद में ही समाप्त होंगे। प्रेमचंद से ही हिन्दी के आधुनिक कथा-साहित्य का वास्तविक इतिहास शुरू होता है, उसका अपना एक जगत बनता है।’
इसी साल पहली बार हिन्दी के एक उपन्यास, गीतांजलि श्री के ‘रेत समाधि’ को दुनिया का प्रतिष्ठित बूकर पुरस्कार मिला है। दक्षिणपंथ के भारी शोर के इस काल में भी गीतांजलि श्री के उपन्यास पर सबसे अधिक शोर उन लोगों ने ही मचाया, जो कहानी में प्रेमचंद की परंपरा के पक्के हिमायती हैं। अर्थात् हिन्दी कहानी में जो भी उल्लेखयोग्य है, वह अब भी प्रगतिशीलों के दायरे के बाहर नहीं है। यही है प्रेमचंद और हिन्दी कहानी की प्राणीसत्ता की बात का तात्पर्य। गीतांजलि श्री के उपन्यास को यह संस्पर्श इसीलिए तात्पर्यपूर्ण है।
जहां तक ‘रेत समाधि’ का सवाल है, हम नहीं जानते कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने बड़े चाव से, जिसे कहते हैं रस लेकर, डूब कर इस उपन्यास को पढ़ा होगा ! यह उपन्यास चाव से पढ़ने या डूबने के लिए लिखा ही नहीं गया है। इसका वह विन्यास ही नहीं है। यह प्रेमचंद के शिल्प की तरह कथ्य से स्वतः निर्मित किसी प्रमाता (subject) का एक पूर्ण विन्यास नहीं है। इसके विन्यास का अपना एक अलग सचेत लक्ष्य है। यह उपन्यास के एक कल्पित चौखटे में प्रमाता के बिखरे हुए अलग-अलग अंगों के जैविक बोध के आख्यानों का समुच्चय है।
किसी भी कथा में रस आता है प्रमाता (subject) के रूप में उसकी एक पूर्ण बोधगम्यता और अर्थवत्ता से, और प्रमाता में अर्थ की सृष्टि होती है उसके बाहर के संकेतकों से उसके संपर्क से। इसके विपरीत प्रमाता की अपनी शुद्ध प्राणीसत्ता का विषय मूलतः उसके अपने अंतर के जैविक बोध से जुड़ा होता है, जिसमें पूर्ण शरीर के बजाय उसके असंबद्ध अंगों का अवबोध होता है। इसमें होना हमेशा न होते हुए होना होता है। न अंतर की, न बाह्य की — किसी पूर्णता का यहां कोई अर्थ नहीं होता। मसलन्, मां हो या बेटी, दोनों पहचान के स्तर पर बस स्त्री हैं। यह स्त्री होने का एक जैविक बोध है। जाहिर है कि स्त्री मात्र होने में अनिवार्य तौर पर उनके होने के उस अर्थ की निश्चित क्षति होती है, जो ‘अन्य’ के क्षेत्र के संकेतक से संपर्क के जरिए बनने वाली कहानी के वितान से पैदा होता है, उनके मां अथवा बेटी अथवा बहन होने से पैदा होता है।

मसलन्, लेखिका के शब्दों में :
कहानी — अर्थात् जिसमें सरहद है, सरहद के आरम्पार है, औरत और सरहद के मेल से वह अपने आप चलती है, वह सुगबुगी है, उड़ती भी है, हवा की दिशा में, डूबते सूरज में भी, आगे जाती है, दाये बाये जाती है, घुमावती, बेहोश सी बढ़ती हुई, किस्से सुनाती सबके, ज्वालामुखी से निकलती, खामोशी से उभरती, भाप और अंगारों और धुए से फूटती स्मृतियों के किस्से समेटती।
औरत – यानी, पहले की और आज की भी। उसकी ख्वाहिशें भी।
मौत – महज एक सरहद को लांघने वाली।
दीवार – एक और सरहद।
शब्द – जो ध्वनि में अपने मतलब को झुला देते हैं।
ध्वनि – शब्द का मतलब झुठलाने वाली।
दरवाजा – अपने अस्तित्व के भूत, वर्तमान और भविषय के अंगों में बिखरा हुआ।
बेटी – जो हवा से बनती है। जिसकी साँस बालों पे आ गिरी नर्म पंखुड़ी थी, समुंदर में दहाड़ती चट्टान सी मारती है।…हवा चलती है, जैसे रूह भरती, सारे में लहराती, करवट बदलती तो चुड़ैल हो जाती, उस पर टूट गिरती।…सब औरतें, मत भूलना, बेटियाँ हैं।
बहन – धींगाधींगी की प्रयोगशाला में कैद कीड़ा।
बचपन – जब आसमान से जमीन अलग नजर नहीं आती थी। “अंडा फूटा…हिल…भाग…फिर हवा चलने लगी और बदल डालने लगी।” (यद्यपि आदमी का बच्चा ‘अंडा’ फोड़ कर निकलने के साथ स्वतः भाग नहीं पाता है।)
मोहब्बत – सेहत के माफिक नहीं। या तो वो निस्वार्थ है और तुम अपनी साँसे दूसरे को दे दोगी या वो खुदपसन्द है और तुम दूसरे की साँसें हड़प लोगी। इक खिला खिला इक मिटा मिटा।
माँ – सबका दुख हरने वाली महासतायी देवी। बेटे पर आश्रित।
बेटी – बाप पर आश्रित जो उसकी अंगूठी का पुखराज है। (हवा से बनी) “बच्ची की जवानी और जिन्दगी हवा में चकचूर हुए।”
जिन्दगी – एक पगदण्डी -हाईवे को जाती हुई।
चिल्लाना – एक परंपरा। प्रभुत्व की कहानी।
दयालुता – घर में मकसद, भाईचारे, प्रेम और सुख-शान्ति का जरिया।
इस प्रकार “चीटी, हाथी, दया, दरवाजा, माँ, छड़ी, गठरी, बड़े ये सब किरदार है।”
आदि, आदि …।
यह एक पूरा अध्याय ही देख लीजिए :
“शब्द की एक पौध। अपनी उसकी लहराहट। उसमें लुकी मुरादें। मरतों के ‘नहीं’ के अपने राज। ‘नहीं’ के अपने ख्वाब।
“इस तरह। कि एक पेड़ खड़ा जड़ा। पर थक तो रहा है उन्हीं उन्हीं चेहरों के साये में घिरने से, उन्हीं खुशबुओं के पत्तों से लिपटने पे, उन्हीं ध्वनियों की डालियों पे चहचह से। होते होते हो गया पेड़ की साँसस उखड़ती से और उसकी बुदबुद में ‘नहीं नहीं।
“मगर हवा है और बारिशश और ‘नहीं’ की फूँक उन में उड़ जो पड़ी है और एक कतरन का आकार भी पा गयी है। जो फरफर फहराती है, फिर फड़ फड़ फड़फड़ाती है और डाली पर मन्नत का फीता बना के उसे, हवा और बरसात मिलकर बाँध देते हैं। हर बार एक गाँठ और लगा देते हैं। एक और गाँठ। एक नई गाँठ। एक नई चाह। नई। नयी। हो जाना। ‘नहीं’ की नयी झंकार। फरफर फड़फड फड़क फड़क।
“तो पेड़ वही। सामने जो नजर में है। उसके तने पर और नीची झुकी डारियों पर धुएँ सी घूँघर ‘नहीं नहीं नहीं’, ऊपर लहराती उलझते ‘नहीं नहीं नई’ और फिर डालियाँ और फुनगियाँ जो हाथ है और उँगलियाँ, आसमान में चाँद को लपकती, ‘नई नयी’।
“या छत से। लपकती खिसकती। या दीवार से।
“जिसमें एक छिद्र मिल गया है, या बन गया है, जहाँ से नन्हा सा जीव, एक कतरा साँस की तरह, बाहर को सरकता। फूँक दर फूँक दीवार गिराता।” (पृष्ठ – 14)
इन सारे ब्यौरों में अन्य के क्षेत्र के संकेतक के संस्पर्श से निर्मित होने वाली एक ‘भ्रामक’ पूर्णता का बोध नहीं, अलग-अलग अंग-प्रत्यंगों की प्राणीसत्तामूलक पूर्णता के कटे-फटे समुच्चय का बोध होगा। सरियलिस्ट कला का यही मूल दर्शन है। सल्वाडोर डाली के चित्रों को देख लीजिए, कला के इस स्वरूप की ठोस सूरत नजर आ जाएगी।
ऐसे किसी भी कथानक में, जिसमें अधिक से अधिक बल प्रमाता की शुद्ध प्राणीसत्ता की ओर प्रेरित होता है, उसकी दिशा उसे संकेतकों से काटने, अर्थात् मूलतः उसके होने के अर्थ को सीमित करने की होती है। साफ शब्दों में कहें तो इसे एक प्रकार से प्रमाता के उस अर्थ के विरेचन की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, जिसे शास्त्रों की भाषा में माया कहा जाता है, जीवन के भ्रमों के इंद्रजाल को छांटने की प्रक्रिया। पर, कहानी की प्रकृति की विडंबना यह है कि यह इंद्रजाल ही जगत की उस बोधगम्य कथा को बुनता है, जिसका प्रमाता की प्राणीसत्ता के साथ ही उससे भिन्न कुछ और अर्थ भी हुआ करता है !
हम जानते हैं कि प्रमाता की प्राणीसत्ता के साथ संकेतक का संस्पर्श एक ओर जहां अवचेतन के उदय से मनुष्य में एक पूर्णता का बोध पैदा करता है, वहीं उसे उसकी जैविक प्राणीसत्ता से हमेशा के लिए काट भी देता है। स्त्री से उसके स्त्रीत्व के बोध का हरण करता है। प्रमाता की इस विच्छिन्नता को उसके बोधिसत्व के स्थायी अंत की वह आदिम परिघटना कहा जा सकता है जिसे, फ्रायडियन आवर्त्तन के सिद्धांत के आधार पर, फिर से प्राप्त करने के लिए ही उम्र के अंतिम वक्त तक मनुष्य तमाम प्रकार के आध्यात्मिक उपक्रमों में लगा रहता है। प्रमाता की जैविक प्राणीसत्ता की ओर प्रेरित होने की हर कोशिश इसी श्रेणी में पड़ती है। यह कला को एक आध्यात्मिक क्रिया मानने वाली खास अभिव्यंजनावादी शैली कहलाती है जिसमें किसी भी प्रकार के बाह्य उद्देश्य का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता है। जैविक अवबोध, जिसे अंतःप्रज्ञा का क्षण भी कहा जा सकता है, में सिर्फ संवेदना और आनंद की सहजानुभूतियां ही मूर्त हुआ करती हैं।
मनोविश्लेषक जॉक लकान ने अपने Ecrits में प्रमाता के बारे में लिखा था कि वह सर्वप्रथम जब mirror stage में अर्थ के बाहरी संदर्भ, अपनी चाक्षुस छवि के प्रति सचेत होता है, जो उसमें एक पूर्णता का बोध पैदा करता है, तभी इस पूर्णता के साथ ही उसमें अलगाव का एक अहसास भी पैदा होता है, अपनी जैविक प्राणीसत्ता से अलगाव का अहसास। प्रमाता दर्पण की भ्रामक छवि में ही अपनी एकजुट प्राणीसत्ता को देखता है, पर बोध के स्तर पर वह हमेशा के लिए अपनी आंतरिक जैविक अनुभूति को गंवा देता है।
ऐसे में जाहिर है कि जब जैविक प्राणीसत्ता के बोध को पाने के लिए किसी भी आख्यान में व्यापक अर्थ की तलाश कर रहे प्रमाता की बोधगम्य उपस्थिति को ही खत्म करने की कोशिश होती है, तो इसका एक अनिवार्य असर होता है कि वह प्रमाता के लिए ही असहनीय हो जाती है। इन तनावों से निर्मित पाठों में कुछ अलग प्रकार का खिंचाव जरूर पैदा होता है और यही वजह है कि व्यापक सामाजिक अर्थ के बजाय लेखन में प्राणीसत्ता के चयन के आग्रह का भी अपना एक महत्व होता है। कविता के विन्यास की तो मूल जमीन यही है। साहित्य में यथार्थवाद और भाववाद के बीच के सूक्ष्म फर्क की भी जमीन है। पर इस हल्की सी दरार में कविता के लिए तो यथेष्ट स्थान मिल जाता है, पर कहानी इसमें काफी निचुड़ कर, रूखी-सूखी हो जाती है !
कहानी में अर्थ के क्षय की हानि पाठ में रोचकता और प्रवाह के अभाव के एक बड़े कारण के रूप में सामने आती है। इसका औपन्यासिक विस्तार तो इसे और भी कठिन और उबाऊ बना देता है ! उपन्यास अपठनीय हो जाता है।
कहानी और कविता की प्रकृति का यह एक बुनियादी फर्क है कि कविता की दिशा प्रमाता की प्राणीसत्ता की तलाश की ओर होती है और कहानी की दिशा मूलतः कथा के बाहर के अन्य के क्षेत्र से जुड़ कर प्रमाता के विस्तार और उसके अधिक से अधिक अर्थों को प्रेषित करने की होती है। कहानी का वितान अन्य के क्षेत्र के संकेतों से बुने गए इंद्रजाल से और उसकी सार्थकता इस इंद्रजाल के भेदन के बिंदुओं से प्रमाणित होती है, पर कविता आम तौर पर अन्य के जगत का प्रत्याख्यान करती हुई प्रमाता में केंद्रीभूत होती है। निश्चित तौर पर महाकाव्यों का विन्यास अलग श्रेणी में पड़ता है।
कहानी पर कविता के हावी होने का अर्थ होता है, कहानी के अपने वितान के यथार्थ से उसे अलग कर उसकी प्राणशक्ति के एक बड़े स्रोत से उसे काट देना।
जब भी हम जीवन के संकेतकों के जरिए किसी स्त्री को मां अथवा बेटी के रूप में पहचानते हैं, उनके स्त्रित्व की प्राणीसत्ता पर एक पर्दा गिरता है, पर जब हम उन्हें शुद्ध स्त्री के रूप में देखते हैं तो उनके मां अथवा बेटी होने का कोई मायने नहीं रह जाता। वे अपने उस खास अर्थ को गंवाती हैं जो उनके बाहर के जगत के संबंधों से तैयार होता है। यह सचमुच किसी भी प्रमाता की विडंबना है कि उससे जुड़े हर आख्यान में वह अनिवार्य तौर पर स्वयं से विच्छिन्न अथवा कुछ न कुछ गंवाता ही है। उसके बाहर के क्षेत्र की क्रियाशीलता ही उसे उसकी प्राणीसत्ता से काटती है। और उसका अपना जैविक बोध संकेतकों से जुड़े उसके आत्म-विस्तार से, उसके होने के अर्थ के विस्तार की संभावना से काटता है।
‘रेत समाधि’ में कमोबेश यही बात, संकेतक के संपर्क से जुड़ कर पाए गए अर्थ को गंवाना, अपनी प्राणीसत्ता में सिमटना इस उपन्यास के सब चरित्रों और वस्तुओं के आख्यानों पर लागू होती है।
इस उपन्यास के विन्यास की और भी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि चरित्रों की जैविक अथवा किसी निश्चित प्राणीसत्ता की ओर प्रेरित इसका विस्तृत पाठ किसी एक चरित्र की अपनी धुरी पर टिका हुआ नहीं है। जैसे काव्यात्मक विन्यास वाले ही अल्बर्ट गार्सिया मार्केस का उपन्यास ‘ऑटम ऑफ पैट्रियार्क’ तानाशाहों की तमाम छवियों और कथा बिंबों के साथ तानाशाही की धुरी पर सख्ती से टिका रहता है। ‘रेत समाधि’ में परिपार्श्व की वैसी ही झांकियां कहानी की डगर और कठिन बनाती है। उन सबके सम्बद्ध-अर्थ को बस भाँप लेना होता है, अन्यथा भाषा के अन्य अनेक प्रयोगों की तरह वे सब चलती हुई रेल की खिड़की पर से सरपट गुजरती जाती है, उनसे एक गति के अलावा कोई चाक्षुस बिंब नहीं बनता। जिसे present continuous tense कहते हैं, किसी काम का जारी रहना, उस गति का एक क्षीण अहसास जरूर होता है।
इस उपन्यास में ‘सरहद’, जिसे कुछ लोगों ने इसका बीज शब्द भी कहा है, एक पर्दा है, चरित्रों के अभाव को ढकने, परिदृश्य को छिपाने और चरित्रों की गोपनीय लालसाओं को प्रकट करने और दृश्य के परे किसी और चीज़ के होने की संभावना को पेश करने वाला पर्दा। इन कामों के लिए सरहद या पर्दे के बिंब से बेहतर कोई दूसरा बिंब नहीं होता है। पर्दा प्रमाता के बाह्य का वह रूप है जो बिना किसी क्रिया के प्रमाता की प्राणीसत्ता को क्रियाशील कर सकता है। सरहद की मौजूदगी ही सरहद पार जाने की कामना को पैदा कर सकती है। जैसे पूर्णता के प्रथम बोध से जुड़ा प्रमाता का विच्छन्नताबोध ही स्वातंत्र्य के मूल्यबोध को मनुष्य की प्राणीसत्ता से अभिन्न रूप में जोड़ देता है।
कहना न होगा, माई की ‘नहीं’ और कुछ नहीं, उसकी प्राणीसत्ता से जुड़ा स्वातंत्र्य का मूल्यबोध है, जिसके बारे में लेखिका कहती है –
“ नहीं। बच्ची का ‘नहीं’ सबको बड़ा सुहाता। बचपन में वो ‘नहीं’ की बनी थी।
जब बचपन गया, पर उसका ‘नहीं’ उसके संग बालिग़ हुआ।”
हमने यहां ऊपर इस ‘नहीं’ के काव्यात्मक बयान का एक पूरा अध्याय ही दिया है।
‘रेत समाधि’ उपन्यास अनायास ही किसी को भी गीतांजलि श्री के ‘माई’ उपन्यास की याद दिला सकता है। उसमें गीतांजलि श्री कहती है, “कहीं है माई और वहाँ पूरी है, हम पकड़ के, शब्दों में बांधकर, उसे अधूरा न कर दें कहीं।” (पृष्ठ : 11) लेखिका वहां भी माई के बोधजगत में उसकी पूर्णता को शब्दों से व्याहत करना नहीं चाहती। पर यहां तो, पूर्णता के किसी भी बाह्य से उन्हें परहेज लगता है।
माई में भी पर्दा है,
“खिड़की-दरवाज़े पर टंगे परदे को देख कर हम अच्छी तरह जानते थे कि इसके पीछे एक पूरा, सजा-सजाया कमरा है …घर है…जहाँ किसी के जीवन का स्पंदन हर चीज़ को स्पर्श करता है। …यह तो हमने कभी न सोचा कि शून्य में फहराता पर्दा है, न उसके पीछे कुछ न आगे कुछ। कि बस उसी के फड़फड़ाते सन्नाटे में उलझके रह गए ?
“माई का पर्दा देख हमें उसके पीछे का ख़्याल ही न आया। “ (वही, पृष्ठ : 22)
पर वह पर्दा अन्यों के लिए है। वह पर्दा अन्यों से जुड़ कर एक अर्थ ग्रहण करता है।
‘माई’ के बाद ‘रेत समाधि’, जाहिर है कि किसी भी विषय पर एक समय के अंतराल के उपरांत लौटना, उस अंतराल को एक अलंघनीय चट्टान बना देता है। जहां तब थे, वहीं लौटना असंभव होता है। दरअसल, माई की कहानी लेखिका के अवबोध की कहानी थी। “हमें छोड़ कर माई थी ही नहीं।” वह प्रमातृत्व (subjectivity) की शैली थी। पर रेत समाधि प्रमाद की शैली है जो प्रमाता के अहम् से जुड़े उसके सवाल के रूप में सामने आता है। इसमें सवाल उठाने के लिए ही अपनी पहचान का प्रयोग किया जाता है। प्रमादग्रस्त स्त्री जानना चाहती है कि औरत होना क्या होता है ?
गीतांजलि श्री लिखती है — “‘नहीं’ से राह खुलती है। नहीं से आजादी बनती है। नहीं से मजा आता है। नहीं अहमकाना है। अहमकाना सूफियाना है।”
अर्थात् आजादी और अहमकपन में फर्क की लकीर बहुत महीन हुआ करती है। ऐसी स्थिति में जब सवाल विश्लेषण का आता है, मनोविश्लेषकों ने पाया है कि प्रमाता के अहम् के साथ समझौता करना बुनियादी तौर पर एक गलत शुरूआत होती है। इसका अंत परस्पर के साथ सिवाय छल के और कुछ नहीं होता। प्रमाता के साथ छल और प्रमाता का विश्लेषक के साथ छल। प्रमाता की आक्रामक आत्मरति से मुक्ति तभी संभव होती है जब प्रमाता की अपनी पहचान, उसकी प्राणीसत्ता अपने ही विरुद्ध खड़े होने का रास्ता बनाती है। वह संकेतक के लिए रास्ता होता है। इसमें प्रमाता के अहम् से जुड़े आदर्श की भी भूमिका होती है। वह प्रमाता के स्वातंत्र्य के मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों, अर्थात् उसके और प्रतीकात्मक जगत के बीच के संबंधों को सामान्य करता है। यहीं विचारधारा की भूमिका हुआ करती है।
बहरहाल, ‘रेत समाधि’ का पूरा विन्यास हमें एक बहुत सचेत विन्यास प्रतीत होता है, जिसमें शुरू से अंत तक लेखक की हरचंद कोशिश चरित्रों की यथार्थ पहचान को लुप्त करके उन्हें उनकी जाति-सत्ता में सिमटा देने की है, जिसे कि हमने बार-बार दोहराया है। इसमें न कोई मां है और न कोई बेटी, दोनों सिर्फ स्त्रियां है। चरित्र और वस्तुएँ हैं, पर असम्बद्ध, स्वयं-संपूर्ण। यह एक उतना ही सचेत विन्यास है, जैसा अंग्रेजी साहित्य की कींवदंती बन चुके आइरिश कवि जेम्स जॉयस के बारे में जॉक लकान कहते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं को कुछ इस प्रकार गढ़ा था ताकि जॉयस के ही शब्दों में “ अकादमिक्स के पास कभी काम की कमी नहीं रहे।” अर्थात्, जब तक विश्वविद्यालय व्यवस्था कायम रहेंगी, वह उनकी कविता के पाठों में ही सिर धुनती रहेगी।
लकान ने अपने लेख ‘James Joyce – A Symptom’ में जॉयस की कविता ‘फिन्ह्गन्स वेक’ (Finnegans Wake) का विश्लेषण करके बहुत गहराई से दिखाया था कि कैसे उसमें लेखक ने पूरी तरह से अपनी सनक के अनुसार शब्दों तक को अपनी मर्जी के हिसाब से ढाला था। अकादमिक दुनिया को ताउम्र व्यस्त कर देने का जॉयस के लेखन का वह एक अनोखा मिशन था। (देखें, अरुण माहेश्वरी, अथातो चित्त जिज्ञासा, पृष्ठ – 389-400)
इसीलिये, अंत में कहने की इच्छा होती है कि यह उपन्यास रेत समाधि कुछ इस प्रकार, सरियलिस्ट शैली में, अर्थात् कहानी पर चित्रकला की एक खास यथार्थ-विरोधी शैली को लाद कर लिखा गया है जो इसे पढ़ने के बजाय, पुरस्कार हासिल करने के लिए एक सर्वथा निरापद और उपयुक्त कृति बनाता है।
यह उपन्यास प्रेमचंद के यथार्थवादी आदर्शवाद पर टिके कथा साहित्य के पूर्ण नकार के बिल्कुल दूसरे छोर पर खड़ा है।