
‘अन्तिम किला’ के गिरने की चिन्ता
- रविभूषण
विगत दो वर्षों के भीतर न्यायपालिका, विशेषतः सुप्रीम कोर्ट को लेकर नागरिकों में ही नहीं, वहाँ के वकीलों और जजों में भी कई प्रकार की चिन्ताएँ देखने को मिली हैं। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जिन चार वरिष्ठ जजों ने प्रेस कान्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर आरोप लगाये थे, उनमें एक रंजन गोगोई थे। दीपक मिश्रा 42वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनके पहले भाजपा की सरकार के समय में जो चार मुख्य न्यायाधीश (जस्टिस राजेन्द्र मल लोढ़ा, 27.4.2014 – 27.9. 2014, जस्टिस एच. एल. दत्तू, 28.9.2014 – 2.12.2015, जस्टिस टी. एस. ठाकुर, 3.12.2015 – 4.1.2017 और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, 4.1.2017 – 27.8.2017) थे, उनका कार्यकाल विवादास्पद नहीं था। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार चार वरिष्ठ जजों (जस्टिस जे॰ चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ) ने प्रेस कान्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश पर गम्भीर आरोप लगाते हुए लोकतन्त्र के खतरे में होने की बात कही।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा मुख्य मामलों को लेकर गठित बेन्चों द्वारा दिये गये फैसलों को देखें, तो उनमें से कई सरकार के पक्ष में दिखाई देते हैं। इन दो वर्षों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के प्रति संदेह और अविश्वास कहीं अधिक बढ़ा है। जस्टिस रंजन गोगोई की, मुख्य न्यायाधीश बनने के पहले जो भूमिका थी, क्या बाद में वह उसी तरह बनी रही? मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद उनका कार्यकाल बेहद विवादास्पद रहा है। वे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश (3.10.2018 – 17.11.2019) थे। सेवा-निवृत्ति के मात्र चार महीने बाद सरकार ने उन्हें राज्य सभा का सांसद मनोनीत किया। राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्य बनाने का अधिकार है। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान देने वालों में से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का चयन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के. टी. एस. तुलसी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे, जिनका कार्यकाल 24 फरवरी 2020 को समाप्त हुआ। उस रिक्त पद पर जस्टिस रंजन गोगोई का चयन हुआ। 16 मार्च 2020 को गृह मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना (का.आ.1091 अ.) में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नामित किये जाने के बाद इस नियुक्ति पर लगातार विवाद जारी है। उनके पक्ष में यह तर्क दिया गया कि वे प्रमुख विधिवेत्ता और विधि विशेषज्ञ हैं, पर देश में कई और प्रमुख विधिवेत्ता हैं – के॰ परासरन और फली नरीमन जैसे।

अब रंजन गोगोई राज्य सभा के सांसद हैं। राज्यसभा में पहली बार किसी सदस्य के शपथ-ग्रहण के समय ‘शेम, शेम’ के नारे लगे और काँग्रेस सदस्यों ने वॉक आउट किया। प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता का है। राज्य सभा में उनकी नियुक्ति को ‘न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता के सिद्धांतों से समझौता’ कहा गया है। इसे इनाम(क्विड प्रो को) माना गया है क्योंकि रंजन गोगोई ने ऐसे कई फैसले दिये हैं, जो सरकार के पक्ष मे जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश बनने के पहले वे जो थे, क्या बाद में भी वैसे ही बने रहे? अगर नहीं, तो उनमें अन्तर क्यों आया? कैसे आया? मुख्य न्यायाधीश बनने के पहले जुलाई 2018 में तृतीय रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान में उन्होंने ‘दो भारत’ की बात कही थी और गरीबी की रेखा से नीचे जिन्दगी जीने वालों के लिए ‘विधि अदालतों’ को ‘उम्मीद की किरण’ कहा था। उन्होंने यह कहा था कि ‘इस संस्था को आम आदमी के लिए सेवा योग्य और राष्ट्र के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए और जमीनी चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी सुधार की नहीं, क्रांति की जरूरत है।’
यह भी पढ़ें – भारत हिन्दू राष्ट्र की ओर – रविभूषण
चार जजों की प्रेस कान्फ्रेंस में उनकी भूमिका साहसिक थी और इस व्याख्यान में उन्होंने स्वतन्त्र पत्रकारों और हल्ला बोलने वाले जजों की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता अलेक्ज़ेंडर हैमिल्टन (11.1.1755 या 57 – 12.7.1804) को उद्धृत किया था, जिन्होंने न्यायपालिका से डरने की बात कही थी। प्रेस कान्फ्रेंस में शामिल चार वरिष्ठ जजों में से जस्टिस टी॰ चेलमेश्वर और जस्टिस जोसेफ ने पद पर रहते हुए ही यह कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वे सरकार द्वारा दिया गया कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। न्यायपालिका की भूमिका कहीं बड़ी है। उसकी स्वतन्त्रता लोकतन्त्र का सुदृढ़ आधार है। प्रेस कान्फ्रेंस में वरिष्ठ जजों ने उसकी स्वतन्त्रता बाधित होते हुए चिन्ता प्रकट की थी और जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया था। उन्होंने केसों के आवंटन का मामला उठाया था। मास्टर ऑफ रोस्टर होने के कारण मुख्य न्यायाधीश ही किसी भी केस के लिए जजों की बेंच गठित करते हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा ने सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए मनोनुकूल बेन्चों का गठन किया था। उस समय जज लोया का भी मामला था।

भारतीय अर्थशास्त्री और वकील प्रो॰ के॰ टी॰ शाह (1888 – 1953) बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने संविधान-सभा में ही यह सलाह दी थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार की ओर से कोई कार्यकारी कार्यालय नहीं लेना चाहिए। इस सलाह को उस समय अम्बेडकर ने खारिज किया था कि जजों के ऐसे फैसलों में उनका कोई हित नहीं होगा। वे दिन कुछ और थे जबकि आज के समय की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। अम्बेडकर के समय में न्यायपालिका में अधिक विवाद और झगड़ा निजी होता था, जिस पर निर्णय होते थे। नागरिकों और सरकार के बीच केस की संख्या न के बराबर होती थी, जिससे न्यायपालिका द्वारा सरकार को फायदा पहुंचाने का कोई सवाल नहीं था। न्यायपालिका अधिक स्वतन्त्र थी। सरकार द्वारा न्यायपालिका के किसी भी सदस्य को प्रभावित करने की बात को अम्बेडकर ने दूर की बात कही थी।
यह भी पढ़ें – सामाजिक न्याय की राजनीति और दलित आन्दोलन
आज पहले जैसी स्थिति नहीं है। कोर्ट में सरकार सबसे बड़ी वादी है। अब स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 70 प्रतिशत जज को रिटायरमेंट के बाद कोई-न-कोई पद प्राप्त होता है। रिटायरमेंट के बाद जजों की पद-प्राप्ति की 5 श्रेणियों की बात कही गई है। पहली श्रेणी में यह पद सरकारी व्यवस्था में न होकर निजी जीवन में है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी॰ एस॰ ठाकुर और जस्टिस खेहर को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी श्रेणी में प्राप्त पद सरकार द्वारा न होकर न्यायपालिका द्वारा है। तीसरी श्रेणी में सेवा-निवृत्ति के पश्चात राजनीति में जजों की उपस्थिति है। इस श्रेणी में जज राजनीति से न्यायपालिका में आते हैं और न्यायपालिका से राजनीति में आते हैं। जे चेलमेश्वर जज बनने से पहले राजनीति में थे। वे रामाराव के विरोधी थे। के एस हेगड़े, जस्टिस छगला, जस्टिस बहरुल इस्लाम और के सुब्बाराव इसी श्रेणी के अंतर्गत हैं। पाँचवीं श्रेणी के अंतर्गत वैधानिक पद हैं। पाँचवीं श्रेणी को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रंजन गोगोई की राज्यसभा में नियुक्ति इसी श्रेणी में है।

रिटायरमेंट के बाद जजों को पद मुफ्त में या मात्र उनकी योग्यता के आधार पर नहीं दिये जाते। जिनके फैसले सरकार के पक्ष में होते हैं, सरकार स्वाभाविक रूप से उन पर मेहरबान होती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका ऐसी स्थिति में अपने स्वतन्त्र अस्तित्व में नहीं रहते। इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद मोदी के कार्यकाल में पिछले दो-तीन वर्ष से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता बाधित हुई है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष एम सी सेतलवाड (1884 – 1974) की अध्यक्षता में विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में जजों की सेवा निवृत्ति के बाद पद प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाने के लिएकानून बनाने की अनुशंसा की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों सहित प्रमुख दलों के सभी प्रमुख नेताओं के साथ बार काउंसिल ने भी अपनी सहमति प्रकट की थी, पर कोई कानून नहीं बना। अस्सी के दशक में मुख्य न्यायाधीश वाई वी चन्द्रचूड़ (16वें मुख्य न्यायाधीश 22.2.1978 से 11.7.1985 तक), पी एन भगवती (12 जुलाई 1985 से 20 दिसम्बर 1986 तक) और मुख्य न्यायाधीश आर एस पाठक (21 दिसम्बर 1986 से 18 जून 1989) ने भी इस मामले पर सेवा-निवृत्ति के बाद सरकार द्वारा दिये गए कसी भी पद पर न जाने सम्बन्धी कोई कानून नहीं बना। सब कुछ जजों की मर्जी पर निर्भर रहा कि वे रिटायरमेंट के बाद पद स्वीकार करते हैं या नहीं? ![Supreme Whispers: Conversations with Judges of the Supreme Court of India 1980-89 by [Abhinav Chandrachud]](https://m.media-amazon.com/images/I/51V0xu3Y52L.jpg)
![Supreme Whispers: Conversations with Judges of the Supreme Court of India 1980-89 by [Abhinav Chandrachud]](https://m.media-amazon.com/images/I/51V0xu3Y52L.jpg)
मुम्बई हाई कोर्ट के वकील और भारत के 19 पूर्व न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के 66 से अधिक पूर्व जजों के इंटरव्यू पर आधारित पुस्तक ‘सुप्रीम व्हिसपर्स : कन्वर्सेशंस विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया’(1980 -89) के लेखक अभिनव चन्द्रचूड़ ने अपने लेख ‘हिदायतुल्ला एक्जाम्पल’(इंडियन एक्सप्रेस, 18 मार्च 2020) में लिखा है कि जजों को यह स्वयं निर्णय लेना होगा कि वे सरकार द्वारा दिया गया पद कम-से-कम कुछ वर्षों तक नहीं स्वीकारें। रिटायर होने के कुछ समय पहले कई जज सरकार के पक्ष में फैसले देते हैं – रिटायरमेंट के बाद पद-प्राप्ति की प्रत्याशा में। इससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता बाधित होती है। 1970 में हिदायतुल्ला प्रिवी पर्स केस की सुनवाई कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस पर दिया गया फैसला उनका अन्तिम फैसला था| उस समय यह खबर थी कि सरकार उन्हें रिटायर होने के बाद वर्ल्ड कोर्ट में लोकपाल के पद पर नियुक्त करेगी | कई वकीलों और जजों ने उन्हें इस केस की सुनवाई ना करने का आग्रह किया था| हिदायतुल्ला ने ऐसे किसी भी ऑफर को ना स्वीकारने की बात की थी| कई वर्ष बाद जनता पार्टी की सरकार के समय उपराष्ट्रपति बने थे|

जस्टिस रंजन गोगई की राज्य सभा में नियुक्ति उन कई जजों की पूर्व नियुक्तियों से भिन्न है,जिनका हवाला दिया गया है| सेवा निवृत जजों की नियुक्ति नेहरू के समय से ही आरम्भ हो चुकी थी| फजल अली (1986 – 22.81959) 50के दशक के आरम्भ में सुप्रीम कोर्ट के जज (15.10.1951- 30.5.1952) थे| बाद में वे ओडिशा के तीसरे राज्यपाल (7.6.1952-9.2.1954) बने थे| जस्टिस एम.सी. छागला (30.9.1900-9.2.1981) बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (1947 से 1958 तक) थे| बाद में वे 1958 से 1961 तक अमेरिका में राजदूत, अप्रैल 1962 से सितम्बर 1963 तक यू.के. में हाई कमिश्नर, 21 एम्बार 1963 से 1966 तक केन्द्र में शिक्षा मन्त्री और 14 नवम्बर 1966 से 5 सितम्बर 1967 तक विदेश मन्त्री रहे| रंजन गोगई की राज्य सभा में नियुक्ति के पक्ष में जो पहले के कुछ उदहारण दिये गये हैं, उनकी नियुक्तियों और गोगई की नियुक्ति में अन्तर है| बहरुल इस्लाम (1.3.1988-5.21993) जज बनने से पहले कॉंग्रेस में थे| उन्होंने 1956 में कॉंग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी| वे राज्य सभा के सांसद 3 अप्रैल 1962 से 20 जनवरी 1972 तक थे| इसके बाद ही वे असम और नागालैण्ड हाईकोर्ट में जज और गोहाटी हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्ययाधीश बने| सुप्रीम कोर्ट में वे जज 4 दिसम्बर 1980 से 12 जनवरी 1983 तक थे |
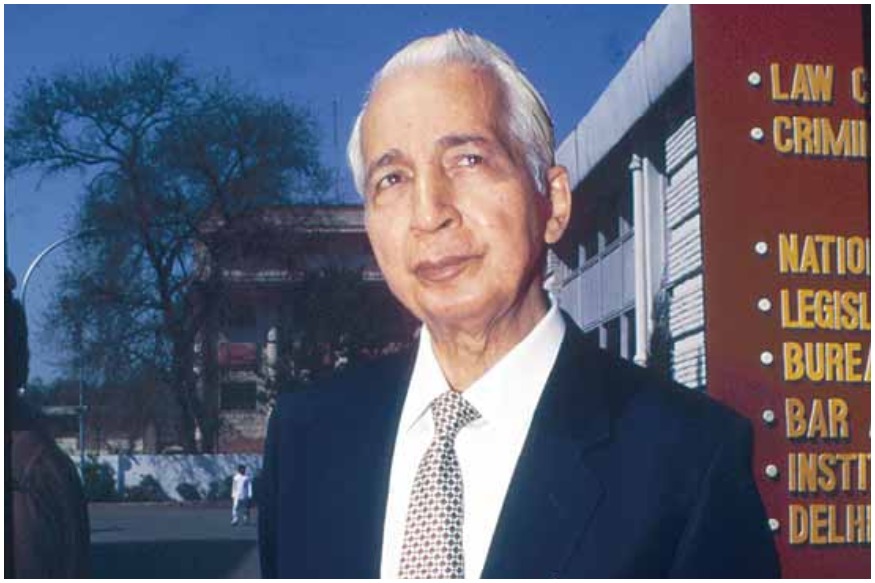
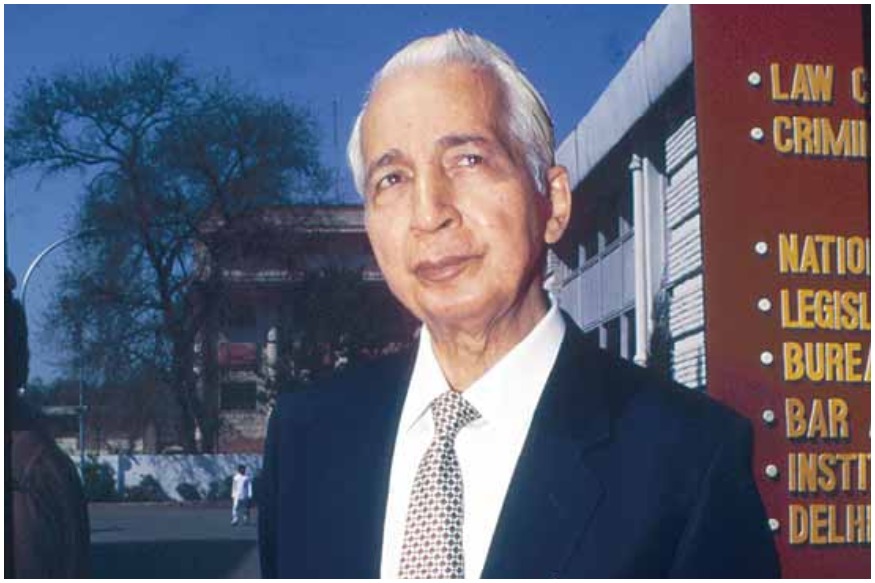
12 जनवरी 1983 को त्यागपत्र देकर वे लोकसभा चुनाव असम के बारपेटा से लड़ने पहुंचे पर 1984 में असम में चुनाव स्थगित रहा था, वे पुनः राज्यसभा में आये- बिहार कोपरेटिव घोटाले में जगन्नाथ मिश्र को ‘क्लीन चीट’ देने के बाद| सुप्रीम कोर्ट के नौवें मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बाराव (30.6.1966-11.4.1967) ने विरोधी दलों की ओर से चौथे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था| सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीबी रिटायर होने के बाद तमिलनाडु की राज्यपाल बनीं | 21 वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र और 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई की सेवा निवृति के पश्चात हुई नियुक्ति में अन्तर है| रंगनाथ मिश्र 25 सितम्बर 1990 से 24 नवम्बर 1991 तक मुख्य न्यायाधीश थे| छह सात वर्ष बाद वे कॉंग्रेस के राज्य सभा सदस्य 1998 में बने| इसके पहले वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे| 1984 में दिल्ली के सिख संहार पर गठित आयोग- जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग के वे अध्यक्ष थे| इस नरसंहार में उन्होंने कॉंग्रेस नेताओं को ‘क्लीन चीट’ दी थी| पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सताशिवम ने प्रजापति एनकाउंटर में अमित शाह को ‘क्लीन चीट’ दी थी| रिटायर होने के बाद वे केरल के राज्यपाल बने|
यह भी पढ़ें – राजनीतिक पराजय के बाद की पुकार!
रंजन गोगई ने पहले यह कहा था कि रिटायार्मेन्ट के बाद जजों की कहीं भी नियुक्ति बदनुमा दाग है| वे अपने कथन पर कायम न रहे| 2012 में जब केन्द्र में कॉंग्रेस की सरकार थी, अरुण जेटली ने जजों द्वारा रिटायर होने से पहले रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले काम से प्रभावित होने की बात की थी| 2013 में पीयूष गोयल ने भी इसी से मिलती जुलती बात कही थी| सेवा निवृति के बाद जजों के लाभान्वित होने पर काफी कुछ लिखा गया है| फली एस नरीमन ने इन्दिरा गाँधी के समय आपातकाल में न्यायपालिका की स्थिति पर प्रकाश डाला है| उनकी पुस्तक है ‘गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट’| सेन्टर फॉर पालिसी रिसर्च की सीनियर फेलो शैल श्री शंकर ने ‘स्केलिंग जस्टिस: इंडियाज सुप्रीम कोर्ट’ ( ओक्स्फोर्ड, 2009) सुप्रीम कोर्ट की न्याय विधि पर विचार किया है| 1999 से 2014 तक के केस का अध्ययन हुआ है और आने वाले दिनों में दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों – दीपक मिश्रा और रंजन गोगई के समय के फैसलों पर भी सम्भव है कोई पुस्तक प्रकाशित हो|

रंजन गोगोई की राज्य सभा में नियुक्ति की काफी आलोचना हुई है| 2018 में जब वे प्रेस कॉन्फ्रेस में थे, उस समय से आज कहीं अधिक लोकतन्त्र पर खतरा है| उनके सामने 43वें मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर का उदहारण था| जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने ‘आप’ पार्टी द्वारा राज्य सभा की सदस्यता का ऑफर ठुकरा दिया था| रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवम्बर 2019 तक मुख्य न्यायाधीश थे| मुख्य न्यायाधीश बन्ने के पहले उनकी जो छवि थी, बाद में उसके ठीक विपरीत हो गयी| अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक कनिष्ठ कोर्ट असिस्टेंट ने उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था| अपने केस में वे स्वयं बैठे| राफेल, अनुच्छेद 370, एलेक्ट्रोल बौंड, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा का केस, सबरीमाला, तीन तलाक, अयोध्या विवाद में विवादित जमीन पर राम मन्दिर निर्माण के पक्षs gurumurti में फैसला- सब सरकार के पक्ष में रहे हैं| दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले से भी जुड़ा मामला है जिस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता| एस. मुरलीधर के तबादले के पक्ष में कई जज नहीं थे| दिसम्बर 2019 और जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट कौलीजियम में उनके तबादले पर विचार हुआ था|


संघ विचारक एस.गुरुमूर्ति ने गौतम नवलखा वाले केस में उनके आदेश की आलोचना की थी| गुरुमूर्ति के ट्वीट पर हाई कोर्ट के जज हिमा कोहली और योगेश खन्ना ने उनपर अवमानना की नोटिस दी थी। इसी के बाद जस्टिस मुरलीधर के तबादले का जिक्र आया और 12 फरवरी 2020 को कालेजियम ने उनका तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया। 26 फरवरी को मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा के लिए सरकार और पुलिस को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और उसी रात उनका तबादला हो गया। जो जज सरकार के साथ नहीं है, उन्हें सरकार का कोपभाजन होना पड़ता है, जो सरकार के लिए फायदेमंद है, सरकार उन्हें सेवा-निवृत्ति के बाद इनाम( क्विड प्रो को) देती है। इससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता समाप्त होती है। रंजन गोगोई ने 19 मार्च को राज्यसभा में शपथ-ग्रहण के बाद ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ से हुई बातचीत में बिना नाम लिए आधा दर्जन लोगों के गैंग की बात की, जो जजों को फिरौती देते हैं। स्वतन्त्र न्यायपालिका के लिए इस गैंग का गला घोंटना जरूरी माना। गला घोंटने का काम न्यायपालिका ही करेगी, जिसमें मुख्य भूमिका मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों की होगी। उन्होंने राज्यसभा में अपने नामांकन को अहसान या तोहफा नहीं माना है, उन्होंने लॉबी द्वारा प्रत्येक संभव मार्ग से जजों को प्रभावित करने की बात कही। यह भी कहा जज शांति से रिटायर होना चाहते हैं। स्पष्ट है, कि ऐसे जजों को न्यायपालिका और संस्था से पहले अपनी चिन्ता है। शपथ-ग्रहण के पहले असम में एक न्यूज़ चैनल को उन्होंने एक समय विधायिका और कार्यपालिका को राष्ट्र-निर्माण के लिए एक साथ काम करने की बात कही थी। उन्होंने राज्य सभा में अपनी नियुक्ति को एक अवसर के रूप में देखा, जहां वे न्यायपालिका का पक्ष और उसकी बातें रखेंगे। उन्होंने जो भी कहा है, उसमें अर्थ नहीं है।

रंजन गोगोई की राज्यसभा में नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर तीव्र प्रहार है। जस्टिस मदन बी॰ लोकुर ने अंतिक किला के गिर जाने की बात कही है। विधायिका और न्यायपालिका का कुछ बिन्दुओं पर ही सही, एक साथ कार्य करना खतरनाक है। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब के कार्य निश्चित हैं। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के बिना लोकतन्त्र कायम नहीं रह सकता। रंजन गोगोई की व्यापक आलोचना के पीछे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, अखंडता के साथ संविधान और लोकतन्त्र की रक्षा का सवाल है। अनेक प्रमुख वकीलों, सेवा निवृत्त जजों ने उनकी आलोचना की है। राज्यसभा में उनकी नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर आघात है। प्रताप भानु मेहता ने उनके पद-स्वीकार को ‘शर्मनाक’ कहा है। अपने केस में स्वयं जज बनने को मेहता ‘पाप‘ कहते हैं। अपने लेख ‘द गोगोई बिट्रेअल’ (इंडियन एक्सप्रेस, 19 मार्च 2020) में उन्होंने लिखा है कि रंजन गोगोई ने राज्यसभा का पद स्वीकार कर जैसे यह संदेश दे दिया है कि कानून भारतीय नागरिकों की सुरक्षा नहीं करेगा क्योंकि इसने समझौता कर लिया है। अब सवाल यह है कि कानून में आस्था रखने वाले भारतीय नागरिक क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के ही एक वरिष्ठ जज कह रहें हैं कि किला गिर गया है। इसे न सरकार बचायेगी न कोई बाहर का आदमी। न्यायपालिका को बचाने का जिम्मा सबसे पहले न्यायमूर्तियों का है।
.










