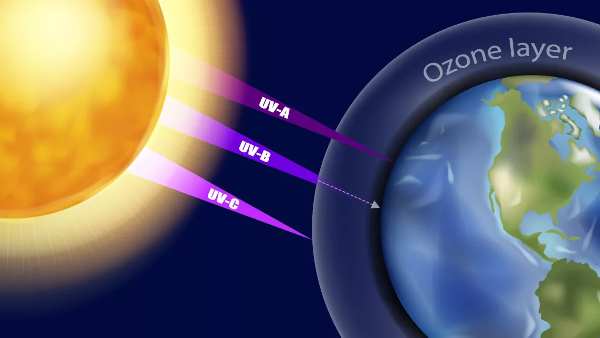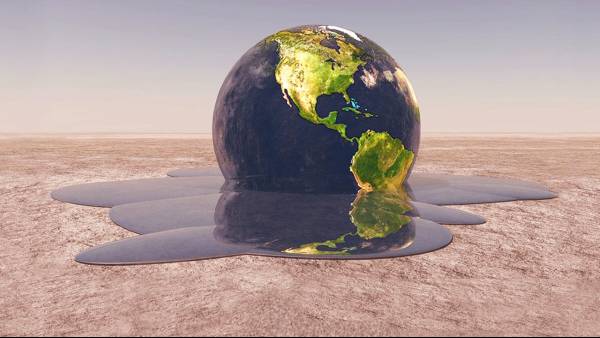पारम्परिक खेती : खाद्य सुरक्षा का विकल्प
मानव ने दस हजार वर्ष पूर्व खेती करना आरम्भ किया। उस युग में खेती करने के लिए सबसे पहले उगाए जाने वाले अनाजों में धान की खेती की गई क्योंकि इसकी खेती दूसरे अनाजों की तुलना में ज्यादा आसान थी। प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सरस्वती घाटी से पूर्वोत्तर की दिशा में सांवा (श्यामक) और धान की खेती होती थी क्योंकि धान की खेती करने के लिए हल की जरूरत नही होती इसके पौधों की रोपाई पानी से भरे जमीन में सीधे की जा सकती है। शायद इसी कारण नृतत्वशास्त्रियों का मानना है कि स्वत: उग आने वाले जंगली वनस्पतियों से प्रेरित होकर खेती का आविष्कार महिलाओं ने किया होगा।
प्रकृति की निकटता में रहने वाले आदिम जनजातियों में पुरूष और महिलाओं के कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया गया था जिसमें पुरूष घर से दूर शिकार व वन्य सामग्री एकत्र करने का कार्य करता था और महिलाएं घर पर रहकर संतानों की देखभाल के साथ भोजन व्यवस्था के लिए अपने आसपास की भूमि पर बीज बौने व उसे सींचना आदि का काम करतीं थीं। इसी क्रम में स्त्रियों द्वारा झूम खेती का आविष्कार किया गया होगा।
आरम्भिक युग में खेती करने के लिए किसी नुकीली लकड़ी या खंतीनुमा औजार का प्रयोग किया जाता था। उस युग में जोताई का काम भी स्त्रियां ही करती थी। इसका प्रमाण आदिम जनजातियों में उस मान्यता से प्राप्त होता है जब वर्षा करवाने के लिए इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात के समय स्त्रियां नग्न होकर हल खीचतीं थी और हलवाह भी स्त्रियां ही होती थी। इस विधि को करने के समय किसी भी पुरूष को उस स्थान पर जाने की अनुमति नही होती थी। यानि कृषि के आरम्भिक चरणों में हल खीचनें का काम पशु के स्थान पर मनुष्य करता था जिसमें महिलाएं भी अपना योगदान देती थीं। आज भी ग्रामीण भारत में लगभग 73.2% महिलाएँ कृषि कार्य करती हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि केवल 12% महिलाओं के पास खेत है।


भारत में खेती की कई आदिम प्रणालियां रही हैं। आदिम कृषि प्रणाली को भारत में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। उडीशा, बिहार और आंध्र प्रदेश में आदिम कृषि को ‘पोंडू’ कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में इसे ‘झूम खेती’ और छत्तीसगढ़ तथा बस्तर के क्षेत्र में यह खेती ‘पेंदा’ नाम से जानी जाती है। इसी तरह मध्य प्रदेश में बैगा अपनी आदिम खेती प्रणाली को ‘बेंवर’ कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए वेबर खेती जिसे झूम खेती भी कहा जाता है कि उपयोगिता आज सिद्ध होने लगी है। आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सुखी व समृद्ध किया है लेकिन पारम्परिक व अनुभवजन्य ज्ञान और विज्ञान आज भी महत्वहीन नहीं हुए हैं इसका उदाहरण है बैगा जनजाति द्वारा किए जा रहे पारम्परिक बैवर खेती जो आज पर्यावरणीय संकट को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं।
बैवर खेती पारम्परिक विज्ञान और लोक ज्ञान का अनुपम उदाहरण है। इस प्रणाली में कई प्रकार के बीजों का एक साथ उत्पादन किया जाता है। हर बीज अपने आप में बहुत सी भिन्नताएं और गुण लिए हुए होते हैं। जैसे एक बीज में अकाल सहने का गुण होगा, तो दूसरे में बाढ़ से मुकाबला करने का तीसरें में पाले से लड़ने की क्षमता होगी तो चौथा किसी अन्य प्राकृतिक संकट को झेलने की क्षमता रखता होगा। इसलिए बैगा एक साथ कई प्रकार के बीजों को रोपते हैं। ऐसा करने के पीछे उनके अपने अनुभवजन्य ज्ञान और खाद्य आवश्यकताएं होती थी। इस विधि की कृषि से एक साथ कई बीजों के रोपण द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के समय भी बैगाओं को साल भर के लिए ज़रूरी खाद्यान्न की कमी नही पड़ती थी।


बैवर खेती करने के लिए बैगा सबसे पहले खेती करने वाली जगह पर छोटी-छोटी झाड़ियों को काटकर बिछा देते हैं। झाड़ियों को अच्छी तरह से सूख जाने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। जब वे सूख जाती हैं, तब उनमें आग लगा दी जाती है। एक-दो दिनों तक झाड़ियां जलती रहती हैं। अंगारे धीरे-धीरे राख बनते रहते हैं। राख ठंडी होती जाती है। और यही राख खाद की तरह उनके खेतो को उर्वर बनाते हैं। बरसात आने से एक सप्ताह पहले राख की परत के नीचे कई प्रकार के बीजों को बो दिया जाता है। वर्षा का पानी पड़ते ही बीज अंकुरित होने लगते हैं और कुछ समय बाद फसल के रूप में तैयार हो जाता हैं।
बैगाओं की यह पद्धति ‘डाही घूंकना’ कहलाती है। इस प्रणाली में न तो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता और न ही कीटनाशकों का। यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है जिसे आज की भाषा में आर्गेनिक खेती कहा जा सकता है। इस पद्धति की खेती आदिवासी व जनजातीय समाज कई हजार वर्षों से करता आ रहा है। इस प्रकार की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में भी की जाती हैं – मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोतर राज्यों में झूम खेती करने की परंपरा अभी भी देखी जा सकती हैं। झूम की खेती करने के लिए किसान अपनी फसल को काटने के बाद अपने खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ देता है। खाली जमीन पर पेड़ व पौधे उग जाते है। जिन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता उन्हें सिर्फ जलाया जाता है और जब तक मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है, तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके बाद इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़-पौधे उग आते हैं। दूसरी जगह खेती के लिए वन भूमि को साफकर खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। लगातार एक ही स्थान पर खेती न करके थोड़े थोड़े समय के अंतराल खेती की जाती है। इस प्रकार झूम कृषि स्थानानंतरणशील कृषि है, जिसमें थोड़े-थोड़े समयांतराल पर खेत बदलते रहते हैं।
लेकिन बढ़ती जनसंख्या व परती भूमि के सरकारी संरक्षण व पर्यावरण बदलाव के कारण देश के उत्तर पूर्वी भाग में झूम खेती करने वाले किसानों ने खेती के अपने स्थान को बदलने का अंतराल कम कर दिया है। पहले खेती करने के बाद एक स्थान को 10-15 वर्षो तक छोड़ा जाता था लेकिन अब मजबूरी में 5 वर्ष बाद खेती के लिए पुनः उसी जमीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। भूमिका की उर्वरता कम होने में खाद की समस्या भी एक वजह है। वन संरक्षण अधिनियम के कारण जमीन व जलावन के लकड़ी की कमी के कारण अब किसानों को गाय या भैंस के गोबर से बने उपलो का उपयोग करना पड़ता है जबकि पहले यह गोबर किसानों की खेती के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे लेकिन अब इसमें कमी आ गई है।


कुल मिलाकर भूमि, जल , वनस्पतियों और जानवरों से जीवन के रूप में प्राप्त संसाधनों का काफी तेजी से दोहन किया जा रहा है। पहले मानव समाज विवेक और सीमित जरूरतों के लिए ही प्रकृति संसाधनों का उपयोग करता था लेकिन अब औद्योगिकीकरण , शहरीकरण व बढ़ती जनसंख्या के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का मात्रा से अधिक दोहन होने लगा है। जंगल पहले आदिवासियों के संरक्षण में थे। जंगल आदिवासी समाज की सम्पत्ति मानी जाती थी इसलिए इसके उपयोग के अपने नियम व कानून थे लेकिन औपनिवेशिक काल में वन व कृषि भूमियों पर सरकार का नियंत्रण होने लगा। वर्ष 1864 में स्थापित इम्पीरियल फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विभिन्न वनमंडलों द्वारा वनों को ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन कर दिया गया।
इस अधिनियम द्वारा वनों को तीन श्रेणियों- आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और ग्राम वनों में वर्गीकृत करके वनवासियों द्वारा वनोपज के संग्रहण को विनियमित करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के साथ वनों पर राज्य नियंत्रण स्थापित करके वन पर स्थानीय नागरिक के अधिकारों को प्रतिबंधित करके वनोपज संग्रहण को अपराध की श्रेणी में लाया गया और कारावास तथा जुर्माने द्वारा दंडित करने का प्रावधान किया गया। यानी अब वन राज्य की संपत्ति है। ब्रिटिश वन प्रबंधक यह मानते थे कि झूमखेती वनों को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि वनों पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा झूम की खेती को लेकर आम लोगों में ये दुष्प्रचार किया जा रहा था ताकि आदिवासी व जनजातिय लोग अपने पारम्परिक खेती को छोड़कर वन पर अपने आदिम अधिकारों को भी छोड़ दें।


झूम खेती को रोकने का पहला गंभीर प्रयास 1860 के दशक में किया गया। इसके पीछे इस प्रांत के चीफ कमिश्नर रिचर्ड टेंपल ने मुख्य भूमिका निभाई। इनका मानना था कि झूम खेती पुरानी सभ्यता से जुड़ी प्रथा है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार बैगा लोगों को झूम खेती छोड़ कर हल द्वारा खेती करने के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया गया। इसके कारण कई स्थानों पर झूम खेती से उनकी फसलों को खेतों में ही बर्बाद कर दिया गया। जब बहुत से बैगा आदिवासी पड़ोस की रियासत में भाग गए तब सरकार ने कुल्हाड़ी खेती की आदत को धीरे-धीरे खत्म करने की नीति अपनाने की सलाह दी। क्योंकि बैगा लोग पेड़ों को काटने और वन उत्पादों को एकत्रित करने में पारंगत थे और वन विभाग इन लोगों के श्रम पर निर्भर था इसलिए वन विभाग ने 1890 में बैगा चक की स्थापना की। यह जंगल 23920 एकड़ में फैला हुआ था।
सरकार ने झूम खेती करने वाले सभी लोगों को यहां बसाया और उन्हें झूम खेती करने की अनुमति दी। लेकिन अन्य स्थानों पर ब्रिटिश सरकार झूम खेती करने वाले किसानों को हतोत्साहित करने की नीति पर बल देने लगी। फिर भी बैगा लोगों ने हल द्वारा खेती के करने के बजाय झूम खेती को ही अपनाया। क्योंकि वह धरती को मां कहते है और मां के सीने पर हल नहीं चलाने की धार्मिक मान्यता ने बैगाओ को झूम खेती से जोड़े रखा। इस जनजाति के लोग हल के बिना ही जंगल में खेती लायक जमीन पर बीज का छिड़काव कर देते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले फसल से वह जीवनयापन करते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार मां अपने पुत्र का किसी भी परिस्थिति में पेट भरती और संरक्षण करती है। उसी प्रकार धरती भी हमारे लिए अन्न उगाती है जिससे हम अपना पेट भरते हैं।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में 250 मिलियन से अधिक आबादी अपनी जीवन निर्वाह के लिए स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है। अत: धुमंतु व आदिवासी लोगों की खाद्य सुरक्षा की दिशा में झूम या स्थानांतरित कृषि के लिए परती भूमि के पुनरुद्धार को कानूनी मान्यता देकर उनके उपयोग के लिए स्थानीय निवासियों को प्रेरित किया जाना चाहिये और इससे होने वाले उपज को उन समूहों में बांट दिया जाना चाहिए जो स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि एक प्रकार से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है भले ही इससे पर्याप्त नकदी या धन की प्राप्ति नहीं हो सकती लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जी रहे उन किसानो को जो उर्वरक या कृषि उपकरणों को खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वे किसान स्थानांतरित खेती द्वारा अपने परिवार की खाद्य जरूरतों को पूरा कर सकतें हैं। वास्तव में झूम खेती को आर्गेनिक खेती का विकल्प बनाया जा सकता है और कीटनाशक व अन्य कृत्रिम खाद्य प्रयोग के कारण हो रहे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए स्थानांतरित खेती अपनाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित किया जा सकता है।