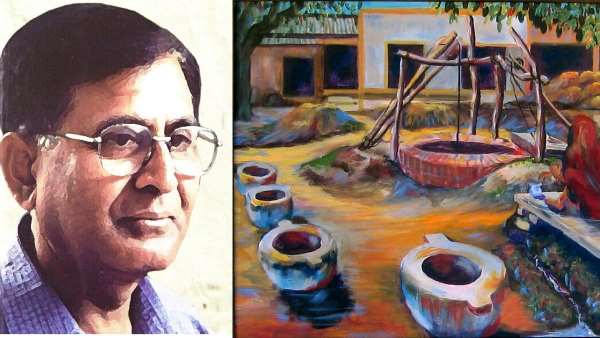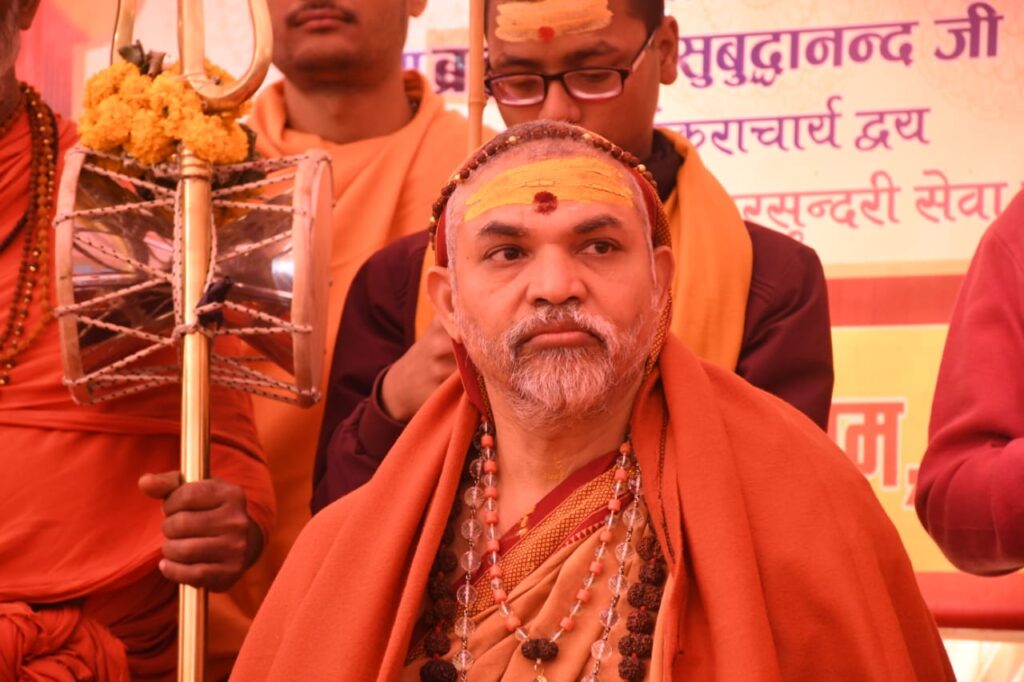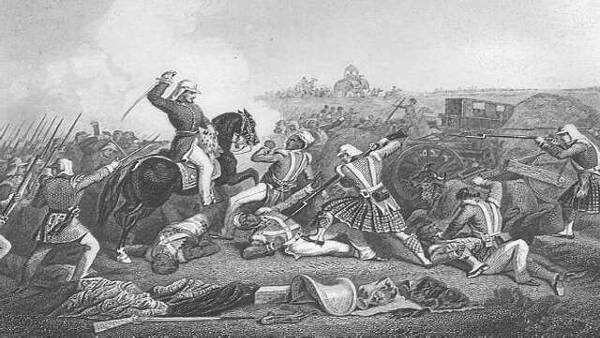आसान नहीं दिख रहा वैश्विक बाल श्रम उन्मूलन की राहें
बाल श्रमिक एक ऐसा शब्द है जिसके जिह्ना पर आते ही एक ऐसी तस्वीर आँखों के सामने तैरने लगती हैं जो अन्तर्मन में करूणा जगा जाती है। चकाचैंध की दुनिया से बेखबर ढीला ढाला कुर्ता पहने नन्हें बच्चें अपने हाथों मे पकड़े बोरियों मे टनन-टनन बजती हुइ रम व बियर की बोतलें मानों झुकी हुई उनकी पीठ की रीढ़ से वार्तालाप करती हो- “कैसे हो, कैसा है मण्डी का हाल।” परन्तु वह अपनी धून में मशगूल बढ़ता चला जाता है। इनकी नजरें इस वक्त बड़ी तीक्ष्ण हो जाती हैं। सडकों और नालियों से प्लास्टिक औरे काँच के टुकड़े झपट कर बोरी मे भरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है विचरते लोगों में कोई यह न पूछ बैठे कि बोरी मे क्या डाला दिखलाओ?
ऐसी बात नहीं कि बाल श्रमिक सिर्फ हमारे देश मे ही हैं। सबसे अधिक ऐसे बच्चे विदेशों में हैं जो मजदूरी के नाम पर अत्यधिक शोषित किए जाते रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि दक्षिणी देशों के अतिरिक्त दुनिया भर के देशों में ऐसे कामगार बच्चे जिनकी आयु 5 से 14 वर्ष की रही है, पेट की भूख और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वे ‘क्लब, कैफे, बार, डिस्को, बाग-बगिचों, ढाबा, चाय दुकानों, होटलों एवम् कारखानों इत्यादि में अपना बचपन कोड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हैं।
शायद हममे से बहुतों को यह बात मालूम नहीं होगा कि उन्नीसवीं सदी के मध्य मे लंदन शहर मे रेल की पटरियाँ बिछाने से लेकर चिमनियों को साफ करने का काम बच्चे ही किया करते थे। बाल मजदूर के रूप में उन दिनों चार – पाँच साल का बच्चा जो अभी तुतला कर बोलता है शहर की गलियों में फेरे लगाता हुआ कहता है- ‘वीप वीप!’ अथार्त कहना चाहता है ‘स्वीप’-’स्वीप’ यानी झाड़ू-बुहारू। परन्तु मुँह से निकलता है ‘वीप’। वहसिपन की हद तो तब होती थी, जब घरों के चिमनियों को साफ करने के लिए बच्चों को उसमें घुसाया जाता था। चूँकि चिमनियाँ पतली होती थी इसीलिए उनकी सफाई हेतु दुबले पतले बच्चे ही उसमें घुसेड़े जाते थे। जिससे इनका दम घुटने लगता था। चिमनियों के कालिख गले, नाक और मुँह इत्यादि मे फँस जाती थीं। जब बच्चे को चिमनी में जल्दी ऊपर सरकने की हिम्मत नही पड़ती थी, तो नीचे लुत्ती लगा दी जाती थी। और तब उस चिमनी में घुसा बच्चा आग- धुएँ के डर से आगे सरकता चला जाता था। उनके सरकने से तंग चिमनियाँ साफ हो जाती थी। लेकिन यह क्रम अधिक दिनों तक नहीं चल पाता था और वह बाल मजदूर जल्दी ही चमड़ी के कैंसर और टी.बी. से आक्रांत होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। जिसे जानकर आज हमारी रूहें काँप जाती है।
आज भी दियासलाई, पटाखें और कालीनों के कारखानो में कम मजदूरी के लालच मे तरह-तरह के जानलेवा ख़तरों के आगे खड़ा कर दिया जाता हैं। जिन्हें अभी साफ-साफ बोलना भी नहीं आया, जिनके दूध के दाँत भी नहीं टूटे हैं, उन्हें इन चिमनियों में घुसेड़े जाते हैं। ऐसे बच्चों को धन्धों मे लगाकर लोग अपनी तो मोटी कमाई कर रहे हैं, परन्तु इन मासूमों और लाचार बच्चों की इह लीला फलने-फूलने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। इस उम्र में बच्चे को न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेवारी रहती है। बस हर वक्त अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना-कूदना और पढ़ना ही एक मात्र दिनचर्या होनी चाहिए। परन्तु गरीबी, लाचारी और माता-पिता की प्रताड़ना के चलते आज लाखों बच्चे बाल-मजदूरी के इस दलदल में धसते चले जाते हैं।


आज दुनिया भर में सैकड़ों मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जिनका समय स्कूलों में, कॉपी-किताबों और दोस्तों के बीच बीतनी चाहिए वह होटलों, घरों, उद्योगों, चाय दुकानों, झाड़ू पोछा और औजारों के बीच बीताने को मजबूर हैं। बड़े शहरों के अतिरिक्त कुछ छोटे शहरों में भी हरेक गली-मुहल्ले में कई छोटू, राजू, चवन्नी और मुन्ना मिल जायेंगे जो हालातों के चलते बाल-मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके हैं। साथ ही यह बात सिर्फ बाल-मजदूरी तक ही सीमित नहीं हैं। इसके साथ ही बच्चों को कई धिनौने कुकृत्यों का भी सामना करना पड़ता है। जिनका बच्चों के मासूम मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके मद्देनजर कई स्वयं सेवी संस्थाएं (एन.जी.ओ) समाज में फैली इस कुरीति को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास करते नजर आते हैं। इन एन.जी.ओ. के अनुसार 50.2 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह के सातो दिन काम करते हैं। 52.22 प्रतिशत यौन प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं साथ ही 50 प्रतिशत बच्चे शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं।
बाल मजदूरों की इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया था जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया। साथ ही रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई। इसके साथ ही सरकार ने नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के रूप में बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा चुकी है। जनवरी 2005 में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों के 250 जिलों तक बढ़ाया गया। चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम की सफलता हेतु सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है, लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई पड़ रही है। बच्चों के माता-पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उनके जाने से परिवार की आमदनी कम हो जाएगी। माना जा रहा है कि आज 60 प्रतिशत बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं। अगर ये आंकड़े सच हैं तो सरकार को अपनी आंखे खोलनी होगी।
आंकड़ों की यह भयावहता हमारे भविष्य का कलंक बन सकती है। भारत में बाल मजदूरों की इतनी अधिक संख्या होने का मुख्य कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीबी है। यहाँ एक तरफ तो ऐसे बच्चों का समूह है जो बड़े-बड़े महंगे होटलों में 56 भोग का आनंद उठाते हैं और दूसरी ओर ऐसे बच्चों का समूह है जो गरीब और अनाथ हैं, जिन्हें भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता। दूसरों के जुठनों के सहारे वे अपना जीवनयापन करने को विवश हैं।


पिछ्ले 20 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई है। दुनिया भर में 10 में से एक बच्चा काम कर रहा है, जबकि लाखों और बच्चे पिछले दो वर्षों से पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण जोखिम में हैं। पिछ्ले दिनों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कहा है कि वर्ष 2016 में बाल श्रमिकों की संख्या 152 मिलियन (15.2 करोड़) से बढ़कर 160 मिलियन (16 करोड़) हो गई है। इसमें जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के कारण अफ्रीका में सबसे अधिक कामगार बच्चों की वृद्धि हुई है। यूनिसेफ की हेनरीटा फोर ने 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस से पहले कहा था कि वे बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में निर्धारित लक्ष्य को खो रहे हैं और इन दिनों इस लड़ाई को और भी मुश्किल कर दिया है।’
साथ ही वैश्विक लॉकडाउन के दूसरे वर्ष में स्कूल बंद होने के कारण और आर्थिक संकट ने दुनिया भर के परिवारों को और भी बदतर जीवन यापन करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम विफल होता दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करना और 2025 तक इस प्रथा से निजाद पाने में अभी अनेकों बाधाओ का सामना करना पड़ सकता है । अतः बाल श्रम उन्मूलन हेतु तत्काल बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के चलते उतपन्न आर्थिक झटके और विद्यालयों के बंद होने के कारण बाल मजदूरों को अब अत्यधिक समय तक, और बद से बदतर परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है, जो दुनिया भर के लिए एक चिन्ता का विषय है। जहाँ तक भारत की बात है सयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को 2030 ई. में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की जो प्रतिबद्धता जताई है, वह भी मुश्किल लग रही है।
इस आन्दोलन में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की अग्रणी भूमिका रही है। श्री सत्यार्थी ने अब तक बाल श्रमिकों की समाप्ति हेतु और बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकारों के लिए वैश्विक आन्दोलन निर्माण में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। उन्होंने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और एक ऐसी दुनिया के निर्माण का सपना देखा है, जहाँ हर बच्चे को स्वतन्त्र, स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार मिल सके। उनके इसी योगदान के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें एस.डी.जी. एडवोकेट बनाया है, जो देश के लिए गौरव की बात है। परन्तु श्री सत्यार्थी को एस डी जी एडवोकेट ऐसे समय मे बनाया गया है, जब पूरी दुनिया में बाल श्रम में अभूतपुर्व वृद्धि देखने को मिली है।