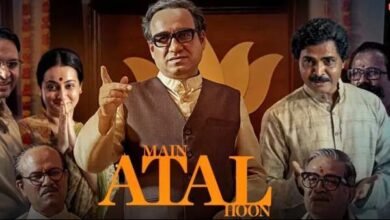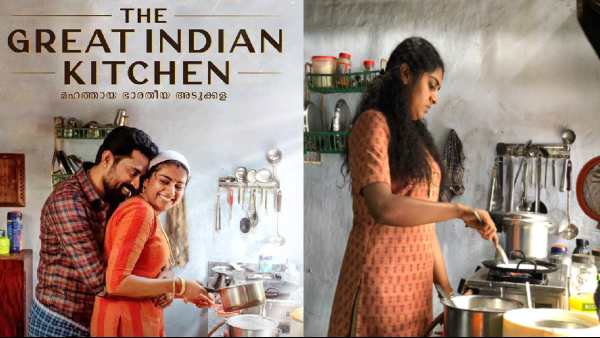
अन्नपूर्णा का अपूर्ण आख्यान ‘द ग्रेट इंडियन किचन’
{Featured in IMDb Critics Reviews}
भारत देवियों का देश है और हमारे घरों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है, अन्नपूर्णा देवी। रसोईघर घर का अभिन्न अंग है अन्नपूर्णा देवी की प्रतिष्ठा यहीं होती है विवाह के उपरान्त वह सभी को कुछ पकवान बनाकर परिवार को भोग लगाती है जी हाँ उसे भोग नहीं लगाया जाता। और पास होने पर ताउम्र वह सभी का पोषण करती रहती है तभी अन्नपूर्णा कहलाने की अधिकारिणी बनती है अन्यथा…। हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों में परोसी जा रही हिंसा, अनैतिकता, गाली-गलौज की कटु आलोचना करते हैं, जो बड़ी ही सहजता से घर-घर में घर कर चुकी हैं लेकिन इसी माहौल में संवेदनशील व अनिवार्य मुद्दों को उठाने वाली फिल्में भी आती हैं जिन पर कम बात होती है या फिर उन कोई बात करना नहीं चाहता क्योंकि वे हमारे पितृसत्ता समाज पर गहरी चोट करती है, हम बात कर रहें है मलयालम फ़िल्म ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ फ़िल्म का शीर्षक अंग्रेजी में है जो भाषिक विविधताओं से परिपूर्ण एकसमान भारतीय मानसिकता को समेट लेता है।
सम्पूर्ण फ़िल्म परिवार का मुखिया माने जाने वाले पुरुष पर कटाक्ष करती है, जो स्त्री को अन्नपूर्णा कहता है (मानता नहीं)। तमाम सामाजिक नियमों से टक्कर लेने वाली यह फिल्म भारतीय समाज के उस रूप को हमारे सामने रखती है जिसे हमारे लोकप्रिय सिनेमा ने हमेशा बहुत खूबसूरती से सजा-धजा कर प्रस्तुत किया, ये फ़िल्म बड़ी सहजता से उस छवि की धज्जियां उड़ा देती है। बेटा बरसों बाद पढ़ाई करके लौट रहा है, मां के हाथों का हलवा/खीर वह बहुत मिस कर रहा था (माँ को नहीं) कभी बेटी विदेश से पढकर आई ही नहीं, तो कभी हम ऐसा दृश्य भी देखते जिसमे बेटी माँ को या खीर को याद करती हो बेटी तो सदा माँ का हाथ बटाती हुई नजर आती है। लोकप्रिय सिनेमा माँ के परम्परागत अन्नपूर्णा के रूप को ही सार्थक करता दीखता है वह हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दृढ़ करने में ही अपनी भूमिका निभाता आया है।
मैंने यह फिल्म अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ देखी, अंग्रेजी सबटाइटल्स न भी हों तो भी भाषा यहाँ कहीं भी बाधक नहीं लगती क्योंकि दृश्य और भावाभिव्यक्ति अभिव्यंजना को तुरन्त पकड़ लेते हैं यहाँ तकनीक की सार्थकता सिद्ध होती है और साहित्य से एक कदम आगे बढ़ जाती है। फ़िल्म देखते हुए मेरे दस वर्षीय बेटे का प्रश्न किया कि मम्मी अभी तो इस लड़की की शादी हुई थी और अब यहाँ यह मैड बन गयी क्या ये इस फ़िल्म में डबल रोल निभा रही है। यह मुझे कुरेदता है कि मैं इसपर कुछ लिखूं उसने पूछा देवियों में अन्नपूर्णा का महत्व सबसे ज्यादा है क्योंकि वही पारिवारिक पोषण करती है यही कारण है लड़कियों को पाकशास्त्र में निपुण करवाया जाता है इसके अतिरिक्त किसी और शास्त्र में पुरुष की रूचि नहीं। बचपन से ही उसे छोटे-छोटे घरेलू कामों में इस तरह से लगा दिया जाता है कि मानो किसी रोबोट में कार्यप्रणाली को फिट किया जा रहा है समय आने पर अपनी सेवाएं दें। फिल्म अन्नपूर्णा की महामंडित प्रतिमा पर जब कुठाराघात करती है। 
फ़िल्म के एक दृश्य में समाजशास्त्र का अध्यापक (नायक) कक्षा में छात्राओं को परिवार की संकल्पना समझा रहा है, कि समाज की सबसे सरल और बुनियादी विश्वव्यापी संस्था है ‘परिवार’ जिसके केद्र में पति-पत्नी और बच्चे हैं। यह परिवार विवाह पर निर्भर है फ़िल्म का आरम्भ विवाह से ही होता है और दूसरे दृश्य में परिवार की सैद्धांतिक संकल्पना की यथार्थ छवि उभरने लगती है, जिसे हम रोज़ अपने परिवारों में देखते हैं और जो परिवार में रहकर, पास से हम अनुभव नहीं कर पाए फ़िल्म के दृश्य स्पष्ट करते जाते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार की खाई को स्त्री सशक्तिकरण के युग में भी भरना नामुमकिन ही है। फ़िल्म का अन्त इसका खुलासा करती है।
चूंकि विवाह के बाद तकरीबन सभी समाज में लड़की अपना घर छोड़कर पति के घर जाती है, इसलिए पति अपना अधिकार समझता है कि वह कभी भी इस फ़िल्म के संवाद की भांति कह सकता है ‘यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा’ और जब पत्नी अपने सम्मान को ओर नहीं कुचलने देने का संकल्प लेकर घर से चली जाती है तो… अगले दृश्य में अन्य लड़की (पत्नी) रसोईघर घर सँभालने के लिए हाज़िर है, सभी कुछ तो पहले जैसा है, कुछ भी तो नहीं बदला, चाय पीकर कप वहीँ स्लैब पर छोडकर पति रसोघर से बाहर निकल जाता है जबकि सिंक उसकी बगल ही में है। एक लड़की के बदलने से समाज की सोच बदलने वाली नहीं। धर्म के नाम पर भी स्त्रियों को महान बनाने वाले नियमों पर भी फ़िल्म सवाल उठाती है। जब समाज की प्रगतिशील स्त्रियाँ (सबरीमाला सन्दर्भ) बदलाव चाहती हैं बराबर के धार्मिक अधिकार मांगती है तो इसी समाज पितृसत्ता पोषित स्त्रियाँ ‘धर्म बचाओं’ के नारे लगाती हैंअजब-गजब विडम्बना है, प्रश्न उठता है कि धर्म को बचानाकिससे है? उन (तथाकथित देवी मानने वाली) स्त्रियों से जो मंदिर में पूजा का अधिकार चाहती है?
फ़िल्म स्वछंद नायिका विवाह बंधन में बाँध दी जाती है और परम्परागत पत्नी बहू की भांति उसे भी बंधन में सुख नजर आ रहा है, रजनीगंधा फ़िल्म के नायिका की तरह कितना सुख है बंधन में जो कॉलेज की प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और विवाह के बाद का समां न उसे मालूम न हमें क्योंकि विवाह के बाद तो फिल्मों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है पर यह फ़िल्म विवाह के साथ आरम्भ होती है (आविष्कार फ़िल्म की भांति)। विवाह के बाद नायिका के चेहरे पर नवेली रौनक, काम करते हुए उत्साह और सौम्यता कैसे धीरे-धीरे बेचैनी में परिवर्तित होने लगता है उसका धैर्य कैसे टूटने लगता है, देखते ही बनता है।
फिल्म में पात्रों के भावों को समझ पाना उतना ही सहज है जितना कि किसी मूक जानवर के भावों को समझ लेना कि वह आपसे क्या कहना चाह रहा है और यह अच्छा ही है कि फिल्मों में बहुत कम संवाद रखे गये हैं लोकप्रिय सिनेमा जैसी डायलॉगबाजी वैसे भी हवाबाजी ही होते हैं। पहली सुबह नाश्ते की टेबल पर जब सास औपचारिकतावश कहती है कि तुम भी साथ खाओ मैं संभाल लूंगी तो पति भयभीत-सा चौंक जाता है और पत्नी उसके भाव समझ जाती है, मना करने पर पति को साँस में साँस आती है और कहता कि मम्मी को भी तो कंपनी चाहिए रसोई में। सालों से मम्मी रसोई में काम करती रही बहु के आने से पूर्व कौन कंपनी दे रहा था?बेटे और पति ने कम्पनी नहीं ही दी होगी न? 
देश का सर्वाधिक शिक्षित राज्य वहाँ पर भी लड़कियों को शिक्षा के बाद गृहस्थिन बनने के लिए घर संभालने के लिए ही तैयार किया जाता है, देखकर हैरानी होती है। जब नायिका नौकरी के इन्टरव्यू की बात करती है तो ससुर कहता है कि मेरी पत्नी एम.ए.पास है लेकिन जब उसने नौकरी के लिए कहा तो मैंने भी अपने पिताजी का कहना माना और पत्नी ने मेरा, घर संभाला नौकरी नहीं की। यानी सदियों से स्त्रियाँ घर संभल रहीं है आज भी घर ही संभालेंगी पढ़ लिखकर भी, नौकरी करते हुए भी। लेकिन स्पष्ट है स्त्रियां यदि नौकरी करेंगी तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी ही पर घर संभालने जैसे कार्य में परिवार के अन्य सदस्य समझौता करने को तैयार नहीं है। ससुर साफ कहता है कि चावल चूल्हे में ही पकाना जब के घर में तमाम आधुनिक उपकरण मौजूद हैं वह कहता है कि चटनी को सिलबट्टे पर पीसे ना कि मिक्सी में नहीं।
दिनचर्या एक-सी ही है, सुबह का आरम्भ, घर के दोनों पुरुष अखबार पढ़ने से, योग करने से करते हैं ससुर को तो ब्रश भी हाथ में चाहिए, बाहर जाने पर पत्नी उसकी चप्पल हाथ में उठाकर लाती है, तब वो पहनता है दोनों गृहणियां नाश्ते की तैयारी में लगी हुयी है लाज़िम है कि नित्यकर्म हेतु एक घंटा पहले उठी होंगी और रात में पत्नी रसोई समेट रही हैं। पति मोबाइल में व्हट्सअप पर व्यस्त है (व्यस्त?) यानी गृहणियां जल्दी उठकर देर से सोती हैं नाश्ता सिमटता नहीं लंच की तैयारी शुरू उन्हें कब फुर्सत कि आराम करें अपने बारे में सोचे। यही दिचर्या हम रोज़ अपने परिवारों में देख रहे होते है लेकिन सिनेमा के दृश्यों ने इस भेदभाव को इतनी बारीकी से प्रस्तुत किया है जो हमें कभी नजर ही/समझ ही नहीं आता। या हमारी सोच को सीमित किया जा चुका है बोनसाई की भांति, जितना चाहिए जैसा चाहिए काट-छांट कर तैयार कर दिया सजा दिया।
यह भी पढ़ें – स्त्री मन की आकांक्षाओं का लैंडस्केप
फिल्मों (विशेषकर अंग्रेजी फिल्मों) में बड़ी से टेबल पर खाने से सजी टेबल के दृश्य बहुत दिखते हैं लेकिन भोजन बनाने की पूर्व की प्रक्रिया और उसके बाद के जूठन को समेटना इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता घर में ये प्रश्न सभी करते हैं आज क्या बन रहा है लेकिन कैसे? कौन? और उसके बाद की प्रक्रिया पर कोई बात नहीं करता। फ़िल्म के एक दृश्य में रेस्तरां में पति के टेबल मैनर्स पर पत्नी टिपण्णी करते हुए कहती है यहाँ तो आप सलीके से खा रहें हैं?मतलब घर पर तो झूठा टेबल पर ही गिरा देते हो तो यह बात पुरुष के अहं को चोट पहुंचाती है, वो ‘मेरा घर है’ का दावा करते हुए, कम्फर्ट ज़ोन की बात करता है क्योंकि वहाँ तो टेबल पर से झूठा उठाने वाली माँ और पत्नी हैं न! जिन्हें उनके उठने के बाद खाने के लिए साफ़ स्थान भी नहीं मिलता।
ये आम-सी लगने वाली बात अन्नपूर्णा के जीवन की कितनी तकलीफदायक स्थिति है इसे फ़िल्म बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करती है। जब सास की गर्भवती बेटी माँ को अपनी सेवा के लिए, यह कहकर कि अब तो बहु आ गयी है घर संभल लेगी उसके बाद बहु नायिका की स्थिति दयनीय बन जाती है, एक स्वछंद, उन्मुक्त और मेहनती लड़की की सृजनात्मकता कुंठित होती रहती है। रसोई की सिंक में पानी जमा होता रहता है जो उसके मन में गुब्बार की तरह भरता जा रहा है पति बार बार कहने पर भी प्लम्बर बुलाना भूल जाता है और एक दिन सब्र का बाँध टूटता है तो सम्बन्ध भी टूट जाते है नायिका सिंक का पानी दोनों पर उछल कर अपने घर वापस लौट जाती है।
लेकिन रसोईघर का चक्र तो चलता रहेगा जिसे चलने के लिए दूसरी मूर्ती की प्रतिष्ठा हो जाती है हमारे समाज में यह अत्यंत सरलता से होने वाली प्रक्रिया है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को होममेकर जैसा आधुनिक नाम तो दे दिया लेकिन वह स्वयं अभी भी उन्हीं परम्परागत जड़ रुढ़ियों से बंधी हुई है, आज भी कर्तव्य के नाम पर उनका महिमामंडन कर उनके श्रम को नकारा जाता है सुरक्षा के नाम पर उन्हें देवी ती तरह घरों में सुशोभित कर वास्तव में उनका दोहन ही होता है। फ़िल्म समाज के दोगले व्यवहार की पोल खल कर रख देती है। लेकिन अन्त और भी भयानक तस्वीर सामने रखता है जो जाता है कि हम पर कोई असर नहीं होने वाला हम जसे थे वैसे ही रहेंगे और (स्त्री) तुम्हें भी नहीं बदलने देंगे।