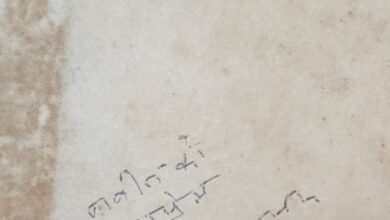धर्म, राजनीति, लोकतन्त्र और राष्ट्र
भारत में सदियों से धर्म और राजनीति एक-दूसरे से गुत्थम-गुत्था रहे हैं। कम से कम उस समय से जबकि राजनीतिक विजय के पश्चात राजसत्ता के माध्यम से धर्मसत्ता स्थापित करने का भी अभियान चलाया गया यहाँ के मूल या स्थानीय धर्म/धर्मों को उन्मूलित करके। जब से राजनीतिक विजय को किसी धर्म विशेष की जय के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा तब से ही धर्म और राजनीति के बीच एक फांक बन गयी, क्योंकि विजित समुदाय की राजनीतिक पराजय मानो उनके धर्म और आस्था की भी पराजय थी। बारहवीं सदी तक धर्म और राजनीति अलग-अलग विषय जरूर थे लेकिन उनके बीच भेद करने की जरूरत शायद ही अनुभव की गयी हो। यहाँ धर्म सत्ता का कोई एक केन्द्र कभी नहीं रहा पोप या खलीफा की तरह। जब कई क्षेत्रों में बौद्ध धर्म राजकीय धर्म के रूप में भी फल-फूल रहा था तब भी ऐसा कोई केन्द्र और ऐसी कोई संहिता नहीं थी जो राजसत्ताओं को अपने ढंग से निदेशित करे। चूंकि उपनिवेश काल में भी राजसत्ता किसी धर्म विशेष की सत्ता का भी प्रतिनिधित्व करने लगी तब उसका प्रतिकार शुद्ध रूप से राजनीतिक हो, उसमें धार्मिक आग्रह-दुराग्रह नहीं हो, ऐसा मानना वास्तविकता से आंख चुराने जैसा है। इसलिए स्वतन्त्रता आन्दोलन राजनीतिक उद्यम ही नहीं था, वृहत्तर अर्थों में धर्मकाज भी था। गाँधीजी को यह श्रेय या दोष दिया जाता है कि उन्होंने धर्म और राजनीति को मिला दिया, एकमेव कर दिया।
लेकिन गाँधीजी ऐसा करने वाले पहले नेता नहीं थे। उनके पहले लोकमान्य तिलक और श्री अरविन्द जैसे नेताओं के लिए भी स्वतन्त्रता संघर्ष राजनीतिक कार्य मात्र नहीं था। सच पूछिए तो उपनिवेशवाद के खिलाफ जो भी संघर्ष हुआ उसके पीछे कहीं न कहीं धार्मिक या सांस्कृतिक कारक भी अवश्य रहे थे। मुसलमानों को सांस्कृतिक दमन का अनुभव अट्ठारहवीं सदी में कंपनी शासन के स्थापित होने के बाद ही हुआ। अब हिन्दू-मुसलमान के साझे निशाने पर गोरे अंग्रेज और उनके पश्चिमी, ईसाई मूल्य थे, उनका राजनीतिक-आर्थिक शोषण-दमन तो था ही। इसीलिए सन् 1857 का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम दोनों समुदायों ने मिलकर लड़ा। कैसी विचित्र विडम्बना है कि इसके नब्बे वर्ष पश्चात हिन्दू और मुसलमान इतने अलग हो गये कि मुसलमानों ने अलग देश ही बना डाला। स्वतन्त्रता आन्दोलन की विरासत, उसके मूल्य,गाँधीजी और काँग्रेस की अहिंसा और उनकी कौमी एकता के तमाम प्रयास, यहाँ तक कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस का मुक्ति अभियान जिसमें हिन्दू-मुसलमान साथ शामिल थे, भी धरा का धरा रह गया। इसका एक आशय यह निकलता है कि एक समुदाय के रूप में मुसलमानों ने ब्रिटिश की राजनीतिक-सांस्कृतिक पराधीनता का स्वाद चखा था और उससे किसी प्रकार मुक्त भी हो रहे थे, अब वे हिन्दुओं के अधीन नहीं होना चाहते थे – किसी भी कीमत पर।

भारत में जब भी धर्म की चर्चा होगी ‘रिलीजन’ के संदर्भ में, तो यह तथ्य ध्यान में रखना होगा कि हिन्दू धर्म, बहुदेववादी हिन्दू धर्म इब्राहिमी धर्म-पन्थ और एकेश्वरवादी धार्मिक साम्राज्यवाद से पिछले लगभग आठ सौ सालों से जूझ रहा है और यह स्थिति आज भी जारी है। यह मूलतः अस्तित्व रक्षा का संघर्ष रहा है।
अब बजाए इसके कि प्रताड़ित हिन्दू समुदाय के प्रति सहानुभूति न सही, कम से कम तटस्थ, वस्तुनिष्ठ रुख या दृष्टिकोण रखा जाता, राजनीतिक और अकादमिक क्षेत्र में हिन्दुओं को ‘प्रताड़ित’ नहीं वरन ‘प्रताड़क’ के रूप में देखा और प्रस्तुत किया जाता है। धार्मिक आधार पर उनके उत्पीड़न को मान्यता ही नहीं दी जाती, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं। उत्पीड़न अगर हुआ भी हो तो इसके राजनीतिक और सामाजिक कारण और औचित्य तलाशे जाते हैं। दुनिया में किसी भी उत्पीड़ित समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ होगा।
अतीत में हिन्दुओं की हार और केंद्रीय सत्ता से बेदखली के लिए जाति प्रथा को उत्तरदायी ठहराया जाता है जबकि वास्तविकता यह है कि इस्लाम ने अपने प्रसार अभियान में जिन मूल संस्कृतियों को नष्ट किया वह भी पूरी तरह, वहाँ तो कोई जाति प्रथा नहीं थी। अँग्रेजों ने और दूसरे यूरोपीय साम्राज्यवादियों ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ जिन दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाया वहाँ भी कोई जाति प्रथा नहीं थी। जहाँ तक आक्रांताओं से लड़ने अथवा अपने अस्तित्व रक्षा के लिए ही संघर्ष करने की बात हो, तो सिर्फ क्षत्रियों ने या राजपूतों ने शस्त्र उठाया हो यह तो निराधार तथ्य है। राजपूताना में भी लड़ाइयां केवल राजपूतों ने नहीं लड़ीं। पिछले ढाई हजार सालों में हमारे जितने भी रक्षक या उद्धारक राष्ट्रपुरुष हुए उनमें से अधिकांश जन्मना क्षत्रिय नहीं थे बल्कि कर्मणा क्षत्रिय थे।
हिन्दू केवल पत्थर और गोली खाते समय ही एक समुदाय है, वरना अगड़ा, पिछड़ा, दलित, बहुजन, अल्पजन, अवर्ण, सवर्ण.. आदि आदि है। गौर से देखिए तो भारत में राजनीति की जितनी धाराएं हैं वह सब इसी हिन्दू विभाजन के सिद्धांत पर आधारित हैं, विभाजन की इसी जमीन पर उगी हैं और फल-फूल रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां भी इससे बरी नहीं हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी आंतरिक तौर पर कहीं न कहीं यह विभाजन काम करता रहता है। वहाँ तो अभी पिछड़ी जातियों का ही वर्चस्व बना हुआ है। धर्म की राजनीति हिन्दुत्ववादी राजनीति का बाहरी चेहरा है जबकि जाति की राजनीति उसकी आंतरिक व्यवस्थाओं का नियमन और संचालन करती है। भारत की राजनीति में यह एक विचित्र विडम्बनापूर्ण स्थिति है।

भारत विभाजन हिन्दुओं का एजेंडा होता और वे ही प्रभावी होते तो विभाजन के बाद भारत में अलग राष्ट्र के रूप में मुसलमान कदापि नहीं रह गये होते। उन्होंने तो गाँधीजी और काँग्रेस की बात मान ली और पूर्ण विभाजन की जिद नहीं की, जिसकी सिफारिश बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी। विचारणीय सवाल यह भी है कि भारत के हित में, भारत राष्ट्र के हित में मुसलमानों ने क्या छोड़ा, वे अपनी पोजीशन से कितना हटे और किस हद तक समझौता किया। याद रहे कि वे ‘अलग राष्ट्र’ होने के नाम पर अलग देश ले चुके थे, और अगर वे इस देश में रह गये तो इसका मतलब था कि उन्होंने अपने को अलग(मुस्लिम) राष्ट्र के रूप में नहीं देख कर भारत राष्ट्र की इकाई के रूप में इससे जुड़ना स्वीकार किया था। भारत के संविधान और राजनीतिक प्रणाली में उनकी अडिग आस्था होनी चाहिए थी और इस आधार पर संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित समान नागरिक संहिता की ओर देश को बढ़ना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं ही नियामक बन गईं।
भारत राष्ट्र के अंतर्गत मुस्लिम राष्ट्र कहीं न कहीं बना रह गया, यह क्यों न कहा जाए! मुस्लिम पहचान को लेकर काँग्रेस, कम्युनिस्ट तथा सोशलिस्ट मुस्लिमों से भी ज्यादा संवेदनशील रहे। मुसलमानों के लिए सेकुलर होने की जरूरत ही नहीं रह गयी, उसे केवल हिन्दुओं की जरूरत बना दिया गया। सेकुलरवाद मानो एक रूढ़ धर्म बन गया। मुसीबत की जड़ यहाँ है। यह अजीब बात है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत में हिन्दू-मुस्लिम मतभेद के मूलभूत बिंदुओं पर अपना मत अथवा स्टैंड कभी नहीं बदला। उन्होंने इस बात को स्वीकारने से भी परहेज किया कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान ज्यादतियां हुई थीं (और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अपने आप में खालसा पन्थ का उदय है)। हिन्दू समुदाय अपने प्रमुख तीर्थ स्थलों और धार्मिक केन्द्रों को लेकर संवेदनशील रहा है, उसमें वंचना और क्षोभ का भाव रहा है। एक समुदाय के रूप में भारत की स्वतन्त्रता से उनकी भी आशाएं और आकांक्षाएं जुड़ी थीं, लेकिन अकल्पनीय रूप से उन्हें मिला रक्तरंजित विभाजन के बाद कटा-फटा भूखंड – भारत! अगर मुस्लिम नेतृत्व कम से कम अयोध्या-काशी-मथुरा पर हिन्दुओं का दावा स्वीकार कर लेता तो इसका मुसलमानों की स्थिति पर, उनकी धार्मिक पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इससे देश में सामुदायिक सौहार्द की स्थिति बनती, अन्तर-सामुदायिक सम्बन्ध मजबूत बनते और हम एक राष्ट्रीयता की ओर बढ़ते। लेकिन स्वतन्त्रता आन्दोलन के परवर्ती दौर में ही राजनीति में वोट बैंक की अवधारणा सामने आई और सबकुछ बदल गया।
आज हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों पर खुल कर बात करने की जरूरत आन पड़ी है। सबसे पहले तो यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि भारत का बंटवारा हिन्दू-मुसलमान के बीच हुआ था, सेकुलर और मुसलमान के बीच में नहीं। काँग्रेस, गाँधीजी और नेहरू हिन्दू भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भले ही यह मानने में उन्हें या आज के सेकुलर जमात में हिचक हो। समस्या यह रही कि नेहरू बंटवारे-पूर्व की मानसिकता में ही जीते रहे और मानो अब भी अपने को अविभाजित भारत का निर्विवाद नेता मानते रहे। जिन्हें हिन्दुओं से समस्या थी उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, काँग्रेस ने दे भी दिया। जो भारत हिन्दुओं के लिए बच भी गया उसमें सेकुलरवाद इस कदर हावी हुआ कि सत्ताधारी वर्ग को हिन्दू पहचान और प्रतीकों से भी समस्या होने लगी। देसी शासक हिन्दुओं से इतना भय खाने लगे जितना कि मुगलों और अँग्रेजों ने भी नहीं खाया होगा। गाँधीजी की हत्या से इस प्रवृत्ति को और बल मिला। ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि यह सब लोकतांत्रिक भारत में सत्ता की राजनीति की जरूरतें थीं। काँग्रेस ने स्वतंत्र भारत के राजकाज में जिन थोड़े प्रचलनों और प्रविधियों को आगे बढ़ाया, वोट बैंक की राजनीति उनमें सबसे नायाब आविष्कार थी।

वोट बैंक की राजनीति में धर्म के आधार पर स्वतंत्र भारत में मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग किया, फिर जातीय समीकरण के नाम पर हिन्दुओं को भी हिन्दुओं से अलग कर दिया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और इस कांग्रेसी आविष्कार का लाभ आज सभी दल उठा रहे हैं। हमारा उदार, समावेशी लोकतन्त्र ‘जातियों के लोकतन्त्र’ में रिड्यूस कर दिया गया। जनसंख्या और जमीनी ताकत के बल पर प्रभुत्वशाली जातियां ही यह तय करती रहीं कि सत्ता किस दल को मिलेगी। आज यही जातियां जातीय जनगणना के माध्यम से राजनीति पर अपना वर्चस्व और मजबूत करने में जुटी हैं। कुछ लोग इसे मंडलीकरण के दूसरे चरण के रूप में भी देख रहे हैं और क्योंकि मंडलीकरण की प्रक्रिया ने प्रत्येक दल को प्रभावित किया इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की भी यह जरूरत है। इसके लिए ‘राष्ट्रवाद’ को डाइल्यूट या विलयित किया जा सकता है। वैसे भी आज की भाजपा शुद्र वर्चस्व वाली पार्टी है। लेकिन अत्यंत पिछड़ी जातियां और कम जनसंख्या वाली दलित जातियां जातीय जनगणना को शंका और जुगुप्सा से देख रही है, वे अपनी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति और हैसियत कमजोर पड़ने की आशंका से ग्रस्त हैं। इसलिए जातीय जनगणना को ‘मंडलीकरण-दो’ कतई नहीं कहा जा सकता, कम से कम आज तो नहीं।
यह विचार करने की जरूरत है और इस पर अभी तक विचार किया नहीं गया कि जिस देश के बहुसंख्यक समुदाय में धर्मांतरण की कोई प्रथा या प्रचलन ही ना हो वहाँ आखिर अल्पसंख्यकों में धर्मांतरण के प्रति आग्रह क्यों होना चाहिए? उनके लिए तो अस्तित्व रक्षा का कोई संकट नहीं है! लोकतन्त्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी जरूरी है , वहीं बहुमत की चिंताओं और आशंकाओं की कबतक अनदेखी की जा सकती है। शांति और सौहार्द के लिए उनको विश्वास में लेना राज्य और समाज का दायित्व है।

यह एक तथ्य है कि संसार में जितने भी धर्म-पन्थ हैं उनकी अपनी एक प्रतिरक्षा प्रणाली है। ईसाई और इस्लाम धर्मपन्थ की सुरक्षा स्वयं राज्य करता है जहाँ वे बहुमत में होते हैं, और जहाँ वे अल्पमत में होते हैं वहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक संगठन और संस्थाएं उनके हितों के संरक्षण के लिए काम करती हैं। वे अन्तरराष्ट्रीय दबाव बनाने तक की हैसियत में होती हैं, यह भी एक प्रमाणित तथ्य है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब हिन्दुओं की जनसंख्या लगभग पचासी प्रतिशत (मुसलमान लगभग दस प्रतिशत) होने के बावजूद राज्य उनका संरक्षक नहीं था, न ही है। एक समुदाय के रूप में हिन्दुओं की अपेक्षाओं-आकांक्षाओं का राज्य की दृष्टि में कोई महत्व नहीं। दूसरी ओर धार्मिक अल्पसंख्यकों का पूर्ण संरक्षण भारतीय राज्य का संवैधानिक दायित्व है जिसमें उनके विवाह, उत्तराधिकार, धर्म, शिक्षा और सांस्कृतिक पहचान आदि विषय समाहित हैं। याद कीजिए अभी पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था और नेहरु जी ने हिन्दू कोड बिल पारित कराना चाहा था जिस पर राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी सहमति नहीं दी थी। लेकिन 1955-56 में निर्वाचित सरकार का मुखिया रहते उन्होंने हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम आदि चार कानून लागू करवाए थे।
जबकि यह वह अवसर था जबकि एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे। यदि ऐसा होता तो भारत में सांप्रदायिक समस्या का बहुत हद तक समाधान हो गया होता लेकिन काम वास्तव में उल्टी दिशा में होता रहा। 1985 में प्रसिद्ध शाहबानो मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हमारी संसद ने पलट दिया। यदि वास्तव में भारतीय राज्य विभिन्न धर्म-पंथों के प्रति तटस्थ रहता – समान दृष्टि, भाव, और व्यवहार रखता तो सांप्रदायिकता कोई इतनी बड़ी समस्या ही नहीं होती। इस बात पर गहराई से विचार करने की जरूरत है कि अस्सी के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महत्व अचानक कैसे बढ़ गया? क्या वह अपनी जमीन के तीन टुकड़े होने के बाद भी ‘सेकुलर स्टेट’ के द्रोह भाव की स्थिति में हिन्दुओं की आत्मरक्षा की युक्ति के अभाव की पूर्ति ही नहीं कर रहा था, और आज वह उनकी आत्मरक्षा प्रणाली का ही एक प्रतीक नहीं बन गया है?
आज यह प्रश्न भी प्रासंगिक बन गया है कि आखिर हिन्दुओं के पक्ष को सुनने का धीरज सेकुलर लोगों में क्यों नहीं रहा, हिन्दुओं का मन जानने-समझने की कोशिश मुस्लिम पक्ष में क्यों नहीं दिखी? क्यों सेकुलर लोग कोई विवाद या समस्या सतह पर आते ही मुसलमानों की तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं, हाल की पत्थरबाजी की घटना ताजा उदाहरण है। अपने इस व्यवहार के चलते आज के दिन हिन्दू-मुस्लिम एकता में वह सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। यह तय है कि हिन्दू-मुसलमान और दूसरे धर्म के लोगों को साथ रहना है और जब साथ रहना ही है तो मिलजुल कर ही रहने की स्थिति रहनी चाहिए। आज की तारीख में दोनों पक्षों को मिल-बैठकर साथ चलने और आगे बढ़ने का रास्ता निकालना है और इसके लिए परस्पर कुछ खोने की भी तैयारी रखनी है। दोनों तरफ के समझदार लोगों, विशेषकर युवाओं को सामने आना चाहिए और सत्ता की राजनीति के बदले राष्ट्र की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। लोकनीति को आगे बढ़ाने का अवसर हम दशकों पहले गंवा चुके हैं। राष्ट्रनीति की बात करने से कहीं लोकतन्त्र का आग्रह कमजोर तो नहीं पड़ता..राष्ट्र है तभी लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र है तभी राष्ट्र बचेगा , भारत के संदर्भ में ऐसा सोचा या कहा जा सकता है क्या? लोकतांत्रिक राजनीति यदि विभाजन और विखंडन को ही आधार बनाकर सत्ता का मार्ग सुलभ कराएगी तब राष्ट्र बचेगा कैसे!