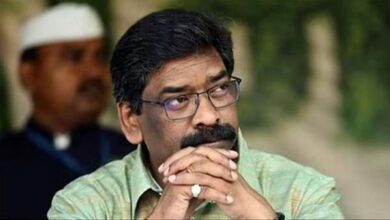पिछले दिनों झारखण्ड के मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन ने हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में देश, दुनिया और अपने राज्य की बातें करते, हुए यह भी कहा कि- आदिवासी हिन्दू नहीं हैं। फलतः, देश के कुछ राजनीतिक, धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया। वहीं दूसरी ओर कई आदिवासी और गैर आदिवासी संगठनों ने तथा रणेन्द्र जैसे साहित्यकार व अन्य बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। अखबारों, सोशल मीडिया में पक्ष-विपक्ष में तर्क, वितर्क होने लगे। पुनः भाजपा में शामिल भूतपूर्व मुख्यमन्त्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि – आदिवासी जन्म से हिन्दू हैं। फलतः, कई आदिवासी-संगठनों ने इसका विरोध किया।
इस मुद्दे पर वातावरण गर्म हो गया। कुछ पत्रकारों के फोन मिले – इस मुद्दे पर आपके विचार क्या हैं? फलतः, बचपन की बातें याद करते अपनी बात कहना चाहूँगा। मेरे दादाजी अँग्रेज साहब पेपी के यहाँ काम करते थे राँची में। उस अँग्रेज साहब की बेटी 1965 तक राँची में रह रही थी। अँग्रेज मेम चूँकि भारत में पैदा हुई थी हिन्दी अच्छी तरह बोलती थी। वह कभी-कभी हमारे निवास की ओर हाल चाल पूछने आती थी। दादाजी पर और माँ पर इसका खास प्रभाव था। मैं करीब बारह-तेरह साल की उम्र तक उन्हें माँ से बात करते देखता था। वह कई बातें कहा करती थी। एक कि गाँव में खेती के लिए सल्फेट आदि प्रयोग न करना, साफ-सफाई से रहना और एक बात वह खास ढंग से कहती थी कि – तुमलोग जैसे भी हो ठीक हो। मेम के कहने का आशय था कि हमारी आस्था, विश्वास जो भी है, ठीक है। तब तक माँ से तथा स्कूल में सिस्टर के माध्यम से इस बात की जानकारी हो गयी थी कि – हम जिस पूजा-विधान का पालन करते हैं उसे सरना या संवसार पूजा कहा जाता है।
माँ ने बताया था कि हम ‘चाला-टोंका’ (सरना पूजा स्थल) में ‘चाला आयो’ (प्रकृति माँ) की पूजा करते हैं। लेकिन, जिस स्कूल में पढ़ता था वह रोमन कैथोलिक मिशनरियों का स्कूल था। बाद में बी ए तक की पढ़ाई मैंने इसी कैथोलिक मिशन के कॉलेज से पूरी की। बचपन से माँ को देखा था वह फग्गु, खद्दी (सरहुल), करम, पच्चो करम (बूढ़ी करम), मुड़मा जतरा, पुना मोखना (नवा खानी) आदि त्योहारों, विधि विधानों की चर्चा करती थी। हम शहर में रहते हुए भी अँग्रेज के उस बड़े कम्पाउन्ड में फाल्गुन पूर्णिमा में गाँव में कुंड़ुख परम्परा के अनुसार फग्गु काटते थे। सेमल की डाली पर कुछ घास-फूस डालकर उसे हमारे काका या बड़े भैया काटते थे। माँ परब त्यौहारों पर खास पकवान बनाती और सबसे पहले तीन सखुआ पत्तों को धरती पर रखकर वहाँ पानी डालती फिर कुछ फूल तथा पकवान को पत्तों पर ऱखती। पूछने पर कहती चाला आयो और पचबालर (पुरखे) को देने के बाद ही हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ यह भी बता दें कि हमारी परम्परा में पुरखों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए खेत खलिहान आदि देकर कर धरती को हमारे जीने लायक बनाया।
यह भी पढ़ें – आदिवासी धर्म कोड की माँग
हम शहर में रह रहे थे लेकिन हमारा रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज सब कुछ एक ग्रामीण कुँड़ुख (उराँव) परिवार जैसा ही था। घर में हम सब कुँड़ुख में ही बात किया करते थे। मात्र पिताजी से हम सब भाई बहन हिन्दी में बात करते थे।
जब अँग्रेज मेम को अपनी जायदाद बेचकर इंगलैण्ड जाना पड़ा तो हमें भी वह कम्पाउन्ड छोड़कर नए मुहल्ले कड़रू, कुम्हार टोली में जाना पड़ा। अब मैं एकान्त से मित्रों की भीड़ में आ गिरा था। लेकिन, धीरे-धीरे यह देखकर हैरत हुई कि पड़ोस के छह-सात घर ही हम जैसे आदिवासी परिवार के हैं और शेष अधिकांश घर ईसाई-आदिवासियों के हैं। फलतः, हम पर मित्रों, पड़ोसियों की सलाह होती थी कि हम ईसाई बन जाएँ। लेकिन, धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि- नहीं हमें अपने मूल संवसार रूप में रहना ही उचित है। ऐसा इसलिए कि तब हमलोग कुछ पढ़ने लगे थे। हमारी मूल-धार्मिक-आस्था के प्रति एक आत्मविश्वास सा जगने लगा था। ईसाई मित्रों द्वारा प्रायः कहा जाता था कि – हम भूत पूजना छोड़ असली ईश्वर के शरण में आ जाएँ। हमारे घर में धर्मयुग, दिनमान, पराग, विज्ञान प्रगति आदि पत्रिकाएँ पढ़ने का माहौल था। ये पत्रिकाएँ मेरी जिद के कारण मंगाई जाती थीं।
इस वजह से, साथ ही एक स्थानीय पत्रिका में मेरे रचना छपने और कुछ प्रतियोगिता जीतने के कारण मुझे खास माना जाता था।इसी तरह पिताजी की नौकरी के कारण पूरे परिवार को भी खास माना जाता था। इसीलिए बाद में कॉलेज के समय हम भाइयों का परिचय, हमारे ईसाई मित्र कुछ इस तरह देते थे –“इन लोगों से मिलो। ये लोग सरना हैं लेकिन पढ़-लिख गए है।”यह हमें अपमानजनक लगता था । सामू जैसे मेरे लेखक मित्र का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। मिडिल स्कूल में हमारे साथ करीब पन्द्रह-सोलह लोग सरना थे, जिसमें से करीब आधे लोग सातवीं पहुँचते, ईसाई हो चुके थे। कॉलेज गया तो मेरे जानते वहाँ कुल पाँच या छह अन्य छात्र थे, जो सरना थे।
वहाँ अक्सर हिन्दू मित्रों के बीच मैं भी ईसाई मान लिया जाता था। नौकरी करने लगा तो देश के आधे हिस्से में ईसाई समझा गया और क्रिसमस की शुभकामनाएँ पाता रहा। ईसाई नहीं होने की अपनी तकलीफें थी। जब भी कहीं नए स्थान में किसी आदिवासी से मिलता तो प्राय़ः ये नए मित्र सीधे प्रश्न करते थे –“अच्छा, टोप्पो जी आप किस चर्च से हैं? या किस मिशन के हैं?” यह प्रश्न मुझे बेहद अटपटा लगने लगा था। दो-चार पढ़े लिखे आदिवासी मिलते थे वे भी चर्च व धर्म की बातों में रूचि व उत्साह दिखाते थे। मन में हमेशा सवाल उठता क्या हमारा आदिवासी होना ही मिलने के लिए काफी नहीं था? शायद नहीं था। आज जब नौकरी से सेवानिवृत हो गया हूँ तब भी यह सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है।पिछले आठ दस सालों से यह सवाल तीखा होता चला गया।
यह भी पढ़ें – एक झारखण्डी का यूनाइटेड नेशन के आदिवासी फॉरम से रूबरू
स्व. कार्तिक उराँव और पद्मश्री रामदयाल मुण्डा की सरहुल जुलूस में सहभागिता से सरना कहे जानेवाले आदिवासियों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान बढ़ता गया। बीच में कार्तिक उराँव द्वारा धर्मान्तरित ईसाइयों को आरक्षण न देने का प्रश्न भी मतभेद व विवाद का कारण बना। इस विवाद के बाद एक परिवर्तन यह दिखा कि हमारे ईसाई भाई आदिवासी संस्कृति की बात करने लगे। बचपन में हमें मिशनरी स्कूल में कुछ सिस्टर करम, सरहुल त्यौहार मनाने को शैतान पूजा करना बताती थीं वे ही लोग मिशन हाता में करम, सरहुल मनाने लगे। जिससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ मित्रों से बहसें भी हुई।
उन्होंने इसे सांस्कृतिक मुद्दा बताया और सरना धर्म कहे जाने को, धर्म मानने से इन्कार किया क्योंकि सरना कहे जानेवाले आदिवासियों का कोई धर्मग्रन्थ नहीं है। सच हमारा कोई धर्मग्रन्थ नहीं था। जो कुछ था सीधे सरल शब्दों में था। पाहन जैसा पुजारी था लेकिन कोई ईश्वरीय प्रतीक, भवन या ईमारत नहीं थी। ऐसा धर्म, कोई धर्म कैसे हो सकता था? स्वर्ग नरक, पाप पुण्य जैसी अवधारणा भी नहीं थी। हाँ, कुछ लोग हिन्दू या ईसाई प्रभाव में आकर ऐसा कहते दिख जाते थे। लेकिन, सचमुच ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। अब पता चला है कि कार्तिक उराँव ने इसीलिए केन्द्रीय सरना समिति का गठन किया था। कुछ साल पहले रामदयाल मुण्डा जी की पुस्तक “आदि धर्म” (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली) का प्रकाशन हुआ फलतः इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा मिली।
नौकरी में रहते अधिकांश अवसरों पर लोग या तो ईसाई कहते और नहीं तो हिन्दू। सरना भी कुछ होता है ऐसा लोगों को मालूम न था न है। फलतः प्रायः मेरे बायोडाटा में मेरा धर्म – हिन्दू लिख दिया जाता था। जिसे सुधरवाना पड़ता था। बाद में मैं त्यौहार अग्रिम की सुविधा अपने प्रसिद्ध त्यौहार खद्दी (खेखेल बेंज्जा, सरहुल) के लिए लेने लगा। इससे मुझे अपनी धार्मिक पहचान के बारे बताने में सुविधा होने लगी।
मैं आदिवासी कुँड़ुख सरना समाज पारम्परिक पूजा, अनुष्ठान, दस्तूर बचपन से देखता रहा हूँ। हमारे रीति रिवाज हमारे पहान, पुजारी या उनकी अनुपस्थिति में किसी बुजुर्ग द्वारा भी सम्पन्न किये जाते हैं। किसी आकृति मूलक देवता की पूजा नहीं की जाती है। हमारे पूजा स्थान ‘चाला टोंका’, ‘जाहेर’ आदि हैं, जिसे कुछ वर्षों से सरना पूजा स्थल कहा जाने लगा है। हम चाहें तो घर में ही पुरखों को और विभिन्न देवी-देवताओं का नाम लेकर उन्हें पानी ढालकर या पहला हंड़िया पानी ढालकर गोहराते हैं (याद कर लेते हैं)। विशेष अनुष्ठान के रूप में ‘पल कसना’ या ‘डंडा-कट्टा’ करते हैं। पूजा के स्थान विशेष पर पानी ढालने का काम घड़ी की विपरीत दिशा में किया जाता है। हमारे अधिकांश कार्य इसी तरह घड़ी की विपरीत दिशा में किए जाते हैं। बुजुर्गों ने इसे धरती का नियम बताया। बाद में भूगोल की पढ़ाई याद करते पाया कि धरती भी, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है।
इसका मतलब हमारे पुरखों को इसका ज्ञान था। हमारा शुभ काम बढ़ती चाँद यानी शुक्ल पक्ष में संम्पन्न किया जाता है। आदिवासी शुभ-लाभ वाली मानसिकता में विश्वास नहीं करता है। लेकिन, सबकी हिफाजत व बरकत के लिए गोहारी जरूर करता है। जन्म, नामकरण, शादी, एवं मृत्यु संस्कार में सभी भाग लेते हैं और इन सभी संस्कारों में महिलाओं के वगैर अंतिम संस्कार तक का अनुष्ठान पूरा नहीं होता। हमारे घर में जो धांगर (नौकर) होता है वह हर वर्ष एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर, घर के सदस्य की तरह पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। उसे घर के मालिक से भी पहले वही भोजन दिया जाता है जिसे घर का मालिक खा रहा होता है। फिर कई बार अखरा में ये ही मालिक और धांगर साथ-साथ नाचते, गाते, बजाते देखे जा सकते हैं। क्या किसी सभ्य समाज में ऐसा दृश्य देखना संभव है?
यह भी पढ़ें – पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रारूप और आदिवासी समाज
पिछले साल एक विश्वविद्यालय में साहित्य में लोककथा के महत्व पर बोलने के लिए आमंत्रित था। सेमिनार के दिन, व्याख्यान समाप्त होने पर भोजनावकाश के समय मेरे पास दो छात्राएँ आईं और उन्होंने बिना कोई परिचय दिए या अभिवादन किए सीधे सवाल किया –“सर, क्या आप क्रिश्चियन हैं?” यह सवाल मेरे लिए अप्रत्याशित था। पहले तो सोचा कि उन्हें डाँट दूं। लेकिन मैंने स्पष्टतः कहा कि- “नहीं, मैं ईसाई नहीं हूँ। लेकिन बचपन से बी.ए. तक की पढ़ाई कैथोलिक शिक्षण संस्थानों की है।” वे दोनों लड़कियां चली गयीं। अगले दो दिनों तक मैं उस संस्थान में रहा। कई छात्र और शिक्षक भी आए, मिले बातें कीं। कुछ आदिवासी छात्रों ने मेरा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया। लेकिन, फिर वे दो छात्राएँ मेरे करीब नहीं आयीं और न मुझसे कुछ पूछा।
अब बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार सरना धर्मावलंबी 49.57 लाख हैं जबकि जैन 44 लाख। इस सरकारी आँकड़े की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और आदिवासियों को उनकी माँग के आधार पर एक धार्मिक पहचान के लिए उनके नागरिक अधिकार का सम्मान करते इसे मान्यता दी जानी चाहिए। आदिवासी पर हिन्दू कानून लागू नहीं होता। उसके जन्म, विवाह, मृत्यु, संस्कार के अपने पारम्परिक रीति रिवाज हैं, रूढ़ि-परम्पराएँ हैं जिसके अनुसार वे जीते हैं, अनुष्ठान करते हैं। वे स्वयम् को प्रकृति-पूजक कहते हैं और वे हैं भी ।
यह एक बहुप्रचलित सामाजिक सिद्धान्त है कि—“एक समुदाय अपने को दूसरे से भिन्न व श्रेष्ठ समझता है और वैसा ही दिखना या दिखाना चाहता है। इसके लिए वह तरह-तरह के मुहावरे, आदर्श, कथाएँ, छवि आदि गढ़ता है और उसे अच्छे-बुरे, देवता-शैतान, श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, शक्तिवान-कमजोर आदि साबित करने के कई मिथक गढ़ता है। दूसरा समुदाय भी प्रतिक्रिया में अपने सिद्दान्त व तर्क गढ़ता है। यह संघर्ष और द्वन्द्व बढ़ता जाता है। कभी इसके सकारात्मक तो कभी नकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। इस जद्दोजहद का परिणाम यह होता है कालान्तर में दोनों कभी-कभी कुछ अच्छाइयों पर खामोश सहमति बना लेते हैं। ”किसी की आलोचना करने पर या तो मैं हिन्दूवादी संगठनों का आदमी कहलाता हूँ तो कभी, ईसाई मिशन हाते का आदमी। दोनों समुदाय के अधिकतम लोग, हम जैसे गैर ईसाई और गैर हिन्दू, सरना कहे जानेवालों को कमतर समझते हैं।
यह भी पढ़ें – सुराज की वह आदिवासी सुबह कब आएगी
क्योंकि यह मिथक गढ़ लिया गया है कि हिन्दू या ईसाई ही श्रेष्ठ हैं। हिन्दू कहे जानेवालों के लिए तो खैर हम रिजर्व कोटा के मंदबुद्धि लोग हैं ही लेकिन, दुख तब होता है जब हम पाते हैं जो ईसाई आदिवासी हैं, वे भी हम जैसे सरना कहे जानेवाले लोगों को कुछ ऐसा ही साबित करने के लिए हर तरह के कदम उठाते रहते हैं। और तो और पिछले कुछ वर्षों से सरना कहे जाते लोगों को हिन्दू साबित करने के लिए सोशल मीडिया में मुहिम सी छेड़ी गयी है। इसके लिए दोनों तरफ से कई बार बहुत ही स्तरहीन, अभद्र टिप्पणियाँ दिखती रहीं हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सचमुच में हमारी छोटी, बड़ी और अन्दरूनी तकलीफों को समझते और हमारे पक्ष में खड़े रहते हैं।
हमारे पुरखा लड़ाका बीर बुधु भगत के बारे यह जानने के बाद कि उसके परिवार के सौ से अधिक लोगों ने तथा अन्य दो सौ से अधिक लोगों ने- आदिवासी-स्वशासन, अध्यात्म, आत्मसम्मान तथा पड़हा, पंचा-मदाइत, धुमकड़िया, जतरा, अखड़ा, चाला-टोंका आदि की गौरवपूर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए अंगरेजी हुकूमत के विरूद्ध शहादत दी। वीर बुधु भगत की चर्चा करते विद्वान इतिहासकार सिर्फ यह कहते हैं कि आदिवासियों की सामाजिक-व्यवस्था बहुत मजबूत थी।लेकिन इस पर विद्वान प्रकाश नहीं डालते। धीरे-धीरे जान पाया कि हमारे आदिवासी-समाज की एकजुटता के लिए पड़हा, अखड़ा, धुमकुड़िया, पचा-मदाईत, जतरा, चाला टोंका आदि की व्यवस्था थी। लगभग यही व्यवस्था अन्य आदिवासी समुदायों में भी विद्यमान थी, अब भी है।
विदेश में शिक्षित तीन आदिवासियों- स्व. जयपाल सिंह, स्व. कार्तिक उराँव और स्व. पद्मश्री डॉ. रामदयाल मुण्डा के संघर्ष, कामों, गतिविधियों, लेखन और विचारों से अवगत होने के बाद आदिवासियों के बारे जान पाया कि प्रकृति, विविधता में ज्यादा उर्वर व सृजनशील बनी रहती है जबकि सभ्यता और विकास के तकनीकी-यंत्र इसे पाँच सौ सालों से व्यापार और मुनाफा के नाम पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। एक सवाल और है आजादी के पहले आदिवासी जनसंख्या-गणना में पहचान थी तो बाद में इसे गायब क्यों कर दिया? आज विश्व भर में उनकी प्रकृति-प्रेरित विशिष्ट आध्यात्मिक, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, स्थापनाओं, आदर्शों, मंतव्यों, अनुभवों, विश्वासों आदि को पृथ्वी-रक्षा के लिए प्रासंगिक और उपयोगी पाकर, मान्यता दी जा रही है। वैज्ञानिकों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आदिवासी जीवन-दृष्टिकोण एवं विचारों को महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में उनकी आस्था, विश्वास, परम्परा, विरासत, पारम्परिक-ज्ञान आदि को मान लेने के बदले इस पर सवाल खड़े करना कुछ लोगों की आत्ममुग्ध, आत्मकेन्द्रित, अहंकारपूर्ण, अलोकतांत्रिक चेष्टा प्रतीत होती है।