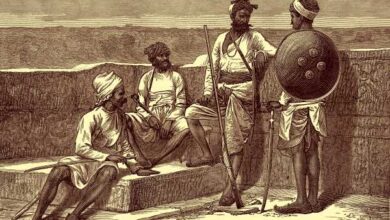पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रारूप 2020 और आदिवासी समाज
फ्रेंड्स ऑफ़ द अर्थ इन्टरनेशनल 74 देशों में पर्यावरण संगठनों का एक अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। फ्रेंड्स ऑफ़ द अर्थ की स्थापना 1969 में सैन फ्रांसिस्को में डेविड ब्राउनर, डोनाल्ड ऐटकेन और गैरी सूकी द्वारा की गयी थी। अक्टूबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जेनेवा के एक सम्मेलन में फ्रेंड्स ऑफ़ द अर्थ इन्टरनेशनल ने विभिन्न राष्ट्रों से आग्रह किया था कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा विदेशी धरती पर संसाधन का दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए बाध्यकारी संधि पर गम्भीर वार्ता करें, ताकि उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।
वर्तमान में विदेशों में अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कानूनी रूप से सैकड़ों बाध्यकारी समझौते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए मानवाधिकार हनन एवं पर्यावरण की क्षति के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर कोई अन्तरराष्ट्रीय बाध्यकारी संधि नहीं है। पूरे सम्मेलन में बार बार सामाजिक संगठनों ने एक बाध्यकारी संधि की आवश्यकता पर विशेष ज़ोर दिया था। मुझे आज भी याद है कि उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यालय अवधी के पश्चात भी पुनः सम्बन्धित अधिकारियों को बुला कर इसमें चर्चा की गयी थी। यह एक अविस्मरणीय घटना है।
यहाँ इस घटना की चर्चा इसलिए आवश्यक जान पड़ी क्योंकि वर्तमान में मार्च 2020 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मन्त्रालय ने 83 पृष्ठ का ‘पर्यावरण प्रभाव आकलन’, का प्रारूप 2020, आम नागरिकों की प्रतिक्रिया के लिए साझा किया है उसका प्रयोजन ठीक इसके विपरीत जान पड़ता है। फ़्रेंड्ज़ ओफ़ द अर्थ इन्टरनैशनल एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने इस सम्मेलन में जो अपना पक्ष रखा था वो अनुभविक तथ्यों पर आधारित था। सामाजिक संगठनों का पक्ष था कि यदि कोई अन्तरराष्ट्रीय कम्पनी किसी देश में व्यवसाय के लिए जाती है और वहाँ नियमों की अवहेलना करतीं है तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर कोई अन्तरराष्ट्रीय बाध्यकारी संधि नहीं है।
ऐसे में कम्पनी मिली भगत से अनेक ग़ैर क़ानूनी कार्य कर सकती हैं और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 प्रारूप में हम देखेंगे कि कैसे यह नकारात्मक हो सकता है और सम्भवतः यह प्रारूप क़ानून बनने के पश्चात अनेक प्रकार के त्रासदी को आने वाले समय में क़ानूनी कवच प्रदान कर सकता है।
अपने पिछले लेख में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र का ज़िक्र किया था। इसी घोषणा पत्र में मूल रूप से अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32 हैं, जो देशज समुदाय के ‘पूर्व सूचित एवं दवाब मुक्त सहमति’, के अधिकार के विषय में चर्चा करती है।संयुक्त राष्ट्र संघ के आदिवासी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19 और 32 के अनुसार जब भी कोई विकासात्मक योजनाएँ कहीं लागू होंगी तो सर्वप्रथम वहाँ के लोगों को पूर्व सूचना एवं दवाब मुक्त सहमति के अनुरूप सार्वजनिक चर्चा करना अनिवार्य होगा और जब वहाँ के निवासी इस योजना पर अपनी सहमति और समर्थन देंगे तभी वह योजना उस क्षेत्र में कार्यान्वित हो सकती है ।

मार्च 2020 को पर्यावरण मन्त्रालय ने इस प्रारूप को सार्वजनिक किया था और इसे नागरिकों के परामर्श के लिए आमंत्रित किया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन के प्रारूप के अन्तर्गत ऐसी अनेक प्रकार की विकासात्मक योजनाएँ आतीं हैं जिनका क्रियान्वयन विभिन्न सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों के द्वारा होता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के अनुसार इन सभी संस्थाओं को सम्बन्धित मन्त्रालय से ‘पर्यावरण स्वीकृति’ लेना अनिवार्य होता है जिसके पश्चात ही वह कोई कारख़ाना है या अन्य किसी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। विकासात्मक योजनाएँ अनेक प्रकार से भारत के नागरिकों और विशेषकर आदिवासियों को प्रभावित करती आई है।
इन योजनाओं को लागू करने में जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण का दोहन होना लगभग तय होता है और प्रतिफल में आदिवासियों को विस्थापन, पलायन, ग़रीबी और प्रदूषण मिलता है। अनेक पर्यावरणविद तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस बात की गहन चिन्ता है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 का प्रारूप 1986 के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के मौलिक तत्वों का नाश कर देगा । यदि इस प्रारूप को पर्यावरण मन्त्रालय ने सदन में रखा और यह क़ानून बनने में सफल हो गया तो आने वाले समय में इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं ।
यदि हम पर्यावरण प्रभाव आकलन के तहत सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रक्रिया के कालक्रम को देखें तो हमें वर्ष 1984 में वापस जाना होगा जब भोपाल शहर कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से गैस रिसाव की एक दुखद दुर्घटना की चपेट में आ गया था। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से गैस के रिसाव से कई लोग मारे गये और हजारों प्रभावित हुए थे। आज तक भोपाल के लोग 1984 की भयावह घटना को याद करते हुए सिहर उठते हैं। समाज में एक तीव्र आक्रोश था और नागरिकों ने सरकार पर अभूतपूर्व दबाव बनाया था। सरकार इस प्रकार के अक्षम्य अपराध के लिए कड़े दण्ड के साथ मजबूत और शक्तिशाली कानून के निर्माण की पहल करने के लिए मजबूर हो गयी थी और वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया।
इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत एक विशेष आहर्ता थी जिसे आज हम पर्यावरण प्रभाव आकलन के नाम से जानते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया 1994 में अस्तित्व में आयी। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके तहत किसी भी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थापना से उस क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के निवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी एक विस्तृत आकलन करती है। आकलन के पश्चात प्रतिवेदन को सम्बन्धित मन्त्रालय में प्रस्तुत कर के वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था। परियोजनाओं में कोयला खदानों, लोहे के खदानों, बांधों के निर्माण, राजमार्गों के निर्माण, प्रतिष्ठानों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे से लेकर बड़ी संख्या में संरचना इस पर्यावरण प्रभाव आकलन के अन्तर्गत आते थे। प्रतिष्ठानों को पर्यावरण मन्त्रालय के तहत 1986 और 1994 के अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करना होता था।
आइए हम सरकार के मानदण्डों के अनुसार पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया को भी समझें। पहले हम आदर्श स्थिति पर चर्चा करेंगे और फिर पूरी प्रक्रिया में कमियों और वास्तविक वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी या प्रतिष्ठान जो कुछ परियोजना या उद्योग स्थापित करना चाहता है वह सबसे पहले एक संभावित निर्माण-स्थान का चयन करता है। तत्पश्चात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुसरण शुरू होता है। पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के बाद प्रतिष्ठान या कम्पनी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करती है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र सम्बन्धित मन्त्रालय से निश्चित प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त होती है।
इस बीच परियोजना के सम्बन्ध में एक सामान्य सार्वजनिक परामर्श प्रभावित जनों के साथ होती है और इस आशय की सार्वजनिक सुनवाई भी अनिवार्य रूप से होती है। फिर सार्वजनिक सुनवाई से प्राप्त रिपोर्ट एक मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस समिति में विशेषज्ञ और वैज्ञानिक होते हैं जो कम्पनी के प्रस्ताव को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित परियोजना का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ समिति परियोजना से होने वाले फायदे और नुकसान का आकलन करती है। समिति इस प्रक्रिया में फायदे और नुकसान का तुलनात्मक अध्ययन करती है।
यदि समिति को लगता है कि प्रस्तावित परियोजना से फ़ायदे अधिक हैं और नुक़सान कम, तब उस परियोजना को आगे की कार्रवाई के लिए समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। यदि प्रस्तावित परियोजना में नुक़सान की अधिकता और फ़ायदों की कमी होती है तो समिति पहले इन कमियों को दूर करने की वैकल्पिक साधनों की तलाश करती है। यदि समिति को यह महसूस होता है कि प्रस्तावित परियोजना में नुक़सानदायक तत्वों की अधिकता है और अथक प्रयास के बाद भी इनको हटाया नहीं जा सकता है, तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। अन्यथा कम्पनी को पर्यावरण मन्त्रालय के माध्यम से स्वीकृति मिल जाती है। ऊपर की गयी चर्चा एक आदर्श स्थिति की है।
वास्तविकता में क्या होता है, इस पर गम्भीर चर्चा की आवश्यकता है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है या निश्चित मानदण्ड के अनुसार जो सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए, वो अनेक बार होती ही नहीं है। यहाँ तक कि कई बार अगर किसी तरह की सार्वजनिक सुनवाई होती भी है, तो कम्पनी के द्वारा प्रपंच रचा जाता है और कम्पनी के लोग ही परोक्ष रूप से ग्रामीणों की ओर से प्रतिनिधित्व कर लेते हैं। कई बार कम्पनी के गुंडे स्थानीय लोगों को कम्पनी के प्रस्ताव का अनुपालन करने के लिए उन्हें धमकाते हैं ताकि ग्रामीण प्रस्तावित परियोजना के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया दें। ऐसा ही एक केस अध्ययन झारखंड स्थित घाटो का है। सामाजिक कार्यकर्ता और नेत्री श्रीमती गीताश्री उराँव की पहल से ‘राष्ट्रीय हरित अधिकरण’, में मामला दर्ज किया गया और अब कम्पनी पीछे हट रहीं है। पर ऐसे सफलता के उदाहरण गिने चुने हैं।
अनेक बार यह भी हुआ है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट जाली बना लिए जाते हैं और उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। यद्यपि पर्यावरण प्रभाव आकलन को 2006 में भी बदला गया था किंतु वह भी इस आकलन प्रक्रिया में उपस्थित त्रुटियों को रोक पान में असमर्थ था। इतने मजबूत कानून होने के पश्चात भी यह देखा गया था कि सार्वजनिक सुनवाई को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। आकलन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। यदि कोई कम्पनी या किसी योजना में त्रुटि दिखाई देती थी या कोई अवहेलना होती थी तो उसे दूर करने की इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिलती है । दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि योजना की क्रियान्वयन के कारण जो पर्यावरण क्षति होती थी उसके लिए कोई भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कड़े कदम लेती है।
यदि आप भारत के प्रमुख पर्यावरणीय त्रासदियों को याद करेंगे तो 1984 का कुख्यात भोपाल गैस त्रासदी आज भी विचलित करता है। हाल के दिनों में असम में तेल के कुओं में आग लगने का कारण अनुचित प्रबन्धन ही था। हाल में एक अन्य उदाहरण विशाखापत्तनम में एक रासायनिक संयंत्र से गैस रिसाव का है जहाँ कम्पनी ने वास्तव में पर्यावरण मन्त्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति कभी हासिल ही नहीं की थी। विशाखापत्तनम के एलजी पॉलेमर गैस रिसाव त्रासदी 7 मई 2020 को घटी और जिसमें 20 लोग मारे गए और अनेक प्रभावित हुए। यह त्रासदी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया 1994 का उपहास उड़ाने वाला कृत्य है। विशाखापत्तनम गैस रिसाव त्रासदी उपरोक्त क़ानून को नज़रंदाज़ करने का ही परिणाम था।
असम के तेल के मामले में भी यह बताया गया कि इस संदर्भ में कोई सार्वजनिक सुनवाई हुई ही नहीं थी। इसलिए हम देख सकते हैं कि कभी-कभी कम्पनी या प्रतिष्ठान, राज्य द्वारा स्थापित नियमों और क़ानून को कितनी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। यह स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की भागीदारी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। प्रशासन और स्थानीय प्राधिकारियों की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रतिष्ठान का पूर्ण रूप से कार्यान्वित होना लगभग असम्भव है। इसमें स्थानीय स्तर के नेताओं का समर्थन भी शामिल हो सकता है।
इन परिस्थितियों में ये कम्पनियां और प्रतिष्ठान इतनी आसानी से नियमों की अनदेखी कर देती हैं कि आपदाएँ अपरिहार्य हो जाती हैं। जहाँ सरकार को पहले से उपस्थित क़ानून को और अधिक सख्त बना कर सख़्ती से उन्हें लागू करवाना चाहिए था ताकि उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माना हो सके और कोई किसी के जीवन से खिलवाड़ करने की हिमाक़त ना कर सके, वहाँ सरकार उल्टे, पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 प्रारूप ला कर 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सजग होना चाहिए और इस बात पर पुरज़ोर बल देना चाहिए कि मौजूदा कानूनों को ही पहले हम सही ढंग से अक्षरश: लागू करवा लें तब आगे की सोचें।
भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मन्त्रालय ने 83 पृष्ट का ‘पर्यावरण प्रभाव आकलन’, का प्रारूप 2020 सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध किया है और 11 अगस्त 2020 तक टिप्पणी करने के लिए आम नागरिकों के लिए खुला है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो गम्भीर चिन्ता का विषय हैं और मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक को इस पर जागरूक होना चाहिए और गम्भीरता से विचार करना चाहिए । पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 का प्रारूप निश्चित रूप से वास्तविकता में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कमजोर करेगा।
पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पास प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए अधिक अवसर होगा और बदले में आसपास के जंगलों और अन्य प्राकृतिक स्थानों में निवास करने वालों के जीवन और उनकी आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करेगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के प्रारूप के कुछ गम्भीर और चिन्ता जनक तथ्यों की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। आने वाले समय में यदि सरकार इन बिंदुओं पर अपना पक्ष स्पष्ट करती है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा।.jpg)
सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 का नया प्रारूप कार्योत्तर स्वीकृति के प्रावधान को अहम स्थान देता है। कार्योत्तर स्वीकृति के अनुसार एक प्रतिष्ठान बिना पर्यावरण प्रभाव आकलन के अपने परियोजना की शुरुआत कर सकता है। इसके उपरांत वह अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया के लिए प्रयास करेगा। यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है क्योंकि कोई एक कम्पनी भारी लागत के साथ अपने प्रतिष्ठान को कहीं स्थापित करने का प्रयास करेगी और एक बार वह उस क्षेत्र में स्थापित हो गया तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन होगा। तब क्या होगा जब उक्त प्रतिष्ठान को पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति अस्वीकार कर देगी? यहाँ पर 2020 का प्रारूप बहुत स्पष्ट नहीं है। कार्योत्तर स्वीकृति वास्तव में 1994 के पर्यावरण प्रभाव आकलन की आत्मा को ही मार देगा। दूसरी बात, यह कार्योत्तर स्वीकृति प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा जो लंबे समय से पर्यावरण स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं।
जरा सोचिए कि यदि एक बार फिर से विशाखापत्तनम या असम या भोपाल के जैसे मामले हुए तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन लेगा। यदि कार्योत्तर स्वीकृति को ड्राफ्ट में लाया जाता है और बाद में यह एक क़ानून बन जाती है तो अनेक त्रासदियों को कानूनी कवच मिल जाएगा और कहीं ना कहीं बड़े छोटे त्रासदी को क़ानूनन चुनौती देना अत्यंत कठिन हो जाएगा। कम्पनी और सभी प्रतिष्ठान कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाएँगे। इस प्रकार से सम्भवतः कोई भी प्रतिष्ठान कहीं भी स्थापित हो सकेगा और हम और हमारे आने वाली पीढ़ी के सर पर एक तलवार हमेशा लटकती रहेगी कि ना जाने कौन सी त्रासदी कब और कहाँ हो जाए?
अप्रैल 2020 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कार्योत्तर स्वीकृति (पोस्ट फ़ैक्टो इन्वायरॉन्मेंटल क्लीयरेंस) की आलोचना की थी।अलेंबिक फ़ार्मा बनाम रोहित प्रजापति अपील संख्या 1526/2016 सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी चिन्ता ज़ाहिर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि सार्वजनिक परामर्श एक संवैधानिक अधिकार है और इसका अनुसरण हर हाल में होना चाहिए।
सरकार पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के प्रारूप के साथ अप्रत्याशित जल्दबाजी दिखा रही है। यह इनके मकसद और इरादे पर सवाल खड़ा करता है। पृष्ठ संख्या 47 के बिंदु संख्या 3.1 के अनुसार, सामान्य सुनवाई का समय जो पहले 30 दिनों में होता था, मन्त्रालय द्वारा घटाकर 20 दिन कर दिया गया है।सार्वजनिक सुनवाई के लिए किसी भी प्रकार का कोरम ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया COVID-19 के अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है और इस घड़ी में सरकार को किसी भी ड्राफ़्ट को लाने से बचना चाहिए था। इस संकट के दौरान प्रारूप को जमीनी स्तर पर संभावित प्रभावितों से चर्चा कर पाना अत्यंत कठिन है।
सामाजिक संगठनों और पर्यावरणविद् को जमीनी स्तर पर आपसी समन्वय और चर्चा कर पाना भी मुश्किल है। वास्तव में जो इस 2020 के प्रारूप के सबसे अधिक प्रभावित होंगे उन तक शायद बात कभी पहुँच ही ना सके और क़ानून बनाने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए। यह संवैधानिक आधिकार का हनन होगा। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद ने इस पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के नए प्रारूप की कड़ी आलोचना की है। आम जनों के साथ सामान्य चर्चा और सार्वजनिक परामर्श करना भी लगभग कोरोना काल में असम्भव है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के प्रारूप के पृष्ठ संख्या 9 में योजनाओं को तीन वर्ग A, B1 और B2 में रखा गया है। वर्ग B2 में ऐसी अनेक योजनाएँ आएँगी जिसमें विशेषज्ञों की मूल्यांकन समिति की स्वीकृति आनिवार्य नहीं होगी।
इसी में 9 (7) के अन्तर्गत ऐसी अनेक योजनाएँ होंगी जो आम जन के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आएँगी और इन परियोजनाओं से सम्बन्धित कोई भी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से साझा नहीं की जाएगी। ज़िम्मेदार नागरिक के नाते हम सब राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इसका ज़रूर सम्मान करते हैं, पर यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इसको रोकेगा कौन?
पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के प्रारूप के पृष्ठ संख्या 29 के बिंदु 22 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान का ज़िक्र है। इसके अन्तर्गत, यदि कोई प्रतिष्ठान या परियोजना किसी स्तर पर नियम की अवहेलना करता है तो शिकायत का अधिकार स्वयं प्रतिष्ठान के पास होगी, या किसी सरकारी अधिकारी, या मूल्यांकन समिति और इस के अलावा विनियमन प्राधिकरण को ही मात्र हस्तक्षेप का अधिकार होगा। ऐसे किसी प्रतिष्ठान या परियोजना जो कार्योत्तर स्वीकृति के द्वारा पहले ही स्थापित हो चुकी है, नियम की अवहेलना के लिए सरकार ने अर्थ दण्ड का प्रावधान रखा है और उस संयंत्र को बंद करने का भी प्रावधान है।हम सभों को समझना होगा कि पर्यावरणीय की क्षतिपूर्ति पैसों से नहीं की जा सकती है।
प्रकृति की मूल स्तिथि को पुनः प्राप्त करना लगभग असम्भव है। पर्यावरणीय सूचकांक के अनुसार भारत में पारिस्थितिक क्षरण की दर बढ़ रही है। पृष्ट संख्या 83 में परिशिष्ट 15 में उल्लंघन के मामले में संभावित प्रक्रिया का ज़िक्र है। किंतु इसे व्यवहार्य में लाना उपरोक्त कारणों से असाध्य लगता है। आम जन के पास किसी गड़बड़ी को चिन्हित करने का कोई शक्ति निहित नहीं है। क्या इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सम्भव है? अब आप समझ सकते हैं कि मैंने फ़्रेंड्स ओफ़ द अर्थ इंटर्नैशनल वाली वाक़या की चर्चा क्यों की थी।
पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के प्रारूप, सरकार को अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से सौ किलोमीटर हवाई दूरी के तहत आने वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखती है। आम जनता उन क्षेत्रों में किसी भी योजना के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न उठाने के अधिकार को खो देगी।
यदि हम सावधानीपूर्वक भारत के मानचित्र को देखें तो सौ किलोमीटर की हवाई दूरी एक विशाल क्षेत्र हो सकती है। संसाधन संपन्न भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के नए प्रारूप की सबसे बड़ा दंश अनुभव कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन के मामले में जनता को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि यह एक निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है। पहले से ही कानून के तहत सरकार को ये अधिकार है कि कुछ रणनीतिक कारणों को वह सार्वजनिक नहीं कर सकती है और यह सार्वजनिक हस्तक्षेप के दायरे में नहीं आता है। भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते हम सभी इसका सम्मान करते हैं। पर यदि इस अधिकार का दुरुपयोग हुआ तो यह किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी?
आदिवासी समुदाय इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होगा। अधिकांश आदिवासी बहुल क्षेत्र 5 वीं और 6 ठी अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं। इतने शक्तिशाली प्रावधानों और क़ानून के पश्चात भी आदिवासियों की परिस्थिति बदतर होती जा रही हैं। इन प्रावधानों और क़ानून को कभी भी सही ढंग से लागू नहीं किया गया और यदि यह प्रारूप क़ानून बन गया तब अत्यंत दयनीय स्तिथि हो जाएगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान अब आदिवासी समाज का और अधिक शोषण करने में सक्षम होगा। आदिवासी क्षेत्र आज भी अनेक प्रकार के संसाधनों को संचित कर के रखने में सफल हुए हैं क्योंकि आदिवासी समाज इनका उपयोग सतत प्रक्रिया से करता आया है ना की लालच पर। आदिवासी समाज अब और बड़ी संख्या में मूकदर्शक बन कर अपनी त्रासदी देखेगा। नए प्रस्तावित प्रावधान में अनापत्ति पत्र किसी भी खनन योजना को 30 वर्ष की जगह 50 वर्ष तक की वैधता देती है। एक पीढ़ी तो शायद ग़ुलाम ही पैदा होगी।
.