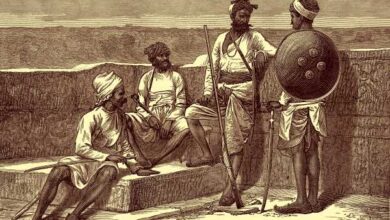अमेरिका के विख्यात मानवशास्त्री प्रोफ़ेसर रॉबर्ट राफ़ ने लुप्तप्राय भाषाओं पर गहन अध्ययन किया है और उनका एक निष्कर्ष बड़ा रोचक है। उन्होंने अपने अनुसन्धान में यह सिद्ध किया कि जिस समाज में धार्मिक क्रियाएँ मातृभाषा में होती हैं वे भाषाएँ स्वयं ही संरक्षित होती हैं। इसके पहले मैंने लुप्तप्राय भाषा पर लेख लिखा था। यह स्पष्ट हुआ कि मातृभाषा, धर्म और संस्कृति के मध्य प्रगाढ़ सम्बन्ध होते हैं। और यहीं से प्रेरणा मिली कि इस संवेदनशील विषय पर भी लिखना चाहिए।
भारत में लगभग 12 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है और इन आदिवासियों में प्राकृतिक या मूल आदिवासी धर्म में आस्था रखने वालों की तादाद अच्छी ख़ासी है। पूरे भारतवर्ष में 80 से भी अधिक मूल आदिवासी धर्म के प्रकार देखने को मिलती है। सभी आदिवासी धर्मों में मूल विधि सामान है किन्तु उनके आदिवासी धर्म के शब्दावली अलग-अलग हैं।
विशिष्ट आदिवासी धार्मिक पहचान की आवश्यकता क्यों? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न और इसके उत्तर, दोनो का आम जन तक सम्प्रेषण अनिवार्य है। जब तक यह सही ढंग से सम्प्रेषित नहीं होगा तब तक एक वृहद् सामाजिक आन्दोलन खड़ा नहीं हो सकेगा। जनगणना के प्रारूप से यह स्पष्ट हुआ कि ‘अन्य धर्म’ का जो रिक्त स्थान होता है उसकी कोडिंग नहीं होती है। लोगों को जनगणना के दौरान प्रारूप में उपस्थित छः धर्मों में से ही किसी एक को चुनना अनिवार्य हो गया था । यह एक अत्यधिक चिन्ता वाली बात है। इस संशोधन से अब आदिवासियों की जनसंख्या निश्चित तौर पर कम दर्शायी जानी थी। दूसरा सबसे बड़ा धक्का यह लगा कि आदिवासियों को अब अन्य धर्म की ओर धकेला जाने लगा। हमारे देश में धर्म और राजनीति में निकटतम सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध ही आदिवासियों को असुरक्षित और आघात योग्य बनाती है।
ऐसे अनेक देश हैं जहाँ अपने पूर्वजों के मूल आदिवासी धर्म के साथ साथ नये धर्म का समावेश बिना किसी अवरोध के देखने को मिलता है। फ़िलिपींज़, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में आदिवासी धर्म के साथ साथ अन्य धर्म का पालन सौहार्द के साथ होता है। किन्तु अनेक देशों में यह भी देखने को मिला है कि उन्हें आदिवासी धर्म को त्यागने पर मजबूर कर के राष्ट्रीय धर्म को मानने पर विवश किया जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले हैं और वहाँ के आदिवासी समुदाय ने एकजुट होकर इसका विरोध भी किया है और अपने आदिवासी धर्म की संवैधानिक मान्यता के लिए ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। इंडोनेशिया में संगठित आदिवासी समुदायों के एक संगठन, ‘अमान’, ने एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है।
भारत जैसे देश में जहाँ अनेक धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं, यहाँ आदिवासियों को परोक्ष रूप से भारत के मूल निवासी के रूप में पहचान प्राप्त है। ऐसे में एक अलग आदिवासी धर्म कोड की माँग न्यायसंगत है। यह मात्र एक इच्छा या मंशा नहीं है, अपितु यह एक संवैधानिक अधिकार है। वर्ष 2006 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था तब सरना कोड की माँग को लेकर कुछ सामाजिक और राजनैतिक प्रतिनिधि जंतर-मंतर में धरना दे रहे थे। हम विद्यार्थियों में से कुछ लोग वहाँ शरीक हुए थे और एक अच्छा अनुभव हुआ था । पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा से भी इस बीच धार्मिक पहचान की लड़ाई पर अनेकों बार चर्चा हुईं। वर्ष 2007 में ज्ञात हुआ कि सरना कोड की माँग को लेकर एक प्रतिनिधि दल रेजिस्ट्रार जेनरल से भी मिला था। कुछ बातें निकल कर पुनः सामने आयीं और वे बड़ी चुनौती थीं। शायद लगा, ये हमारे बस की बात नहीं। वर्षों बीत गये और अलग धार्मिक पहचान के लिए जनगणना में एक अलग से कोड का प्रावधान आज तक सुनिश्चित नहीं हो सका।
दिल्ली में रेजिस्ट्रार जेनरल ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि आदिवासी धर्म कोड की माँग अनेक स्थानों से उन्हें बराबर मिलती रहीं हैं। उन्होंने साझा किया कि हर प्रान्त से अलग नाम से माँग है। झारखण्ड से सरना कोड की माँग है तो मध्य प्रदेश से गोंडी की, राजस्थान से भीली धर्म कोड के लिए माँग है तो छत्तीसगढ़ से कोया पुनेम की। ठीक उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासियों की भी अलग शब्दावली वाली धर्म कोड की माँग है। इन सभों की माँग जायज़ है क्योंकि ये सभी मूल आदिवासी प्राकृतिक धर्म को मानने वाले धर्म हैं। किन्तु रेजिस्ट्रार जेनरल ने एक उचित बात सबके समक्ष रखी थी। उन्होंने कहा कि इन सभी को एक ही आदिवासी धर्म के लिए विभिन्न कॉलम नहीं दिया जा साथ है।
मेरी समझ में इसका एक सरल समाधान है। जिस प्रकार भारत के 732 से भी अधिक जनजाति स्वयं को पहले अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत रखते हैं और बाद में अपने उपजाति के स्थान पर उराँव, मुंडा, हो, गोंड, भील, संथाल, नागा इत्यादि का प्रयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार भारत के सारे प्राकृतिक धर्म को मानने वाले आदिवासी अपनी उप धर्म सरना, जाहेर, गोंडी, भीली, कोया पुनेम इत्यादि लिख सकते हैं। जहाँ तक मुख्य धर्म की शब्दावली की बात है, तो सभी आदिवासी समाज को एकजुट होकर एक नाम पर सहमति बनानी होगी। चाहे वह आदि धर्म हो या कोया पुनेम या फिर सरना धर्म या आदिवासी धर्म।
आदिवासियों को धार्मिक पहचान के संघर्ष में एकजुट होना होगा। अभी जो समय की माँग है, वह एक वृहद् सामाजिक आन्दोलन की है। कुछ समय के लिए राजनैतिक आन्दोलन को दरकिनार करना होगा। मेरी समझ के अनुसार निश्चित ही सामाजिक आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन का संपूरक बन के साथ चलना चाहिए किन्तु निम्नलिखित टिप्पणी को पहले हम समझने का प्रयास करें। वर्षों से सामाजिक आन्दोलन और राजनैतिक आन्दोलन साथ साथ चले किन्तु बहुत सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिला। इसका एक कारण है। मेरा अध्ययन सही नहीं भी हो सकता है किन्तु मंथन आवश्यक है।
अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि जहाँ राजनैतिक उद्देश्य की बात होती है वहाँ समाज विभाजित हो जाता है, चाहे वह कोई भी समाज हो और कोई भी राजनैतिक दल हो। और इसलिए मैंने ज़ोर दिया है कि अभी भारत के सम्पूर्ण आदिवासियों को सामाजिक आन्दोलन की आवश्यकता है और सामाजिक प्रतिनिधि करने वालों को भी एक निस्वार्थ प्रयास करना होगा। सामाजिक हित में व्यक्तिगत आकांक्षाओं को त्यागना होगा। तभी कुछ सार्थक परिणाम होंगे अन्यथा ये संघर्ष आपके बाद भी पीढ़ी डर पीढ़ी चलते रहेंगे जब तक आदिवासी पूरी तरह मिट नहीं जाते।
अनेक धार्मिक सम्मेलन और चर्चाओं में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे आदिवासी समुदायों की चर्चा में प्रायः एक बड़ी विडम्बना देखने को मिलती है। पूरी सभा में एक दो ज़रूर ऐसे उपस्थित रहते हैं जिनका काम ही सामूहिक प्रस्तावों का खण्डन करना होता है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक पक्ष का अलग दृष्टिकोण होता है। किन्तु खण्डन तभी स्वीकार्य होना चाहिए जब सुझाव साथ हो। अनेक बार यह महसूस किया गया है कि खण्डन अहंकार से प्रेरित होता है। यह भी सम्भव है कि ऐसा व्यक्ति बाहरी शक्ति से प्रभावित हो और वह किन्ही और से नियन्त्रित हो रहा हो। समाज को ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है।
विफलता का एक प्रमुख कारण हम सब भी हैं। मात्र त्योहारों में अपना प्राकृतिक धर्म या सरना धर्म जैसे तैसे निभा लेने से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके धर्म की गरिमा और पहचान बनी रहेगी। बाक़ी साल भर हमारी धार्मिक आस्था कहीं और नज़र आती है। इस प्रकार के अधूरे मन से किए गये प्रयास कैसे सफल होंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें ही देना है। शहरी क्षेत्र में आदिवासी धर्म के पालनकर्ता नगण्य हैं, कम से कम मोनोवृत्ति तो ऐसी ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक बार भ्रमण करने का और धार्मिक सम्मेलनों को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अवलोकन से यह बात स्पष्ट होती है कि हमें सामाजिक आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है। धार्मिक आन्दोलन में मात्र हमारी माँ और बहनें ही पूर्ण रूप से शामिल होती हैं।
पारम्परिक वेशभूषा, आराध्या गीत और संगीत में मुख्य रूप से महिलाएँ ही बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। पुरुष वर्ग ऐसे समय में भी एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं। यह एक बड़ी कमी है। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा जो रोचक है। धार्मिक आन्दोलन को जब राजनैतिक सानिध्य की आवश्यकता हुई और अनेक स्थानों में धरना प्रदर्शन भी हुए तब एक साक्षात्कार के दौरान एक महिला ने यह बात कही कि जब संघर्ष की बात आती है तो उन्हें प्रथम पंक्ति में लाठी खाने के लिए ढकेल दिया जाता है। और वहीं जब धार्मिक सामाजिक अधिकार की बात होती है तो उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। पिछले दशक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आदिवासी समाज में देखने को मिला है जिसमें अब महिलाओं को बराबरी का धार्मिक अधिकार प्राप्त हुआ है। और उन्होंने इस अधिकार को बखूबी निभाया भी है।
संयुक्त राष्ट्र संघ, जेनीवा में 2009 में ही जब प्रथम बार ‘एक्स्पर्ट मेकनिज़म ऑन राइट्स ओफ़ इंडिजेनस पीपल्ज़’ की सभा हुई थी तब मैंने वहाँ आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक पहचान के लिए माँग रखी थी। संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी मामलों के देखने वाले अधिकारी से भी अलग से समय ले कर चर्चा की थी। वहाँ से कुछ तथ्य निकल कर सामने आए थे उनकी चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी मामलों के देखने वाले अधिकारी ने स्पष्ट किया था कि वे इस मामले में संज्ञान ले सकते हैं किन्तु भारत के आदिवासियों के बीच से धार्मिक पहचान के लिए ज़मीनी सामाजिक आन्दोलन देखने को नहीं मिले हैं। उन्होंने बतलाया था कि भारत सरकार का अभी तक कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। भारत सरकार का हमेशा से कहना है कि उन्होंने आदिवासियों को ‘अनुसूचित जनजाति’ के अन्तर्गत पहले से ही विशेष प्रावधान संविधान में दे रखा है।
13 सितम्बर 2007 को विश्व भर के आदिवासियों के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन आदिवासियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंगीकृत किया था। अनेक राष्ट्र तुरन्त इसके विरोध में खड़े हो गये थे। किन्तु धीरे धीरे विकसित राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ़िनलैंड इत्यादि ने समर्थन दिया। वहीं यूकरैन, प्रशांत महासागर के उपद्वीप देश, अनेक एशियाई देशों ने उदासीन रवैया अपनाया।
संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12.1 में विश्व के सभी आदिवासी एवं देशज समुदायों को अपने आदिवासी धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रावधान निहित किये हैं। और इसी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12.2 में विभिन्न सरकार को निर्देश है कि वे इन समुदायों के प्राचीन धर्म को बनाए रखने में हर प्रकार से सहयोग प्रदान करें।
कनाडा में वहाँ के आदिवासियों को ‘प्रथम नागरिक’ या ‘फ़र्स्ट नेशन’ का दर्जा प्राप्त है। शुरूआत में कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का विरोध किया था। उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र कनाडा के संविधान के अनुकूल नहीं था और विशेष रूप से कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 35 के ठीक विपरीत था। ‘असेम्ब्ली ओफ़ फ़र्स्ट नेशन’, ने जब संगठित होकर इसके लिए दबाव बनाया तब उनको उत्तर देते हुए तब की कनाडा की सरकार ने कहा कि कुछ आदिवासियों के हित के रक्षा के लिए हम अन्य सामान्य नागरिकों के साथ असंतुलित व्यवहार नहीं कर सकते हैं। असेम्ब्ली ओफ़ फ़र्स्ट नेशन का संगठित प्रयास होता रहा और अन्ततः 12 नवम्बर 2010 को कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया।
ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम चला। और 3 अप्रैल 2009 को ‘रुड्ड सरकार’ ने आदिवासियों के संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया जिसके लिए उनके संविधान में विशेष बदलाव भी करना पड़ा। तत्पश्चात्, ऑस्ट्रेलिया के अनेक सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत पारम्परिक उद्घोषणा के साथ होती है जिसमें वे उस भूमि के पारम्परिक स्वामी, वहाँ के आदिवासियों का आभार व्यक्त करते हैं। वे उन सभी अतीत के आदिवासी पुरखों, वर्तमान आदिवासी समुदाय और आने वाली इस पवित्र भूमि की पीढ़ी का भी आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की उदघोषणा इस बात की परिचायक है कि ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ के आदिवासियों को उनके खोये हुए अधिकार, सम्मान के साथ वापस किया है।
न्यूजीलैंड सरकार ने ‘माओरी’ आदिवासियों के दबाव में 19 अप्रैल 2010 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था। उत्तरी अमेरिका ने भी 16 दिसम्बर 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया।
विकसित देशों से जो सफल उदाहरण हमें देखने को मिले हैं उनका यहाँ एक विशेष सन्दर्भ है। उन देशों में मानवाधिकार के प्रति लोग जागरूक हैं। उन सबमें सामूहिकता है। शिक्षित जन, समाजिक बदलाव को सकारात्मक ढंग से देखते हैं और छद्म उद्देश्यों के लिए समाज को ताक पर नहीं रखते हैं। आपको यदि अपने समाज के अस्तित्व के लिए विशिष्ट धार्मिक पहचान चाहिए तो एकजुट होना होगा।
.