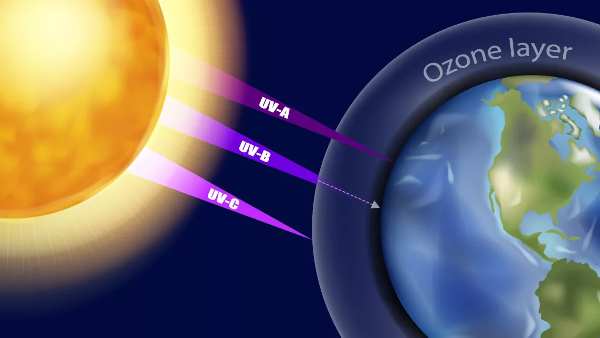पर्यावरण: खाने का और दिखाने का और
पाँच जून को ‘पर्यावरण दिवस’ मनाया जाता है। गिनती में यह कुछ भी हो, पर चरित्र में, पर्यावरण की समझ में, यह पहले समारोह से अलग नहीं होता। 1972 में सौ से अधिक देश संयुक्त राष्ट्र संघ के छाते के नीचे पर्यावरण की समस्याओं को लेकर इकट्ठे हुए थे। तब विकास और पर्यावरण में छत्तीस का रिश्ता माना गया था। सरकारें आज भी पर्यावरण और विकास में खटपट देख रहीं है, इसलिए प्रतिष्ठित हो चुके विकास-देवता पर सिन्दूर चढ़ाती चली जा रही हैं। लेकिन विकास के इसी सिन्दूर ने पिछले दौर में पर्यावरण की समस्याओं को पैदा किया है और साथ ही अपने चटख लाल रंग में उन्हें ढकने की भी कोशिश की है।
सरकारी कैलेंडर में देखें तो पर्यावरण पर बातचीत 1972 में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू होती है। पश्चिम के देश चिन्तित थे कि विकास का कुल्हाड़ा उनके जंगल काट रहा है, विकास की पताकानुमा उद्योग की ऊँची चिमनियाँ, सम्पन्नता के वाहन, मोटर गाड़ियाँ आदि उनके शहरों की हवा ख़राब कर रही हैं, देवता सरीखे उद्योगों से निकल रहा ‘चरणामृत’ वास्तव में वह गन्दा और जहरीला पानी है, जिसमें उनकी सुन्दर नदियाँ, नीली झीलें अन्तिम सांसें गिन रही हैं।
यह देश जिस तकनीक ने उन्हें यह दर्द दिया था, उसी में इसकी दवा खोज रहे थे। पर तीसरी दुनिया के ज़्यादातर देशों को लग रहा था कि पर्यावरण संरक्षण की यह नयी बहस उनके देशों के विकास पर ब्रेक लगा कर उन्हें पिछड़ा ही रहने देने की साजिश है। ब्राज़ील ने तब ज़ोरदार घोषणा की थी कि हमारे यहाँ सैकड़ों साफ नदियाँ हैं, चले आओ, इनके किनारे अपने उद्योग लगाओ और उन्हें गन्दा करो। हमें पर्यावरण नहीं, विकास चाहिए। भारत ने ब्राज़ील की तरह बाहर का दरवाज़ा जरूर नहीं खोला, लेकिन पीछे के आँगन का दरवाजा धीरे से खोलकर कहा था कि गरीबी से बड़ा कोई प्रदूषण नहीं है। गरीबी से निपटने के लिए विकास चाहिए। और इस विकास से थोड़ा बहुत पर्यावरण नष्ट हो जाए तो वह लाचारी है हमारी। ब्राज़ील और भारत के ही तर्क के दो छोर थे और इनके बीच में थे वे सब देश जो अपनी जनसंख्या को एक ऐसे भारी दबाव की तरह देखते थे, जिसके रहते वे पर्यावरण संवर्धन के झण्डे नहीं उठा पाएँगे। इस दौर में वामपन्थियों ने भी कहा कि ‘हम पर्यावरण की विलासिता नहीं ढो सकते।’
इस तरह की सारी बातचीत ने एक तरफ तो विकास की उस प्रक्रिया को और भी तेज किया जो प्राकृतिक साधनों के दोहन पर टिकी है और दूसरी तरफ गरीबों की जनसंख्या को रोकने के कठोर से कठोर तरीके ढूँढे। इस दौर में कई देशों में संजय गाँधियों का उदय हुआ, जिन्होंने पर्यावरण संवर्धन की बात आधे मन और आधी समझ से, पर परिवार नियोजन का दमन चलाया पूरी लगन से। लेकिन इस सबसे पर्यावरण की कोई समस्या हल नहीं हुई,बल्कि उनकी सूची और लम्बी होती गयी।

पर्यावरण की समस्या को ठीक से समझने के लिए हमें समाज में प्राकृतिक साधनों के बँटवारे को, उसकी खपत को समझना होगा। सेंटर फ़ॉर साइंस एँड एनवायर्नमेंट के निदेशक अनिल अग्रवाल ने इस बँटवारे का एक मोटा ढाँचा बनाया था। कोई 5 प्रतिशत आबादी प्राकृतिक साधनों के 60 प्रतिशत भाग पर क़ब्ज़ा किए हुए है। 10 प्रतिशत आबादी के हाथ में कोई 25 प्रतिशत साधन हैं। फिर कोई 25 प्रतिशत लोगों के पास 10 प्रतिशत साधन हैं। लेकिन 60 प्रतिशत की फटी झोली में मुश्किल से 5 प्रतिशत प्राकृतिक साधन हैं।
हालत फिर ऐसी भी होती, तो एक बात थी। लेकिन इधर 5 प्रतिशत हिस्से की आबादी लगभग थमी हुई है और साथ ही जिन 60 प्रतिशत प्राकृतिक साधनों पर आज उसका क़ब्ज़ा है, वह लगातार बढ़ रहा है। दूसरे वर्ग की आबादी में बहुत थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है और शायद उनके हिस्से में आए प्राकृतिक साधनों की मात्रा कुछ स्थिर सी है। तीसरे 25 प्रतिशत की आबादी में वृद्धि हो गयी है और उनके साधन हाथ से निकल रहे हैं। इसी तरह चौथे 60 प्रतिशत वाले वर्ग की आबादी तेज़ी से बढ़ चली है और दूसरी तरफ उनके हाथ में बचे-खुचे साधन भी तेज़ी से कम हो रहे हैं।
यह चित्र केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया का है। और इस तरह देखें तो कुछ की ज़्यादा खपत वाली जीवन शैली के कारण ज्यादातर की, 80-85 प्रतिशत लोगों की जिन्दगी के सामने आया संकट समझ में आ सकता है। इस चित्र का एक और पहलू है। आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा बस किसी तरह जिन्दा रहने की कोशिश में अपने आसपास के बचे-खुचे पर्यावरण को बुरी तरह नोचता-सा दिखता है तो दूसरी तरफ वह 5 प्रतिशत वाला भाग पर्यावरण के ऐसे व्यापक और सघन दोहन में लगा है जिसमें भौगोलिक दूरी कोई अर्थ नहीं रखती। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में लगे कागज उद्योग आसपास के जंगलों को हजम करने के बाद असम और उधर अंडमान निकोबार के जंगलों को भी साफ करने लगे हैं।
जो जितना ताक़तवर है चाहे वह उद्योग हो या शहर, उतनी दूरी से किसी कमज़ोर का हक छीन कर अपने लिए प्राकृतिक साधन का दोहन कर रहा है। दिल्ली जमुना किनारे है, उसका पानी तो वह पिएगी ही, पर कम पड़ेगा तो दूर गंगा का पानी भी खींच लाएगी। इंदौर पहले अपनी छोटी-सी खान नदी को अपने प्रदूषण से मार देगा और फिर दूर बह रही नर्मदा का पानी उठा लाएगा। भोपाल पहले अपने समुद्र जैसे विशाल ताल को कचराघर बना लेगा, फिर 80 किलोमीटर दूर बह रही नर्मदा से पीने के पानी का प्रबंध करने की योजना बना सकता है। पर नर्मदा के किनारे ही बसा जबलपुर नर्मदा के पानी से वंचित रहेगा, क्योंकि इतना पैसा नहीं है।
कुल मिलाकर प्राकृतिक साधनों की इस छीना झपटी ने उनके दुरुपयोग ने पर्यावरण के हर अंग पर चोट की है और इस तरह सीधे उससे जुड़ी आबादी के एक बड़े भाग को और भी बुरी हालत में धकेला है। आधुनिक विज्ञान, तकनीक और विकास के नाम पर हो रही यह लूटपाट प्रकृति से (ख़ास कर उसके ऐसे भंडारों से, जो दोबारा नहीं भरे जा सकेंगे, जैसे कोयला,खनिज पेट्रोल आदि) पहले से कहीं ज्यादा कच्चा माल खींच कर उसे अपनी जरूरत के लिए नहीं, लालच के लिए पक्के माल में बदल रही है। विकास कच्चे माल को पक्के माल में बदलने की प्रक्रिया में जो कचरा पैदा करता है, उसे ठीक से ठिकाने भी लगाना नहीं चाहता। उसे वह ज्यों-का-त्यों प्रकृति के दरवाज़े पर पटक आना जानता है।
इस तरह इसने हर चीज को एक ऐसे उद्योग में बदल दिया है जो प्रकृति से ज्यादा-से-ज्यादा हड़पता है और बदले में इसे ऐसी कोई चीज नहीं देता, जिससे उसका चुकता हुआ भण्डार फिर से भरे। और देता भी है तो ऐसी रद्दी चीजें, धुआँ, गन्दा जहरीला पानी आदि कि प्रकृति में अपने को फिर सँवारने की जो कला है, उसका जो सन्तुलन है वह डगमगा जाता है। यह डगमगाती प्रकृति, बिगड़ता पर्यावरण नये-नये रूपों में सामने आ रहा है। बाढ़ नियन्त्रण की तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले दस सालों में देश के पहले से दुगने भाग में, 2 करोड़ हेक्टेयर के बदले 4 करोड़ हेक्टेयर में बाढ़ फैल रही है। कहाँ तो देश के 33 प्रतिशत हिस्से को वन से ढकना था, कहाँ अब मुश्किल से 10 प्रतिशत वन बचा है।
उद्योगों और बड़े-बड़े शहरों की गन्दगी ने देश की 14 बड़ी नदियों के पानी को प्रदूषित कर दिया है। गन्दे पानी से फैलने वाली बीमारियों, महामारियों के मामले, जिनमें सैकड़ों लोग मरते हैं कभी दबा लिए जाते हैं तो कभी इस वर्ष की तरह सामने आ जाते हैं। इसी तरह कलकत्ता जैसे शहरों की गन्दी हवा के कारण वहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा साँस, फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हो रहा है। शहरों के बढ़ते कदमों से खेती लायक अच्छी जमीन कम हो रही है, बिजली बनाने और कहीं-कहीं तो खेतों के लिए सिंचाई का इन्तजाम करने के लिए बाँधे गये बाँधों ने अच्छी उपजाऊ जमीन को डुबोया है। इस तरह सिकुड़ रही खेती की जमीन ने जो दबाव पैदा किया उसकी चपेट में चारागाह या वन भी आए हैं। वन सिमटें हैं तो उन जंगली जानवरों का सफाया होने लगा है जिनका यह घर था।

किसान नेता शरद जोशी ने खेतों के मामले में जिस इण्डिया और भारत के बीच एक टकराव की-सी हालत देखी है: पर्यावरण के सिलसिले में प्राकृतिक साधनों के अन्याय भरे बँटवारे में यह और भी भयानक हो उठती है। इसमें इण्डिया बनाम भारत तो मिलेगा, यानी शहर गाँव को लूट रहा है, तो शहर-शहर को भी लूट रहा है, गाँव-गाँव को भी और सबसे अन्त में यह बँटवारा लगभग हर जगह के आदमी और औरत के बीच भी होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में ही जमनापार के लोगों का पानी छीन कर दक्षिण दिल्ली की प्यास बुझाई जाती है, एक ही गाँव में अब तक ‘बेकार’ जा रहे जिस गोबर से गरीब का चूल्हा जलता था अब सम्पन्न की गोबर गैस बनने लगी है और घर के लिए पानी, चारा ईंधन जुटाने में हर जगह आदमी के बदले औरत को खपना पड़ता है।
बिगड़ते पर्यावरण की इसी लम्बी सूची के साथ-ही-साथ सामाजिक अन्यायों की एक समानान्तर सूची भी बनती है। इन समस्याओं का सीधा असर बहुत से लोगों पर पड़ रहा है। पर क्या कोई इन समस्याओं से लड़ पाएगा? बिगड़ते पर्यावरण को सँवार न पाएँ तो फिलहाल कम-से-कम उसे और बिगड़ने से रोक पाएँगे क्या? इन सवालों का जवाब ढूँढ़ने से पहले बिगड़ते पर्यावरण के मोटे-मोटे हिस्सों को टटोलना होगा। विकास की सभी गतिविधियाँ ‘उद्योग’ बन गयी हैं या बनती जा रही हैं। खेती आज अनाज पैदा करने का उद्योग है, बाँध बिजली बनाने या सिंचाई करने का उद्योग है, नगरपालिकाएँ शहरों को साफ पानी देने या उसका गन्दा पानी ठिकाने लगाने का उद्योग है। सचमुच जो उद्योग हैं वे अपनी जगह हैं ही। इन सभी तरह के उद्योगों से चार तरह का प्रदूषण हो रहा है।
उद्योग छोटा हो या बड़ा, एक कमरे में चलने वाली मंदसौर की स्लेट-पैंसिल यूनिट हो या नागदा में बिड़ला परिवार की फ़ैक्टरी या समाजवादी सरकार का कारखाना–इन सबमें भीतर का पर्यावरण कुछ कम-ज़्यादा खराब रहता है। इसका शिकार वहाँ काम करने वाला मजदूर बनता है। वह संगठित है तो भी और असंगठित हुआ तो और भी ज़्यादा। फिर इन सबसे बाहर निकलने वाले कचरे से बाहर का प्रदूषण फैल रहा है। यह जहरीला धुआँ, गन्दा पानी वगैरह है। इसकी शिकार उस उद्योग के किनारे या कुछ दूर तक रहने वाली आबादी होती है। तीसरी तरह का प्रदूषण इन उद्योगों से पैदा हो रहे पक्के माल का है। जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएँ आदि। चौथा प्रदूषण वहाँ होता है जहां से इन उद्योगों का कच्चा माल आता है। इनमें से पहले तीन तरह के प्रदूषणों का कुछ हल निकल सकता है, वह आज नहीं निकल पाया है तो इसका कारण है मजदूर और नागरिक आन्दोलनों की सुस्ती।

आज भी परम्परागत मजदूर आन्दोलन उद्योग के भीतर के प्रदूषण को अपने संघर्ष का मुद्दा नहीं बना पाया है। ज्यादातर लड़ाई मजदूरी वेतन या बोनस को लेकर होती है। इसलिए कभी प्रदूषण का सवाल उठे भी तो इसे भी पैसे से तोल लिया जाता है। मध्य प्रदेश में सारणी बिजली घर की मजदूर यूनियन ने धुआँ कम करने की माँग के बदले धुआँ-भत्ता माँगा है। दूसरा प्रदूषण उद्योग से बाहर निकलने वाली चीजों का है। अगर उससे पीड़ित नागरिक संगठित हो जाएँ तो उससे भी लड़ा जा सकता है। पक्के माल के रूप में ही सामने आ रहे प्रदूषण से लड़ना जरा कठिन होगा, क्योंकि इसके लिए उन चीज़ों की खपत को ही चुनौती देनी पड़ेगी। लेकिन विकास के इस ढाँचे के बने रहते चौथी तरह के प्राकृतिक साधनों के कच्चे माल के रूप में दोहन के कारण हो रहे प्रदूषण से लड़ना सबसे कठिन काम होगा क्योंकि एक तो इस तरह का प्रदूषण हमारे आसपास नहीं काफ़ी दूर होता है और उसका जिन पर असर पड़ता है- वनवासियों पर, मछुआरों पर, बंजारा समुदायों पर, छोटे किसानों, भूमिहीनों पर, वे सब हमारी-आपकी आंखों से ओझल रहते हैं। ऐसी जगहों से भी विरोध की कुछ आवाजें उठ जरूर रही हैं पर उनकी कोशिशें पूरे समाज की धारा के एकदम विपरीत होने के कारणजल्दी दब जाती हैं, दबा दी जाती हैं। ऐसे आन्दोलन अक्सर अपने बचपन में ही असमय मर जाते हैं। फिर भी पर्यावरण के बचाव के लिए उठी इन छोटी-मोटी आवाज़ों ने सरकार के कान खड़े किए हैं।
पर्यावरण की वास्तविक चिन्ता की फुसफुसाहट बढ़े तो उसे नक़ली चिन्ता के एक लाउडस्पीकर से भी दबाया जा सकता है। बेमन से कुछ विभाग, कुछ क़ानून बना दिए गये हैं। उनको लागू करने वाला ढाँचा जन्म से ही अपाहिज रखा जाता है। जल प्रदूषण नियन्त्रण कानून को बने 10 साल हो जाएँगे। पर आज तक उसने नदियों को गिरवी रख रहे उद्योगों को, नगरपालिकाओं को कोई चुनौती भी नहीं दी है। पहले केंद्र में और अब सभी राज्यों में खुल रहे पर्यावरण विभाग भी उन थानों से बेहतर नहीं हो पाएँगे जो अपराध कम करने के लिए खुलते हैं।
पर्यावरण की इस चिन्ता ने पिछले दिनों पर्यावरण शिक्षा का भी नारा दिया है। विश्वविद्यालयों में तो यह शिक्षा शुरू हो गयी है, अब स्कूलों में भी यह लागू होने वाली है। पर इस मामले में शिक्षा और चेतना का फर्क करना होगा। पर्यावरण की चेतना चाहिए, शिक्षा या डिग्री नहीं। चेतना बिगड़ते पर्यावरण के कारणों को ढूँढ़ने और उनसे लड़ने की ओर ले जाएगी, महज शिक्षा विशेषज्ञ तैयार करेगी जो अन्ततः उन्हीं अपाहिज विभागों में नौकरी पा लेंगे। नकली चिन्ता का यह दायरा हजम किए जा रहे पर्यावरण से ध्यान हटाने के लिए ऐसी ही दिखावटी चीजें, हल और योजनाएँ सामने रखता जाएगा।
जब तक पर्यावरण की चेतना नहीं जागती, जब तक विकास के इस देवता पर चढ़ाया जा रहा सिन्दूर नहीं उतारा जाता तब तक पर्यावरण लूटा जाता रहेगा, उस पर टिकी तीन-चौथाई आबादी की जिन्दगी बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन विकास की इस धारा को चुनौती देकर विकल्प खोजना एक बड़ा सवाल है। अन्याय गैरबराबरी से लड़ने की प्रेरणा देने वाली मार्क्सवाद विचाराधाराओं तक में विकास के उसी ढाँचे को अपनाया गया है जो पर्यावरण के क़ायमी उपयोग ढूँढ़े बिना पर्यावरण बिगड़ता ही जाएगा। गरीबी-गैरबराबरी बढ़ेगी, सामाजिक अन्यायों की बाढ़ आएगी। समाज का एक छोटा-सा लेकिन ताकतवर भाग बड़े हिस्से का हक छीन कर पर्यावरण खाता रहेगा, बीच-बीच में दिखाने के लिए कुछ संवर्धन की बात भी करता रहेगा। खाने और दिखाने के इस फर्क को समझे बिना 5 जून के समारोह या पूरे साल भर चलने वाली चिन्ता एक कर्मकाण्ड बनकर रह जाएगी।
* अनुपम मिश्र का यह लेख किशन कालजयी द्वारा सम्पादित तथा पेंग्विन द्वारा प्रकाशित (2006) पुस्तक ‘साफ माथे का समाज’ में संकलित है। लगभग 25 वर्ष पहले लिखा यह लेख आज भी उतना ही प्रासंगिक है।