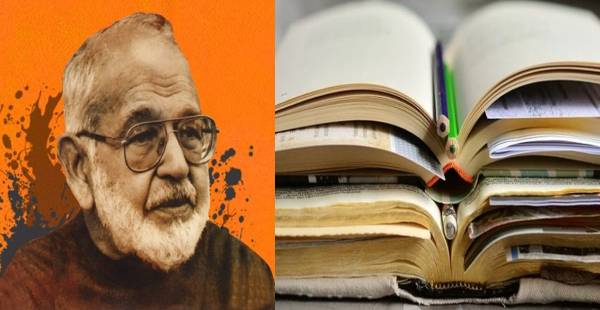
भाषा का नवाचार या भ्रष्टाचार
कभी अज्ञेय ने, ख़ासकर साहित्य के संदर्भ में, शब्दों से उनके छूटते व घिस चुके अर्थों से व्यग्र होकर लिखा था –
“ये उपमान मैले हो गए हैं।
देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच।
कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है।”
(कलगी बाजरे की, अज्ञेय)
शब्द और अर्थ के सहसम्बन्ध व सहअस्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए बहुत पहले तुलसी ने अपनी वंदना में इसकी अभिन्नता को उपमान स्वरूप सीता राम की जोड़ी के लिए प्रस्तुत किया था-
“गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न।
बंदऊँ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न।”
शब्द से अर्थ की अभिन्नता की जो बात तुलसी कह रहे हैं कालांतर में अज्ञेय भी इसी अभिन्नता को स्वीकार करते हुए एक कदम आगे की बात करते हैं। समय के साथ शब्द के मायने वही जादू नहीं पैदा करते; जो एक समय कभी करते रहे होंगे।अज्ञेय की कविता से उद्धृत उपर्युक्त चार पंक्तियों को कई-कई बार अलग संदर्भों में quote किया जाता रहा है।
मैं जिस आशय में अपनी बात कहना चाह रही हूँ, उसमें उनकी कविता की इन चार पंक्तियों के बरअक्स आख़िरी की दो पंक्तियाँ ज़्यादा मानीखेज़ हैं-
“शब्द जादू हैं-
मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है?”
मानव जाति और मानव सभ्यता के विकास में भाषा का अद्भुत व अद्वितीय योगदान रहा है, इस बात की तस्दीक़ युवाल नोआ हरारी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे कई विद्वान / मानव समाज वैज्ञानिक करते रहे हैं। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध ‘नाख़ून क्यों बढ़ते हैं’ में भाषा को मनुष्य की सहजात वृत्ति मानते हुए लिखते हैं, “मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भाँति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गईं हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अंजान में भी, अपने आप काम करती हैं। …असल में सहजात वृत्तियाँ अंजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक् की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले।”

द्विवेदी जी भाषा को उतना ही स्वाभाविक मानते हैं जितना मनुष्य का पलक झपकाना या उसके दाँतों का दो बार उगना। शीन काफ़ निज़ाम शाइर मीराजी के बारे में लिखते हैं , “एक अच्छा शाइर अर्थ से अधिक शब्द का स्वभाव सम्प्रेषित करता है।” (मीराजी : उस पार की शाम)
‘भाषा’ जिसका चरित्र इतना अकृत्रिम और स्वाभाविक हो, जो आदम काल से मानव जीवन में रक्त, हवा और जल की तरह घुली हो, उसकी अपरिहार्यता और उसके जादू को समझना मुश्किल नहीं।
हम आते हैं भाषा के सम्प्रेषण धर्म की ओर। सम्प्रेषणीयता भाषा का धर्म भी है और उसके होने की वज़ह भी। मनुष्य, जो स्वभावत: सामाजिक प्राणी माना जाता है, बिना अपने मन-भाव-विचार को साझा किए सुकून से नहीं रह सकता। मनोचिकित्सक – समाज वैज्ञानिक इस तथ्य की कई बार पुष्टि कर चुके हैं। सम्प्रेषण में भाषा की भूमिका के अलग-अलग आयाम, माध्यम और प्रकार होते हैं। प्रापक प्रेषक द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के इन रूपों से तभी प्रभावित होता है जब वे उसकी रूह से गुज़रते हैं। कह सकते हैं भाषा अपने अर्थ सम्प्रेषण में तब तक बेअसर, अर्थहीन या प्राणहीन होगी; जब तक प्रेषक के शब्द (उच्चरित, मौखिक, लिखित, डिजिटल, सांकेतिक या अन्य किसी भी रूप में) प्रापक को उसी मायने में प्रभावित नहीं करते, जो उस शब्द का रूढ़िवादी अर्थ है।
प्रश्न उठता है कि समय के साथ शब्द के क्या वही मायने रह जाते हैं जो एक समय थे? क्या शब्दों के अर्थ की हत्या में काल का ही सबसे अहम रोल है? क्या भाषा प्रयुक्ति के सभी क्षेत्रों में शब्दों के घिस जाने या अर्थ बदल जाने की घटना घटित होती है/होती होगी?
यदि इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि भाषा मनुष्य द्वारा व्यवहृत होती है। मनुष्य के लिए भाषा साधन भी है और साध्य भी। समाज में जिस गति से मनुष्य के चरित्र और व्यवहार में फ़र्क़ आता गया, जैसे-जैसे उसके जीवन-मूल्य, सिद्धांत बदले, उसकी प्राथमिकताएँ बदलीं, वैसे- वैसे उसका व्यवहार परिवर्तित और फिर इनसे नियंत्रित और चालित होने लगा। मनुष्य की भाषा के प्रयुक्ति क्षेत्र बेहद व्यापक हैं। भाषा के भावों की तब्दीलियाँ बहुत कुछ उन प्रयुक्ति क्षेत्रों में आई तब्दीलियों पर निर्भर करती रही। जिस क्षेत्र का चरित्र जिस गति से बदला, भाषा अपने प्रचलित अर्थ में उतनी ही बेमानी होने लगी। इस संदर्भ में दो क्षेत्र ख़ासकर ग़ौरतलब हैं- एक राजनीति और दूसरा प्रेम सम्बन्ध। मैं यहाँ राजनीति में भाषा के बदलते अर्थ की बात करूँगी।
भारत के संदर्भ में राजनीति में आज़ादी के बाद से ही जिस तरह की चारित्रिक गिरावट देखने में आई उसने हर तरह भरोसे को डस लिया। भाषा ही नहीं, आम आदमी के लिए इस क्षेत्र के लोगों का व्यवहार, परिधान, जीवन-शैली सब कुछ शक के घेरे में आते-आते पूरी तरह भरोसे से बाहर हो गया। गाँधीवाद, गाँधीगीरी, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्रांति, आज़ादी, देशप्रेम, नैतिकता, संविधान, संसद, कर्तव्य, निष्ठा, न्याय, लोकतंत्र, क़ानून समानता, समान अधिकार, आरक्षण और बहुसंख्यक हित, लोकपाल बिल। नारों के ताज़े-तरीन उदाहरण- ‘अच्छे दिन आएँगे’, ‘ हिंदू ख़तरे में है’, ‘हर -हर मोदी, घर -घर मोदी’, ‘सबका साथ, सबका विकास’, ‘पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया’, ‘स्किल इंडिया शाइन इंडिया’, ‘काला धन आएगा’..अन्य प्रयुक्तियाँ जैसे, विश्वगुरु भारत, पकौड़ा राजनीति, जुमला सरकार , बेंचू सरकार, फेंकू सरकार, गोदी मीडिया, धर्म संसद, आदि-आदि।
नई तकनीक के चलते अत्यंत गम्भीर मुद्दों और विषयों पर भी तुरंत तैयार हो जाते नए मीम्स, रील्स, चुटकले, राइमिंग; मुद्दे की गम्भीरता को तो डायल्यूट कर ही रहे हैं, भाषा के अर्थ गांभीर्य को भी खोते जा रहे हैं। ‘जुमले’ या ‘जुमलेबाज सरकार’ का प्रयोग जिस तादाद में होकर जिस तरह हँसी-मज़ाक और हल्के में लिया जाने लगा है, यह असल में सरकार की संविधान और देश के प्रति उस जबावदेही को हल्का करना है, जिस के लिए उसे सत्ताच्युत हो जाना चाहिए।

उल्टे भाषा का ‘डीमीनिंग’ होना, ख़ासकर पिछले दशक से जोरों से जारी है, जैसे – जय श्री राम, राष्ट्रवाद, देशद्रोह, देशप्रेम, आंदोलन, आंदोलनजीवी/परजीवी, टुकड़े-टुकड़े गैंग, अभिव्यक्ति की आज़ादी, योगा, अग्निवीर/क्रांतिवीर/राजनीतिवीर आदि-आदि। सत्ता, विपक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा लगभग रोज़ एक नया नारा, शब्दों का पिटारा ; लोगों के सामने फेंक दिया जाता है। लोग जब तक उन शब्दों को सुनकर उनके अर्थों तक पहुँचते हैं, तब तक एक नया शब्द/ नारा लगभग चुनौती लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। ये सारा माज़रा किसी चूहे-बिल्ली के खेल-सा लगता है। इनमें से कई बार कई शब्द आतंक पैदा करते हैं और कई बार वे अर्थहीन होकर हास्यास्पद होकर क़तई बेअसर हो जाते हैं।
सच तो ये है कि राजनीति में भाषा की विकृति, राजनीति की विकृति का परिणाम है। भाषा के प्रति, असम्वेदनशीलता व्यवहार में मनुष्य की असम्वेदनशीलता का प्रमाण है। यह स्थिति जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, हम एक क्रूर, निरंकुश, ग़ैर-भरोसेमंद सत्ता और समाज के अधीन होते जाएँगे। प्रो. अपूर्वानंद 30 जून 2022 के अपने एक ट्वीट में लिखते हैं, “ बेहतर हो कि इस वक़्त की भयावहता को समझें, क़बूल करें कि हमारी भाषा इसका वर्णन करने में अभी असमर्थ है। सस्ती, हल्की तुकबंदी, चुटकलेबाज़ी इस मुश्किल का सामना करने से हमें बचा ले जाती है। भाषा का सतहीकरण फ़ासीवाद का रास्ता और आसान करता है।”











