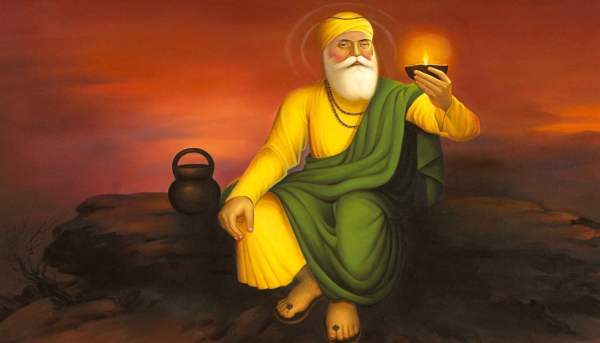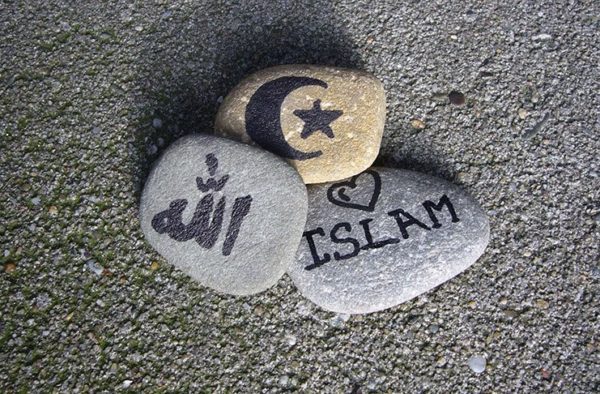
क्या इस्लाम मूर्तिभंजक है?
अरब में सातवीं सदी में एक साधारण से मकान के दरवाजे पर एक स्त्री ने परदा टांग दिया। परदे पर पशु-पक्षियों याने जीवित प्राणियों की आकृतियाँ काढी हुई थीं। जब उसका पति घर लौटा तो परदा देख कर उसे खुशी नहीं हुई और उसने परदा हटा दिया। लेकिन परदा बेकार नहीं हुआ। उस स्त्री ने परदे को काट कर तकिया और तोशक के गिलाफ इस प्रकार बना लिए कि उन पर काढ़ी हुई आकृतियाँ साफ़ दिखाई पड़ें। आखिर उन चित्रों से ही तो शोभा थी।
वह कोई साधारण मकान नहीं था और वे पति-पत्नी भी साधारण दम्पति नहीं थे। पति इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद थे और स्त्री उनकी पत्नी आयशा जिसने यह वाकया बाद में अपनी सहेलियों को बताया और उसके बाद पिछ्ले करीब 1500 वर्ष से यह कहानी परम्परागत रूप से चली आ रही है। देखने में सामान्य-सी इस घरेलू घटना ने दुनिया के एक बड़े धर्म की परम्परा में ‘जीवित प्राणियों की प्रतिच्छवि के प्रश्न पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है।
लेकिन इससे एक बहुत बड़ी अनिश्चितता का भी पता चलता है। वास्तव में हजरत मोहम्मद को आपत्ति परदे पर कढ़ाई की गयी आकृतियों पर नहीं थी, वरन उन आकृतियों को इस प्रकार महत्व दिए जाने पर थी, क्योंकि तब नमाज पढने के वक्त मुहम्मद का ध्यान उन आकृतियों पर पड़ने की संभावना थी और इस प्रकार नमाज में विघ्न पड़ सकता था। पर लिहाफ और तोशक के गिलाफ के रूप में वे आकृतियाँ ठीक थीं।
यही वह अनिश्चिति है जिसके कारण अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध की विशाल मूर्ति ढहा दी गयी,डेनमार्क में कार्टून को लेकर और फिल्मों में मुहम्मद के प्रस्तुतीकरण पर बवाल मचा तथा पिछले दिनों पेरिस की एक व्यंग्य पत्रिका में छापे गए मुहम्मद के कार्टून को लेकर भीषण नरसंहार। यानी कला और धर्म के जटिल सम्बन्ध के प्रश्न पर दुनिया भर के मुसलमानों में बिना सोचे-समझे आक्रोश !
इस अनिश्चितता को दूर करने का कुछ हद तक प्रयत्न किया है हार्वर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस से कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित जमाल जे। एलियास की पुस्तक ‘आयशा’स कुशंस : रिलीजियस आर्ट, परसेप्शन एंड प्रेक्टिस इन इस्लाम’ [1] ने। पुस्तक वस्तुतः इसी प्रश्न से शुरू होती है। ‘इस्लाम में जीवित प्राणियों के चित्रण पर’ लेखक ने जिस ढंग से विचार किया है वह पूरी तरह संतोषजनक भले ही न हो, पर मैं समझता हूँ कि इस विषय में रूचि रखने वालो और आए दिन मुहम्मद के चित्रों के नाम पर बवाल मचाने वालों के लिए यह एक अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण पठनीय पुस्तक है।
पुस्तक वस्तुतः इसी प्रश्न से शुरू होती है। ‘इस्लाम में जीवित प्राणियों के चित्रण पर’ लेखक ने जिस ढंग से विचार किया है वह पूरी तरह संतोषजनक भले ही न हो, पर मैं समझता हूँ कि इस विषय में रूचि रखने वालो और आए दिन मुहम्मद के चित्रों के नाम पर बवाल मचाने वालों के लिए यह एक अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण पठनीय पुस्तक है।
जिन लोगों को इस्लाम और मुस्लिम संस्कृति के विषय में थोड़ी बहुत चलताऊ जानकारी है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम में कला, विशेषकर छवि-अंकन, का प्रश्न किस तरह विवादास्पद है। इस्लाम में एक ओर तो जीवित प्राणियों विशेषकर मुहम्मद के छायांकन को लेकर बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक संकल्पनाएँ हैं और दूसरी ओर दमिश्क की उमय्यद मस्जिद के बाहरी भाग में मोजाक में सभी प्रकार के पेड़-पौधों, वनस्पतियों (ये भी एक प्रकार से जीवित प्राणी ही हैं) का चित्रण है। शियाओं में तो पैगम्बर मुहम्मद के परिवार जनों के
धर्मनिष्ठात्मक चित्र तो आम बात है और ईरान में तेहरान के बाजारों में मोहम्मद के चित्र वाले पेन्डेन्ट (गले में लटका कर पहिनने वाले लाकिट) खुले आम बिकते हैं। (इस लेख का लेखक दमिश्क और तेहरान जा चुका है)। वहाँ बिकने वाले कालीनों पर और पेंटिंग्स में भी जानवरों का अंकन और मानवीय क्रियाएं उकेरी जाती हैं। पुरानी पांडुलिपियों में भी इस प्रकार का चित्रांकन मिल जाता है। तो सही बात क्या है? इस्लाम में इस प्रकार की छवियों की मान्यता है या नहीं? यह कैसी विडम्बना है कि एक ओर तो ईरान जैसे मुस्लिम देशों के बाजारों में लोग मुहम्मद के चित्र वाले पेन्डेन्ट बेच कर अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ करते हैं (कर रहे हैं) और दूसरी ओर डेनमार्क और फ्रांस में इसी बात को लेकर कत्ले-आम हो रहा है !
मेरी समझ में तो यही आता है कि इस प्रश्न पर यानी किसी की आकृति के चित्रण के पीछे कलाकार की क्या मंशा है या रही है – यही मुख्य बात है और होनी चाहिए। यह धार्मिक भावनाओं को उभाड़ने की बात वैसी नहीं है जितनी जान-बूझ कर किसी का अपमान करने की बात और जिस बात को लेकर मुसलमान सडकों पर उतर आते हैं।
इस पुस्तक के लेखक का मत है कि यह एक प्रकार से ईसाई मत और इस्लाम की भी आपसी प्रतिद्वंद्विता है। ईसाई संस्कृतियों में छवि अंकन की भरमार है और वे इस्लाम की ओर- जिसमें छवि अंकन का पूरी तरह निषेध कहा जाता है – कुछ किंकर्तव्यविमूढता से देखते हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय बात है कि मुहम्मद के आगमन के पहले अरब जगत में और अन्य देशों में भी मुसलमानों में पत्थर की मूर्तियाँ और इसी प्रकार की अन्य त्रिआयामी आकृतियों की पूजा की प्रथा आम बात थी।
इनमें भी भारत प्रमुख था। अल-बरूनी और अल-काजवीनी जैसे पर्यटकों ने मुलतान और सोमनाथ के मंदिरों की मूर्तियों की कलात्मक विशेषताओं के सम्बन्ध में बहुत ही प्रशंसात्मक ढंग से लिखा है। लेखक का अन्ततः निष्कर्ष यही है और यह गलत नहीं है कि इस्लाम सीधे-सीधे मूर्तिभंजक नहीं है और यह इसबात पर निर्भर है कि कृति या मूर्ति बनाने में कृतिकार या मूर्तिकार की मंशा क्या थी या रही।
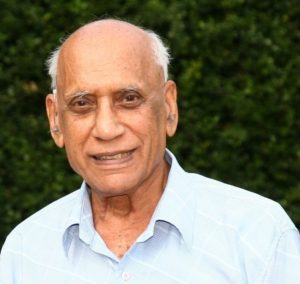
महेंद्र राजा जैन
[1] Aisha’s Cushion : Religious Art, Perception and Practice in Islam / Jamal J. Elias. Harvard University Press