
हरिशंकर परसाई: व्यंग्य-दृष्टि और वर्ग-बोध
हिंदी-व्यंग्य के शीर्ष-पुरुष हरिशंकर परसाई के जन्म-शताब्दी-वर्ष में जिज्ञासा होती है कि उनकी कहानियों में व्यंग्य की चेतना प्रारंभ से थी, या वह धीरे-धीरे समय के साथ विकसित हुई। परसाई जबलपुर आने के बाद समाजवादियों के संपर्क में आए। लेकिन उसके पूर्व 1946-47 में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली रचना ‘दूसरों की चमक-दमक’ (बाद में उनकी रचनावली में ‘पैसों का खेल’ शीर्षक से संकलित) 23 नवंबर, 1947 को ‘प्रहरी’ में ‘उदार’ उपनाम से छपी एक कहानी थी जिसमें उन्होंने जबलपुर में घटित एक अनुभव को ‘कल्पनाशीलता और भाषा की सामर्थ्य के साथ’ ज्यों-का-त्यों लिखा था।
‘दूसरों की चमक-दमक’ की घटनात्मक वास्तविकता को उन्होंने सादगी के साथ बयान किया था। प्रकट यथार्थ को दो विरोधी प्रत्ययों के द्वंद्व में, उनके अंतर्विरोधों के साथ, देखने की यह लेखकीय दृष्टि उनकी सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय पक्षधरता से प्रेरित थी। उनकी इस पहली रचना में व्यंग्य नहीं था जिसके लिए वह जाने गए, बल्कि छलछलाती हुई करुणा थी।
लेकिन उन्हीं दिनों एक और कहानी ‘स्वर्ग से नरक जहाँ तक’ मई, 1948 में ‘प्रहरी’ में ही प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसमें व्यंग्य के माध्यम से समाज की आंतरिक विसंगतियों की पहचान का संकेत है। करुणा और व्यंग्य उनकी रचनाओं में परस्पर संगति में विकसित हुए हैं, और एक-दूसरे में गुँथे हैं। लेकिन उनकी आरंभिक कहानियाँ कथ्य और संरचना की दृष्टि से पुष्ट-परिपक्व नहीं हैं। उनमें नए लेखक का स्वाभाविक कच्चापन है। फिर भी उनमें व्यंग्य के संकेत मिलते हैं।
प्रारम्भ में उन्होंने अपने निजी दुखों को लिखा मगर जल्द ही इस आत्ममोह से बाहर आ गए। समाज में व्याप्त अंतर्विरोध समझने की दृष्टि अर्जित की। मूल्यों की लगातार गिरावट, भ्रष्टाचार, पाखंड, दोमुँहापन, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई अनैतिकता—इन सबका असर उन पर पड़ा। बाद में मार्क्सवाद ने उन्हें तार्किक ढंग से जीवन को समझने की दृष्टि दी।

परसाई के रचनात्मक मानस में व्यंग्य और विसंगति का बोध भी अंतर्भूत था। 1952 में कम्युनिस्टों के निकट आने पर मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। उनमें सामाजिक अंतर्विरोधों की समझ और उसके अनुरूप रचना-दृष्टि विकसित हुई। महेंद्र वाजपेयी ने उन्हें मार्क्सवादी साहित्य से परिचित कराया। फिर 1954 में मुक्तिबोध के संपर्क में आए तो उनके व्यक्तित्व और वैचारिकता की तेज़ आँच से सामना हुआ। वह वामपंथी और जन-प्रतिबद्ध राजनीति के अधिक क़रीब आये। उनकी समाज-दृष्टि और साहित्य-दृष्टि में बदलाव हुआ। इसी मोड़ पर उनमें नव स्वतंत्र राष्ट्र के भीतर उपजी विसंगतियों को पहचान सकने की दृष्टि विकसित हुई।
लेकिन मुक्तिबोध और परसाई हिन्दी में आसानी से स्वीकार नहीं किये जा सके और लंबे समय तक उन्हें समुचित मान्यता नहीं मिली। इसके बावजूद परसाई अख़बारों में साहित्य लिखने का जोखिम उठा कर धीरे-धीरे लोकप्रियता अर्जित कर रहे थे। ‘प्रहरी’ में वह ‘नर्मदा के तट से’ शीर्षक से स्तम्भ लिख रहे थे। इसमें मिली-जुली गद्य रचनाएँ होती थीं जो अख़बार के पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थीं। सेठ गोविंददास और द्वारिका प्रसाद मिश्र की राजनीति पर व्यंग्य लिखते-लिखते उन्होंने व्यक्तिगत कटाक्ष के बजाए अब अपनी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्य करने का रास्ता अपनाया लिया था। उस दौर में उन्होंने निबंध कम, कहानियाँ ज़्यादा लिखी।
परसाई की कहानियों का पहला संग्रह ‘हँसते हैं रोते हैं’ मुक्तिबोध से सम्पर्क होने के पहले 1951 में प्रकाशित हो चुका था। इसे स्वयं प्रकाशित कर वह बेचते थे। ‘हँसते हैं रोते हैं’ की कहानियों में अपने आसपास के जीवन से जुड़ने की कोशिश और निम्नमध्यवर्गीय जीवन के अभावों, वंचनाओं और विडंबनाओं को चित्रित करने की स्पृहा दिखाई देती है—यद्यपि कुछ कहानियों को छोड़ दें तो प्रायः उनमें निर्दोष भावुकता और छायावादी भावबोध का प्रभाव ज़्यादा है। वे परिवेश के अनुभवों और घटनाओं से प्रभावित रचनाएँ हैं, किसी सुचिंतित रचना-दृष्टि और समाज-बोध से प्रेरित नहीं। सामाजिक विडम्बनाएँ उनमें रूमानी आवरण में लिपटकर आती हैं। उनमें तीक्ष्णता, विद्रूप के उद्घाटन की मर्मज्ञता झलकती अवश्य है, लेकिन सामाजिक विरूपताओं को लेकर पुष्ट तार्किक दृष्टि की वैसी प्रखरता नहीं है जो आगे चलकर परसाई की विशिष्ट पहचान बनी। ‘हँसते हैं रोते हैं’ की कहानियाँ प्रायः भावात्मक वृत्त में हैं। लेकिन उनमें ‘भीतर का घाव’ जैसी अपेक्षाकृत बेहतर कहानी भी है जो मनुष्य के त्रासद जीवन और उसकी वेदना को उकेरती हैं और समाज के भीतर व्याप्त नैतिक-सामाजिक धारणाओं के खोखलेपन को उद्घाटित करती हैं।
‘भीतर का घाव’ दहेज के लालच में एक युवा स्त्री की इरादतन हत्या की मार्मिक कथा है। इसमें भावाकुलता का उद्रेक है जो उद्वेलित करता है और करुणा जगाता है। इस कहानी में करुणा का प्रबल वेग है लेकिन उसकी परिणति में व्यंग्य नहीं है। शुरुआत के दो अनुच्छेदों में विरूपण (कैरिकेचर) के ज़रिए विसंगति-बोध उत्पन्न करने की कोशिश की गई है लेकिन वह कहानी के मूलतः भावात्मक स्वर के साथ पूरी तरह जुड़ नहीं पाता—बल्कि नैरेटर के प्रति किंचित दया-भाव ज़रूर जगाता है।
‘हँसते है रोते हैं’ की कहानियों में प्रबल भावात्मकता और करुणा के बावजूद यथार्थवादी दृष्टि और व्यंग्य-बोध मौजूद है। ‘भीतर का घाव’ कहानी की मार्मिक परिणति उसे गहन काव्यात्मक संवेदना के क़रीब ले जाती है। कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जो ऊपर से शिक्षाप्रद या किसी नैतिक एजेंडा से बँधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी संवेदना व्यापक मानवीय धरातल को स्पर्श करती है। उदाहरण के लिए ‘भीतर का घाव’ दहेज़-प्रथा की अमानवीयता पर लिखी गई रचना नहीं है। ‘पड़ोसी के बच्चे’ परिवार-नियोजन और जनसँख्या-विस्फोट को संदर्भ बनाती है लेकिन उस विषय पर केंद्रित नहीं है। मानवीय धरातल पर आकर यह कहानी समानता के अधिकार का पक्ष लेती है। ‘क्रान्ति हो गयी’ क्रान्ति के नारे का उपहास नहीं करती, बल्कि क्रान्ति के रूमानी विचार की अवैज्ञानिकता को प्रश्नांकित करती है। उसमें उठाये गए प्रश्न बाद में सत्तर के दशक में जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति के विचार के संदर्भ में नए सिरे से प्रासंगिक सिद्ध हुए। ऐतिहासिक और कालगत संदर्भ बदल जाने के बावजूद यह कहानी अपनी अर्थवत्ता नहीं खोती।
‘क्या कहा’ और ‘साड़ी का रंग’ प्रेम पर एकाग्र हैं, लेकिन ये प्रेम कहानियाँ नहीं हैं। ये कहानियाँ प्रेम के मिथ्याडंबर को उद्घाटित करती हैं। ये प्रेम की किशोर धारणा और प्लेटॉनिक आदर्श के ढहने और उसकी वास्तविकता के उजागर होने की कहानियाँ हैं। ‘नरक से बोल रहा हूँ’ और ‘भूख के स्वर’ सामाजिक विषमता, झूठ की स्वीकार्यता और मनुष्य के निर्मम उत्पीड़न की सचाई को उद्घाटित करती हैं। उनका बुनियादी स्वर व्यंग्य का है। ये कहानियाँ प्रतिवाद की चेतना को रेखांकित करती है।

उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में ‘सेवा का शौक’ कहानी भी है। यह ‘हँसते हैं रोते हैं’ में संकलित नहीं है; बाद में मई, 1953 में प्रकाशित हुई थी। यह भी अपेक्षाकृत बेहतर कहानी है। इसमें लेखक का ‘अपना ही दुःख’ और ‘आत्ममोह’ नहीं है। यह दूसरे के दुःख की, यानी सामजिक करुणा की कहानी है, जिसमें भावुकता और व्यंग्य का मेल है। यह व्यंग्यपूर्ण हल्के वाक्यों के साथ शुरू होकर बीच-बीच में कुछ चुटीले वाक्यों में आगे बढ़ती है। यह विधवा माँ और विवाह-योग्य बड़ी बहन के परिवार का बोझ कंधे पर लिए 16-17 वर्ष के बालक रामनाथ की कहानी है जिसे समाजसेवा के शौक़ में पंडित मातादीन अपने गाँव के स्कूल में शिक्षक नियुक्त करते हैं। लेकिन दामाद की सनक के चलते उसे निकाल देते हैं। उसकी कथा के सिचुएशन में ही करुणा है।
संयोगवश ‘हँसते हैं रोते हैं’ पर द्विवेदीयुगीन साहित्यकार और ‘सरस्वती’ के सम्पादक पदुमलाल पुन्नालाल बख़्शी ने एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखी। इससे परसाई का मनोबल बढ़ा। इसी बीच रेखाचित्रों और कहानियों का उनका दूसरा संग्रह ‘तब की बात और थी’ जून 1956 में प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध ने परसाई की रचनाओं की ओर हिंदी-जगत का ध्यान आकृष्ट करते हुए ‘नया ख़ून’ के दीपावली विशेषांक में एक लेख लिखा—‘मध्यप्रदेश के जाज्वल्यमान कथाकार हरिशंकर परसाई’।
परसाई की रचनाशीलता पर यह पहली गंभीर समीक्षात्मक टिप्पणी थी। मुक्तिबोध ने इसमें परसाई की कहानियों के दो गुणों की चर्चा की थी—खरापन और खुरदुरापन। उन्होंने लिखा—‘खरेपन में खुरदुरापन है जो मौजूदा यथार्थ का गुण है, किसी आत्मग्रस्त सब्जेक्टिव वृत्ति का लक्षण नहीं।’[1] आत्मग्रस्त सब्जेक्टिव वृत्ति से मुक्तिबोध का तात्पर्य उन दिनों नई कविता और नई कहानी के नाम पर प्रचलित ख़ास साहित्यिक प्रवृत्ति से है जो पश्चिम के विश्वयुद्धोत्तर चिंतन और शीतयुद्ध की विचार-दृष्टि से प्रेरित होकर ‘अनुभव की प्रामाणिकता’, ‘क्षणवाद’ और ‘लघुमानव’-जैसी अवधारणाओं के रूप में चलाई जा रही थी।
परसाई नए लेखक थे लेकिन मुक्तिबोध की राय थी कि उन दिनों पश्चिम में प्रशंसित अनेक भारतीय लेखकों की तुलना में ‘परसाई कलात्मक दृष्टि से प्रगतिशीलता के क्षेत्र में, उनसे कहीं अधिक समर्थ हैं।’ उन्होंने परसाई की रचनात्मक संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए उन्हें एक ऐसे बीज की तरह निरूपित किया जिसमें ‘सघनच्छाय भव्य वृक्ष’ होने की पूरी संभावना है। मुक्तिबोध ने लिखा कि ‘तब की बात और थी’ के पाठकों को परसाई की क्षमता का पता लग जायेगा। उन्होंने ‘एक घण्टे का साथ’ को ‘सर्वश्रेष्ठ कहानी’ बताया और उसे हिन्दी की उच्च्च कोटि की कहानियों में परिगणित किया। इसके अलावा अपनी समीक्षा में मुक्तिबोध ने ‘स्मारक’ और ‘भेड़िये और भेड़ें’ कहानी का ज़िक्र किया।
‘एक घण्टे का साथ’ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो प्रतिभावान और गुणी होने के बावजूद उपेक्षित और कुंठित है। उसका अवगुण है, बेरोज़गारी। उसकी हताशा उसकी बातों और व्यवहार में झलकती है। यह उस दौर की कहानी है जब परसाई व्यंग्यकार के रूप में नहीं जाने गये थे। लेकिन इस कहानी में भी व्यंग्य की सूक्ष्म अंतर्धारा प्रवाहित होती हुई कहानी की कलात्मकता और सौंदर्य-मूल्य का विस्तार करती है। इस कहानी की कलात्मक गुणवत्ता के कारण ही मुक्तिबोध ने प्रशंसा की है। इसमें मार्क्सवाद के वैचारिक प्रभाव का साक्ष्य वाचक द्वारा वर्गभेद और वर्गचेतना-जैसे शब्दों के प्रयोग में मिलता है। स्वयं पात्र द्वारा प्रयुक्त शब्दों, ‘आप लोग’ और ‘हम लोग’ के द्वैत में यह स्पष्ट है।
विद्रूप के उद्घाटन की क्षमता के कारण ‘स्मारक’ कहानी का उल्लेख भी मुक्तिबोध ने किया है; हालाँकि उनकी दृष्टि में यह साधारण कहानी है। लेकिन वह साधारण इसलिए रह गई है कि ‘बड़ी-से-बड़ी बात उड़ते-उड़ते कहने की सहज-सुलभ बहिर्मुखी वृत्ति के कारण, वह कहानी अपनी पूरी ऊँचाई पर पहुँच नहीं सकी।’ फिर भी इस कहानी ने मुक्तिबोध का ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा—‘उसमें जो कुछ भी है वह परफ़ैक्ट है। किन्तु वह परफ़ैक्टपन हमेशा ऊँचाई नहीं होती, यद्यपि हो सकती है।’[2] लेकिन हो न पाई क्योंकि कहानी में ‘चरित्र की आन्तरिकता’ के प्रति परसाई पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। ज़ाहिर है, कहानी सपाट और सरलीकृत मालूम पड़ती है।
आगे मुक्तिबोध हिंदी की तत्कालीन साहित्यिक संस्कृति में ‘सचाई के प्रकटीकरण पर हदबन्दी’ का ज़िक्र करते हुए उसकी पृष्ठभूमि में, और उसके बरअक्स परसाई की कला के ‘सहज ही वामपक्षी’ हो जाने को रेखांकित करते हैं। अपने लेख के अंत में मुक्तिबोध ने तीन महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो यह कि परसाई भौंडे ढंग से प्रगतिशील या नारेबाज़ नहीं हैं। दूसरा यह कि ‘असलियत को छुपाने के लिए उसे बिगाड़ देने की कला उनके पास नहीं है।’ तीसरी बात यह कि ‘उनकी कला यथार्थ को प्रकट करने के लिए अनेक मार्गों, यहाँ तक कि दंतकथाओं का प्रयोग करती है।’
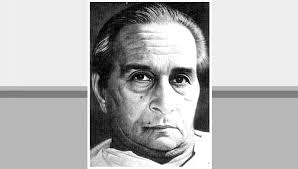
पहली दो बातें परसाई की रचनाओं को विषयवस्तु के गुणों को प्रकट करती हैं। तीसरी का सम्बन्ध उनके शिल्पगत उद्यम और कलात्मक वैशिष्ट्य से है। ‘यथार्थ को प्रकट करने के लिए अनेक मार्गों’ में जाने की कला आगे चलकर उनके कृतित्व में और अधिक निखार पाती है। ये अनेक मार्ग कहानी के आख्यान को प्रस्तुत करने की विविध रीतियाँ या शिल्प-युक्तियाँ हैं। इनमें रूपक कथा या फ़ेबल, पुराण कथा, फ़ैंटेसी, लोककथा, विडम्बना , प्रतीक कथा आदि सम्मिलित हैं। प्रारम्भिक कहानियों में आख्यान का घटनात्मक विस्तार सीमित है। नई कहानी के अपने समकालीनों की तरह परसाई ने यहाँ चरित्रों की मनःस्थिति के सघन विवरण नहीं दिए हैं, न ही आख्यान की एकरैखिक सरल गति में विक्षेप उत्पन्न किया। भाषा और प्रविधि के चामत्कारिक प्रयोग इन कहानियों में नहीं हैं, लेकिन शिल्प और आख्यान-प्रविधि की दृष्टि से किये गए उनके प्रयोग अनूठे-अद्वितीय हैं। अंतर्वस्तु में कुछेक भावात्मक प्रभाव वाली कहानियों (‘तब की बात और थी’, ‘स्मारक’ आदि) को छोड़ दें तो उनकी इन प्रारम्भिक कहानियों का कथ्य कोरमकोर समकालीन, कालगति के अनुरूप और निस्संदेह प्रासंगिक है। परसाई मध्यवर्गीय नागरिक जीवन की सतही, सीमित और प्रायः कृत्रिम समस्याओं पर एकाग्र होने के बजाए समकाल से सीधे जुड़ते हैं, और उसके अंतर्विरोधों को उजागर करते है।
‘तब की बात और थी’ संग्रह की कहानियों में वयंग्य है, परसाई का व्यंग्यकार बहुत मुखर नहीं है। वह मुँह खोलने की कोशिश में है। फिर भी जहाँ वह है उसकी प्रखरता ध्यान खींचती है। अधिकतर कहानियाँ, कुछ अपवादों के बावजूद, यथार्थ की गति को प्रेमचंदीय शिल्प में पकड़ती हैं। ‘बाबू की बदली’-जैसी कहानी में भावात्मकता अत्यंत प्रबल है लेकिन वह तंत्र के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करने के साथ ही मनुष्य की लालसा और उसकी क्षुद्रता के विरुद्ध उसकी भद्रता और नैतिक संवेदनशीलता को खड़ा कर देती है। यही काम व्यंग्य भी करता है। इस कहानी में अफ़सर द्वारा बाबू की स्त्री के दैहिक शोषण को स्त्री की निरीह सामाजिक स्थिति की विडम्बना के रूप में प्रस्तुत कर, परसाई करुणा और निरीहता को ही प्रतिवाद का उपकरण बनाते हैं।
‘भेड़ें और भेड़िया’ कहानी में फ़ेबल की कथा-प्रविधि का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की रीति-नीति पर तीव्र कटाक्ष किया गया है। इसमें जंगल में लोकतन्त्र की स्थापना का वृत्तान्त है। भेड़ें और भेड़िया के रूपक में व्यक्त ‘निर्बल और शक्तिशाली का द्वैत’ या ‘लोक और तंत्र का द्वैत’ वस्तुतः लोकतन्त्र के चारित्रिक गठन में इस तरह से विन्यस्त है कि आज यह उसका स्वाभाविक गुणधर्म जान पड़ता है। उस दौर में परसाई मानो भारतीय लोकतंत्र की नियति को देख पा रहे थे। परसाई अकेले कथाकार थे जिन्होंने लोकतंत्र और स्वाधीनता के भीतर के अंतर्विरोधों को प्रखर राजनीतिक बोध और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ उजागर किया।
इसी दौर में परसाई के रचना-संसार के भीतर वर्गबोध का दाख़िला हुआ। दिलचस्प है कि वर्गबोध, प्रखर राजनीतिक चेतना की संगति में और व्यंग्य के मुहावरे में व्यक्त हो रहा था। ‘मोटर और प्यार’ कहानी को इसके साक्ष्य के तौर पर देखा जा सकता है। हरी कार और पीली कार की प्रतीकवत्ता में यह कहानी एक सम्पन्न प्रेमी युगल और एक मेहनतकश प्रेमी युगल के प्रेम का द्वंद्व रचती है, और उसे वर्गबोध के साँचे में ढाल देती है। ज़ाहिर है, यह मार्क्सवादी परसाई की रचना है। ‘मोटर और प्यार’ कहानी-कला की दृष्टि से पुष्ट रचना नहीं है, लेकिन यह इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि यह परसाई की कथा-भूमि में वर्ग-बोध के उर्वरक के साथ व्यंग्य के बीज-वपन का साक्ष्य प्रस्तुत करती है।
[1] मुक्तिबोध रचनावली, खंड-5, पृष्ठ 427
[2] मुक्तिबोध रचनावली, खंड-5, पृष्ठ 428






