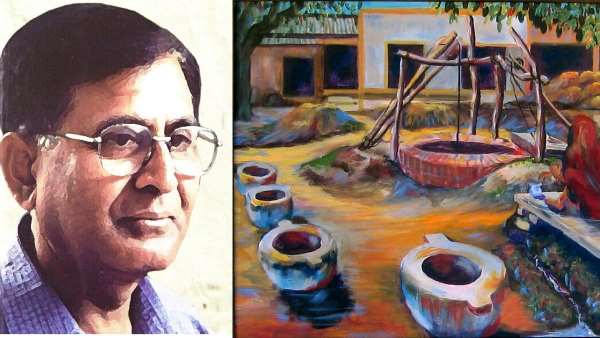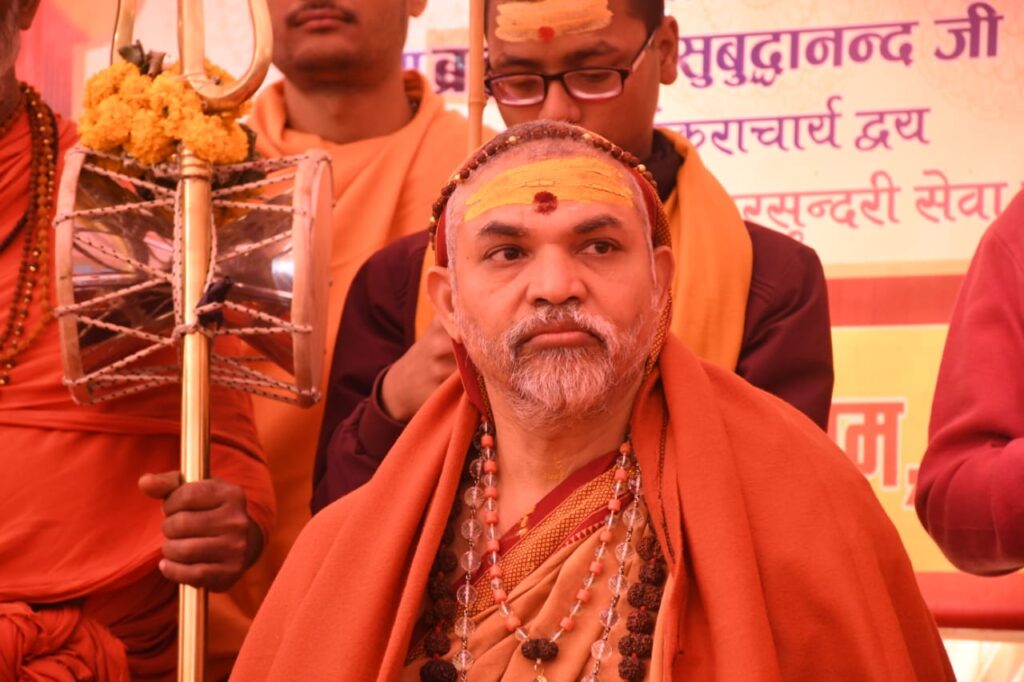पेसा कानून : कितना मानेंगी सरकारी मोहकमे
संसद में अपने पारित होने के करीब 26 साल बाद मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटैल ने ‘पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम – 1996’ यानि ‘पेसा’ को लागू करने के लिए संबंधित विभागों की सहमति मांगी है। जैसा आमतौर पर होता है, सरकारी विभागों ने इस कानून पर भी अपनी-अपनी कच्ची-पक्की राय दी है, लेकिन राज्यभर में फैली करीब 23 प्रतिशत आदिवासी आबादी पर इसका क्या असर होगा? प्रस्तुत है, इसकी पड़ताल करता राज कुमार सिन्हा का यह लेख। –संपादक
हाल में एक समाचार पत्र में मध्यप्रदेश के राज्यपाल के ‘जनजातीय सेल’ द्वारा ‘पेसा’ कानून के मसौदे को विभिन्न विभागों को भेजकर उनकी सहमति प्राप्त करने की खबर छपी है। केवल वन विभाग ने इस पर कोई स्पष्टता नहीं की और उसी दिन के अखबार में वनमंत्री विजय शाह द्वारा अपने गृह जिले खंडवा में तेंदू पत्ता के संग्रहण एवं व्यापार का अधिकार ग्रामसभाओं को देने से इंकार करने की खबर भी छपी है। तो क्या ‘पेसा कानून’ लघु-वनोपजों पर आदिवासियों के अधिकार की अनदेखी करता है?
लघुवनोपज आदिवासी क्षेत्रों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है जिसको लेकर संविधान संशोधन के उपरांत प्रावधान किए गए हैं। वन क्षेत्रों पर ‘पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम – 1996’ (पेसा) के अन्तर्गत लघु-वनोपज का स्वामित्व ग्रामसभा को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ‘वन अधिकार कानून – 2006’ में ग्रामसभा को वन-प्रबंधन का अधिकार देने का उल्लेख किया गया है।
संविधान में मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के वन प्रबंधन में ग्रामसभा का अधिकार सुनिचित करने ‘भारतीय वन कानून – 1927’ में आवश्यक संशोधन हेतू केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया गया है। वन विभाग द्वारा वन प्रबंधन ‘भारतीय वन कानून – 1927’ के अनुसार किया जाता है जो कि वन को केवल राजस्व प्राप्ति का साधन मानता है।

‘पेसा कानून’ के मसौदे में भूमि अधिग्रहण के पूर्व ‘परामर्श’ का उल्लेख किया गया है, जबकि ‘परामर्श’ की जगह ‘सहमति’ और उनके द्वारा पारित प्रस्ताव को बंधनकारी बनाया जाना चाहिए, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में ज़बरन विस्थापन रोका जा सके। आदिवासी क्षेत्रों में फर्जी ग्रामसभा अथवा प्रशासन तंत्र द्वारा दबाव डालकर या प्रलोभन देकर परियोजना के पक्ष में सहमति लेने की अनैतिक कार्यवाहियां सुर्खियां बटोर चुकी हैं।
गांव में शांति बहाली और विवाद निपटाने का अधिकार ग्रामसभा का होगा, परन्तु ‘ग्राम न्यायालय कानून’ के द्वारा विवाद निपटाने के अधिकारों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। ‘पेसा कानून’ के मसौदे में कहा गया है कि यदि कपट पूर्वक जमीन पर कब्जा किया गया है तो उसे दिलाने का अधिकार ग्रामसभा का होगा। यह अधिकार ‘पेसा कानून’ आने के बाद ‘मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता – 1959’ में संशोधन कर दे दिया गया है।
संशोधन के अनुसार यदि ग्रामसभा अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जनजाति के किसी सदस्य की भूमि पर कोई गैर-जनजाति का व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो ग्रामसभा ऐसी भूमि का कब्जा दिलाएगी। यदि ग्रामसभा ऐसी भूमि का कब्जा दिलाने में असफल रहती है तो वह मामला उपखंड अधिकारी (एसडीएम) की ओर निर्देशित कर भेजेगी जो तीन महिने के अंदर पीडित व्यक्ति को जमीन का कब्जा दिलाएगा।
शराब की नई दुकान खोलनी है या पुरानी दुकान का स्थल परिवर्तन किया जाता है तो मंजूरी ग्रामसभा देगी। यह अधिकार भी ‘पेसा कानून’ आने के बाद ‘मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम – 1915’ में संशोधन करके दिया गया था। इसी प्रकार ‘पेसा कानून’ के अनुरूप ‘मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम – 1934’ में व्यापक बदलाव किया गया है, परन्तु जिला-स्तर के अधिकारी / कर्मचारी इनको लागू करने पर ध्यान नहीं देते। राज्यपाल को ‘पेसा कानून’ के अनुसार बदले गए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए।

गौरतलब है कि ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग’ की 14वीं रिपोर्ट (2018-19) में दिये गए सुझाव और अवलोकन पर कार्यवाही करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 अप्रेल 2022 को राज्यपाल के सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लिखा गया है कि राज्यपाल को ‘पांचवीं अनुसूची’ के क्षेत्रों में लागू होने वाले कानून, विनियमन, अधिसूचना का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए। उन्हें यह अधिकार संविधान से मिला हुआ है।
सवाल है, क्या वाकई राज्यपाल इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल आदिवासियों के कल्याण के लिए किये गए कार्य संबंधी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को दें। ‘पांचवीं अनुसूची’ के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट आवश्यक रूप से जनता की पहुंच में होना चाहिए। राज्यपाल के सचिव को कहा गया है कि ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग’ के सुझावों को संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अपनाएँ।
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए राज्यपाल को ‘पांचवीं अनुसूची’ के तहत नियम बनाने का व्यापक अधिकार दिया गया है जिसमें राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार तक को सीमित किया गया है। राज्यपाल को व्यापक विधायी और प्रशासनिक अधिकारों से सम्पन्न किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद – 244 में व्यवस्था है कि किसी भी कानून को ‘पांचवीं अनुसूची’ वाले क्षेत्रों में लागू करने के पूर्व राज्यपाल उसे ‘जनजातीय सलाहकार परिषद’ को भेजकर अनुसूचित जनजातियों पर उसके दुष्प्रभाव का आकलन करवाएंगे और तदनुसार कानून में फेरबदल के बाद उसे लागू किया जाएगा। आमतौर पर इस संवैधानिक व्यवस्था की अनदेखी ही की जाती है।
डॉक्टर अशोक मर्सकोले, विधायक (निवास, मंडला) का कहना है कि 26 वर्षो बाद ‘पेसा कानून’ के नियम बनाना स्वागतयोग्य है, परन्तु इस सम्बन्ध में आदिवासी जन-प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर विश्वास में नहीं लेना आश्चर्यचकित करता है। (सप्रेस)