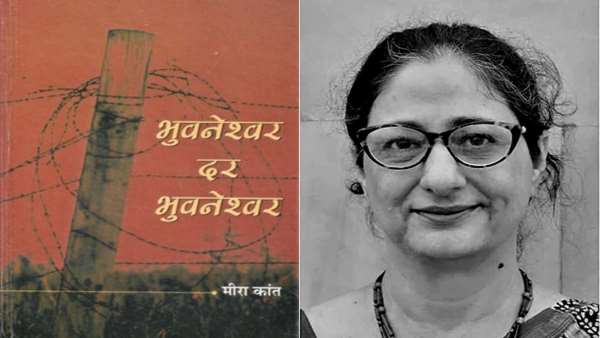लोक नाटकों में दलित अभिव्यक्ति
नाटक चाहे शास्त्रीय हो या लोक आज अगर इसमें दलित अभिव्यक्ति को ढूंढा जा रहा है तो किसी को भी शंका हो सकती है कि क्या पूर्व में इसको नजरअंदाज किया गया है? नजरअंदाज भी किया गया है तो किसी पूर्वाग्रह के कारण? ऐसे सवाल अब केवल नाटक में ही नहीं, साहित्य और इतिहास में भी उठने लगे हैं। कुछ लोग इस पर भी आपत्ति उठाते हैं कि साहित्य तो साहित्य होता है और नाटक तो नाटक, फिर इसमें अलग से दलित अभिव्यक्ति ढूंढने का क्या मतलब? अलग – अलग बांट कर देखने से न साहित्य का भला होने वाला है, न नाटक का। ऐसी बात करने वालों की नीयत अगर साफ होती तो साहित्य या नाटक में वंचित – उत्पीडतों के लिए कोई स्पेस होता। और अगर होता तो नजर भी आता।
केवल नाटक पर ही बात करें तो शास्त्रीय नाटक का जो विपुल संसार हैं उसको खंगालने की जरूरत है। जहाँ पहले से निर्देश जारी कर दिया गया है कि संस्कृत नाटकों का नायक उच्च कुल का, हर गुणों से सम्पन्न, सुंदर, सुशील देववाणी संस्कृत वाचन करने वाला ही होगा तो अवर्ण, अपढ़, असुंदर व्यक्ति को भला कौन नायकत्व प्रदान करेगा? अगर सामंतों के वैभव, उनके उत्थान – पतन, परस्पर द्वंद को केंद्र में रख कर ही नाटक रचना उद्देश्य होगा तो समाज के निचले पायदान की व्यथा कथा कैसे प्रकट हो पायेगी? अगर संस्कृत नाटकों से लेकर वर्तमान के आधुनिक नाटकों तक में इस बहुसंख्यक समाज को अभिव्यक्त नहीं किया गया तो यह केवल भूलवश नहीं है।
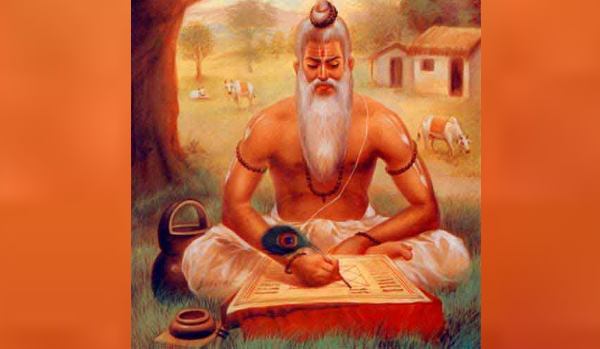
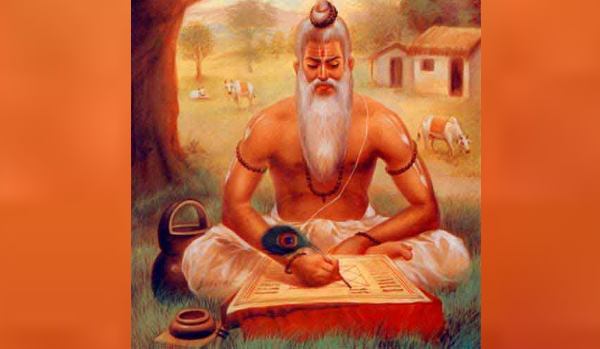
लोक नाटकों का जब भी जिक्र आता है, लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आता है कि भरतमुनि के नाटक की जो धारा है, क्या उसी से निकली हुई है? इस संबंध में आद्य रंगाचार्य के जो विचार हैं , उस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। उनका कहना है कि ‘भरत के नाट्यशास्त्र से पूर्व कुछ ऐसे लोकधर्मी नाटकों का जन्म हो चुका था, जिनमें बड़ा ही असम्भ्रांत आचरण देखने को मिला था। उन नाट्य प्रयोगों के उन अशिष्ट आचरणों से विक्षुब्ध होकर ही देवों, दानवों और गंधर्वों आदि ने पितामह ब्रह्मा के पास जाकर शिकायत की थी।‘ प्रश्न उठता है कि भरत के पूर्व के उन असम्भ्रांत तथा संभ्रांत नाटकों का क्या स्वरूप रहा होगा? इस संदर्भ में विद्वानों का एक मत है कि संभ्रांत नाटकों के पहले असंभ्रांत अर्थात लोक नाटकों का उद्भव हुआ है। अगर पहले हुआ है तो असंभ्रांत अथवा लोक नाटक किस प्रकार के रहे होंगे? इस संबंध में कुछ लोगों का मानना है कि आज विश्व के अनेक क्षेत्रों के आदिवासियों में जो नृत्त, नृत्य तथा नाटकीय प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके आधार पर नाटक के आरंभिक स्वरूप की कुछ कल्पना की जा सकती है। शेल्डान चेनी ने इसी आधार पर अपनी किताब ‘थिएटर’ में कुछ स्थापनाएं रखी हैं।
पिछले कुछ वर्षों से एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि सन एक हजार से सत्रहवीं शती तो हमारे देश में मुसलमान शासकों द्वारा जो आक्रमण हुए, उनके आगमन के बाद जो नया शासन स्थापित हुआ, उसमें भारतीय रंग परंपरा को प्रश्रय न मिलने के कारण दरबारों , नगरों से पलायन कर गांवों की तरफ चले गए। जाने का एक कारण इन शासकों के मजहबी दुराग्रह भी बताते हैं। वे कहते हैं कि इनके मजहब में नाटक करना गैर इस्लामिक है। कुछ लोग इसके लिये ‘हराम’ शब्द भी प्रयोग करते हैं। हालांकि नृत्य, संगीत से उन्हें कोई परहेज नहीं था इसलिए ये कलायें राज दरबार में शोभा बढ़ाती रही।
सत्ता द्वारा पुष्पित – पल्लवित होती रही। लेकिन सत्ता की नजरों में खटकने के कारण नाटक को आस – पास फटकने भी नहीं दिया गया। और जो कला सत्ता की बैशाखियों पर टिकी होती है, जनता में जिनका आधार नहीं होता है, जिनमें जनता की धड़कन नहीं सुनाई देती है, उसके साथ क्या किसी भी कला के साथ यही दुर्गत होता है। सत्ता चाहे इस्लामिक हो या सनातन, कला को अपने तरीके से संचालित करना चाहती है। मौका मिलता है तो विरोधी कला रूपों को तहस – नहस करने में कोई मुरव्वत नहीं करती है। पुष्यमित्र शुंग और खिलजी जैसे राजाओं ने देश की संस्कृति – कला के साथ जो किया, वैसे उदाहरण कहीं भी ढूंढे जा सकते हैं।
ये कोई संयोग की बात नहीं है कि मध्यकाल में भक्तिकालीन जो प्रमुख कवि हुए हैं, उनमें बहुतायत समाज के निम्न वर्ण के हैं। कबीर, रैदास, पीपा, चोखा और सेना नाई जैसे कवियों ने चौराहों पर सत्संग लगाकर जो दोहे, सबद, कवित्त गाये हैं, उसमें समाज के निचले तबके के साथ धर्म के नाम पर जो शोषण – उत्पीड़न हुआ है, उस स्वर को साफ, सरल शब्दों में व्यक्त किया है।


इसी धारा में सन 1855 में फुले का लिखा नाटक ‘तृतीय रत्न’ है। कह सकते हैं कि लोक नाटकों में यह पहला नाटक है जिसमें दलित अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से सामने आता हुआ दिखता है। यह वही काल है जब पेशवा का शासन खत्म हो चुका था। मुल्क पर अंग्रेज का राज था। लेकिन ब्राह्मणवाद की जड़े कमजोर नहीं हुई थी। भोली – भाली अपढ़ जनता अभी भी भाग्यवाद, धार्मिक कर्मकांड के जाल में फंसी हुई थी। फुले ने इस नाटक के माध्यम से बड़े चुटीले ढंग से ब्राह्मणवाद का भंडाफोड़ करते हुए दलित चेतना के विकास पर बल दिया था। इस नाटक में एक खेतिहर किसान के घर पर न होने का मौका देखकर पुरोहित ब्राह्मण उसकी गर्भिणी स्त्री को दिन, नक्षत्र आदि का डर दिखा कर, संकट टालने के लिए , कर्मकांड का सहारा लेते हुए जिस तरह आर्थिक दोहन करता है, मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
महाराष्ट्र की लोकप्रिय लोक शैली ‘खेतीवाड़ी’ में लिखे गए नाटक को मंचित करने के लिए कोई ताम – झाम वाले मंच की जरूरत नहीं होती है। यह नाटक मध्यकाल में भक्तिकालीन कवियों द्वारा लगाई जाने वाली ‘सत्संग’ की तरह कहीं भी खेला जा सकता है। इसमें भी अन्य लोक नाट्य शैली की तरह विदूषक जैसा करैक्टर है जो नाटक की कथा के साथ – साथ तो चलता ही है, जरूरत पड़ने पर नाटक से निकल कर, रंगमंच की चौथी दीवार को तोड़कर दर्शकों से सीधा रूबरू हो जाता है। दर्शकों को मंच पर घट रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए रह – रह कर उकसाता भी है। मध्यकाल में ‘कबीर – रैदास संवाद’ नाटक के द्वारा संवाद शैली में कथा को जिस तरह नाटकीय रूप प्रस्तुत होते हुए देखते हैं, उसी फॉर्म में बाद के दिनों में फुले की चर्चित रचना ‘गुलामगिरी’ और ‘किसान का कोड़ा’ में भी देखते हैं। सन 1873 में लिखा ‘गुलामगिरी’ दलितों पर छल – प्रपंच के सहारे ब्राह्मणवाद द्वारा ढाए गए अत्याचार का दस्तावेज है।
असुरों की मिथकीय कथा को सोलह परिच्छेदों में ज्योतिराव और धोंडी राव नामक चरित्रों के माध्यम से सवाल – जवाब रूप में रखा गया है। इसमें फुले को जो कहना है, उन्होंने कथा के द्वारा ही कहा है। अलग कहीं से भाषण व उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह उन्होंने कई पंवाड़ा भी लिखा है जिसमें सामाजिक सवाल को गायन के माध्यम से उठाया है। किसी पंवाड़ा मे इंजीनियरिंग विभाग में ब्राह्मण कर्मचारी के लूट – खसोट को विषय बनाया गया है तो किसी में मारवाड़ी, ब्राह्मण – पुरोहित की चालाकी तो किसी में शूद्रों के भोलेपन को।


भोजपुरी के कवि हीरा डोम की कविता ‘अछूत की शिकायत’ सन 1914 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली हिंदी की ‘सरस्वती’ नामक साहित्यिक पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पादन में प्रकाशित हुई थी। इसमें हीरा डोम ने दलित जीवन के दुख, अवसाद और पीड़ा को गहराई से व्यक्त किया है। आदि हिन्दू के प्रवर्तक स्वामी अछूतानंद ‘हरिहर’ का आर्य समाज से मोहभंग होने के बाद अम्बेडकर से जुड़े थे। उसका उनकी कविता के साथ – साथ नाटक पर जो प्रभाव दिखा, वो काफी महत्वपूर्ण है। उनके दो प्रकाशित नाटक आज उपलब्ध हैं। ‘मायानंद बलिदान’ और ‘राम राज्य न्याय’। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने ‘राम राज्य न्याय’ नाटक के परिचय में लिखा है, ‘ स्वामी जी के दिमाग में कई नाटकों के प्लाट थे, जिनके द्वारा वे आदि हिन्दू ज्ञान को साकार करना चाहते थे। किंतु उनका जीवन इतना व्यस्त और चिन्ताग्रसित था कि वे अपनी इच्छानुसार उन्हेँ लिख न सके।
उनके मनोभिलाषित नाटक थे – ‘समुन्द्र मंथन’, ‘बलि छलन’, ‘एकलव्य’, एवं ‘ सुदास और देवदास’। इन नाटकों का संक्षिप्त परिचय देते हुए जिज्ञासु जी लिखते हैं, ‘ नाटक ‘समुन्द्र मंथन’ का विषय आर्य देवों की प्रवंचना और धूर्तता एवं विष्णु का मोहनी औरत बन कर आदिवासी असुरों को धोखा देना था, ‘ बलि छलन’ का महादानी और महापराक्रमी आदिवासी असुर सम्राट महाराजा बलि को आर्य देवों और ब्राह्मणों के षड्यंत्र द्वारा बौने ब्राह्मण का रुप धर कर विष्णु का छलना था, ‘एकलव्य’ नाटक में अदिवतीय धनुर्धर निषाद पुत्र एकलव्य का अत्यंत नीचता से अंगूठा कटवाना था तथा ‘सुदास और देवदास’ में यह दिखाना था कि वे दोनों भारत के आदि निवासी राजा थे। इनमें देवदास विभीषण और जयचंद की तरह, आर्यों के सेनापति इंद्र से मिल गया था, जिसकी साजिश से सुदास पराजित हुआ और सिंध एवं पंजाब प्रदेश पर आर्यों का प्रभुत्व कायम हो गया।‘
सन 1933 में अछूतानंद बीमारी के कारण आकस्मिक गुजर गए। उनके चले जाने से इन नाटकों के लिखने की जो परिकल्पना थी, वो अपूर्ण ही रह गयी। लेकिन जिन दो नाटकों को लिखा, उसने दलित थिएटर के लिए मजबूत आधार दिया।
आज़ादी के पहले और बाद में इप्टा के नेतृत्व में देश व्यापी जो सांस्कृतिक आंदोलन चला, उसमें दलितों पर होने वाले जुल्म को वर्ण की अपेक्षा वर्ग के धरातल पर सैद्धान्तिक रूप से विश्लेषण करने पर ज्यादा जोर दिया गया। यही कारण है कि इप्टा के उस दौर के अधिकतर नाटकों में दलित उपस्थिति तो दिखाई देती है , लेकिन वर्ण और वर्णवादी व्यवस्था से जुड़ी सामंती तत्वों से कहीं टकराते हुए नजर नहीं आते हैं।
हबीब तनवीर इप्टा के आंदोलन से शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं। इससे अलग होने पर भी उनके मिजाज में कोई बदलाव नहीं आया। वे मूल रूप से वाम धारा के ही थिएटर एक्टिविस्ट थे। वाम धारा को लेकर उनके अंदर कोई जड़ नहीं था। वर्ग संघर्ष से अगर सहमत थे तो समाज में व्याप्त वर्ण भेद – वर्ण संघर्ष को भी एकदम खारिज नहीं करते थे। न अपने नाटकों में जान – बूझ कर लाने से कहीं कोताही करते थे। न वैचारिक आधार पर अपने को कहीं रोका है।


‘पोंगा पंडित’ हबीब तनवीर का लिखा हुआ नाटक नहीं है। आज़ादी के पहले से ही, सन 1935 – 36 के आस – पास से छत्तीसगढ़ के गांवों में लोक कलाकारों द्वारा होता आ रहा है। नाटक में पंडित, भकला और जमादारिन तीन पात्र हैं जिनके माध्यम से समाज में उच्च वर्ण के द्वारा निम्न वर्ण के प्रति किस तरह भेद – भाव, छुआ – छूत का व्यवहार होता है, उसे छोटे – छोटे चुटीले इम्प्रोवाइज्ड संवादों के बहाने रखा गया है। जैसा कि लोक नाटकों में गीत बहुत कारगर होते हैं, हबीब तनवीर ने अजय उस्ताद और स्वर्ण कुमार साहू से नाटक के अनुकूल जो गाने लिखवा कर डाले, उसने नाटक के लोक तत्व को और मजबूत कर दिए थे। हबीब तनवीर ने इस नाटक को हिंदुस्तान के कई शहरों में खेला। हास्यरूपी यह नाचा बहुत बड़ी – बड़ी बातें बहुत गहराई से, मगर बहुत सहज ढंग से कह जाता है। विषय में एक लोभी पंडित का लालच भी शामिल है, छुआछूत की बुराइयों पर भी फबती है, और सबसे बड़ी नाटक की ये खूबी है कि भगवान से नाता रिश्ता, बिना किसी माध्यम के, सीधे भी स्थापित किया जा सकता है, बड़े हल्के – फुल्के ढंग से, मजाक – मजाक में कह जाता है।
ये कहना शायद गलत न होगा कि ‘पोंगा पंडित’ नाचा शैली का एक शाहकार, एक क्लासिक, एक मास्टरपीस है। सबसे चर्चित नाटक ‘चरनदास चोर’ में भी हबीब तनवीर ने इस विचारधारा का निर्वाह किया था। उन्होंने विजयदान देता की कहानी को छत्तीसगढ़ में प्रचलित सतनाम धर्म की परंपरा को इस नाटक से जोड़ दिया। सतनाम धर्म के मूल प्रतिपादक थे गुरु घासीदास। सतनाम धर्म का मूलभूत सिद्धान्त है – सत्य ही ईश्वर है। इस नाटक का नायक चरनदास भले निम्न जाति का था, पेशे से एक चोर था, लेकिन सतनाम गुरु के दिये गए वचन को सत्ता के दवाब पड़ने पर भी टूटने नहीं दिया। हबीब तनवीर ने अपने नाटकों में लोक धर्म का हमेशा निर्वाह किया। उनके अधिकतर कलाकार चूंकि समाज के इसी पृष्ठभूमि से आते थे, हबीब तनवीर की कल्पना को यथार्थ की जमीन पर जीवंत रूप से उतारने में सौ फीसदी सफल रहे।
भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने आरा, छपरा, बलिया, सोनपुर, हाजीपुर जैसे जिलों में जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ एक लंबे समय तक नौटंकी शैली में जो बाद में उनके ही एक लोकप्रिय नाटक ‘बिदेसिया’ के सफल होने के कारण ‘ बिदेसिया’ कहा जाने लगा, किया है। लोगों की जुबान पर यह नाटक इस तरह चढ़ गया कि उनके लिखे सारे नाटक के नाम से भले अलग – अलग हों, शैली के रूप में ‘बिदेसिया’ ही कहा जाने लगा। सन 1887 में जन्मे लोक कलाकार भिखारी ठाकुर ने अपने 74 साल के जीवनकाल में कैथी और देवनागरी में लगभग 29 पुस्तिकाओं की रचना की। लोक नाटकों तथा सैकड़ों लोक भजन, कीर्तन, गीत, कविता की रचना करने के साथ – साथ अपनी बनायी मंडली के प्रशिक्षक, प्रबंधक भी थे। उन्होंने जो लिखा , उसे खुद अपनी मंडली के दलित, पिछड़ी जाति के कामगार – कलाकारों के साथ तैयार किया और गांव – गांव घूम कर भोजपुरी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण का संदेश फैलाया।
‘बिदेसिया’ में पति – वियोगिनी नारी, ‘भाई – विरोध’ में संयुक्त परिवार के विघटन, ‘विधवा – विलाप’ में विधवा के प्रति सामाजिक अत्याचार, ‘ गंगा – स्नान’ में धार्मिक आडंबर, ‘पुत्र – वध’ में नारी चरित्र के विचलन, ‘गबरघिचोर’ में मानव को वस्तु के रूप में देखने की मानसिकता, ‘ननद – भउजाई’ में बाल – विवाह, ‘ कलियुग – प्रेम’ में समाज में बढ़ रही नशाखोरी एवं उनके दुष्परिणामों तथा ‘बेटी – वियोग’ में बेटी को बेचने तथा अनमेल विवाह जैसी समस्याओं को भिखारी ठाकुर ने उठाया और आम जनता को इन सामाजिक समस्याओं के प्रति शिक्षित किया ताथैं स्थितियों से उबरने के संकेत भी दिए।


सन 1956 के बाद अम्बेडकर के निजी प्रयास पर महाराष्ट्र में दलित थिएटर का जो उदय हुआ, उसने पूरे देश के रंगकर्मियों पर गहरा असर डाला। महानगरों के रंगमंच पर तो उत्पीडतों का जीवन दिखा ही, विभिन्न लोक नाटकों में भी मुखर होकर आया। अब विषय के रूप में केवल शोषण – उत्पीड़न – सहानुभूति ही प्रमुख नहीं होता था, उनका प्रतिरोध – संघर्ष भी खुल कर आता था। उन्हें अभिजात्य रंगकर्मियों के नेगेटिव रिमार्क्स की परवाह नहीं रहती थी। उनके सामने दर्शकों की एक बहुत बड़ी संख्या होती थी जो अपने नायकों को मंच पर देखना चाहती थी। विशेष कर हिंदी में पैरियार ललई सिंह यादव, रामअवतार पाल, अमर विशारत, मोहनदास नैमिशराय, सूरजपाल सिंह चौहान , ओमप्रकाश बाल्मीकि और माता प्रसाद जैसे दलित नाटककार ने अपने नाटकों में जिन मिथकीय पात्रों को आज के संदर्भों से जोड़ते हुए रखा, उसका स्वागत अगर शहरी रंगमंच पर हुआ तो उससे कई गुना अधिक लोक नाटकों में बस कर उनकी चेतना को जागृत किया है।
वर्णवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहे बुद्ध, कबीर, रैदास और अम्बेडकर को अपने राजनीतिक हित के लिए संदर्भों से काटकर अपने तरीके से पेश करे, लेकिन सांस्कृतिक आंदोलन की जो दलित धारा चली है , वह इतिहास और वर्तमान के सारे पन्ने खोल – खोल कर सामने रखते जा रही है। लोगों को उन पन्नों की तरफ इशारा कर रही है जहाँ बुद्ध, कबीर, रैदास, फुले और अम्बेडकर दलितों के हक में पुरजोर ढंग से आवाज उठा रहे हैं।