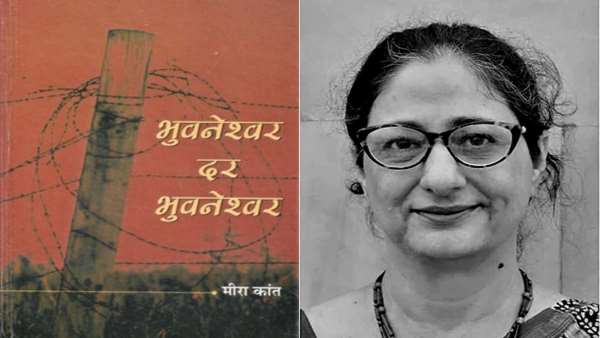ब्रेष्टियन शैली में राजनीतिक रंग दृष्टि
ब्रेष्ट के समय जर्मन में हिटलर राष्ट्रवाद की ओट में जिस तरह यहूदियों पर दमन कर रहा था, आर्यन जाति को श्रेष्ठ साबित कर अल्पसंख्यकों पर यातनाएं ढा रहा था, विरोध करनेवालों पर राष्ट्रद्रोह का आरोप मढ़ कर जेल की सलाखों के पीछे कैद कर रहा था, संभवतः उस समय की शैलियों में संप्रेषित करना ब्रेष्ट को कारगर नहीं लग रहा होगा। नाटकों के लिए ब्रेष्ट जिस तरह के कथ्य उठा रहे थे, उसे जनता के बीच ले जाने के लिए किसी ऐसी शैली की तलाश में थे जो देखनेवालों को केवल तटस्थ की मुद्रा में न छोड़े, चेतना के स्तर पर उन्हें सक्रिय करते हुए व्यवस्था परिवर्तन की भूमिका में लाने के लिए विवश करे। ब्रेष्ट का ‘एपिक थिएटर‘ रंग जगत के सामने आया तब जाकर यह तलाश पूर्ण हुई।
ब्रेष्ट स्वीकारते हैं कि एपिक थिएटर की परिकल्पना उनकी कोई निजी खोज नही है। उस वक्त पूरी दुनिया में फासीवाद के विरुद्ध जो उथल – पुथल चल रहा था, विशेष कर एशिया में प्रतिरोध के रंगमंच का जो स्वरूप उभर कर आ रहा था, ब्रेष्ट उससे काफी प्रभावित थे। उस पर गहरी नजर रखे हुए थे। वर्ष 1935 में ब्रेष्ट की मुलाकात विश्वविख्यात चीनी एक्टर माई लान फांग से मास्को में हुई थी। वहाँ उन्होंने लान फांग को एक प्रस्तुति में स्त्री की भूमिका में देखा था। लान फांग ने नदी में किश्ती खेती हुई स्त्री की भूमिका को जिस तरह निभाया था, ब्रेष्ट को रोचक लगा था। लान फांग के अभिनय में आंगिक – वाचिक और आहार्य को प्रतिस्थापित करने का जो स्वंत्र तरीका था, ब्रेष्ट को बिल्कुल नया लगा।
कालांतर में ब्रेष्ट की यही सोच, रंगमंच की एक नई अवधारणा ‘एपिक थिएटर’ के रूप में हमारे सम्मुख आया, जिसके आधार में लोक परम्परा की नींव थी। जिसका ज्यादा जोर नाटकीयता और अभिनय पर होता था। जन – जन के बीच नाटक को ले जाकर, दर्शकों को चेतना के स्तर पर मजबूत कर आन्दोलनकारी भूमिका में लाने के लिए यथार्थवादी रंगमंच के टूल्स पर ज्यादा भरोसा नहीं किया, बल्कि प्रोसिनयम थिएटर के उपकरणों और उनके प्रभावों को नकली, कृत्रिम कहा। ब्रेष्ट अपने रंगमंच पर कहानी कहने लगे, घटनाओं का वृतांत सुनाने लगे। दर्शकों को अपने नाटकों में इन्वॉल्व करने के बजाय आइसोलेट रखते थे।
उन्हें आब्जर्वर की भूमिका में लाने की कोशिश करते थे जिससे दर्शकों की क्रियात्मक क्षमता निष्क्रिय होने के बजाय उनकी आलोचनात्मक पक्ष में वृद्धि होती थी। वे निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र होते थे। ब्रेष्ट अपने दर्शकों को नाटक के प्रदर्शनों के दौरान हमेशा इस बात का अहसास दिलाते रहते थे कि वे ऑडिटोरियम में हैं और वे नाटक देख रहे हैं। सामने मंच पर जो घटित हो रहा है, यथार्थ नहीं है। जो देख रहे हैं वो केवल अतीत या वर्तमान का वृतांत है। ब्रेष्ट नाटक और दर्शक के बीच किसी तरह का तादात्म्य स्थापित करने के पक्ष में नहीं रहते थे। वे कतई भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के प्रयास में नहीं रहते थे। नाटक देखते समय दर्शक सजग – सचेत रहे, इसके लिए नाटक में नई – नई युक्तियां इजाद करते रहते थे। अगर कोई युक्ति पुरानी परम्परागत शैली में भी दिख जाती थी तो उसे अपनाने में हिचकते नहीं थे।
इसके लिए ब्रेष्ट अपने रंगमंच में alienation theory , संक्षेप में A – effect, हिन्दी में कहे तो अलिप्तिकरण, वियुक्तिकरण या फिर अलगाव का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ब्रेष्ट इस सिद्धांत को एपिक थिएटर में निर्रथक नहीं लाते हैं, इनके कारणों के पीछे के तर्क को भी जानना जरूरी है। ब्रेष्ट के बड़े नाटक हो या छोटे नाटक या उनके स्ट्रीट कार्नर सीन, सबों में आम आदमी की ज्यादतर भागीदारी होती थी। उनके पात्रों में अधिकतर दुकानदार, मजदूर, मिल में काम काम करने वाले होते थे। जब नाटक का ऐसा करैक्टर किसी घटना को अभिनय करके बताता था तो केवल वह अभिनय ही नहीं करता था, उस घटना की सत्यता की जांच करता था, घटना को तटस्थ भाव में देख कर वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण कर अपना नजरिया भी प्रस्तुत करता था। इस तकनीक से दर्शकों को भी अपने तर्क से विश्लेषण करने की पूरी स्वतन्त्रता मुहैय्या करता था। यह सिद्धांत केवल तकनीक तक सीमित नहीं था।
इसमें कहीं न कहीं ब्रेष्ट की राजनीतिक दृष्टि भी थी। वे अपने वक्त में दर्शकों को उस फासीवाद के खिलाफ भी तैयार कर रहे थे। वे पारंपरिक यथार्थवादी रंगमंच की तरह दर्शकों को सुसुप्तावस्था में ले जाने के पक्ष में कतई नहीं थे। न यथार्थवादी रंगमंच के तर्ज पर थिएटर को स्त्री – पुरुष सम्बन्ध में उलझाए रखना चाहते थे। औद्योगिकरण और महायुद्ध जैसी घटनाओं के बाद लोग धर्म – अर्थ के मुद्दों से जिस तरह रोज – रोज की जिन्दगी में टकरा रहे थे, ब्रेष्ट का जोर इस पर ज्यादा था। और किसी भी सत्ता या व्यवस्था को यह कहाँ बर्दाश्त होने वाला है? ब्रेष्ट अपने नाटकों के द्वारा सत्ता पर चोट कर रहे थे वो हिटलर और नात्सी शासन को गले के नीचे नहीं उतर रहा था।
सन 1933 में नात्सी शासन से बचने की गरज से ब्रेष्ट को मजबूरन जर्मन से पलायन करना पड़ा। सन 1933 से 39 तक स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क में रहने के बाद स्वीडन, फ़िनलैंड और रशिया से होते हुए अमेरिका के केलिफोर्निया नगर में सन 1942 से 49 तक रहे। पलायन के वर्षों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण नाटकों का लेखन किया। सन 1949 में वापस जर्मनी लौटे। पूर्वी बर्लिन में हेलेन वाइगेल के साथ ‘बेलीर्नर एनजेम्बल‘ की नींव रखी। यहाँ के रंगमंच पर ब्रेष्ट ने जिन नाटकों का मंचन किया, कथ्य और सिद्धान्त के कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति हुआ।
आज भले हिटलर हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज कई देशों में हिटलर की प्रवृत्ति वाले नए – नए रूपों में दिखाई देने लगा है। साम्राज्यवाद और पूँजीवाद अपने वास्तविक रूप में आने के बजाय राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर फासीवाद को नए तरीके से लाने के प्रयास में है। हिटलर का फासीवाद एक बार फिर धर्म, युद्ध और राष्ट्रवाद के बहाने जगह – जगह उभरने लगा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के निशाने पर लगातार हैं। शुद्ध रक्त और जन्मजात श्रेष्ठता का स्वर उभरने लगा है। ऐसे में रंगकर्मियों को अभिव्यक्त करने के लिए ब्रेष्टियन थिएटर से कारगर और कोई नहीं हो सकता है। विशेषकर भारतीय परिपेक्ष्य में तो ब्रेष्टियन थिएटर बिल्कुल मौजू है। दरअसल एपिक थिएटर में प्रतिरोध के जो रूप हैं, लोक परम्परा में पहले से उपस्थित हैं। ब्रेष्टियन थिएटर का जो सिद्धान्त है, कहीं से आयातित नहीं लगता है।
भले एपिक थिएटर इस मुल्क में न गढ़ा गया हो, लेकिन यहाँ के लोक में वर्षों से व्यवहार में है। ज्योतिबा फुले ने सन 1855 में ‘तृतीय रत्न’ नाम का जो नाटक लिखा था उसमें उन्होंने ब्राह्मण वर्ग द्वारा धार्मिक पाखण्डों के नाम पर भोले – भाले अशिक्षित दलित किसानों का लूटने – ठगने को बड़े रोचक ढंग से दिखाया था। ब्राह्मणवाद का भंडाफोड़ करते हुए फुले ने दलितों को शिक्षित होने तथा अंधविश्वास से मुक्त होने का आह्वान किया था। उनदिनों देश में पारसी नाटक शुरू ही हुआ था, तब फुले इस मराठी नाटक को महाराष्ट्र की लोक शैली ‘खेतवाड़ी’में देहातों में लगातार कर रहे थे। उनके नाटक करने का उद्देश्य केवल ग्रामीण समाज को मनोरंजन देना मात्र नहीं था, बल्कि यह उनके आन्दोलन का हिस्सा था।
यह नाटक ब्रेष्ट के एपिक थिएटर के ही तरह है। फुले अपने नाटक की कथा को बार – ,बार तोड़ते हैं। बल्कि इसमें जो विदूषक है वो दर्शकों से लगातार संवाद स्थापित करता हुआ दिखता है। विदूषक नाटक में चरित्र निभाता है और जरूरत पड़ने पर नाटक की कथा से बाहर आकर दर्शकों से नाटक पर बात भी करने लगता है। नाटक के पात्रों के बारे में टिप्पणी भी करने लगता है और दर्शकों को सचेत करते हुए प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है।
ब्रेष्ट की तरह फुले भी इस लोक शैली ‘खेतवाड़ी’ को ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फासीवाद – पूँजीवाद के खिलाफ ब्रेष्ट के नाटकों में जो राजनीतिक रंग दृष्टि थी, उसी तरह की रंगदृष्टि सामाजिक बदलाव के लिए फुले के रंगमंच में थी। ब्रेष्ट की शैली हमारे यहाँ संस्कृत और लोक नाटक दोनों में बहुत पहले से है। ऐसे कई उदाहरण भिखारी ठाकुर के नाटकों में सहज मिल जाएंगे। बल्कि भिखारी ठाकुर का नाटक ‘गबरघिचोर’ और ब्रेष्ट का ‘खड़िया का घेरा’ नाटक के कथासार में इतना साम्य है कि दर्शकों को फर्क करना मुश्किल हो जाता है।
भारत में बीसवीं सदी के छठे दशक के बाद समाज के एक बहुत बड़े तबके को जब वर्तमान सत्ता से मोहभंग हुआ और प्रतिक्रिया में जगह – जगह मजदूर आन्दोलन होने लगे, सामन्तों के खिलाफ किसान संघर्ष करने लगे तो सांस्कृतिक हलकों में अभिव्यक्ति के लिए जिस प्लेटफार्म को तलाशा जाने लगा, उसमें ब्रेष्ट लोगों को ज्यादा मुफीद लगे। न केवल उनके नाटक बल्कि उनकी धारदार कविताएं, छोटे – छोटे नाटक या कहे स्ट्रीट कार्नर सीन नुक्कड़ों – मंचों पर धमक के साथ आने लगे। उनके नाटक सभी तबकों को भाते थे। एक तरफ ब्रेष्ट अगर वामधारा से जुड़े रंगकर्मियों को पसंद थे तो सत्ता संस्थानों को भी कम आकर्षित नहीं करते थे।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे दूसरे सरकारी नाट्य संस्थानों में तो नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिये ब्रेष्ट पढ़ाये भी जाते हैं। व्याहारिक पक्ष की जानकारी देने के लिए उनके किसी नाटकों का मंचन भी किया जाता है। लेकिन सरकारी नाट्य संस्थानों में ब्रेष्ट जब किये जाते हैं तो उनका ज्यादा जोर फॉर्म पर होता है। कंटेंट को ज्यादा उभारने के बजाय उनकी जो शैली है, उसको हाईलाइट करने में ज्यादा बल देते है। ब्रेष्ट अपने नाटकों से सत्ता, व्यवस्था पर जिस तरह हमले करते थे, इनका उद्देश्य वो नहीं होता है। बल्कि इनका प्रयास होता है कि सरकार, धर्म, व्यवस्था पर जो निशाने हैं, उसे डायल्यूट कर दिया जाय। कलात्मक रूप से नाटक को इतना सजा दिया जाय कि नाटक ब्रेष्टियन शैली का तो लगे, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ न जाय। उस पर तीखे प्रहार न करे। कभी – कभी तो सत्ता के पक्ष में भी खड़ा करने की कोशिश करते है।
पिछले दिनों लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी में छात्रों को ब्रेष्टियन शैली की सैद्धान्तिक – व्यवहारिक जानकारियां देने के लिए ब्रेष्ट के ‘खड़िया का घेरा’ का महीने भर की तैयारी के बाद मंचन किया गया। ब्रेष्ट के नाटकों में कोरस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोरस में जो गाने – बजाने वाले होते हैं, वे अपने गायन से दर्शकों को मंत्र – मुग्ध नहीं करते हैं। वे कथा को आगे बढ़ाने का सूत्र देते हैं, लय को खंडित कर जहाँ जरूरत होती है, पद्यात्मक – गद्यात्मक रूप में दर्शकों को राय भी देने लगते हैं। लेकिन इस छात्र प्रस्तुति में निर्देशक ने कोरस के सारे कलाकारों को भगवा वस्त्र पहनाकर, ललाट पर लाल तिलक – त्रिपुंड लगाकर, ऐसे बैठा दिया मानो सनातन धर्म की कोई कथा सुना रहे हो। गायन का भी ऐसा अंदाज था जैसे किसी विशेष धर्म की महिमा गायी जा रही हो। संभवतः निर्देशक पर वर्तमान सरकार का दवाब हो या प्रसन्न रखने के लिए किया गया व्यक्तिगत प्रयास हो।
कहीं से नाटक वर्तमान सत्ता को अपने से रिलेट नहीं कर रहा था। न देखने वालों को इस नाटक में वर्तमान सत्ता की निरकुंशता, अधिनायकता का आभास हो रहा था। पुरुष अभिनेता लान फांग का केवल मुद्राओं द्वारा नदी में किश्ती खेती हुई महिला का करुण अभिनय जो ब्रेष्टियन शैली का आधार बना, वह दर्शकों को कल्पना की पूरी स्वतन्त्रता देता है। भ्रम में नहीं रखता है कि फांग कोई स्त्री अभिनेता है। दर्शकों तक संप्रेषित हो जाता है कि मंच पर जो स्त्री का चरित्र है, वो पुरुष निभा रहा है और मुद्राओं से ये भी स्पष्ट हो जा रहा है कि उस स्त्री की नदी पर करने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन बीएनए की प्रस्तुति में नायिका को जब नदी पर बनी पुल पर से पार करके दिखाना होता है तो निर्देशक उसे अभिनीत करने के लिए अलगाव सिद्धान्त का प्रयोग करने के बजाय मंच सज्जा में सीढ़ी का पुल लाते हैं और उस पर से चलते हुए नायिका को नदी के उस पार ले जाते हैं। मुद्राओं द्वारा इसे अभिनीत के बजाय यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करने पर दर्शकों का ध्यान बांस के बने पुल के अत्यधिक हिलने – डुलने पर ही लगा रहता है, नायिका का जद्दोजहद उभर कर आ ही नहीं पाता है।
ऐसा ही एक उदाहरण सफदर हाशमी ने पारंपरिक रूपों और डिवाइसेज के सवाल को उठाते हुए अपने एक लेख में दिया था। उन्होंने लिखा था कि ब्रेष्ट के नाटक खड़िया का घेरा का प्रोडक्शन रैना ने किया पराई कुक्ख के नाम से और एक प्रोडक्शन किया कविता नागपाल ने मिट्टी ना होवे मैत्रेय के नाम से। दिलचस्प बात यह है कि दोनों प्रोडक्शन एक ही स्क्रिप्ट पर आधारित थे, यहाँ तक कि दोनों का संगीत, गीतों की धुनें तक वही थी। लेकिन पराई कुक्ख एक रीलैंटलेसली पोलिटिकल प्रोडक्शन था, उसमें जोर था माहौल पर, कथ्य पर। दूसरा प्रोडक्शन स्पेक्टेक्युलर था, उसमें कैलेंडर वाली क्वालिटी थी। उन्हीं पारंपरिक धुनों के बावजूद दूसरा प्रोडक्शन मेरी नजर में हरगिज नहीं जम पाया। फर्क था निर्देशकों के रवैये में, परम्परा और उनके रिश्ते की पुख्तगी में। इसीलिए जहाँ एक प्रोडक्शन में परम्परा डिवाइस बनकर गूंजी, दूसरे में वह डिवाइस न बन पायी, अपनी प्योरिटी को स्थापित करने की कोशिश में बेजान हो गयी, निर्जीव हो गयी।’
एनएसडी, बीएनए या इसी के समदृश्य संस्थाएं जो सत्ता की धारा के साथ चलती हैं, वो अगर ब्रेष्ट का नाटक करती है तो जरूरी नहीं कि उसमें वही रंगदृष्टि हो जो ब्रेष्ट की है। उनकी स्थापना ब्रेष्ट के विपरीत भी हो सकती है। बीएनए का ही उदाहरण लीजिए, ब्रेष्ट अपनी शैली से जिस फासिस्ट सत्ता का विरोध कर रहे हैं, वहीं शैली बीएनए में हिन्दू फासीवाद के समर्थन में चला जा रहा है। ब्रेष्टियन शैली की क्या राजनीति है, अगर स्पष्ट नहीं होगी तो वो प्रस्तुति सत्ता के पक्ष में जाने की पूरी संभावना है। ब्रेष्ट लगभग तीस वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर समर्थक रहे, अलबत्ता यह दूसरी बात है कि वे कभी भी पार्टी के सदस्य नहीं रहे। सन 1947 में अपने विरुद्ध एक मुकदमें की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था, ‘यह मेरे लिए सबसे अच्छा था कि मैं किसी भी (राजनैतिक) दल का सदस्य न बनूं … मेरा ख्याल है कि वे (अर्थात जर्मन कम्युनिस्ट) मुझे मात्र एक ऐसे लेखक के तौर पर मान्यता देते हैं जो सच लिखना चाहता ही, जैसा कि उसने देखा : लेकिन एक राजनैतिक व्यक्ति की तरह नहीं … मैंने पाया कि ये मेरा काम नहीं है।’
इसमें कोई शक नहीं कि ब्रेष्ट एक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी नाटककार थे, लेकिन अपने नाटकों में पार्टी की विचारधारा को कभी उपदेशात्मक या प्रचारात्मक रूप में नहीं रखा। सच है कि उनके नाटकों में राजनीति की वैचारिकी जगह – जगह उभर कर आयी है, लेकिन वो इतने कलात्मक रूप में है कि एक नया सौंदर्य स्थापित करता है।
आज हमारा देश जिस संकट से गुजर रहा है, फासिस्ट तत्व जिस तरह राजनीति और संस्कृति के क्षेत्र में पैर पसार रहा है, उसमें ब्रेष्ट के नाटक हमारे लिए ज्यादा सहयोगी साबित होंगे। और ब्रेष्टियन शैली ही रास्ता दिखाएगी कि जब अंधेरा हो … सामने कुछ नजर न आये … जो इधर- उधर बिखरे हैं, उन्हें एक कोरस का रूप दे कर अंधेरे के समय में … अंधेरे के ही विरुद्ध गीत गाए ।
.