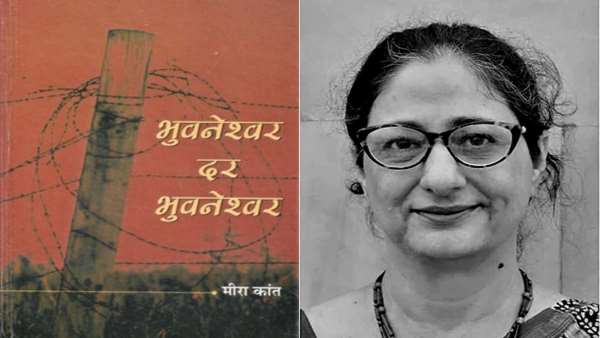राज बिसारिया के रंगमंच की दुनिया
लखीमपुर खीरी में जन्मे राज बिसारिया आज 86 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जहां अधिकतर रंगकर्मी रंगकर्म को अलविदा कर देते हैं, अस्वस्थ होने के कारण लाचार हो जाते हैं, नॉस्टेल्जिया में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, राज बिसारिया आज भी व्यवहारिक और सैद्धान्तिक स्तर पर किसी युवा की तरह एक्टिव हैं। भले उनके हाथ में एक छड़ी आ गयी हो, लेकिन चाल वही है। झुके नहीं है। न आवाज लड़खड़ायी है, न तलफूज्ज में किसी तरह की लड़खड़ाहट आयी है। बोलने का वही अंदाज। हल्की नहीं, कड़क। खालिस लखनवी। मजाल है कि कहीं किसी शब्द में जहां नुक्ता चाहिए, भूल से भी छूट जाए। देखने में भले दूर से अंग्रेजीदा नजर आते हैं, पास जाने पर लखनऊ की सौंधी–सौंधी ताजी खुश्बू आती रहती है…
अंग्रेजी नाटक से रंगकर्म की यात्रा शुरू करने वाले राज बिसारिया का जो प्रारंभिक काल था, वो दौर नेहरूयुगीन था। आजादी के बाद सत्ता की जिम्मेदारी जिस नेहरू को दी गयी थी उससे राजनीति ही नहीं सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े लोगों को भी काफी आशाएं थी। नए भारत में जो कल्पनाएं कर रखी थी, पूरी होने की संभावनाएं दिख रही थी। उसका एक कारण यह भी था कि नेहरू एक आधुनिक ख्याल वाले राजनीतिक शख्स थे। उनके यहां परंपरा के नाम पर संकीर्णता–कूपमंडूकता के लिए कोई जगह नहीं थी। रंगमंच में उनदिनों आधुनिकता के प्रवेश के साथ-साथ पाश्चात्य देश का जो यथार्थवाद हमारे यहां आया था, उसका एक कारण नेहरू की आधुनिकता, समाजवाद के प्रति गहरी निष्ठा भी थी। रंगकर्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा तबका नेहरू की विचारधारा में बिलीव कर रहा था। कोई शक नहीं कि राज बिसारिया के रंगकर्म पर प्रारंभ में उसका असर पड़ा हो। नेहरू के आधुनिक भारत की परिकल्पना से कुछ हद तक सहमत भी हों। लेकिन उनके नाटकों में तत्कालीन सरकार का कोई हिडन एजेंडा रहता था, इससे कतई सहमत नहीं हुआ जा सकता है। न ऐसा कोई उदाहरण उनके किसी नाटक में देखने को मिलता है।
अब तक के अपने जीवन काल में उन्होंने कई राजनीतिक सत्ता को अपने पास से आते और जाते देखा है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उन्होंने ऐसा कोई धार्मिक, राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दिया है जो किसी खास जाति, वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय व पार्टी के प्रति किसी तरह की प्रतिबद्धता दिpखाती हो। अगर राज बिसारिया के रंगकर्म के सम्पूर्ण जीवन काल पर माइक्रोस्कोपिक ढंग से भी विश्लेषण करने की कोशिश करें तो ऐसा कोई उदाहरण हाथ नहीं आनेवाला जो किसी वर्ग, समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला हो। उसका बड़ा कारण शायद उनकी तालीम का भी है। वे जिस विषय के शिक्षक थे, उसमें तो मास्टर थे ही, रंगकर्म में भी सिद्धहस्त हैं।

सन 1964 में जब उन्होंने लखनऊ में ‘थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप’ नाम से रंगकर्म को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए संस्था बनायी तो प्रारम्भ में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि मोटर की वर्कशॉप होती है, राज बिसारिया तो अब थियेटर की वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं। भला थिएटर भी वर्कशॉप में तैयार की जाती है? लोगों को जो कहना था, कहते रहे। राज बिसारिया को जो रंगमंच में करना था, बिना किसी के कमैंट्स पर ध्यान दिए, निराश हुए, लगातार 55 साल से ऊपर आज भी करते आ रहे हैं। रंगमंच को देखने का उनका अपना एक नजरिया है। वे अपने रंगमंच के बारे में कहते भी कि उन्होंने किसी व्यवसाय के लिए थिएटर नहीं किया है। न महज किसी शौक के लिए नाटक करते हैं। वे अपने रंगमंच को ‘पेशेवर रंगमंच’ के रूप में कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने नाटकों के मंचन में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। किसी पक्ष को कमजोर रखने के पक्ष में नहीं रहते हैं। न इस संबंध में किसी की दया पसंद करते हैं, न अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज़ देते हैं।
राज बिसारिया को जब सन 1969 में लंदन से निमंत्रण आया तो उन्हें लगा कि 5–6 महीने का जो ये प्रशिक्षण है, यह सही मौका है रंगमंच को जानने–करीब से देखने–समझने का। अपने देश में विधिवत रंगमंच के प्रशिक्षण की जो कमी रह गयी थी, उसकी भरपायी यहां की जा सकती है। वे कहते भी हैं कि जिस तलाश में यहां आए थे, प्रशिक्षण ने उनके रंगमंच की जमीन और पुख्ता कर दी। व्यवहारिक और सैद्धान्तिक दोनों स्तर पर। यहां उन्हें दुनिया भर के महान नाटक देखने को मिला। नाटकों में भाग लेने वाले कलाकारों की तैयारी की प्रक्रिया को करीब से ऑब्जरवेशन करने का मौका मिला। और केवल अभिनय, निर्देशन ही नहीं मंच सज्जा, मुख सज्जा, आहार्य की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हासिल करने का अवसर मिला।
वहां से लौटने के बाद जो उन्होंने सीखा था, अपने रंगमंच पर उतारना शुरू कर दिया। अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के नाटकों की जो स्थिति थी, उसे सम्मान दिलाने के लिए अपनी संस्था के द्वारा जो किया सो किया, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी की जो स्थापना की, मील का पत्थर साबित हुआ। अब तक नाट्य विद्या केवल दिल्ली तक केंद्रित थी, उसे विकेन्द्रित कर के छोटे–छोटे शहरों – कस्बों के रंगमंच से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान दिला पाने में सफल रहे। कहीं न कहीं यह कह पाने में सफल रहे कि अगर नाटक को लोगों तक ले जाने की नीयत है तो केवल केंद्र में सीमित कर गढ़ बना देने से कला का उद्धार नहीं होगा। केवल एक जुबान में नाटक कर देने से रंगमंच का विकास नहीं होगा। लखनऊ की तर्ज पर हर राज्यों में नाटक के स्कूल खोले जाने की जरूरत है।

राज बिसारिया ने अपने वक्त में जो लड़ाई लड़ी थी, उसी का परिणाम इतने वर्षों के बाद आज हमें ये देखने को मिल रहा रहा है कि मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्कम, बनारस, बंगलरू, चंडीगढ़, हैदराबाद जैसे शहरों, महानगरों में नाटक की अलग–अलग विधाओं में स्पेशलाइजेशन कोर्स की पढ़ाई हो गयी है। इसके लिए राज बिसारिया को वर्तमान सत्ता से कई स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ी। उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमें चले। रंगमंच से जुड़े कई जड़ – परंपरागत रंगकर्मियों ने के तरह–तरह के आक्षेप लगा कर व्यक्तिगत स्तर इनका विरोध किया, लेकिन राज बिसारिया का जो व्यक्तित्व था, वो कभी झुका नहीं। और झुकना–दब जाना उनकी आदत में शुमार भी नहीं है। फलतः 23 सितंबर 1975 में जिस भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की, 1980 में रंगमण्डल बनाया, सन 1986 में सत्ता के हस्तक्षेप और अंदरूनी उठा–पटक से निराश कहे यह विक्षुब्ध होकर त्यागपत्र दे दिया। सरकार की विवशता या लाचारी कहिए, स्वीकार नहीं किया। नाराजगी के बावजूद सन 1989 तक कार्य करते रहे।
फिलहाल लखनऊ विश्व विद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त होकर लखनऊ, गोमतीनगर में रहते हैं। पदमश्री, यश भारती, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, आदित्य विक्रम बिरला अवार्ड, टैगोर नेशनल फ़ेलोशिप सहित कई सम्मान, पुरस्कार से सम्मानित हैं। लेकिन कोई भी पुरस्कार उनके मंचन की धार को शिथिल नहीं कर सका। सत्ता के लोग उनके घर आशीर्वाद लेने भले चले जाए, ये कभी भी राजनेता का किसी पार्टी के इर्द–गिर्द घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे। पिछले दिनों जब भारतेंदु नाट्य अकादमी के परिसर में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों संस्थान के कलाकारों को सम्मान के मौके पर राज बिसारिया की उपस्थिति को लेकर कुछ रंगकर्मियों ने सोशल मीडिया पर ऐतराज जतायी थी। उनकी प्रस्तुति ‘बेयर फुट इन एथेंस’ के हवाले से कहा गया कि सुकरात जैसे विद्रोही, सत्ता के विरोध में खड़ा होने वाले नागरिक को मंच पर इतने दमदार से प्रस्तुत करने वाले राज बिसारिया को फासीवादी व्यवस्था के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। पूरी बहस में राज बिसारिया ने कहीं कोई सफाई देने की जरूरत नहीं महसूस की।
शायद उसका कारण ये हो कि राज बिसारिया को जो भी कहना होता है, वे अपने नाटक के माध्यम से कहते हैं। जहां दूसरे निर्देशक अपने नाटकों में सत्ता के दवाब में पार्टी के एजेंडा को किसी न किसी रूप में रखते हुए दिखते हैं, पार्टी प्रतीकों को रखने से परहेज नहीं करते नजर आते हैं … वहां राज बिसारिया ‘जूलियस सीजर ‘, ‘एन्टीगनी’, ‘ बेयरफुट इन एथेंस’ जैसे नाटकों के मंचन से वर्तमान मे आनेवाली अधिनायकवादी, फासीवादी आहट को पहचान कर निरंतर खबरदार करते हुए दिखते हैं। सुकरात के माध्यम से मजबूत गणतंत्र की वकालत करते हुए दिखते हैं। आज के दौर में जिस तरह लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, कार्यपालिका के साथ – साथ देश की न्यायपालिका किस तरह सत्ता के इशारे पर संचालित हो रही है, इस संकट को राज बिसारिया ने शायद बहुत पहले पहचान लिया था। देश के कोने–कोने में उन्होंने ‘बेयरफुट इन एथेंस’ यूंहि नाटक करने के लिए नाटक नहीं किया था। करना होता तो सन 2010 में ही कर देते।

अपने 75 वें जन्मदिन पर अर्थात 2010 में ही उन्होंने बधाई देने के लिए आये सूर्य मोहन कुलश्रेष्ट को सुकरात की भूमिका करने के लिए कह दिया था। लेकिन तब नहीं किया। किया कुछ वर्षों के बाद। भारतीय लोकतंत्र में जिस तरह की राजनीतिक बदलाव आ रही थी, धर्म–राष्ट्रवाद मुख्य स्वर के रूप में उभर रहा था, कहीं न कहीं राज बिसारिया को लोकतंत्र पर कुछ हमले का अहसास होने लगा था। एक सच्चे, ईमानदार संस्कृतिकर्मी की जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वो सन 2014 के बाद के उनके नाटकों में साफ दिख रहा है। सन 2013 में ‘द सीगल’, सन 2014 में ‘द केयरटेकर’, और सन 2015 में ‘जूलियस सीजर’ जैसे राजनीतिक नाटक का मंचन महज इतेफाक नहीं, सांस्कृतिक क्षेत्र में राज बिसारिया का अपना स्टैंड है।
राज बिसारिया के रंगकर्म के लिए भाषा प्रमुख नहीं है, महत्व है वो जीवन जिसमें मानवता दिखाई दे। समानता पर जोर हो। बार–बार वो ‘पिता’ नाटक इसलिए करते हैं कि उन्हें समाज में व्याप्त पितृसत्ता कतई बर्दाश्त नहीं है। किसी नाटक में कोई निर्देशक क्या ढूंढता है, वह उसका फैसला होता है। और उसके लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है। अगर वो किसी विदेशी नाटक में मिल जाता है तो उसे केवल विदेशी होने के कारण खारिज कर देना न्याय संगत नहीं है। यह एक प्रकार की संकीर्णता है। राज बिसारिया ने कई भारतीय भाषाओं के नाटकों का हिंदी में मंचन किया है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। ‘बाकी इतिहास’,’ गिनीपिग’, ‘अंधों का हाथी’, ‘सुनो जनमेजय’, ‘अकेला जीव सदाजीव’, ‘आधे–अधूरे’, ‘बहुत बड़ा सवाल’, का नाम उनलोगों के लिए लेना जरूरी है जो उनके रंगकर्म के साथ भाषा का विवाद खड़ा कर उनका कद छोटा करना चाहते हैं।
‘सन 1979 में जब उन्होंने धर्मवीर भारती का नाटक ‘अंधा युग’ को बॉटनिकल गार्डन के प्रांगण में, पुरानी इमारत को नाटक का एक अहम हिस्सा बनाते हुए मंचन किया था तो उसकी रिपोर्ट ‘धर्मयुग’ में विस्तार से छपी थी। इस मंचन ने न केवल राज बिसारिया के निर्देशन को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाई थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के रंगमंच की समृद्धता से महानगर के रंगकर्मियों को अपना परिचय दिया था। दिवंगत रंगकर्मी जुगल किशोर जो सन 1979 में राज बिसारिया के साथ जुड़े थे, बीएनए के कार्यवाहक निदेशक भी रहे हैं, उनका कहना था कि ‘राज बिसारिया जबरदस्त शिक्षक और निर्देशक हैं। उनके नाटक टेक्स्टबुक प्रोडक्शन होते हैं। उनके नाटकों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सिर्फ लाइट या सेट डिज़ाइन करना ही नहीं, एक्टिंग और कोरियोग्राफी भी। ये उनके काम की खूबी है। व्यक्तिगत तौर पर में कह सकता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी काम मुझे आता है चाहे अभिनय का या निर्देशन का, उन्हीं की वजह से आता है।

राज बिसारिया अपने रंगकर्म को लेकर किसी चौहद्दी तक सीमित नहीं है। भले वो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनके रंगकर्म से पूरा देश वाकिफ है। जितने अधिकार से उन्होंने बीएनए के छात्रों को पढ़ाया है, उतने ही डेडिकेशन से एनएसडी के स्टूडेंट्स को। एनएसडी रंगमण्डल के साथ कई नाटकों को तैयार किया है। विशेषकर वेस्टर्न ड्रामा की तालीम देने के लिए आज भी एनएसडी के गलियारे में घूमा–फिराकर उन्हीं का नाम आता है।
राज बिसारिया के रंगकर्म को अभिजात्य का मुलम्मा लगा कर जो कमतर करने की कुचेष्टा करते हैं, उनसे ये जरूर पूछा है चाहिए कि ‘ओथेलो’, ‘किंग लियर’, ‘मैकबेथ’, ‘जूलियस सीजर’ में सामंतवाद की विसंगतियों, परस्पर अंतद्वंदों, संबंधों की विकृतियों को जो लाया है ,वो क्या रंगमंच का अभिजात्यपन है? शेक्सपियर ने सामंतों का जो डार्क पक्ष सामने लाया है, क्या भारतीय सामन्त का चेहरा इससे अलग है? ‘पिता’ में पितृसत्ता पर लगातार जिस तरह प्रहार किया गया है, वर्तमान में रंगकर्म से जुड़े कितने लोग हमारे देश की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का खंडन करते हुए दिखते हैं? आदमी का जो नितांत अकेलापन है, रोज–रोज व्यक्तिगत–पारिवारिक समस्याएं हैं, कोई अगर ‘राज’, ‘बाकी इतिहास’, ‘गिनीपिग’ जैसे नाटकों से कोई निर्देशक अभिव्यक्त करता है तो उसे अभिजात्य निर्देशक कह कर आम जन मानस से से काट देना तर्क संगत है?
मंच पर नाटक कर देने से ही कोई निर्देशक अभिजात्य नहीं हो जाता है। मंच पर नाटक करना कोई गुनाह नहीं है। नाटक कहाँ किया जा रहा है, ये प्रमुख नहीं है। नाटक में क्या किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। राज बिसारिया अपने नाटकों के माध्यम से दर्शकों के बीच क्या रख रहे हैं, इस पर विचार होना चाहिए। एक बात और जान लीजिए राज बिसारिया एक नाटक निर्देशक है। उनके नाटकों से कोई सॉल्यूशन की मांग करता है तो उनके साथ अति कर रहा है। वो कोई पोलिटिकल आदमी नहीं है, न उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जो किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या का हल निकाल दे। हो सकता है कुछ नाटक पॉलिटिकल हो, लेकिन हर नाटक पॉलिटिकल नहीं हो सकता। वैसे उन्होंने अपने बारे में कभी कहा भी नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकल डायरेक्टर है।
किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि राज बिसारिया नाट्य निर्देशक के साथ–साथ एक टीचर भी हैं। आजकल उनके हाथ में छड़ी भी रहती है, जिसका इस्तेमाल अगर चलने के लिए करते हैं तो रंगमंच की सही दिशा दिखाने के लिए भी...