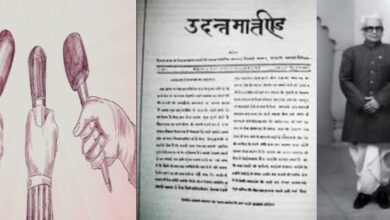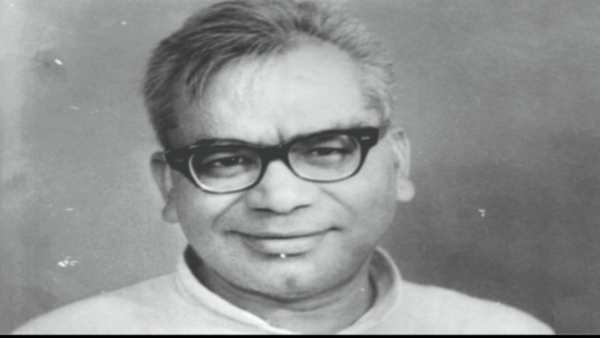व्यापक सांस्कृतिक आन्दोलन की जरूरत
आज के समय में साहित्य के सामने जो संकट है वह इस रूप में इसके पहले कभी नहीं था। दुर्भाग्यवश हिन्दी समाज और हिन्दी साहित्य का संकट बाकी भारतीय भाषाओं की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। मौजूदा समय की यह दुःखद सच्चाई है कि हिन्दी समाज का हिन्दी साहित्य से रिश्ता जीवन्त नहीं रह गया है। हिन्दी के अधिकांश पाठक वही हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लेखन से वास्ता रहा है। व्यापक हिन्दी समाज का हिन्दी के लेखकों और रचनाकारों से यह विराग हिन्दी जगत में एक तरह की सांस्कृतिक शून्यता रच रहा है। अपसंस्कृति के शोर ने रचनात्मक और विचार सम्पन्न संस्कृतिकर्म को हाशिये पर धकेल दिया है।
सच्चे संस्कृतिकर्मी सहमे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में एक उदास चुप्पी छाई हुई है। यही वजह है कि हिन्दी समाज, साहित्य और संस्कृतिकर्म के सकारात्मक प्रभाव से प्रायः वंचित है। सांस्कृतिक तौर पर अकाल पीड़ित लगभग सम्पूर्ण हिन्दी इलाका धार्मिक पाखण्ड, साम्प्रदायिक हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। इसलिए यह अकारण नहीं कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की दुर्घटना हो या आरक्षण आन्दोलन की हिंसा, बर्बर बलात्कार के बाद निर्भया की हत्या हो या बलात्कारी बाबा के अनुयायियों का घनघोर ताण्डव- ये परिघटनाएँ ही हिन्दी इलाके के चेहरे बन गए हैं।
जिस हिन्दी पट्टी में 1857 का सिपाही विद्रोह, महात्मा गाँधी का चम्पारण आन्दोलन, स्वामी सहजानन्द सरस्वती का किसान आन्दोलन और 1974 का बिहार आन्दोलन हुआ हो वहाँ संस्कृति का सूखा हो यह बात हजम नहीं होती। यहाँ तो सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक रूप से वह सक्रियता होनी चाहिए थी जो पूरे देश को आन्दोलित करे।
यह सच है कि हिन्दी में नवजागरण अपेक्षाकृत थोड़ी देर से आया, इसलिए यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ थोड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन है। 19वीं सदी की शुरुआत में राजा राम मोहन रॉय विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध कर रहे थे और 21वीं सदी के मुहाने पर हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सामाजिक सोच में हिन्दी का यह पिछड़ापन है या हिन्दुत्व की कट्टरता का हिन्दी पर प्रभाव?
जिस हिन्दी समाज से मलिक मुहम्मद जायसी, कबीर, रहीम, सूरदास और तुलसीदास जैसे रचनाकार हुए वह हिन्दी यदि आज लोक की भाषा नहीं बन पाई है तो कसूर किनका है? मराठी, बांग्ला या दक्षिण की भाषाओं के साहित्यकारों का उनके पाठकों के साथ सहोदराना और जीवन्त सम्बन्ध है, इसलिए समाज में उनका जो सम्मान है वह हिन्दी के साहित्यकारों का नहीं है। पश्चिम बंगाल के नेता और नौकरशाह वहाँ के सांस्कृतिक आयोजनों में आम आदमी की तरह सरीक होते हैं। बिहार-उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों की तो छोडि़ए मुखिया भी कारों के काफिले के बगैर नहीं चलता। अपने अनुयायियों और अनुचरों के बीच वह प्रायः महाराजा की तरह ऐंठा और अकड़ा (इतिहास में कुछ राजा कभी विनम्र भी हुए होंगे) रहता है।
वैभव का अश्लील प्रदर्शन हिन्दी इलाके में समारोह पूर्वक जिस बेशरमी से होता है, वैसा अन्यत्र कम होता है। दिखावे की भूख रोटी की भूख से ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए इस दिखावे की भूख को मिटाने के लिए अनाप-शनाप तरीके से पैसे जुटाने होते हैं। भ्रष्टाचार और काले धन की कमाई की शुरूआत यहीं से होती है। हिन्दी पट्टी के साहित्यकारों (गिनती के कुछ अपवादों को छोड़कर) में प्रदर्शनप्रियता और पुरस्कार प्राप्ति की आतुर आकांक्षा ने भी उन्हें पाठकोन्मुख नहीं रहने दिया है। उनकी कथनी (लेखनी) और करनी का फर्क लगातार बढ़ता रहा है और उनके विचार एवं व्यक्तित्व के बीच का अन्तर्द्वन्द्व पाठकों के बीच उजागर होते रहे हैं। ऐसे में पाठक उनको ‘इंटरटेनर’ मानता है अपना सांस्कृतिक नायक नहीं। इसलिए दक्षिण और पूरब के राज्यों में या पश्चिम बंगाल में कई प्रतिष्ठित साहित्यकार राजनीति में सक्रिय मिल जाएँगे, मुख्यमन्त्री का पद भी वे वे बखूबी सम्हालते मिलेंगे_ लेकिन हिन्दी पट्टी के साहित्यकारों की राजनीति ज्यादा से ज्यादा लेखक संगठनों तक ही सीमित रहती है।
एक समय था जब जवाहर लाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया जैसे लोग राजनीति में सक्रिय थे, तब के साहित्य पर उनकी राजनीति का प्रभाव स्पष्ट दिख जाता था। उनके विचारों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है लेकिन उनके महत्त्व को खारिज करना मुश्किल है। साहित्य के कई अध्येता और शोधार्थी मिल जाएँगे जिन्होंने इन विषयों पर शोध किया होगा, क्या आज की हिन्दी पट्टी की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके आचरण और विचार का प्रभाव साहित्य पर हो? निःसंदेह नहीं।
यदि राजनीति अपनी जिम्मेवारी से विमुख हो गयी है तो क्या साहित्य को भी चुप रहना चाहिए? हिन्दी पट्टी में व्याप्त सांस्कृतिक संकट के खिलाफ क्या साहित्य का एक संयुक्त मोर्चा नहीं बन सकता? सभी लेखक संगठन मिलकर एक कार्यक्रम तय करे और हिन्दी पट्टी के दसों राज्यों के सांसदों और विधायकों से संवाद करे कि हिन्दी पट्टी में जातिवाद को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक आन्दोलन की रूपरेखा क्या हो सकती है और इस आन्दोलन में आपकी भूमिका क्या होगी? बाद में सांसद और विधायक इस संवाद को पंचायत और जिला स्तर के जन प्रतिनिधियों तक भी फैलाकर एक व्यापक विमर्श की परियोजना बना सकते हैं जिसमें संस्कृतिकर्म और पढ़ने की संस्कृति और लेखक-पाठक सम्बन्ध पर भी विचार हो सकता है। पढ़ने में यह सुझाव मासूम कल्पना की तरह लग सकता है लेकिन क्या ठिकाना किसी को एक सांस्कृतिक आन्दोलन का बीज इसमें दिखाई पड़ जाए।
.