
पूँजी के भंवर में मनुष्यता की संभावनाओं का अन्त
प्रत्येक आदमी संभावनाओं का समुच्चय है। और ये संभावनाएं उसके भीतर की बहुआयामिकता से निकलती है। उसकी बहुआयामिकता उसकी प्रकृति के साथ-साथ उसके जीवन की सार्थकता भी है। यूँ समझे कि हर आदमी अपने आप में एक छोटा-मोटा लियोनार्दो द विन्ची होता है। वह रचना चाहता है, कुछ गढ़ना चाहता है जिससे आनेवाली पीढियां लाभान्वित हो सके, लेकिन बदलते हुए समय और समाज में आदमी के अन्दर का विन्ची मरता जा रहा है उसकी रचनात्मकता ख़तम होती जा रही है। जीवन अब उबड़-खाबड़ धरातल भी नहीं रह गया है, जहाँ आप थकने के बाद आराम कर सकें और फिर आगे की यात्रा जारी रख सकें, बल्कि अब यह दहाड़ मारती नदियों पर निरन्तर तैरने का प्रयास मात्र है, आपने तैरना बन्द किया नहीं कि आपकी यात्रा “महायात्रा” बनी।
भला जीवन की इस डूबने वाली संस्कृति में आदमी के अन्दर का विन्ची कैसे बचा रह सकता है! किसी तरह अगर उसने सौन्दर्य को उकेड़ा भी तो उसमें मोनोलिसा की मुस्कराहट नहीं आ सकती। और अगर कुछ गाया भी तो बीथोवन का संगीत नहीं आ सकता। विन्ची होने के लिए, बीथोवन या पिकासो होने के लिए समय चाहिए, जबकि आज के समय की विडंबना है कि इसमें न तो समय है और न इसकी स्वीकृति। इसलिए शायद अब विन्ची नहीं होते, पिकासो या बीथोवन नहीं होते, अगर होते भी होंगे तो होते ही मर जाते होंगे।
त्रासदी
एमानुएल कैसेल ने ऐसे ही समाज के लिए कहा- ‘समय के बिना समय’। समय को अपने अस्तित्व के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। समय को अनुभव करने के लिए समय नहीं है। यह बस बीता जा रहा है; इस बीतने में एक त्रासदी है, यह त्रासदी ऐतिहासिक है, इससे पहले कभी समय ऐसे नहीं बीता। उसका अतीत और भविष्य के साथ एक संतुलन था, अब वह संतुलन नहीं रहा। अतीत मिटा दिया गया है और भविष्य मिटने के कगार पर है-बस समय है कि बीता जा रहा है। समयहीनता ने एलिनेसन को जन्म दिया, एक अलगाव को जन्म दिया। यह अलगाव मार्क्स के औधोगिक समाज के एलीनेशन से अधिक क्रूर है। उसमे अलगाव को अनुभव किया जा सकता था, अब उस अलगाव का बोध नहीं रहा, क्योंकि समय का अभाव है।
आदमी समाज से तो कटा ही अब अपने आप से कटा जा रहा है। हम कौन हैं? हम क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, ये सभी यक्ष प्रश्न हैं, और यक्ष प्रश्न ही रहेंगे। ऐसे प्रश्न पर विचारने का समय नहीं। ये प्रश्न सार्थक हैं या नहीं यह प्रश्न भी निरर्थक है। रूककर सोचेंगे तो आपकी आगे की यात्रा रोक दी जायेगी। दौड़ते रहना है, और इस दौड़ का कोई अन्त नहीं, क्योंकि समय नहीं। आपकी दिशा तय कर दी गयी है, निर्धारित दिशा से बाहर सोचना नहीं, विचारना नहीं। भीतर के अन्दर की जो मानवीय संभावनाएं हैं उनकी जरुरत नहीं, मशीनी निश्चिताओं से तय होना ही नियति है। 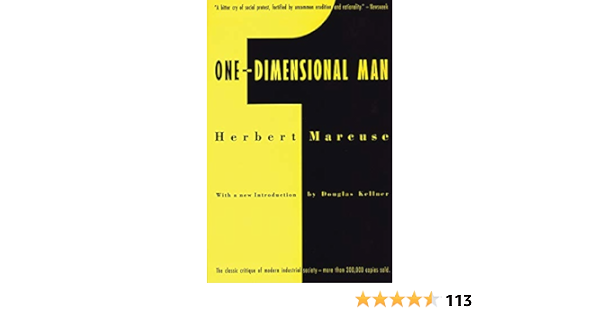
हर्बर्ट मार्कुज ने ऐसे ही समाज और व्यक्ति के लिए ‘वन डायमेंशनल मैन’ या ‘एकांगी मानव’ की अवधारणा दी। आदमी अपने अन्दर के अनगिनत मानवीय पक्षों को कुचल चुका है। पूँजी की अधिकता और उसके प्रचंड प्रभाव ने आदमी को बस रोजी-रोटी की जुगार में ही झोंक दिया, उसने अपने अन्दर की संभावनाओं से एक तरह से समझौता सा कर लिया। वह जीता है केवल जीवित रहने के लिए। उसके जीवन और मृत्यु के बीच न तो कोई अन्तर है और न इसकी कोई सार्थकता।
पूँजी की दुनिया का हर सफल दिखता आदमी भी भीतर की असफलता के साथ बेचैन भटक रहा है। वह कवि हो सकता था, वह लेखक हो सकता था, वह गायक हो सकता था, वह दुनिया को घूम सकता था, और अपने पसन्द की किताबों को पढ़ सकता था, खेल सकता था, अपने घर पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ गप्पें कर सकता था, नदियों और पहाड़ों के बीच जाकर अनन्त सृष्टि से संवाद कर सकता था, और न जाने जीवन के और कितने रंगों को वह देख सकता था, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता! भागमभाग वाली दिनचर्या में कोई भी गति जीवंत नहीं। दौड़ती हुई दुनिया में सबकुछ रुका-रुका सा है।
हम ‘गोल्डन-स्ट्रैटजैकेट’ या ‘स्वर्ण-वस्त्र’ में कैद हैं, हिल-डुल नहीं सकते, चल-फिर नहीं सकते, शरीर अकड़ा जा रहा है, लेकिन इस जैकेट को कैसे उतारें जैकेट सोने का है।अब घूमना बन्द कर दिया है, टहलना बन्द कर दिया है। ऐसे में मानवता के भीतर की सामाजिकता भीतर ही दम तोड़ रही है। कहिं कोई जगह नहीं जहाँ आपके मन-विचार ठहर कर कुछ रच सके, कुछ गढ़ सके। स्थायित्व का अन्त हो चुका है, चीजें बनती हैं और बनते ही बिखड़ने लगती है और फिर मिट जाती है। कार्ल पोल्यानी इसलिए लिखते हैं कि पहले समाज के किनारे पर बाजार हुआ करता था, अब बाजार ही बाजार है उसमे समाज कहिं-कहिं मात्र सांसें ले रहा है। यह प्राणहीन मनुष्यता का समय है।
भविष्य
तथ्य है कि दुनिया के तेज आर्थिक विकास के मॉडल ने एक ‘तीसरी-दुनिया’ का निर्माण किया जो भूख और बीमारी से आज भी जूझ रहा है। यह भूखमरी इसका इतिहास नहीं था, धरोहर नहीं था। यह उनपर थोपी गयी पहचान है। वे अपनी ज्ञान-परम्परा और अर्थतंत्र को खोकर अब एक बेजान भू-खंड की तरह रह गए हैं जहाँ पश्चिमी देशों के इशारे पर उनका आर्थिक दोहन हो रहा है, परन्तु प्रश्न है कि हमने अतीत की गलतियों से जमीनी स्तर पर कुछ सीखा भी या नहीं! शायद नहीं, क्योंकि सरकारी आर्थिक नीतियाँ जिन रास्तों पर चल रही है उसमे सतत विकास, समावेशी विकास की सम्भावना नहीं दिख रही। ऐसा लगता है ऐतिहासिक गलतियों को दुहराने की एक विशाल परियोजना तैयार की जा रही है।
स्मार्ट-सिटिज परियोजना हो, या फिर बुलेट ट्रेनों को चलाने की पहल, या फिर शहर केन्द्रित नीतियाँ या फिर कॉरपोरेट के हितों को ध्यान में रखकर बनाये गए कानून, या फिर बाजार को प्रदान की गयी असीम शक्तियां, लेबर कानून, नया कृषक बिल इन सबों के सहारे एक समावेशी और स्वस्थ समाज या राष्ट्र का निर्माण संभव होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। इस नव-उदार वादी मॉडल में उदारता केवल बाजारू शक्तियों के प्रति है, आम आदमी नीतिगत अनुदारता का शिकार है। विकास का जो मूलभूत सिधांत है वह ‘ट्रिकल-डाउन-थ्योरी’ पर टिका है। मतलब धनकुबेरों के और अधिक धनी होने पर निर्धनों की निर्धनता घटेगी। जबकि इससे क्या मिला वो दुनिया में चारों तरफ फैली भूखमरी और गरीबी बता रही।
एक पश्चिमी विद्वान मिलानोविक ने वर्ष 2009 के अपने एक अध्ययन में यह दिखाया किया किकैसे वर्ष 1820 से 2002 के बीच यह विषमता घटने के बजाए बढती चली गयी। इस त्रासदी का अन्तिम स्वरूप, निर्धनता और विषमता के अतिरिक्त और भी अधिक व्यापक है; इसने समाज और व्यक्ति के भीतर की अनगिनत संभावनाओं और उसके मानवीय पक्षों का भी संहार कर दिया। हो सकता है हम निर्धनता घटा दें, हो सकता है हम भूखमरी मिटा दें, लेकिन मनुष्यता के मन और विचारों के भूख का क्या! उसके लिए क्या जो रचना चाहता है, उसके लिए क्या जो जीना चाहता है अपने अन्दर के विन्ची, पिकासो और बीथोवन के साथ! क्या यह पूँजी के भंवर में मानवीय संभावनाओं का अन्त नहीं? मनुष्यता की सृजनशीलता सुनियोजित तरीके से मार दी गयी है और यह मौत अन्ततः मानवता की ही है!
.











