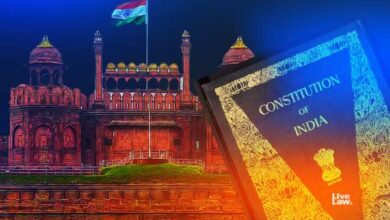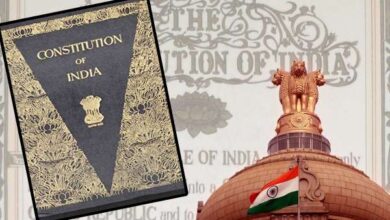विविधता में एकता का नाम है भारत
भारत एक बहुलतावादी देश है। जिसके कारण यहाँ बहुजातीय, बहुसांस्कृति और बहुधार्मिक मान्यताओं में विश्वास करने वाले लोग बसते हैं। यह अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल है। भारत का सम्बन्ध किसी एक धर्म से न होकर अनेक धर्मों से है। अतः कहा जा सकता है कि भारत किसी एक धर्म की अस्मिता या पहचान नहीं है अपितु वह तो सभी धर्मों का अधिवास है। भारत वह है जो ऊंच-नीच की भावना से ऊपर उठकर सभी को प्रेम भाव से अपने भीतर आत्मसात करता है।
भारतीय होने का भाव सभी धर्मों की मूल चेतना है और यही चेतना हमारे गौरव का आधार भी है। भारतीय होने के लिए किसी धर्म रूपी बैसाखी की नहीं अपितु मानवतावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि भारतीयता का कोई धर्म नहीं होता। भारतीयता तो मनुष्यता का पर्याय शब्द है। जो सभी के प्रति समान दृष्टि रखती है। जीवन को शास्त्रों द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो अज्ञेय के अनुसार हम सिर्फ टाईप बनाते हैं। जहाँ व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और उसका अस्तित्व बोझिल सिद्धांतों तले दब जाता है। जब हम विभिन्न निर्णयों में से अपने विवेक से किसी एक का चयन करते हैं तब हम अपने आप को गढ़ रहे होते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यकितत्व उसके द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही बनता है।
आज साम्प्रदायिकता, स्वार्थपरता, अवसरवादिता, हृदयहीनता, घृणा, द्वेष और हिंसा तत्कालीन समय का यथार्थ है। जो अच्छे भले समाज को खोखला कर देने के लिए काफी है। आज सहानुभूति, साम्प्रदायिक सहिष्णुता, दया, करुणा जैसे मूल्य इतने हल्के हो गए हैं कि मनुष्य इन तक नहीं पहुंच पाता। जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सोचने की क्षमता उसमें समाप्त होती जा रही है। जो कि किसी भी देश के विकास को अवरुद्ध कर सकता है। धर्म एक वाह्य आवरण बनकर रह गया है। उसके मूल अर्थ को भुला दिया गया है। भीष्म साहनी के अनुसार-“धर्म में आस्था रखने वाले लोग भी सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ हैं जो धर्म के आलोक में हर इन्सान को अपना सगा-सम्बन्धी समझते हैं, प्रेम भाव की लौं उनके जे़हन को रौशन किए रहती है। पर कुछ हैं जिनका धर्म अपने भाईयों की एकजुटता, विधर्मियों से लोहा लेने की उनकी क्षमता पर केन्द्रित होता है, यहाँ तक कि किसी भी विधर्मी का खून बहाना उनके लिए सबाब का काम होता है।” (नीलू नीलिमा निलोफर- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, पहला संस्करण-2000)
धर्म की जब-जब गलत व्याख्या प्रस्तुत की गयी है तब-तब उसने केवल मनुष्यता को नुकसान ही पहुंचाया है। प्राचीन काल में धर्म तय करता था कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और उसी के अनुसार वह अपना जीवन जीने का प्रयास करता था किन्तु अब समय बदल चुका है, अब वो परिस्थितियां नहीं रहीं हैं। अब मनुष्य को धर्म के अनुसार नहीं अपितु धर्म को मनुष्य के अनुसार ढालना होगा। अब मनुष्य स्वयं इस बात का निश्चय करेगा कि धर्म का रूप कैसा होना चाहिए। अब धर्म के लिए मनुष्य नहीं, बल्कि मनुष्य के लिए धर्म होना चाहिए। उसकी परिभाषा मानवहितों की संगति में गढ़ने की आवश्यकता है। 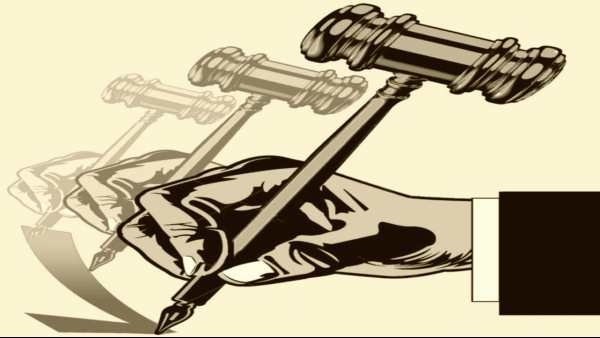
जिस प्रकार समय के साथ-साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है ठीक उसी प्रकार धार्मिक विधि-विधानों और नियमों में भी समय के अनुसार संशोधन होना चाहिए। समाज सुधार के साथ-साथ धर्म सुधार की जरूरत समय की मांग है। धर्म की मध्यकालीन सोच ही देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है। यह सोच ही हिंसा को जन्म देती है। धर्म को मानने वाले एक रेखीय होते जा रहे हैं, जिस दिन वे धर्म के वास्तविक मूल को जानने लगेंगे तभी वह मनुष्य के हित के साथ-साथ देश के विकास में भी अपना सकारात्मक योगदान देने में समर्थ हो पाएंगे।
साम्प्रदायिकता का जहर जिस समाज में घुल जाता है वह समाज अपने साथ-साथ देश को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले अक्सर संस्कृति की दुहाई देते हैं। प्रेमचंद ने अपने लेख ‘साम्प्रदायिकता और संस्कृति’(1934) में कहा है कि- “साम्प्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है उसे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है। इसलिए वह गधे की भांति, जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर रौब जमाता फिरता था। संस्कृति का खोल ओढ़कर आती है। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति मगर आज हम भी हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं।” (Krantiswar.blogspot.com)
सही और गलत का पैमाने का तो पता नहीं किन्तु भारतीय मानस के अवचेतन मन में पड़ी हुई एक दूसरे के प्रति नफरत रूपी नागिन आज फन फैलाए खड़ी है। न जाने कितने रिश्तों को यह डसेगी। वर्तमान परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप युवा मानस दो भागों में विभाजित हो चुका है। जो इस तरफ खड़े हैं उनके अनुसार दूसरी तरफ वाले तमाम लोग इन्सानियत के दुश्मन ही नहीं आंतकवादियों को पनाह देने वाले भी हैं। आज भारत की युवा पीढ़ी कुछ अराजकता फैलाने वाले लोगों की बातों में आकर उनके समर्थन और विरोध के चक्कर में अपने भाई-चारे का गला घोंट रहें हैं। इसका मूल कारण फेलता हुआ साम्प्रदायिक जहर है।
यह भी पढ़ें – हिन्दी में नवयुग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र
जिस समय में हम रह रहे हैं वह साम्प्रदायिकता के उत्थान का समय नही अपितु आर्थिक उत्थान का समय है। आज हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझा सकें। धर्म के नाम पर किए गए पाखण्ड द्वारा देश का उत्थान संभव नहीं है। प्रेमचंद जी ने अपने लेख ‘साम्प्रदायिकता और संस्कृति’ में इसी पर प्रकाश डालते हुए कहा है- “यह जमाना साम्प्रदायिक अभ्युदय का नहीं है यह आर्थिक युग है और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपने आर्थिक समस्याओं को हल कर सके जिससे यह अन्धविश्वास और यह धर्म के नाम पर किया गया पाखण्ड या नीति के नाम पर गरीबों को लुभाने की कथा मिटाई जा सके।”(Krantiswar.blogspot.com)
भारतीय परम्परा संवाद की परम्परा रही है। यहाँ असहमतियों को भी स्वीकारा जाता है। मनीषियों ने कहा भी है कि अहसमतियों से नए विचार का रास्ता खुलता है। भारतीय वाड्मय कहता है- “वादे वादे जयते तत्व-बोध:।” किन्तु अब हमारे समाज में असहमतियों की जगह नहीं है। उन्हें अब दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। असहमतियों से नवोन्मेष होता है किन्तु अब उसे कुचला जा रहा है। नाराज हुए बिना असहमत होने की प्रवृत्ति कहीं ओझल हो चली है। भावनात्मक रूप से आहत व्यक्ति हिंसा का रूप धारण कर लेता है और अपने से विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति को कुचल डालने का प्रयास करता है। ऐसी मानसिकता का पनपना देश के लिए अहितकारी साबित होता है। क्योंकि इसकी मूल वृत्ति हिंसा द्वारा संचालित होती है। हिंसा कोई भी करे वह गलत होती है। हिंसा को कभी भी, किसी भी तर्क द्वारा सही साबित करने का प्रयास ही निर्थक है। किन्तु जो लोग विचारधारा का पट्टा अपने गले में बांधते हैं। वे विपरीत विचारधारा को समाप्त करने के प्रयास की प्रक्रिया में की गयी हिंसा को कई मायनों में सही ठहराते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी विचारधारा की स्थापना कर अपने वर्चस्व को कायम रखना होता है। 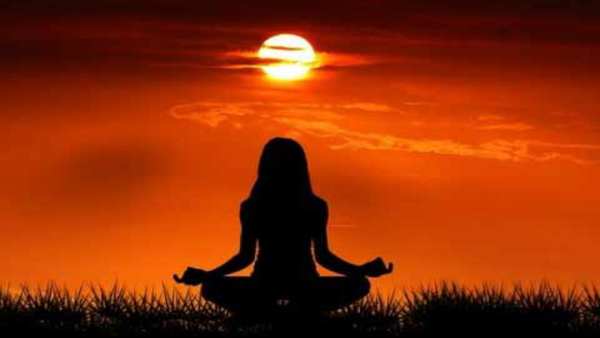
मनुष्य को लचीला होना चाहिए और उसे वक्त के साथ चलना चाहिए। कुछ भी शाश्वत नहीं है। कट्टर होना जड़ होना होता है। जो जड़ हो गया वह रुक गया, जो रुक गया वो मर गया। जीवन तो बहती धारा का प्रतीक है। उसे भला कैसे जड़ किया जा सकता है। विचारधारा अपनी हो या दूसरे की उसे सदैव सकारात्मक आलोचना की कसौटियों पर कसना चाहिए। वक्त के अनुसार उसमें बदलाव भी करना चाहिए। जहाँ से जो भी अच्छा मिले उसे ग्रहण कर अपनी ज्ञान राशि को समृद्ध करना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता ही एक स्वस्थ्य समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि देश वहाँ के लोगों से बनता है। जैसी लोगो की मानसिकता होगी देश भी वैसा ही होगा। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से असहमत होने का पूरा अधिकार है। और इस तथ्य को स्वीकारना चाहिए।
भावनात्मक रूप से जो व्यक्ति परिपक्व होगा वही असहमतियों को स्वीकार करने की क्षमता रख पाएगा। मतभिन्नता के कारण बोखला जाना और अपशब्दों का प्रोयग करने वाला व्यक्ति अपने साथ-साथ, अपने समाज का और अपने देश का भी नुकसान करता है। इसीलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नही करना चाहिए जिससे कि रिश्तों को संचालित करने वाली सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएं। जिस समय में हम जीते हैं वही हमारे लिए सत्य होता है। उस समय में जीते हुए हम जो भी करते हैं वही सही लगता है। किन्तु उसकी सार्थकता का मुल्यांकन हम उस समय नहीं कर सकते क्योंकि उस समय की मानसिकता परिस्थितियों के अधीन होती है।
किन्तु कुछ समय के उपरांत जब परिस्थितियां बदलती हैं और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब उसका मुल्यांकन करना सरल होता है। जब एक परिवार में झगड़ा होता है तो झगड़े के दौरान शब्दों की मर्यादा का पालन करना मुश्किल होता है और हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। शायद कुछ ऐसा भी जो अत्यंत कड़वा हो। किन्तु यदि शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन होता है तो वे शब्द हमेशा के लिए मानस पटल पर छाप छोड़ जाते हैं। झगड़ा समाप्त हो जाता है किन्तु रिश्तों में खटास आ जाती है। इसीलिए किसी को सिर्फ उतना ही भला-बुरा कहना चाहिए जिससे कि रिश्तों में एक साथ रहने की गुंजाइश बनी रहे।
हमारा भारत देश भी एक परिवार है और इस परिवार में वैचारिक मतभेद को मनभेद नहीं बनने देना चाहिए। पूरी दुनिया में कोरोना नामक महामारी ने तबाही मचा रखी है। किन्तु सकारात्मक पक्ष पर बात करें तो इस काल ने हमें खुद को जानने का एक सुनहरा मोका भी दिया है। न जाने इस बाजारवाद में हमनें खुद को कहाँ छोड़ दिया है। बेसक आज हम एक-दूसरे से शारीरिक रूप से दूरियां बना रहे हैं और इस बीमारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु हमनें अपने आप से कितनी दूरी बना ली है कभी सोचा है? आज हम खुद को कितना जानते हैं। जिन चीजों को लेकर हम भाषण देते हैं, उन्हें हम खुद व्यवहार में कितना उतारते हैं, या फिर हमारी सोच, हमारे विचार सिर्फ दूसरों के लिए हैं? क्या वह स्वयं के लिए नहीं हैं? कोरोना ने इस रफ्तार भरी जिन्दगी में जो ब्रेक लगया है, यह खुद को रोककर, खुद की ही विचारधारा पर सोचने का एक सुअवसर है। क्योंकि कोई भी विचार अपने आप में पूर्ण नहीं होता उसे समय के साथ चलना पड़ता है, समय की मांग को पूरा करना पड़ता है, यदि ऐसा करने में वह असमर्थ है तो उसे वर्तमान समय की परिस्थितियों के साथ उसका मूल्यांकन कर उसमें उचित परिर्वतन करना चाहिए।
यह भी पढ़ें – भारतीय तत्व–चिन्तन का प्राणतत्व : पंथी होकर भी पंथ–निरपेक्ष!
विचारधारा की आँखों पर पट्टी बांध कर सिर्फ उसका अंधानुकरण करने वाले लोग समाज में सिर्फ अराजकता को जन्म देते हैं। वक्त की नब्ज़ को पहचान कर अपनी सोच और अपने विचार का इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में हम कितने भी अलग-अलग क्यों न हों किन्तु विपरीत परिस्थितियों में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि वाद-विवाद का भी एक वक्त होता है। जिसमें सभी को अपनी बात रखने का मोक मिलता है और मिलना भी चाहिए। यदि हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी एकता को त्याग कर खण्ड-खण्ड में बटकर एक दूसरे को कोसकर, एक दूसरे को नीचा दिखाकर, दोषारोपण करेंगे तो हम हार जाएंगे। अच्छा काम किसी के द्वारा भी किया जाए, वह किसी भी विचारधारा का हो, किसी जाति, समुदाय या धर्म से सम्बन्ध रखता हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज हम विचाधाराओं के ऐसे खूंटे में बंधे हैं जिसे तोड़ पाना कठिन है, जिसके चलते हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में न स्वीकार कर उसे धर्म और जाति के रूप में स्वीकार करते हैं।
उपयोगितावादी दृष्टिकोण समाज के लिए क्या उपयोगी है इसके साथ-साथ हमारे लिए कौन और कितना उपयोगी है यह भी तय करने लगा है। उपयोगिता इतनी ज्यादा हावी है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी लोग अपनी विचारधारा के समर्थन और दूसरे के विरोध में अनगिनत तथ्य जुटाने में लगे हुए हैं। यह वक्त क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता, वर्गीयता, आदि मनुष्य को संकीर्ण बनाने वाली तमाम चीजों को नकारने का है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इनके प्रति अपनी गौरव भावना को दबा दिया जाए किन्तु कभी-कभी ऐसा दौर आता है जब इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर मनुष्यता के धरातल पर हमें एक-दूसरे से जुड़ना पड़ता है। यह वही समय है जहाँ हमें एक होना है। भारत देश की ताकत एकता में है और इस एकता का निर्माण एक रेखीय न होकर बहुरेखीय है। यह विविधता से बनी हुई एकता है।
इतिहास गवाह है उच्च पद पर आसीन लोगों ने जब भी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने हेतु फैसले लिए हैं, जो भी बयानबाजियां की हैं उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही भुगतना पड़ा है। कारण जनता का भेड़ियाधसान चाल चलना। भारतेंदु जी ने तो भारतीयों को रेल की गाड़ी कहा है जो बिना इंजन नहीं चल सकती। आज भारत के पास फर्स्ट क्लास इंजन है लेकिन चलाने वाले को यही नहीं पता कि रेल कहाँ ले जानी है। ज्यादातर चालक उसे अपनी इच्छा अनुसार नफरत के स्टेशन पर छोड़ देते हैं। किन्तु भारतवासियों को नफरत के स्टेशन पर उतरकर कैसे प्रेम के फूल खिलाने हैं भलि-भांति आता है। भारत का हृदय अत्यंत विशाल है। इतिहास गवाह है भारत ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया और यही इसकी महानता है।
उपसंहार
भारत का अपना एक व्यक्तित्व है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण विविधता से हुआ है। विविधता का होना इसके व्यक्तित्व की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें धार्मिक विद्वैष को भुलाकर एक ऐसे देश का निर्माण करना है। जिसके मूल में प्रेम हो, जहाँ हर व्यक्ति दूसरे के प्रति सद्भाव रखता हो, जहाँ मनुष्य की पहचान उसके द्वारा किए गए कार्यों से तय होती हो, जहाँ मनुष्य की श्रैष्ठता का आधार उसके गुण हों।
हम भारतवासियों को एक ऐसा धर्म बनाना है। जिसके केंद्र में मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति, आदि सभी का हित हो, कहीं कोई बटवारा नहीं, सब एक दूसरे से प्रेम भाव से जुड़ें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसा कोई बंधन न हो जो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति का दमन करता हो, जहाँ आस्था और विश्वास मनुष्य की भलाई पर आश्रित हों। हमें वैचारिक मतभेद से ऊपर उठकर मनुष्यता के धरातल पर जुड़ना होगा। तभी हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे। जो विकास का ही नहीं प्रेम और सद्भाव का भी पर्यावाची बनकर उभरेगा। भारतीय समाज में हृदय पक्ष सदैव मजबूत रहा है और धर्म का सम्बन्ध हृदय से होता है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होता है। जिस युग में हम हैं उसमें हमें अपना निर्णय तार्किक विश्लेषणों के आधार पर ही लेना चाहिए। मनुष्य को अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को समझने की जरूरत है।
.