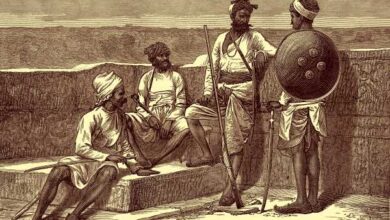किसानों की संघर्ष-गाथा
पहले झगड़ा अमर फल का हुआ करता था। अब अमरत्व का समूचा रायता फैल गया है। अमरत्व के खाते में सात ही लोग हैं। आठवें स्थान के लिए होड़ लगी है। पता नहीं, कौन बाजी मार ले। दुनिया में तानाशाह इतिहास में एक ही हुआ है। दूसरे स्थान के लिए जुझम-जुज्झा मची है। ऐसे बलशालियों के रहमो करम पर दुनिया टँगी रहती है। राग अघोर भैरव गाती है और तन्त्र-साधना करती है। शायद गंगा इसलिए ही बनी है कि लोग वहाँ डुबकी लगाएँ और तानाशाही मनोविज्ञान का जलबा प्राप्त करें। कहते हैं गंगा-स्नान में बड़े पैमाने पर फल छुपे रहते हैं। कब किसका भाग्य निकल भागे। भाग्य का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी तो तरह-तरह के साधु-संत, बाबा तरह-तरह के करतब दिखाने में भिड़े हैं। कोई साँटी सड़सड़ाता है; कोई लात मारकर ठीकठाक करता है। लोक-कल्याण की बाँसुरी से पता नहीं, कौन-कौन से स्वर झरने लगें।
एक ओर किसान अपने हकों के लिए काले कानूनों की वापसी के लिए निरन्तर संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी ओर मंदिर-निर्माण के लिए चंदा उगाही हो रही है। किसानों का एजेंडा लोहा लेने का है और दूसरा एजेंडा है हिंदुत्व के नाम पर धूम धड़ाके का। जिन्हें धूम धड़ाका चाहिए, वे उगाही की दुनिया में मस्त हैं। खेत बंजर हो जाएँ; किसान आत्महत्याओं की खोह में बिला जाएँ; उनका सर्वनाश हो जाए; लेकिन भव्य मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। किसानों की कितनी लाशें बिछ चुकी हैं, कितनी बिछेंगी, इसका कोई हिसाब नहीं। यह तो प्रभु-लीला है। लीलाएँ कई तरह से खुलती हैं और कई रूपों में प्रकट होती हैं। लीलाएँ जारी रहेंगी। यह दौर वीभत्स और क्रूर भर नहीं है; बल्कि अत्यंत शर्मनाक भी है। जोधन कह रहे थे कि वह शर्मनाक होने की सभी सीमाओं को लाँघ चुका है। हर चीज़ को लाँघना सत्ता का रोज़-रोज़ का स्थायी खेल है। देखिए आगे क्या-क्या लाँघे जाने की परम प्रतापी मुकम्मल योजनाएँ हैं।
हम लोहार भी नहीं बन सके; जो लोहे को पिघला-पिघलाकर कई तरह के औजार गढ़ता है। उसमें खुरपी, फावड़ा, गैंती, चिमटा, तवा, हँसिया, बाँका, बरछा, हल के फाल, बख्खर, तमाम तरह के चक्के और अन्य चीजें आती हैं। कहते हैं, हमारा प्रेम लोहा जैसा होना चाहिए और हमारी राष्ट्रभक्ति फ़ौलाद जैसी। हमें किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। वह जमाना गया जब स्वर्ग-नरक के टिकट बाँटें जाते थे। अब तो मूर्खताओं, लंपटताओं, झूठ और झाँसे की इबारत लिखी जा रही है। किसानों की रगों में में पानी नहीं, ख़ून बह रहा है। इस समय पाखण्ड-लीला के रेले पर रेलों का अखण्ड जाप चल रहा है। विज्ञान-प्रविधि को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है या ऐसी-तैसी कर दी गई है। इस देश का किसान पढ़ना-लिखना और अपने हकों के लिए लड़ना भी जानता है। वह किसी के रहमो करम पर जीवित नहीं है; बल्कि उसकी शह पर जीवित है व्यवस्था। वह अन्न उपजाता है और हर जगह पहुँचाता है।

आज पूरा देश मंडी बना दिया गया है। सभी कुछ बेंचा जा रहा है। देश के नागरिकों को मूर्ख बनाया जा रहा है। देश का किसान, युवा पीढ़ी, विद्यार्थी हमारी जिन्दगी की मूल चिंताओं में नहीं हैं; जबकि वह इस देश की मुख्य धाराओं में है। मंदिर के खाते में और चंदा उगाही हमारी मूल चिंता में हो गया है। सत्ता जोड़-जुगाड़ और तुकबन्दी में जीवन लगा देती है तब सामान्य आदमी आशाओं से भी खारिज़ कर दिया जाता है। हमारे स्वाभाविक पग विच्छृंखलित कर दिए जाते हैं। क्या कोई हवाओं से चल सकता है। हमें अतीत की खोहो में फँसा दिया गया है तथा वर्तमान को लहूलुहान और कलंकित कर दिया गया है; ताकि हम भविष्य के न तो सपने देखें और न भविष्य के लिए साँस ले सकें। वसंत केवल नए-नए पल्लवों का फूटना, कलियों का मुस्कुराना भर नहीं है; बल्कि वसंत हमारे जीवन की पहचान भी है और पच्चीकारी भी।
किसान के पास जो है, जितना है, वही तो उसका आसरा है। वह किसी ब्याज के सहारे हाथ-पर-हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। वह अपने ही सामर्थ्य पर, अपने ही नाखूनों से खोदेगा खनेगा, पसीना ओंटेगा, तभी उसे कुछ मिलेगा। लोग समझते हैं या सत्ता द्वारा समझाए जाते हैं कि ये फालतू लोग हैं; ये अपनी वास्तविकता और हिम्मत से निकले लोग हैं, कोई किराए के टट्टू नहीं। ये अपनी भाषा और व्याकरण रचने वाले लोग हैं। इसलिए इनकी धार भी है अपना इलाका भी। आख़िर कब तक उनकी परीक्षा ली जाएगी; कब तक झूठ की भट्टी से उनकी सच्चाई को खत्म करने की खतरनाक नेटवर्किंग की कोशिश की जाएगी। क्या अच्छे दिन और उनको ठगने का धंधा जारी रहेगा। लोग-बाग इधर लोहे की कीमत समझना भूल गये हैं। 
बड़ी मुश्किलों के साथ लोहा फ़ौलाद बनकर किसानों के रूप में ढला है। पुरखे बताते हैं कि स्वाधीनता-आन्दोलन में किसानों ने अंग्रेज़ी हुकूमत से लोहा लिया था और उनकी हेकड़ी ख़त्म की थी। किसान कभी भी तमगे के भूखे नहीं रहे। उनके खेत, खलिहान, धरती और फसलें ही उनका असली सोना है और उन्हीं से दु:ख-सुख में उनका काम चलता है। वे इसी लोहे की ताक़त से बने हैं। सत्ता और कारपोरेट घरानों को सोना और हीरा चाहिए, वैभव चाहिए। इसलिए तो वे सब कुछ बेंच देना चाहते हैं। यहाँ तक कि लोगों का ज़मीर भी। लोहा तो किसानों, मजूरों और छोटे-छोटे लोगों के कवच और बख्तरबंद हैं। समूची प्रकृति, पहाड़, पर्वत, झरने, पेड़-पौधे, नदियाँ, घाटियाँ, खेत-खलिहान और श्रम ही उनकी पूँजी है। उनकी आँखों की पुतलियों में समूचा संसार बसा है।
किसान-आन्दोलन और शाहीन बाग प्रसंग की रूह भी देखिये। लोकतन्त्र में इस दौर में सत्ता में काबिज़ लोगों के हौसले कई तरह से बढ़े हैं। सत्ता हर प्रसंग को निषेध से लेना और रद्दी की टोकरी में डालना जानती है। इसी के साथ एक लम्बी फेहरिस्त है; जिसमें नोटबन्दी, कालाधन वापसी, जीएसटी, नागरिकता के सवाल; मसलन एनआरसी और एनपीआर भी हैं। शाहीन बाग-आन्दोलन कोरोना वायरस की त्रासदी की भेंट चढ़ गया। विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त से संविधान का एवं नैतिकता का कचूमर निकाल दिया गया। सत्ता के हौसले इसी तरह बढ़ते हैं। आज़ादी और महात्मा गाँधी और स्वाधीनता-आन्दोलन के रणबाँकुरों का दिन-ब-दिन क्षरित होते जाना इसी के सबूत के रूप में देखा जाना चाहिए। जाहिर है कि जब सत्ता से जनआकांक्षाएँ विदा ले लेती हैं तब किसी भी तरह के प्रतिरोध को ठिकाने लगा दिया जाता है तो भयावहता-क्रूरता का जन्म होता है और तानाशाही की फिजा चहुँ ओर फैल जाती है।
यह भी पढें – किसान आन्दोलन : आगे का रास्ता
यह दौर थोथे भाषणों की ओर झुकाया जा रहा है। लगातार झूठ बोल-बोलकर सब कुछ समाप्त किया जा रहा है। किसानों को दर किनार रखकर भारत को ऊँचा उठाने का सपना बोया जा रहा है; जबकि वास्तविकता यह है कि यह सब देश में गप्प लगाने के अलावा कुछ नहीं है। ऊल-जलूल बातों से कैसे भरमाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्त में एकांत श्रीवास्तव की कविता का एक अंश पढ़ें— “जीने के लिए इस संसार में/रोज़ लोहा लेना पड़ता है/एक लोहा रोटी के लिए लेना पड़ता है/दूसरा इज्ज़त के साथ/उसे खाने के लिए/एक लोहा पुरखों के बीज को/बचाने के लिए लेना पड़ता है/दूसरा उसे उगाने के लिए/मिट्टी में, हवा में, पानी में/पालक में और ख़ून में जो लोहा है/यही सारा लोहा काम आता है एक दिन/फूल जैसी धरती को बचाने के लिए।”
अच्छी बात यह है कि पहली बार किसानों ने अपनी असली ताक़त पहचान ली है। अन्नदाता को निरन्तर अवहेलित किया जाता रहा है। उन्हें लगातार भ्रम के खूँटे में बाँधकर उन्हें कुचलने की योजनाएँ चल रही हैं। उनकी जि़न्दयगी को नरक बना दिया गया है। किसान लगता है इस देश के न तो बाशिंदा हैं, न नागरिक। ये वे लोग हैं जो पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं और उन्हें जीवन देते हैं। उनके लिए अनवरत निषेध में काम किया जा रहा है। किसानों के साथ वे लोग खड़े हैं, जो उनको समझते हैं। अन्नदाताओं के साथ युवा, विद्यार्थी, जिम्मेदार लेखक और मज़दूर साथी भी हैं। जो सत्ता के साए में हैं, वे उनसे काफी दूर हैं। किसान आन्दोलन कोई बच्चों का आन्दोलन नहीं है। देश ने कई किसानों के आन्दोलन देखे हैं। अंग्रेजों के समय में भी।
यह भी पढ़ें – किसान आन्दोलनः सवाल तथा सन्दर्भ
गणतन्त्र दिवस पर किसानों की एकजुटता अदभुत रूप से दिखाई दी। दो महीनों से ज्यादा चल रहे आन्दोलन ने शांति-सद्भाव और सहयोग की मिसाल कायम की। तरह-तरह की ख़बरें फैलाई जाती रहीं। उसमें सत्ता से जुड़े हामी भी थे। सत्ता के गलियारों से जुड़े लोग थे, जिन्होंने कई तरह के रूप धरकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश की। इसके प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। ये वे लोग हैं, जो किसानों के नाम पर गणतन्त्र दिवस के दिन गड़बड़ियाँ करते रहे। समूची ट्रैक्टर रैलियाँ शांति पूर्ण थी। हाँ, उनमें उत्साह अकूत था। देखना चाहिए कि किसानों ने कोई लूट-पाट की क्या? हालाँकि उन्हें उकसाने के निरन्तर प्रयास किए गये। यह किसानों की एकजुटता, साहस और धैर्य का प्रमाण है। आन्दोलन को तोड़ने के अनंत प्रयास किए गये। तरह-तरह के भ्रम फैलाए गये और उनको नीचा दिखाने के प्रयास भी हुए। इस बार सरकार ने किसानों की ताक़त भी देख ली। सत्ता अवाक है, क्योंकि जो क्रूरता उन्होंने की, ग़ैर जिम्मेदारी दिखाई और असंवेदनशीलता प्रदर्शित की वह भारतीय जनतन्त्र के इतिहास में दर्ज़ हो चुकी है।
जनतन्त्र केवल सत्ता का नहीं होता, बल्कि वह समूचे देश, नागरिकों का और देश में रहने वाले लोगों का भी होता है। जनतन्त्र गुमान से नहीं चलता, बल्कि देश के लोगों की सहमति और सद्भाव से चलता है। जनतन्त्र कोई ठिठोली या मजाक नहीं है। जनतन्त्र कारपोरेट घरानों, मीडिया और सत्ता का खेल भी नहीं है। जनतन्त्र में प्रतिरोध की आवाज़ों को भी गंभीरता से सुना और गुना जाता है। किसान आन्दोलन ने समूचे देश में एक नया वातावरण निर्मित किया लगातार एक उत्सााह दिखाई पड़ रहा है । किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। वह किसी भी देश की मुख्य रीढ़ और मुख्यधारा भी है। इस देश ने किसान आन्दोलन के इतने तेजस्वी रूप को शायद पहली बार देखा है।
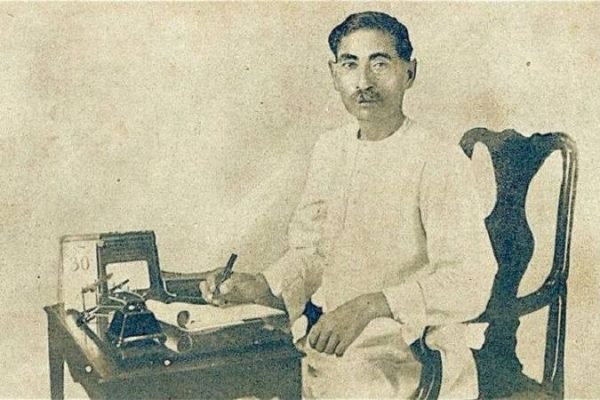
प्रेमचंद ने 09 अक्टूबर 1933 के जागरण के संपादकीय में लिखा था- ‘’सारी राज व्यवस्था, यह बड़ी बड़ी सेनाएँ, ये जंगी बेड़े ये हवाई जहाजों की परें इन्हीं व्यापारियों के फ़ायदे के लिए तो हैं! वे संसार के स्वामी हैं पार्लामैंट और सेनेट सिंडिकेट तो उनके खिलौने हैं। भारत भी उनके मायाजाल में फंसा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा है।‘’ संदर्भ बदला हुआ है वह अंग्रेजों का समय था और अब अपने देश भारत का समय है। जिसमें लंबे अरसे से जनतन्त्र है। देश किस बात का इन्तजार कर रहा है और आखिर सत्ता क्या चाहती है? किसानों की समस्याओं को ऊपरी तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। किसानों की अंदरूनी हालातों पर भी गौर किया जाए। कुछ बड़े किसानों को छोड़ दिया जाए तो मध्यम एवं लघु किसान कई तरह की आपदाओं में फंसे हैं। बाज़ार और कारपोरेट घरानों का बहुत बेजा असर समूचे भारत में दिखाई दे रहा है। सत्ता उदारीकरण, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण और बाज़ारीकरण एवं कारपोरेट रूपों में जन विरोधी नीतियों को बो रही है। आज के समय में कोई भी किसान सुरक्षित नहीं है। पहले तो उसे बीज विहीन किया गया फिर रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से ज़मीन को बंजर बनाने के उद्यम किए गये।
बाज़ार और कारपोरेट घराने किसानों पर कई तरह के हमले करते रहे हैं। किसानों की मूल समस्याओं को न सुलझाकर उन्हें आत्म हत्याओं की ओर ढकेल दिया गया। समूचा देश जिनके बल पर भोजन, खाद्यान्न और आहार प्राप्त करता है। उन्हें सत्ता ने फालतू बना दिया, क्योंकि सत्ता की परिकल्पना में संवेदनशीलता नाम की चीज़ शायद नहीं है। यह असंवेदना देश को कहाँ ले जाएगा। यह किसान आन्दोलन मुझे स्वाधीनता आन्दोलन की वास्तविकता बताता है और याद दिलाता है। दो माह से अधिक का समय हो गया है। सरकार अपनी ज़िद पर अड़ी है। किसानों की मूलभावनाओं और समस्याओं को उसने पीठ दिखा दी।
यह भी पढ़ें – कृषि कानून और किसान आन्दोलन
हमारे प्रजातन्त्र को किसकी नज़र लग गयी। किसानों का विरोध वे लोग भी कर रहे हैं जो वाकई में किसान हैं। उन्हें हिंदुत्व के शंखनाद से भर दिया गया है। उसमें किसान के बेटे भी हैं। नौकरी पाने के बाद वे खा गर्रा रहें हैं। यह देश धीरे धीरे नपुंसकता से भर दिया गया है। वे भले ही आपका कलेजा चाक कर दें। आपको बार-बार शर्मिंदा करते रहें। उन्होंने कम से कम एक तीखा विष भरा हिंदुत्व दिया है और सभी वर्गो से घृणा करना सिखाया है। अरसे बाद वे अपनी वास्तविकता में सामने आए हैं। ऐसे परम प्रतापी लीला बिहारी किसी भी चीज़ को सही नहीं रहने देंगे। वे सत्ता का असली मंत्र पा चुके हैं। इधर किसानों के बारे में अनेक अध्ययन हुए हैं। भूमंडलीकरण के कारण कारपोरेट घरानों की पूँजी की नज़रें ललचाई हुई हैं। वे गाँवों के खेतिहर समाज ही नहीं अन्य इलाकों, स्थानों के किसानों पर लगातार नज़रें गड़ाए हैं और बे-तादाद जमीनें खरीद रहे हैं और लगातार ख़रीदते जा रहे हैं। माल संस्कृति, फार्म हाउस संस्कृति उसी का विकसित रूप है। वे जनतन्त्र भी ख़रीद चुके हैं। भारत को बचाने की भूमिका शहर नहीं खेतिहर समाज ही निभा पाएगा, क्योंकि जब ग्रामीण समाज में आक्रोश बढ़ता है तब उसकी तार्किक परिणति खेतिहर समाज ही कर सकता है।
देश में जनतन्त्र की गिरावट कहाँ तक होगी? इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खेल केवल सत्ता का, साम्प्रदायिकता और फ़ासिज़्म भर का नहीं है। लोकतन्त्र धीरे-धीरे लोक शाही से तानाशाही मनोविज्ञान में पहुँच रहा है। इस देश के नागरिक अब खेल भी जानने-पहचानने लगे हैं। इतिहास में किसान आन्दोलन पूर्व में भी हुए हैं जैसे अवध का किसान आन्दोलन। हमारे साहित्य और अन्य माध्यमों में इसके रिकॉर्ड हैं।किसानों को कमतर आँकने के कई रूप विकसित हुए हैं। प्रेमचंद ने कहा था- ‘’यह आशा करना कि पूँजीपति किसानों की हीन दशा से लाभ उठाना छोड़ देंगे, कुत्ते से चमड़े की रखवाली करने की आशा करना है। इस खूँखार जानवर से अपनी रक्षा करने के लिए हमें स्वयं सशस्त्र होना पड़ेगा।‘’(जागरण,06 नवम्बर 1933
.