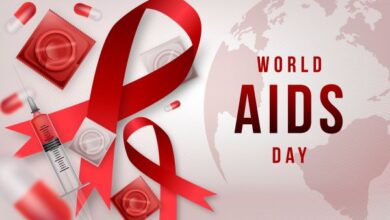- प्रेमपाल शर्मा
दिल्ली विश्वविद्यालय की बर्बादी पर एक लेख आप ने छापा है। https://sablog.in/save-delhi-university-dec-2018/ अच्छा लगा किसी की नजर तो गई लेकिन पढ़कर निराशा हुई. क्या विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षकों की भर्ती, पे कमिशन और खर्चे के लिए होते हैं? क्या कभी यह भी देखा है कि विद्यार्थी पढ़ने आते हैं या नहीं? बिहार, यूपी का सारा क्रीमी लेयर (उसमें दलित और सवर्ण सभी शामिल हैं) आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर है. पिछले 1 वर्ष में में कम से कम 10 कॉलेजों में गया हूं. कॉलेजों के प्रांगण में जाता हूं तो क्लास रूम में भी जाता हूं.
किरोड़ीमल कॉलेज बीकॉम तृतीय वर्ष में साठ बच्चों में से सिर्फ 8 आए हुए थे. मैंने पूछा क्यों नहीं आते? एक चुप्पी। उनका कहना था कि हम भी कई रोज के बाद आए हैं. विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का कहना था कि हर बार मुश्किल से 20% बच्चे आते हैं और बे भी बदल-बदल कर. क्यों? किसकी गलती है? क्या लाखों की तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों ने सोचा? आप तर्क देंगे कि वह स्थाई नहीं हैं. जो स्थाई नहीं हैं, जो टेंपरेरी हैं, उसकी क्लास ज्यादा भरी हुई पाई मैंने. क्योंकि वह नियमित रूप से आ रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे. स्थाई होने के बाद तो बिहार और यूपी का शिक्षक सिर्फ राजनीति में उलझा हुआ है। जब देखो तब रोस्टर की बातें। बैकलॉग की बातें। एक बार भी मैंने पिछले 10 सालों में नहीं सुना, प्रयोगशाला में शोध की स्थिति पर बात हो या सामाजिक विज्ञान में किसी शोध पर बात हो रही हो। बच्चों का साफ कहना है कि हमने सिर्फ नाम सुना था। यहां कुछ भी नहीं बचा है. तो पड़ोस के मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान या करोल बाग में वहां 300 बच्चों की क्लास में क्यों कोई अनुपस्थित नहीं रहता? इन सभी शिक्षकों के बच्चे भी इन्हीं कोचिंग संस्थानों में हैं. वहां उन्होंने कभी रोस्टर की बात नहीं उठाई. वहां उन्हें क्वालिटी, स्तर चाहिए और सरकारी विश्वविद्यालयों में सिर्फ तनख्वाह, आत्मा लोचन की जरूरत है. दोस्तों, हमें इस तस्वीर को बदलना होगा. गरीबों की सिर्फ बात कहने से, नारे लगाने से जिम्मेदारी से नहीं बच सकते.

क्यों सारे बच्चे कोचिंग में भरे पड़े हैं. सिर्फ पढ़ने के लिए ही ना? यदि उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का माहौल मिलता, शिक्षक पढ़ाते तो वहां क्यों जाते? इन गरीबों को कोचिंग संस्थानों में लाखों की फीस देनी पड़ रही है. मजबूर हैं बेचारे. भविष्य का मामला है. जाएं तो कहां जाएं? क्या कभी किसी शिक्षक ने इनकी फरियाद सुनी? ऐसे अनुभव हैं कि प्रथम वर्ष में तो भी बच्चे आते हैं, उसके बाद आना बंद कर देते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक कहता है कि मैं प्रथम वर्ष के बच्चों की क्लास नहीं लेता. क्योंकि वे रोज आ जाते हैं. यानी कि बच्चों का रोजाना आना उन्हें अखरता है. विश्वविद्यालय के शिक्षक पिछले 20 सालों से वही वेतनमान पा रहे हैं. जो सिविल सेवकों की है. पहले एक भी पोस्ट प्रोफेसर की नहीं थी. हिंदी विभाग में अब 10 है प्रोफेसरों का स्केल और ग्रेड कॉलेजों में भी देने की तैयारी है. कोई सुविधा ऐसी नहीं कि जो सिविल सेवाओं से कम हो. लेकिन ना आने की पाबंदी, ना गोपनीय रिपोर्ट. दिन-रात एक राजनीति के अखाड़े और आवरण में. बुद्धिजीवी होने का दंभ अलग. कोई दल अछूता नहीं है जिसने इनको नहीं पाल रखा हो. इसीलिए यह कभी कोई ऐसा आयोग भी नहीं चाहते जो इनकी भर्ती को नियंत्रित करें. इनके ऊपर अंकुश लगाए.

यूरोप अमेरिका के विश्वविद्यालय अगर चल रहे हैं तो स्थाई नौकरी की वजह से नहीं, इस आधार पर अगर उन्होंने कोई अच्छा शोध नहीं किया तो उन्हें अगले ही वर्ष दरवाजा दिखा दिया जाएगा. या तो आप स्वयं अपनी नैतिकता से कुछ मानदंड बनाएं वरना सरकार को बनाने पड़ेंगे और सरकार ने मान लिया है कि स्थाई भर्ती के बजाय टेंपरेरी ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं. बरबादी का कारण सिर्फ उदारीकरण नहीं है. उदारीकरण ने तो आपको बड़ी-बड़ी गाड़ियां दी हैं, बड़े-बड़े वेतनमान दिए हैं. मोबाइल दिए हैं. लेकिन आपने शिक्षा का स्तर क्या किया? क्यों हर अमीर का बच्चा देश छोड़कर भागने को मजबूर है? पहले वह बिहार, यूपी, हरियाणा से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पूना जाता है और उसकी अगली उड़ान विदेश की है. हिंदी राज्यों की और उसके नागरिकों की तो स्थिति और भी बुरी है. अफसोस यही कि जब भी विश्वविद्यालय पर लिखते हैं तो सिर्फ अपनी तनख्वाह, पगार, सुविधाओं पर. ऐसे शिक्षकों के रहते और ऐसी रिपोर्टों के रहते विश्वविद्यालय तो डूबेंगे ही.
प्रेमपाल शर्मा

लेखक स्तंभकार और रेलवे बोर्ड के पूर्व संयुक्त सचिव हैं.
मो. 9971399046