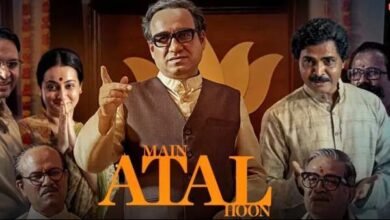नयनाभिराम सौंदर्य का अविराम और अप्रतिम फिल्मांकन। इस कदर खूबसूरत की यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि यह चित्र हैं या जीवंत दृश्य, लेकिन मन में उठते इन संदेहों को उस दृश्य में उड़ता कोई पाखी जिंदा कर जाता है। संसार में जो अनेक सभ्यतायें हैं, उसकी खूबसूरती को दर्ज करती यह अपने किस्म की अनूठी फिल्म है। छवियों की जो श्रृंख्ला है वह आपको पलक झपकने नहीं देती है। पल भर में ना जाने सौंदर्य के किस हिस्से को देखने से आप वंचित हो जायें। सिनेमेटोग्राफी की कोई हद हो सकती है तो यह फिल्म उसे छूती है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाई जाने वाली रंगोली-सी कला के सामने संसार की कोई भी कला बेमानी जान पड़ती है। आँखों में न समा सकनेवाले सौंदर्य को यह फिल्माती है। हर दृश्य के साथ अश-कश करते रह जायेंगे। सौंदर्य देखनेवाले की आँख में होती है, अफसोस कि वह आँख सबके पास नहीं होती। सभ्यता के ध्वंसावशेषों को, प्रकृति की नेमतों को, मरूभूमि को, ज्वालामुखी को, जलप्रपात को, ऊंघते वनों को और अलसाये मंदिरों को और मूर्तियों के भग्नावशेषों को यह अविस्मरणीय तरीके से फिल्मती है।
ऐसी फिल्में अदम्य साहस, अपने माध्यम पर प्राणांतक आस्था, अपनी कला के सामथ्र्य पर अचूक विश्वास से बनती हैं। यह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। दृश्यों के जरिये अपनी बात कहती है। प्रत्यक्षीकरण की प्रविधि में अपनी बात रखती है। दो दृश्यों को आमने-सामने रख कर नतीजा आप पर छोड़ देती है। एक ओर प्रकृति और उसकी छांव में रहनेवाले आदिवासियों का जीवन है तो दूसरी ओर विज्ञान और तकनीक के उन्नत पायदान पर खड़ी दुनिया। सभ्यता के अलग-अलग छोरों पर खड़ी दुनिया को यह आमने-सामने रखने का काम करती है। आप देखें कि कौन सुंदर है? सुंदरता के पक्ष में यह अनूठे ढंग से खड़ी होती फिल्म है। सौंदर्यशास्त्र के हमारे बोध को नये सिरे से गढ़ती-सिरजती है। मशीन और इंसान के मिटते फर्क को भी यह फिल्म बहुत बारीकी से दर्ज करती है। जिंदगी के मायनों को भूल कर किस कदर हम वस्तुओं की भीड़ में खोते जा रहे हैं, यह अहसास कराती है। किस कदर हम वस्तुओं की बजाय कबाड़ से घिरते जा रहे हैं, कैसे हम मशीनी होते जा रहे हैं, इसे भी जताती है। कचड़े की ढेर से प्लास्टिक चुनती आबादी हो गंधक ढोते कंधे, सभ्यता के विकास के दावों पर किसी बदनुमा दाग की तरह उग आई यह छवियाँ विकास के तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी है।
यह भी पढ़ें – बढ़ता तापमान, बढ़ती आबादी, घटता जल, घटता जीवन
खपत की पूर्ति में विज्ञान किस कदर मददगार हुआ है? डिब्बा बंद माँस और दूध के बने उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को यह जिस ढंग से दर्ज करती है, उसके बाद शायद आप खाने की अपनी आदतों को बदलने को मजबूर हो जायें। मनुष्य कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच गया है, फिल्म इसको बहुत संजीदगी से रेखांकित करती है। रोजमर्रे के जीवन की हरकतों से सभ्यता के मूल्यांकन की दक्षता रखती फिल्म है। जिंदगी को जीने के बारे में सोचने पर विवश करती फिल्म है। असम्बद्ध-सी लगनेवाली छवियों के जरिये इस काम को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। एक-एक दृश्यों की कड़ियाँ जोड़ना जितना श्रमसाध्य कार्य रहा होगा, उससे कमतर उनको फिल्माना नहीं रहा होगा। संसार भर की जो छवियाँ इसमें जुटाईं गईं हैं, उसके चुनाव और फिल्मांकन में इस फिल्म का असल श्रम समाहित है। नामालूम कितनी यात्राओं और कितने सब्र से यह फिल्म साकार हो सकी है। कोलाज वाले फार्म में बनाये गये इस सिनेमा के मूल में काम करनेवाली सिनेमाई चेतना को नजरंदाज कर पाना इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि इन छवियों को अलग-अलग देखते हुए इनको साथ रखने से मिलनेवाले संदेश का अनुमान असंभव जान पड़ता है। यह किसी असंभव को संभव कर देने जैसा है। ताबूत की कलात्मकता मनुष्यों की मूर्खता को नये सिरे से समझने का सूत्र देती है। वैभवशीलता के मूल में छिपी कीमत का सही-सही अनुमान लगाने के प्रति यह फिल्म आपको सजग करती है।
हथियार बनाने और खिलौना बनाने में कोई फर्क नहीं रह गया है। उसको असेम्बल करने का तरीका एक-सा है। उसे असेम्बल करनेवाले कामगारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क उनको इस्तेमाल करनेवालों में जरूर है। लेकिन फिल्म इस बात को अलग से रेखांकित करना नहीं भूलती है कि चाहे वह आदिम समुदाय हो या उत्तर आधुनिक संसार हथियार अब हर कहीं मौजूद है। लगातार हिंसक होती दुनिया की नियति यही है। इससे अछूता रह पाना अब संभव नहीं है। कारतूसों के सौंदर्य को उसके इस्तेमाल से प्रभावित मनुष्य को सामने रख कर यह फिल्म जब काउंटर करती है तो फिल्मकार के सिनेमाई चेतना में विन्यस्त उसकी सतत राजनीतिक दृष्टि की ओर आपका ध्यान बरबस जाता है कि इस फिल्मकार के पास दुनिया को लेकर एक तस्सवुर है। वह उस दुनिया को कामिल होते देखना चाहता है। इस दुनिया में विकास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर जो कुछ हो रहा है, फिल्म उसको प्रश्नांकित करती है। उसके दुष्प्रभावों को छवियों के मार्फत् सामने लाती है। जिस ढंग से यह इस काम को अंजाम देती है, किसी और विधा के जरिये इसे इस रूप में साकार कर पाना संभव नहीं है। विधा के बतौर सिनेमा के सामथ्र्य और संभावनाओं के दायरे को यह एक अलग स्तर पर ले जाती फिल्म है।
 रक्षा के नाम पर नागरिकों मन-मस्तिष्क में बोई जानेवाली आक्रामकता, सैन्य रक्षा पर किये जानेवाले खर्च, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर की जानेवाली बाड़ेबंदी आदि को भी फिल्म अपने दायरे में लेकर आती है। किसी बच्चे की गेंद देश की सीमा रेखा के पार चली गई है। बाड़ के उस ओर जा पाना संभव नहीं है। ‘बच्चे ने गुस्से की एक भंगिमा वाली कार्टून के साथ उस सीमा रेखा की दीवाल पर यह पंक्तियाँ लिख डाली हैं कि ‘मैं अपनी गेंद वापस चाहता हूँ।’ यह सभ्यता की दयनीयता को उजागर करनेवाली पंक्तियाँ हैं। जहाँ सीमा रेखा बच्चों का गेंद निगल रही है। उसका देश उसे वह गेंद वापस दिला पाने में सक्षम नहीं है। लगातार संशयालु होती दुनिया एक बच्चे के विश्वास उसकी मासूमियत की रक्षा कैसे कर सकती है।
रक्षा के नाम पर नागरिकों मन-मस्तिष्क में बोई जानेवाली आक्रामकता, सैन्य रक्षा पर किये जानेवाले खर्च, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर की जानेवाली बाड़ेबंदी आदि को भी फिल्म अपने दायरे में लेकर आती है। किसी बच्चे की गेंद देश की सीमा रेखा के पार चली गई है। बाड़ के उस ओर जा पाना संभव नहीं है। ‘बच्चे ने गुस्से की एक भंगिमा वाली कार्टून के साथ उस सीमा रेखा की दीवाल पर यह पंक्तियाँ लिख डाली हैं कि ‘मैं अपनी गेंद वापस चाहता हूँ।’ यह सभ्यता की दयनीयता को उजागर करनेवाली पंक्तियाँ हैं। जहाँ सीमा रेखा बच्चों का गेंद निगल रही है। उसका देश उसे वह गेंद वापस दिला पाने में सक्षम नहीं है। लगातार संशयालु होती दुनिया एक बच्चे के विश्वास उसकी मासूमियत की रक्षा कैसे कर सकती है।
सामी धर्मों के तीर्थस्थलों और उसके विश्वासियों के आस्थाओं और इबादत की भंगिमाओं को बहुत शाइस्तगी से यह फिल्माती है। सिस्टाईन चैपल से इतर मक्का को इतनी भव्यता में बहुत कम मौकों पर फिल्माया जा सका है। बौद्ध मठों को उनके परिवेश के संग फिल्माने में भी गजब की सफलता अर्जित की है। यों तो फिल्म के संदेश से आपको कुछ लेना देना ना हो तो भी केवल सिनेमेटोग्राफी या पिक्चराइजेशन के लिए इसे देखा जा सकता है। बिना एक शब्द खर्च किये हुए छवियों और ध्वनियों के बूते भी ऐसा शाहकार सिरजा जा सकता है, यह अकल्पनीय है। जिसे केवल देख कर महसूसा जा सकता है। गर आप ज्यादा संवेदनशील हुए तो इसे देखते हुए लग सकता है कि आप अपनी जिंदगी कहाँ घर, परिवार और दफ्तर में गारत कर रहे हैं, असली दुनिया और जिंदगी इसके बाहर है। असली कामयाबी जैसी बची है वैसी की वैसी इस दुनिया को बचा लेने में है। रौन फ्रिक की 2011 में बनी यह फिल्म ‘मस्ट वाच’ की श्रेणी वाली है।
.