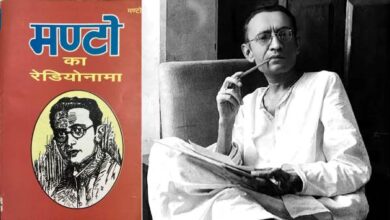गंवई कथारस और मानवीय संवेदना के अद्भुत चितेरे “रेणु”
फणीश्वरनाथ रेणु के कथा साहित्य में बिहार के गाँवों की आत्मा उतर आई है। वहाँ की बोली- बानी, भाषा, कहावतों, मुहावरों और गीतों में वहाँ के लोक जीवन की कथा बड़ी ही मार्मिक और सरस शैली में कहते हैं, “रेणु”। प्रेमचंद जहाँ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उकेरते हैं वहीं रेणु के कथा -साहित्य में बिहार का जीवन और वहाँ की समस्याएँ यथार्थ रूप में अंकित हुई हैं। प्रेमचंद और “रेणु” के साहित्य को अगर समग्रता में पढ़ा जाए तो उसके माध्यम से उत्तर भारत के गाँवों की मुकम्मल तस्वीर बनती जान पड़ती है। “रेणु” के साहित्य की बड़ी विशेषता यह है कि उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जिस सामाजिक यथार्थ को वह चित्रित कर रहे हैं उसे उन्होंने बहुत दूर से देखा या जाना है बल्कि ऐसा लगता है कि अपने द्वारा नित देखे गये सत्य, भोगे गये यथार्थ और जीए गये जीवनानुभवों को ही कहानियों में पिरो कर, पूरी ईमानदारी के साथ पाठकों के समक्ष रख देते हैं इसीलिए पाठक जब उनकी रचनाओं को पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उन घटनाओं का साक्षात एक पाठक के रूप में नहीं बल्कि एक चरित्र के रूप में कर रहा हो।
कभी-कभी उनकी कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम एक कला फिल्म देख रहे हैं जहाँ जीवन की सच्चाई पूरी तटस्थता के साथ अंकित हुई है। इस फिल्म के पात्र अपने चेहरे पर कोई नकली रंग-रोगन लगाकर पाठकों या दर्शकों के सामने नहीं आते बल्कि यथार्थ जीवन के मंच पर अपने टूटे-फूटे औजारों के साथ इस तरह से सामने आते हैं कि पाठक रूपी दर्शक को लगता है कि वह सिनेमा नहीं देख रहा है या कहानी नहीं पढ़ रहा है बल्कि जीवन के यथार्थ से रूबरू हो रहा है।
“रेणु” ने जहाँ कई कालजयी उपन्यासों की रचना की है, वहीं बहुत सी कहानियाँ भी लिखी हैं। रेणु रचनावली- भाग 1 में उनकी तकरीबन 6३ कहानियाँ संकलित हैं और उनमें से कुछ कहानियाँ निस्संदेह कालजयी कहानियाँ हैं। उनकी कहानी “तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम” पर शैलेंद्र ने 1966 में “तीसरी कसम” नाम से फिल्म बनाई थी और सशक्त अभिनेता राज कपूर तथा भावप्रवण अभिनेत्री वहीदा रहमान ने कहानी के पात्रों को रजतपटल पर जीवंत कर दिया था। एक और कहानी “पंचलैट” पर भी हाल ही में फिल्म बनी है।
रेणु की कहानियाँ अगर फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती हैं तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि उनकी कहानियों में यह क्षमता है कि वह ग्रामीण भारत के यथार्थ को उकेरने के कारण एक बड़े दर्शक वर्ग के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब होती हैं। एक खास वर्ग अर्थात पुरबिया समाज के लोगों को तो ये कहानियाँ अत्यधिक प्रभावित करती हैं क्योंकि उनमें उन्हें अपनी ही जिन्दगी प्रतिभासित होती जान पड़ती है। साथ ही “रेणु” की कहानियों से झांकता मूल्य बोध भारतीय समाज का वह मूल्य बोध है जो न कभी पुराना पड़ा है और न ही पड़ेगा। कई बार छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से वह ऐसी बड़ी बात कह जाते हैं पाठक घंटों तक सोचने के लिए विवश हो जाता है और विचारों के प्रवाह में डूबते-उतराते वह कथाकार के संदेश से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता।
“रेणु” की एक छोटी सी कहानी है “संवदिया”, जिसे पढ़ते हुए हम एक मूल्य बोध को ही नहीं सहेजते बल्कि इतिहास के एक कालखंड से भी साक्षात करते हैं। एक ऐसा कालखंड जो इतिहास के म्यूजियम या मानव स्मृति की मंजूषा में बड़े यत्न के साथ सहेज कर रखा गया है। एक समय में उत्तर भारत के गाँवों में संदेशवाहकों के माध्यम से संदेश भेजने की परम्परा थी। बहुओं को अपने मायके कोई जरूरी संदेश भेजना हो और वह संदेश अत्यंत गुप्त रूप से भेजना हो तब संवदिया की मदद ली जाती थी जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सूचना लेकर के दिन की धूप और रात के अंधेरे की परवाह किए बिना, उसे अपने गंतव्य तक पहुँचा देता था।
यह भी पढ़ें – मेहनतकश जनता के लेखक थे फणीश्वरनाथ रेणु
आज के दौर में जब चिट्ठी- पत्री तक लिखना लोग भूलते जा रहे हैं और चिट्ठियों का स्थान मेल अथवा सोशल मीडिया पर लिखे जाने वाले संदेशों ने ले लिया है तथा एक उंगली के स्पर्श मात्र से ही आप अपने मन की बात दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति तक पहुँचा पाने में सक्षम हो जाते हैं तो संवदिया हमें प्राचीन युग का एक ऐसा व्यक्ति लगता है जिसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है लेकिन “रेणु” अपने कथा- साहित्य में इतिहास के उस कालखंड को बेहद सूक्ष्मतापूर्वक सहेजते हुए संवदिया नामक प्रजाति को अमरत्व प्रदान करते हैं।
एक छोटा सा संवदिया अर्थात हरगोबिन “रेणु” की लेखनी का स्पर्श पाकर एक अद्भुत और जीवंत व्यक्तित्व में ढल जाता है जो भले ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता लेकिन बड़ी बहुरिया के बड़े मान को जौ भर भी डिगने नहीं देता। बड़ी बहुरिया जो परिस्थितियों से घबड़ाकर अपना गाँव छोड़कर मायके में शरण लेना चाहती हैं और संवदिया के माध्यम से यह संदेश अपने नइहर भेजती हैं, उस संदेश या संवाद को संवदिया कह पाने में स्वयं को असमर्थ सा पाता है। उसे बड़ी बहुरिया का गाँव छोड़कर जाना गाँव की लक्ष्मी के गाँव से चले जाना जैसा लगता है। वह अपनी भूमिका को विस्मृत कर अपने गाँव -घर की इज़्ज़त ही नहीं बचाता बल्कि गाँव की उस परम्परा का निर्वाह भी करता है जिसमें गाँव के तमाम लोग जाति बंधन को भुलाकर एक गंवई रिश्ते की डोर में बंधे होते हैं। जहाँ एक घर की बहुरिया दूसरे घरों की इज्जत भी होती है। उसका दुख सबको व्यथित करता है। और बड़ी बहुरिया भी प्रेमचंद की कहानी “बड़े घर की बेटी” की तर्ज पर अपने घर का मान बचाकर संतुष्ट ही होती हैं। वह यह जानकर प्रसन्न होती हैं कि उनके घर की मर्यादा मायके वालों के सामने बनी रही क्योंकि वह संवाद भेज तो देती हैं लेकिन “संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी।”
भेजे हुए संवाद या संवदिया को फिरा लेने का कोई उपाय बड़ी बहुरिया के पास भले ही नहीं था लेकिन उनका विश्वस्त संवदिया मानो उनके मन की बात को जान गया था। एक साधारण संवदिया भी यदि इतना संवेदनशील हो सकता है कि अपने सामने परोसी गई सुस्वादु भोजन की थाली को देखते हुए उसे बड़ी बहुरिया का बथुआ खाकर दिन निकालना याद आ जाता है तो भला मन में छिपी बात को वह कैसे नहीं समझता। वह हर कीमत पर अपने गाँव की लक्ष्मी को गाँव में रोके रखने की कोशिश करता है और बड़ी बहुरिया भी थोड़ा सा डगमगाई भर थीं, उन्होंने भला मुश्किलों के सामने घुटने कहाँ टेके थे। वह तो मन ही मन हरगोबिन को अशीषती हुई उसकी तीमारदारी में लगे जाती हैं।
ये हैं रेणु- साहित्य के अविस्मरणीय चरित्र जो जीवन का सार अपने व्यक्तित्व में समेटे हुए हैं। एक ऐसी जिजीविषा की थाती उनके पास है जिसके सहारे वे बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी घबराते नहीं और अपने आत्मसम्मान के साथ जिन्दगी जीने में यकीन रखते हैं। इन पात्रों में यह जीवट उनके गाँव की माटी से भी आता है और माहौल से भी, वही माटी और माहौल जिसपर लगातार अपसंस्कृति का खतरा मंडरा रहा है।
यह भी पढ़ें – भारतीयता के लेखक रेणु की प्रासंगिकता
इसी तरह का एक और स्वाभिमानी और संवेदनशील चरित्र है, “ठेस” कहानी का कलाकार, सिरचरन। “रेणु” सिरचरन का चरित्र गढ़ते हुए मानो यह सिद्ध कर देते हैं कि जो अति संवेदनशील होते हैं वही अपने स्वाभिमान की रक्षा भी कर सकते हैं और मानवीय मूल्यों की भी। कलाकार स्वाभाविक रूप से थोड़े सनकी भी होते हैं और अपने आत्मसम्मान के प्रति सजग भी, सिरचरन भी ऐसा ही है। आज के बाजारु समय में भले ही कला और कलाकार बदलते समय के साथ बदल गये हैं लेकिन “रेणु” की कहानियों में ऐसे चरित्र भी सहेजे गये हैं और उनके स्वाभिमान को भी सम्मान के साथ उकेरा गया है। भले ही गाँव के कुछ नासमझ या होशियार लोग “सिरचनरन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले” लेकिन उसकी कला के मुरीद जानते थे कि हस्तकलाओं के लुप्तप्राय या बाजारू होते दौर में कलाकारी तो उस जैसे कलाकारों के हाथ में ही रह गई थी इसीलिए समझदार लोग उसकी कला का सम्मान करते थे, रूपयों से उसका मोल नहीं आंकते थे।
किसी के घर में जहाँ कलाकार सिरचनरन के आत्मसम्मान को जरा सी ठेस लगी नहीं कि वह वहाँ से अपना डेरा डंडा समेटकर चल पड़ता है लेकिन प्यार और स्नेहसिक्त अधिकार बोध से उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। और यह कलाकार प्रेम के सामने झुकता ही नहीं उस गंवई परम्परा का मान भी रखता है जिसके अनुसार किसी की बेटी गाँव भर की बेटी होती है। ससुराल में उसके मान- सम्मान की जिम्मेदारी सब गाँव घर वालों की होती है। भले ही अपने स्वाभिमान को लगी ठेस के कारण वह मानू की विदाई में देने के लिए बुनी जा रही चिक को अधूरा ही छोड़कर चला आता है और “मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही” थी लेकिन सिरचनरन मानो के ससुराल वालों की माँग और मानू की साध को अधूरा नहीं रहने देता।
अपने स्वाभिमान को परे सरकाकर, मन को लगी ठेस को भुलाकर मानू को पूरे मान- सम्मान के साथ अपनी ओर से अद्भुत विदाई देते हुए कहता है-“यह मेरी ओर से है। सब चीज है दीदी! शीतलपाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी, खुश की।” अपने श्रम का दाम लेने से पीछे हटकर सिरचरन सिर्फ एक कलाकार का सम्मान ही नहीं बचाता, उस भाई का सम्मान भी बचा लेता है जो अपनी बहन को ससुराल में ससम्मान राजी- खुशी देखना चाहता है। गंवई परम्पराओं की यह प्रतिष्ठा “रेणु” के साहित्य की अद्भुत विशेषता है। हालांकि अब वह गाँव भी नहीं बचा और गाँव की वे परम्पराएं भी। छद्म विकास और तकनीकी विनाश की आंधी ने सबको लील लिया है लेकिन साहित्य एक ऐसा अजायबघर है जहाँ तमाम लुप्तप्राय चीजें सहेजकर रखी जाती हैं, वे कलाकारों का स्वाभिमान हों या गाँव का सरल -स्वाभाविक और मानवीय परिवेश।
आलोच्य कहानी के माध्यम से “रेणु” लुप्तप्राय होती जा रही लोककला और सामाजिक परिदृश्य से लगातार घटते या विलुप्त होते होते जा रहे कलाकारों, के पीछे के कारणों की ओर भी बारीकी से संकेत करते हैं। जब हमारे अपने मन में, गाँवों में, गाँववासियों के ह्रदय में कला और कलाकारों के प्रति सम्मान बोध नहीं बचेगा तो कलाएँ भी नहीं बचेंगी। और शायद यही कारण है कि निपट देहात के घर- घर में पलने ओर पनपने वाले कला कौशल फैशन और आधुनिकता की आँधी में उड़कर क्रमशः गायब होता जा रहे हैं। सरकारी संरक्षण में कलाओं को बचाने की कितनी भी कोशिशें हों वे पूरी तरह सफल तभी होंगी जब कला और कलाकारों को अपने- अपने घर-परिवार और समाज में पूरा सम्मान और स्वीकार मिलेगा।
यह भी पढ़ें – परती परिकथा : एक आम पाठक की नजर में
“रेणु” के कथा साहित्य में मानवीय संवेदनाओं से लैस बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो पाठकों के मन पर गहरी या स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। इन चरित्रों की सबसे बड़ी खासियत है, इनकी सहजता। ये हमारे आस- पास के परिवेश से उठाए गये और मानवीय रेशों से गढ़े गये चरित्र हैं जो इंसानी खूबियों और खामियों को अपने भीतर बड़ी सहजता से समेटे नजर आते हैं। इनमें एक ओर मान -अभिमान, रोष और अहंकार है तो दूसरी ओर गंवई संवेदना का अजस्र स्रोत भी प्रवाहित होता है जो अपनी उदारता और स्नेह की धार में अपने आस- पास के सभी लोगों को समेट लेना चाहता है। “लालपान की बेगम” कहानी की बिरजू की माँ एक ऐसा ही चरित्र हैं जिसका गुस्सा जितना तेज है प्रेम उतना ही मीठा। मन में अहंकार भी बसता है और प्रेम भी, लेकिन कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, कहना मुश्किल है।
उसके मन में अपने बैलों के प्रति सहज अभिमान या फिर कहें तो अहंकार है जिसके बल पर बलरामपुर का मेला देखने जाने की घोषणा वह गाँवभर में कर चुकी है लेकिन गाड़ी के आने में होनेवाली देरी उसकी क्रोधाग्नि भड़का देती है जिसकी आँच में बिरजू, चंपिया और मखनी फुआ सभी झुलसते हैं। जंगी की नयी नवेली मुँहजोर पतोहू जो कुर्माटोली की सभी झगड़ालू सासों से मोर्चा ले चुकी है, भी उसकी तीखी बोली और अन्योक्तियों से धधक कर उसे “लालपान की बेगम” कहकर पुकारती है। लेकिन यह बेगम, सही मायने में अपने- आपको बेगम समझकर तब संतुष्ट होती है जब अपने बैलों द्वारा हाँकी जानेवाली गाड़ी में, देर रात ही सही शान से सज- संवरकर मेला देखने जाती है। उस समय एक उदार रानी या बेगम की तरह ही वह जंगी की मुँहजोर बहू को भी गाड़ी बैठाती हैं और उन तमाम छूटी हुई औरतों को भी जो अलग-अलग कारणों से मेला घूमने नहीं जा पाई थीं। और उसके इस व्यवहार में कहीं भी उन औरतों पर रौब ग़ालिब करने या उन्हें नीचा दिखाने का भाव नहीं था बल्कि सहज मानवीय और गंवई संवेदना थी जो अपनी खुशी को सबके साथ बाँटकर उसे दोगुना -चौगुना बढा़ लेती है। शायद इसीलिए वह जंगी की पतोहू की ओर देखकर मन ही मन कहती हैं, “कितनी प्यारी पतोहू है” और सबको मीठी रोटियां खिलाकर, उन्हें सिनेमा का गाना गाने को कहकर, सभी को सुखी -संतुष्ट देखकर स्वयं भी प्रसन्न हो जाती है।
सब की खुशी में खुश होना ही तो मनुष्यता की पहचान है, इसीलिए तो गुस्से में भभक उठनेवाली और सबको आहत कर देने वाली बिरजू की माँ स्थितियों को संवारना भी जानती हैं और सबको हँसाना भी। बिरजू की माँ के “क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा” चरित्र को स्वाभाविकता से उकेरते हुए “रेणु” गाँव की उस सभ्यता की बात भी कर रहे थे जहाँ दुख और सुख दोनों सार्वजनिक होते थे, व्यक्तिगत नहीं। आदमी अगर क्रोध में एक दूसरे से लड़ लेता था तो दूसरे ही क्षण किसी खुशी में वे सब साथ शामिल भी होते थे। ताने- तिश्ने और बोली -ठोली के साथ प्रेम का सागर भी लहराता था, और यही सच्चे सामुदायिक आचरण या अच्छे समाज की पहचान थी। बिरजू की माँ, मखनी फुआ और जंगी की पतोहू सभी एक दूसरे के साथ इसी सहज सामूहिक रिश्ते से जुड़े थे, जो रिश्ते, साथ रहने, एक साथ हँसने- रोने या लड़ने -झगड़ने से बनते हैं।
वहाँ किसी किस्म का बनावटी शीतयुद्ध नहीं है जिसके साथ जीना भी मुश्किल हो और उससे पार पाना भी। “लाल पान की बेगम” जैसी कहानियों के द्वारा “रेणु” सिर्फ भाषा और शैली के स्तर पर ही गंवई परिवेश की रचना नहीं करते बल्कि संवेदना के स्तर पर भी वास्तविक गाँव की तस्वीर उतारते हैं, वही तस्वीर, जिसमें पूरा गाँव एक संयुक्त परिवार की तरह होता है। उस परिवार में नोंक- झोंक भी होती है और तकरार भी, लेकिन इन सबके बावजूद परिवार टूटता- बिखरता नहीं। आपस में सब प्रेम की डोर से बंधे होते हैं। आज जब संयुक्त परिवारों का अस्तित्व तकरीबन समाप्ति की ओर है, ऐसे में “रेणु” के कथा -साहित्य में सुरक्षित ऐसे वृहत्तर परिवार को देखना/पढ़ना सच में सुखकर ही नहीं आश्वस्तिदायक भी है।
यह भी पढ़ें – महामारी के बीच मैला आँचल के डॉ. प्रशान्त
इसी पारिवारिक या सामुदायिक भावना को पुष्ट करती एक और कहानी “रसूल मिसतिरी” का जिक्र करना चाहूंगी। यह कहानी चरित्र प्रधान कहानी है या संवेदना प्रधान या फिर मानवतावादी कहानी है, यह कहना जरा मुश्किल है। रसूल मिस्त्री जैसे चरित्र आसानी से भले ही नहीं दिखाई देते लेकिन निरंतर स्वार्थी और आत्मकेंद्रित होते जा रहे समाज में ऐसे चरित्र संख्या में भले ही कम हों लेकिन हैं तो जरूर ही, तभी तो समाज भी बचा हुआ है, संवेदनाएँ भी और इंसानियत भी। घर फूंक तमाशा देखनेवाले या दूसरे के दुख और परेशानियों के पीछे अपना काम- धाम भुलाकर उन परेशानियों को भरसक दूर करने में लग जानेवाले मिस्त्री जैसे चरित्र शायद हर गाँव, मुहल्ले में एक- आध ज़रूर होते हैं और अगर नहीं होते हैं तो होने चाहिएं, अन्यथा समाज कैसे बचेगा। हम सब अंधी रेस के घोड़ों की तरह अपनी -अपनी इच्छाओं के पीछे पागलों की तरह भागे जा रहे हैं, यह भी पता नहीं कि मंज़िल क्या और कहाँ है।
वहाँ पहुँच भी पाएंगे या नहीं और अगर पहुँच गये भी, तो भला क्या हासिल कर लेंगे, यह भी हमें ठीक से नहीं पता। वहीं रसूल मिस्त्री जिनकी दुकान पर मरम्मत का काम होता है, उसे राम भरोसे या रहीम (बेटा) भरोसे छोड़कर हैरान -परेशान आदमियों के दिलों या आदमियत की मरम्मत के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि इस कहानी की पृष्ठभूमि में गाँव नहीं एक छोटा सा “गंवारू शहर” है जो जमाने की हवा के प्रभाव से आशा और आवश्यकता से अधिक बदल चुका है लेकिन इस अंधाधुंध बदलाव के बावजूद “सदर रोड में- उस पुराने बरगद के बगल में रसूल मिस्त्री की मरम्मत की दुकान को तो जैसे जमाने की हवा लगी ही नहीं।” रसूल मिस्त्री की दुकान का वर्णन पूरे विस्तार से करते हुए कथाकार “रेणु” मानो उसके परिवेश और मिजाज की अपरिवर्तनशीलता को लेकर आशवस्त और संतुष्ट नजर आते हैं, मानो कुछ तो है जो बचा हुआ है और बचा रहना चाहिए भी, ताकि बची रहे पूरी कायनात।
रसूल मिस्त्री के व्यक्तित्व का वर्णन बेहद धैर्य और सलीके से करते हुए वे उसे पाठकों की दृष्टि के समक्ष जीवंत कर देते हैं -“मझोला कद, कारीगरों सी -काया और नुकीले चेहरे पर मुट्ठी-भर ‘गंगा -जमनी’ दाढ़ी। साठ वर्ष की लंबी उम्र का कोई भी विशेष लक्षण शरीर पर प्रकट नहीं हुआ। चुस्ती -फुर्ती जवानों से भी बढ़कर। सादगी का पुतला-मोटिया कपड़े की एक लुंगी और कमीज़। पान, चाय और बीड़ी का बंडल। कभी हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठना, वह जानता ही नहीं। ‘गप्पी’ भी नम्बर एक का, पर अपनी जिम्मेदारी को कभी न भूलनेवाला। काम के साथ ही साथ वह बातचीत का सिलसिला भी जारी रख सकता है।” रसूल मियां की बड़ी खासियत की ओर लेखक गहराई से संकेत करते हैं कि वे सही मायने में भारत की गंगा जमुनी तहज़ीब का प्रतिनिधित्व करते हैं और धर्म तथा जाति से परे हर किसी के दुख और परेशानियों में बराबर के शरीक ही नहीं होते बल्कि उसे दूर करने की भरसक कोशिश भी करते हैं।
यह भी पढ़ें – ‘जीवन में स्पंदन का मंत्र : चटाक-चट-धा!’
तकलीफ फखरूद्दीन की हो या समस्या सुदमिया की, रसूल मियां दोनों के साथ समान रूप से खड़े नजर आते हैं। वह अपने मिस्त्री होने की जिम्मेदारी भले ही भूल जाएं पर इंसानियत का फर्ज कभी नहीं भूलते। शायद इसीलिए लेखक उनकी दुकान पर जहाँ लिखा था, “रसूल मिसतिरी-यहाँ मरम्मत होता है” की बगल में किसी नटखट लड़के द्वारा लिखे गये वाक्य -“यहाँ आदमी की भी मरम्मत होती है।” को पढ़ते हुए उसका मन ही मन समर्थन करता है। रसूल मिस्त्री जैसे लोग समाज की पाठशाला में मानवीय मूल्यों और संवेदना का पाठ पढ़ाकर सच में आदमी गढ़ रहे थे। नागार्जुन की कविता के ‘दुखहरन मास्टर’ अपने बेबस बच्चों (विद्यार्थियों) पर तमाचे बरसाकर भी उन्हें नहीं गढ़ पाता लेकिन रसूल मिस्त्री जैसे लोग अपने जीवन और आचरण का आदर्श सामने रखकर सही मायने में इंसान गढ़ते हैं। इस तरह के झक्की, मस्तमौला, गप्पी पर ईमानदार और अपने आस -पास के लोगों के प्रति समर्पित और सही अर्थों में माटी से जुड़े, माटी के मानुष जिस समाज में होते हैं, वह समाज सच में स्वर्ग बन जाता है।
“रेणु” के कथा- साहित्य की खासियत है कि वह उस गंवई अंचल की विशेषताओं, बोली- बानी, मुहावरों के साथ उसकी समस्यायों पर बात करता हुए उस आदमियत या इन्सानियत को भी सामने लाता है जिसके बिना समाज या देश का न तो अस्तित्व संभव हो सकता है ना विकास। रेणु को पढ़ते हुए हमारा परिचय जीवन की पाठशाला के असली चरित्रों से होता है, जिनसे मिलकर जिन्दगी को देखने/ समझने की एक समझ विकसित होती है जिससे हमें क्षुद्र और संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊपर उठकर वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनने की शिक्षा मिलती है। आज हम खुद बहुत कुछ बनना और अपने बच्चों को भी बनाना चाहते हैं लेकिन इस कुछ बनने या पाने या किसी खास मुकाम पर पहुँचने की होड़ में मनुष्यता बहुत पीछे छूट जाती है। साहित्य हमारे अंदर बसे या छिपे उसी मनुष्यता को उभारता है। “रेणु” का साहित्य इस दृष्टि से अप्रितम है कि वहाँ जीवन की विरूपताएँ पूरी भयावहता के साथ चित्रित हैं तो उन विरूपताओं को संवारकर जिन्दगी को जीने लायक या खूबसूरत बनाने वाले पाठ भी कम नहीं हैं, जरूरत है तो इस पाठ को समझने, सहेजने और जीवन में उतारने की।
.