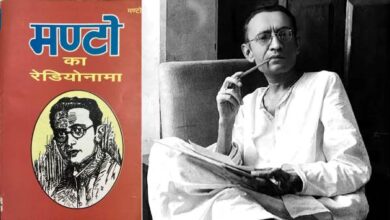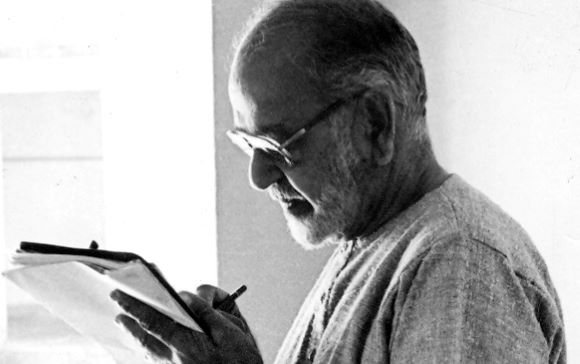
राजनीति, साहित्य और स्वाधीनता
क्या राजनीतिक स्वाधीनता और साहित्यिक स्वतन्त्रता में कोई अन्तर है? क्या भारत में साहित्यकारों ने भी स्वतन्त्रता उसी समय पाई जब भारत राजनीतिक रूप से स्वाधीन हुआ, यानि 15 अगस्त, 1947 को? आम तौर पर लेखकीय स्वतन्त्रता को देश की स्वाधीनता से अलग नहीं समझा जाता।
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ ने 1967 में यह कहने की कोशिश की थी कि भारतीय लेखक तीस के दशक में ही स्वाधीन हो चुका था, देश को आजादी भले ही दस बारह वर्ष बाद मिली। अज्ञेय ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए तीस के उत्तरार्ध के समय को भारतीय लेखक के स्वतन्त्र होने का समय माना है। यानि देखा जाए तो उनके हिसाब से प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के समय यानि 1936 में जब प्रेमचन्द जीवित थे तो भारतीय लेखक स्वतन्त्र थे जबकि देश तब भी अँग्रेजों के अधीन ही था। वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर हम बीस के आसपास के हिन्दी साहित्य की तुलना तीस के दशक के साहित्य से करें तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाएगा।
अज्ञेय के किसी कथन को सीधे सीधे मानने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। पर इस बात को अधिकतर लोग मानेंगे कि जब प्रेमचन्द ने ‘साहित्य का उद्देश्य’ के बारे में, 1936 में अपना भाषण दिया तो प्रदेश में एक नये युग का सूत्रपात हो चुका था। 1936 से 1940 के बीच साहित्यकारों में तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को लेकर बहुत तेज बहस चली थी इसमें सन्देह नहीं। यशपाल ने आचार्य नरेंद्र देव के हवाले से यह बात कही है और इस नये तेवर को अपनी महत्त्वूर्ण पुस्तक- ‘गाँधीवाद की शव परीक्षा’ में दर्ज भी कर दिया था।
देखा जाए तो 1936-1937 के आसपास भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। काँग्रेस के भीतर वामपन्थी और समाजवादी रुझान वाले युवा नेतृत्व ने संगठन के उद्देश्यों और कार्यक्रमों में बड़े रेडिकल परिवर्तन लाने की कोशिश की जिसकी एक अभिव्यक्ति फैजपुर के काँग्रेस अधिवेशन में दिखलाई पड़ती है और उसके बाद सुभाष चन्द्र बोस द्वारा गाँधीवादी नेतृत्व के सामने खड़े होने के निर्णय में। इस दौर में ही भारतीय लेखक स्वाधीन हुआ, ऐसा ही अज्ञेय की बात में ध्वनित होता है। क्या इसे स्वतन्त्र होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता?

अज्ञेय के इस कथन पर कोई विशेष प्रतिक्रिया 1967 या उसके बाद के समय में हुई या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, पर ऐसा लगता है कि शायद नहीं हुई। तब तक के अधिकांश लेखकों को यह लगने लगा होगा कि लेखकीय स्वतन्त्रता और देश की राजनीतिक स्वाधीनता के बीच के अन्तर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
यशपाल ने लेखक के स्वाधीन होने के उस दौर को जिया था और एक मायने में इसका नेतृत्व किया था। उसे वे भूले नहीं थे इसका प्रमाण यह है कि अज्ञेय के इस कथन के सात साल बाद जब उनका उपन्यास ‘मेरी तेरी उसकी बात’ लिखा गया उसमें उस दौर की राजनीतिक कथा में तीस के उत्तरार्ध में आए रेडिकल परिवर्तन पर बहुत बल दिया गया था।
इस महत्त्वपूर्ण उपन्यास में सुभाष चन्द्र बोस को काँग्रेस से निकाले जाने की कथा को तो विस्तार से दिया ही गया है,1942 के आन्दोलन और 1942 से 1947 के बीच के वर्षों में साम्प्रदायिक माहौल और राजनीतिक रूप से स्वाधीन होने की प्रक्रिया पर बहुत ही विस्तृत विश्लेषण भी है। इसमें जिस माहौल का वर्णन है उसमें तत्कालीन राजनीति का जो खाका उभरता है वह बहुत जटिल है। जो लोग लड़ रहे थे वे काँग्रेसी नेतृत्व से बहुत निराश भी थे। उन्हें लगता था कि हम आजादी लड़ कर क्यों नहीं ले सकते? अँग्रेज यूरोप में फँसे हुए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व का यह दायित्व है कि जनता के असन्तोष को नेतृत्व दे। इस सन्दर्भ में यशपाल ने सोसलिस्ट, काँग्रेसी, वामपन्थी और अन्य प्रकार के राष्ट्रवादियों की तो चर्चा की ही है राय (मानवेंद्र नाथ) के समर्थकों की भी विस्तृत चर्चा की है। देखा जाए तो इस पूरे वृत्तान्त में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का प्रश्न है लेकिन ज्यादा जोर आजाद होने के बाद के समय पर है।
इस सन्दर्भ में याद किया जा सकता है कि तीस के दशक की शुरुआत में जवाहरलाल नेहरु ने इलाहाबाद में एक भाषण में कहा था कि हमारे लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तो पुरानी चीज हो चुकी है अब हमको आर्थिक क्रान्ति के बारे में सोचना होगा। यह सही है कि नेहरु ने अपने इस भाषण (जिसे ‘व्हीदर इण्डिया’ के नाम से प्रकाशित किया गया) की स्पिरिट को बाद में कायम नहीं रखा और गाँधी के दबाव के कारण वे नरम हो गये, पर उनसे प्रभावित समाजवादी इसी लाइन पर चलते रहे। उनके लिए भी आजादी तो आएगी ही, असली सवाल था आजादी के बाद क्या होगा, मजदूर किसान को न्याय मिलेगा कि नहीं? उस समय के किसान आन्दोलनों को और किसान नेताओं के भाषणों को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे राजनीतिक मुक्ति के संकल्प से आगे की सोच रहे थे। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं जिससे यह कहना सम्भव है कि सोच यह थी कि भारत में आजादी तो आ ही जाएगी असली सवाल है अँग्रेज से सत्ता किसके हाथ में आएगी। 1935 के एक्ट ने तो इस बात पर मुहर लगा ही दी थी।
यहाँ राजनीतिक इतिहास में बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। इसपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। संक्षेप में यहाँ यह कहा जा सकता है कि काँग्रेस भीतर से दो भागों में विभक्त हो चुकी थी। संगठन पर सरदार पटेल के नेतृत्व में गाँधीवादी सुधारवादी और समझौते से राष्ट्र हित को साधने वालों का नियन्त्रण था। वे समझते थे कि आजादी के लिए व्यर्थ में लड़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक बातचीत ही सबसे अच्छा रास्ता है। वे अपनी सांगठनिक राजनीतिक शक्ति को इतनी बढ़ा लेना चाहते थे कि अँग्रेज झुक जाए। लेकिन नौजवान इससे सन्तुष्ट नहीं थे। वे लड़ना चाहते थे। उनको लगता था कि काँग्रेसी नेतृत्व जनता की भावना के अनुरूप आचरण नहीं कर रही। वे नये भारत के लिए संघर्ष करना जरूरी समझते थे। इस पुराने और नये के बीच संगठन पर कब्जा करने की एक आन्तरिक लड़ाई चल रही थी। सुभाष चन्द्र बोस ने जब इस नेतृत्व के सामने डट जाने का साहस दिखाया तो काँग्रेस नेतृत्व बहुत सतर्क हुआ और येन केन प्रकारेण गाँधी को अपने पक्ष में लाने में सफल हुआ। यह स्पष्ट होते ही कि गाँधी काँग्रेस नेतृत्व के साथ है नरेंद्र देव समेत सोशलिस्ट पीछे हट गये। नेहरु ने भी परिस्थिति का अन्दाजा लेते हुए यही तय किया कि गाँधी के साथ ही रहकर जो किया जा सकेगा वे करेंगे।
बौद्धिक जगत के इस दौर के आपसी द्वन्द्व अगले बीस तीस सालों में बने रहे। इस लेखकीय स्वाधीनता का क्षरण समय के साथ इस तरह होता रहा कि साठ तक आते आते बुद्धिजीवी राजनीति के आगे नहीं पीछे चलने लगे। साठ के दशक में अधिकतर बौद्धिक प्रतिभाएँ अकादमिक फैक्ट्री में गला दिए गये। तीस के उत्तरार्ध से साठ के दशक तक की इस यात्रा में कुल मिलाकर यही स्थिति बनती दिखलाई पड़ती है।
किसी दूसरे सन्दर्भ में अज्ञेय ने 1967 में ही एक बात स्पष्ट रूप से कही थी कि आजादी के पूर्व पत्रकारिता एक आदर्श था और अब यह धन्धा हो चुका है। यह बात कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के उपन्यास भी कहते हैं लेकिन इस ओर ध्यान कम दिया गया कि ऐसा हुआ क्यों? साथ ही यह प्रश्न भी पूछा जा सकता था कि क्या यह अपरिहार्य था और सक्रिय और साहसी बुद्धिजीवी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे? आखिर कोई भी कुर्बानी तभी कर सकता है जब उसे यह लगे कि कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी।
जो बात ठोस रूप में कही जानी चाहिए वह यह कि 1947 के बाद जिसके हाथ में राजनीतिक सत्ता आयी उन्होंने नये भारत की व्यवस्था को इस तरह से संचालित किया जिससे राजनीतिक एकता की रक्षा का उद्देश्य तो पूरा हुआ लेकिन आर्थिक क्रान्ति का वह संकल्प पीछे छूट गया जिसके बारे में 1931 के अपने इलाहाबाद के भाषण में नेहरु ने कहा था।
1947 से 1950 के बीच में जो कुछ हुआ उसमें सबसे केन्द्रीय राजनीतिक व्यक्तित्व सरदार पटेल थे। जिस दृढ़ता से उन्होंने भारत के राष्ट्र राज्य के हित को सबसे ऊपर रखकर काम किया उसकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए। वे और नेहरु दोनों ने मिलकर भारतीय सक्रिय बौद्धिकों के लिए एक व्यवस्था की जिसमें सरकार के सहयोग का विकल्प दिया गया। सिर्फ बौद्धिक ही नहीं काँग्रेस के प्रति जो क्रिटिकल होकर लड़ने वाले राजनीतिक दलों के लोग थे उनको भी सरकार ने अपने यहाँ स्थान दिया। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता से लेकर क्रान्तिकारी आन्दोलन के बड़े लोग भी अब काँग्रेस के एमपी बन गये !
आजाद भारत में जो लोग क्रान्तिधर्मी थे और उसी तेवर को बनाए रखना चाहते थे उनके लिए सरकार बहुत कठोर रवैया रखती रही। धीरे धीरे लड़ने की मानसिकता बौद्धिकों की कम होती गयी और वे स्वाधीन भारत में बौद्धिक आजादी से दूर होते चले गये। लिखने की स्वतन्त्रता का सम्बन्ध सिर्फ कानूनी दबाव से नहीं होता परिवेश से भी होता है। अगर परिवेश में लड़ने वाले की तुलना में मिलाजुलाकर चलने वालों का मान अधिक हो तो धीरे धीरे यह सन्देश चला जाता है कि अधिक रेडिकल होने में कोई फायदा नहीं। लेखक समाज खुद ही अपने को एडजस्ट कर लेता है, किसी सरकारी संस्थान से जुड़ जाता है या किसी सेठाश्रयी संस्था के साथ जुड़ जाता है। सरदार पटेल ने हैदराबाद अभियान के दौरान जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों को खत्म करने के प्रयास को जारी रखा उसने भी एक कड़ा सन्देश दे दिया कि सरकार के साथ लड़ने पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यह बात खुल चुकी है कि स्टालिन से फटकार खाने के बाद हैदराबाद के कम्युनिस्ट सदस्यों ने हथियार डालने का निर्णय लिया। इसके बाद नेहरु ने सख्ती छोड़ी और उनके विशेष प्रयास से बहुत सारे कम्युनिस्टों के प्राण बचे!
भारतीय बौद्धिक समाज में सभी इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जो तैयार नहीं थे उन्हें सरकारों का सहयोग नहीं मिला। राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों को भी सरकारी सहयोग नहीं मिला। स्वाधीनता के बाद भारतीय बौद्धिकों की स्वतन्त्रता कम हुई यह कहने पर बहुत सारे लोगों को यह एक अतिरेकी कथन लगेगा लेकिन इसमें सचाई है। 1930 के उत्तरार्ध में जिस विश्वास और दृढ़ता से इस देश के बौद्धिक सोचते थे वे 1947 के बाद कमज़ोर होते चले गये। इसलिए1937 से 1947 के बीच के लेखन की तुलना में 1947 से 1957 के बीच का लेखन नरम प्रतीत होता है। बहुत सारी किताबों में पिछले दशक की धमक है जैसे ( मैला आँचल) लेकिन फिर एक नयी समन्वय की दृष्टि का विकास राजसत्ता की शीतल छाया में होने का दौर शुरु हुआ जो बदलाव की बात भी करता था और समन्वय की भी। बदलाव और समन्वय में धीरे धीरे दूसरा पक्ष अधिक प्रबल होता गया।
इस पूरे प्रसंग में इस बात को भी याद रखा जाना चाहिए कि साहित्यकार के लिए राष्ट्र हित को ध्यान में रखना उचित है या कि उसके आदर्श इससे भी ऊँचे हो सकते हैं। याद किया जा सकता है गोएटे को। गोएटे ने अपने देश प्रशिया (जर्मनी) पर फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के आक्रमण की बात सुनी तो उन्हें इस बात की प्रसन्नता हुई थी कि फ्रांस के विजय के बाद उनके देश में फ्रांस की क्रान्ति से उपजे नये विचार प्रविष्ट होंगे और उसे नये विचारों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। गोएटे को जर्मनी के सबसे बड़े साहित्यिक के रूप में देखा जाता है इसलिए इस बात का विशेष महत्त्व है कि वे अपने राष्ट्र की सैनिक पराजय को अपने देश के लिए शुभ मान रहे हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर भी उस समय जब राष्ट्रवाद की ओर तेजी से बढ़ रहे थे उन्हें यह जरूरी लगा कि वे राष्ट्रवाद के आसन्न खतरों से अपने पाठकों को सावधान कर सकें। टॉलस्टाय ने तो राष्ट्रवाद को ही अशुभ माना था। ये तीन बड़े साहित्यकारों के उदाहरण इसलिए दिए जा सकते हैं ताकि यह कहा जा सके कि साहित्यकार राष्ट्र राज्य के सत्ता धारी प्रभुओं के पीछे चलने वाले रहे हों ऐसा नहीं है।
जैनेन्द्र ने 1967 में ही यह पूछे जाने पर कि जब उनसे पूछा गया कि अगले तीस वर्षों के बाद वह कैसा समय देख रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि दो सभ्यताओं के बीच में टक्कर होगी। जिन दो संस्कृतियों का उन्होंने उल्लेख किया था उन्हें उन्होंने ‘साहित्यिक संस्कृति’ और ‘वैज्ञानिक (यान्त्रिक) संस्कृति’ कहा था। उनका मानना था कि इन दोनों के बीच में ही भिड़न्त होगी और लोगों को अपने चुनाव करने होंगे। 1967 में जैनेन्द्र के इन विचारों को आज हम याद करें तो हम स्पष्ट देख सकते हैं की वह साहित्यिक संस्कृति और वैज्ञानिक (यान्त्रिक) संस्कृति के बीच के तनाव को स्पष्ट रूप से देख रहे थे और आने वाले समय में इन दोनों के बीच के चुनाव के बारे में भी सोच रहे थे।
क्या यह कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे समय बीतता गया साहित्यिक संस्कृति कमजोर होती गयी और समाज वैज्ञानिक (यान्त्रिक) संस्कृति की ओर ज्यादा बढ़ता गया। इस क्रम में स्वतन्त्रता साहित्यकार के लिए भी धीरे-धीरे इसी रूप में ज्यादा महत्त्वपूर्ण बनी रही जिसमें समाज और राज्य सत्ता की स्वीकृति समाहित हो। इस कारण से आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि साहित्यिक संस्कृति का स्वायत्त संसार धीरे-धीरे यान्त्रिक संस्कृति के अधीन अपने को पा रहा है। भारतीय बौद्धिक वर्ग साहित्यिक संस्कृति से अब दूर होने में ही अपनी भलाई मान रहा है। यह निश्चित रूप से कोई शुभ लक्षण नहीं है अगर समाज को सही दिशा में मशाल बनकर मार्ग दिखलाने का कार्य भार साहित्य का है, जैसा कि प्रेमचन्द समझते थे।
हमारे पास ऐसे साहसी और सक्रिय साहित्यकारों के उदाहरण हैं, जिन्होंने (टॉलस्टाय) रूस में रहकर जार का विरोध करना जरूरी समझा। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान जब पूरा देश गाँधी के पीछे चल रहा था तब उनसे असहमत होने का नैतिक साहस रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दिखलाया। जब पूरा देश गाँधी की जय जयकार कर रहा था उस समय यशपाल ने ‘गाँधीवाद की शव परीक्षा’ जैसी किताब लिखने की हिम्मत की, इतना ही नहीं जब जवाहरलाल नेहरू का विरोध करना बहुत मुश्किल था, उस समय उन्होंने ‘झूठा सच’ जैसा उपन्यास लिखकर बौद्धिक दुनिया में नेहरू को कटघरे में खड़ा कर दिया।
इस तरह के उदाहरण और भी दिए जा सकते हैं। ऐसे साहित्यकारों की परम्परा में अपने को रखकर आज का साहित्यिक समाज अगर साहित्यिक संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तुत हो तो कोई कारण नहीं है कि वह अपने समाज में एक नयी रोशनी दिखलाने की कोशिश में अपने को खड़ा न पाएगा। साहित्यिक संस्कृति वैज्ञानिक (यान्त्रिक) संस्कृति के सामने विकल्प बनकर उभर सके यही साहित्यिक स्वतन्त्रता के लिए सबसे जरूरी है।