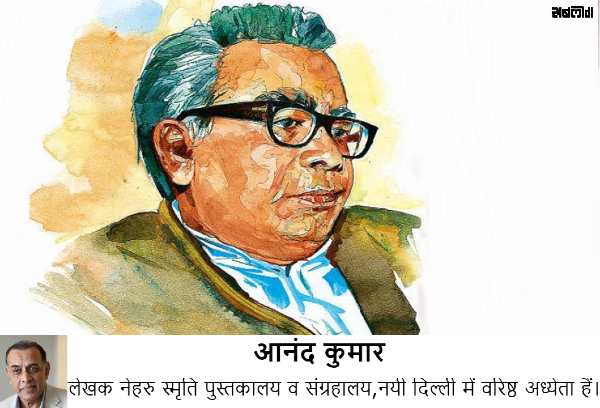भारतीय मूल्यदृष्टि का वर्तमान
- रमेश चन्द्र शाह
भारत के सामाजिक इतिहास की लय-गति पश्चिम से बहुत अलग है। वहाँ ‘राज्य’ यानि स्टेट की भूमिका बहुत प्रबल है और सत्ता-संघर्ष भी बहुत उग्र रहा। तर्क-बुद्धि को वहाँ शुरू से ही निर्णायक महत्व मिला है, मगर साथ ही, धर्म विश्वास के स्तर पर मतवाद या ‘डागमा’ को हर तर्क से परे प्रश्नातीत मान कर चलने का आग्रह भी वहाँ उतना ही चरम है।
इसके विपरीत भारतीय अन्तःकरण सामाजिक सम्बन्धों को सहज अन्तर्ज्ञान से निबाहने और यथासंभव विरूद्धों के सामंजस्य पर बल देता रहा है।यहाँ मानुष-भाव का निर्वाह भी ‘जियो और जीने दो’ की बुनियादी साझेदारी के बूते चलता रहा – उसके पीछे दृष्टि मानव-केन्द्रित, मानववादी नहीं, अपितु चराचर निष्ठ, चराचरवादी रही है। संस्कृति की मूल प्रतिज्ञा भी सर्वभूतहितेरतः के भीतर से ही आत्म-साक्षात्कार करने की रही।
श्री अरविन्द ने कहा था – ‘आधुनिक जगत पर पश्चिमी विचारों का अनुचित आधिपत्य है। हम इसका प्रतिकार करते हुए भारतीय मूल्य-दृष्टि का महत्त्व फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ………….कि किस तरह एक दूसरे स्तर पर महात्मा गांधी ने भी लगभग ऐसा ही अनुभव करते हुए पश्चिम-प्रेरित आधुनिकता का कठोर प्रत्याख्यान करते हुए लगभग यही बात कही है किन्तु आज के सामान्य भारतीय आचरण में इन दोनों विचार-सरणियों के लिए कोई गुंजाइश दिखती है ? क्या सोरोकिन द्वारा निरूपित ‘सेंसेट कल्चर’ (ऐंद्रिक भोगवाद) का भी वही तांडव हमारे यहाँ भी हावी होता नहीं लगता? इस सर्वग्रासी तूफान मेँ अब हमारी भूमिका क्या निरीह दर्शक या आत्महीन नकलची की ही रह गई है? याकि इस मूल्यमूढ़ता को मूल्यों के पुनर्वास की ओर मोड़ने की अभी भी कोई गुंजाइश बची है?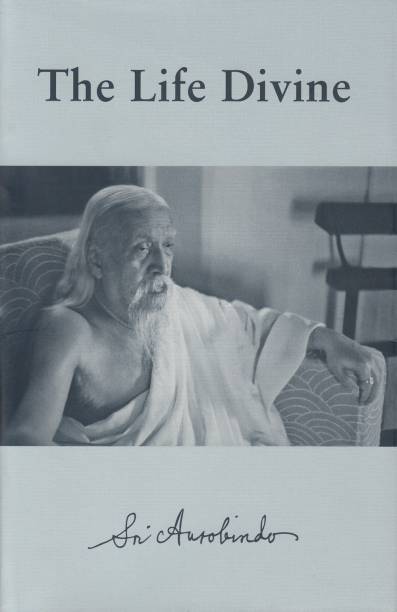
भारतीय दृष्टि ‘जीवन की समग्रता” पर ज़ोर देती रही है प्रारम्भ से ही – एकांगिता को नकारते हुए। पर क्या हमारी संस्कृति भी कालान्तर में एक दूसरी एकांगिता से ग्रस्त नहीं हुई? श्री अरविंद ने अपने ‘दि लाइफ डिवाइन’ में जहाँ एक ओर पाश्चात्य सभ्यता के भौतिक नकारवाद को रेखांकित किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सभ्यता की अधोगति को भी ‘असेटिक डिनायल’ अर्थात जीवन-देवता के ‘सन्यासमुखी तिरस्कार’ की तरह परिभाषित नहीं किया है ?क्या हमारी मौजूदा हालत उसी तिरस्कार का कुफल नहीँ है? आखिर हमारे एक प्रमुख मनीषी गोविन्द चन्द्र पाण्डेय ने अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ ‘भारतीय परम्परा के मूल स्वर’ में ठीक इसी हकीकत पर तो उंगली रक्खी है – यह कहते हुए कि “ मध्य युग में भारत वैदिक सम्पूर्णता के आदर्श से स्खलित होकर विश्व मिथ्यात्व की दलदल में जा धंसा।“ तभी न जयशंकर प्रसाद की एक आरंभिक कविता कहती है – ‘ऐसों ब्रह्म लेइ का करिहैं / जो जन-पीर न हरिहैं ?’ यह भी देखिये कि जहाँ सांख्य दर्शन के अनुसार “यह दुनिया कभी बदलने वाली नहीं है, ऐसी ही रहने वाली है” (‘न हि कदाचिदनीदृशंजगत’) वहीं, इसके ठीक उलट हमारा यह आधुनिक ऋषि स्वयं आध्यात्मिक साधना को जीवन के सम्पूर्ण कायाकल्प के साधन की तरह प्रयोग करने की जरूरत को रेखांकित कर रहा है।

तो, यही वह इतिहास लभ्य पीठिका है, जिस पर हमें अपने वर्तमान और भविष्य के विचार और कर्म को प्रतिष्ठित करते हुए आगे की राह निकालनी है, हमें अपने मौलिक विचारकों और कर्मज्ञों पर ध्यान देना चाहिए- जो हम नहीं देते। विद्यानिवास मिश्र यूं ही नहीं कहते कि “दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिरोध पश्चिमी सभ्यता को भारत ने दिया, किन्तु, दूसरी ओर, सबसे सहानुभूति पूर्वक पश्चिम को समझने वाले भारतीय ही हैं।“ वे साफ –साफ चेताते हैं कि “न तो पश्चिम के ऊपर अपनी आध्यात्मिकता का रौब डालने से काम चलने वाला है, न अपनी परम्परा को – भारतीयता को कोसने से,”स्वातन्त्रयोत्तर भारत दुर्दशा को भी उन्होंने ध्यातव्य आँका है- “हम अनेक में एक की बात करते हुए परस्पर आक्रामक और संशयालु हो गए हैं, अनेकवादी और आपस में ही आक्रामक हो गए हैं। यह भी,कि “हमारे देशवासी छोटे-छोटे सुरक्षा के घेरे बनाकर मारे डर के उन्हीं में छिपने के आदी हो गए हैं।“ किसी ने भी इन घरौंदों के अलावा कोई सुरक्षा का अवसर पैदा नहीं किया। उल्टे घरौंदों के बल पर ही शक्ति संतुलन हो सकता है, राजनीतिक स्थिरता बनी रह सकती है, यही स्थिति हमने स्वीकार कर ली है।“
स्वाधीनता-पूर्व भारत में जिस मौलिक राष्ट्र-बोध का जागरण हुआ था वह बाद में उत्तरोत्तर शिथिल होता गया है तो इसके पीछे अज्ञेय ने जिस ‘आलोचक राष्ट्र’ के निर्माण की बात उठाई थी- स्वतन्त्रता की देहरी पर ही- उसकी भी सरासर अनदेखी भी बड़ा कारण रही है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं, वह वैचारिक स्वराज के बिना कैसे सुदृढ़ हो सकती है? इस भयानक विपर्यय को तो देखिये जरा। जनमानस में अधिकारों की चेतना जिस अनुपात में बढ़ी है, कर्तव्य चेतना क्या ठीक उसी के उल्टे अनुपात में लगातार नहीं सिकुड़ती गई है? सर्वाधिक शोचनीय स्थिति तो सांस्कृतिक समृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ‘शिक्षा’ की ही गुणवत्ता के निरंतर ह्रास और विघटन की है। विडम्बना तो देखिये, कि अकादमिक ही क्यों, स्वयं साहित्यिक क्षेत्र में भी ऐसे ही लोगों की घुसपैठ और दबदबा बढ़ता गया है, जो न केवल जिस चराचर वादी चेतना के बूते भारत है, और गहरे में ऐक्यमूलक भी, उसी मूल और मूल्य-चेतना और एकता की जड़ खोदने में जुटे रहते हैं, ये परोपजीवी जोकों की बिरादरी वाले बुद्धिजीवी वास्तविक वैचारिक स्वराज के सबसे भीतरघाती दुश्मन हैं, इस तथ्य को जानते-बूझते नजरंदाज किया जाता रहा है कई दशाब्दियों से। इनके लेखे भारतीय संस्कृति अनेक समुदायों के सतही समझौतों से उपजी एक मनमाने जोड़-तोड़ की सुविधाभोगी व्यवस्था भर है, जिसे वे घोर पुण्यात्मा आत्म तुष्टि के साथ कम्पोजिट कल्चर (सामासिक संस्कृति) बखानते नहीं थकते। किसी ने बिलकुल सही कहा है कि “ सामासिकता के नाम पर भारतीय संस्कृति की मुख्यधारा की निरंतर उपेक्षा होती रही है और यही हमारे देश और समाज की ट्रेजेडी है।“ गीता में जो जबर्दस्त यथार्थवादी चेतावनी दी गई है कृष्ण द्वारा कि ‘ समाज के तथाकथित श्रेष्ठ जन जैसा करते-बरतते हैं, बाकी सारे लोग उन्हीं का अनुकरण करने को बाध्य होते हैं (यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजन:, स यत्प्रमाणङ्कुरुते लोकस्तदनुवर्तते) हमारे साथ ठीक वही हुआ और हो रहा है। ठेठ आज की तारीख में भी। स्वयं तथाकथित हिन्दुत्ववादियों में भी ऐसे लोग खोजना कठिन होगा जिन्हें आनन्द कुमारस्वामी या वासुदेवशरण अग्रवाल या प्रसाद-निराला ….अज्ञेय सरीखे लेखकों का ही नहीं, अभी हाल के राजीव मल्होत्रा सरीखे सत्य शोधकों के किये-धरे का भी सचमुच पर्याप्त गुण-ज्ञान हो। तथाकथित आइडियोलाजी भले वह ‘हिन्दुत्व’ की ही क्यों न हो, वास्तविक विचार शक्ति का पर्याय कदापि नहीं हो सकती।
सर्वाधिक शोचनीय स्थिति तो सांस्कृतिक समृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ‘शिक्षा’ की ही गुणवत्ता के निरंतर ह्रास और विघटन की है। विडम्बना तो देखिये, कि अकादमिक ही क्यों, स्वयं साहित्यिक क्षेत्र में भी ऐसे ही लोगों की घुसपैठ और दबदबा बढ़ता गया है, जो न केवल जिस चराचर वादी चेतना के बूते भारत है, और गहरे में ऐक्यमूलक भी, उसी मूल और मूल्य-चेतना और एकता की जड़ खोदने में जुटे रहते हैं, ये परोपजीवी जोकों की बिरादरी वाले बुद्धिजीवी वास्तविक वैचारिक स्वराज के सबसे भीतरघाती दुश्मन हैं, इस तथ्य को जानते-बूझते नजरंदाज किया जाता रहा है कई दशाब्दियों से। इनके लेखे भारतीय संस्कृति अनेक समुदायों के सतही समझौतों से उपजी एक मनमाने जोड़-तोड़ की सुविधाभोगी व्यवस्था भर है, जिसे वे घोर पुण्यात्मा आत्म तुष्टि के साथ कम्पोजिट कल्चर (सामासिक संस्कृति) बखानते नहीं थकते। किसी ने बिलकुल सही कहा है कि “ सामासिकता के नाम पर भारतीय संस्कृति की मुख्यधारा की निरंतर उपेक्षा होती रही है और यही हमारे देश और समाज की ट्रेजेडी है।“ गीता में जो जबर्दस्त यथार्थवादी चेतावनी दी गई है कृष्ण द्वारा कि ‘ समाज के तथाकथित श्रेष्ठ जन जैसा करते-बरतते हैं, बाकी सारे लोग उन्हीं का अनुकरण करने को बाध्य होते हैं (यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजन:, स यत्प्रमाणङ्कुरुते लोकस्तदनुवर्तते) हमारे साथ ठीक वही हुआ और हो रहा है। ठेठ आज की तारीख में भी। स्वयं तथाकथित हिन्दुत्ववादियों में भी ऐसे लोग खोजना कठिन होगा जिन्हें आनन्द कुमारस्वामी या वासुदेवशरण अग्रवाल या प्रसाद-निराला ….अज्ञेय सरीखे लेखकों का ही नहीं, अभी हाल के राजीव मल्होत्रा सरीखे सत्य शोधकों के किये-धरे का भी सचमुच पर्याप्त गुण-ज्ञान हो। तथाकथित आइडियोलाजी भले वह ‘हिन्दुत्व’ की ही क्यों न हो, वास्तविक विचार शक्ति का पर्याय कदापि नहीं हो सकती।
अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा पद्धति का एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीयों में अपनी ही संस्कृति-सभ्यता को लेकर हीन-भाव के साथ –साथ पाश्चात्य सभ्यता के प्रति समर्पण और अनुकरण लिप्सा विकसित हो। मानना होगा कि उनकी यह मंशा बावजूद श्री अरविंद और महात्मा गांधी सरीखे मार्ग द्रष्टाओं के खूब फली-फूली। सच पूछा जय तो वर्तमान शिक्षा गुलामी के दिनों की शिक्षा पद्धति से भी कहीं अधिक संस्कार-विहीन और भ्रष्ट साबित हुई है। क्योंकि इस शिक्षा में भाषा का बुनियादी महत्व ही मिटा दिया गया है। इस विडम्बना को भी पहचानना है कि भारत में अपनी भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान तो काफी दृढ़ रही किन्तु उसकी अपनी सांस्कृतिक …..शक्ति के अनुरूप राजनैतिक शक्ति के यथार्थ की …..अभाव ही रहता आया। निराला की शक्ति पूजा का वह महा वाक्य – ‘शक्ति की करो मौलिक कल्पना ‘अब हमारा दिशा निर्देशक सूत्र होना चाहिए। प्रसाद के ‘स्कंदगुप्त’ में चित्रित आपसी फूट, विश्वासघात और देशद्रोह का कुचक्र क्या जताता है? हिन्दुओं में और उनके तथाकथित हिन्दुत्व में ऐसी क्या दुर्बलता है कि उनका संगठित होना ही मानो एक दूसरी समस्या उपजा देता है और इस तरह उन्हें नहीं फलता जिस तरह वह बिखरी दूसरी जतियों-समुदायों को फलता रहा है। क्या महान आत्म-बलिदानी सिक्ख पंथ के अभ्युदय-काल में उसकी खालिस्तानी परिणति की कोई कल्पना भी कर अकता है? ठीक इसी जगह हमें अज्ञेय के आलोचक राष्ट्र के निर्माण का आह्वान प्रखर-.प्रासंगिक लगने लगता है। ताकि हमारे घर के भेदिये नहीं बल्कि घर के आलोचक ही हमारे लिए पुष्टिकारी बनें। हमें अपने समूचे इतिहास का मंथन करते हुए उस प्रवृत्ति से सावधान रहना होगा जो एक ओर तो आत्मभ्रामक आत्मतुष्टि का शिकार हो जाती है और दूसरी ओर हीन भाव प्रेरित परोपजीवी बौद्धिक अहमन्यता के वशीभूत होकर अन्तर्घात का विष-वमन करती रही है।

अधिकारी विद्वान गोविन्द चन्द्र पाण्डेय जी का यह कथन एकदम सही है कि भारतीयता और भारतीय संस्कृति मानवता की पारमार्थिक विकास-साधना की धारा है। इसका साधना-मार्ग मात्र इतिहास-चक्र आश्रित और अनुवर्ती नहीं है, इसका अर्थ आज की तारीख में कार्यरत हम भारतीयों के लिए यही न हुआ कि जिन मनीषियों-कर्मज्ञों के जीवन और कृतित्व में भारतीयता का यह सदा सृजनशील स्वरूप साक्षात चरितार्थ होता रहा है, उन्हें हमें फिर से अद्यतन बुद्धिमत्ता और कर्म-कौशल के जरिये अर्जित और स्वायत्त करना। साहित्य समेत सभी क्षेत्रों के महारथियों-अतिरथियों के जिन्दा प्रमाण को गंभीरता पूर्वक स्वायत्त करना चाहिए—उस अधूरे पुनर्जागरण को पूरा करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए। निस्संदेह हमारा भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अपना शासन तो लोकतान्त्रिक पद्धति से न्यूनाधिक सफलतापूर्वक चलाता रहा है परन्तु शैक्षिक-सांस्कृतिक-चारित्रिक यांत्रिकता और अराजकता के फलस्वरूप गंभीर अन्तर्विरोधों-अन्तर्द्वंद्वों से भी पटा हुआ है। इसलिए आत्मालोचन और कर्तव्य चेतना का पुरुषार्थ हमारे लिए आज की तारीख की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इत्यलम।

लेखक प्रसिद्द साहित्यकार हैं|
सम्पर्क- +919424440574, rcshahaakhar@gmail.com
.