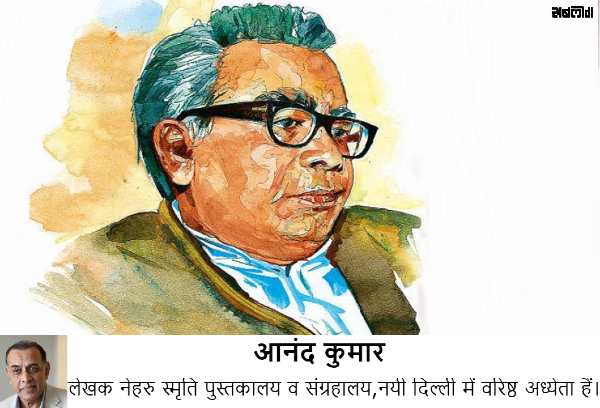स्वाधीनता और संस्कृतिकर्मी
स्वाधीनता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जब हम भारतीय समाज के वर्तमान पर दृष्टि डालते हैं तो हमें काफ़्का के नायकों की याद आती है। काफ़्का के नायकों को अपने ढंग से समझते हुए इवान क्लीमा ने कहा था कि ‘उसके नायकों की परेशानी यह नहीं है कि वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते, बल्कि उनकी परेशानी का कारण यह है कि वे वास्तविक दुनिया में ठीक ढंग से रहकर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में अक्षम हैं।’
चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध आलोचक और नाटककार इवान क्लीमा की राय को अपने सन्दर्भों में देखने पर कई दिलचस्प निष्कर्ष सामने आते हैं। पर उन निष्कर्षों को थोड़ी देर के लिए छोड़कर भी देखें तो क्या यह नहीं लगता कि आज के भारतीय समाज में अपनी सचाई को जीते हुए व्यक्ति का अपेक्षित कर्त्तव्य निर्वाह सम्भव नहीं है? गाँव से कस्बा और नगर से महानगर तक इस विडम्बना के कई रूप दिखाई दे सकते हैं। ईमानदार रहकर जीना सम्भव नहीं रह गया है और जीते हुए ईमानदार रह पाना। जो जितना स्वच्छ दिखना चाहता है, उसे उतना ही कुटिल हो जाना पड़ता है। हर तरफ बेपनाह आकांक्षाएँ बल मार रही हैं। साधन कम हैं, जीने के बेहतर तरीके की स्थितियाँ भी कम हैं। ऐसे माहौल में जब समाज, जीवन की आपाधापी में उलझा है-संस्कृति की परिवर्तनकामी धारणाओं का क्या हो? – यह एक कठिन प्रश्न है।
उपभोक्तावादी शिकंजे में कसे रहकर व्यक्ति इतना क्षरित हुआ है कि वह मूल्य विपर्यय का ही शिकार हो गया है। छोटी-छोटी ज़रूरतों के बीच न चाहते हुए भी वह समझौते करने को विवश है और उससे अनैतिक कहे जानेवाले कर्म हो जाया करते हैं। बावजूद इसके उस व्यक्ति को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं माना जाता। यह विडम्बना है और वह व्यक्ति सिर्फ इस आचारवादी निर्धारण के समक्ष एक चुनौती की तरह खड़ा रह सकता है, यह जरूरी नहीं कि आचारवाद उसे चुनौती मानने को विवश हो। यह विडम्बना का एक दूसरा स्तर है।
यह व्यक्ति जो अवश और विवश है, वह कोई और नहीं, वही सामान्य व्यक्ति है जो गाँवों में रात-दिन एक करके काम करता है और कस्बों, शहरों में भविष्य की उम्मीदें पाले जीता है। इसे न दल की चिन्ता है और न विचारधारा की और न क्षुद्र स्वार्थी राजनीति की। उसके जीवन के पाले में ऐसी तकलीफदेह कील है जो उसके कन्धों को असहनीय चुभन देती है, पर वह मजबूर है कि अपना कन्धा साहस के साथ वहीं टिकाए रखे। अगर वह पाला बदलता है या कील से ज़ख्मी होने की चिन्ता करता है तो वह अपनी और अपने परिवार की ख़ैर मनाए, दो वक़्त की रोटी भी तब शायद ही मयस्सर हो। यह ठीक दूसरे की शर्तों पर जीने का वाजिब उदाहरण है जो औसत भारतीय कहे जाने वाले लोग जीते हैं या जिनके लिए साहित्य सरोकारों की बात करता है। अब प्रश्न यह है कि ये लोग, यह समुदाय, जो पश्चिम में अट्ठारहवीं शती में और भारत में उन्नीसवीं शती के अंत में मध्यवर्ग माना गया, कहाँ तक हमारे साहित्य का हिस्सा बन पाया है? आज़ादी के बाद इस बृहत्तर समुदाय के जीवन स्तर में कई तरह के बदलाव लक्षित हुए हैं। उच्च वर्ग के बहुत आगे निकल जाने के बाद संसाधनों की कमी तथा जनसंख्या की बेपनाह वृद्धि के कारण यह वर्ग धीरे-धीरे पिछड़ता हुआ मध्य वर्ग से निम्न मध्यवर्ग में आ पहुँचा है जहाँ जरूरतें तो बढ़ी हैं, पर उसकी पूर्ति के साधनों में भारी गिरावट आई है। कुछ सर्वेक्षणों से तो यह निष्कर्ष सामने आया है कि भारतीय विकास दर की न्यूनतम गति तेज़ी से मध्यवर्ग के क्षय का परिणाम है। मूल्यों में ह्रास, नैतिक मानदंडों की पतनशीलता तथा पारिवारिक विघटन का एक बड़ा कारण निम्न मध्यवर्ग का उभार है क्योंकि यहाँ न तो परवाह की मर्यादा का बोध होता है और न सामाजिकता का दबाव। यही कारण है कि सारे विकास के लटकों के बावजूद समाज में कोई गुणात्मक सुधार की गुंजाइश कम ही प्रभावी हो पाई है।

राजनीति तो ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहाँ समाज में न्यून मात्रा में प्राप्त साम्प्रदायिक विद्वेषों और जातिवादी सोचों में से किसी न किसी को तूल देकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। केन्द्रीय और क्षेत्रीय राजनीति के निशाने पर आज यही दो तत्त्व लाभकर प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए व्यवस्था की वर्तमान दिशा यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि यह सारा राजनीतिक तामझाम देश की खुशहाली के लिए है या सत्ता का निष्कंटक खेल चलाने देने के लिए? बार-बार जिस लोकतान्त्रिक और संसदीय पद्धति की असफलता का ज़िक्र हो रहा है, उसमें कोई भी आगे बढ़कर यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि असफल तो सत्ता के वृत्त में घूमनेवाले नेता हो गए हैं जिन्होंने जनता को सेवक और अपने को तानाशाह बना लिया है। इसके विपरीत आर्थिक उदारीकरण का व्यापक खेल खेलकर स्वदेशी उद्योगों को नष्ट करने की युक्तियों पर काम हो रहा है। भारतीय भाषाओं, संस्कृति और चिन्तन के दरवाजों पर पश्चिमी प्रभाव की ऐसी जबर्दस्त दस्तक पड़ी है कि अब शायद ही भारतीय बुनियाद का ताना-बाना रह पाए।
ऐसी स्थिति में भारत का व्यक्ति किस क्रान्ति का पैरोकार बनेगा, यह तो समय ही बताएगा पर यह दिखाई दे रहा है कि उसके आगे अंधेरा है और दूर-दूर तक रौशनी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसमें पराजित नायकत्व ही दिखाई दे सकता है; शौर्य में मदमस्त कोई विद्रोही या नायकत्व देनेवाला भले ही अपवाद में लक्षित हो। हर नायक अपनी खोल में सिकुड़ा पराजय की मार झेलने को विवश और समझौते के लिए तैयार बैठा है। वर्षों पहले ‘आधे अधूरे’ नाटक में मोहन राकेश ने जिस महेंद्र को सिरजा था, आज गली-मुहल्ले का रचित चरित्र बन चुका है। उसमें संवेदना तो है, पर आँखों में सूखे आँसू हैं। ज़िल्लत और जहालत में जिसकी आत्मा गिरवी रख दी गई है, जो अपने विवेक से निर्णय तक नहीं ले पाता। जो जीवन में शुरू तो होता है आक्रामक होकर पर उसकी परिणति टूटन में होती है।
सचाई का पक्ष तो और भी मारक है। तब दर-ब-दर भटकने की जगह भी नसीब न हो शायद। आज का नायक ‘अंधा युग’ का वह युयुत्सु भी है जो असत्य के लिए भाइयों का भी साथ छोड़ता है और सत्य के पक्ष को लेकर लड़ रहे पांडवों का साथ देता है, पर पाता है वहीं प्राणघातक उपालम्भ, यातना, जीता है वही क्रूर विडम्बना कि जिसके हाथ जीत भी आकर बन गई है शर्मनाक पराजय। माँ भी जिससे घृणा करती है: पिता भी उसकी आवाज से घृणा करता है और पांडव खेमे से पाता जाता है तिरस्कार, जिसके कारण वह आत्महत्या करता है। धर्मवीर भारती की पंक्तियां बरबस याद आती हैं- “अन्तिम परिणति में दोनों ही जर्जर करते हैं-पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का।”
आज के भारतीय समाज का एक पक्ष विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास ‘नौकर को कमीज’ में दिखाई देता है जिसका नायक किराए के मकान की टपकती छत से जरूरी सामान को सहेजने में ही जीवन गुप्तार देता है, जिसकी कमाई से दो प्राणियों के पेट तक ठीक से नहीं भरते और जिसकी सारी सोच इसी उधेड़बुन में खप जाती है। आज का नायक वह अभागा क्लर्क संतू ही लगता है जिसका ‘देश’ उसका टपकता, उजाड़ किराए का खपरैल-घर है और ‘संसार’ म्यूजियम सी शक्लवाला वीरान दफ्तर, जहाँ ऐसी ही दुनिया के लोगों का ठिकाना है जिनके लिए पेटभर अन्न, पहनने को कपड़ा और सवारी के लिए साइकिल भी एक सपना है। क्या ये हमारी कथित क्रान्ति के नायक लगते हैं, जिन्हें राजनेता और बुद्धिजीवी वर्षों से ढोल पीटकर जगा रहे हैं? समाज को विभिन्न कोणों से देखने के बाद यही सचाई सामने आती है कि उसमें जीनेवाले व्यक्ति की कल्पना भी खंडित हो रही है, सपनों की तो बात ही और है।

भारतीय समाज का किसान कहा जानेवाला तबका तंगी और स्रोतों के अभाव में न तो खेतिहर मजदूर बन पा रहा है और न किसान रह गया है। जिनके पास मुकम्मल जमीनें हैं, वे उसे दखल और आबाद कर पाने में ही असमर्थ हो गए हैं, उसमें जायदाद के जरिये लाभ कमाना तो दीगर मामला है। ठीक ठाक भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा न कर पाने के कारण देश का यह बड़ा वर्ग झूठी राजनीति के सब्जबागों से निराश हो चुका है। उसमें भी साम्प्रदायिक और जातीय विद्वेषों ने उसकी दरकिनार जिन्दगी को भी नरक बना छोड़ा है। वह किससे अपनी बात कहे और उसके लिए लड़े कौन? सरकारी कर्मचारियों की तो यूनियनें हैं, वे हड़ताल करते हैं, अपनी मांगें मनवाने के उनके पास अनेक उपाय हैं, पर ये किसान तो सिर्फ बढ़ती जाती महँगाई और तत्काल प्रभाव से लागू होते जाते अध्यादेशों के गुलाम हैं। उन्हें जो लादो जाय वह ढोना है क्योंकि उनके प्रतिनिधियों ने यह छवि स्थाई कर ली है कि वे झूठे वायदे करने वाले मतलबपरस्त नेता हैं जो प्रतिबद्धता के नाम पर भाषण दे सकते हैं और जनसेवा के नाम पर सम्बंधित इलाके का दौरा।
ऐसे में वातानुकूलित सभागारों में चलनेवाली बहसों और किताबों के जरिये किए जाने वाले आह्वानों का कितना और क्या मतलब है, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हिन्दी समाज का साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी और जनता की लड़ाई का दम भरनेवाले क्रान्तिचेता कितने बेमानी होते जा रहे हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। साहित्य से बृहत्तर समाज का जीवन, उसका अंतद्वंद्व गायब हो रहा है। उसकी जगह शहरों की बासी अनुभूतियों को जगह देने की बाढ़ आई है। संस्कृतिकर्मी धुआँ होती जा रही भारतीय संस्कृति को पकड़ने की ताक में हैं और क्रान्तिचेता जनपक्षधरता के नाम पर लोगों को अपने स्वार्थों के लिए गोलबन्द करने में जुटे हैं। जितने पंथ, उतने नायक और एक-दूसरे के शत्रु। बुद्धिजीवियों की सारी लड़ाई अवसर पाने तक सीमित हो चुकी है जिसमें हिन्दी सिर्फ हथियार रह गई है “धार तो अंग्रेजी से ही आती है।
इन परिस्थितियों में समूचा देश अगर न सही तो कम से कम हिन्दी समाज, काफ़्का के उपन्यासों का क्षेत्र ही लगता है जिसमें संघर्ष करता हुआ नायक चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है जो कहीं से निकलने का रास्ता नहीं पाता। वह अपने लक्ष्य तक इस संघर्ष से पहुंचेगा कि नहीं, यह तो उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, पर वह सही ढंग से जी भी नहीं पाता। सही ढंग से जीना ही उसके लिए एक सपना है, सपनों की दुनिया है। क्या हम सपनों की दुनिया में भी जीने का खयाल कर पा रहे हैं या कि वे भी हमें डराने लगे हैं?
इस पर अब नए सिरे से विचार होना चाहिए। हमें लगता है कि भारतीय स्वतन्त्रता के पचहत्तरवें वर्ष को स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए जो कि दुर्भाग्य से हमने हासिल नहीं किया है और न हम स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के बुनियादी फर्क को ही समझ पाए हैं। यह समझ तब बन सकेगी जब खुली आँखों से हम वर्तमान से भविष्य को देखने की कोशिश करेंगे और अतीत के उन सपनों को याद करेंगे जिनके लिए हमारे पुरखों ने लंबा संघर्ष किया था। इस दिशा में सोचने की प्रक्रिया तो शुरू होनी ही चाहिए। यह वर्ष अगर हममें यह प्रेरणा भी न दे सका तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा।