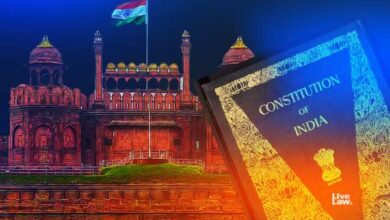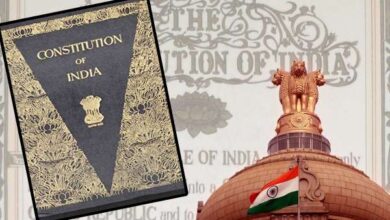एक चुनाव दूसरे चुनाव के लिए
मतदाता क्या अगली पीढ़ी को यह भरोसा दिलाता है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के अपने फैसले से नागरिक समाज के बनने में सहायक होने की जिम्मेदारी पूरा करेगा, यह एक बड़ा सवाल यहां उठाना चाहते हैं। चुनाव अगले चुनाव के लिए हो रहे हैं, विचारों को चुनावी समाज तक सीमित कर देने के गंभीर नतीजे दिखने लगे हैं। (लेखक)
हम पांच राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव के नतीजे और उसके 2024 के लोकसभा चुनाव पर होने वाले असर को लेकर बातचीत करने की सीमा में बंधे हुए हैं। राज्यों में लड़ाई तीन तरफा हैं। एक तरफ दो राष्ट्रीय स्तर की कही जाने वाली पार्टियां- काँग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ वे पार्टियां हैं जिन्हें हम राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टिया कहते हैं। लेकिन गणतन्त्र में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो अवधारणा होती है उस स्वर का प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय पार्टियां ही करती है। राष्ट्रीय पार्टियां आखिरकार सत्ता के केन्द्रीकरण के पक्ष में होती है। काँग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सत्ता के अनुभव से भी यह हासिल होता है।
दूसरी बात कि भारतीय चुनावी राजनीति में यह मान लेना कि राज्यों के चुनाव नतीजे संसद के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, यह पक्के तौर पर हीं कहा जा सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्य स्तरीय जीत हो सकती है लेकिन दिल्ली में लोकसभा में एक भी सीट पर कामयाब नहीं हो सकती है। ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं। चुनावी लोकतन्त्र के शुरुआती दौर में यह धारणा बनी थी कि किसी उपचुनाव के नतीजे भी संसदीय चुनाव के नतीजों के संकेत दे सकते हैं। मसलन जब चिकमगलूर से इंदिरा गांधी ने लोकसभा के लिए चुनाव जीता तो यह संकेत मिलने लगे थे कि 1977 में बुरी तरह से पराजीत होने वाली इंदिरा गाधी और उनकी पार्टी की 1980 में ही शानदार वापसी हो सकती है। राज्यों के लिए किसी अन्य पार्टी के नेतृत्व के नाम पर मतदान का बहुमत हिस्सा जा सकता है तो वहीं हिस्सा केन्द्र में सत्ता के लिए किसी और पार्टी अथवा नेतृत्व के नाम की तरफ लुढक सकता है। इसका यह अर्थ लगता है कि विचारधारा के स्तर पर पार्टियों में जो दूरियां थी वह सिमटती चली गई है। यानी चुनावी लोकतन्त्र में पार्टियां एक दूसरे की छाया प्रति होती चली गई है और चुनाव नतीजे इस बात पर निर्भर करने लगे हैं कि चुनाव जीतने की तैयारी किसने किस तरह से की है।

तीसरी बात यह है कि गवर्नेंस का अर्थ मतदाताओं को सत्ता से लालच की संस्कृति विकसित करने की तरफ ले जाना और विचारधारात्मक स्तर पर वर्चस्ववाद को मजबूत करने का एक मिश्रित माध्यम में चुनावी लोकतन्त्र विकसित हुआ है। गरीबी की सबसे ज्यादा बातें होती है लेकिन चुनाव अमीर लड़ते हैं। 95 प्रतिशत से आबादी नागरिक के रुप में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से बाहर हो चुकी है और वह सिर्फ वोट की मशीन का बटन दबाने वाली एक मशीन की तरह हो गई है। इंदिरा गांधी भी गरीबी मिटाने की बात करती थी और नरेन्द्र मोदी भी अस्सी करोड़ लोगों को पांच किलो का थैला अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का ऐलान करते नहीं थक रहे हैं। इसके साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान पुरपानी भाषा में कितना विरोधाभासी लगता है लेकिन चुनावी लोकतन्त्र की भाषा में यह खासियत के रुप में प्रतिष्ठित हैं।अमीरी और चुनावी लोकतन्त्र का रिश्ता स्थापित हुआ है। अपराध चुनावी लोकतन्त्र में प्रतियोगिता के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच स्वीकार्य हुआ है। मतदाता नागरिक के रुप में कमजोर हुआ है। इसका कोई डाटा या ग्राफिक्स किसी चुनावी नतीजे से नहीं निकलता है। उसकी झलक बस कई तरह की घटनाओं में मिलती है। चुनावी लोकतन्त्र में सबसे ज्यादा बातें धर्म निरपेक्षता की हुई है लेकिन चुनावी प्रतियोगिता में जाति और साम्प्रदायिकता खून की तरह दौड़ती है। संविधान का इस्तेमाल सत्ता और सत्ता पर वर्चस्व रखने वाली विचारधारा की वस्तु बन गई है।
इसे पांच राज्यों के चुनावों के विश्लेषण व उसके नतीजों एवं उसके अगले चुनाव पर असर के बारे में बतौर पृष्ठभूमि लिखने की वजह यह है कि हम किसी एक बुरी राजनीतिक प्रवृति या विकसित की जा रही अलोकतांत्रिक संस्कृति को लेकर एक चुनाव में हार जीत तक अपने विश्लेषण की सीमा को कैद करते जा रहे हैं। पांच राज्यों में चुनाव से राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार हारेंगे व जीतेंगे।लेकिन क्या इससे राजनीतिक स्तर पर जो चुनावी प्रतियोगिता का ढांचा बन चुका है, उसमें बतौर नागरिक किसी स्तर पर हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश दिखती है? पांच राज्यों में यही तय होना है कि पहले से सत्ता को चलाने वाली पार्टियां और नेतृत्व रहेगा व बदल जाएगा। इसे ही मतदाताओं की जीत के रुप में दर्ज किया जाता है। यह बिडम्बना है कि चुनावी युद्ध जीतने की तैयारी राजनीतिक पार्टियां व उसके नेतृत्व द्वारा किया जाता है और उसमें हर वो चीज शामिल होती है जो कि एक हित विरोधी दुश्मन को हराने के लिए जरुरी होने की मान्यता हासिल कर चुका है। यहां तक कि पांच वर्षों के लिए होने वाले चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद भी जरुरी नहीं है कि सत्ता बहुमत हासिल करने वाली पार्टी की ही बनी रह सकती है।

पांच राज्यों के चुनाव को इस नजरिये से देखा जा सकता है कि समाज में और सत्ता के जरिये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ लड़ने की चेतना किस तरह से सक्रिय है और उसे किन रास्तों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के नतीजों से समाज में एक नये ढांचे के बनने और सत्ता के भीतर बनने वाले दमनकारी ढांचे पर चोट मारने के लिए किस तरह की उर्जा और सांगठनिक क्षमता हासिल हो रही है, यह पड़ताल महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक चुनावों के विश्लेषण करने वालों व टिप्पणियों करने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि वह नागरिक के सशक्तिकरण में किसी चुनाव की भूमिका क्या हो सकती है। चुनाव एक तरह से मतदाताओं का एक नये तरीके से स्वंय पुनर्गठित होने की प्रक्रिया होती है और वह अनुभवजनित होनी चाहिए ताकि मतदाता समूह अपने नागरिकपन और नागरिक समाज को सशक्त कर सके। एक मतदाता के एक वोट की गिनती महज एक में नहीं होती है। वह मतदाता आबादी के बड़े हिस्से का प्रतिनिधि होता है। यानी 18 वर्ष कम उम्र की आबादी का वह किसी चुनाव में मतदाता के रुप में प्रतिनिधित्व करता है और उसे यह भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी होती है कि अगली पीढ़ी को बेहतर नागरिकपन की परिस्थितियों के तैयार होने व नागरिक समाज के सुदृढ़ होने में उसका फैसला सहायक होगा। अभी यह स्थिति दिखती है कि राजनीतिक पार्टियां व उसके उम्मीदवार उन मतदाता समुहों को अपने प्रभाव व असर में लेने की हर स्तर पर कोशिश करती है जो महज वोटों की गिनती में सबसे ज्यादा नंबर बनने में सहायक हो सके। चुनावी लोकतन्त्र का सांस्कृतिक रिश्ता नागरिक समाज के लिए बने, यह बड़ी चुनौती समाजिक विश्लेषकों की होनी चाहिए।