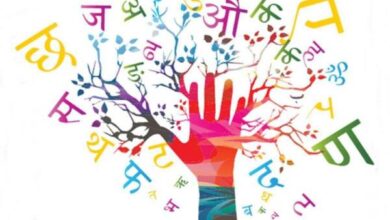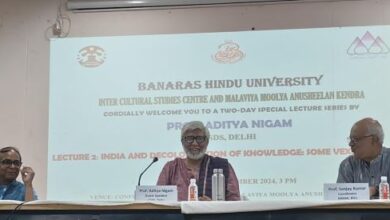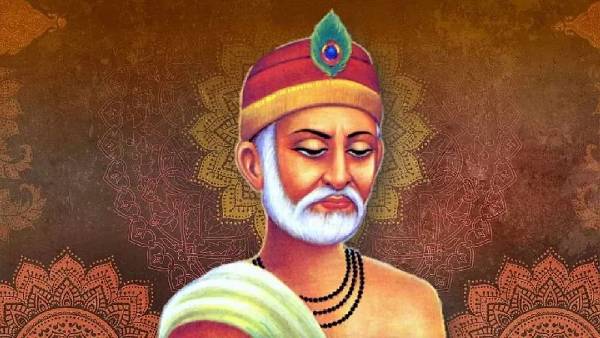जनसरोकारों की भाषा बने राजभाषा हिन्दी
हिन्दी संवैधानिक स्तर पर भारत की राजभाषा घोषित तो हुई परन्तु राजभाषा के रूप में अभी तक उसे जितना विकसित होना अपेक्षित था उतनी वह नहीं हुई और लगभग जनसरोकारों से कटी हुई दिखाई देती है। मूलत: हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है क्या? और यदि हैं तो कहाँ है? इसपर भी प्रश्न उपस्थित होता है और इस प्रश्न पर गम्भीर विचार होना अपेक्षित है। स्वतन्त्रता से पूर्व स्वदेशी भाषा प्रेमियों ने हिन्दी को राजभाषा बनाने का अधिक आग्रह पकड़ा इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। हिन्दी के सिवा दूसरा कोई उत्तम विकल्प या उपाय भी तो राष्ट्र के सामने नहीं था? स्वतन्त्र भारत के लिए राजकीय कामकाज की भाषा के रूप में किसी स्वदेशी यानी भारतीय भाषा का होना अधिक जरूरी हो गया था। ऐसी भाषा जिसे देश की सामान्य जनता समझती हो और जो जनसरोकारों से जुड़ी हो।
चुनौती यह भी थी कि भारत को राजनीतिक दासता से मुक्त होकर एक ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में विकसित करना जिसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति हो। देश की ऐसी छवि जो भारतीय लगे। यानी दुनिया भारत को भारत के नाम से पहचाने। उसकी प्रकृति यानी शरीर के हर अंग में भारतीयता का अंश घुलमिला दिखाई दे। यह कैसे हो सकता था कि देश अंग्रेजों की दासता से मुक्त हो जाये पर अँग्रेजी की दासता से मुक्त न हो सकें? उस समय के हमारे राष्ट्रनिर्माताओं ने यदि संघ की राजभाषा के लिए किसी भारतीय भाषा का आग्रह पकड़ा हो और वह हिन्दी हो तो इसमें दूर-दूर तक कोई आपत्तिजनक बात तो थी नहीं। पर जब हम आज स्वतन्त्र भारत की 76-77 वर्ष की विकासयात्रा का अवलोकन करते हैं तो क्या दिखाई देता है? इसपर कभी किसी ने सोचा है? हिन्दी भाषा देश की राजभाषा तो बनी है और उसे इस तरह कानूनी मान्यता भी प्राप्त है पर देश की प्रमुख कामकाजी भाषा के रूप में आज भी वह दुर्बल अवस्था में हैं। एक मनोरंजन का क्षेत्र छोड़ दिया जाये तो शिक्षा, उच्चशिक्षा, व्यापार, रोजगार की भाषा का माध्यम आज भी अँग्रेजी ही हैं।
अभी कुछ माह पूर्व देश के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने कानूनी कामकाज की भाषा के रूप में देशज भाषाओं को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने डॉ. राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए यह स्वीकार किया कि हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अदालतों में जिरह और फैसले हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होने चाहिए। क्या इसपर देश में कोई सोच रहा हैं? अभी कुछ दिनों पूर्व भारतीय दंड संहिता को निरस्त कर उसके स्थान पर 1 जुलाई, 2024 से “भारतीय न्यायसंहिता 2023” पूरे देश में लागू की गई। इसके 191 पृष्ठों का हिन्दी ड्राफ्ट अभी मैंने गूगल से डाउनलोड किया।
जब मैंने भारत की इस नवीनतम न्यायसंहिता के हिन्दी पाठ का अवलोकन किया यानी इसे पढने और समझाने की कोशिश की तो मैं काफी हैरान और उद्विग्न हो गया। इसके कुछ अध्यायों की हिन्दी को पढ़ते-पढ़ते मेरा हाल-बेहाल हो गया। मैं कोई राजभाषा विशेषज्ञ नहीं हूँ और न केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्यरत हूँ। एक सामान्य हिन्दी सेवी यानी हिन्दी का प्रोफेसर होने के बावजूद यह हिन्दी मुझे काफी कठिन और दुरूह प्रतीत हुई। मैंने हिन्दी के ऐसे शब्द आजतक न कभी पढ़े थे और न सुने थे। कुछ प्रयुक्तियाँ एवं वाक्यरचना मुझे इतनी जटिल, दुरूह और अटपटी लगी कि क्या कहूँ? ऐसी कुछ प्रयुक्तियों एवं वाक्यों को चुनकर मैं यहाँ आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी देखिए कि क्या ऐसी हिन्दी आपने कहीं पढ़ी-सुनी है? :
- मृत्यु दण्डादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण
- एकांत परिरोध
- जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर
- न्यायाकितः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य
- कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभाव्य है
- ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है
- अपने इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण
- सम्मति से किया गया कार्य जिसमें कार्य जिसमें घोर उपहति कारित करने का आशय न हो
- दुष्प्रेरण या दुष्प्रेरक
- बलात्संग एवं बलात्संग के लिए दंड
- प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन
- विधिपूर्व विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास
- उपहति या स्वेच्छया उपहति कारित करना
- दण्डावधियों की भिन्नें
- एकांत परिरोध की अवधि
- कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है
- ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध है
- सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना
- प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें
- दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है
- दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो
अब ऐसी हिन्दी का क्या और कितना औचित्य है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जनता की समझ में क्या आयेगा? कानूनी भाषा के जानकार भी इसे समझ नहीं सकते। जब चीफ जस्टिस यह कह रहे हैं कि हम कानून के सिद्धांतों को आम जनता तक पहुँचाने में विफल हो रहे है तो यह राजभाषा हिन्दी की प्रकृति को लेकर बहुत जरुरी टिपण्णी है ऐसा मैं समझाता हूँ। इसका सीधा सरल अर्थ यह हैं कि यह भाषा जनसरोकारों से जुड़ी हुई बिलकुल प्रतीत नहीं होती या हम इसे जानबूझकर जनसाधारण से जोड़ना नहीं चाहते। कहना तो यह भी पडेगा कि ऐसी हिन्दी भाषा से तो अँग्रेजी ही अच्छी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हिन्दी को लेकर विद्वत हिन्दी समाज से अभी तक कोई मानीखेज प्रतिक्रिया पढ़ने को नहीं मिली है। हिन्दी को लेकर यही आजतक होता रहा हैं इस देश में। हिन्दी की इस तरह की रूपरचना एवं प्रकृति का गठन करके हमने एक बड़ी सीमा तक हिन्दी की क्रूर हत्या की है या उसकी चीरफाड़ बेखौफ होकर करते जा रहे हैं और हमारे उन राष्ट्र निर्माताओं का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने बड़े संघर्ष के बाद हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिलवाया था। आजकल तो हिन्दी के इस पक्ष और स्थिति पर कोई बोल ही नहीं रहा है।
देखिए, राजभाषा की जो प्रकृति होती है और जो शब्द और वाक्यसंरचना होती हैं वह मूल समस्या का मुद्दा है। राजभाषा की यह संरचना वास्तव में तब बनी जब इससे पहले हिन्दी राजभाषा के रूप में संवैधानिक स्थान ग्रहण कर चुकी थी। मराठी में इसे “पोटावर कुंकू लावने” यानी बच्चे का जन्म होने से पूर्व ही उसका विवाहसम्बन्ध निश्चित कर देना है या नाम रख देना कहा जाता है। संघ की राजभाषा हेतु हिन्दी को अधिक उपयुक्त माननेवाले राष्ट्रनिर्माताओं और संविधान निर्माताओं के सामने तो केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी की ही संरचना उपस्थित थी और वे इसे ही सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में देखना चाहते थे। भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व राजभाषा हिन्दी की कोई विशेष प्रकृति या संरचना ही निर्मित नहीं हुई थी। जिस हिन्दी से उस समय सब लोग परिचित थे वह राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा हिन्दी थी जो जनाभिव्यक्ति की मुख्य भाषा थी।
यदि राजभाषा की कोई प्रकृति उस समय उपस्थित होती तो संविधान भी उसी प्रकृति के अनुसार हिन्दी में लिखा जाता। पर संविधान तो मूल रूप से अँग्रेजी में लिखा गया और इस अँग्रेजी ड्राफ़्ट का जिस हिन्दी में अनुवाद किया गया वह राजभाषा हिन्दी गृहीत मान ली गई। आज भी जिस राजभाषा हिन्दी की प्रकृति अथवा शब्द, अर्थ एवं वाक्यसंरचना की बात हम करते हैं वह मौलिक राजभाषा हिन्दी नहीं है बल्कि अँग्रेजी शब्दों के हिन्दी रूपांतरण से युक्त हिन्दी है। मैं तो इसे अनूदित हिन्दी भी नहीं कह सकता क्योंकि यह अनुवाद या रूपांतरण हिन्दी की मौलिक प्रकृति के अनुरूप तो हुआ लगता ही नहीं है। वह इसलिए नहीं हुआ कि मौलिक हिन्दी तो राष्ट्रभाषा हिन्दी थी जो इस देश के लोगों के जुबाँ-जुबाँ पर चढ़कर बोलती थी। अब यह जो कचहरियों वाली हिन्दी बनी इसका तो बोलचाल की हिन्दी या व्यावहारिक हिन्दी से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं था यानी स्पष्ट रूप से कहें तो जनसरोकारों से बिलकुल सम्बन्ध नहीं था। यह कृत्रिम एवं बनावटी हिन्दी प्रतीत होती है यानी कंस्ट्रक्ट हिन्दी।
मेरे समझ में बिलकुल साफ़ तरीके से यह आ रहा हैं कि संविधान में हिन्दी को राजभाषा घोषित करने से पूर्व हिन्दी के समर्थकों को यह बिलकुल पता नहीं था कि जिस हिन्दी की वह पैरवी या आग्रह पकड़ रहे हैं वह हिन्दी आगे चलकर वैसी हिन्दी बिलकुल नहीं होंगी। बोलने और सुनने के लिए तो वह हिन्दी लगेगी परन्तु समझने के मामले में बिलकुल भिन्न होगी। इतनी भिन्न कि न उसे भाषा कहा जा सकता हैं और न राजभाषा। लिखापढ़ी का काम तो उसमें सहजता से होगा ही नहीं। लगता यह है कि जो राष्ट्रभाषा हिन्दी है वह अलग है और जो राजभाषा हिन्दी है वह अलग हैं। दोनों में खून का क्या, मन का भी रिश्ता नहीं हैं। दोनों का डी.एन.ए. मिलता ही नहीं है। इस पर तुक्के की बात तो यह है कि साहित्यिक हिन्दी इन दोनों से भिन्न है। वस्तुत: हिन्दी की राजभाषा के अनुरूप प्रकृति के विकास की ओर तत्कालीन साहित्यकारों को अधिक ध्यान देना चाहिए था। लेकिन वें सभी तो उस समय प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायावादी कविताएँ लिखने में व्यस्त थे। ज्यादातर यह कविताएँ भी जनसरोकारों से पर्याप्त मात्रा में जुडी हुई नहीं थी। इसके कुछ कवि तो राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत कविताएँ लिखकर राष्ट्रकवि घोषित हो गए। सभी का ध्यान केवल अंग्रेजों को हटाने पर था, अँग्रेजी को हटाने पर नहीं। संविधान सभा की बहसों के रेकॉर्ड यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा कि हमें अँग्रेजी आती हैं और अँग्रेजी में अंग्रेजों से बात करके ही हमें आज़ादी मिली हैं।
.