
ज्ञान की भाषा के रूप में हिन्दी
मैं अपनी बात को तीन बिंदुओं पर केन्द्रित करने का प्रयास करता हूँ। एक तो आधुनिकता, दूसरा अनुवाद और तीसरी चीज़ है, हिन्दी और हिन्दी में इसकी परिणति।
समाज विज्ञानी और साहित्यकार समेत अधिकांश लोग मानते हैं कि वास्तव में आधुनिकता एक यूरोप केन्द्रित परियोजना थी। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, सन् 1998 में डेडलस का एक अंक “अर्ली मॉडर्निटी” पर आता है, जिसमें संजय सुब्रह्मण्यम और शेल्डन पोलॅक के दो लेख छपते हैं और जिसमें पहली बार यूरोप केन्द्रित आधुनिकता की परियोजना को प्रश्नांकित किया जाता है।
संजय सुब्रह्मण्यम के उस लेख का एक वाक्य जो मेरे दिमाग़ में बैठ गया है, उसे आपके सामने रखता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि उन तथ्यों को समझाने में सुविधा होगी जिसका ज़िक्र आगे किया गया है। संजय सुब्रमण्यम उस लेख में कहते हैं कि आधुनिकता कोई वायरस नहीं है, जो यूरोप में पैदा हुआ और कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। वस्तुतः हर सभ्यता अपने ढंग से आधुनिकता का एक स्वरूप विकसित करती है। यहीं से एक तरह से यूरोप केन्द्रित आधुनिकता को प्रश्नांकित करने का, उसे चुनौती देने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आयीं किंतु यहाँ उस विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक पुस्तक का मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा, जिससे मुझे अपनी बात को कहने में थोड़ी सुविधा होगी।
संभवतः सन् 2000 में आई दीपेश चक्रवर्ती की किताब ‘प्रोविंसीअलाइजिंग यूरोप’, जिसमें बहुत व्यवस्थित ढंग से यूरोप केन्द्रित ज्ञान को सार्वभौमिक ज्ञान के रूप में समूची दुनिया में प्रचारित करने की प्रवृत्ति को चुनौती दी गयी और कहा गया (जैसा कि आप शीर्षक से अंदाज़ा लगा सकते हैं) कि ‘यूरोप का ज्ञान अन्ततः यूरोप का ज्ञान है।’ उसको उसी प्रोविंस तक सीमित करना चाहिए। उसको सर्वव्यापी बनाने का जो पूरा तरीका रहा है, उसकी अपनी समस्याएं हैं। उसको उसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूरोप केन्द्रित आधुनिकता की इस चुनौती के साथ जो तीन नई शब्दावलियाँ सामने आईं, उनसे सभी परिचित हैं। एक तो अर्लीमॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट आया, जिसे हम लोग आजकल हिन्दी में ‘आरम्भिक आधुनिकता’ कहते हैं। इसमें यह माना गया कि लगभग मुग़ल काल से ही हमारे यहाँ आरम्भिक आधुनिकता का दौर शुरू हो जाता है। इस तरह की बात हिन्दी में रामविलास शर्मा पहले भी लिख चुके थे। लेकिन जैसे ही यूरोप के ज्ञान के प्रतिष्ठित केंद्रों से इस तरह की बात सामने आयी तो उसकी स्वीकार्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ गयी। दूसरी शब्दावली है ‘वैकल्पिक आधुनिकता’ (अल्टरनेटिव मॉडर्निटी) और उसी से जुड़ी हुई तीसरी शब्दावली है ‘देशज आधुनिकता’ (इंडीजिनस मॉडर्निटी)।

इस तरह इन तथ्यों के आलोक में अगर हम हिन्दी की ज्ञान संपदा के बारे में विचार करें तो कुछ दिलचस्प नतीजे निकाले जा सकते हैं। वास्तव में जब से भारतीय भाषाओं का लेखन की भाषा के रूप में अभ्युदय हुआ, तभी से उनकी स्वतन्त्र पहचान बनी। अगर हिन्दी क्षेत्र की बात करें तो, हम जिसे सामान्य रूप से पहले मध्यकाल कहते थे और अब आरम्भिक आधुनिक काल कहने लगे हैं, उस दौर में हिन्दी के जो नाम हैं, जिनमें साहित्य लिखा गया, वे तीन हैं- मैथिली, अवधी और ब्रज। हालांकि यह बात ज़रूर है कि 18वीं शताब्दी तक आते-आते इस पूरे क्षेत्र में ब्रजभाषा फैल गयी और उसे साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ब्रजभाषा की स्वीकार्यता समूचे हिन्दी क्षेत्र में तो हुई ही, हिन्दी क्षेत्र के बाहर भी गुजरात से लेकर बंगाल, असम तक भी हुई।
इस विषय में किशोरीदास वाजपेयी लिखते हैं कि ‘एक तरह से ब्रजभाषा ने संस्कृत की विरासत को संभाला।’ किन्तु इस विषय पर उतना काम नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था। लोग अनुवाद और ज्ञान को कहीं न कहीं एक दूसरे से जोड़कर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें इस संदर्भ पर ध्यान देना चाहिए। उस दौर में संस्कृत के बहुत सारे ग्रन्थों को ब्रजभाषा में लाया गया किंतु संस्कृत के ग्रन्थों को ब्रजभाषा में लाना अनुवाद नहीं था। ‘अनुवाद’ शब्द की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि उस दौर में अनुवाद शब्द का वही अर्थ नहीं था, जिस अर्थ-संदर्भ में आजकल अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अलग-अलग क्षेत्रों में महाभारत और रामायण के अनुवाद के भिन्न-भिन्न रूप देखने को मिलते हैं।
यदि इस दौर में संस्कृत के ग्रन्थों को ब्रजभाषा में लाने का इतिहास देखें तो उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे यहाँ जिसे पश्चिमी ढंग का ‘अनुवाद’ कहते हैं, उस तरह के अनुवाद का चलन 19वीं सदी से पहले नहीं था। यदि इस भारतीय ढंग के अनुवाद (रिक्रिएशन) को और अधिक स्पष्ट करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि हमारे विद्वानों ने संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया और उसे अपने ढंग से बदला। अतः 19वीं सदी में अनुवाद के रूप में जिस तरह का ‘आईकॉनिक ट्रांसलेशन’ हमारे सामने आया (जिसमें अनुवादक को मूल रचना के प्रति ‘फ़ेथफुल’ होना पड़ता है, वह अपनी तरफ से छूट नहीं ले सकता) उस तरह के अनुवाद के साक्ष्य 19वीं सदी से पहले ख़ासतौर से हिन्दी के पुराने रूपों में नहीं मिलता है।
इसीलिए लेखक और अनुवादक का जो पदानुक्रम है वह भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अनुवाद में हमेशा से उसे बदलने की छूट मिलती रही है। काव्यशास्त्र मर्मज्ञ राजशेखर ने कहा है कि भारतीय परंपरा में स्वीकरण का भाव है। उसका ज़िक्र मुकुंद लाठ ने भी किया है कि हम पहले किसी रचना को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करते हैं। इसलिए एक ही संस्कृत ग्रंथ को अलग-अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं में अपने अपने ढंग से रचा है और वे सब स्वतन्त्र लेखक या रचनाकार हैं। तुलसीदास, वाल्मीकि के रामायण के अनुवादक नहीं है। यह परम्परा 18वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ चलती रही। 18वीं शताब्दी के आस-पास इससे अलग एक साक्ष्य मिलता है जिसका सबंध आगरा से है।
जॉन कोर्ट का एक निबंध है, जिसमें उन्होंने बनारसीदास जैन के ग्रन्थों के अनुवाद को आइकॉनिक ट्रांसलेशन के आस-पास का कहा है। हालांकि ऐसा एक ही साक्ष्य मिलता है सिर्फ़ एक। अनुवाद की दृष्टि से 16वीं शताब्दी में अकबर का, 17वीं शताब्दी में बनारसीदास जैन का और 18वीं शताब्दी में काशी नरेश का नाम उल्लेखनीय है। काशी नरेश के सहयोग से संस्कृत महाभारत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया गया। इस अनुवाद को अगर संस्कृत के टेक्स्ट से मिला कर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेक्स्ट सामने रखकर उसे अपनी भाषा में ढाल रहा हो।
अगर हम इस अनुवाद को देखें तो ऐसा लगता है कि यह काफी कुछ ट्रांसलेशन के आस-पास की चीज़ है, किंतु पूरी तरह वह भी नहीं है। क्योंकि अनुवादक कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त कर देता है या कुछ को छोड़ देता है। फिर भी 18वीं शताब्दी में काशी नरेश के सहयोग से तैयार हुआ ‘महाभारत दर्पण’ काफी कुछ आइकॉनिक ट्रांसलेशन जैसा है। ‘ट्रांसलेशन’ के अर्थ में अनुवाद का हिन्दी में उसका सबसे पहला प्रयोग भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने किया। उससे पहले हिन्दी में अनुवाद शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। दूसरी ख़ास बात यह है कि यदि संस्कृत के शब्दकोश में अनुवाद का अर्थ देखें तो उसका वही अर्थ नहीं मिलेगा, जिस अर्थ में उसे हम आज लेते है। शब्द तो पुराना है लेकिन हम जानते हैं कि 19वीं सदी में ‘अनुवाद’ को अंग्रेजी के ‘ट्रांसलेशन’ के पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया। शब्द कई बार वही रहता है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे ‘राष्ट्र’ शब्द वेदों में आता है लेकिन उस राष्ट्र शब्द का वो अर्थ नहीं है जो आज के ‘नेशन’ का है। वैसे ही अनुवाद शब्द का 19वीं शताब्दी से पहले वह अर्थ नहीं होता था जो अर्थ 19वीं सदी से पहले होता था। हमने पश्चिमी ढंग के आइकॉनिक ट्रांसलेशन के अर्थ में अनुवाद को उन्नीसवीं सदी में स्वीकार किया। अनूदित ग्रन्थों में जब इस तरह का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा, तब अनुवाद शब्द का अर्थ बदल गया। तब वास्तव में ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में अनुवाद शब्द का प्रयोग होने लगा।
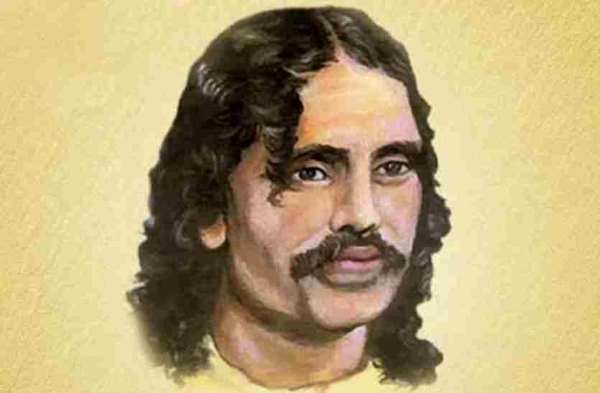
19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने शेक्सपियर के ‘मर्चेंट ऑफ़ वेनिस’ का ‘अनुवाद’ किया। उस ‘अनुवाद’ में भी उस तरह का ‘फेथफुल ट्रांसलेशन’ नहीं मिलता, उसमें काफी कुछ उन्होंने अपने ढंग से ‘रीक्रियेट’ किया है। कई बार तो वे लेखक के नाम का भी उल्लेख नहीं करते। बांग्ला के किसी उपन्यास को उन्होंने अपने ढंग से रीक्रियेट किया लेकिन उसके लेखक का नामोल्लेख करने की भी ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी। ऐसा नहीं है कि वे बेइमानी कर रहे थे, उस दौर में यही परंपरा थी कि यदि लेखक (अनुवादक) ‘मूल’ लेखक का ज़िक्र न भी करें तो कोई हर्ज़ नहीं।
अनुवाद का एक तरीका वह है जो 19वीं सदी में आया, जिसको विद्वान आइकॉनिक ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसमें मूल का एकदम ‘फ़ेथफुल’ अनुवाद करना होता है। दूसरा तरीका वह है जो 19वीं सदी से पहले तक हमारे यहाँ था। और इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर पश्चिमी तरीके का आइकॉनिक ट्रांसलेशन हमारे यहाँ नहीं था तो एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्ञान कैसे जाता था? अमर्त्य सेन ने अपनी किताब ‘द आर्ग्युमेंटेटिव इंडियन’, में इस बात का ज़िक्र किया है कि चाहे पश्चिम के स्कॉलर हों या चीनी और अरबी के स्कॉलर, उन्होंने भारत के तमाम ग्रन्थों का अनुवाद किया। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने दूसरे देशों या सभ्यताओं के जिन ग्रन्थों का अनुवाद किया है, उसकी संख्या बहुत कम है। अब प्रश्न यह है कि अगर उन लोगों ने पश्चिमी ढंग से अनुवाद नहीं किया तो क्या यह कह सकते है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं थी? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि बिना अनुवाद किये दूसरी भाषाओं के ज्ञान को हम अपने ढंग से आत्मसात कर लेते थे। मुग़ल काल तक तो इसके स्पष्ट साक्ष्य हैं कि यूरोप में जो कुछ घटित हुआ वह यहाँ के लोगों को मालूम था। इसलिए कोई न कोई और तरीका अवश्य ही रहा होगा, जिसे अगर हम आइकॉनिक ट्रांसलेशन की शब्दावली में देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा।
अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यूरोप के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का स्वीकार ही एकमात्र तरीका है तो ये सच नहीं है। इसलिए भारतीय ढंग के पुराने तरीकों की खोज-पड़ताल की जानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे तरीके सार्थक हैं या नहीं?
बर्नाड कोह्न का लेख है ‘कमांड ऑफ़ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ़ कमांड’। उसमें उन्होंने लिखा है कि ‘यूरोप ने भारत के केवल भौगोलिक क्षेत्र पर ही विजय प्राप्त नहीं की, उन्होंने यहाँ की समूची ज्ञान परम्परा पर भी विजय प्राप्त की।’ जो भारतीय ज्ञान परम्परा थी, उसमें हो सकता है कुछ अच्छा भी रहा हो। जैसे मुझे लगता है कि भारतीय ढंग का अनुवाद का तरीका त्याज्य नहीं है। उससे हम अवश्य ही कुछ सीख सकते हैं। अगर हम ज्ञान और अनुवाद को जोड़कर देखें तो अनुवाद का यह तरीका जिसमें हम अपने ढंग से उसको ग्राह्य बनाते है और उसमें कुछ जोड़ते भी हैं, यदि वह पाठक के लिए ग्राह्य है तो वह भी एक तरीका हो सकता है। उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।
अगर आप मध्यकाल के इतिहास को देखें, तो शेल्डन पोलॅक ने अपने एक लेख में कहा है कि ‘भक्तिकाल और मध्यकाल में हिन्दी की जो पांडुलिपियाँ हैं, उनमें ज़्यादातर साहित्यिक धार्मिक विषयों पर लिखी गयी पांडुलिपियाँ हैं।’ आगे वे एक बात और जोड़ते हैं कि भक्तिकाल में (जिसके बारे में कहा जाता है कि सब कुछ स्थानीय भाषाओं में लिखा जाने लगा) साहित्य की भाषा तो स्थानीय भाषा बनी लेकिन ज्ञान की भाषा संस्कृत ही रही।

इसलिए इस तथ्य को हिन्दी की ज्ञान सपंदा की समस्या से भी जोड़कर विचार करने की ज़रूरत है। अंग्रेजी शासन आने के बाद, मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के बाद अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच जो संबंध बना, उसे भी इस संदर्भ से जोड़कर देखने की ज़रूरत है। वहाँ यह कहा गया कि ज्ञान की भाषा तो अंग्रेजी ही होगी। चूंकि सबको अंग्रेजी नहीं पढाई जा सकती, इसलिए ये जो वर्नाकुलर्स हैं, उस ज्ञान को आम जन-मानस तक पहुँचाने का काम करेंगी। यानी ये वर्नाकुलर्स अपनी तरफ़ से कोई ज्ञान पैदा नहीं करेंगी। अंग्रेजी में निर्मित ज्ञान को ही सर्वजन सुलभ बनाने का प्रयास करेंगी।
चाहे भक्तिकाल हो, अंग्रेजी शासन का दौर हो, अंग्रेजी शासन के बाद भारतीय स्वाधीनता का दौर हो या आज का दौर, हिन्दी की समस्या यही रही है कि वह अनुवाद की भाषा बन गयी है। उसमें अपना ज्ञान बड़े पैमाने पर रचने की सम्भावना नहीं विकसित की गयी है। ऐसा क्यों हुआ? इस पर विचार किया जाना चाहिए। अनुवाद के द्वारा उसको हम कितना समृद्ध कर सकते हैं? अनुवाद के पूर्व औपनिवेशिक भारतीय तरीके को क्या हम पुनर्जीवित कर सकते है! विदेशी भाषाएँ सभी लोग नहीं सीख सकते। इसलिए विदेशी भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनुवाद के द्वारा लाने और अपनी भाषाओं में मौलिक ज्ञान-सृजन की सम्भावनाएँ विकसित करने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।







