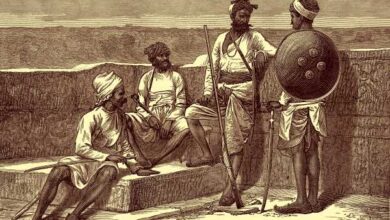आत्मनिरीक्षण का समय
राष्ट्रवाद की आँधी में केवल जाति-धर्म के समीकरण नहीं लड़खड़ाए, क्षेत्रीय हित भी गौण हो गए; सबसे बढ़कर रोज़गार के दिलफरेब गम भी ओझल हो गए| 18 से 22 साल के जो वोटर पहली बार मतदान कर रहे थे, उनके सामने रोज़ी-रोटी की चुनौती नहीं थी, उनमें लगभग आधे राष्ट्रवाद की उत्ताल तरंगों में बह रहे थे| यह सही है कि केवल राष्ट्रवाद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका नहीं निभाई| उसके साथ मुख्यभूमि में हिंदुत्व का गाढ़ा रंग मिलाया गया था, उत्तरपूर्व में अलगाववादी भावनाओं को जोड़ा गया था, दखिन में धर्म-संप्रदाय को घोल चढ़ाया गया था| संक्षेप में, राष्ट्रवाद की छतरी के नीचे सैकड़ों ऐसी भावनाएँ संकलित करके एक मायावी परिदृश्य (नैरेटिव) तैयार किया गया था जो आपस में टकराती थीं और राष्ट्रवाद के भी आड़े आती थीं| राजनितिक भाषा में इसे अवसरवाद कहा जाता है लेकिन सफलता सारे पाप धो देती है|
जिस बात को समझने में प्रतिद्वंदी चूक गए, वह बहुत मामूली-सी है| केवल प्रतिक्रिया करके, नकारात्मक प्रचार से देशव्यापी चुनाव नहीं जीता जाता| जोड़-तोड़ से, समीकरण से जनमत को आकर्षित नहीं किया जा सकता| सबसे ज़रूरी है वैकल्पिक नजरिया-सकारात्मक सन्देश| इसके अभाव में संघ-भाजपा परिवार दो बातों में सफल हुआ| एक, अपने हिन्दुत्ववादी उन्माद को पहले की सत्ताधारी पार्टियों के ‘छद्म-धर्मनिरपेक्षता’ की प्रतिक्रिया के रूप में मान्यता दिलाना; दूसरा, अपने सांप्रदायिक कार्यक्रम को राष्ट्रवाद के नामपर लोगों के गले उतरना, जिसे पुलवामा-बालाकोट की प्रायोजित-सी लगनेवाली घटनाओं ने विश्वसनीयता दे दी| यही करण है कि धर्मनिरपेक्षता तो ‘छद्म’ हो गयी, और छद्म-राष्ट्रवाद देशभक्ति बन गया| पुलवामा-बालाकोट की जुगलबंदी ने पाकिस्तान-विरोधी भावनाओं से उग्र हिंदुत्व को औचित्य प्रदान करके साम्प्रदायिकता को राष्ट्रवाद की तरह स्थापित करेने में सहायता की| लेकिन यह सब मनमाने तरीके से नहीं हुआ| इसके लिए अब तक हावी राजनीति की असफलताएँ और अदूरदर्शिता भी जिम्मेदार है| उस चूक का निरिक्षण आवश्यक है जिसने ध्रुवीकरण को एक लोकप्रिय और ग्राह्य मुद्दा बना दिया है| यह निरिक्षण इसलिए भी आवश्यक है कि काँग्रेस की निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों का विकल्प मोदी की भाजपा नहीं है| जो उस रास्ते पर और बेझिझक होकर चल रही है; फिर भी वह अपने को ‘विकल्प’ के रूप में प्रस्तावित करने में सफल हुई| 
वर्तमान भारत की अधिकांश समस्याओं के केंद्र में निजीकरण-उदारीकरण की यही नीतियाँ हैं| बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार पूंजीवाद की जन्मघुट्टी में है; पूँजीवाद जितना मनमाना होगा, उतना ही ये समस्याएँ निरंकुश होंगी| सत्ताधारी राजनीति जब सामाजिक संकट नहीं सुलझा पति, तब धर्म का सहारा लेती है| ‘अबकी पहन लिया है उसने भक्तिन वाला बाना’- नागार्जुन ने यह बात इंदिरा गाँधी के लिए कही थी| नवें दशक के उत्तरार्ध तक सामाजिक संकट अधिक गहरा हो चला था| राजीव गाँधी की काँग्रेस ने एक तरफ शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हुए कट्टरपंथी मुल्लाओं को बल पहुँचनेवाला कानून संसद में पारित किया, दूसरी तरफ हिंदुत्व को प्रोत्साहन देनेवाला निर्णय लेते हुए राममंदिर का चार दशक से बंद ताला खुलवाया| उसके बाद से जनतान्त्रिक राजनीति लगातार हाशिए पर पहुँचती गयी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ‘राष्ट्रवाद’ का पर्याय बन गया है| अंतर बस इतना है कि काँग्रेस हिन्दू और मुस्लिम दोनों प्रकार की साम्प्रदायिकता से खेलती थी, पूरी तरह किसी पर निर्भर नहीं थी, भाजपा पूरी निष्ठां से हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिसे वर्तमान संविधान के कारण राष्ट्रवाद कहने को विवश है| क्षेत्रीय दलों की स्थिति इन दोनों से विशेष है| उत्तर प्रदेश-बिहार में यादव जाति को केंद्र में रखकर राजनीति करनेवाले दलों ने धर्मनिरपेक्षता का जो रूप प्रस्तुत किया, उसने तुष्टीकरण के आरोपों को बल पहुँचाया| मुलायम को तो ‘मौलाना’ ही कहा जाता था और वे खुद इस संज्ञा के प्रचार को बल देते थे| लालू ने आडवाणी का रामरथ रोककर अपने को धर्मनिरपेक्ष दलों का लाडला बना लिया था|
इन बातों का दूरगामी असर रहता यदि ये दल भ्रष्टाचार में लिप्त न होते और इतना ही स्पष्ट विरोध मुसलमानों में बढती कट्टरता का करते| पिछड़ा वर्ग की इस राजनितिक धर्मनिरपेक्षता के ज्वार में वामपंथी पार्टियाँ भी यह भूल गयीं कि सामाजिक दृष्टि से जितनी हानिकर साम्प्रदायिकता है, उससे अधिक हानिकर जातिवाद है| वह अधिक विखंडनकारी है| जितने संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जाएगी, उतना ही विघटन की शक्तियाँ बल पाएँगी| जातिवाद के सहारे साम्प्रदायिकता से लड़ने की नीति न केवल वामपंथियों के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई बल्कि वह समूचे लोकतान्त्रिक वायुमंडल के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुई| इसमें संदेह नहीं कि सभी क्षेत्रीय दल एक साँचे में ढले नहीं हैं| उड़ीसा में बीजू जनता दल, बिहार में जनता दल (यूनाइटेड)| आन्ध्र में तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसे दल न तो तृणमूल की तरह खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलते हैं, न बहुसंख्यक (सांप्रदायिक) राष्ट्रवाद की राह पर| लेकिन हिंदुत्व के साथ इनका रिश्ता सीधा-सरल नहीं है| धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का यह बिखराव इस बात का द्योतक है कि भारतीय राजनीति अभी सिद्धांत के आधार पर नहीं चलती| अन्य जिन आधारों पर चलती है, वे न हमारे समाज के हित में हैं, न लोकतंत्र के| इन दलों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वे अपने स्थानीय हितों से उठकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नीतियाँ अपनाने में असमर्थ रहते हैं| इसलिए उन्हें कभी साम्प्रदायिकता से मिलते देखा जाता है, कभी अलग होते; इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे खुद सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं या नहीं|
जहाँ तक नीतिगत विकल्प का प्रश्न है, काँग्रेस या भाजपा ही नहीं, क्षेत्रीय दलों का भी विकल्प वामपक्ष को होना था| आर्थिक नीति हो या सांप्रदायिक समस्या, उसके पास एक समग्र वैकल्पिक कार्यक्रम है| किन्तु अपनी अक्षम्य गलतियों के कारण वह स्वयं हाशिए पर चला गया है| बल्कि आज वह अपने सबसे गंभीर अस्तित्वगत संकट से जूझ रहा है| वामपंथी नेतृत्व ने पिछले ढाई दशकों में एक के बाद एक अनेक आत्मघाती भूलें की हैं—ज्योति बासु को 1996 में प्रधानमंत्री बनने से रोकना हो या 2008 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी, प्रत्येक गलती की कीमत चुकानी पड़ी है| इसीके साथ सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर भी कुछ गलतियाँ हैं| वामपंथी संस्थानिक बुद्धिजीवी और नेता धर्म और संस्कृति के संबंधों को लेकर बेहद भ्रामक समझ रखते हैं| वे दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, यह उचित है, इससे बंगाल में उन्हें जनाधार निर्मित करेने में सहायता मिली; किन्तु उत्तर भारत में वे मेले-ठेले और रामलीलाओं के उपयोग को ग़लत मानते हैं| अल्पसंख्यकों के प्रति अतिरिक्त उदारता प्रायः कट्टरतावाद के प्रति नरमी का रूप ले लेती है और बहुसंख्यकों के प्रति उपेक्षा अधिकांशतः संस्कृति के प्रति उदासीनता का रूप ले लेती है| बहुत-से वामपंथी बुद्धिजीवियों ने काँग्रेसी शासन से अपने स्वार्थ जोड़ रखे थे, वे अपनी सुविधाजनक स्थिति बनाये रखने से अधिक किसी मूलभूत सामाजिक परिवर्तन के बारे में नहीं सोचते| ऐसे एनजीओ-बुद्धिजीवियों से राहुल गाँधी घिरे रहे हैं| ये वाम-बुद्धिजीवी फासिस्ट-विरोधी संयुक्त मोर्चे के सिद्धान्तकर ज्यौर्जी दिमित्रोव की यह सीख भूल गए हैं कि जो कम्युनिस्ट जनता की परम्पराओं के प्रति उपेक्षा-उदासीनता दर्शाता है, वह अपनी सारी महान विरासत अपने हाथों फासिस्टों को सौंप देता है|
इन विभिन्न स्थितियों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि क्रमशः साम्प्रदायिकता की या ध्रुवीकरण की प्रवृत्तियाँ समाज में गहरे पैठ गयी हैं| उन्हें किसी एक दल की सत्ता या सफलता में सीमित कर देना पुनः आत्मघाती होगा| सचाई यह है कि पूरे समाज में उत्तेजना और नफ़रत उतनी आज़ादी के बाद भी नहीं थी जितनी आज है| तब एक नए भारत के निर्माण का स्वप्न था, अब एक विफल मनोरथ जनता की उदासी है; तब साम्राज्यवाद से मुक्ति का अहसास था, अब साम्राज्यवाद का फंदा भी मुक्ति का भ्रम जगाता है| इन विषम परिस्थितियों को समझकर ही हम वर्तमान भारत के सार्थक भविष्य को मूर्तिमान कर सकते हैं, अन्यथा सामाजिक पीड़ा बहुत लम्बी होगी|