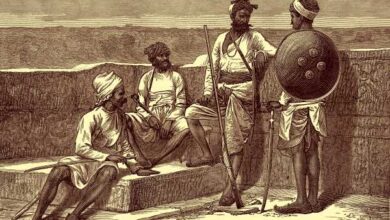विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू जनजातियां और साहित्य
इतिहास गवाह है भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध लोक जागरण – बुद्ध काल, भक्ति आन्दोलन व स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के सारथी दलित, वंचित और हाशिये का समाज से थेजिनके संघर्ष के बिना ये जागरण निस्संदेह असम्भव थे किन्तु उन्हें बिसरा दिया गया। इसी प्रकार का वंचित समाज है, घुमंतू, खानाबदोश जनजातियाँ, जो योद्धा/लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण कभी अंग्रेजी राज में अपराधी घोषित हुए, तो कभी अपनी ही सरकार के द्वारा‘ हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी’ घोषित हुए।
आज देश स्वतंत्रता का ‘75वाँ अमृत उत्सव’ मनाने की शुरुआत कर चुका है लेकिन यह समाज संग्राम के मंथन का अमृत भी न चख़ पाया बावज़ूद राहू-केतु-सा कलंक ढोने को विवश है। समाज से बहिष्कृत माने जाने वाला विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू समाज आज भी स्वतंत्रता के अमृत से वंचित है। सहानुभूति और संवेदना का संचित कोष साहित्य भी नैतिक आदर्शों की मूल धारणा के कारण इस समाज को न अपना सका तो अस्मिता मूलक विमर्शो में भी इस समुदाय की अस्मिता और सम्मान पर चिंतन नहीं होता। मराठी साहित्य के आत्मकथात्मक उपन्यास इस संदर्भ में रेखांकित करने वाले है जहाँ एक एक तरफ तो इस समुदाय का विकृत चेहरा सामने आता है तो हमारे समाज की विद्रूपताओं को भी रेखांकित करतें है।
शायर असराल-उल-हक़ मजाज़ इन विमुक्त-घुमंतू जनजातियो का दर्द बयां करते हैं-
बस्ती से थोड़ी दूर, चट्टानों के दरमियां
ठहरा हुआ है, ख़ानाबदोशों का कारवां
उनकी कहीं जमीन, न उनका कहीं मकां
फिरते हैं यूं ही शामों-सहर ज़ेरे आसमां
‘घुमंतू’ का शाब्दिक अर्थहै, ‘घुमक्कड़’ जो बिना कारण इधर-उधर घूमे अथवा जब कोई शौक से, अनुभव लेने को, ज्ञान प्राप्ति हेतु यात्रायें करता है, जिसके लिए खूब पैसा और समय चाहिए। एक शब्द ‘जनजाति’ विशेषण के साथमेरी चेतना से टकराता है – घुमंतू जनजातियां यानी वे विशेष जाति जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता और आजीविका की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते हैं और घूमना इनका शौक नहीं विवशता है। इसी के संदर्भ में हमारे देश में आज घुमंतु, अर्ध-घुमंतू, विमुक्त जनजातियों में लगभग 840 जातियां है, जिनमें भारतीय समाज का सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़ा वर्ग है कालबेलिये, नट, भांड, पारधी, बहुरूपिये, सपेरे, मदारी, कलंदर, बहेलिये, भवैया, बणजारे, गुज्जर, गाड़िया लुहार, सिकलीगर, कुचबंदा, रेबारी, बेड़िया, नायक, कंजर, सांसी जैसी सैकङौं जातियाँ हैं।
शिक्षा के अभाव में ये जातियां जानवरों से बदतर जीवन व्यतीत करने को विवश है। एक पक्षी भी घोंसला बनाकर रहता है, गली का जानवर भी एक स्थान खोज लेता है और जीवन भर वहां रह लेता है, लेकिन विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू जनजातियां इनकी विडम्बना की घर की ‘चाहना’ रखकर भी ये घर नहीं बना सकते, मूलभूत आवश्यकताओं की घोर कमी के साथ-साथ एक सामाजिक अभिशाप या कलंक इन्हें सदैव ढोना पड़ता है। अजीब विडम्बना है कि जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को स्थायीकरण के कारण सदा सम्मान मिला वहीं अपनी घुमक्कड़ प्रवृति के चलते सम्मान मिलना तो दूर आपराधिक (वो भी परम्परागत /जन्मजात) जातियों का दंश झेलना पड़ा।
‘विश्व के लगभग 53 देशों में अंग्रेज़ों का शासन था, (लेकिन ‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट’ 1871 ब्रितानी हुकूमत के दौरान बहुत सारी ऐसी लड़ाकू जनजातियाँ थीं जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स यानी आपराधिक जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था) केवल भारत में लागू किया गया था इसकी पृष्ठभूमि में अंग्रेज़ों की धारणा यह थी कि जिस तरह से भारत में जातिगत व्यवसाय होते हैं जैसे लौहार का लड़का लौहार होता है, बढ़ई का लड़का बढ़ई, चिकित्सक का लड़का चिकित्सक, इसी तरह अपराधी की संतानें अपराधी ही होती हैं, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करने वाली,भारत की इन लड़ाकू जातियों की संतानों को भी अनिवार्य रूप से जन्मजात अपराधी मान लिया गया था विमुक्त जनजातियों के प्रति पूर्वाग्रह अंग्रेजों द्वारा घोषित की गई अपराधी जनजातियों या विमुक्त जनजातियों (Ex-Criminal Tribes) के बारे में आज भी तथाकथित अभिजात्य वर्ग एवं जन सामान्य का सोच यह है कि यह चोरी-चकारी जैसे आपराधिक कृत्य में संलिप्त जातियां हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है इस पूर्वाग्रह पूर्ण नज़रिये के कारण ही इन समुदायों के उत्थान के लिए शासक वर्ग ने कोई कारगर उपाय नहीं किए
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ किंतु इन घुमंतु, अर्ध घुमंतू जनजातियों को 31 अगस्त 1952 को स्वतंत्रता मिली जब इन्हें ‘विमुक्त’ घोषित किया गया। और इसके स्थान पर है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लागू कर दिया इसका अर्थ यह हुआ कि जो ब्रिटिश विद्रोही समुदाय 1952 तक जन्मजात अपराधी माने जाते थे, वे अब ‘आदतन अपराधी’ माने जाने लगे मगर उनके नाम के आगे विमुक्त का शब्द जुड़ गया जिससे पता चले कि यह पहले अपराधी जनजाति के थे। भारत के विमुक्त जनजाति आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण सिद्धराम रेनके जो स्वयं “महाराष्ट्र में डमरू बजाकर भीख मांगने वाली कम्युनिटी के हैं, वे कहते थे कि मैं अपने पिता के साथ में मुंबई में भीख मांगता था। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम किया। 17 अनुशंसाएं कीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। …” वे मानते हैं कि इन जनजाति के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलना ही सबसे अहम क़दम होगा।
सामाजिक स्थिति
2011 की जनगणना के अनुसार घुमंतू जनजातियों की आबादी 15 करोड़ है जो आज यह 20 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। ‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट’ के कारण समाज इन्हें परंपरागत मानता है यह विडम्बना ही है कि जन्म लेते ही अबोध शिशु अपराधी श्रेणी में मान लिया जाता है। यही कारण है कि ये कहीं भी घर बना नहीं बना पाते, इन्हें खदेड़ दिया जाता है, ग्लोबल भारत की संकल्पना में इन लोगों के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं बचा जिन खाली स्थानों पर ये घर बना लिया करते थे वहां पर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हैं, खाने पीने की तो बात ही अलग है नहाना-धोना, पानी, शौच जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी मुहैया नहीं। कुछ सामाजिक दबाव तो कुछ व्यक्तिगत विवशताएं ये जाने-अनजाने असामाजिक कार्यों से जुड़ते चले गए। स्त्रियों की दशातो और भी दर्दनाक है, आजीविका हेतु देह का इस्तेमाल करना इनकी विवशता है बेड़नी, नचनारी, नचनिया, पथुरिया, धंधे वाली जैसे अपमानजनक शब्दों से रोज़ दो-चार होतीं हैं। इन्हें कभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला अन्यथा इन जातियों की लोक संस्कृति में, संगीत, नृत्य-कला जड़ी बूटियों का ज्ञान आदि धरोहर के रूप में विद्यमान है लेकिन इन्हें संरक्षित करने का किसी ने नहीं सोचा।
साहित्य में विमुक्त घुमंतू जनजाति
सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य ने ही विमुक्त घुमंतू जनजाति की नकारात्मक/बुरी छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत की। इस तरह के साहित्य को एट्रोसिटी लिटरेचर Atrocity Literature कहा जाता है यानी किसी समाज, व्यक्ति, घटना आदि के प्रति क्रूरता, अतिदुष्ट व्यवहार, अत्याचारी सोच लेकर चलने वाला साहित्य। किसी संस्कृति या देश को खराब दिखाने के लिए एकत्र की गई काल्पनिक कहानियों , तथ्यों को जाने समझे बगैर, प्रस्तुत करता है। इन्हीं किताबों में से एक किताब का नाम ‘कन्फेशन ऑफ ठग’ है। जिसे 1839 में ‘फिलिप मेडोज’ ट्रेलर ने लिखा था। जिसमें ठग्स/पिंडारी (Thugs of Hindustan) को कुख्यात लुटेरा, हत्यारा और डकैत बताया गया था। ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि अंग्रेजों की खिलाफत करने वाले आदिवासी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे, पिंडारियों यानि ठग कहे जानेवालों से, गोरी सरकारआतंकित थी, … ठग्स ऑफ़ हिन्दुस्तान’ नामक फिल्म बनी थी। फिल्म की कहानी ठगों अर्थात ब्रिटिशकाल के ‘एंटी हीरो’ पर आधारित है। पर यह भी सच है कि जिसे समाज का हीरो दिखाया गया है, वह समाज आज भी गुलामों-सी जिंदगी जी रहा है। आजादी के बाद देशभक्तों को पुरस्कृत किया गया, ये पिंडारी स्वयं ही ठगे गए। यह भी विडम्बना ही है कि भारतीय साहित्य ने इस नकारात्मक छवि में बदलाव लाने हेतु या समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन हेतु कोई प्रयास नहीं मिलते।
साहित्य
‘उत्तर आधुनिककाल’ में अस्मिताओं की टकराहट से नए-नए विमर्श उभर कर आए। दलित, स्त्री, आदिवासी, किन्नर, विकलांग आदि विमर्श। विमुक्त घुमंतू जनजातियां जो निम्नतर कोटि का जीवन व्यतीत कर रहें हैं, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भीइनके उत्थान हेतु अथवा इस समुदायों की चेतना जाग्रत करने के लिए कोई साहित्यिक विमर्श या आन्दोलन अथवा पहल किसी की तरफ से क्यों न हो सकी?विमर्शों की मूल शब्दावली अस्तित्व, अस्मिता, सशक्तिकरण, विद्रोह, मान-सम्मान जैसे शब्दों की मूल संकल्पना से ही अभी येकोसों दूर हैं। अज्ञान, सामाजिक बहिष्कार, आपराधिक कलंक अस्थायित्व और सबसे अधिक अशिक्षाके कारण अस्मिता की चेतना अभी इनमें जाग्रत नहीं हो पा रही। साहित्य में वंचित दलित समाज का विमर्श की शुरुआत मराठी साहित्य से हुई और अब विमुक्त घुमंतू जनजातियों की आत्मकथाओं का आरम्भ भी मराठी साहित्य में आत्मकथाओं से हो रहा है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के हिसाब से साहित्य की कुछ नैतिक मान्यताएं रहीं हैं जो इस समाज पर लागू नहीं हो पाती एक ऐसा व्यक्ति या जाति जो घोषित/आदतन अपराधी है उसके प्रति सहानुभूति जागृत करना भी शायद अपराध की श्रेणी में आ जाए, इसलिए अब तक साहित्य में इनके प्रति साहित्यकारों ने कोई सहानूभूति भी न दिखाई। हाँ रांगेय राघव ने ‘कब तक पुकारूँ’ व ‘धरती अपना घर’उपन्यास में क्रमश:इन नट या करनट व गाड़िये लोहार के जीवन को उकेरा हैपर कोई परंपरा नहीं चल पाई। बांग्ला लेखिकामहाश्वेता देवी का नटी नामक उपन्यास स्वातंत्र्य संग्राम की प्रथम चिंगारी और संघर्ष के बीच मोती नामक नटी /नर्तकी की कथा है।
आत्मकथात्मक साहित्य
पूर्व में प्रेमचंद और अनेक प्रमुख साहित्यकारों द्वारा दलितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने पर भी विमर्शों का कोई दौर, आन्दोलन न हो पाया, वह चेतना दलित आत्मकथाओं ने विकसित की। इसके बाद आज तक विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की लगभग 35 के आसपास आत्मकथाएं लिखी गई हैं। और अब समय आ गया है कि उन पर नया विमर्श खड़ा होगा, नया साहित्य आने लगेगा। दलित विमर्श की भांति विमुक्त समाज के लोग साहित्य के क्षेत्र में आ रहें है।
शोलापुर के नागनाथ विट्ठलराव गायकवाड़ की एक कविता कहती है :
उठ मेरे विमुक्त भाई
अपनी दुनिया ही है निराली, पैदा होते ही हम अपराधी
न गाँव, न घर, न जंगल, न कोई हक, कहाँ के हम शिकार
उठ मेरे विमुक्त भाई, गुलामी के जंजीरों से बाहर निकल
क्रांति की फैली है किरण, संघर्ष कर, न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल।
मराठी में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की आत्मकथाओं का पदार्पण 1980 में लक्ष्मण माने की आत्मकथा ‘पराया’ (1981 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित) से माना जाता है कैकाडी समाज का नायक दाहक अनुभव संघर्ष और सामाजिक उपेक्षा की यात्रा करते हुए हमारे समाज के चेहरे के नकाब नोंच कर एक ऐसा आईना प्रस्तुत करता है जिसमें सभ्य समाज अपना ही विकृत चेहरा देख सिहर उठता है। घोरदरिद्रता, अछूतेपन और अज्ञानता के अन्धकार में डूबा हुआ कैकाडी समाज घुमक्कड़ समाज है। स्वयं लक्ष्मण माने जी के अनुसार“सतारा में हर वर्ष बाबा साहब अंबेडकर व्याख्यानमाला आयोजित करते हैं इसके लिए दया पवार और राव साहब कस्बे वक्ता के रूप में आए थे उन्हें जाति बिरादरी के कुछ प्रसंग सुनाए, बातें करते-करते, सहजता से उन्होंने कहा लिखो! पर मैं साहस न कर सका यह मेरा क्षेत्र नहीं है बाद में अनिल अवचट जी ने भी लिखने को कहा कि अब नहीं लिखेगा तो कब लिखेगा? और फिर जो जिया जो भोगा, जो अनुभव किया, देखा, वही सब लिखता गया, वही जीवन बार-बार जीता गया… इस पुस्तक के कारण खानाबदोश जातियों-जनजातियों के सवालों पर सामाजिक विचार मंथन शुरू हो, बंजारे सामाजिक चर्चा के विषय बने, उनके लिए काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले, … मैं समझूंगा पुस्तक लिखने का मेरा परिश्रम सार्थक हो गया। पीढ़ियों से गधों की पीठ पर अपना घर संसार लादे, जीवन जीने वालों की वेदना यदि समाज समझ सका तब भी काफी है। ”(अनुवादक दामोदर खडसे) वास्तव में अपने दुःख दर्द को बयां करना सरल नहीं खासकर जब हम जान रहे हो कि समाज हमें गंभीरता से नालेगा हमारे प्रति घृणा करता है उसकी सम्वेदना को उद्वेलित करना उनके लिए आसान न था।
1989 में साहित्य अकादमी सम्मानित लक्ष्मण गायकवाड लिखित मराठी आत्मकथात्मक उपन्यास ‘उलच्या’ एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है, ‘उलच्या’ का अर्थ है ‘’ चोरी करने वाली जातिजिसे समाज ने हमेशा से नकारा। पेशे से लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण गायकवाड विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से महाराष्ट्र की विमुक्त जनजातियों में सामाजिक जागरूकता अभियानों से जुड़े हैं। यह लेखक के अनुभवों पर आधारित है इसमें सामाजिक असमानता पर पैना व्यंग्य और स्पष्ट स्वीकारोक्ति दोनों मुखर हैं। उचक्का समाज के छोटे-मोटे अपराधों पर पल रहेवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यह एक व्यक्तिके माध्यम से समाज की विकृतियों कथा है।
भूमिका में लेखक लिखते हैं कि “जिस समाज में मैं जन्मा उसे वहां की वर्ण व्यवस्था और समाज व्यवस्था दोनों ने नकारा है सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से… अंग्रेज सरकार ने तो गुनहगार का ठप्पा हमारे समाज पर लगा दिया और सब ने हमारी ओर गुनाहगार के रूप में देखा और आज भी उसी रूप में देख रहे हैं…हम पर थोपे गए चोरी के इस व्यवसाय का उपयोग ऊपर वाले ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया आखिर हमें अपराधी की मोहर जो दी गई उसका कभी तो समाजशास्त्रीय अध्ययन भी होगा, बचपन से ही मैं अपने आसपास उठाई गिरोह की दरिद्रता, उनकी मजबूरी, भूख के कारण होने वाली उनकी छटपटाहट और अभावग्रस्त था, को देखता आ रहा हूं… उनकी व्यथा को उनके सम्मुख प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही यह लेखन मैंने नहीं किया, अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखकर प्रस्थापित समाज हमारी और नए दृष्टिकोण से देखें, विचार करें और साथ ही इन जनजातियों में तैयार होने वाले नव शिक्षित युवक युवा समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें, इसलिए मैंने यह आत्मकथा लिखी। …रिश्वत और भ्रष्टाचार से लाखों रुपए कमाने वाले लोग यहां अपराधी गुनहगार नहीं माने जाते परंतु भूख से परेशान होकर 15-20 की चोरी करने वाले यहां गुनाहगार माने जाते हैं…मैं बेचैन हो जाता हूं… अधिकार अचानक और एक रात में मिलने वाला नहीं है इसके लिए निरंतर जागृति संघर्ष और संगठन की जरूरत है। मैंने यह अनुभव किया कि नैतिक मूल्य और ईमानदारी की हमारी संकल्पना में जबरदस्त विसंगति है। यह आत्मकथा वास्तव में एक कार्यकर्ता का मुख्य चिंतन है इस कारण इस आत्मकथा का साहित्य का मूल्यांकन करने की अपेक्षा समाज शास्त्रीय मूल्यांकन हो यह अपेक्षा है। (उचक्का लक्ष्मण गायकवाड अनुवाद सूर्यनारायण रणसुभे राधाकृष्ण प्रकाशन 2014 पृष्ठ पेज 15)
मराठी में विमुक्त जनजातियों की अन्य प्रमुख आत्मकथाएं हैं-जिनमें प्रमुख हैं –भीमराव गश्ती कृत बेरड, आत्माराम राठौर कृत तांडा। भीमराव गति कृत आक्रोश शिवाजी राठौड़ कृत टाबरो, भीम राव जाधव कृत कटोरी तारेच्या कुंपणाची राउडी राठौर टांडेल, रामचंद्र नलावडे कृत दगडडफोद्या चोरटा, आदि। मराठी साहित्य में घुमंतू और विमुक्त विमर्श अंकुरावस्था में है किन्तु अनुवाद के माध्यम से सम्पूर्ण समाज में न केवल इस समुदाय के प्रति लोगों में संवेदना जाग्रत होगी अपितु सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अन्य भारतीय साहित्यकारों और स्वयं भारत के अलग अलग हिस्सों में बिखरे विमुक्त जनजाति के लोगों में भी जागरूकता आएगी। यदि इस प्रकार का साहित्य हमारे बुद्धिजीवियों के संपर्क में आता है तो निश्चय ही इस समाज की सुध लेने के लिए यह एक अच्छी पहल हो सकती है।
हिंदी में विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू साहित्य
हिंदी में विमुक्त जनजाति से संबंधित आत्मकथाएं नहीं मिलती। हाँ, विमुक्त समुदाय को आधार बनाकर लिखित उपन्यास इस शोषित समाज के जीवन का दर्दनाक नग्न यथार्थहमारे समक्ष रखते है। ‘कब तक पुकारूं’ राजस्थान के बैर ग्राम तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में रहने वाले हैं नटों की उपजाति करनट के जीवन व्यापार की कथा है, पीड़ित मनुष्यता के लिए इंसाफ पाने की पुकार है। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था में ज़मींदारों द्वारा शोषित जाति की विवशताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। अभाव ग्रस्त जाति पर किए गए अत्याचारों की अपराध गाथा जहाँ कोई नैतिकता, देह से जुड़ें नियम नहीं, स्त्रियां सरकारी अमलदार और जमींदारों द्वारा भ्रष्ट की जाती हैं। राघव जी की संवेदना और मार्मिक दृष्टि से मानवीयता और प्रेम का मूल तथ्य नहीं छूट पाता इसलिए वे देह से परे कजरी और प्यारी का सुखराम के प्रति प्रेम, वफादारी, आत्मसम्मान उच्च उदात्त गुणों को ईमानदारी से चित्रित करते हैं।
स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानने वाले गाड़िये-लुहारों पर आधारित है उपन्यास “धरती मेरा घर”जिसमें अपने ही सिद्धान्तों, आदर्शों और जीवन मूल्यों पर जीने वाले, कभी घर बनाकर न रहने वाले, खानाबदोशों की तरह जीवन यापन करने वाले और समाज से अलग रहने वाले इन गाड़िये-लुहारों के जीवन के अनछुए और अनदेखे पहलुओं का जैसा सजीव वर्णन हमें मिलाता है। उदय शंकर भट्ट कृत ‘सागर लहरें और मनुष्य’( 1955) में मुंबई के वर्सोवा बीच के कोलियों के संघर्ष प्रस्तुति मिलती है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास ‘कचनार’ की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है उपन्यास का घटना काल 1792 से 1803 के मध्य का है गौड़ टोलियों से अंग्रेज हमेशा आतंकित रहे। मणि मधुकर द्वारा लिखित उपन्यास ‘पिंजरे में पन्ना’राजस्थान की गाडिये लोहार जनजाति पर आधारित है यह जनजाति राजस्थान के मरुस्थल में खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में यह मान्यता है कि वे राजपूतों की संतान रहे हैं मुगलों ने जब चित्तौड़गढ़ से बच निकले वापस नहीं लौटे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक चित्तौड़गढ़ पर कब्जा नहीं कर लेंगे पलंग पर नहीं सोएंगे दीपक नहीं जलाएंगे घर नहीं बस आएंगे तब से उन्होंने वह उपयोगी लोहे के हथियार बनाने का कार्य आरंभ किया इसी व्यवसाय में संलग्न खानाबदोश हो गए।
मैत्रयी पुष्पा का ‘अल्मा कबूतरी’ उपन्यास बुंदेलखंड की यायावर कबूतरा जनजाति की व्यथा को उजागर करने वाला उपन्यास है वे कहतीं हैं “इनके पुरुष जंगल में रहते हैं या जेल में स्त्रियाँ शराब की भट्टियों पर या किसी के बिस्तर पर। कभी-कभी सड़कों, गलियों, में घुमतेया अखबारों कीअपराध- सुर्ख़ियों में दिखाई देनेवाले कंजर सांझी, नट, मदारी, सपेरे, पारदी, हाबुड़े, बंजारे, बावरिया कबूतरे न जाने कितनी-कितनी जन जातियां जो सभ्य समाज के हाशियों पर डेरा लगाए सदियां गुज़ार देती हैं , हमारा चौकन्ना सम्बन्ध सिर्फ कामचलाऊ ही बना रहता है उनके लिए हम है ‘कज्जा’ और ‘दिक्कू’यानी सभ्य-संभ्रांत, परदेसी। उनका इस्तेमाल करने वाले शोषक। उनके अपराधों से डरते हुए , मगर उन्हें अपराधी बनाये रखने के आग्रही। हमारे लिए वे ऐसे छापामार गुरिल्ले हैं जो हमारी असावधानियों की दरारों से झपट्टा मारकर वापस अपनी दुनियां में जा छिपते हैं” (उपन्यास के कवर से )
भगवानदास मोरवाल का‘रेत’ उपन्यास कंजर यानी कानन, जंगल में घूमने वाली जनजाति की लोमहर्षक गाथा है। इनका दर्द इस सम्वाद में झलकता है-“ बिना इजाजत या इत्तिला दिए कोई कंजर गाँव छोड़कर नहीं जा सकता …और जाता है तो मुखिया को इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसकी इत्तिला मुखिया को थाने में देनी होती है। ”… इनकी महिलाओं को भी थाने जाकर हाज़िरी देनी पड़ती है। भगवानदास मोरवाल -प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन 2009 रेत, पृ. 51
लेखिका शरद सिंह के “पिछले पन्ने की औरतें”उपन्यास स्त्री विमर्श केन्द्रित विमुक्त घुमंतू बेड़िया जनजाति की ही मार्मिक अभिव्यंजना है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बेड़ियां जनजाति की महिलायें जो सदियों से उपेक्षित, वंचित, उत्पीड़ित एवं आर्थिक बदहाली का जीवन जी रहीं हैं, सभ्य समाज के लिए बेड़नी मात्र नाचने गाने वाली भोग्यऔरतें हैं। वेश्यावृत्ति करने वाली ये स्त्रियां अपने समाज और परिवार में अपेक्षाकृत अधिक सम्मान और अधिकार पाती हैं। अज्ञानता के वशीभूत इन्हें स्वयं भी देह व्यापार से कोई शिकायत नहीं रहती यह इसे ही परंपरा मानकर निभाती रहती हैं।
इसी श्रृंखला में कोली/कोरी समुदाय की वीरांगना झलकारी बाई , रानी लक्ष्मी बाई की सखी का महत्त्व है अंग्रेज़ो ने इस जाति को खूनी जाति घोषित किया था, जबकि प्रथम विश्वयुद्ध में इसी को योद्धा जाति माना गया था क्योंकि वहां इस जाति ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। वीरांगना झलकारी बाई स्वतंत्रता सेनानी थी इस उपन्यास के लेखक मोहनदास नैमिशरायजी ने स्वयं झांसी जाकर शोध के बाद ही तथ्य प्रस्तुत किये। विमुक्त जनजातियों की शौर्यगाथा के साथ गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत कर भी हमारी सोच को एक दिशा प्रदान की जा सकती है क्योंकि आज ये अपने इतिहास को स्वयं ही विस्मृत करते जा रहे हैं।
निष्कर्ष
जिस समाज में जाति आधारित गालियाँ बनी हो और धड़ल्ले से बोली भी जाती हों, घुमंतू जनजातियों के लिए आपराधिक शब्दावलियों का प्रयोग होता है तो अत्यंत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि विकृत तो हमारी मानसिकता है। हाँ, हर समाज की अपनी कमजोरियां होती हैं कमियां होती हैं ऐसे आचार-व्यवहार होते हैं जिसे उसी समाज का दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं करता लेकिन इस चुनौती को अगर समर्थ संपन्न समाज पढ़ा-लिखा समाज नहीं समझेगा और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को नहीं जागृत करेगा तो यह समाज का हिस्सा हमेशा ही कमजोर रहेगा और हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए शरीर का एक हिस्सा अगर कमजोर होता है तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं पूरे शरीर को करना पड़ता है। क्यों ना समाज के इस हिस्से को समर्थ शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जाए, यदि इन्हें शिक्षा, रोज़गार, सम्मान दिया जाये तो ये क्योंकर अपराध की दुनिया में आना चाहेंगे। लक्ष्मण गायकवाड़ जी बताते हैं कि हमारे समाज में चोरी सिखाने के लिए शिक्षक होते हैं जो दुखद इसके विपरीत यदि हम उन्हें किताबें थमाएंगे तो किताबें ही पढ़ेगे, लेकिन ऐसे हालात बने तो? इसके लिए तथाकथित सभ्य, बुद्धिजीवी समाज को संवेदनशील बनना होगा, बनाना होगा और साहित्य इसका सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है।
अध्ययन सामग्री स्रोत
*उचक्का लक्ष्मण गायकवाड अनुवाद सूर्यनारायण रणसुभे राधाकृष्ण प्रकाशन 2014 पृष्ठ पेज 15)
*पराया, लक्ष्मण माने अनुवादक दामोदर खडसे, साहित्य अकादमी
*भगवानदास मोरवाल -प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन 2009 रेत, पृ. 51