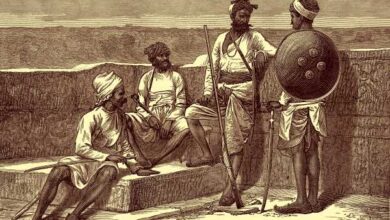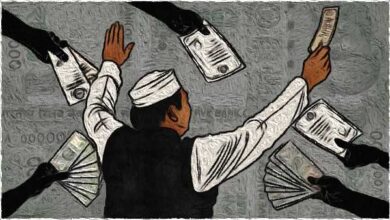कोरोना की त्रासदी और हमारा समय
कोराना वायरस की सूचना दिसम्बर, 2019 में पहली बार सामने आई थी। फिर उसकी भयावहता के चरण धीरे-धीरे बढ़े और एक समय वह आया जब समूचे भूमण्डल में उसका कोहराम छा गया। यह भी देखने में आया कि कोई वैभव, ऐश्वर्य और सत्ता, पैसा-रुपया किसी भी तरह काम नहीं आया। धार्मिकता से ओतप्रोत मंदिर, मस्ज़िद, गुरुद्वारे, चर्च; जिनका विराट वैभव लोगों के दिलों में रहा है, वे भी सहम गये। हमारे सामाजिक साहचर्य और सम्पर्क की विविधताएँ सिमटने लगीं। कोरोना वायरस का कहर, भय उसके मूल में था। हम सभी जान लें कि धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है। वह न तो कोई वैभव है, न प्रदर्शन, न कोई विशेष प्रकार की दुनिया।
पहली बार शिद्दत के साथ प्रकट हुआ कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं; आस्था का कोई मरकज नहीं; समाज-सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। यह सिद्धांतों में खूब कहा गया। उसका आदर्श लोक भी रहा; लेकिन वह हमारे जीवन-व्यवहार में प्रकट नहीं हुआ। यह भी साबित हुआ कि हम क्षुद्र स्वार्थों की खोहों में घूम रहे हैं और अहंकार के अंधलोक में टनटना रहे हैं। हमारे धर्म, मजहब में जो कर्तव्यबोध और आचरण संसूचित किए गये हैं, उन्हें हमने अपनी जड़ताओं से पाट दिया है। स्वार्थों के झंझावात में हमारी भक्ति के उस रसायन को नफ़रत, विद्वेष और अनैतिकता के शिलाखण्डों में बदल दिया गया। हमारी सामाजिक संरचनाओं में बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन आए। यही नहीं, भक्ति के अर्थ-सम्बन्ध भी बदल गये। जब परिवर्तन घटित होते हैं तो वे सामाजिक संरचना को तो बदलते ही हैं, हमारी धर्म-संरचना को बाहर भी परिवर्तित करते हैं और भीतर भी।
आपदा है या महामारी, मैं इसे भीषण त्रासदी के रूप में देखता हूँ। जो अपने को शक्तिशाली मानते थे, वे घुटनों-घुटनों आ गये। अपने बचाने के लिए वे एक भयावह युद्ध-युद्ध चिल्ला रहे हैं। वह इसलिए कि उनकी शक्तिशाली लीलाएँ ढीली और बेकार हो गयी हैं। विकास के नारे लगाते-लगाते, बंकर ध्वंस करने वाली ताकत, स्मार्ट सिटी, बुलेट प्रूफ की गुहार लगाते-लगाते वे स्वयं निरीह हो गये। सच मानिए, अस्पतालों में इक्विपमेंट की बेहद कमी, लॉक डाउन के दौर में जितना इंतजाम किया गया, वह अपर्याप्त साबित हुआ। अफरा-तफरी, भागम-भाग, भूख-प्यास, रहने के बंदोबस्त व्यापक जीवनचर्या की ठोस कार्रवाई की माँग करते हैं। क्या हुआ, समूचा गर्जन-तर्जन कम हुआ है।
आरोप-प्रत्यारोप की मात्रा बहुत तेज़ गति से बढ़ी है। कहा जा रहा है, नफ़रत का खेल मत खेलिए; जो अपराधी हैं उन्हें दण्डित किया जाएगा। अमरीका, इटली, जर्मनी का गुमान क्यों टूट गया! सबका भ्रम चकनाचूर है। जो घर जाने के लिए बेचैन हैं, उनके पास कुछ दिनों के लिए भी इंतजाम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं; जिनके खान-पान और परिवहन के साधन हैं, कपड़े-लत्ते हैं, फिर भी बेबस हैं। इस महामारी में लॉक डाउन के साथ सोशल डिस्टेंस भी चाहिए। गरीब को क्या चाहिए, खाने रहने की बस थोड़ी सी सुविधाएँ। रहीम का एक दोहा याद आ रहा है— “चाह गयी, चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह/जिनको कछू न चाहिए, वे साहन के साह।”
हमारे लोक में, जीवन में सामाजिक-सांस्कृतिक सुरक्षा हेतु कुलदेवी, कुलदेवता के नए-नए साँचे भी बने। हम अपने जीवन में आश्वस्ति चाहते हैं; सबका कल्याण चाहते हैं। इसलिए इस तरह की तमाम चीज़ें तलाश कर निश्चिंत होने की ख़्वाहिश रखते हैं। हमारी सामाजिक ज़रूरतें निरन्तर समय-समय पर बदलते हुए अपनी कार्रवाई करती हैं। इस परिवर्तन-यात्रा में कितना पानी बह चुका है! सामाजिक संरचना और उसके मूल स्वरूपों में परिवर्तन घटित हुए तो धर्म-संरचनाओं में भी जटिलताएँ पनपी और स्वार्थी तत्त्वों ने उन्हें अपने लाभ-लोभ के लिए मनुष्यता को बार-बार रौंदा। हमारी धार्मिक भावनाओं में यदि विवेक न हो तो स्वार्थी तत्त्व आस्था के नाम पर कितने आवरणों में छिपकर तहस-नहस करते हैं। गालिब का एक शेर इस दुर्दांत समय और महत्त्वाकांक्षाओं में बार-बार सामाजिक-सांस्कृतिक विकास और मनुष्यता को खण्डित करने के सम्बन्ध में रोशनी डालता है; हमारी आत्मा को तोड़ने से बचाता है और स्वार्थ के भयावह रूपों की ओर इशारा करता है— “उम्र भर गालिब भूल ये करता रहा/धूल चेहरे में थी, साफ़ आईना करता रहा।”
प्रश्न है कि हम किसको क्या कहें। हम मंदिर, मस्ज़िद और गुरुद्वारे में उलझे रहे; हम हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के संदर्भों को उछालते रहे; जनता को इन टोनों-टोटकों में उलझाए रहे और स्वार्थ की सुरंग खोदते रहे। हमारे जीवन के, समाज के असली मुद्दे ध्वस्त होते रहे। देश में ही नहीं, समूची दुनिया मानवता के असली रास्ते से भटकती रही और हम राजनीतिक परिदृश्य को, जनकल्याण को ध्वस्त करने में तल्लीन रहे। कोरोना वायरस की महामारी से चारों ओर से घिरकर अपाहिज होने और किंकर्तव्यविमूढ़ होने के बाद जब समझ आया कि हमें कोई नहीं बचा सकता, तब हमारा ध्यान स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य सेवाओं एवं सुविधाओं की तरफ गया; कालान्तर में सरकारी अस्पताल-संस्थान, डॉक्टर, नर्स, सफाई अमले, पुलिस, फ़ौज और गरीबों को सच्ची मदद करने वाले समाजसेवी हमारे ध्यानाकर्षण में आये। जिनको हम महत्त्वहीन मानते थे, उनसे ही हमारे जीवन-कल्याण के तमाम रास्ते खुलते नज़र आए।
कोरोना का मुकाबला करने के लिए हमारे देश और दुनिया में कोई दवा नहीं; कोई खास इक्विपमेंट नहीं। हम तो राजनीतिक रोटियाँ सेंक रहे थे; सरकारें बना बिगाड़ रहे थे। जो पैसा हमने विशालकाय, भारी भरकम मूर्तियाँ गढ़ने में, राजनीति चमकाने में लगाया था, काश! हमने स्वास्थ्य संस्थान ठीक किए होते! अभी तो आगे चलकर हमें शिक्षा की खराब स्थितियों के बारे में रोना-कलपना होगा; चरित्र की हत्या और भ्रष्टाचार की लीलाओं में फँसे देश-दुनिया के लिए छाती पीटने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
देश में भागम-भाग जारी है। पता नहीं, कौन कहाँ भाग जाना चाहता है; किल्लतें सबकी कुंडी उखाड़ रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा इंतज़ाम अपनी सीमाओं में काफी किए गये। अव्यवस्था ने बार-बार पोलें खोलीं। कुछ गड़बड़ी लोगों ने की हैं, तो उन्हें कहीं भी खोंस कर चाहो तो पूरे कौम को बदनाम कर दो। होना तो यह चाहिए कि जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन्हें ठीक करो। अभी भी जहर की खेती जारी है। इस सबके बावजूद जिन्होंने सेवा की, स्वास्थ्य-सेवाएँ बड़ी मेहनत और लगन से कीं, उन्हें सलाम करने की बलवती इच्छा बनी हुई है और बनी रहेगी। घृणा फैलाने वाले लोग शृंखला बनाये हुए हैं। उनका अपना धंधा है। घृणा फैलाए बगैर उनका खाना नहीं पचता। फ़िराक़ गोरखपुरी ने सच कहा है— “जब तक न ऊँची हो जमीर की लौ/आँख को रोशनी नहीं मिलती।” हम विपत्तियों से जूझ रहे हैं और वे जहर की फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं। कमियाँ बेहिसाब हैं; लेकिन अपनी कूबत भर जो किया जा रहा है, उसे कम नहीं आँकना चाहिए।
कोरोना वायरस के काल में जितना उत्पादन राजनीति के इलाके में हुआ, उतना ही उमड़-घुमड़कर कविता और साहित्य लिखा गया। लॉक डाउन के दौर में निराशाएँ भी उपजीं। मैं देश के लोगों के धैर्य को बहुत इज्जत के साथ देखता हूँ। पहले तीन हफ़्ते, फिर 19 दिन यानी लगभग तीन हफ्ते और। खेती-किसानी ठप्प। छोटे-छोटे लोग यानी रोज़-रोज़ कमाने-खाने वाले किस तरह जी रहे हैं! सब अपने-अपने घरों में लगभग बंद हैं। कोरोना टाइम लेगा और अन्य रोगों की तरह वह भी जड़ से जाएगा या नहीं? सभी लोग चिन्ताओं के भँवर में हैं। हम केवल उम्मीद कर रहे हैं। कहना यह है कि सत्ता के नशे के बावजूद एक दुनिया है। धर्म आस्थाओं और दिखावों के बावजूद भी एक जिजीविषा भरी दुनिया है। कोरोना ने सबको अपनी असली ज़मीन भी दिखा दी। उसने यह भी संदेश दिया कि ज्यादा न उड़ो; संसार की वास्तविकता के इलाके भी अनुभव करो। कोई दवाई नहीं; कोई एँटीबॉयटिक नहीं।
कोरोना-त्रासदी में भी एक बारीक बुनावट है। पूरी जिम्मेदारी जैसा हो या नहीं; आधा-अधूरा ही सही; न से तो बेहतर है। हाँ, उसे जिम्मेदारी जैसा दिखना चाहिए और वैसा ही बरतना भी चाहिए। संकट का काल होता ही ऐसा है कि जो है जैसा है, किसी-न-किसी रूप में चलता रहे। ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुछ-न-कुछ होगा; कुछ-न-कुछ होना है। सामान्य जन को हर हाल में रोना है। उनकी जीवन-रेखाओं में कुछ इसी तरह की लकीरें खिंची हैं। भ्रष्ट्राचार आजकल खुलकर नहीं, छिपकर दहाड़ रहा है। गरीबों का राशन और अन्य सुविधाएँ जो किसी न किसी माध्यम से सरकारी व्यवस्था से ज़रूरतमंदों तक पहुँचाये जाने थे उनमें अनेक अनियमितताएँ भी सुनने में आईं। खैर, जहाँ पूरी सुविधाएँ दी जानी चाहिए, वहाँ आधी-अधूरी ही सही और कभी आश्वासन-एजेंट की तरह।
लॉक डाउन ने काफ़ी हद तक कोरोना की लम्बी चैन को रोका है। सोशल डिस्टेंस इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लॉक डाउन की अवधि बन्धनों के साथ बढ़ती रहेगी। वास्तविक ज़रूरतमंद इस त्रासदी की आग में झुलसते रहेंगे। संपन्न और सुविधा में रह रहे कहीं-न-कहीं आखिर बच ही जाएँगे। अच्छी बात यह है कि आप चाहे जिस तरह की चालें चलो, राष्ट्र की हिफाज़त के जादू में उसे हर हाल में अच्छा ही माना जाएगा। कुछ तो बाकायदा हो रहा है। सामान्य स्थिति कब तक बहाल होगी, यह एक तरह का यक्ष प्रश्न है। इसका कोई ठोस पैमाना किसी लुकमान अली के पास नहीं है। आप केवल तुकांत भिड़ा सकते हैं। इसे घरबन्दी, तालाबन्दी या लॉक डाउन कुछ भी कहिए। इस त्रासदी के पीछे शासन-प्रशासन की सभी तरह की नाकामयाबियाँ छुप जाएँगी या छुपा ली जाएँगी— बेरोज़गारी, शिक्षा का पतन, हत्याएँ, मनमानी, लोगों की जिन्दगी और आशाओं की आवाज़। प्रशासन भी एक तरह से जादू ही है। मँहगाई, गरीबी और न जाने क्या क्या है, नागरिकता के मुद्दे ठिकाने लगा दिए जाएँगे। एक ही राग समूचे वातावरण को छेंक लेगा। कोरोना है तो सब मुमकिन है।
मुझे एक ही चीज़ पर ताज्जुब है कि कोरोना के संदर्भ में भी लोग दर्शन, विज्ञान एवं जीवन की अध्यात्मिकता तलाश रहे हैं। कोई सरकार के पक्ष में पुन्नेठी झाड़ रहा है; कोई राजनीति का दारुण खेल खेलने में व्यस्त है। हमारा जीवन अन्तिम दाँव पर लगा हुआ है और हम प्रलोभन के झंझावातों के भव्याकार रूपाकारों के पैंतरे सँभाल रहे हैं। हम सभी जीवन खोज रहे हैं। अब शान्ति, सद्भाव राजनीति के चश्में से मत देखिए; मात्र आस्था और पूजा-अर्चना के संस्थानों में मत झांकिये; उसे जीवन की वास्तविकता, निर्मलता और सेवा-भावना में भी देखिए। राष्ट्र हमारी आत्मा का अमूल्य दर्पण है। वह राज सिंहासन की सीढ़ी नहीं है। मानवता में जीवन का उत्कर्ष खोजने की ज़रूरत महसूस कीजिए; अन्यथा न आपको वैभव-ऐश्वर्य बचा सकता है, न अहंकार आपको सुरक्षा कवच पहना सकता है। जीवन और जिजीविषा ही हमें विकास की मंजिलें दे सकते हैं।
तुलसीदास की एक चौपाई मुझे बरबस याद हो आई— “परहित सरिस धरम नहिं भाई/पर पीड़ा सम नहिं अघमाई।” हमारा जीवन एक तपस्या है। वह एक उच्च स्तर की साधना भी है। घृणा ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। दिन-ब-दिन जहर बोए जा रहे थे। शायद यह एक सबक है हम सभी के लिए। पंजाबी कवि पाश की एक कविता अचानक हमसे कुछ कह रही है— “भारत/मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द/जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए/बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं/इस शब्द के अर्थ/खेतों के उन बेटों में हैं/जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से/वक़्त मापते हैं/उनके पास, सिवाय पेट के, कोई समस्या नहीं/और वह भूख लगने पर/अपने अंग भी चबा सकते हैं/उनके लिए जिन्दगी एक परम्परा है/और मौत के अर्थ हैं मुक्ति।” (भारत)
.