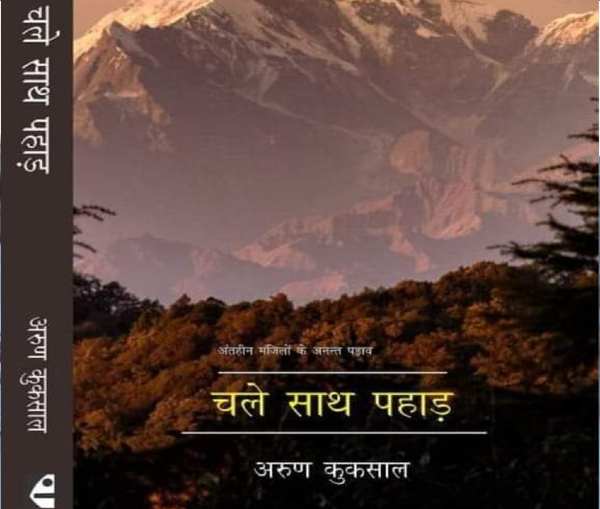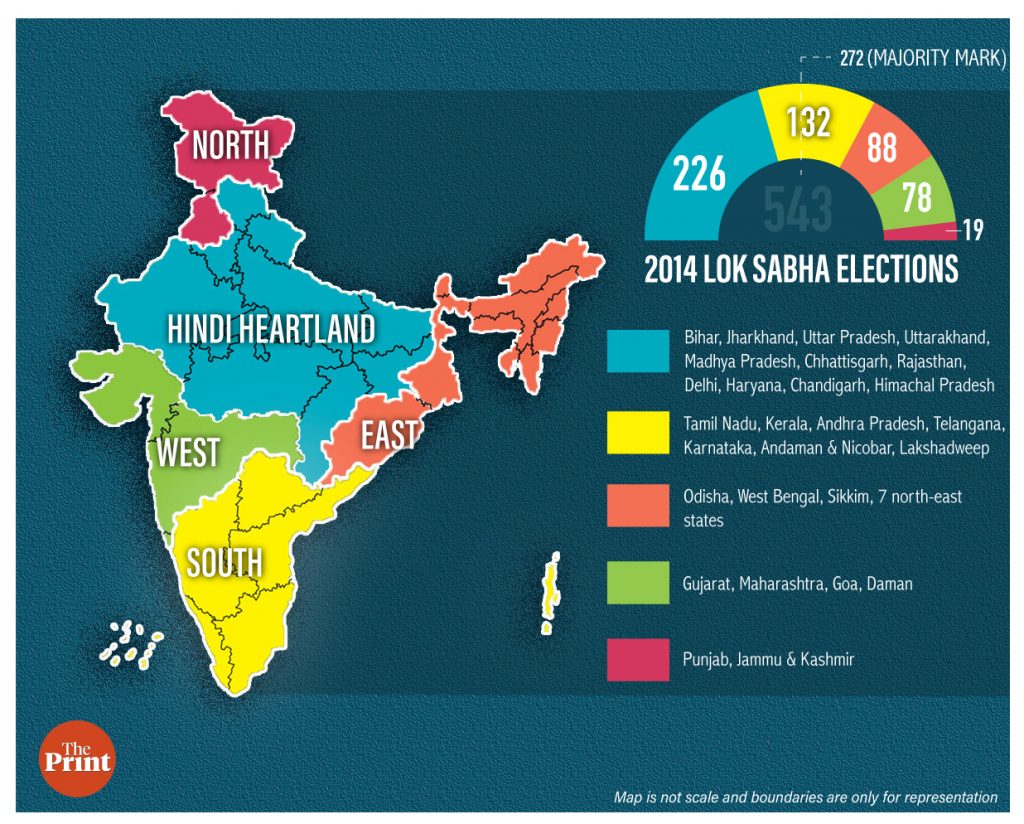महामारी के इस दौर में स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करती एक कहानी
महामारी की पहली लहर के बाद जब लगा था कि हालात अब सुधरने लगे हैं तभी दूसरी लहर ने भारत की आधी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है तो लाखों युवा बेरोजगार हो अवसाद में जी रहे हैं। आज इस निराशा भरे माहौल में भारत को जरूरत है हिम्मत कर फिर से अपने पैरों में खड़े होने की और महामारी के साथ जीना सीखते हुए आगे बढ़ने की। डेढ़ करोड़ से दो करोड़ का टर्नओवर और चौदह से पंद्रह लाख की सालाना आय। मन में कुछ करने की सच्ची लगन हो और बचपन से अच्छा मार्गदर्शन मिले तो सफलता कदम चूमती है। कुछ यही कहानी है मूल रूप से उत्तराखंड के गांव फरसौली, भवाली में 15 जून 1969 को नन्द किशोर भगत (भगतदा) के घर जन्में संजीव भगत की।
संजीव भगत का परिवार एक मध्यमवर्गीय परिवार था जिसमें उनके पिता फॉरेस्ट में क्लर्क, माता गृहणी और दादा जी की भवाली में छोटी सी दुकान थी। संजीव ने अपने बचपन के दिन बड़े ही मुफ़लिसी में काटे उनकी विद्यालयी शिक्षा नैनीताल से हुई। कभी-कभी तो यह स्थिति आ जाती थी कि उनके पास विद्यालय आने-जाने तक के लिए पैसे नही होते थे। संजीव के पिता उन्हें बचपन से ही स्वरोज़गार करने के लिए प्रेरित करते थे। वह स्वयं भी अपने समय से कहीं आगे की सोच लेकर चल रहे थे, नन्द किशोर भगत (भगतदा) एक बार अपनी सरकारी नौकरी छोड़ इलाहाबाद स्थित समाचार पत्र ‘अमृत प्रभात’ में नौकरी करने चले गये थे पर उन्हें अपने परिवार की वजह से वहाँ से वापस आना पड़ा।
भगतदा ने वर्ष 1977 में पदमश्री सुखदेव पांडे की मदद से पूरी तरह से वानिकी पर आधारित एक शानदार मैगज़ीन ‘बनरखा’ निकाली थी पर आर्थिक कारणों से यह सिर्फ एक साल बाद ही बन्द हो गई। उसके बाद वह ‘उत्तराखण्ड भारती’ और ‘नैनीताल समाचार’ से भी जुड़े रहे। आर्थिक स्थिति मज़बूत न होने के बाद भी शिक्षा के माहौल में पल-बढ़ रहे संजीव जब ग्यारवीं कक्षा में आए तभी उन्होंने ‘उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड’ के कार्यपालक अधिकारी कमल टावरी को कोई उद्योग स्थापित करने के लिए पत्र लिखा।
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य छोटे-छोटे उद्योगों तथा कम पूँजी निवेश के उद्योगो को स्थापित कराकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। अपने समय के बेहतरीन आईएएस रहे कमल टावरी का ज़ोर ग्राम स्वराज पर अधिक रहा है। उन्होंने इस पत्र को गम्भीरता से लिया और पत्र के जवाब में कुछ दिन बाद हल्द्वानी से कुछ लोग उद्योग का मॉडल देखने आए तो वह एक किशोर को देख चौंक गये।
संजीव को एसबीआई बैंक से लोन लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। जिसकी शिकायत उन्होंने ‘उद्योग बन्धु’ में भी की थी। ‘उद्योग बन्धु’ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया एक संगठन है, इसके अलावा यह उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए है जो विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु कार्य करता है। तत्कालीन डीएम दीपक सिंघल ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई की पर फिर भी उनका लोन स्वीकृत नही हुआ।
इसके बाद संजीव ने अपने पिताजी के पचास हज़ार रुपए से 1989 में फूड प्रोसेसिंग के लिए बिल्डिंग बनाई। 1989-1995 तक नैनीताल में रह प्राइवेट माध्यम से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके साथ ही वह दैनिक समाचार पत्र ‘उत्तर उजाला’ से जुड़ गये और इससे ही उनका जेबख़र्च भी चलता था। पत्रकारिता की ओर मुड़ रहे संजीव ‘दैनिक जागरण’ के ब्यूरो चीफ भी बन गये।

वर्ष 1993 में उद्योग लगाने के लिए संजीव भगत का 2,63,000 का लोन पास हुआ जिससे उन्होंने ‘फूड प्रोसेसिंग’ की फैक्टरी स्थापित की। ‘फूड प्रोसेसिंग’ उद्योग का मतलब खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश करने के कारोबार से है। भारत में लोगों की तेजी से बदलती लाइफ स्टाइल ने खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग में लगातार बढ़ोतरी की है।
पत्रकारिता में रम चुके संजीव के लिए पत्रकार होने का रौब छोड़ना और खुद का अख़बार शुरू करने का सपना छोड़ना मुश्किल काम हो रहा था पर उन्होंने फूड प्रोसेसिंग को ही अपना कैरियर बनाने की ठान ली थी। उन्होंने कभी किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नही भरा। संजीव की तीनों बहने उच्च शिक्षा प्राप्त थी जिनमें से उनकी बड़ी बहन ने इग्नू से फूड प्रोसेसिंग से सम्बंधित कोर्स किया था। उन्होंने संजीव की उद्योग स्थापित करने के शुरुआती दिनों में बहुत मदद की।
वर्ष 1993 में जब यह काम शुरू हुआ तो संजीव ने इसको लेकर तीन साल का लक्ष्य रखा था। वर्ष 1994 में उन्होंने जब बाज़ार में सामान डाला तो उनका सारा पैसा बाज़ार में फंस गया। वर्ष 1995 में संजीव के पिताजी ने फिर अपनी जमापूंजी से उनकी मदद करी। वर्ष 1996 में उनका थोड़ा पैसा बाज़ार से वापस आने लगा। वर्ष 1996-97 में नुकसान में रहकर भी उन्होंने उद्योग चलाया।

वर्ष 1998 फरसौली में फूड प्रॉडक्ट्स का ‘नैनीताल फूड प्रॉडक्ट्स’ नाम से अपना पहला शोरुम खोलने के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नही देखा। भवाली के पास ज्योलीकोट में वर्ष 2004 में उन्होंने अपना दूसरा शोरूम बनाया पर वह आपदा में बह गया। इसके बाद उन्होंने भवाली में ही शोरूम बनाने के लिए जमीन ली पर काम अच्छा चल जाने पर बाद में वर्ष 2011 में उन्होंने उस जगह एक होटल बनाया। इस समय संजीव भगत के ‘नैनीताल फूड प्रॉडक्ट्स’ नाम से पांच शो रूम चल रहे हैं। जिसमें दो का स्वामित्व उनके और तीन अन्य के पास है।
अपनी शुरुआत के 27 वर्ष बीत जाने के बाद उनका उत्पाद ‘फ्रुटेज़’ उत्तराखण्ड में अब एक ब्रांड बन गया है जिसका डेढ़ से लेकर दो करोड़ का टर्नओवर है और इससे संजीव की सालाना कमाई पन्द्रह से बीस लाख की है। वह तीस से चालीस लोगों को प्रत्यक्ष और इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त करने वालों में उनकी फैक्ट्री, शोरूम और होटल में काम करने वाले लोग शामिल हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके उत्पादों के लिए फल लगाने, तोड़ने, पैकिंग तैयार करने वाले लोग शामिल हैं।
उनकी संस्था क्षेत्रीय स्तर पर फलोत्पादन को बढ़ावा दे रही है जिसके अन्तर्गत उनकी संस्था द्वारा गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण भी देती है।

इस बीच संजीव भगत ने व्यापार की कई अनुभव भी प्राप्त किए जिसमें उनकी विफलता भी शामिल है। व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से संजीव अपने उत्पादों को बेचने अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, दिल्ली और लखनऊ भी ले गये पर वहाँ उन्हें कोई लाभ नही मिला। संजीव कहते हैं कि “हर उत्पाद के बिकने का अपना एक क्षेत्र होता है। ‘बुरांश’ उत्तराखण्ड का राजकीय वृक्ष है तो नेपाल का राष्ट्रीय। हिमालयी क्षेत्र के लोग तो इसे पहचानते हैं पर मैदान आते-आते लोग इससे अनभिज्ञ हो जाते हैं। वहाँ तक उत्पाद पहुँचाने पर परिवहन, रखरखाव की लागत भी बढ़ जाती है।
फूड प्रोसेसिंग के कार्य में लोगों के स्वाद की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दक्षिण भारतीयों और उत्तर भारतीयों के खाद्य पदार्थों और खानपान में अंतर तो होता ही है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। कोरोना की वजह से अभी काम कम है पर स्थिति सामान्य होने के बाद वह काम बढ़ाएंगे जिसमें वह इम्युनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स भी शामिल करेंगे। स्वरोज़गार और व्यापार के क्षेत्र में कोरोना के बाद से ही कुछ बढ़ोतरी देखने में आई है। सब जगह से हार के आने के बाद स्वरोज़गार ढूंढना और किसी उद्योग बसाने के बारे में सोचना एक हारी हुई लड़ाई को जीतना जैसा है।
अगर किसी के घर में कोई बीमार है या किसी को अपनी बेटी का विवाह करवाना है तो लोग मदद कर लेंगे पर यदि आप व्यापार शुरू करने के लिए किसी से मदद मांगेंगे तो कोई साथ देने के लिए तैयार नही होता। लोग प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित ज्यादा करते हैं। कुछ ताने देते हैं कि यह क्या व्यापार करेगा। लोन खाने के लिए उद्योग लगाया होगा।” व्यापार के प्रति हमारी जो सोच है उसके लिए हमारा सामाजिक ढांचा जिम्मेदार है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक या कोई सरकारी अधिकारी बनाने के लिए ही तैयार करते हैं। हम यह कभी नही सोचते कि हमारा बच्चा व्यापारी, खिलाड़ी, गीतकार, नृतक, पत्रकार या किसान बने।
“हमें अपनी सोच में रचनात्मकता लानी होगी। अभिवावकों से पहले शिक्षकों को अपने बच्चों से यह शुरुआत करनी होगी। इन दोनों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। मैं इसलिए सफल हूं क्योंकि मुझे एक दूरदर्शी सोच वाले पिता मिले।” कौशल के जरिए कम पूंजी वाले काम करना आसान है पर वह कभी हमारे सपने पूरे नही कर सकता। बड़े उद्योग लगाने के लिए डीपीआर बनानी होगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एक परियोजना की योजना और डिजाइन चरण के आउटपुट हैं। डीपीआर परियोजना के लिए एक बहुत ही विस्तृत और विस्तृत योजना है, जो परियोजना के लिए आवश्यक समग्र कार्यक्रम, विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, गतिविधियों और संसाधनों को दर्शाती है।
“हमें विपणन सीखना होगा। बैंक से लोन लेने के लिए वहाँ के चक्कर काटने होंगे, मशीनें लेनी होंगी, जमीन ख़रीदनी होगी, ढांचा बनाना होगा, बिजली- पानी की व्यवस्था करनी होगी और प्रतिस्पर्धा के बारे में जानना होगा। उद्योग स्थापित करने में सालों लग जाते हैं।”
आज हम असफ़ल, बेरोज़गार होने पर सरकार को कोसते तो हैं पर संजीव भगत की कहानी देखकर वास्तव में यह अहसास तो होता है कि कहीं न कहीं हम स्वयं भी इसके लिए दोषी हैं। अगर एक सत्रह साल का बच्चा उद्योग लगाने की ठान पूरे तन्त्र से लड़ सफलता प्राप्त कर एक आम आदमी के लिए उदाहरण बन सकता है तो हम भी क्यों किसी काम की शुरूआत करने से पहले सैंकड़ों बार सोचते हैं और जब निर्णय लेते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
.