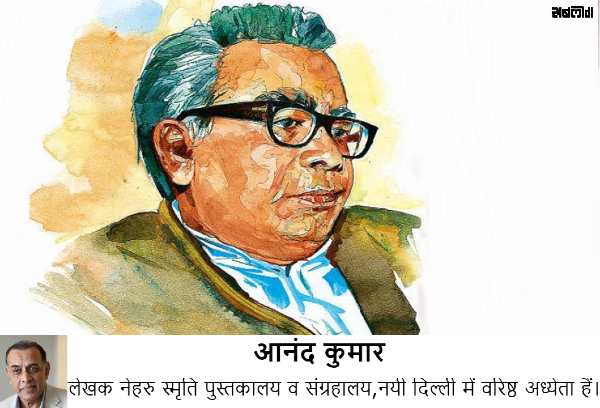क्यों और किसे चुनें अपना प्रतिनिधि – सुनील कुमार
- सुनील कुमार
हमारा देश इन दिनों अपने लिए सांसद और केन्द्र की सरकार चुनने की कवायद में लगा है, लेकिन इसी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को अमल होते हुए देखें तो क्या दिखाई देता है? क्या हम सचमुच ईमानदार लोकतान्त्रिक ढांचे को खड़ा करने में लगे हैं या हमारा मकसद सब कुछ जानते-बूझते चंद देशी पूँजीपतियों की ‘थैलियों’ को भरने भर का है? प्रस्तुत है, आम चुनाव की इस बेला में कुछ जानी-पहचानी बातों की पुनर्पड़ताल आवश्यक है|
कुछ ही दिनों में भारत की सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सहज सवाल उठता है कि उम्मीदवार चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वे अपने-अपने चुनाव अभियानों में क्यों भारी-भरकम रकम लगा रहे हैं? ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’ के अनुसार 1996 के लोकसभा चुनाव में 2500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे जो 2009 और 2014 में बढ़कर क्रमशः 10,000 और 35,547 करोड़ रुपये हो गए थे। वर्ष 2019 के इन चुनावों में 50 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जो कि अमेरिकी चुनाव से भी कहीं अधिक है। जिस तरह उद्योगपति अपने उत्पादों को बेचने के लिए विज्ञापन कम्पनियों का सहारा लेते हैं ठीक उसी तरह चुनाव में जनता तक पहुँचने के लिए विभिन्न पार्टियाँ प्रचार एजेंसियों की सहायता ले रही हैं। प्रचार कम्पनियों के माध्यम से 2009 से इलेक्ट्रानिक चुनाव प्रचार पर बहुत धन खर्च किया जा रहा है। चुनाव में काले धन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इससे यह माना जाता है कि चुनाव के बहाने ही पर्चा, पोस्टर, बैनर, झंडे, बैज बनाने वाले छोटे कारोबारियों, पेन्टरों इत्यादि की जेब में भी पैसे आ जाते हैं और अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार होता है। लेकिन जिस तरह से यह चुनाव अब इलेक्ट्रानिक माध्यमों और सोशल साईटों के जरिए लड़ा जा रहा है उससे यह पैसा भी कुछ मीडिया घरानों की जेब में ही जाता है।
पाँच साल में भाजपा सरकार विज्ञापन पर करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। चुनाव के दौरान और भी ज्यादा रकम खर्च कर अपनी पाँच साल की उपलब्धियों और ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ व अंतरिक्ष में ताकतवर बनने के सपने बेच कर वह दुबारा सत्ता में लौटना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी यूनिवर्सल आय (6,000 रू. प्रति माह) के सपने लोगों को दिखा रही है। क्षेत्रीय पार्टियाँ जाति और अस्मिता के सवाल पर चुनाव जीतना चाहती हैं। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, कोई भी पार्टी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्वतन्त्रता, सुरक्षा या साम्राज्यवाद-पूँजीवाद परस्त नीतियों पर अपना मुँह नहीं खोल रही हैं, जिसके कारण बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है और मेहनतकश आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं।
उपग्रह-रोधी मिसाइल का परीक्षण कर भारत को महाशक्ति बनाने का दुःस्वप्न दिखाना वास्तविकता से मुँह मोड़ने जैसा है। भुखमरी के ‘वर्ल्ड हंगर इंडेक्स’ (विश्व भूख सूचकांक) में भारत, पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे, 103 वें स्थान पर चला गया है जबकि 2014 में वह 55 वें स्थान पर था। हम पड़ोसी देश में एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, लेकिन ‘विश्व खुशहाली सूचकांक’ में पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे 133 वें स्थान पर हैं। सरकार जहाँ पकौड़ा बेचने को भी रोजगार मान रही है, वहीं बेरोजगारी की दर सर्वाधिक आठ प्रतिशत से अधिक पहुँच गई है जिसके चलते सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े ही सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। वर्ष 2014 में किसानों से किये गये वादों को सरकार पूरा नहीं कर पायी तो किसानों को पार्लियामेंट पर नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, जो कि किसी भी लोकतान्त्रिक देश के लिए शर्म की बात है। एक तरफ दलितों, अल्पंसख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासियों की जमीन को छीनकर पूँजीपतियों को दी जा रही है। लूट की इसी कमाई का दो-चार प्रतिशत खर्च कर पूँजीपति अपने मन-मुताबिक सरकार का गठन करते हैं।
चुनाव के नाम पर कुछ धनबली-बाहुबली, गुंडों-माफिया, बलात्कारियों को पैसा लेकर पार्टियाँ जनता पर थोप देती हैं और उन्हीं में से कुछ संसद में जाते हैं। यही कारण है कि पन्द्रहवीं लोकसभा में 300 सांसद करोड़पति-अरबपति थे, तो सोलहवीं लोकसभा में इनकी संख्या 442 हो गई थी। पन्द्रहवीं लोकसभा में 150 आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग संसद में पहुंचे थे, तो सोलहवीं लोकसभा में 179 सांसदों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज थे जिनमें से 114 पर संगीन अपराधों के मुकदमे थे। सभी पार्टियों को कॉरपोरेट जगत रिश्वत की एवज में चुनावी चंदा देते हैं। नतीजे में सरकार उसी पार्टी की बनती है जो कि पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की अच्छी-से-अच्छी सेवा कर सके। इसके बाद कारपोरेट जगत पार्टियों को दिये गये चंदे को सूद समेत कई गुना वसूल करता है। मुकेश अंबानी की कमाई प्रतिदिन 300 करोड़ रुपये है और उसने 2018 में बिलगेट्स, वॉरेन बफे और लैरी पेज जैसे वैश्विक पूँजीपतियों को पीछे छोड़ दिया था। इसी तरह गौतम अदानी की सम्पत्ति जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक दुगने से अधिक (125 प्रतिशत) हो गई। दूसरी तरफ, किसानों को अपनी फसलों का लागत मूल्य निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
जिसको हम बहुमत की सरकार कहते हैं वह आमतौर पर सिर्फ 12-15 फीसदी अधिक वोट पाकर ही बनती है। खुद को सर्वशक्तिमान मानने वाली मौजूदा केन्द्र सरकार भी कुल जमा 31 फीसदी वोट पाकर ही अस्तित्व में आयी थी। यह क्रम 1951 से ही चला आ रहा है, लेकिन आज तक यह लोकतन्त्र हमें पीने का मामूली साफ पानी तक मुहैय्या नहीं करा पाया है। शिक्षा-स्वास्थ्य तो दूर की बात है। आजादी के बाद से देश में प्रायः सभी दलों की सरकारें बनीं। यहाँ तक कि देश और प्रदेशों में अलग-अलग क्षेत्रीय सरकारें भी बनीं, लेकिन आज तक जनता की समस्याएँ कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। आमतौर पर ‘जन प्रतिनिधि’ सांसद, विधानसभाओं में जाकर अपने चुनाव में निवेश की हुई रकम सूद समेत वसूलने में व्यस्त रहते हैं। देशी-विदेशी पूँजीपतियों से पैसा लेकर सरकारें सहमति-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती हैं और लोगों की जीविका के साधन जल-जंगल -जमीन को पूँजीपतियों के हवाले कर देती हैं। पूँजीपति अपने मुनाफे की हवस में लोगों को उनकी बसी-बसाई जगहों से उजाड़ते हैं। जल-जंगल-जमीन से ‘दिन दुनी, रात चौगुनी’ सम्पत्ति को बढ़ाती है और सांसद, विधायक इस लूट में सहयोग कर अपने निवेश किए हुए पैसों को अगले चुनाव तक कई-कई सौ गुना बढ़ाने में लगे रहते हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान-मजदूर हैं लेकिन उनकी स्थिति बदतर होती जा रही है। रोटी-कपड़ा-मकान,जो किसी भी देशवासी के मौलिक अधिकार हैं, उससे भी देश की बहुसंख्यक जनता वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी समस्याएँ मुँह बाए खड़ी हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन उनके पास थे उन पर मुट्ठी-भर पूँजीपतियों का कब्जा होता जा रहा है। जल, जंगल, जमीन से आम जनता को उजाड़ा जा रहा है और खनिज सम्पदा की लूट जारी है। बड़े-बड़े बाँध बनाकर लोगों को उजाड़ा जा रहा है और नदियों के प्रवाह को रोका जा रहा है ताकि लूट को और बढ़ाया जा सके। इसका विरोध करने पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लाठी-डंडों से पीट-पीट कर झूठे प्रकरणों में फँसा दिया जाता है। न्यायपालिका इस पर अपना कानूनी जामा पहना देती है और लूट को कानूनी मान्यता मिल जाती है। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद से भारत की सभी पार्टियाँ केन्द्र व राज्य में सत्ता का सुख भोग चुकी हैं, लेकिन कोई भी पार्टी, सत्ता में रहते हुए इन नीतियों के खिलाफ कोई आन्दोलन नहीं कर पायी। ये वे ही नीतियाँ हैं जिनके कारण किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। किसानों का अन्न बेचने वाली कारगिल, मेनसेन्टों जैसी कम्पनियाँ माला-माल होती जा रही हैं, लेकिन किसानों के अन्न की कीमत संसद में तय की जाती है, जबकि खेती में काम आने वाली खाद, कीटनाशक, दवाएँ, ट्रैक्टर, पम्पसेट इत्यादि बनाने वाली कम्पनियाँ उनका मूल्य खुद निर्धारित करती हैं। सवाल है कि क्या लोकतन्त्र में चुनाव की मार्फत ऐसे ही राजनीतिक दलों, समूहों को सत्ता सौंपी जाए या खुद नागरिक जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने लिए ठीक प्रतिनिधि चुना जाए?

लेखक राजनीतिक-सामाजिक-मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और विभिन्न संस्थान और विश्वविद्यालयों में शोध करते है|
सम्पर्क- sk688751@gmail.com
ये भी पढ़ सकते हैं- राजनीतिक पार्टियों के लिए घोषणा पत्र