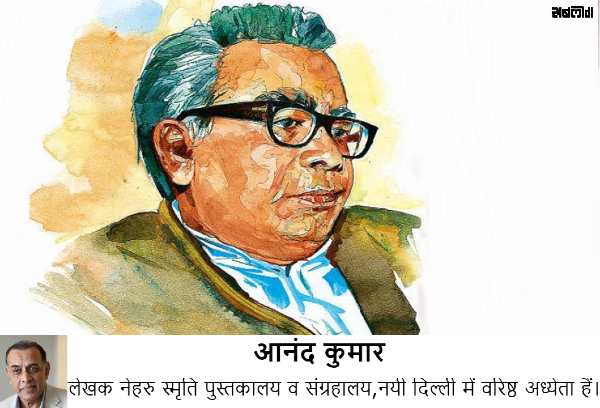चुनाव पूरा तन्त्र लड़ता है
पूरी दुनिया में इस समय चुनावी लोकतन्त्र पर निगाह डालने की जरूरत है। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की जीत हार के लिए सत्ता के उन हिस्सों की भूमिका ज्यादा बढ़ी है जो कि मतदाताओं के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं होती है। गौरतलब है संसद और लोकतन्त्र दो भिन्न शब्द है। लोकतन्त्र संसदीय प्रक्रिया का लक्ष्य है यानी लोक का तन्त्र का विकास लक्ष्य है। संसदीय प्रक्रिया लक्ष्य नहीं है। वह लोक का तन्त्र के उद्देश्य को हासिल करने का माध्यम है। संसदीय प्रक्रिया के संतुलित तरीके से काम करने के लिए उसे मुख्यत: तीन हिस्सों में बांटा गया है जिसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसमें अहमियत मतदाताओं द्वारा चुनी गई संसद की मानी जाती है। लेकिन संसदीय प्रक्रिया के इन किरदारों में जब ये होड़ शुरू हो जाती है कि उनके अधिकार क्षेत्र में संतुलन की स्थिति के बजाय उनका वर्चस्व हावी हो तो सबसे पहले इस प्रक्रिया के उद्देश्य यानी लोकतन्त्र को पीछे छोड़ने का इरादा दिखने लगता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने तो सत्ता संतुलन की स्थापित मानकों को तेजी से उलटा है और इस होड़ में वैश्विक स्तर की सक्रियता भी खुलेतौर पर बढ़ रही है। एक पहलू पर गौर करें कि कैसे पूरी दुनिया में इस समय चुनावों में खुफिया एजेंसियों या खुफियागिरी की भूमिका सबसे ज्यादा बढ़ी है।
स्थापित व सरकारी खुफिया एजेंसियों का मतलब गोपनीय तरीके से उस तरह की जानकारियाँ हासिल करने का एक ढाँचा नहीं है जिससे लोकतन्त्र और समाज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश होती हो। खुफिया एजेंसी सत्ता के एक केन्द्र के रूप में देखा जाना चाहिए और उसका चरित्र एक राजनीतिक उद्देश्य के अनुरूप विकसित होता है। यदि सैन्य तन्त्र की स्थापना के उद्देश्य हो तो खुफिया एजेंसियाँ उसी के अनुरूप काम करती है। लिहाजा संसदीय लोकतन्त्र की खुफिया एजेंसियों में भी लोकतन्त्र का निषेध हो सकता है यदि संसदीय सत्ता पर सैन्य तन्त्र के वर्चस्व की होड़ विकसित हो जाए।
भारत में 1952 के बाद से चुनावों में खुफिया एजेंसियों की भूमिका के बढ़ने के दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन ये खुफिया एजेंसियाँ दुनिया में साम्राज्य स्थापित करने वाली राजनीतिक सत्ता से संचालित होने वाली रही है। यानी विदेशी खुफिया एजेंसियों की भूमिका उसी तरह रही है जैसे विदेशी पैसों की रही है। गरीब और पिछड़े देशों में इस तरह की भूमिका अब भी देखी जाती है। मसलन श्रीलंका के पिछले चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में ये आरोप सामने आया कि कैसे पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी के अलावा अन्य देशों की सत्ता का भूमिका सत्तारूढ़ पार्टी को हराने में रही है। इस बार तो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी सामने आया कि रूस के राष्ट्रपति पूतिन ने हिलेरी को हराने के लिए साइबर के जरिये कैसे कोशिश की है। चुनाव ही जब किसी देश की सत्ता को देश के अंदर या देश के बाहर से नियन्त्रित करने की प्रक्रिया के रूप में कारगर हो तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के जरिये ही सत्ता को नियन्त्रित करने वाली शक्तियाँ अपनी भूमिकाएँ तय करती है।
कहने को भारत में संसदीय चुनाव पार्टियाँ लड़ती है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में एक पहलू ये देखने को लगातार मिला है कि मतदाताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच रिश्ता कमजोर होता गया है। दोनो के बीच की कड़ी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतार छोटी ही नहीं लगभग समाप्त हो गई है। मतदाताओं के बारे में राजनीतिक पार्टियों के बीच यह आम धारणा है कि मतदाताओं की याददाश्त क्षमता क्षणिक होती है और वे पाँच साल के अपने अनुभवों के आधार मत नहीं देते है बल्कि तात्कालिक और भावनात्मक मुद्दों को लेकर मतदान केन्द्रों की तरफ जाते हैं। इसीलिए मतदान के पूर्व के कुछ दिन व महीने महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उन दिनों में मतदाताओं को आकर्षित, प्रभावित करने और उन पर भावनात्मक दबाव बनाने की सबसे ज्यादा कोशिश होती है। यानी मतदाताओं के पूरे मनोविज्ञान को संचार के माध्यमों से बदल देने की सबसे ज्यादा कोशिश होती है। गौर करें कि उन दिनों राजनीतिक पार्टियाँ क्या करती है और राजनीतिक पार्टियों के अलावे सत्ता की मशीनरियाँ क्या-क्या करती है? राजनीतिक पार्टियों के नेता ज्यादा से ज्यादा जनसंचार के साधनों और हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करते हैं। कहें तो ज्यादा से ज्यादा पैसे का इंतजाम करने की होड़ होती है। लेकिन यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि पैसा सीधे तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने का माध्यम नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर मतदाता के पास पैसे सीधे भी पहुँच जाए तो मतदाता ज्यादा से ज्यादा पैसा देने वालों को अपना वोट दे देगा। पैसे की अलग-अलग रूपों में भूमिका तय की जाती है। सीधे पैसे से वोट खरीदने की एक सीमा हो सकती है। दूसरा पैसा आकर्षण, प्रभाव व दबाव बनाने में भी एक हद तक सहायक होता है। लेकिन उस आकर्षण, दबाव व प्रभाव के लिए सामग्री तो तैयार होनी चाहिए। मसलन अमेरिका के चुनाव में एक सामग्री एफबीआई ने ये तैयार कर दी कि हिलेरी का सत्ता में आने पर अपना छिपा एजेंड़ा होता है। हिलेरी के खिलाफ एक अविश्वसनीयता का माहौल एफबीआई ही रच सकती थी। किसी नेता द्वारा आरोप लगाने से हिलेरी के खिलाफ माहौल नहीं बन सकता था। एफबीआई जब हिलेरी के खिलाफ ये माहौल रच रही है तो जाहिर है कि वह एक ऐसी सत्ता का निर्माण करने में सहायक हो रही है जिसमें उसका वर्चस्व बढ़े। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खुफिया एजेंसी एफबीआई की चुनाव में हराने और जीतने की ताकत का एहसास कर लें।
मसलन अमेरिका के चुनाव में एक सामग्री एफबीआई ने ये तैयार कर दी कि हिलेरी का सत्ता में आने पर अपना छिपा एजेंड़ा होता है। हिलेरी के खिलाफ एक अविश्वसनीयता का माहौल एफबीआई ही रच सकती थी। किसी नेता द्वारा आरोप लगाने से हिलेरी के खिलाफ माहौल नहीं बन सकता था। एफबीआई जब हिलेरी के खिलाफ ये माहौल रच रही है तो जाहिर है कि वह एक ऐसी सत्ता का निर्माण करने में सहायक हो रही है जिसमें उसका वर्चस्व बढ़े। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खुफिया एजेंसी एफबीआई की चुनाव में हराने और जीतने की ताकत का एहसास कर लें।
भारत में पिछले संसदीय चुनावों के पूर्व यह पाते हैं कि कैसे आतंकवाद का एक माहौल बनता है।ये माहौल आतंकवाद की वास्तविक घटनाओं की वजह से नहीं बनता रहा है बल्कि आतंकवाद के बढ़ने की आशंकाओं का माहौल होता है और वे आशंकाएँ भी बनावटी होती है। चुनाव के ऐन मौके पर अचानक यदि ये दावा किया जाने लगता है कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करने वाले कई आतंकवादी पकड़े गए और उनके चेहरों को खास तरह के कपड़ों से ढंककर उनकी तस्वीरों को प्रचारित किया जाए और उनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध होने का प्रचार किया जाता है तो ये चुनाव के मौके पर एक खास तरह की राजनीति को आकार लेने में मदद कर सकता है। भले ही वह बाद में फर्जी साबित हो। लेकिन उसका चुनाव के मौके पर तो काम पूरा हो जाता है। जैसा कि अमेरिका में एफबीआई के हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ आरोपों के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कह दिया था कि किसी तरह की जाँच की जरूरत नहीं है। और अब जब रिपोर्ट आई है तो आरोपों को धो पोछ दिया गया है।
जब लोकतन्त्र को मजबूत करने के बजाय संसदीय चुनाव की प्रक्रिया सत्ता के विभिन्न तन्त्रों द्वारा अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने की होड़ की प्रक्रिया बन जाती है तो राजनीतिक पार्टियाँ व नेता उन तन्त्रों के सेवक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भारत में हम देखते है कि हर राजनीतिक पार्टी सैन्य तन्त्र की आलोचना से भी घबराती है और सैन्य तन्त्र व सैन्य विचारधारा को राष्ट्रवाद के पर्याय के रूप में स्वीकार करने लगी है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र के दावे के बीच पिछले बीसेक वर्षों की खास उपलब्धि है। एक एक छवि का लोकतन्त्र में महत्व होता है। यदि हर सार्वजनिक जगहों पर बंदूक ताने सरकारी व किसी कारपोरेट कम्पनी के वर्दीधारी नजर आते हैं तो इसे लोकतन्त्र का विकास नहीं कहना चाहिए। वह वास्तव में सैन्य तन्त्र का विकास है। यानी इस तन्त्र ने चुनावी प्रक्रिया में अपनी अहमियत बढ़ा ली है। और हम बहस ये करते नजर आते हैं कि पाँच वर्षों में एक क्षण के लिए मतदाताओं की कतार लम्बी हुई है या छोटी। मतदाताओं के कतार का तन्त्र विकसित होना महत्वपूर्ण होता है। खुफिया तन्त्र की अहमियत इस हद तक बढ़ गई है कि नागरिक अधिकार व मानवाधिकार बेहोशी के आलम में पहुँच गए है। लेकिन तन्त्र के रूप में यहाँ केवल खुफिया एजेंसी को ही एकमात्र नहीं समझे। तन्त्र विविध रूप में सक्रिय होता है और एक दूसरे को सहयोग करता है।
चुनावी प्रक्रिया में लोक के तन्त्र विकसित नहीं हो रहे है बल्कि सत्ता के वे तन्त्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं कि इतिहास में तानाशाह व फांसीवाद के रूप में चिन्ह्ति किए जाते रहे हैं। संसदीय चुनाव हो रहे हैं लेकिन ये लोकतन्त्र के बजाय सत्ता के उन तन्त्रों को मजबूत करने के लिए हो रहे है जो कि अपनी प्रवृति में सैन्यकरण वाले है। गौर करें कि संसदीय चुनाव की प्रक्रिया में मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में जो नेतृत्व उभरे हैं, उनका विश्लेषण किस रूप में किया जा सकता है। क्या वे लोकतान्त्रिक मूल्यों, लोकतान्त्रिक परम्पराओं, लोकतान्त्रिक मान्यताओं के प्रतिनिधि के बतौर उपस्थित होते है? नरेन्द्र मोदी वास्तविक तौर पर किस तरह की छवि के प्रतिनिधि के रूप में परिभाषित होते हैं? मनमोहन सिंह कभी जनता या मतदाताओं के बीच सक्रिय नहीं रहे और वे संसदीय चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर देश का नेतृत्व करने लगे। लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकें लेकिन दस वर्षों तक प्रधानमन्त्री बने रहें। वास्तविकता तो ये सामने आती है कि सत्ता के तन्त्र चुनावी प्रक्रिया में अपना प्रतिनिधि व नेतृत्व चुनता है और उसे ही हम लोक के तन्त्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।
यहाँ एक रूपक के जरिये हम पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। किसी स्थिति में बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी की जरूरत कैसे पैदा होती है। मान लें कि एक व्यक्ति अपने पास घन संग्रह करता है और उसे तिजोरी में रखना जरूरी हो जाता है तो उसे बचाने की जरूरत भी महसूस होगी। उसे इसकी जरूरत क्यों होती है और वह उसे बचाने के लिए क्या कर सकता है? उसे जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि वह जिस तरह से घन की उगाही कर रहा है उस प्रक्रिया को वह बनाए रखना चाहता है और उस संग्रहित घन को बचाने के लिए उसे उस तरह की ताकत की जरूरत महसूस होगी जो बहुत सारे लोगों की ताकत का अकेले जवाब दे सकें। इसी को सुरक्षा का नाम दिया जाता है। स्पष्ट करने के लिए इस रूपक का एक दूसरा दृश्य भी हम देखते हैं। यदि मान लें कि घन किसी एक व्यक्ति के बजाय बहुत सारे लोगों के बीच बंटा हुआ हो तो वहाँ किसी को किसी से सुरक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? वहाँ असुरक्षा का बोध ही नहीं होगा। यहाँ असुरक्षा का बोध किसे है जो कि बहुत सारे लोगों के बीच वितरित होने वाले घन को अपने नियन्त्रण में रखना चाहता है और वह अपनी असुरक्षा का उपाय हथियारों के जरिये करता है। हथियार ही सुरक्षा के दूसरे नाम के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इस तरह हम देख सकते है कि आर्थिक स्तर पर बढ़ती गैर बराबरी की स्थिति में ही क्यों सैन्य तन्त्र को बढ़ावा दिया जाता है। गाँव के एक समान्त या जमींदार को लठैतों का गिरोह रखना पड़ता था। इसी तरह चुनाव प्रक्रिया पर लठैत तन्त्र और घन तन्त्र ही आखिरकार अपनी जीत दर्ज कराते है।
संसदीय प्रक्रिया में मतदाताओं को ये समझने की जरूरत है कि लोक के तन्त्र को मजबूत करने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बन रहा है या फिर उन तन्त्रों को मजबूत करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है जो कि आखिरकार उसकी स्वतन्त्रता और सदियों के संघर्षों के बाद हासिल अधिकारों के लिए घातक हो सकते हैं। राजनीतिज्ञ यदि मतदाताओं को सम्बोधित कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपने को मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में ही मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। बल्कि ये भी हो सकता है कि वह उन तन्त्रों के प्रतिनिधि के रूप में खुद को मजबूत करने के लिए मतदाताओं से सहयोग का छल कर रहा हो जो तन्त्र लोगों को नियन्त्रित करने का उद्देश्य रखते हो। और वह प्रतिनधि भी उसी नियन्त्रण करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो। इसकी पड़ताल इस तरह से की जा सकती है कि वह प्रतिनिधि किस तरह की सामग्री और किस तरह के संसाधनों के जरिये मतदाताओं के बीच पहुँच रहा है। धनवानों के संसाधन और सैन्यकरण की सामग्री यानी भाषा से गैरबराबरी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और न ही लोकतन्त्र को मजबूत किया जा सकता है। यदि सामग्री में सैन्यकरण की भावना है और पैसे वालों के संसाधन है तो ये मान लेना चाहिए कि वह लोकतन्त्र के प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय नहीं होने की वचनबद्धता से बंधा हुआ है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाता को ये देखना होगा कि सत्ता के किस तन्त्र की भाषा में कौन राजनीतिक पार्टी व उसके नेता बात कर रहे हैं। यदि राजनीतिक नेता मंच पर उसी भाषा में बात कर रहा है जिसकी सामग्री सत्ता का कोई तन्त्र तैयार करके उसे मुहैया करा रहा है तो उन दोनों के बीच के रिश्तों को समझना होगा। लोकतन्त्र में मतदाताओं के लिए यह भूल मानी जाती है कि वह केवल किसी एक नेतृत्व की चिकनी चुपड़ी या मीठी मीठी बातों या भावुक बातों में बहकर पाँच सालों के लिए सत्ता उसे सौप दें। पाँच सालों में जो तन्त्र विकसित होते है वे लम्बे समय तक असर करते हैं। इसीलिए पाँच साल के लिए फैसले पाँच साल के अनुभवों के आधार पर ही किए जाने चाहिए। संसदीय चुनाव में तो ये कहा जाने लगा कि चुनाव से पहले यदि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाए तो चुनाव जीता जा सकता है। साम्प्रदायिक दंगे हो जाए या साम्प्रदायिकता का माहौल बन जाए तो चुनाव जीता जा सकता है। यानी सत्ता के तन्त्र इस तरह से लोकतन्त्र के चुनाव के नतीजों को निर्धारित करने की क्षमता ऱखने की स्थिति में पहुँच जाए तो हमें लोकतन्त्र को भूल जाना चाहिए। यानी इतिहास में पीछे लौट जाने की प्रक्रिया में हम शामिल हो गए है। मतदाताओं की याददाश्त कमजोर नहीं होती है। उसे बस याद करने की फुरसत नहीं देने की कोशिश होती है और ये काम पूरा तन्त्र मिल जूलकर चुनाव के दौरान करता है। लोकतन्त्र के लिए यही बड़ी चुनौती है। जन संचार माध्यमों ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है।