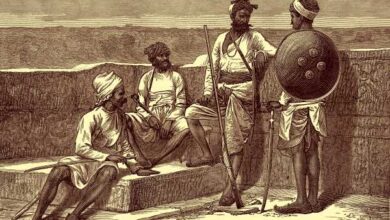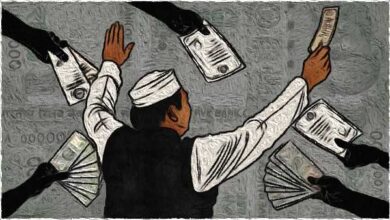नदी हमारी सभ्यता को सींचती हैं
आप जब महानगरीय जीवन शैली में स्वयं को सहसा ही जकड़ा हुआ पाते हैं, तब आपको नदी के किनारे बसा वो अपना शहर याद आता है, या वो गाँव याद आता है, जहाँ के नदी-पोखरों में आपके बचपन की अनेक स्मृतियाँ बसी हुई हैं। वस्तुतः नदी के किनारे बसा वो अपना शहर, वो गाँव याद ही इसलिए आता है कि आप बेतरतीब से फैले जीवन को समेट कर, वापस कुछ क्षण उस नदी के समीप जा बैठ कर कोई गीत गुन-गुना सकें, अपने पुरखों को तर्पण दे सकें या किसी निषाद कन्या से मोल मे लिया एक दीप नदी किनारे प्रज्वलित कर सकें। नदी के समीप बिताए यह कुछ क्षण भी हमें भाव-विभोर कर सकते हैं।
नदियों से हमारा नाता उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। नदियों ने सभ्यताओं का सृजन ही नहीं किया अपितु सभ्यताओं को वात्सल्य एवं भावयुक्त प्रेमाश्रय भी प्रदान किया। इस भावयुक्त प्रेमाश्रय ने ही मानव को संस्कार दिए और संस्कार से ही संस्कृति का सृजन हुआ। नदी के वेग से ही मानव के भाव-वेग का विकास हुआ और जहाँ भाव है वहाँ संभावना भी उत्पन्न हुई, इन्हीं संभावनाओं की तलाश में मानव ने विषम परिस्थितियों में भी सभ्यता को सँजों कर, जीवन के नए आयामों के द्वार खोले।
मानव जाति का नदियों के प्रति लगाव विश्व की हर सभ्यता में अंकित है। सर्वप्रथम यह अभिव्यक्ति हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ऋग्वेद के नदिसूक्त में सभ्यता को पोषित करने वाली प्रमुख नदियों के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए गये हैं। इनमें सात नदियों के नाम प्रमुखता से दोहराए गये हैं। जिसके द्वारा हमें मानव सभ्यता के प्रतिस्ठान “सप्त-सैन्धव” का भौगोलिक विस्तार भी ज्ञात होता है। इन नदियों में से सरस्वती का वर्णन हमें बार-बार मिलता है। परन्तु वर्तमान में इसके साक्ष्य हमें, अतिसूक्ष्म पैलिओचैनल्स (शीलाप्रणाली) के द्वारा ही प्राप्त होते हैं।
 भूतात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि प्लेट-टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण सरस्वती नदी लुप्त हो गयी। आइसोटोपिक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 3000 BCE से 2700 BCE के बीच इन पैलिओचैनल्स में जल प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के पश्चिम मे बहने वाली घग्गर-हकरा नदी का क्षेत्र है। कहने का आशय है कि नदी के विलुप्त होने के कारण भले ही अनेक हो, पर नदी के ह्रास से सभ्यता का भी ह्रास होता है, यह तय है।
भूतात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि प्लेट-टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण सरस्वती नदी लुप्त हो गयी। आइसोटोपिक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 3000 BCE से 2700 BCE के बीच इन पैलिओचैनल्स में जल प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के पश्चिम मे बहने वाली घग्गर-हकरा नदी का क्षेत्र है। कहने का आशय है कि नदी के विलुप्त होने के कारण भले ही अनेक हो, पर नदी के ह्रास से सभ्यता का भी ह्रास होता है, यह तय है।
वर्तमान में गंगा व यमुना की दशा भी किसी से छिपी नहीं है। विगत कुछ वर्षों में गंगा को बचाने की मुहिम शुरू की गयी। एक हद्द तक यह प्रयास सफल भी हो रहे हैं। परन्तु यह सरकारी प्रयास अभी भी तकनीकी तौर पर जन-समुदायों के साथ एक बेहतर तालमेल स्थापित नहीं कर सके हैं। जन-समुदायों से विशेष आशय है, निषाद समुदाय से, जिनकी जीविका नदियों पर आश्रित है। वर्ष 2016 में बनारस में आधुनीक यांत्रिक नावों (ई-बोट्स) का वितरण किया गया था, जिसे लेकर समुदाय के एक वर्ग ने विरोध किया था। उनका कहना था कि हर छोटा मछुआरा ई-बोट्स का वहन नहीं कर पाएगा और इससे छोटे मछुआरों की जीविका पर असर पड़ेगा।
चप्पू से चलने वाली छोटी नाव की लागत और रख-रखाव काफी कम लागत पर हो जाता है, जो छोटे मछुवारों को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। यह भी हो सकता है कि किसी समुदाय की जीविका से जुड़े विषयों पर सरकार को सहजता से आगे बढ़ना चाहिए। निषाद समुदाय स्वयं को गंगापुत्र कहने में गर्व की अनुभूति करते हैं। निषाद एक ऐसा समुदाय है जो नदियों के काया-कल्प में अहम भूमिका निभा सकते हैं। शर्त यह है कि सरकार भी उन्हें इस मिशन में अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान करे।
नदियों के पारिस्थितिकी तन्त्र के ह्रास के जिम्मेदार भी हम हैं और इस ह्रास ने हमें नदियों से दूर भी किया है। ना जाने कितने ही नदियों के किनारे लगने वाले मेले हमारे सामने ही लुप्त होते जा रहे हैं। आज की आवश्यकता है कि हम नदियों की ओर कूच करें और उनके समीप बैठ कर अपने स्नेह से उन्हें सींचें जिन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को हजारों वर्षों तक सींचा है।
.