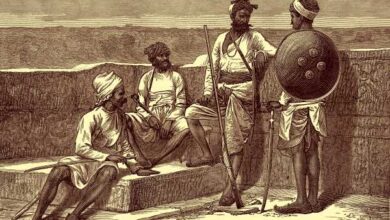हिन्दी में शोध का धन्धा
उच्च शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है अनुसन्धान, उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है अनुसन्धान और उच्च शिक्षा का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है अनुसन्धान। आज के अनुसन्धान की दशा देखकर लगता है कि शोध को उपाधि का पर्याय मान लेना आधुनिक भारत की एक दुर्घटना है और इसके लिए हमारी वह व्यवस्था सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जिसने इसे नौकरी से जोड़ दिया और इस तरह मांग और पूर्ति के गणित में उलझा दिया।
यह सही है कि सभ्यता के विकास में अबतक जो कुछ भी हमने अर्जित किया है वह सब अनुसन्धान की देन है और जिज्ञासु मनुष्य, साधनों के अभाव में भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण अनुसन्धान से जुड़ा रहता है। जेम्सवाट ने किसी प्रयोगशाला में पता नहीं लगाया था कि भाप में शक्ति होती है और न तो धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का पता लगाने के लिए न्यूटन को किसी प्रयोगशाला मे जाना पड़ा था। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने अभावों में भी उन्हे इतने बड़े सत्य के उद्घाटन के लिए विवश कर दिया।

हिन्दी में अनुसन्धान की नींव एक विदेशी जिज्ञासु ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक दायित्व निभाने के लिए रखी थी, वे थे ‘गार्सां द तासी’। 1839 ई. में फ्रेंच में “ इस्त्वार द ला लितरेत्युर ऐंदुई ऐंदुस्तानी” नामक उनकी कृति प्रकाशित हुई थी तथा इसके आठ वर्ष बाद इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। इसकी उपलब्धियां तथा गुणवत्ता विवादास्पद हो सकती हैं किन्तु इसमें हिन्दी उर्दू के कवियों का परिचय, नवीन तथ्य एवं सूचनाएं अनुसंधापरक दृष्टि की परिचायक है। यह एक व्यक्ति का उपाधिनिरपेक्ष निजी प्रयास है। हिन्दी अनुसन्धान के विकास में यह एक महत्वपूर्ण विन्दु है। उन्यासी वर्ष बाद एक दूसरे विदेशी विद्वान ने लन्दन विश्वविद्यालय से उपाधि सापेक्ष अनुसन्धानकार्य किया। वे थे जे.एन. कारपेन्टर और उनका विषय था ‘थियोलॉजी आफ तुलसीदास’। इस शोधकार्य पर उन्हें 1918 ई. में शोध उपाधि प्राप्त हुई।
इस तरह अनुसन्धान के दो आधार हैं, पहला वैयक्तिक प्रयास और दूसरा प्रतिष्ठानिक प्रयास।
हिन्दी अनुसन्धान के विकास में राष्ट्रीय और बौद्धिक जागरण का महत्वपूर्ण योगदान है। 1828 ई. से लेकर 1885 ई. तक का कालखण्ड इस दृष्टि से विशेष महत्व का है।
1828 ई. में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1849 ई. में विधवा विवाह का विरोध, 1856 ई. में इस विषय पर कानून बनना, 1857 ई. में प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा आर्य समाज की स्थापना, अंग्रेजों की दमन नीति में वृद्धि के फलस्वरूप जनता में प्रतिरोध की शक्ति का विकास,1885 में कांग्रेस की स्थापना आदि इस कालखण्ड की ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण भारत के बौद्धिक समुदाय में अपनी अस्मिता के प्रति जागरुकता का संचार हुआ। संचार व्यवस्था, रेल सम्पर्क, छापाखाने आदि भी इसी दौर में विकसित हुए। इससे साहित्य तथा ज्ञान- विज्ञान के क्षेत्र में नई चेतना का संचार हुआ। इन घटनाओं से बंगाल का समाज सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रभावित हुआ जिसे हम बंगला नवजागरण के रूप में जानते हैं।
भारतेन्दु और उनके मण्डल के लेखक निरन्तर बंगाल के सम्पर्क में रहे। इन सबके परिणामस्वरूप हिन्दी भाषी क्षेत्रों के बुद्धिजीवी भी हिन्दी साहित्य की समृद्ध परम्परा के अनुसन्धान की ओर प्रवृत्त हुए। इस अनुसन्धान कार्य में विदेशियों ने भी पर्याप्त भूमिका निभाई। सर जार्ज ग्रियर्सन की ‘माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर आफ नार्दर्न हिन्दुस्तान’ तथा एफ.ई.के. की ‘ए हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचर’ जैसी कृतियां इसी काल खण्ड में आईं। बाद में ‘कविवचन सुधा’ (1868), ‘हिन्दी प्रदीप’ (1877), ‘ब्राह्मण’ (1883) आदि पत्रिकाओं में विभिन्न नवीन विषयों पर अनुस्धानपरक लेख प्रकाशित होने लगे। स्वयं भारतेन्दु ने कालिदास, जयदेव, सूरदास तथा पुष्पदंताचार्य की चरितावली लिखी। पुरातत्व और भारत के साँस्कृतिक इतिहास पर अनुसन्धानपरक निबन्ध लिखे। ‘नाटक अथवा दृश्यकाव्य’ शीर्षक उनका महत्वपूर्ण सिद्धान्तनिरूपक निबन्ध उनकी अनुसन्धान-दृष्टि का सूचक है।
बाद में ‘कविवचन सुधा’ (1868), ‘हिन्दी प्रदीप’ (1877), ‘ब्राह्मण’ (1883) आदि पत्रिकाओं में विभिन्न नवीन विषयों पर अनुस्धानपरक लेख प्रकाशित होने लगे। स्वयं भारतेन्दु ने कालिदास, जयदेव, सूरदास तथा पुष्पदंताचार्य की चरितावली लिखी। पुरातत्व और भारत के साँस्कृतिक इतिहास पर अनुसन्धानपरक निबन्ध लिखे। ‘नाटक अथवा दृश्यकाव्य’ शीर्षक उनका महत्वपूर्ण सिद्धान्तनिरूपक निबन्ध उनकी अनुसन्धान-दृष्टि का सूचक है।
अनुसन्धानपरक आलोचना का व्यवस्थित रूप द्विवेदी युग में सामने आया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत ‘नैषधचरित चर्चा’ में अनुसन्धानपरक समीक्षा का उन्नत स्वरूप ढलता हुआ दिखायी देता है। ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ (1897 ई.) में बाबू राधाकृष्णदास का ‘नागरीदास का जीवन चरित्र’, बाबू श्यामसुन्दर दास का ‘बीसलदेव रासों’, किशोरीलाल गोस्वामी का ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ और ‘पद्मपुराण’, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ‘विक्रमोर्वशी की मूल कथा’ आदि अनेक गंभीर एवं गवेषणापूर्ण आलोचनात्मक निबन्ध सन् 1899 ई. और 1900 ई. के बीच प्रकाशित हुए।
1913 ई. में भारत के विभिन्न स्थानों में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ और देश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, आगरा, नागपुर आदि में विश्वविद्यालय खुलने लगे। यद्यपि सन् 1857 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय खुल चुका था और 1918 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारम्भ हो गयी थीं, किन्तु शोध का कार्य कुछ वर्ष बाद ही आरम्भ हो सका। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 1921 ई. में बाबू श्यामसुन्दर दास की नियुक्ति हिन्दी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गयी और यहां भी एम.ए. के पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिया गया। इसके बाद शोधपरक समीक्षा का समुचित विकास होना संभव हुआ।
यद्यपि सन् 1857 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय खुल चुका था और 1918 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारम्भ हो गयी थीं, किन्तु शोध का कार्य कुछ वर्ष बाद ही आरम्भ हो सका। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 1921 ई. में बाबू श्यामसुन्दर दास की नियुक्ति हिन्दी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गयी और यहां भी एम.ए. के पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिया गया। इसके बाद शोधपरक समीक्षा का समुचित विकास होना संभव हुआ।
प्रतिष्ठानिक आधार पर भारत में हुए अनुसन्धान-कार्य की परम्परा के विकास में 1931 ई. महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष प्रयाग विश्वविद्यालय से बाबूराम सक्सेना को उनके ‘अवधी का विकास’ अनुसन्धान कार्य पर डी.लिट्. की उपाधि मिली। 1934 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल को ‘दि निर्गुण स्कूल आफ हिन्दी पोयट्री’ पर डी.लिट्. की उपाधि मिली। भारत में हिन्दी भाषा पर भाषावैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य से भाषानुसंधान परम्परा का आरम्भ हुआ और कुछ वर्ष के भीतर ही साहित्य के विभिन्न पक्षों पर अनुसन्धान कार्य सामने आने लगे और इस तरह अनुसन्धान के विषयों मे तेजी से विस्तार होने लगा।
इसी अवधि में स्वैच्छिक साहित्यिक संस्थाओं की प्रकाशन योजना में, उनकी सहायता से वैयक्तिक स्तर पर हो रहे अनुसन्धान कार्य भी सामने आने लगे।
अनुसन्धानपरक आलोचना में अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण और उपलब्ध तथ्यों का नवीन आख्यान होता है। इसलिए यह कार्य कोई भी व्यक्ति किसी संस्था से जुड़कर आसानी से कर सकता है। किसी संस्था से जुड़े बिना अनुसन्धान कार्य करना कठिन होता है। इसीलिए विश्वविद्यालयों के खुलने के बाद अनुसंधापरक आलोचना के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ यद्यपि गुणवत्ता में उतनी तेजी से गिरावट भी आई.
आज का हमारा समय सांस्थानिक अनुसन्धान के चरम पतन का दौर है। इस दौर की शुरुआत आठवें दशक से हुई जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के शिक्षकों की अर्हता को पी-एच.डी. की उपाधि से जोड़ दिया। पी-एच.डी. की उपाधि को नौकरियों से जोड़कर व्यवस्था ने जो भूल की उसके दुष्परिणाम कुछ दिनो बाद ही दिखायी देने लगे। आज शोधार्थी को येन केन प्रकारेण पी-एच.डी. की उपाधि चाहिए क्योंकि बिना उसके नौकरी मिलनी कठिन है और शोध निर्देशक को भी अपने प्रमोशन में अधिक से अधिक शोध-प्रबंधों के निर्देशन का अनुभव चाहिए। इस तरह शार्टकट के इस युग में शोधार्थी और शोध-निर्देशक दोनों ने ही श्रम से पल्ला झाड़ लिया है। दोनों में जैसे गुप्त समझौता हो। कौन सिर खपाने जाय, उद्देश्य तो डिग्री हासिल करना है और उसके लिए श्रम की जरूरत कम, व्यवहार- कुशलता की जरूरत अधिक होती है।
वैश्वीकरण के बाद अनुसन्धान के क्षेत्र में और भी तेजी से गिरावट आई है। अब तो हमारे देश की पहली श्रेणी की प्रतिभाएं मोटी रकम कमाने के चक्कर में मैनेजर, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहती हैं और जल्दी से जल्दी विदेश उड़ जाना चाहती हैं। किसी ट्रेडिशनल विषय में पोस्टग्रेजुएट करके शोध करना उन्हें नहीं भाता। जो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाते वे ही अब मजबूरी में शोध का क्षेत्र चुन रहे हैं। वैश्वीकरण और बाजारवाद ने नयी प्रतिभाओं का चरित्र ही बदल दिया है। अब “सादा जीवन उच्च विचार” का आदर्श बेवकूफी का सूचक है। ऐसे कठिन समय में त्यागपूर्ण जीवन का आदर्श चुनना आसान नहीं है। उत्कृष्ट शोध में यह आदर्श अनिवार्य है।
यद्यपि देश भर के विश्वविद्यालयों और शोध-निर्देशकों में इस विषय़ को लेकर भयंकर असंतोष है, पर कहीं से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। देश भर की शिक्षण संस्थाओं और शोध-केन्द्रों में साहित्य की विभिन्न विधाओं पर प्राय: सेमीनार-संगोष्ठियाँ आयोजित होती रहती हैं, किन्तु शोध जैसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण विषय की समस्याओं पर केन्द्रित किसी संगोष्ठी के आयोजन की सूचना सुनने को बहुत कम मिलती है। 
हिन्दी जगत की दशा तो यह है कि शोध के नाम पर जमा किए जाने वाले ज्यादातर प्रबन्ध या तो दस बीस पुस्तकों से उतारे गए उद्धरणों के असंबद्ध समूह होते हैं या निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऊंचे पदों पर आसीन आचार्यों या साहित्यकारों के गुणगान। गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरने वाले प्रबन्ध यदा-कदा ही देखने को मिलते हैं। आखिर क्या कारण है कि शोध के लिए आधुनिक साहित्य ही आजकल शोधार्थियों और निर्देशको को अधिक आकर्षित कर रहा है? और उसमें भी जीवित और रचनाकर्म में रत रचनाकारों पर धड़ल्ले से शोध कार्य सम्पन्न हो रहे हैं। जबकि राजस्थान के जैन मन्दिरों अथवा राजस्थान के प्राच्य विद्या संस्थान की शाखाओं, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता आदि में हस्तलिखित ग्रंथों का अम्बार लगा हुआ है जो अनुसंधुत्सुओं की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुभाषा भाषी इस विशाल देश की विभिन्न भाषा- भाषी जनता के बीच सांस्कृतिक व भावात्मक संबंध जोड़ने के लिए तुलनात्मक साहित्य में शोध की असीम संभावनाएं व अपेक्षाएं हैं। लोक साहित्य, भाषा विज्ञान, साहित्येतिहास आदि के क्षेत्र में शोध की महती आवश्यकता है। किन्तु आज तीन चौथाई से अधिक शोध- छात्र आधुनिक काल और उसमें भी कथा -साहित्य पर ही शोध रत हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह साहित्य की विभिन्न विधाओं में खुलकर बहस होती है और वैचारिक संघर्ष इन विधाओं को जीवंत बनाए रखते हैं, उस तरह अनुसन्धान के काम पर बहस नहीं होती। विश्वविद्यालय जहां शोध होते हैं अब नवोन्मेष के केन्द्र न रहकर व्यक्तिगत झगड़ों के अड्डे बन गए हैं।
शोध के गिरते स्तर का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आज अधिकाँश प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में बहुतेरे शोध छात्र ऐसे लेखकों पर शोधरत हैं जिनके लेखन में अभी असीम संभावनाएं हैं। किसी भी बड़े लेखक की विचारधारा में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। वह जड़ नहीं होता और अध्ययन- चिन्तन- मनन के क्रम में उसकी अवधारणाओं के बदलते रहने की प्रचुर संभावनाएं होती है। इसलिए शोध जैसा गंभीर कार्य उसी साहित्यकार पर होना चाहिए जिसका लेखन या तो पूरा हो चुका हो या पूरा होने के कगार पर हो। तात्पर्य यह कि उसमें अब किसी परिवर्तन की या नया जुड़ने की संभावना न हो क्योंकि किसी साहित्यकार पर शोध करने का अर्थ है उसके ऊपर एक थीसिस या सिद्दांत दे देना और उसपर शोध उपाधि प्राप्त कर लेना। ऐसी दशा में यदि किसी शोधार्थी ने किसी जीवित और सृजनरत रचनाकार पर शोध कार्य पूरा करके उसपर एक थीसिस दे दिया और बाद में वह लेखक अपनी किसी नयी कृति में एक नई और पहले से भिन्न विचारधारा प्रस्तुत कर दी तो पहले का किया हुआ शोध- कार्य का क्या होगा ? क्योंकि अब तो उस व्यक्ति की विचारधारा पहले वाली नहीं रही। 
इतना ही नहीं, आज हिन्दी में शोध- कार्य की दशा यह है कि बिना जे.आऱ.एफ. ( जूनियर रिसर्च फेलोशिप) किए शोध में पंजीकरण बहुत कठिन है। शोध के स्तर को बनाये रखने के लिये यूजीसी समय- समय पर नियमों में तरह- तरह के संशोधन करता रहता है। उन्ही में से एक यह भी है कि अब एक आचार्य स्तर का शोध- निर्देशक भी एक साथ आठ से अधिक शोधार्थियों को शोध नहीं करा सकता। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों को शोध के लिए खाली हुई रिक्तियों के लिय़े परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं।। इन सबका प्रभाव यह हुआ है कि शोध के लिए जगहें बहुत कम हो गयी हैं और जे.आर.एफ. पाने वालों के भी पंजीकरण अब मुश्किल से हो रहें हैं। अब हिन्दी में फल -फूल रहे इस गोरख-धंधे पर विचार कीजिए कि एक जे.आर.एफ. पाने वाला शोधार्थी पाँच वर्ष तक के लिए पंजीकृत होता है और इस अवधि में उसे लगभग 18-20 लाख रूपए शोध- वृत्ति के रूप में मिलते है और उसका शोध -निर्देशक उससे अपने किसी प्रिय या आदरणीय लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध के नाम पर अभिनंदन ग्रंथ लिखवाता है और पी-एच.डी. की डिग्री भी दिलवाता है, ताकि उससे भी वह अपने बारे में प्रशस्ति या पुरस्कार आदि का जुगाड़ कर सके। शोध में तटस्थता अनिवार्य है। क्या किसी जीवित और समर्थ रचनाकार पर शोध करने वाला व्यक्ति उसकी कमियों को रेखांकित करने का साहस कर सकेगा? शोध- वृत्ति के रूप में जो 18-20 लाख रूपए शोधार्थी को मिलते हैं वह जनता की गाढ़े की कमाई का ही हिस्सा है जो सरकार के खजाने में जाता है और जिसे शोध-वृत्ति के रूप में सरकारें प्रदान करती हैं। मेरे संज्ञान में ऐसे दर्जनों पंजीकृत शोधार्थी हैं जो इस तरह से सरकार से धन लेकर अपने शोध- निर्देशकों के मित्रों- शुभचिन्तकों का जीवनवृत्त रच रहे हैं।
आज की दशा यह है कि औसत दर्जे के लेखक अपना जीवन वृत्त लिखते हुए यह उल्लेख करना नहीं भूलते कि उनकी रचनाओं पर किन -किन विश्वविद्यालयों में शोध हो चुके हैं या हो रहे हैं। अब यह भी उनकी योग्यता का एक पैमाना मान लिया गया है। क्या शोध के पतन की यह चरम परिणति नहीं है?
.