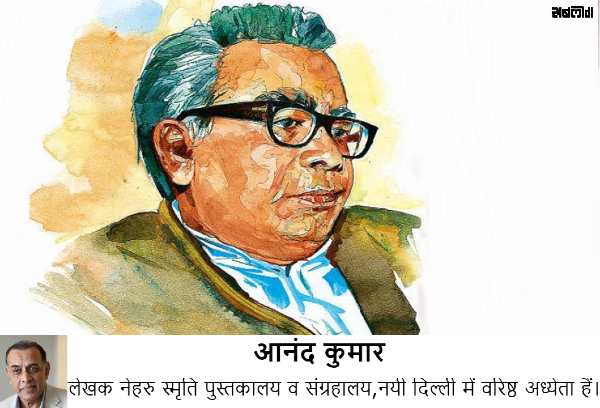सामाजिक न्याय की राजनीति और दलित आन्दोलन
दुनिया के तमाम हिस्सों में जन-आंदोलनों को पढ़ने, लिखने और समझने का मापदंड और नजरिया भी अलग-अलग रहा है| कहीं वर्ग- संघर्ष, कहीं जाति-संघर्ष तो कहीं लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के रूप में इसे देखने और समझने का प्रयास किया जाता रहा है| जहाँ तक भारत में जन-आंदोलनों की बात है तो यहाँ पर हर विषय पर आधारित विभिन्न तरह के जन-आंदोलन को देखा और समझा जा सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय समाज दुनिया के अन्य समाजों से एकदम अलग, जाति और वर्ण पर आधारित समाज है जहाँ वर्ग-संघर्ष के साथ-साथ जाति और वर्ण संघर्ष पर आधारित जन-आंदोलनों का लम्बा इतिहास रहा है| दुनिया के तमाम हिस्सों की तरह एक वर्ग जो इस जाति और वर्ण पर आधारित अलोकतांत्रिक, शोषणयुक्त, सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखना चाहता है तो दूसरी तरफ इस शोषणयुक्त व्यवस्था का शिकार शोषित वर्ग/जातियां इसे ख़त्म कर एक लोकतान्त्रिक मूल्यों द्वारा संचालित स्वंतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का सृजन करना चाहती हैं| जहाँ तक भारत में दलित आंदोलन का सवाल है उसकी कई धाराएँ विद्य्मान हैं, लेकिन दो धाराएं मुख्य रूप से दलित जन-आंदोलन के रूप में अपने आपको स्थापित करने में कामयाब रही है| पहला- डॉ. भीम राव अम्बेडकर द्वारा स्थापित दलित आंदोलन जो मुख्य रूप से सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन है और वह शोषणयुक्त, अलोकतांत्रिक, सामंतवादी विचारधारा पर आधारित ब्राह्मणवादी सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाकर लोकतान्त्रिक मूल्यों द्वारा संचालित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है| इस दलित आंदोलन का प्रभाव मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है|
दूसरा- कांशी राम और बहुजन समाज पार्टी द्वारा स्थापित दलित आंदोलन जो मुख्य रूप से राजनितिक एवं सामाजिक आंदोलन रहा, हालाँकि यह भी अपने को अम्बेडकरवादी दलित आंदोलनकारी होने का दावा करते हैं| इसका प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में है| यदि सांस्कृतिक मुद्दे को छोड़ दिया जाय तो इन सारे दलित जन-आंदोलनों के मुद्दे समान ही रहे हैं और इनका मुख्य उद्देश्य शासन और प्रशासन में दलितों का प्रतिनिधित्व और सहभगिता, समाज में अवसर की समानता, बराबरी का व्यवहार, और लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित समातमूलक समाज की स्थापना के लिए, तथा जातिवाद, वर्णव्यवस्था, और ब्राह्मणवाद (मनुवाद) और असमानता के खिलाफ जनता को एकजुट करना है| भारत में दलित आंदोलन दलित समुदाय के लिए न सिर्फ राजनितिक और सामाजिक पहचान एवं चेतना को मुख्य समाज में स्वीकारोक्ति प्रदान करने में सहायक साबित हुआ है, बल्कि उनमें मनोवैज्ञानिक रूप से बराबरी का एहसास कराने में कामयाब रहा है| इसके अलावा दलित आंदोलन ने दलित समुदाय को गुणात्मक रूप से अपने जीवन को आत्म-सम्मान एवं गौरव के साथ जीने और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है| पिछले साढ़े-चार वर्षों में जबसे ये भाजपा की सरकार केंद्र में सत्ताशीन हुई है भारत में दलित आंदोलन को तो जैसे संजीविनी मिल गयी हो क्योंकि इस सरकार के पहले दलित समुदाय की जो लड़ाइयाँ सामाजिक स्तर पर थीं अब वे सभी लड़ाइयाँ राजनितिक एवं प्रसाशनिक स्तर पर भी मुखर हैं| चाहे वो रोहित वेमुला की आत्महत्या, ऊना के दलितों पर अत्याचार हो या भीमा-कोरेगॉव की ऐतिहासिक गौरवगाथा में उमड़े लाखों की संख्या में दलितों का प्रदर्शन हो ये सब इस बात के ही द्योतक हैं कि अब पहले की तरह दलितों को दबाना आसान नहीं है| देश के कई जानेमाने राजनितिक विश्लेषकों का यह अनुमान था की इस भाजपा सरकार के आने से यदि सबसे ज्यादा किसी आंदोलन को फायदा होगा तो वह दलित आंदोलन है|
इनका अनुमान तब शतप्रतिशत सही हुआ जब यह सरकार तमाम दलित विरोधी, सामाजिक-न्याय विरोधी निर्णय लेने के साथ-साथ बर्षों से चले आ रहे “दलित एवं आदिवासी अत्याचार निरोधक कानून 1989 ” में फेर-बदल कर उसे दंतहीन बनाने की कोशिश करके पूरे देश के दलितों को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका दे दिया| फलस्वरूप 2 अप्रैल 2018 को दलित आंदोलन ने सामाजिक-न्याय के प्रति समर्थन एवं सहानुभूति रखनेवाले आंदोलनों के सहयोग से पूरे भारत का चक्का जाम कर सरकार को न सिर्फ अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया बल्कि एक मजबूत सन्देश दिया की भविष्य में देश का यह एक चौथाई शोषित, बंचित और उपेक्षित समाज अब और अत्याचार बर्दास्त नहीं करेगा| सन्देश यह भी था कि दलित समुदाय अब अपनी लड़ाई सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर से ऊपर राजनितिक स्तर पर भी लड़ने को तैयार है| जिस राजनीतिक चेतना, सामाजिक सोच और सांस्कृतिक स्वतंत्रता और विकल्प की खोज में दलित आंदोलन का काफी लम्बा समय व्यतीत हुआ है, अब ये कहना अतिश्योक्ति नहीं लग रहा कि वर्तमान में यदि कोई डॉ. भीम राव आंबेडकर या मान्यवर कांशी राम जी जैसा बहुमुखी प्रतिभा का धनी, ऊर्जावान जन-नायक मिल जाय और एक बेहतर सोशल-इंजीनियरिंग द्वारा दलित और अन्य पिछड़े समाजों को एक साथ लामबंद करने में कामयाब हो जाय तो देश में दलित आंदोलन को न सिर्फ समतामूलक समाज की स्थापना जैसे सपने को साकार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, बल्कि देश में और भी तमाम सामाजिक-न्याय में विश्वास रखने वाले आंदोलनों को भी एक नया बल मिलेगा| शिक्षा ने दलितों में आत्म-सम्मान, गौरव और स्वाभिमान जगाया और (दलित) आंदोलन ने उन्हें स्वतंत्र व्यक्तित्व का इंसान बनकर सम्मान से जिंदगी जीने की ताकत दी| हालाँकि यह तस्वीर पूरे देश के दलितों की नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि चाहे वह देश के किसी भी कोने में क्यों नहीं हो अब दलित भी स्वाभिमान और स्वतंत्रता के महत्त्व को समझने लगे हैं, हाँ यह बात जरूर है कि देश में घोर-आर्थिक विषमता के सबसे ज्यादा शिकार दलित ही हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होने के कारण वो मजबूरी बस आवाज़ उठाने में असक्षम महसूस करते हैं| इतिहास के हर एक काल में दलित समुदाय हमेशा निचले पायदान पे रहा है, इसके अलावा यह दलित आंदोलन का ही योगदान है कि दलित समुदाय देश में आजादी के बाद भी लोकतंत्र के नाम पर लम्बे समय से हो रहे उनके तमाम अधिकारों की लूट को समझने लगा है| यह समझने लगा है कि किसी भी देश में सचमुच का लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जबतक कि व्यस्था को चलाने वाले सभी संस्थाएं लोकतान्त्रिक ना हो जाएँ| जबतक देश के तमाम संस्थाओं में हर वर्ग का सामान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होगा तबतक न सबको न्याय मिलेगा और ना ही एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है| अतः इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने वाली तमाम संस्थाओं में भी सभी वर्गों को सामान रूप से प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर उसे लोकतान्त्रिक बनाने की पहल अब देश में दलित आंदोलन के लिए मुख्य राजनितिक मुद्दा बनकर भारतीय राजनीती में आयी है जिसे वर्तमान राजनीति में न सिर्फ काफी महत्वपूर्ण समझा गया है, बल्कि देश की भविष्य कि राजनीति के लिए बड़ा राजनितिक परिवर्तन की सुगबुगाहट के रूप में भी देखा जाने लगा है|
निःसंदेह बीजेपी की सरकार ने देश में दलित आंदोलन को एक संजीवनी दे दी है, और इसने दलित आंदोलन और दलित राजनीति के लिए एक नया अवसर भी खोला है, इसके बावजूद देश के अम्बेडकरवादी और गैर-अम्बेडकरवादी दोनों प्रकार की दलित राजनीति पर निर्भर करता है कि इसे वह कितनी दूर लेकर जाते हैं| इसके साथ ही संसदीय राजनीति में दलित आंदोलनों को कई बिंदुओं पर सोचने की जरुरत है| राष्ट्रीय स्तर पर एक कारगर दलित संगठन की जरूरत को महसूसते हुए तमाम दलित संगठनो को एक छतरी के अंदर लाकर देश के तमाम हिस्सों में दलित आंदोलनों द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक न्याय की लड़ाई को संगठित कर समतामूलक समाज के निर्माण को साकार करने में दलित आन्दोलन एक देशव्यापी भूमिका निभा सके इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्भाषित भी करनी पड़े, या राजनीतिक रणनीति के अनुसार हिसाबी भी होना पड़े तो कोई बात नहीं| दलित आन्दोलन के प्रभाव में इतना तो हुआ कि वर्तमान भारतीय राजनीति में तमाम मुख्य राजनितिक पार्टियों को दलित मुद्दे पर सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है| भविष्य की भारतीय राजनीति इससे ही तय होने वाली है कि देश और देश की सामाजिक व्यवस्था का शिकार सदियों से शोषित, बंचित और उपेक्षित इन समुदायों के हितों की कैसे और कितनी रक्षा हो पाती है, साथ ही साथ ये दलित आंदोलन और उसके कार्यकर्त्ता सामाजिक न्याय के समर्थकों के साथ मिलकर अपने आंदोलन और राजनीति को कैसे पुनर्गठित करते हैं|